अली सरदार जाफरी के कबीर भी कबीर न रहकर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर के माफिक ‘अक्खड़-फक्कड़’, सिर से पांव तक मस्तमौला और ‘बन पड़ी तो सीधे-सीधे और नहीं दरेरा देकर कहने’ वाले ‘भाषा के डिक्टेटर’ कबीर से मेल खाने लगते हैं। इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी और अली सरदार जाफ़री के कबीर एक हो जाते हैं!
मो. उमर.
सुलझाकर कहने वाले कबीर के व्यक्तित्व और विचारों को आज तक हिंदी साहित्य की मुख्यधारा की आलोचना ने सुसंगत ढंग से रखने के बजाय गप्पों, किंवदंतियों यों में उलझाकर रखा है। मुख्यधारा वाली आलोचना का जी तुलसी में ही अधिक रमा है। तथाकथित प्रगतिशील और मार्क्सवादी आलोचना की स्थिति भी कमोबेश यही रही है। जबकि कबीर के चिंतन और उनकी सुस्पष्ट वाणी को उसी ढंग से रखना उसकी जिम्मेदारी थी, जिस ढंग से इस चिंतक ने अपने समय में रखी थी। लेकिन इसके विपरीत मार्क्सवादी दिग्गज तुलसी के काव्य में सामंत विरोधी मूल्य और उस स्वर को खोजने लगे, जो वहां लुप्त था। वह स्वर था कबीर के पास। एक ओर थे प्रतिरोध के स्वर कबीर और दूसरी ओर समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय की चेष्टा ऐसी विराट हुई कि कबीर तुलसी हो गए और तुलसी कबीर। प्रतिरोध के स्वर वाले कबीर कहीं हाशिए पर चले गए और वैष्णव कबीर सामने आ गए। कभी सूफ़ियों जैसे लगने लगे इस कबीर के पास कुछ मौलिक नहीं था। सब तत्कालीन समाज के दूसरे पंथों से उधार लिये गए विचार थे। आलम यह है कि कबीर प्रगतिशील होते नहीं कि जल्दी ही उन्हें आध्यात्म और पाखंड के सागर में डुबो दिया जाता है। सभी सवर्ण और तथाकथित प्रगतिशील चिंतकों की ही तरह कबीर का कुछ यही हाल किया है प्रगतिशील कवि और चिंतक माने जाने वाले अली सरदार जाफ़री ने। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अन्य दूसरे आलोचकों के कबीर संबंधी विचारों की जमकर आलोचना हुई और गंभीर विमर्श पैदा हुआ। इस बीच डॉ. धर्मवीर की आलोचना ने यह जरूर किया कि कबीर संबंधी अब तक हुए चिंतन को प्रश्नांकित कर दिया। उन्होंने कबीर पर गंभीर और ठोस पुनर्लेखन की मांग की। इस क्रम में दर्जनों पुस्तक लिखकर डॉ. धर्मवीर ने कबीर संबंधी तब तक की मान्यताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। दलित आलोचना ने पाश्चात्य चिंतन को फ़लक पर नए सिरे से उभारा और परिणाम यह हुआ कि एफ.ई. केइ के कारण ‘कबीर और कबीरपंथ’ प्रकाश में आए। फ़िलहाल अली सरदार जाफरी की कृति ‘कबीर बानी’ पर विचार करते हैं। इस पुस्तक पर तार्किक और आलोचनात्मक ढंग से उस तरह विचार कम ही हुआ है, जिस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी रामविलास शर्मा व नामवर सिंह सहित अन्य प्रगतिशील माने जानेवालों के कबीर संबंधी विचारों पर हुआ है। इसलिए सरदार जाफ़री के कबीर संबंधी विचारों को जानना और उसका गहन वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण आवश्यक है।
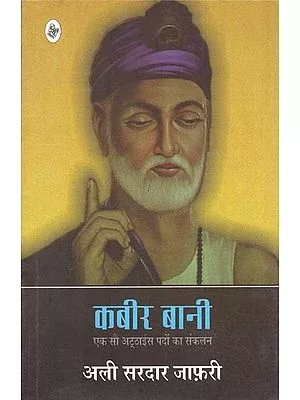
सन् 1965 में प्रकाशित ‘कबीर बानी’ कबीर के 128 पदों का संकलन है। इन पदों का संकलन किया है अली सरदार जाफ़री ने और भूमिका भी उन्होंने ही लिखी है। इसके अलावा, जहां-जहां जिन पदों के लिये अली सरदार जाफ़री ने आवश्यक समझा है, उन्होंने उनमें अपनी ओर से टिप्पणियां भी जोड़ी हैं। इसकी भूमिका लिखते हुए उन्होंने शुरुआत में कबीर के व्यक्तित्त्व पर टिप्पणी की है–
“यह बात शायद पुराने इतिहासकारों को नहीं मालूम थी कि इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संबंधों के परिवर्तन की कहानी भी है और विचार और चेतना की प्रगति की भी। इस वातावरण में आते-जाते पात्र परछाइयों की तरह घूमते रहते हैं और अगर परछाइयों का नाम लोग भूल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार और चेतना की प्रगति जारी रहती है। यही कारण है कि परिस्थितियों और घटनाओं का कबीर, सन् और तारीख का कबीर जिंदा नहीं है, लेकिन विचार और चेतना का कबीर, भावनाओं और अनुभूतियों का कबीर, कविता और गीत का कबीर जिंदा है। हर दोहा उसका अस्तित्व है, हर पद उसका व्यक्तित्व, हर विचार उसकी ज़बान। और जब हम उसके बोले हुए शब्दों को दोहराते हैं तो कबीर का साज़ बजने लगता है। शाही फ़रमान और डंकों की आवाज़ें गूंगी हो जाती हैं और कबीर के दिल से निकलने वाले अनाहत नाद से आत्मा मस्त हो जाती है। पंडित का मंत्र और मुल्ला की अज़ान आसमानों के सन्नाटे में गुम हो जाती हैं और कबीर की प्रेम-वाणी धरती के सीने में धड़कती रहती है।”[1]
सचमुच कबीर का व्यक्तित्त्व और कबीर की कविताएं आज भी धरती के सीने में धड़क रही हैं। कबीर के विचार जितने प्रासंगिक अपने समय (पंद्रहवीं-सोलहवीं सदी) में थे, आज भी ऐसा लगता है कि वे उतने पुराने नहीं पड़ गए हैं, बल्कि कई बार वे आज भी प्रेम और बंधुता का संदेश देते हैं। कबीर की वाणियों में जो स्पष्टता है, जो ओज है और जिस ढंग की मुखरता है, शायद ही मध्यकाल में किसी और कवि के पास हो। कबीर की वाणियों का स्वर दो टूक है। बेहद सीधा और सरल है। यही सरलता और बेलौसपन कविताओं को विशिष्ट बना देती है। यही कारण है कि कबीर की कविताएं पाखंडों से टकराती हैं और रूढ़ियों को मुंह चिढ़ाती हैं तथा सत्ताधारी वर्ग को चुनौती देती हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक सामाजिक ढांचे के आधार में विषमता रहेगी, तब तक कबीर अपनी कविताओं और उनमें व्यक्त विचारों के माध्यम से समाज में मशाल की तरह पथ प्रदर्शित करते रहेंगे।
संकलनकर्ता अली सरदार जाफरी ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि कबीर के जन्म का सन, तवारीख़, जन्मस्थान और मां-बाप तथा जाति-धर्म और रहन-सहन से अधिक महत्वपूर्ण उनके विचार हैं। तुच्छ विषयों पर लड़ने वाले निर्रथक और हास्यास्पद मालूम होते हैं– “इस पर लड़ने-मरने वाले कि कबीर लुंगी पहनते थे या धोती बांधते थे, यह भूल जाते हैं कि वास्तविकता वस्त्रों में नहीं, नग्नता में है। जिसने अर्थ के शरीर से शब्दों के परदे हटा दिए हों और राम और रहीम को एक कर दिखाया हो, उसे सूत और कपास के वस्त्र पहनाने की कोशिश और उस वस्त्र भिन्नता पर मतभेद और घृणा फैलाना कितना हास्यास्पद मालूम होता है।”[2]
स्वयं कबीर के लिए इन बातों का बहुत अधिक महत्व नहीं है। कबीर न ही इस्लाम से संबद्ध हैं और न ही तत्कालीन वैष्णव या शैवादि संप्रदायों से। कबीर का मार्ग इन सभी से भिन्न है। कबीर रूढ़िवादी धार्मिक चिंतनों और मान्यताओं को सिरे से नकार देते हैं। कबीर के लिए न काशी महत्वपूर्ण है और न काबा। कबीर के लिये मनुष्य महत्वपूर्ण है। ह्रदय का महत्त्व है। कबीर किसी मंदिर-मस्जिद की कल्पना नहीं करते। कंकड़-पत्थर की इमारतें उनके लिए व्यर्थ हैं। वे तो कहते हैं कि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो पहाड़ को पूजा जा सकता है। कबीर के यहां सब निरर्थक है। कबीर का पथ अन्य सभी पथों से भिन्न है। जो कुछ है, इसी घट (शरीर) में है, और इसी घट में इसका निर्माता है। इसी घट में सातों समंदर हैं। अनहद नाद इसी घट में गूंज रही है। पद देखिए–
“इस घट अंतर बाग-बगीचे, इसी में सिरजनहारा।
इस घट अंतर सात समुंदर, इसी में नौ लख तारा।
इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखनहारा।
इस घट अंतर अनहद गरजै, इसी में उठत फुहारा।
कहत कबीर सुनो भई साधो, इसी में सांई हमारा।।”[3]
एक जगह और कबीर कहते हैं–
“चंदा झलकै यहि घट माहीं। अंधी आंखन सूझे नाहीं।।
यहि घट चंदा यहि घट सूर। यहि घट गाजै अनहद तूर।।
यहि घट बाजै तबल-निसान। बहिरा शब्द सुनै नहि कान।।
जब लग मेरी मेरी करै। तब लग काज एकौ नहिं सरै।।
जब मेरी ममता मर जाय। तब लग प्रभु काज संवारै आय।।
ज्ञान के कारन करम कमाय। होय ज्ञान तब करम नसाय।।
फल कारन फूलै बनराय। फल लागे पर फूल सुखाय।।
मृगा पास कस्तूरी बास। आप न खोजै खोजै घास।।”[4]
अर्थात “इसी घट (शरीर) में चांद झलकता है, लेकिन अंधी आंखों को दिखाई नहीं देता। इसी घट में चांद है और इसी घट में सूरज। इसी घट में अनहद तूर (अनाहत ध्वनि) सुनाई देता है। इसी घट में ढोल और डंके बज रहे हैं, लेकिन बहरे कानों को कुछ सुनाई नहीं देता। जब तक आदमी मेरी-मेरी करता रहता है, तब तक कोई काम नहीं बनता। जब यह अहंकार मिट जाता है तब भगवान स्वयं आकर हर काम को संवार देते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के आते ही कर्म बेकार हो जाता है। जैसे फूल, फल पैदा करने के लिए खिलता है, लेकिन फल लगने के बाद फूल मुरझा जाता है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन वह उसे अपने शरीर के बजाय घास में खोजता फिरता है।”
कबीर को अली सरदार जाफ़री ने भी अनपढ़ माना है। वे कहते हैं– “यह बात सर्वसम्मति से मानी जाती है और ख़ुद कबीर ने इसे स्वीकार किया कि वे अनपढ़ थे।”[5] अर्थात लेखक ने इस बात को उसी तरह स्वीकार कर लिया, जिस तरह सभी यह दुहराते चलते हैं कि कबीर अनपढ़ थे। यह इतनी बार कबीर के लेखकों ने दुहराया है कि यह बात आम हो गई है कि कबीर अनपढ़ थे। हालांकि स्वयं अली सरदार जाफ़री ने कबीर के पदों की व्याख्या करते हुए उसे वेदांत और इस्लाम के सूफीवाद से लेकर जिन तमाम दार्शनिक ऊंचाइयों की सैर कराई है, उससे कभी नहीं लग सकता कि यह किसी अनपढ़ की कविताएं होंगी।
लेखक ने कबीर को शेख़ तक़ी से भी संबद्ध माना है और दूसरी ओर रामानंद से भी जोड़ा है। कबीर के ज्ञान पर आश्चर्य करते हुए उन्होंने यह माना है कि यह शेख़ तक़ी और रामानंद के सत्संगों में शामिल होने का फल है–
“रामानंद ने कबीर को अपने मंडल में ले लिया। कुछ लोगों का मत है कि कबीर उनकी सोहबत में एक अरसे तक रहे, लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि यह सोहबत बहुत कम दिन रही और इसका सबूत इससे भी मिलता है कि कबीर के विचारों पर रामानंद का प्रभाव धीरे-धीरे धुंधला होता चला जाता है। रामानंद से मिलने से पहले और बाद भी कबीर के इधर-उधर भटकते रहने की बात हमें यह अनुमान लगाने पर विवश कर देती है कि अनपढ़ होने के बावजूद, जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उन्हें ज्ञानियों का सत्संग मिला था। झूंसी के शेख तक़ी की सोहबत का जिक्र कबीर ने खुद किया है, चाहे वह उनके शागिर्द बने हों या उनके साथ सिर्फ़ उठते-बैठते रहे हों।”[6]
कबीर को ज्ञानियों का सत्संग मिला था या कबीर अनपढ़ थे? कबीर को अनपढ़ मान लेने पर यही विकल्प बचता है कि उनका गुरु किसी को बताया जाय या ऐसे ज्ञानीजनों के सत्संगों में बिठाया जाय। यह क्षण भर रुककर सोचने वाली बात है कि यदि कबीर का ज्ञान और उनके पदों में मौजूद उनके विचार कबीर के अपने मौलिक नहीं हैं और वह आध्यात्मिक सत्संगों के परिणाम हैं तो कबीर की कविताओं की क्या महत्ता रह जाती है, सिवाय इसके कि कबीर ने सभी पंथों और दार्शनिक चिंतनों से पल्लवग्राही ढंग से ज्ञान बटोरकर उसे फेंटकर संतुलन साधते हुए प्रस्तुत कर दिया, जहां सूफी परंपरा के लोगों को तसव्वुफ़ और इश्क़ हक़ीक़ी जैसी अवधारणाएं मिल जाएंगीं और दूसरी ओर वेदांतियों को अद्वैतवाद मिल जाएगा? यही बात तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ‘हिंदी साहित्य के इतिहास’ में कबीर के विषय में कही है–
“… इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद (भक्तिमार्ग) का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी बानी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं।”[7]
आचार्य शुक्ल ने अपने मत को बेहद दृढ़तापूर्वक रखा और उत्तरोत्तर के आलोचकों और लेखकों ने भिन्न-भिन्न ढंग से वही बात दुहराई है। यह एक खास किस्म का कबीर के आलोचकों और लेखकों का संतुलनवाद है लेकिन कबीर ऐसे किसी संतुलन की चिंता नहीं कर रहे थे। अली सरदार जाफरी लिखते हैं–
“कभी-कभी इस दर्शन के दीवाने ‘अलमस्त फ़क़ीर’ का गीत इस्लामी चिंतनधारा की लहरों में बदल जाता है। ‘या करीम, बलि हिकमत तेरी, ख़ाक़ एक सूरत बहुतेरी’। अर्थात् ऐ करीम (दयानिधि), मैं तेरी हिकमत पर कुरबान जाऊं, एक खाक़ से इतनी सारी सूरतें बना डालीं। और कभी वह इस्लामी आस्थाओं की भूमि से उठकर वेदांत के शून्य आकाश में चले जाते हैं, जहां निर्गुण और सगुण से भी चेतना ऊंची हो जाती है। फिर कभी-कभी वह इस्लामी शब्द इस्तेमाल करते हैं और हिंदू-पद्धति अपना लेते हैं। जैसे– “नबी आंखों में मौजूद है, काले और सफ़ेद तिलों के बीच में एक तारा है, जिसमें लाखों सूरज उदय होते हैं। मगर इस हज़ार-रंग अंदाज़ के अंदर अभीष्ट एक ही है, जो एक शब्द ‘प्रेम’ में समा जाता है, बाक़ी बातें उसकी व्याख्या हैं।”[8]
अली सरदार जाफ़री की यह व्याख्याएं निस्संदेह महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थापनाएं भ्रामक हुआ करती हैं। होता यह है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व कहीं पीछे छूट जाता है और कबीर के क्रांतिकारी विचार वेदांत, इस्लाम और सूफीवाद जैसे दार्शनिक दायरों के बीच कलाबाजियां खाने लगते हैं और उनका स्वर मद्धम पड़ता हुआ एक अजीबोगरीब समन्वय में बदल जाता है। ‘आंखिन देखी’ कबीर ‘कागद की लेखी’ वाले कबीर में बदल जाते हैं और प्रतीत होने लगता है कि ‘ढाई आखर प्रेम’ का संदेश देने वाले पुजारी के विचारों को भारी-भरकम पोथियों से गुज़रकर समझा जा सकता है। यह स्वयं कबीर के शब्दों में सुलझाने के बजाय उलझा देना है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाय तो जिस वेदांत के सागर में कबीर डुबकी लगा रहे हैं, वह वेदांत मत कबीर के समय तक इतना लोकप्रिय भी नहीं था। इरफान हबीब लिखते हैं–
“मेरे मत से शांकर वेदांत सत्रहवीं सदी से पूर्व सर्वत्र रूप से व्याप्त नहीं था। अपने इस सुझाव द्वारा मैं यह संकेत देना चाहता हूं कि शांकर वेदांत पंद्रहवीं तथा सोलहवीं सदियों के लोकवादी एकेश्वरवाद का न तो स्रोत था और न ही उस पर उसके प्रभाव की कोई संभावना दिखाई पड़ती है।”[9]
आम जनमानस का कवि अचानक आम जनमानस के हाथों से यूं ही छिटक जाता है। लोक-एकेश्वरवादी संत परंपरा हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण धारा बन जाती है, जो इसके ठीक विपरीत खड़ी सगुण धारा से मिलकर एक बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिसमें निर्गुण धारा की सारी क्रांतिकारिता सगुण के समन्वयवाद के साथ मिल जाती है, जहां कबीर तुलसी हो जाते हैं और तुलसी कबीर। निर्गुण-सगुण का भेद महज दार्शनिक लगने लगता है और ऐसा लगता है मानों सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को तिलांजलि दे दी गई हो। इस तरह संत कवियों के क्रांतिकारी विचार निस्तेज हो जाते हैं और कबीर ‘कबीर बानी’ के संकलनकर्ता अली सरदार जाफरी की दृष्टि में एक मुसलमान सूफ़ी बन जाते हैं जो हिंदू भक्ति की भाषा में बात करते हैं। वे लिखते हैं– “कबीरदास एक मुसलमान सूफ़ी थे जो हिंदू भक्ति की भाषा में बात कर रहे थे। चूंकि उन्होंने अपने-आप को बार-बार जुलाहा कहा है इसलिए यह यक़ीन के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने इस्लाम का परित्याग नहीं किया था, लेकिन उनकी धज हिंदुओं की-सी थी। माथे पर तिलक लगाते थे, और शरीर पर जनेऊ पहनते थे और साहस तो इतना था कि ब्राह्मणों पर व्यंग करते थे– ‘तू बाम्हन मैं कासी का जुलहा, बूझौ मोर गियाना।’”[10]
ऐसा लगने लगता है कि कबीर ‘सर्वधर्म समभाव’ के प्रतीक बन गए हैं। अली सरदार जाफरी के कबीर भी कबीर न रहकर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर के माफिक ‘अक्खड़-फक्कड़’, सिर से पांव तक मस्तमौला और ‘बन पड़ी तो सीधे-सीधे और नहीं दरेरा देकर कहने’ वाले ‘भाषा के डिक्टेटर’ कबीर से मेल खाने लगते हैं।[11] इसके बाद स्वाभाविक है कि इस तरह के रूप-रंग वाले व्यक्ति को ‘अक्खड़ फक्कड़’ और ‘अलमस्त फ़क़ीर’ ही कहा जाएगा। इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी और अली सरदार जाफ़री के कबीर एक हो जाते हैं!
कबीर के जन्म और रामानंद को अपना गुरु बनाने संबंधी मिथकीय कहानियों को कबीर के इस लेखक ने भी अन्य पूर्ववर्ती लेखकों की तरह ही दोहराया है। लेखक चाहता तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इन कथाओं का खंडन कर सकता था। संतुलन कायम रखने के लिए कबीर का यहां रामानंद से भी संबंध है और शेख़ तक़ी से भी। अली सरदार जाफरी ने भी रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण संबंधी मिथकीय घटना को शुक्ल जी की तरह ही प्रस्तुत किया है–
“पंद्रहवीं शताब्दी के बनारस में रामानंद की बड़ी ख्याति थी। वैसे तो वह हिंदू संत थे, लेकिन उनकी गोष्ठी में हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक होते थे। कबीर का लड़कपन था लेकिन उन्होंने भी रामानंद को ही अपना गुरू चुना। अब मुश्किल यह थी कि एक मुसलमान जुलाहे को वह अपना शिष्य बनाएंगे या नहीं। कबीर ने इसका हल जिस तरह खोजा वह बहुत दिलचस्प है। रामानंद रोज़ सुबह-सवेरे गंगा में स्नान करने जाते थे। एक रोज़ सुबह के वक़्त जब अंधेरा ही था, कबीर गंगा के किनारे सीढ़ियों पर लेट गए। थोड़ी देर में जब स्वामी रामानंद आए तो उनका पैर कबीर के सिर पर पड़ गया और अनायास उनके मुंह से ‘राम-राम’ निकल गया। कबीर खुश हो गए कि मंत्र मिल गया और उस दिन से अपने-आप को रामानंद का चेला कहने लगे।”[12]
यदि मान भी लिया जाय कि रामानंद कबीर के गुरू थे तो भी यह घटना बेसिर-पैर की लगती है। सोचने की बात है कि रामानंद के कबीर के शरीर पर पैर पड़ने और उसके बाद रामानंद के मुंह से निकले ‘राम-राम’ को कबीर ने कैसे गुरु मंत्र मान लिया? यदि मान लिया तो फिर कबीर-कबीर न रहकर कुछ और ही हो जाते हैं, तार्किक और बुद्धिवादी कबीर नहीं रह जाते। यह घटना सहज बुद्धि से ही असंगत लगती है। कबीर के जन्म और गुरू प्राप्ति के संबंध में फैली इन भ्रामक कथाओं का खंडन करते हुए प्रो. कुंवर पाल सिंह, रामचन्द्र शुक्ल को भी निशाने पर लेते हैं–
“यह सब कबीर के क्रांतिकारी स्वरूप को धूमिल करने का प्रयास है। न कबीर प्रगट हुए और न रामानंद के शिष्य थे, वे वैष्णव परंपरा के साथ कभी नहीं रहे। जिस अवतारवाद की वे जीवन-भर निंदा करते रहे, उसके वह समर्थक नहीं हो सकते। उनके नासमझ शिष्य कहते हैं कि कबीर पैदा नहीं हुए, बल्कि प्रकट हुए। उन्हें चमत्कारी कबीर चाहिए, सुधारक कबीर नहीं। आचार्य शुक्ल जैसे इतिहासकार भी भ्रम फैलाते हैं– ‘रामानंदजी के माहात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस (पंचभंगा) घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से रामानंदजी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय रामानंदजी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंदजी बोल उठे– ‘राम-राम कह’। कबीर ने इसी को गुरुमंत्र मान लिया और वे अपने को रामानन्द का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे।’ यह कबीर के विचारों और दर्शन से मेल नहीं खाता और न इतिहास-सम्मत है। संत काव्य की मूल भावना को समझे बिना लोगों ने ये सब चीजें आरोपित की हैं। किसी व्यक्ति के विद्रोही चरित्र को धूमिल करना है, तो उसे मठ और मंदिर में स्थापित कर दीजिए, अवतारवाद से जोड़ दीजिए, चमत्कारों की कहानियों से उसे आभामंडित कर दीजिए, उसे पूजा की वस्तु बना दीजिए।”[13]
कहीं-कहीं अली सरदार जाफ़री कबीर के क्रांतिकारी व्यक्तित्त्व के कुछ पहलुओं को निश्चित ही रेखांकित करते हैं। जैसे कि लेखक का स्पष्ट मानना है कि कबीर गृहस्थ थे। कबीर का भगवान इसी संसार में मिलता है, मुक्ति का मार्ग यहीं से होकर जाता है। कबीर जीवन के संघर्ष से भागने वाले नहीं थे, बल्कि वे उनका सामना करने में विश्वास रखते थे। भूखे पेट भजन कबीर को नहीं जंचता था। यह संसार कबीर के लिये उस अर्थ में माया नहीं था, जिस तरह अन्य धार्मिक संतों और पीरों के लिए होता है। कबीर की माया की व्याख्या संसार को भ्रम मानकर भाग खड़े होने की सलाह नहीं देती। कबीर के यहां माया का आशय लालच से है। निश्चित ही कबीर न तो वैष्णव वैरागियों से प्रभावित हैं और न ही इस्लाम या सूफीवाद से। इस तरह वे उन तमाम दार्शनिक मतों और धाराओं से भिन्न हैं, जिनके चौखटे में कबीर को बिठाने की कोशिश की जाती है। जिस भी चौखटे में कबीर को बिठाया जाता है, वे वहां से उठकर चल देते हैं और मानों आज भी यही कह रहे हों–
“मेरा तेरा मनुआं कैसे इक होई रे।
मैं कहता हां आंखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी।
मैं कहता सुरझावनहारी, तू राख्यौ उरझाई रे।
मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे।”[14]
अर्थात, मेरा और तेरा दिल एक कैसे हो सकता है? मैं आंखों-देखी कहता हूं और तू किताबों में लिखी बात सुनाता है। मैं सुलझाने वाली बात कहता हूं और तू उलझाने वाली। मैं कहता हूं कि जागते रहना और तू सोता रहता है।
‘कबीर बानी’ में कबीर के पदों के संकलनकर्ता ने कबीर के अधिकतर सुंदर पदों का चयन किया है। कबीर के 128 पदों में कुछ को छोड़ दिया जाय, जो निश्चित ही कबीर के नहीं लगते, लेकिन ऐसे हैं जो कबीर के मूल विचारों की झलक दे जाते हैं। भूमिका की अधिकतर स्थापनाओं का खंडन स्वयं वे पद ही करते हैं, जिनकी बेहद सटीक व्याख्या स्वयं इन पदों के संकलनकर्ता ने की है। एक पद देखिए–
“मन ना रंगाये रंगाये जोगी कपड़ा।
आसन मारि मंदिर में बैठे
ब्रह्म-छांड़ि पूजन लागे पथरा।
कनवा फड़ाय जटवा बढ़ौले
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गैले बकरा।
जंगल जाय जोगी धुनिया रमौले
काम जराय जोगी होय गैले हिजरा।
मथवा मुंड़ाय जोगी कपड़ा रंगौले गीता बांच के होय गैले लबरा।
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांधल जैबे पकड़ा।।”[15]
जोगी के मन में प्रेम का रंग है नहीं, उसने सिर्फ कपड़े रंगवा लिये हैं, आसन मारकर मंदिर में बैठ गया है और ब्रह्म को छोड़कर पत्थर की पूजा कर रहा है। उसने अपने कान चीरकर कुंडल पहन लिये हैं, बाल लंबे कर लिये हैं और दाढ़ी बढ़ाकर बकरा बन गया है। जोगी जंगल में जाकर धूनी रमा रहा है और काम-वासना का दमन करके जोगी हिजड़ा हो गया है। सिर मुंडाकर जोगी ने कपड़े रंग लिये हैं और गीता पढ़के बड़ी-बड़ी बातें बना रहा है। सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं कि इस तरह तू हाथ-पांव बांधकर यमराज के दरवाजे पर डाल दिया जाएगा।”
‘मध्यकालीन लोकवादी एकेश्वरवाद तथा उसका मानवीय स्वरूप’ शीर्षक अपने निबंध में इतिहासकार इरफ़ान हबीब ने कबीर के वैष्णव वैरागियों से संबंधों के खंडन के साथ ही शैवनाथ योगियों और तांत्रिकों से संबंध के तत्त्वों को भी कम ही पाया है। वे लिखते हैं कि– “कबीर के यहां ब्राह्मणों के अस्वीकार के सिवा योगियों अथवा तांत्रिकों से संबंधित तत्व बहुत ही कम हैं। अपितु उन्होंने योगियों की बहुत सी बातों को बड़ी हिकारत और नफरत से अस्वीकार किया है।”[16] स्वयं कबीर की रचनाएं इस बात का प्रमाण हैं। इस्लाम से कबीर कितने दूर हैं, इसका प्रमाण उनका यह पद है–
“ना जानै साहब कैसा है।
मुल्ला होकर बांग जो दैवे,
क्या तेरा साहब बहरा है। कीड़ी के पग नेवर बाजे
सो भी साहब सुनता है।
माला फेरी तिलक लगाया,
लंबी जटा बढ़ाता है।
अंतर तेरे कुफर-कटारी,
यों नहिं साहब मिलता है।”[17]
एक पद और देखिए–
“तोर हीरा हिराइल बा किचड़े में।
कोई ढूंढ़े पूरब कोई पश्चिम
कोई ढूंढ़े पानी पथरे में।
दास कबीर ये हीरा को परखैं
बांध लिहलै जीयरा के अंचरे में।।”[18]
कबीर के विचारों को इन दार्शनिक कोटियों और मतवादों में उलझाने से अधिक आवश्यकता उनके समाजशास्त्रीय अध्ययन की है। जो भाव और विचार कबीर की कविताओं में हैं, उनका उनके वर्ग और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से कितना संबंध था, यह जानने की ज़रूरत आज अधिक है। कबीर की कविताओं में मौजूद रहस्यवाद आदि की रूढ़िवादी किस्म की व्याख्या कबीर को कुछ खास वैचारिक दायरों में कैद कर देती है। क्या विषमताओं से भरे समाज में तार्किकता को तरजीह देने वाला विचारक अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति चिंतित न होता रहा होगा? पारंपरिक धर्म और पाखंड को तिलांजलि देकर मनुष्य को केंद्र में रखने वाले कबीर के समाज में बहुसंख्यक आबादी कबीर के विचारों के विपरीत दिशा में थी। ऐसे समाज में सुलझाकर कहने वाले कबीर बेहद उलझ जाते रहे होंगे। उलझाकर कहने वाले ही उस समाज में सफल थे। उन्हीं का शासन था। सीधी और सरल भाषा में कहना कई बार इस समाज में कठिन हो जाता था। अक्सर उल्टा कहना सीधे कहने से ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि वह मारक होता है। व्यंग्योक्ति कबीर की कविताओं की विशेषता है। इन व्यंग्योक्तियों में गहरी विडंबना है। कबीर की ऐसी कविताएं अचूक प्रभाव छोड़ती रही होंगी।
कबीर की कल्पनाओं में जो भी ब्रह्म है वह निश्चित ही कबीर के समतावादी विचारों का ही प्रतिबिंब है। इस ब्रह्म को पा लेने पर मनुष्य ऊंच-नीच जैसे तमाम अमानवीय भावों से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म जाति-धर्म से परे है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है। वहां अमृत ही अमृत है और सुख ही सुख है। इस तरह की अवधारणाएं भी कबीर के यहां हैं। इन अवधारणाओं से कबीर के कल्पनाओं के संसार का चित्र कल्पित किया जा सकता है जो तत्कालीन समाज से भिन्न है। कबीर के यहां व्यवहार के धरातल पर ऐसी कोई स्थिति सम्भव नहीं थी। यह कबीर की कल्पना के उड़ान को दर्शाता है कि कबीर अपने समाज में होते हुए ऐसी कल्पनाएं कर सकते थे, जो सत्य से कोसों दूर तो लगती थीं, लेकिन कहीं न कहीं कबीर की प्रगतिशील चेतना को दर्शाती थीं, जो बेहद उन्नत थी। यथा–
“अवधू बेगम देस हमारा।
राजा-रंक-फकीर-बादसा सबसे कहीं पुकारा।
जो तुम चाहो परम पद को, बसिहो देस हमारा।।
जो तुम आये झीने होके, तजो मन की भारा।
धरन-अकास-गगन कछु नाहीं, नहीं चंद्र नहिं तारा।।
सत्त-धर्म की हैं महताबें, साहेब के दरबारा।
कहैं कबीर सुनो हो प्यारे, सत्त-धर्म है सारा।।”[19]
कबीर का तत्कालीन विषमताओं पर प्रहार देखते बनता है–
“पांड़े बूझि पियहु तुम पानी।
जिहि मिटिया के घरमहं बैठे, तामहं सिस्ट समानी।
छपन कोटि जादव जहं भींजे, मुनिजन सहस अठासी ॥
पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सरि भा मांटी।
तेहि मिटिया के भांड़े पांड़े, बूझि पियहु तुम पानी ॥
मच्छ-कच्छ घरियार बियाने, रुधिर-नीर जल भरिया।
नदिया नीर नरक बहि आवै, पसु-मानुस सब सरिया ॥
हाड़ झरि झरि गूद गरि गरि, दूध कहाँ तें आया।
सो लै पांड़े जेवन बैठे, मटियहिं छूति लगाया ॥
बेद कितेब छाँड़ि देउ पाँडे, ई सब मन के भरमा।
कहहिं कबीर सुनहु हो पाँडे, ई तुम्हरे हैं करमा ॥”[20]
कबीर के इस तरह की और भी सुंदर कविताओं और विचारों का संकलन ‘कबीर बानी’ में मिलता है, लेकिन भूमिका में प्रस्तुत विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा सकता। अली सरदार जाफ़री ने कबीर के विचारों को सूफियों और वैष्णव-वेदांतियों की धज ओढ़ा दी है, जिससे सहमत होना मुश्किल है। कुछ-कुछ जगहों पर वास्तविक कबीर के चित्र को उभारने की कोशिश जरूर की है। यथा–
“हमें आज भी कबीर के नेतृत्व की ज़रूरत है, उस रोशनी की ज़रूरत है जो इस संत सूफ़ी के दिल से पैदा हुई थी। आज दुनिया आज़ाद हो रही है। विज्ञान की असाधारण प्रगति ने मनुष्य का प्रभुत्व बढ़ा दिया है। उद्योगों ने उसके बाहुबल में वृद्धि कर दी है। मनुष्य सितारों पर कमंदें फेंक रहा है। फिर भी वह तुच्छ है, संकटग्रस्त है, दुखी है। वह रंगों में बंटा हुआ है, जातियों में विभाजित है। उसके बीच धर्मों की दीवारें खड़ी हुई हैं। सांप्रदायिक द्वेष है, वर्ग-संघर्ष की तलवारें खिंची हुई हैं। बादशाहों और शासकों का स्थान नौकरशाही ले रही है। दिलों के अंदर अंधेरे हैं। छोटे-छोटे स्वार्थ और दंभ हैं, जो मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना रहे हैं। जब वह शासन, शहंशाहियत और प्रभुत्व से मुक्त होता है तो खुद अपनी बदी का गुलाम बन जाता है। इसलिए उसको एक नए विश्वास, नई आस्था और नए प्रेम की आवश्यकता है, जो उतना ही पुराना है जितनी कबीर की आवाज़। और उसकी प्रतिध्वनि इस युग की नई आवाज़ बनकर सुनाई देती है।”[21]
लेकिन सनद रहे कि हम अली सरदार जाफ़री के इन सुंदर शब्दों के साथ ही उस कबीर की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहे हैं, जिसकी प्रतिमा उपरोक्त उद्धरित शब्दों के लेखक ने गढ़ी है, बल्कि हम उस कबीर की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं जो न ही हिंदू है, और न ही मुसलमान, बल्कि एक भिन्न मार्ग का प्रशस्तकर्ता है, जहां तर्क है, ज्ञान के दीपक हैं और जहां मनुष्य मात्र मनुष्य समझा जाता है न कि मालिक, गुलाम या अन्य वर्णगत श्रेणियों में विभक्त है। आज उस कबीर की आवश्यकता है, जो महज इसलिए भी प्रासंगिक हो सकता है कि सत्ता और कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष में जो तार्किकता, स्पष्टवादिता और साहस कबीर के भीतर तब था, उसकी आज भी उतनी ही आवश्यकता है।