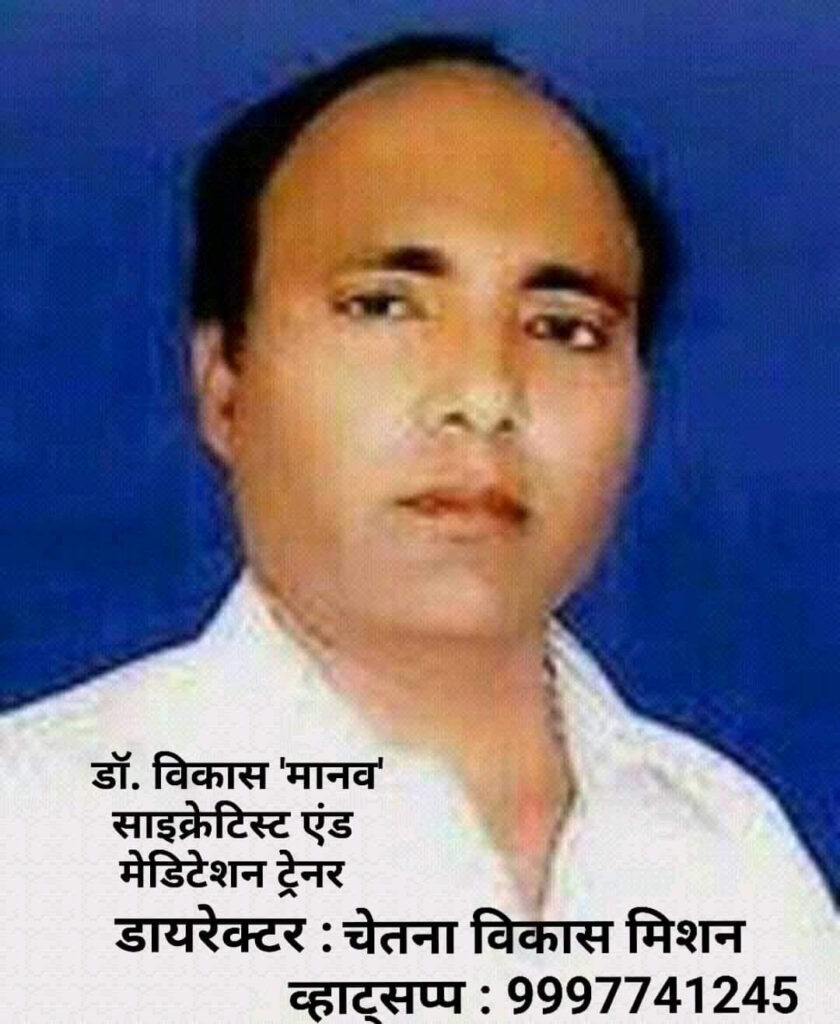डॉ. विकास मानव
सत्यार्थप्रकाश, में जीवात्मा के तीन शरीरों की चर्चा की है, परन्तु इनके लिए प्रमाण- ग्रन्थ नहीं बताए गए हैं। सांख्यदर्शन के द्वारा इनमें से दो शरीरों की पुष्टि हो जाती है, जबकि तृतीय ‘कारण’ शरीर को सम्भवतः महर्षि कपिल नहीं मानते।
सत्यार्थप्रकाश कारण शरीर के बारे में कहता है : जिसमें सुषुप्ति अर्थात् गाढ़निद्रा होती है । वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिए एक है (सत्यार्थप्रकाशः, नवम: समुल्लासः) – तब इससे यह एक जीवात्मा का अलग शरीर न होकर, कोई सामान्य कोष प्रतीत होता है।
इस प्रकार, वहां भी प्रत्येक जीवात्मा के दो शरीर ही मानना सही प्रतीत होता है, तथापि यह विषय, विशेषकर कारण शरीर का स्रोत-ग्रन्थ, अन्वेषणीय है।
दो शरीरों के विषय में कपिल ने विस्तृत जानकारी दी है, जो कि बहुत ही रुचिकर है।
शरीर का प्रसंग सांख्यदर्शन के तृतीय अध्याय के आरम्भ में आता है। इसको हम कपिल के सूत्रों के क्रम में ही देखते हैं।
प्रथम सूत्र इस प्रकार है :
अविशेषाद्विशेषारम्भः ॥३।१॥
कपिल बताते हैं कि अविशषों = तन्मात्रों/सूक्ष्मभूतों से विशेषों = पंच महाभूतों का सृजन होता है। यह तो वे प्रसिद्ध १।२६ सूत्र पर भी कह आए थे।
यहां उन्होंने ‘अविशेष’ व ‘विशेष’ नई संज्ञाएं दी हैं, यह दर्शाने के लिए कि जहां तन्मात्र न्यूट्रौन, प्रोटौन, इलैक्ट्रौन की तरह सब वस्तुओं में एक समान होते हैं, उनके पांच भेद छोड़कर, पंच महाभूत ही संसार के विभिन्न पदार्थों में विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, जैसे न्यूट्रौन, प्रोटौन, इलैक्ट्रौन से सभी दृष्ट पदार्थ उपलब्ध होते हैं। शारीर-प्रसंग में यह सूत्र भूमिका के रूप में भी है।
तस्माच्छरीरस्य ॥३।२॥ अनुवृत्तिः विशेषात्, आरम्भः
कपिल यहां स्पष्ट कर देते हैं कि पंच महाभूतों से यह दृष्ट शरीर उत्पन्न होता है। यहां वे केवल पांचभौतिक, या भौतिक, शरीर की ही चर्चा कर रहे हैं, यह आगे स्पष्ट हो जाएगा।
तद्बीजात् संसृतिः ॥३।३॥ अनुवृत्तिः शरीरम्
उस शरीर के ‘बीज’ = प्रजनन अणु से जीवजाति का विस्तार होता है। यह तो सभी जानते हैं कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, और वह उत्पत्ति किसी प्रकार के बीज, या प्रजनन अणु, से ही होती है।
किन्हीं जीवजातियों में पुरुष-मादा का जोड़ा आवश्यक होता है, कुछ में नहीं, परन्तु जीवित शरीर, चाहे वह स्थावर पेड़-पौधों का हो, या फिर जंगम जन्तुओं का हो, की आवश्यकता रहती ही है।
आविवेकाच्च प्रवर्तनमविशेषाणाम्॥३।४॥
अर्थात् अविशेषों का जीवात्मा के साथ सम्बन्ध विवेक होने तक बना रहता है।
यहां बहुत-सी बातें कपिल ने एक झटके में कह दी हैं. पहले तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ३।२ में जिस शरीर की बात हो रही थी, वह केवल भौतिक था, यहां चर्चा सूक्ष्म शरीर की हो रही है। फिर, यह बताया गया कि सूक्ष्म शरीर विवेकख्याति के हो जाने तक रहता है, अर्थात् मुक्तात्मा स्थूल या सूक्ष्म, दोनों ही प्रकार के शरीरों से रहित होता है।
इस कथन की अतिपत्ति के द्वारा हम जान सकते हैं कि, यदि यह शरीर जन्म से नहीं उत्पन्न होता है, तो वह सृष्टि के आरम्भ से ही आत्मा के साथ जुड़ जाता होगा। यह भी कि मोक्ष ही नहीं, प्रलय में भी इस शरीर का अन्त हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी कार्य पदार्थों का बना हुआ है, जो कि प्रलय में नहीं रहते।
जबकि यहां केवल अविशेषों की चर्चा की गई है, तथापि उन्हें सभी सूक्ष्मतर तत्त्वों का उपलक्षण समझना चाहिए, अर्थात् इन्द्रियां, प्राण, अहंकार, मन व बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर के भाग हैं।
यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥यजुर्वेदः ३४।३॥
अर्थात् वह मन जो प्रज्ञावान् है, चेतन है, स्मृतिवान् है, वह प्रजाओं (प्राणियों) के अन्दर अमृत ज्योतिरूप है।
यहां ‘मन’ से बुद्धि, मन, अहंकार, आदि, सूक्ष्म शरीर के अवयव अभिप्रेत हैं। उनको मन्त्र में अमृत = अमरणधर्मा बताया गया है।
उपभोगादितरस्य ॥३।५॥ अनुवृत्तिः शरीरस्य, आ प्रवर्तनम्
अर्थात् दूसरा शरीर (विशेषों का) तब तक चलता है जब तक उपभोग रहते हैं। जब तक आत्मा में भोग की इच्छा बनी रहती है, भौतिक शरीर भी बना रहता है।
इस तात्पर्य में यह दोष प्रतीत होता है कि, उपभोग के भी मोक्ष तक बने रहने से, भौतिक शरीर भी अमर है, ऐसा कहा जा रहा है परन्तु, इसका निराकरण ३।३ में हो ही गया है।
कहीं कुछ संशय न रह जाए, इसलिए कपिल उपर्युक्त का और स्पष्टीकरण देते हैं –
सम्प्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम् ॥३।६॥ अनुवृत्तिः विशेषाविशेषाभ्याम्
इस समय (जन्म धारण करते हुए), आत्मा दोनों विशेष व अविशेष से लिपटी है, अर्थात् प्राणावस्था में आत्मा के दो शरीर होते हैं – सूक्ष्म व स्थूल।
इन दोनों में भेद को पुनः बताते हैं–
मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥३।७॥ अनुवृत्तिः अविशेषाणां, शरीरम्
स्थूल शरीर प्रायः माता-पिता से उत्पन्न होता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर इस प्रकार नहीं उत्पन्न होता।
यहां कपिल ३।३ सूत्र का और विवरण देते हुए कहते हैं कि स्थूल शरीर अन्य स्थूल शरीरों से उत्पन्न होता है – कभी अपने-आप नहीं उत्पन्न हो सकता। इससे बहुतों के विचार कि जीव को मूल तत्त्वों से उत्पन्न करना सम्भव है, अथवा अन्य कई शरीरों के भागों को मिलाकर उत्पन्न किया जा सकता है, का निराकरण हो जाता है।
दूसरे, अधिकतर स्थूल शरीर मादा और पुरुष के अलग-अलग बीजों से उत्पन्न होता है। आज पाश्चात्य विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि इससे भावी पीढ़ियां अधिक पुष्ट उत्पन्न होती हैं। परन्तु बीज के अन्य भी प्रकार होते हैं – जैसे एक पेड़ स्वयं बीज उत्पन्न कर लेता है, अथवा, केले के पेड़ के समान, अपने एक भाग से दूसरा पेड़ उत्पन्न कर देता है।
जन्तुओं में भी इसी के समान कई प्रजनन-प्रकार पाए जाते हैं। तथापि, दो जीवों से उत्पन्न होने वाली सन्तान अधिक पाई जाती है और अधिक श्रेष्ठ होती है।
दूसरी ओर, सूक्ष्म शरीर पंच महाभूतों और माता-पिता से नहीं उत्पन्न होता।
कहीं यह संशय न रह जाए कि सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी ही क्यों जाए ? सम्भवतः, वह प्रलय में भी आत्मा के साथ रहती हो, और मोक्ष में भी।
पुनः स्पष्ट करते हुए कपिल कहते हैं –
पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य॥३।८॥
अनुवृत्तिः – शरीरस्य, आ विवेकात् प्रवर्तनम्, स्थूलस्य, अविशेषस्य
पूर्व उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म शरीर कार्य है; भोग के कारण एक शरीर का निर्धारण होता है, दूसरे का नहीं। अर्थात्, सूक्ष्म शरीर कार्य ही है, क्योंकि उसके तत्त्व भी उत्पन्न होते हैं। वह भौतिक शरीर से पहले ही सृजित हो जाता है। उसका निर्धारण भोग उपलब्ध कराने के लिए परिवर्तित नहीं होता, केवल भौतिक शरीर ही इस कारण से भिन्न-भिन्न सृजित होते हैं.
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः॥
योगदर्शनम् २।१३॥
अर्थात्, क्लेशों से युक्त कर्म करने पर, उनके फलरूप जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। यहां ‘जाति’ भौतिक शरीर को ही कह रहा है। परन्तु क्लेशयुक्त बुद्धि आदि हमारी एक भौतिक शरीर से दूसरे में प्रयाण करती रहती है।
सप्तदशैकं लिङ्गम्॥३।९॥
अर्थात् लिंग (शरीर) १७+१ = १८ तत्त्वों का बना है।
१।८९वें सूत्र में ‘महत्’ को ‘लिंग’ कहा गया था, परन्तु यहां इस पद का वह अर्थ नहीं है, अपितु प्रकरणानुसार अर्थ ‘सूक्ष्म शरीर’ है।
ये १८ तत्त्व हैं – पंच तन्मात्र, १० इन्द्रियां, अहंकार, मन व बुद्धि, अर्थात् पंच महाभूत व कारण प्रकृति को छोड़कर सभी प्राकृतिक विकार। स्वामी दयानन्द ने, ५ कर्मेन्द्रियों को न गिनाकर, ५ प्राणों की गणना की है। इससे कर्मेन्द्रियों और प्राणों के घनिष्ठ सम्बन्ध का हमें ज्ञान होता है।
कपिल ने भी प्राणों की चर्चा की है (सूत्र २।३१), जहां उन्होंने इनकी सामान्य करणवृत्ति बताई है। यह भी कर्मेन्द्रियों और प्राणों के सम्बन्ध की पुष्टि करता है।
यहां यह विचारने योग्य है कि कपिल ने १७+१ क्यों कहा, अष्टादश कह देते तो वही बात हो जाती ? सो, यहां ‘एकम्’ ‘लिङ्गम्’, अर्थात् महत् अथवा बुद्धि, का विशेषण है।
इस प्रकरण में, लिंग से अन्य १७ तत्त्वों का भी ग्रहण करना है, अर्थात् सूक्ष्म शरीर का ग्रहण करना है, यही द्योतित करना इसमें कारण है। परन्तु एक तत्त्व के अन्तर्गत अन्यों को मान लेना यह भी बताता है कि इन सबमें मुख्य तत्त्व बुद्धि ही है।
लिंग शरीर सभी आत्माओं के लिए समान क्यों न हों.
व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात् ॥३।१०॥ अनुवृत्तिः – लिङ्गे
अर्थात्, कर्मों के भेद के अनुसार, लिंग शरीर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भेद होता है।
यह सूत्र एक बहुत ही सूक्ष्म बात कह रहा है – जो हम सब के व्यक्तित्व में भेद पाते हैं, वे वस्तुतः सूक्ष्म शरीर के भेद को दर्शाता है।
इस भेद का स्वरूप क्या है ? कर्म जो अतीत में जीव कर आया, वे तो अब सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध हैं नहीं; जो उपलब्ध है, वह है कर्मजनित संस्कार। अवश्य ही विभिन्न मनुष्यों में हम पाते हैं कि उनकी महत्त्वाकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं, उनके द्वेष भिन्न-भिन्न होते हैं।
ये संस्कारों में भेद ही व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। अब, यह जानना आवश्यक है कि इन संस्कारों का निवासस्थान बुद्धि होती है। इसलिए यह समझना चाहिए कि बुद्धि के कारण ही सूक्ष्म शरीर में भेद आता है, अन्य सब अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियां सबकी एक समान ही होती हैं। इसीलिए पिछले सूत्र में लिंग को महत्त्व दिया गया है।
तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः॥३।११॥ अनुवृत्तिः – लिङ्गस्य
अर्थात्, लिंग शरीर का आश्रय होने से, ‘लिंग शरीर’ कहे जाने पर (स्थूल) देह का भी कथन हो जाता है।
यहां स्पष्ट होता है कि लिंग शरीर को स्थूल शरीर की आवश्यकता है। परन्तु, हमने तो ३।४ में देखा था कि लिंग शरीर ही एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है; यदि वह स्थूल पर आश्रित होता, तो यह यात्रा कैसे करता ? इस सूत्र के कथन से यह जानना चाहिए कि स्थूल देह सूक्ष्म शरीर का आश्रय तो है, परन्तु सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है।
तो फिर किसके लिए आवश्यकता है ? सो, कर्म करने के लिए व भोग भोगने के लिए स्थूल शरीर आवश्यक है। कर्म क्या होता है ? जब हम सांसारिक वस्तुओं के ऊपर कोई क्रिया करते हैं अथवा उनका चिन्तन ही करते हैं, तब वह कर्म कहाता है।
जैसा मैंने पूर्व भी अनेक बार बताया है, ज्ञान का ग्रहण व उसको उत्पन्न करने वाली क्रियाएं और ध्यानसे सम्बद्ध क्रियाएं ‘कर्म’ नहीं होतीं, क्योंकि उनसे कोई फल नहीं उत्पन्न होता। हां, जब हम उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जैसे चन्द्रमा को यान भेजते हैं, अथवा किसी अन्य को पढ़ाते हैं, तब वह कर्म बन जाता है।
इसीलिए परोपकार भी कर्म की श्रेणी में ही आता है, जिसका फल सुख होता है; उसे ‘निष्काम कर्म’ कहना, और यह मानना कि उससे कोई फल नहीं मिलता या मोक्ष प्राप्त होता है, यह भ्रम है।
इस प्रकार, स्थूल शरीर से संलग्न होने पर ही जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुछ कार्य कर सकता है। तो स्थूल शरीर क्या स्वतन्त्र है ?
न स्वातन्त्र्यात् तदृते छायावच्चित्रवच्च ॥३।१२॥ अनुवृत्तिः – लिङ्गस्य, देहः
अर्थात् स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बिना, स्वतन्त्रता रूप से नहीं रह सकता, छाया या चित्र के समान।
यह तो सामान्य ज्ञान है ही कि मृत्यु होने पर भौतिक शरीर चेतनारहित हो जाता है। इससे यह अनुमान लगता है कि जिस कारण से वह चेतन था, कार्यरत था, वह अब उसमें नहीं है, अर्थात् जीवात्मा उसमें नहीं है। क्योंकि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से लिपटी हुई होती है, जैसा कि हम ३।४ सूत्र में देख चुके हैं, इसलिए यह मानना युक्तियुक्त है कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही स्थूल शरीर प्रचालित था।
महर्षि कपिल इस सम्बन्ध को समझाने के लिए दो सुन्दर उपमाएं, अर्थात् उपमान प्रमाण, देते हैं। जैसे किसी वस्तु की छाया उस वस्तु से वास्तव में तो भिन्न होती है, परन्तु उस वस्तु से ही उसका अस्तित्व होता है, उसमें क्रिया होती है, ऐसा ही सम्बन्ध स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से होता है – सूक्ष्म शरीर से भिन्न होते हुए भी, स्थूल शरीर उससे स्वतन्त्र नहीं होता। इसी प्रकार जो कोई चित्र होता है, वह चित्रित वस्तु से भिन्न तो होता है, परन्तु उसका अस्तित्व, उसका आकार-प्रकार, उस वस्तु के कारण ही होता है।
मूर्तत्वेऽपि न सङ्घातयोगात् तरणिवत्॥३।१३॥ अनुवृत्तिः – लिङ्गं, छायावच्चित्रवच्च॥
अर्थात्, लिंग शरीर के मूर्त होने पर भी, वह संघात-रूपी स्थूल शरीर से जुड़ा नहीं होता, जिस प्रकार नाव अथवा सूर्य होते हैं (इसी कारण से उपर्युक्त उपमाएं भी सम्यक् हैं)।
अगले सूत्र में हम देखेंगे कि सूक्ष्म शरीर, अतिसूक्ष्म होते हुए भी, परिमाण वाला है। इसलिए हम सोच सकते हैं कि, कहीं न कहीं, सूक्ष्म व स्थूल शरीर का मिलन होता होगा, स्पर्श होता होगा। परन्तु कपिल बड़े यत्न से हमें समझाते हैं कि इन दोनों का सम्बन्ध बिना किसी स्पर्श वाला है।
यहां दी ‘तरणिवत्’ उपमा दो प्रकार से पढ़ी जा सकती है – ‘तरणी’ से नाव अथवा सूर्य का अर्थ लिया जा सकता है। नाव पानी पर चलती तो है, परन्तु पानी का कोई भाग ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश चक्षु ग्रहण करता है, परन्तु सूर्य का स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही पिछले सूत्र में दी छाया वस्तु से जुड़ी भी होती है, परन्तु अलग भी; चित्र वस्तु पर आधारित भी होता है परन्तु कहीं उसका स्पर्श नहीं करता। सूक्ष्मशरीर को इस प्रकार समझना बहुत आवश्यक है।
अणुपरिमाणं तत् कृतिश्रुतेः॥३।१४॥ अनुवृत्तिः – लिङ्गं, मूर्तत्वम्
अर्थात् लिंग शरीर कार्य है, ऐसा श्रुतिप्रमाण होने से, वह अणु (सूक्ष्म) परिमाण वाला है, यह जाना जाता है।
यदि सूक्ष्म न हो, तो एक कोशिका वाले जैसे अदृश्य जीवाणुओं में वह समा न पाए ! इसलिए, कपिल स्पष्ट करते हैं कि कार्य होने से इस तत्त्व का परिमाण तो है (जैसा कि कपिल ने “परिमाणात् ॥१।९५॥” सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया था), परन्तु उसे अतिसूक्ष्म ही जानो । इस तथ्य के लिए कपिल वेद का परम शब्द प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षादि के तो यह परे है।
तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ॥३।१५॥ अनुवृत्तिः – अविशेषाणां, शरीरः, मूर्तत्वम्
अर्थात् वेदों से हमें ज्ञात होता है कि अविशेषों का बना यह शरीर अन्नमय होता है।
यह तथ्य बहुत ही विचित्र प्रतीत होता है, क्योंकि जो पदार्थ अन्न से कहीं सूक्ष्मतर है, और स्वयं स्वतन्त्र सत्ता रखता है, उसपर अन्न का कैसे प्रभाव पड़ सकता है ? तथापि, हम व्यवहार में देखते हैं कि बादाम आदि से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, मदिरा आदि से वह ठीक से कार्य करना बन्द कर देती है, आदि, आदि।
सात्त्विक, राजसिक व तामसिक भोज्य पदार्थों में यही तो अन्तर है ! सो, इस विषय को ऐसे समझना चाहिए कि सूक्ष्म बुद्धि को कार्यान्वित स्थूल मस्तिष्क करता है। वह स्थूल मस्तिष्क इन पदार्थों से प्रभावित होकर सूक्ष्म बुद्धि को भी कार्य नहीं करने देता। इस प्रकार खाए हुए अन्न का प्रभाव बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर के कार्य पर पड़ता है।
इस लिंग शरीर के एक शरीर से दूसरे में जाने का प्रयोजन क्या है ?
पुरुषार्थं संसृतिर्लिङ्गानां सूपकारवद्राज्ञः॥३।१६॥
अर्थात् लिंग शरीरों का एक शरीर से दूसरे में जाना पुरुष, अर्थात् जीवात्मा, के लिए होता है, जिस प्रकार राजा के लिए उसका पाचक (उसके साथ-साथ जाता है)।
राजा जब भी कभी राजधानी से बाहर जाता है – निरीक्षण पर, शिकार पर या युद्ध आदि के लिए – तो उसके साथ उसका पाचक भी जाता है, जिससे राजा को भोजन की कोई चिन्ता न करनी पड़े।
कपिल इस उपमा द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर, विशेषकर बुद्धि जिसमें सारे संस्कार निहित होते हैं, जीवात्मा के प्रयोजन से, उसके साथ-साथ चलता है। अनेकों जन्मों में वह जो संस्कार इकट्ठा करता है, वे उसके साथ जुड़े रहते हैं, जिससे कि भोग पाने के समय वे उपस्थित हो सकें। ये संस्कार, अथवा वासनाएं, अनन्त हैं, इसका दिग्दर्शन कपिल ने इस सूत्र में कराया था –
न श्रवणमात्रात् तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्त्वात्॥२।३॥
अनादि काल से इकट्ठी की हुई वासनाओं के बलवान् होने के कारण मोक्ष की सिद्धि केवल (मोक्षपरक ज्ञान के) सुननेमात्र से नहीं होती।
कर्मों के करने में भी सूक्ष्म शरीर की प्रधान भूमिका है, चाहे अन्ततः कर्म मस्तिष्क, हाथ, आदि, स्थूल अवयवों से ही किए जाते हैं, क्योंकि उसमें निहित संस्कार ही हमें कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जन्मजन्मान्तर में संस्कारों के सातत्य को बनाए रखने के लिए ही लिंग शरीर, स्थूल शरीर के समान, नष्ट नहीं होता। स्थूल शरीर तो स्वयं भोग का एक अंश है.
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः
पतंजलि योगसूत्र ॥२।१३॥
अर्थात् क्लेशयुक्त कर्मों के आशय शेष रहते, उनके फल जाति (जन्मयोनि अर्थात् देहविशेष), आयु व भोग होते हैं।
यह समझने में कोई भी कठिनता नहीं है कि शरीर के अनुसार ही सुख-दुःख के भोग होते हैं, यथा मनुष्यशरीर में हम अनेक प्रकार के सुखों का भोग कर सकते हैं, जो कि पशुजातियों को उपलब्ध नहीं हैं।
योग का अभ्यास करते-करते जब हमारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तब लिंगशरीर के संस्कार भी नष्ट हो जाने से, उसका प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, और आत्मा प्रकृति से निवृत्त हो जाता है। यही बताना पूरे सांख्यदर्शन का मुख्य उद्देश्य है।
सांख्य के बताए इन दो शरीरों में, स्थूल शरीर को तो हम सभी भली प्रकार जानते हैं, सो वहां अधिक संशय नहीं होता, परन्तु सूक्ष्म शरीर बहुत रहस्यमयात्मक प्रतीत होता है। इसलिए इस विषय में वेदों और अन्य ग्रन्थों में प्राप्त कतिपय अन्य उल्लेखों को मैं नीचे निरूपित कर रही हूं.
अथर्ववेद कहता है –
अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम्।
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः.
अथर्ववेदः ९।१०।८॥
अर्थात् (तुरगातु) शीघ्रकारी ब्रह्म (ध्रुवम्) नित्य (जीवम्) आत्मा को (पस्त्यानां मध्ये) भौतिक शरीरों के बीच में (आ शये) भली प्रकार स्थापित करता है, और (अनत्) उसको प्राणों से युक्त करता है। (मृतस्य) मरे प्राणी का (अमर्त्यः जीवो) अमरणशील आत्मा (स्वधाभिः) अपने संस्कारों के साथ (मर्त्येन) मर्त्य सूक्ष्म शरीर के साथ (सयोनिः) समान योनि वाला होता हुआ (चरति) (एक शरीर से दूसरे शरीर को) गतिमान होता है।
वास्तव में, सूक्ष्म प्राकृतिक तत्त्वों से बने होने के कारण, है तो वह भी मर्त्य ही! सृष्टि के प्रारम्भ में वह उत्पन्न होकर जीवात्मा से जुड़ जाता है और मोक्ष अथवा प्रलय होने पर नष्ट होकर मूलप्रकृति में परिणमित हो जाता है।
‘सयोनि’ से यहां आत्मा व सूक्ष्म शरीर के साथ को बताया गया है – मरणोपरान्त जीवात्मा एकाकी नहीं विचरता, अपितु सूक्ष्म शरीर से लिपटा रहता है। यही बात सांख्यदर्शन में भी कही गई थी।
संस्कारयुक्त चित्त का जन्म-जन्मान्तर में आत्मा के साथ बने रहना जब हम समझ जाते हैं, तो शास्त्रों के अन्य वचन स्वतः समझ में आने लगते हैं।
यथा योगदर्शन कहता है –
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्॥योगदर्शनम् ४।९॥ अनुवृत्तिः – वासनानाम्॥
अर्थात् जाति (प्राणी की योनि), देश और काल से व्यवहित वासनाओं की भी निरन्तरता होती है, स्मृति और संस्कारों की एकरूपता के कारण।
इससे पतञ्जलि जनाते हैं कि जन्मजन्मान्तर में अर्जित वासनाएं संस्कार रूप में हमारे चित्त में बसती हैं, और वे संस्कार स्मृतिरूप ही होता है। संस्कार जैसा कोई भेद चित्त का नहीं बताया गया है। उसका कारण इस कथन से स्पष्ट हो जाता है – चित्त के स्मृति अंश में ही संस्कार स्थित होता है। परन्तु यह संस्काररूपी स्मृति का अन्य स्मृतियों से यह भेद होता है कि यह योनि, देश और काल से व्यवहित नहीं होती – जन्मजन्मान्तर में बनी रहती है।
अन्य स्मृतियां, जैसे हमने किन घरों में निवास किया, किस खिलौने से बचपन में खेले, आदि, चाहे हमें जीवनभर इस जन्म में याद रहें, परन्तु अगले जन्म में ये सब लुप्त हो जाती हैं। संस्कारों के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों में भेद होता है। इस सूत्र से यह निष्कर्ष निकला कि संस्कारों को संग्रहीत करने वाला चित्त भी जन्मजन्मान्तर में बिना नष्ट हुए बना रहता है, अर्थात् सूक्ष्म शरीर बना रहता है।
देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं तु देहिनः।
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥
मनुस्मृतिः १२।४०॥
अर्थात् सात्विक आत्माएं अगले जन्म अथवा मोक्ष में देव बनते हैं; सामान्य देही, जो प्रधानरूप से राजसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, मनुष्य बनते हैं; और तामसिक वृत्ति वाले लोग पशु योनियों में जन्म लेते हैं। यहां यह देखना आवश्यक है कि यहां योनि केवल कर्मफल के अनुरूप नहीं मिल रही है, अपितु जिस चित्तवृत्ति की हमने इस जन्म में वृद्धि की, उसके अनुसार भी जन्म मिलता है।
जैसे – सात्विक वृत्ति ज्ञानप्रेमियों की होती है। अब ज्ञानार्जन तो कर्म होता ही नहीं, तो उसका फल कैसा? सो, चित्त की जो प्रवृत्ति अधिक थी, अगले जन्म में उसी प्रवृत्ति के अनुरूप स्थान मिल जाता है। इससे चित्त में सुरक्षित सात्विक आदि संस्कारों की अमरता का हमें ज्ञान होता है, जिससे पुनः चित्त का अमृतत्व सिद्ध हो जाता है। या इसके विपरीत जानें तो, बिना चित्त के अमृतत्व के, उपर्युक्त त्रिविधा गति सम्भव ही नहीं है।
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः.
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्॥
कठोपनिषत् ५।७॥
अर्थात् देही = प्राणी अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां ज्ञान उपर्युक्त सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियों को ही कह रहा है – जो आत्माएं अधिक ज्ञानार्जन करती हैं, वे सात्विक योनियां, जो कर्म में दक्षता प्राप्त करती हैं, वे मनुष्य आदि योनियां, और जो , जड़ता, अकर्मण्यता और क्रूरता आदि निकृष्ट प्रवृत्तियों का आलम्बन लेती हैं, वे पशु-पक्षी व स्थावर (स्थाणु) योनियों को प्राप्त करती हैं।
जिस काम में भी हम इस जन्म में प्रयत्न द्वारा निपुण हो जाते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे सांसारिक कर्म हों, जैसे राजनीति, संगीत, नृत्य, और चाहे वह क्रूरता आदि तामसिक व्यवहार हो, यह ज्ञान, ये संस्कार, हमारी अगले जन्म में भी दृच्टिगोचर होते हैं। ब्रजभाषा में मुहावरा है – पूत के लच्छन पालने में दिख्खें – इसी बात को द्योतित कर रहा है कि नवजात शिशु में ही ये संस्कार प्रतीत होने लगते हैं।
यदि सूक्ष्म शरीर पिछले शरीर के साथ ही मर जाता, तो ये संस्कार कहां से पुनः उत्पन्न होते?
इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व व उसके अमरत्व का संकेत हमें अनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है, चाहे यह तथ्य हमें अर्थापत्ति से ही सिद्ध क्यों न करना पड़े! वेद भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं। वस्तुतः, यह ज्ञान वेदों से ही निष्पन्न हुआ है।
महर्षि कपिल आगे के तीन सूत्रों में स्थूल शरीर की रचना का विषय लेते हैं, परन्तु वह अंश इतना रुचिकर न होने से, हम अपनी लेखनी को यहीं पर विराम देते हैं।
सांख्यदर्शन के सूत्रों में हमें जो सूक्ष्म शरीर की रचना, उसका स्थूल शरीर से सम्बन्ध और उसके प्रयोजन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वह, मेरे सीमित ज्ञान में, किसी और ग्रन्थ में नहीं मिलता। मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान अत्यावश्यक है।