रामकिशोर मेहता
‘कविता का जनपक्ष’ प्रसिद्ध आलोचक शैलेन्द्र चौहान के द्वारा आलोचना के क्षेत्र में सन् 1990 से लेकर 2016 लिखे गए आलेख हैं। इन आलेखों को पढ़ कर मेरा दृष्टि विस्तार हुआ। कोई आलोचक जब किसी रचनात्मक लेखन का मूल्यांकन करता है तो उसके औजार क्या होते हैं, उसके आधार क्या हैं, पैमाना क्या है, और उसकी दृष्टि और दिशा क्या है; इसकी समझ बढ़ी । कोई रचनात्मक लेखक तो अपनी संवेदनशीलता, दृष्टि, दिशा, ज्ञान, विचारधारा और बहुत बार मन की गहराइयों में रचे बसे और अर्जित किए हुए संस्कारों के आधार पर अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलता चला जाता । बहुत बार तो उसे इस बात की चिन्ता भी नहीं होती कि कोई आलोचक उसकी रचना में बारे में क्या कहेगा ?
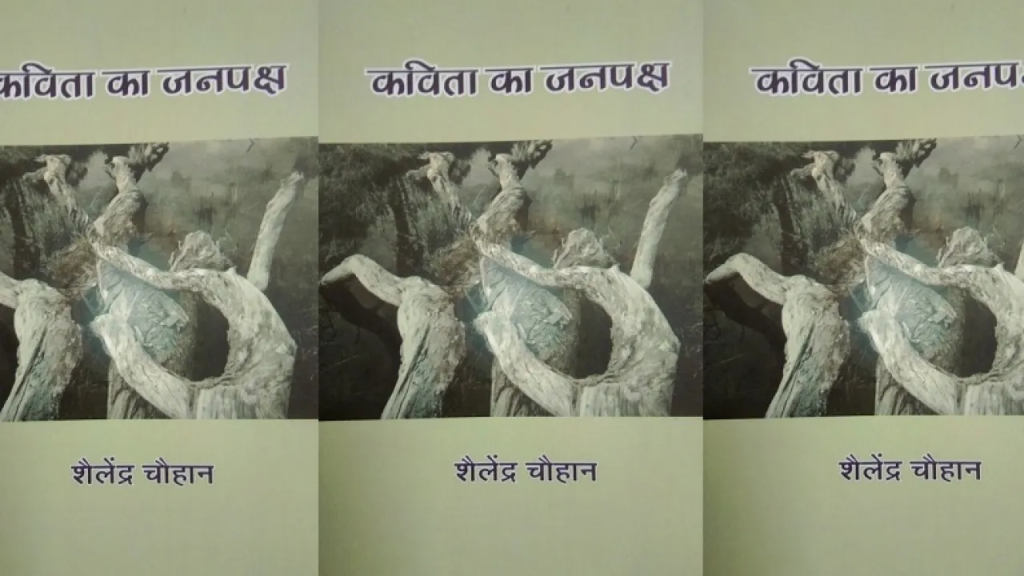
एक आलोचक कुछ सीमा तक परीक्षक है परन्तु उसके काम की सीमा अंक देना या काटना मात्र नहीं है और प्राप्तांकों के आधार पर वर्गीकरण करना भी नहीं है । वह एक इण्टरव्यूअर भी नहीं है जिसका काम सामने बैठे व्यक्ति के ज्ञान और समझ की सीमा को जान कर उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना हो। आलोचक का परीक्षण गणनात्मक (क्वान्टीटेटिव) नहीं गुणात्मक (क्वालिटेटिव) होता है ।
एक रचानात्मक लेखक के लिए आलोचक बहुत बार उसके और पाठक के बीच की बड़ी आवश्यक कड़ी होता है। वह लेखक के मन्तव्यों को खोलता है, पाठकों तक लेकर जाता है। वह लेखन की खूबियों को बहुविध समझाता है और खामियों को इंगित कर लेखक का पथ प्रशस्त करता है। वह ‘अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट’ की कला का मालिक है। एक अच्छा आलोचक रचनाकार का मित्र होता है । उसे ‘आंगन कुटी छवाय’ रखा जाना चाहिए। कई बार आलोचक रचना को वे अर्थ भी देता है जो रचनाकार को स्वयं भी मालूम नहीं होते ।
रचनात्मक लेखन एक कला तो है ही परन्तु उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य भी होता है । लेखक बहुत बार यह कह कर आलोचना से बचने का प्रयत्न करते हैं कि उनका लेखन ‘स्वांतः सुखाय’ है। हर लेखन ‘स्वांतः सुखाय’ तो होता ही है । प्रश्न हमेशा यह उठा करता हैं कि वह बहुजन हिताय भी या नहीं । यह बहुजन हिताय का प्रश्न आज की जटिल परिस्थितियों में बहुत बार रचना के कला पक्ष से टकराता प्रतीत होता है विशेष कर कविता में। कुछ आलोचक कला पक्ष को प्राथमिकता देते दिखाई पड़ते हैं और कुछ कविता के जन पक्ष को । इसी कारण कविता के आलोचकों में स्पष्ट विभाजन दिखाई पड़ता है । इस बात को लेखक ने अपने प्राक्कथन में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है । जो रचनाकार इन दोनों पक्षों को अच्छे से साधते दिखाई पड़ते हैं विशेष रूप से कविता में वे अच्छे कवि हैं । ऐसे कवि विरले ही होते हैं । लेखक ने जनपक्षधरता की ओर झुकाव लिए कवियों को अपनी इस पुस्तक में आलोचना के लिए चुना है । साथ ही आपने उन आलोचकों के विचार/ पक्ष को प्राथमिकता से रखा जो कविता में कला पक्ष की तुलना में जनपक्ष को प्राथमिकता देते रहे हैं ।
‘स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना : एक अवलोकन’ में ‘तार सप्तक’ और उसमें ‘अज्ञेय’ की भूमिका, और परिमल ग्रुप की स्थापना और आधुनिकता का बोध, प्रयोगशीलता, नई भाषा, नई संवेदना और अनुभूति की बात की । आलोचनाओं की तत्कालीन स्थापनाओं यथा शैलीगत, अस्तित्ववादी, समाजशास्त्रीय, रूपवादी व मिथकीय की बात करते हैं। उन आधारों की बात की जिन पर कृति की विवेचना उस काल में की जाती थी। ‘आद्य प्रगतिवादी आलोचक किसी कृति के मूल्यांकन के आधारों के बारे में कहते हैं “ आलोचक चाहे जिस दृष्टि से साहित्य का विवेचन करें ; इसमें लेखक को व्यक्तिगत रूप से जानना, समझना, उसके जीवनानुभवों को जान लेना, उसके दृष्टिकोण एवं विश्वबोध को समझना या सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों से जोड़ कर उसकी रचना के पात्रों को समझने की कोशिश, उनके मनोविज्ञान, व्यवहार और यथार्थ स्थितियों से उसका तदात्म्य आदि सभी साधन, माध्यम और उनका विश्लेषण अंततः मूल्यांकन करने का ही प्रयास तो है । दूसरी और ‘नई आलोचना’ नामक प्रवृत्ति के अनुसार साहित्य की कृतियों का मूल्यांकन ‘ एक अनावश्यक और साहित्येतर कार्य है ।‘ लेखक ने अन्यान्य प्रगतिवादी आलोचकों के विचार भी रखे हैं । इनमें प्रकाश चंद्र गुप्त का कहना है “मार्क्सवाद मनुष्य को जीवन, समाज और संस्कृति को समझने की नई दृष्टि प्रदान करता है। यह सतत् विकासमान विचारदर्शन और वैज्ञानिक दृष्टि है । डा. रामविलास शर्मा ‘भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रख कर मूल्यांकन करते हैं । किसी रचनाकार ने अपने समय के साथ कितना न्याय किया है उसे मूल्यांन की कसौटी मानते है । मार्क्सवादी आलोचकों में डॉ. शिवकुमार मिश्र और डॉ. रमेश कुन्तल ‘मेघ’, डॉ विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉ मैनेजर पाण्डेय और प्रो. नित्यान्द तिवारी का मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र किए गए उल्लेखनीय कामों की लेखक ने इस लेख में विशेष चर्चा की है ।
इस पुस्तक का अगला आलेख ‘सत्य का क्या रंग: पूछो एक संग’ मार्क्सवादी आलोचना के विकास में उठ रहे मत – मतांतरों और विमर्शों का आलेख है। पिछली सदी के ‘पाँचवें दशक का हिन्दी साहित्य और आलोचना’ प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादियों के बीच संघर्ष का युग था । इस संघर्ष में सरकार भी सुविधाजीवी लेखकों को अपने हित में ढालने का भी खेल भी खेल रही थी । बहुत सारे मार्क्सवादी लेखक भी पाला बदल रहे थे। यह वादों में विचलन का समय था । इस काल में मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में डॉ. राम विलास शर्मा की तूती बोलती दिखाई पड़ती है। “ डॉ रामविलास शर्मा ने अपने बैसवाड़ी लाल लंगोट को इस तरह आक्रामक मुद्रा में लहराना शुरु किया था कि बाकी सभी पहलवानों की मछलियाँ ढीली पड़ गईं थी ‘डॉ रामविलास शर्मा का कहना था कि ‘ये मूर्तिविधान वहीं सार्थक है जो भावों से अनुप्राणित हो जिसमें सहज इन्द्रियबोध का निखार हो । दूर की कौड़ी लाना काव्य रचना नहीं बौनों का बौद्धिक व्यायाम है।’
यह छायावाद और तार सप्तकों (और उनकी भूमिकाओं लिखे गए अज्ञेय के आलेखों) का समय था । यह उन साहित्यकारों के निर्माण का समय था जिन्हें हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में श्रद्धा से पढ़ते आएं है । इस काल में बड़े बड़े रचनात्मक साहित्यकारों को आलोचकों के वाण और उनकी अवहेलना/ उपेक्षा झेलनी पड़ी थी। अपनी सुरक्षा के लिए खुद आलोचना के क्षेत्र में उतरना पड़ता था। इनमें राहुल सांकृत्यायन, त्रिलोचन, शील, शैलेन्द्र आदि हैं । साहित्यिक उठा – पटक यह खेल सर्वकालिक है । यदि हम भी इसके शिकार हैं तो कोई खास बात नहीं है ।
अगला आलेख ‘जन जन के घर आंगन का सूरज भासमान’ इसी श्रृंखला का अगली कड़ी मालूम पड़ता है । यहाँ भी तार सप्तक है । अज्ञेय की भूमिका के माध्यम से उसकी राजनीति है । छायावाद है । साहित्यिक उठा पटक है । पूर्वपीठिका में देश, धर्म, समाज, अर्थ और युद्ध, की राजनीति है। किनारे किए गए साहित्यकारों का संघर्ष है विशेष कर शमशेर का । शमशेर का यह कथन मन को छूता है “इस दुनिया में दुर्भाग्य की सारी जड़ यही सरलता, खुलापन, सच्चाई और सच बोलने की वह प्रवृत्ति है जिसे धूर्त, चतुर, चालाक, अवसर परस्त, कैरिएरीस्ट और डोंगी व्यवहारिक जन कतई सहन नहीं कर पाते। वे सच बोलने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहते हैं।”
‘जनपक्षीय आलोचना का विचलन’ शीर्षक से लिखे गये आलेख में समय के साथ कविता के शीर्ष मार्क्सवादी आलोचकों के मत-मतान्तरों में आए विचलनों का लेखा जोखा है। जिनमें शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राम विलास शर्मा और नामवर सिंह प्रमुख हैं। इसे पढ़ कर लगता है कि किसी भी वैचारिक रूप से प्रगतिशील कवि की कविता को आलोचक चाहे तो आकाश में बिठा सकता है और चाहे गर्त में स्थापित कर सकता । यहाँ आलोचकों की भाषा में आए शब्दों के पारिभाषिक अर्थों को समझना अपने आप में दुरूह काम है । यह भाषा प्रकारान्तर से न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के समकक्ष कही जा सकती है जिसे केवल वकील और न्यायाधीश समझते हैं। ऐसा भी लगता कि कवि की स्थापना – विस्थापना की अपेक्षा आलोचक कवियों को भयाक्रांत कर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों के समानान्तर कई चतुर व्यवसायी रचनाकार भी आलोचकों का उपयोग कर ले जाते हैं । एक अच्छे रचनाकार को ऐसे भंवर से बच कर निकल जाना चाहिए।
मेरे विचार में आलोचक का काम रचनाकार और पाठक के बीच सेतु का होना चाहिए । उसे ऐसा व्याख्या कार होना चाहिए जो ‘अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट।’ शायद इसी की तलाश में हम रचनाकार आलोचक से समालोचक से समीक्षक ओर बढ़ चले हैं ।
पुस्तक में यहाँ आकर हमें आलोचना के मायाजाल से मुक्ति मिलती है। अगला आलेख ‘भाषा, लोक. और काव्य’ पर है। इसमें भाषा कि व्युत्पत्ति, विकास एवं लोक और सत्ता से उसके संबंध और ‘शोक से जन्में श्लोक’ से कविता के जन्म की बात है । जन की सहज अनुभूतियाँ सरल भाषा और जटिल अनुभूतियाँ प्रांजल भाषा में होने की बात कही है ।
आलोचना की कुछ समझ विकसित होने का सुख अगले कुछ अध्यायों में होता है जब हम अपने से पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रसिद्धि / स्वीकृति प्राप्त कवियों का मूल्यांकन पढ़ते है । इस क्रम में सबसे पहला आलेख है ‘निराला की कविता के अंतर्त्तत्व’। महाप्राण निराला को हम सब ने खूब पढ़ा, सुना, समझा, पसंद किया है और लगभग हर आलोचना पद्धति पर मूल्यांकित किया गया है । ‘गतानुगतिकता के प्रति तीव्र विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अंत तक बना रहा । यह ध्यान देने की बात है कि निराला जी के आरम्भिक प्रयोग छंद के बंधन से मुक्ति पाना के प्रयास हैं। छंद के बंधनों के प्रति विद्रोह करके उन्होंने उस मध्ययुगीन मनोवृत्ति पर पहला आघात किया था जो छंद और कविता को प्रायः समानार्थी समझती थी । उसमें भी एक प्रकार की झंकार और एक प्रकार की ताल और लय थी ।‘ लेखक ने निराला के काव्य की विवेचना बड़ी समग्रता से की है । उसमें कुछ चुनकर कुछ छोड़ कर बात नहीं की जा सकती । उनकी कुछ कविताएं तो जनमानस में बहुत गहराई से बसी हैं । जुही की कली तोड़ती पत्थर , भिक्षुक. और ‘राम की शक्ति पूजा’ प्रमुख हैं । राम की शक्तिपूजा कविता के हर आयाम पर प्रभावशाली है । निराला बंगाल में बड़े हुए हैं। वे बंगाल की शाक्त परंपरा से प्रभावित है। विष्णु के अवतार राम के द्वारा शक्ति की पूजा करवा कर वे स्त्री के पक्ष में खड़े हैं यह उनकी प्रगतिशीलता है । पर वे मिथक को ही पुष्ट करते हैं यह मेरी निगाह में एक विचलन है। निराला महाकवि ही नहीं महामानव भी हैं।
शमशेर के बारे में आपके आलेख ‘शमशेर की कविताई’ में जो लिखा उसके एक पैराग्राफ को उद्धृत करना चाहता हूँ जो उनके बारे में मेरे मन की बात कहता है । “शमशेर की कविता में वे सारे गुण एवं लक्षण हैं जो कि प्रगतिशील कविता में उपलब्ध होते हैं जैसे लोकमंगल की भावना, जनतांत्रिकता, प्रेम और सौंदर्य, मानवीय करुणा एवं संवेदना आदि। किंतु उसे व्यक्त करने का उनका जो ढंग है, शैली है उसके कारण उनकी कविता सामान्य पाठकों के लिए ही नहीं विशिष्ट पाठकों के लिए भी दुरूह हो जाती है। वास्तव में उनकी कविता के दो छोर हैं। कुछ बोधगम्य सरल कविताएं और कुछ नितांत जटिल कविताएँ। जटिल कविताएँ इनकी अवचेतन मन की सृष्टियाँ है। उनकी सहज सरल कविताओं में एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है ‘बात बोलेगी’-‘ बात बोलेगी / हम नहीं/ भेद खोलेगी/ बात ही/सत्य का / क्या रंग/ पूछो, एक संग/ एक जनता का दुःख एक/ हवा में उड़ती पताकायें अनेक/ दैन्य दानव। क्रूर स्थिति।/ कंगाल बुद्धि : मजदूर घर भर / एक जनता का अमर वर : एकता का स्वर / अन्यथा स्वातंत्र्य इति।
शमशेर के शिल्प की विशेषता को बारीकी से रेखांकित करते हुए मुक्तिबोध ने लिखा ‘अपने स्वयं की शिल्प का विकास केवल वही कवि कर सकता है जिसके पास अपने निज का कोई मौलिक विशेष हो, जो यह चाहता हो कि उसकी अभिव्यक्ति उसी के मनस्तत्वों के आकार की, उन्हीं मनस्तत्वों के रंग की, उन्हीं के स्पर्श और गंध की हो।
‘शाम का बहता हुआ दरिया कहाँ ठहरा! / सांवली पलकें नशीली नींद में जैसे झुकें / चांदनी से भरी भारी बदलियां है/ ख्वाब में गीत पेंगे लेते हैं / प्रेम की गुइयां झुलाती है उन्हें/ उस तरह का गीत, वैसी नींद, वैसी शाम-सा है/ वह सलौना जिस्म/ उसकी अधखुली अंगड़ाइयाँ है- कमल के लिपटे हुए दल/ कसे भीनी गंध में बेहोश भौंरे को।‘ शमशेर जी अपनी कवितायी के बारे में कहते हैं “कवितायी ना मैंने पायी, न चुरायी। इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा है। यह मेरी अपनी है और मुझे प्राण से भी अधिक प्यारी है।
बिम्ब – चित्रों, प्रतीकों और अत्यंत असंबद्ध स्थितियों के चित्रण से इनकी कविता साधारण पाठक की समझ एवं पकड़ से बहुत दूर चली जाती है।”। शमशेर और मुक्तिबोध साधारण पाठक लिए बहुत कठिन हैं । इनकी कविताओं को पढ़ाया जाना चाहिए।
केदारनाथ अग्रवाल सरल सीधे लगते हैं । उनका कहना है “यदि जिंदा रहना है तो प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। यथास्थिति में परिवर्तन न आया तो अलदें और मुक्तिबोध मरते ही रहेंगे। हम लेखक को प्रतिबद्ध रचना लिखनी चाहिए खतरे के बावजूद। कबीर, रैदास छोटे तबके के लोग थे, चिंतक, जागरूक थे। उन्होंने भंडाफोड़ किया व्यवस्था का। निराला ने भी यही किया” “हमें कला का उपयोग व्यवस्था बदलने, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए करना है। हमारे जवाब का यही रास्ता है। मैं सोचता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ, जब तक मौत न आए तब तक जीऊँ, उसका उपयोग करूँ। मैं अपना विकास पाने के लिए बेचैन हूँ। मुझे जीने का अर्थ वेद में, उपनिषद में कहीं नहीं मिला। मिला तो प्रतिबद्धता में। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पैब्लो नैरूदा मॉयकोव्सकी नाजिम हिकमत की तरह जीने की जरूरत है। यही जिंदगी का राज़ है और इसी से कविता बनती है ।” मेरे लिए यही मूलमंत्र है ।
आजादी की लड़ाई के उन उथल पुथल भरे बरसों में उनकी कविता में सामंतवाद के विरुद्ध भारतीय किसान संघर्ष का उद्घोष भी है और ब्रिटिश पूंजीवादी हितों के साथ नाभीनालबद्ध राष्ट्रीय नेताओं पर व्यंग्य भी । केदारनाथ अग्रवाल की राजनीतिक दूरदर्शिता यहाँ देखी जा सकती है कि 1947 की आजादी को सत्ता हस्तांतरण मानने की जो समझ प्रलेस की एक दशक बाद बनी उसकी ओर संकेत उन्होंने 1946 में ही कर दिया था- ‘लंदन गए/ लौटा आए/ बोलो, आज़ादी लाए/ नकली मिली है/ कि असली मिली है/ कितनी दलाली में कितनी मिली है /’ आजादी के बाद अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद का नव स्वाधीन देशों पर मंडराता कर्ज का मायाजाल हो, प्रशासकों, पूंजीपतियों, नेताओं का गठजोड़ हो या देश में घटित राजनीतिक मोड़ – उदाहरणार्थ आपात काल हो केदारनाथजी की कलम सभी मुद्दों पर चली है।
इस पाखंडी और विकृत समय में जो कहने का है उसे जनकवि बाबा नागार्जुन से बेहतर कोई नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं “प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित ‘स्व’ की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ़, अंध-बघिर व्यक्तियों को सही राह में लाने के लिए, अपने आप को भी ‘व्यामोह’ से बारंबार उबारने की खातिर, प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ शतधा प्रतिबद्ध हूँ। बाबा की कविताएँ अपने समय के समग्र परिदृश्य की जीवंत एवं प्रामाणिक दस्तावेज है उदयप्रकाश में सही संकेत किया है कि बाबा नागार्जुन की कविताएँ प्रख्यात इतिहास चिंतक डी. डी. कौशांबी की इस स्थापना का कि एक इतिहास लेखन के लिए काव्यात्मक परमाणु को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए अपवाद सिद्ध होती है वे कहते हैं कि हम उनकी रचनाओं से अपने देश और समाज के पिछले कई दशकों के इतिहास का पुनर्लेखन कर सकते हैं । एमरर्जेंसी पर लिखी हुई उनकी कविता – इन्दु जी इन्दु जी क्या हुआ आपको/ चर्चा की मस्ती में भूल गयी बाप को/ इंदु जी इन्दु जी क्या हुआ आपको/ बेटे को तार दिया/ बोर दिया बाप को / क्या हुआ आपको/ क्या हुआ आपको/ आपकी चाल ढाल देख देख लोग दंग/ घूमती नशे का वाह वाह कैसा चढ़ा रंग/ सच बताओ कि क्या हुआ आपको……. उनकी एक और चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कविता है ‘अकाल’- ‘कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास/ कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास/ कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त / कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त / दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद/ धुआं उठा आँगन के ऊपर कई दिनों के बाद/ चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद/ कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद/’
दीन, हीन, मजदूर किसान के पक्ष में और स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत गीत लिखने वाले जनवादी मूल्यों को समर्पित कवि मन्नूलाल शर्मा ‘शील’ की तत्कालीन आलोचकों में घोर उपेक्षा की और यह दृष्टि संपन्न कवि आँख से ओझल ही रहा । उनकी कविता जनवादी मूल्यों के लिए समर्पित कविता है जो बड़ी सहज सरल भाषा में होती थी कि बच्चे भी उनको समझते थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ निकलने वाली प्रभात फेरियों में गाते थे । ‘दिल्ली जगी, जगे मद्रासी जबलपुर ,लाहौर जगा / सिख, अछूत, हिन्दू, मुस्लिम का सोया हुआ हृदय सुलगा /’
शील जी के आत्म संघर्ष की यह कविता देखें -राह हारी मैं न हारा / थक गए पथ धूल के / उड़ते हुए रज कण घनेरे/पर न अब तक मिट सके हैं / वायु में पद चिह्न मेरे । जो प्रकृति के जन्म ही से / ले चुके गति का सहारा / राह हारी, मैं न हारा /
उस काल के जनमानस का चित्रण करते हुए कहते हैं – खाते पीते दहशत जीते /घुटते पिटते बीच के लोग / वर्ग धर्म पटकनी लगाता / माहुर पीते बीच के लोग / घर में घर की तंगी- मंगी / भ्रम में लटके बीच के लोग / लोभ – लाभ की माया लादे / झटके खाते बीच के लोग/ घना समस्याओं का जंगल / कीर्तन गाते बीच के लोग / नीचे श्रमिक विलासी ऊपर / बीच में लटके बीच के लोग ।
गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’ का जितना विराट और दुरूह रचना संसार कि उसको पढ़ना और समझना किसी आम पाठक के लिए तो नितान्त असंभव है । और उसके बारे में थोड़े में कुछ कहना अपने आप को उलझाना है । उसके लिए उनके ही शब्दों में ‘ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान’ दोनों की आवश्यकता होती है । उनके बारे में मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहा कि इस जनवादी कवि के टार्गेट पाठक /श्रोता कौन हैं ? मैंने अपनी वय के हिन्दी के प्रोफैसरों को यह कहते सुना है कि हमें मुक्तिबोध समझ में नहीं आते। उनकी कविता के हर शब्द का अर्थ जानने के बावजूद उनकी कविता समष्टि में क्या कहती समक्ष में नहीं आता। शायद वे समय से बहुत आगे थे । हम उनके प्रतीकों , बिम्बों को समझ ही नहीं पाते । शायद वे बड़े आलोचकों को बड़ा काम देकर गए हैं । लगभग चालीस साल पहले कवि मित्र सुभाष दसोत्तर ने उनकी एक कविता ‘ब्रह्मराक्षस’ को समझाया तो कुछ समझ में आया था ।
अपने आलेख ‘ आभाओं के उस विदा काल में’ के अंत शैलेन्द्र चौहान जी लिखते हैं – मुक्तिबोध मध्यवर्ग के अपने निजी कवि हैं । मध्यवर्गीय संघर्ष और विषमताओं को वे अपनी ताकत बनाते हैं। मुक्तिबोध के भीतर एक कसक, एक छटपटाहट हैं जो उन्हें चैन नहीं लेने देती है । सच तो यह कि उनके भीतर एक ब्रह्मराक्षस पैठा है जो ज्ञान पिपासु है और अपनी पीड़ा की पकड़ में कैद है । मगर दूसरों की पीड़ा उन्हें खलती है । “मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता/ जिससे कि उसका अधूरा कार्य/ उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुँचा सकूँ।
त्रिलोचन में एक ऐसे कवि हैं जो अपने निजी अनुभवों को, दुख और सुख को मात्र अपने साथ घट रही घटना या त्रासदी नहीं मानते बल्कि उसे दूसरों के अनुभव, दुख – सुख के साथ जोड़कर संवेदनों और भाव आवेगों का विस्तार करते हैं। ऐसा कवि जो शब्द और जीवन को एक दूसरे का पर्याय मान कर जीवन की अभिव्यक्ति शब्दों में करता है, बहुत शांत भाव से, न हो हल्ला, न शोर, न आक्रोश वह कवि है त्रिलोचन । उनकी कविता एक अंश देखे ‘कभी कभी लगता है कोई अर्थ नहीं है/ इस जीवन का यदि कुछ है तो मारकाट है/ हत्या और आत्महत्या है लूटपाट हैं/ बलात्कार है जग में कौन अनर्थ नहीं है/ निराकरण में कोई कहीं समर्थन नहीं है। ‘ संघर्ष श्रम अन्याय और शोषण के अतिरिक्त त्रिलोचन के रचना संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम सौंदर्य प्रकृति चित्रण और प्रफुल्लता ।
कवि रघुवीर सहाय की विशेषता ये है कि वे मध्यवर्गीय अंतर्विरोधों और आभासी अनुभवों की दुनिया में गहरे पैठकर अपने वस्तुगत निष्कर्ष निकालते हैं और उन्हें बहुत बारीकी से कविता में व्यंजित कर देते हैं। अपने समय के सत्य को आरपार में पकड़ने का न केवल गंभीर प्रयत्न करते हैं बल्कि अपनी कविता के माध्यम से समाज को वह सत्य बताना भी चाहते हैं । देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रांतों की राजधानियाँ और जिलों की कचहरियों तक की साड़ी हुई अधकचरी व्यवस्था और ढोंगी प्रशासन के विरुद्ध उनमें एक गहरी वितृष्णा मिलती है। मीडिया, भाषा, राजनीति, साहित्य, कला सभी उनके कैनवास पर सहज रूप से आदमी की देनदिन विडंबनाओं के चित्र उकेरने में स्वाभाविक उपकरण की तरह प्रयुक्त होते हैं । सहज भाषा में इतनी सारी व्यंजना पैदा करने में बिरले कवि ही सिद्धहस्त होते हैं। सत्ता का अपराधी चरित्र सदैव समाज में अपराधियों को प्रश्रय देता रहा है। हर शहर, कस्बे और गांव में ऐसे घृणित दुर्दांत अपराधी फलते फूलते हैं। पुलिस प्रशासन और राजनीति उनके कुकृत्यों के प्रति उदासीनता बरतते हैं। वे कवि के व्यँग्य के पात्र है। रघुवीर सहाय पत्रकारिता से कविता के क्षेत्र में आए। इसका उनकी कविता पर प्रभाव है। उनकी कविता में रहस्य, जिज्ञासा, राग, भय और साहस दर्ज है। सहाय ने राजनीतिक मुद्दों पर भी काफी लेखनी चलाई है लेकिन उनका विषय नेतृत्व चलाने वाले लोग न हो कर जनता होती थी जिस पर नेतृत्व किया जा रहा है। उनकी एक कविता के कुछ अंश देखें –‘हँसो तुम पर निगाह रखी जा रही है/ हँसो पर अपने पर न हँसना क्योंकि/ उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी/ और तुम मारे जाओगे’।
कुमार विकल को ये एहसास है कि आज की कविताओं में आनंद की अनुभूति कम होती जा रही है अपनी एक कविता में वे कहते हैं ‘मैंने चाहा था की मेरी कविताएं / नन्हें बच्चों की लोरियां बन जाएं/ जिन्हें युवा माँएं शैतान बच्चों को सुलाने के लिए गुनगुनाएं/ मैंने चाहा था कि मेरी कविताएं/ लोकगीतों की पंक्तियों में खो जाएं/ जिन्हें नदियों में मछुआरे/ खेतों में किसान /मेलों में मजदूर झूमते हुए गाएं’। आज की मायानगरी को कुमार विकल कुछ इस तरह चित्रित करते हैं ‘मैं भटका हूँ इसी कुटिल नगरी के तहखानों में/ जहाँ आदमी के खिलाफ़ साजिशें होती हैं।’ जहाँ साहित्य एक संसाधन है, विचारशून्य बनाने का हथकंडा है, जटिल और कुटिल भोग विलास है और पूरा तंत्र है जो इसके प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। वहाँ मंत्रालय है, सचिव हैं, अकादमी हैं, विश्वविद्यालय हैं, अखबार हैं, दूरदर्शन है, पत्रिकाएं हैं, यानी पूरा लवाजमा है। ये लावाजमा लोक विद्वेषी और लोक शोषक है । यह अपने जाल में उन सभी को फंसा लेता है जो अतिशीघ्र कुछ पाना चाहते हैं। मीडिया इस कार्य में पूरा सहायक होता है और वहाँ दलाल बैठे होते हैं कि कोई पंछी आए और दाना चुगे।
नाट्यकर्मी शिवराम की कविताओं में आत्मीय सहजता है, गहन संवेदना है, गहरा दायित्व बोध है, स्पष्ट दृष्टिकोण हैं, रोष है, व्यंग्य है, नाटकीयता है, संप्रेषणीयता है । निरंतर जागृत दार्शनिक, राजनीतिक चेतना के बावजूद उनकी कविताएं दर्शन राजनीति और विचारधारा के बोझ से दबी हुई नहीं हैं। उनकी कविताओं में विपरीत और जटिल परिस्थितियों से जूझते जीवन की अभिव्यक्ति है । यहाँ मृत सपने नहीं, दृढ़ इरादों का संकल्प है, करुणा की भिक्षा वृत्ति नहीं चुनौती और चेतावनी का साहस है, बड़बोला पन नहीं है, ईमानदार आलोचना है । ‘कोई कुछ करता दिखा तो मीनमेख निकाली /लंगडी मार दी/ या उपहास में उड़ा दिया / अपनी श्रेष्ठता का खुद नक्शा बनाया/ अपनी शान में खुद का कसीदे पढ़े/ डरते रहे भीतर तक/ लेकिन अपनी बहादुरी का डंका पीटते रहे। एक दूसरी कविता का अंश –‘ हम अमीरों की हवेलियों को किसानों की पाठशालाएं नहीं बना पाए/ नहीं खोल पाए हम अंधेरे का ताला /हम नहीं पढ़ पाए वह पाठ जिसे पढ़ते हुए देखना चाहते थे तुम हमें।
शिवराम कहते हैं कि रात इतनी भी नहीं है सियाह कि निराशा के घटाटोप में डूब जाए – ‘चंद्रमा की अनुपस्थिति के बावजूद/ और बावजूद आसमान साफ न होने के/ रात इतनी भी नहीं है सियाह/ कि राह ही न सूझे/
‘लोक परंपरा और समकालीन कविता’ शीर्षक आलेख में लेखक पुनः लोक पर लौट कर आते हैं। जिसमें वे सामंतवाद और उनके आश्रय में पलते हुए दरबारी कवि और उसके बाद भक्तिकाल के कवियों के बारे में बात करते हैं जिसमें कबीर, तुलसी, दादू, रैदास आदि प्रमुख हैं। उनका कहना है कि कबीर से ज्यादा सांप्रदायिकता विरोधी और तुलसी से अधिक समन्वयवादी उस युग में कौन था। शबरी के झूठे बेर खाते हैं कुलीन राजकुमार राम । वनों में घूमते घूमते ही राम केवट, सुग्रीव, जामवन्त, जटायु , आदि विभिन्न जनजाति के प्रतिनिधि लोगों से मैत्री करते हैं। कबीर हाथ में लाठी लिए आह्वान करते हैं कि जो घर बारे अपनों चले हमारे साथ। जन जीवन के साथ इन पुराने कवियों का बहुत गहरा सम्बन्ध है, व्यापक अनुभूतियां हैं, भौगोलिक ज्ञान, प्रकृति और मानवता से उनका घनिष्ठ संबंध है। उसी परम्परा से जुड़ते हैं बहुत सारे आधुनिक कवि जिनमें मुक्तिबोध, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, कुमार विकल, कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह, हरीश भदानी, शलभ श्रीरामसिंह, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना और विजेंद्र भी उस परंपरा से जुड़ते हैं। राजेश जोशी, अरुण कमल, उदयप्रकाश, वीरेन डंगवाल, गोरख पांडे आदि भी आगे जाकर उसी परम्परा से जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी परंपरा के विस्तार हैं महेन्द्र नेह , चंद्रकांत देवताले, विनय दुबे, कौशल किशोर, कुमार अम्बुज, भगवत रावत, मोहन डहेरिया, नरेन्द्र जैन, मदन कश्यप, पवन करण, गोविन्द माथुर , विनोद परदज आदि.।
विभिन्न कवियों की कविताओं के मूल्यांकन के बीच ‘वैज्ञानिक चेतना और साहित्य’ शीर्षक से प्रकाशित लेख एक अलग स्तर पर जनपक्षीय कविता का मूल्यांकन है। इस आलेख में चौहान साहब कहते हैं तर्कनिष्ठ वस्तुनिष्ठ वादियों ने परंपरागत दर्शन की आलोचना करते हुए उसे आघात देने वाली सबसे अधिक तीक्ष्ण बात यह कहीं है कि तत्व – मीमांसा के कथन में न केवल असत्य होते हैं अपितु निरर्थक होते हैं । सार्थक कथन केवल वे हैं जिनका गोचर तथ्यों की भारतीय मानस कसौटी पर निरीक्षण किया जा सके । चूकि परंपरागत तत्व-मीमांसा के वक्तव्य (जैसे आत्मा अमर है, दुनिया का रचयिता ईश्वर है, हम इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं आदि) गोचर अनुभव या इंद्रिय ज्ञान द्वारा परीक्षणीय नहीं होते, जैसे कि विज्ञान के कथन होते हैं। इसलिए वे अर्थहीन माने जाने चाहिए। निष्कर्ष यह है कि दर्शन का कोई मंतव्य निश्चयात्मक नहीं हो सकता।
अनेक अवैज्ञानिक अंधविश्वासी घटनाएं जोर पकड़ रही है जो हमारे संविधान की भावना को मुँह चिढ़ाती है। बाबाओं के आश्रमों में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। हमारे देश में आज आस्था वादी लोग नए सिरे से बुद्धि विवेक, तर्क, विज्ञान, भौतिक पदार्थ आदि का निषेध कर सामाजिक जड़ता व यथास्थितिवाद के पोषण का अभियान चला रहे हैं। राजनीति, सत्ता इसे प्रोत्साहित करती है, प्रश्रय देती है।
लेखक का कहना है आज भी हमारे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अपनी भाषा सटीक नहीं है ।यदि विज्ञान को जनमानस की संवेदना का हिस्सा बनाना है तो हमें भारतीय भाषाओं की और विशेष रूप से हिंदी की महत्ता को समझना ही पड़ेगा। इसी आलेख में वे मुक्तिबोध की कुछ कवितांशों का उदाहरण भी देते है ।
आलोक धन्वा की कविताओं को लेखक ने ‘रुमानी और मध्यवर्गीय पक्षधरता की और अभिजनवादी कविताएं’ कहा है जो जनसाधारण के पक्ष में होते हुए भी अपनी रचनात्मकता में जन तक न पहुँच कर केवल पढ़े लिखे शहरी अभिजन तक ही पहुँचती है । लेखक कहते हैं ‘’इंदिरा गांधी के शासन काल में आपात स्थिति से पहले ‘जनता का आदमी’ शीर्षक कविता काफी चर्चित रही है। उन दिनों कांग्रेसी शासन अपनी तानाशाही, अक्षमता, भ्रष्टाचार, और अराजकता के शिखर पर था। महंगाई ने जनमानस की कमर तोड़ दी थी ।कानून व्यवस्था लचर हो गई थी और फिर बेरोजगारी का दैत्य डैने पसारे आकाश में कुलांचे भर रहा था। जनता इस कुशासन से तंग आ चुकी थी और उसकी परिणति इंदिरा गांधी की राजनीतिक और कानूनी हार में हुई थी। इस इमरजेंसी के पूर्व आलोक धन्वा ने लिखा
‘यहाँ सिर्फ दांत और पेट है/ मिट्टी में धंसे हुए हाथ है/ आदमी कही नहीं/ केवल एक नीला खोखला है/ जो केवल अनाज मांगता रहता है/’’
आलोक धन्वा की एक और बहुचर्चित कविता है ‘भागी हुई लड़कियाँ’ ‘कितनी- कितनी लड़कियां भागती है। मन ही मन अपने रतजगे, अपनी डायरी में/ सचमुच की भागी लड़कियों से/ उनकी आबादी बहुत बड़ी है/’
इस पुस्तक में लेखक ने पुराने और नए कवियों की कई पीढ़ियों पर लिखा हैं । परन्तु बहुत से छूट भी गए । जो जनवादी कविता लिख रहें हैं या उस क्षेत्र की आलोचना में काम कर रहे है उनके लिए इस पुस्तक में बहुत कुछ है।
पुस्तक : कविता का जनपक्ष (आलोचना)
लेखक : शैलेन्द्र चौहान
मूल्य : रुपये 249/- मात्र
प्रकाशक : मंथन प्रकाशन,
85/175, प्रताप नगर, जयपुर-302033
————————-
संपर्क ; बी-11, शिवालिक बैंगलोज, बोपल, अहमदाबाद-380058
मो.9408230881