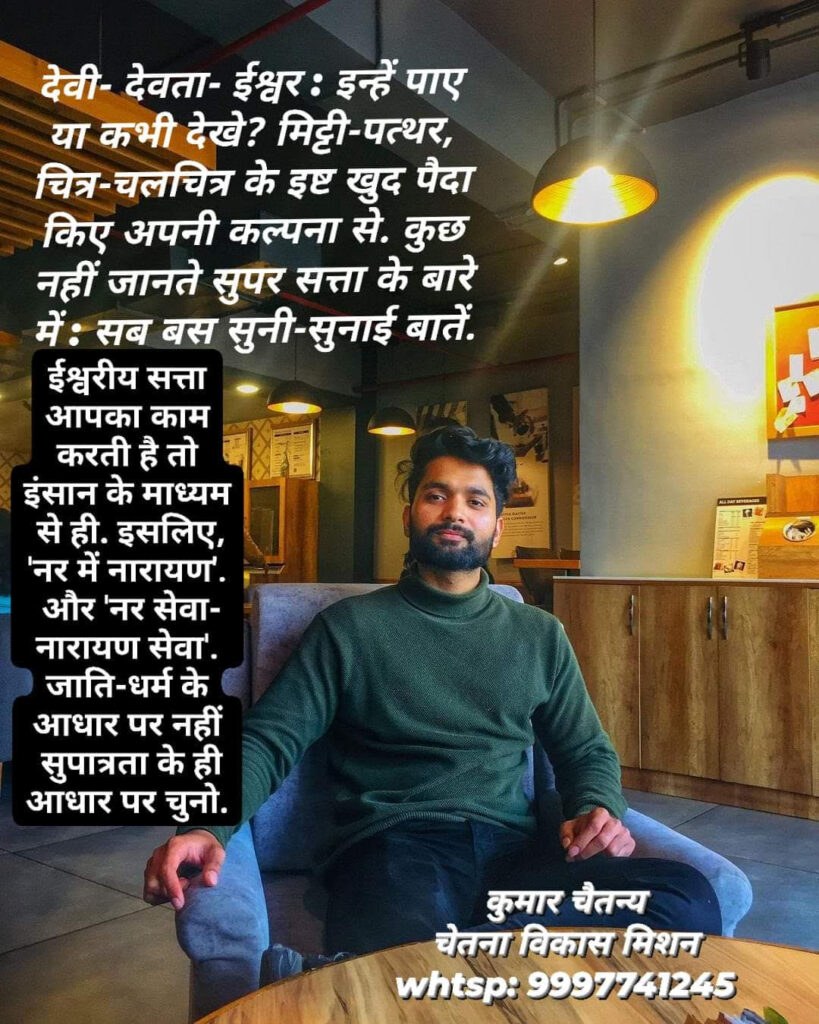कुमार चैतन्य
साधुओं की हालत कैदियों जैसी है! साधु मुक्त नहीं है। साधु सोच रहा है, मुक्ति के लिए पहले तो बंधन करने पड़ेंगे। यह भी खूब मजे की बात है! मुक्ति के लिए पहले बंधन मानने पड़ेंगे। मुक्त होने के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए।
कृष्णमूर्ति की एक किताब है: द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम – पहली और अंतिम मुक्ति। वह अष्टावक्र का आधुनिकतम वक्तव्य है।
अगर मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ। यह मत सोचो कि अंत में मुक्त होएंगे। पहले चरण पर ही मुक्त होना है; दूसरे चरण पर नहीं। क्योंकि अगर पहले ही चरण पर सोचा कि तैयारी करेंगे मुक्त होने की, तो उसी तैयारी में नये बंधन निर्मित हो जाएंगे।
फिर उन नये बंधनों से छूटने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी में फिर नये बंधन निर्मित हो जाएंगे। तो तुम एक से छूटोगे, दूसरे से बंधोगे। कुएं से बचोगे, खाई में गिरोगे।
देखो, गृहस्थ बंधा है और संन्यस्त बंधे हैं! दोनों के बंधन अलग- अलग हैं। मगर फर्क कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मौलिक मूर्च्छा जब तक नहीं टूटती, तुम जो भी करोगे बंधन होगा।
एक आदमी की स्त्री भाग गई, तो उसे खोजने निकला। खोजते-खोजते जंगल में पहुंच गया। वहां एक साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने पूछा कि मेरी स्त्री को तो जाते नहीं देखा? घर से भाग गई है। बड़ा बेचैन हूं।
तो उस साधु ने पूछा, तेरी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, ‘मेरी स्त्री का नाम, फजीती।’ साधु ने कहा, ‘फजीती ! तुमने भी खूब नाम रखा। ऐसे तो सभी स्त्रियां फजीती होती हैं, बाकी तूने नाम भी खूब चुन कर रखा। तेरा नाम क्या है? साधु उत्सुक हुआ कि यह तो नाम में बड़ा होशियार है। उसने कहा, ‘मेरा नाम बेवकूफ।
वह साधु हंसने लगा। उसने कहा, तू खोज-बीन छोड़। तू तो जहां बैठ जाएगा, फजीतियां वहीं आ जाएंगी। कोई कहीं तुझे जाने की जरूरत नहीं। तेरा बेवकूफ होना काफी है। फजीतियां तुझे खुद खोज लेंगी।
संसार को छोड़ कर आदमी भाग जाता है तो संसार छोड़ने से उसकी मंदबुद्धिता तो नहीं मिटती, उसकी मूढ़ता तो नहीं मिटती। मूर्च्छा तो नहीं मिटतो; वह उस मूर्च्छा को लेकर मंदिर में बैठ जाता है, नये बंधन बना लेता है। वह मूर्च्छा नये जाले बुन देती है। पहले संसार में बंधा था, अब वह संन्यास में बंध जाता है, लेकिन बिना बंधे नहीं रह सकता।
मुक्ति है प्रथम चरण पर। उसके लिए कोई आयोजन नहीं। आयोजन का मतलब हुआ कि अब आयोजन में बंधे। इंतजाम किया तो इंतजाम में बंधे। फिर इससे छूटना पड़ेगा। तो यह कहां तक चलेगा? यह तो अंतहीन हो जाएगा।
एक आदमी डरता था मरघट से निकलने से। और मरघट के पार उसका घर था। तो रोज निकलना पड़ता है। इतना डरता था कि रात घर से नहीं निकलता था, सांझ घर लौट आता था तो कंपता हुआ आता था। आखिर एक साधु को दया आ गई।
उसने कहा कि तू यह फिकर छोड़। यह ताबीज ले। यह ताबीज सदा बांध कर रख, फिर कोई भूत-प्रेत तेरे ऊपर कोई परिणाम न ला सकेगा।
परिणाम हुआ। ताबीज बांधते से ही भूत-प्रेत का डर मिट गया। लेकिन अब एक नया डर पकड़ा कि ताबीज कहीं खो न जाए। स्वाभाविक, जिस ताबीज ने भूत-प्रेतों से बचा दिया, अब वह आधी रात को भी निकल जाता मरघट से, कोई डर नहीं।
भूत-प्रेत तो कभी भी वहां नहीं थे। अपना ही डर था। ताबीज ने डर से तो छुड़वा दिया, लेकिन नया डर पकड़ गया कि यह ताबीज कहीं खो न जाए। तो वह स्नान-गृह में भी जाता तो ताबीज लेकर ही जाता; बार-बार ताबीज को टटोल कर देख लेता। अब वह इतना भयभीत रहने लगा कि रात सोए तो डरे कि कोई ताबीज न खोल ले, कोई ताबीज चुरा न ले जाए; क्योंकि ताबीज उसकी जिंदगी हो गई।
डर अपनी जगह कायम रहा-भूत का न रहा तो ताबीज का हो गया। अब अगर कोई इसको ताबीज की जगह कुछ और दे दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इस आदमी की भयभीत दशा तो नहीं बदलती। भूत का थोड़ी प्रश्न है, भय का प्रश्न है।
भय को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो। बहुत से लोग इसी तरह का वालीबाल का खेल खेलते रहते हैं; गेंद इधर से उधर फेंकी, उधर से इधर आई, बस फेंकते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और इस बीच जिंदगी गुजरती चली जाती है।
अष्टावक्र कहते हैं, समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं।
अष्टावक्र कहते हैं, अभी और यहीं घोषणा करो मुक्त होने की ! तैयारी मत करो। यह मत कहो कि पहले तैयार होंगे, फिर। क्योंकि फिर तैयारी बांध लेगी। फिर तैयारी को कैसे छोड़ोगे ?
एक रोग से छूटते हैं, दूसरा रोग पकड़ जाता है। यह तो कंधे बदलना हुआ। तुमने देखा, लोग मरघट ले जाते हैं लाश को, तो कंधे बदल लेते हैं; एक कंधे पर रखे-रखे थक गए तो दूसरे कंधे पर रख ली। थोड़ी देर राहत मिलती है। फिर दूसरा कंधा दुखने लगता है तो फिर बदल लेते हैं। ऐसे तो तुम जन्मों-जन्मों से कर रहे हो। बस यह सिर्फ राहत मिलती है।
इससे परम विश्राम नहीं मिलता। छोड़ो मुर्दों को ढोना। घोषणा करो! अगर तुम चाहो तो एक क्षण में, क्षण के एक अंश में घोषणा हो सकती है।
सिर्फ घोषणा करने की बात है। कुछ और करना थोड़े ही है; सिर्फ घोषणा करनी है। इस घोषणा को अपने हृदय में विराजमान करना है कि मैं संन्यस्त हूं, तो तुम संन्यस्त हो गए; कि मैं मुक्त हूं, तो तुम मुक्त हो गए। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा जीवन है।
घोषणा करने की हिम्मत करो। क्या छोटी-मोटी घोषणाएं करनी ? घोषणा करोः अहं ब्रह्मास्मि ! मैं ब्रह्म हूं! – तुम ब्रह्म हो गए। अंतस से करो, तन मन मस्तिष्क से नहीं.
आगे अष्टावक्र कहते हैं, ‘यह संसार तुझसे व्याप्त है, तुझी में पिरोया है। तू यथार्थतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो।’
क्या छोटी-छोटी बातों से जुड़ता है? कभी जोड़ लेता – यह मकान मेरा, यह देह मेरी, यह धन मेरा, यह दुकान मेरी! क्या क्षुद्र बातों से मन को जोड़ रहा है? त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः।
तुझसे ही सारा सत्य ओत-प्रोत है! तुझसे ही सारा ब्रह्म व्याप्त है!
शुद्धबुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्।।
क्यों छोटी-छोटी बातों की घोषणा करता है? बड़ी घोषणा कर! एक घोषणा चैतन्य स्वरूप हूं! शुद्ध-बुद्ध स्वरूप हूं।’ क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो ! हमने बड़ी छोटी-छोटी घोषणाएं की हैं। जो हम घोषणा करते हैं वही हम हो जाते हैं।
मंसूर ने मुसलमानों की दुनिया में घोषणा की, ‘अनलहक! मैं सत्य हूं,’ उन्होंने मार डाला। उन्होंने कहा यह आदमी जरूरत से बड़ी घोषणा कर रहा है। ‘मैं सत्य हूं!’ – यह तो केवल परमात्मा कह सकता है, आदमी कैसे कहेगा !
लेकिन हमने अष्टावक्र को मार नहीं डाला, न हमने उपनिषद के ऋषियों को मार डाला, जिन्होंने कहा, अहं ब्रह्मास्मि ! क्योंकि हमने एक बात समझी कि आदमी जैसी घोषणा करता है वैसा ही हो जाता है। तो फिर छोटी क्या घोषणा करनी !
जब तुम्हारी घोषणा पर ही तुम्हारे जीवन का विस्तार निर्भर है तो परम विस्तार की घोषणा करो, विराट की घोषणा करो, विभु की, प्रभु की घोषणा करो। इससे छोटी पर क्यों राजी होना ? इतनी कंजूसी क्या? घोषणा में ही कंजूसी कर जाते हो। फिर कंजूसी कर जाते हो तो वैसे ही हो जाते हो।
क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे; विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी मान्यता तुम्हारे जीवन की शैली है। ‘तू निरपेक्ष (अपेक्षा-रहित) है, निर्विकार है, स्वनिर्भर (चिदघन-रूप) है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धिरूप है, क्षोभ-शून्य है। अतः चैतन्यमात्र में निष्ठावाला हो।’
एक निष्ठा पर्याप्त है। साधना नहीं- निष्ठा। साधना नहीं – श्रद्धा। इतनी निष्ठा पर्याप्त है कि मैं चैतन्यमात्र हूं। इस जगत में यह सबसे बड़ा जादू है।
मनस्विद कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार-बार कहो कि तुम बुद्धिहीन हो, वह बुद्धिहीन हो जाता है। जितने लोग दुनिया में बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हैं, ये सब बुद्धिहीन नहीं हैं। ये हैं तो परमात्मा। इनको बुद्धिहीन जतला दिया गया है, बतला दिया गया है। इतने लोगों ने इनको दोहरा दिया है और इन्होंने भी इतनी बार दोहरा लिया है कि बुद्ध हो गए हैं। जो बुद्ध हो सकते थे, वे बुद्ध होकर रह गए हैं।
मनस्विद कहते हैं, किसी आदमी को तुम राह पर मिलो- वह भला-चंगा है- तुम देखते ही उससे कहो, ‘अरे तुम्हें क्या हो गया? चेहरा पीला है! बुखार है! देखें हाथ। बीमार हो! तुम्हारे पैर कंपते से मालूम पड़ते हैं।’
पहले तो वह इनकार करेगा क्योंकि सोचा भी नहीं था क्षण भर पहले तक-वह कहेगा, ‘नहीं-नहीं! मैं बिलकुल ठीक हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं?’ ‘ठीक है, आपकी मर्जी !’ फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी उसको मिले और कहे, ‘अरे! चेहरा पीला पड़ गया है, क्या मामला है?’ अब वह इतनी हिम्मत से न कह सकेगा कि मैं बिलकुल ठीक हूं। वह कहेगा, हां कुछ तबीयत खराब है। वह राजी होने लगा। हिम्मत उसकी खिसकने लगी।
फिर तीसरा आदमी मिले और कहे कि अरे ! अब तो वह घर ही लौट जाएगा कि तबीयत मेरी ज्यादा खराब है। अब बाजार जाने से कुछ सार नहीं।
एक ब्राह्मण एक बकरी को खरीद कर लाता था। तीन- चार लफंगों ने उसे देखा और उन्होंने सोचा कि इसकी बकरी तो छीनी जा सकती है। लेकिन ब्राह्मण मजबूत था और छीनना आसान मामला न था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी कूटनीति करो।
एक उसे मिला राह के किनारे और कहा कि गजब, यह कुत्ता कितने में खरीद लाए! उस आदमी ने, ब्राह्मण ने कहा, ‘कुत्ता! तू अंधा तो नहीं है? पागल कहीं के! बकरी है! बाजार से खरीद कर ला रहा हूं। पचास रुपये खर्च किए हैं।’
उसने कहा, ‘तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जानो। ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर लिए हो! भई, मुझको तो कुत्ता दिखाई पड़ता है। हो सकता है मेरी गलती हो।’
ब्राह्मण चला सोचता हुआ कि यह आदमी भी कैसा है! मगर उसने एक बार टटोल कर बकरी के पैर देखे। उसने कहा, बकरी ही है। दूसरे किनारे पर राह के दूसरा उन्हीं का सगा साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का खरीदा !
अब ब्राह्मण इतनी हिम्मत से न कह सका कि कुत्ता नहीं है; हो न हो कुत्ता ही हो! दो आदमी गलत नहीं हो सकते। फिर भी उसने कहा कि नहीं-नहीं, कुत्ता नहीं है। लेकिन अब कमजोर था। कह तो रहा था, लेकिन भीतर की नींव हिल गई थी। उसने कहा कि नहीं-नहीं, बकरी है। उसने कहा कि बकरी है? इसको बकरी कहते हैं?
तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी ब्राह्मण देवता! अगर इसको बकरी कहते हैं तो फिर कुत्ता किसको कहेंगे ? वैसे आपकी मर्जी। आप पंडित आदमी हैं, हो सकता है बदल दें। नाम की तो बात है। चाहे कुत्ता कहो, चाहे बकरी कहो- रहेगा तो कुत्ता ही। कहने से कुछ नहीं होता।
वह आदमी तो चला गया, ब्राह्मण ने बकरी उतार कर नीचे रख कर देखी, बिलकुल बकरी है। बिलकुल बकरी जैसी बकरी है। आंखें मींड़ीं। रास्ते के किनारे लगे नल से पानी से आंखें धोईं। क्योंकि अपना पड़ोस करीब आता जाता और लोग देख लें कि ब्राह्मण कुत्ता सिर पर लिए है तो पूजा और पांडित्य को धक्का लगेगा। पूजा करवाते हैं, लोग न करवाएंगे, लोग पागल समझेंगे।
मगर फिर देख-दाख कर उसने सब तरह से कि बकरी है; लेकिन इन दो आदमियों को क्या हुआ ! फिर रख कर चला, लेकिन अब जरा डरता हुआ चला कि फिर कोई और न देख ले। वह तीसरा उनका साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का है। कहां से लाए? हम भी बड़े दिन से कुत्ता चाहते हैं।
उसने कहा, बाबा तू ही ले ले! अगर कुत्ता चाहते हो तुम्हीं ले लो। यह कुत्ता ही है। एक मित्र ने दे दिया है, इससे छुटकारा करो मेरा।
वह भागा वहां से घर की तरफ कि किसी को पता न चल जाए कि कुत्ता इसने लिया है।
आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुमने जो मान रखा है वह तुम हो गए हो। और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं; जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने प्रयोजन हैं। पुरोहित समझाना चाहता है कि तुम पापी हो; क्योंकि तुम पापी नहीं हो तो पूजा कैसे चलेगी? उसका हित इसमें है कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े।
पंडित है, अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो उसके पांडित्य का क्या होगा ? उसकी दुकान कैसे चलेगी? धर्मगुरु है, वह अगर तुम्हें समझा दे कि तुम अकर्ता हो, कर्म- शून्य हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं – तो उसकी जरूरत क्या है?
यह तो ऐसा हुआ कि डाक्टर के पास तुम जाओ। और वह समझा दे कि बीमार तुम हो ही नहीं, बीमार तुम कभी हुए ही नहीं, बीमार तुम हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है- तो यह डाक्टर आत्महत्या कर रहा है अपनी। इसकी दुकान का क्या होगा ? तुम डाक्टर के पास जाओ भले-चंगे, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तब जाओ, तब भी तुम पाओगे कि वह बीमारी खोज लेगा।
तुम जा कर देखो! बिलकुल भले-चंगे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। जाकर, जरा चले जाओ, डाक्टर से कहना कि कुछ जांच-पड़ताल करवानी है। ऐसा डाक्टर खोजना बहुत मुश्किल है जो कह दे कि तुम बीमार नहीं हो।
एक बाप का बेटा डाक्टर हुआ। तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही है? उसने कहा कि काफी अच्छी चल रही है। मैंने कहा कि तुम कैसे समझे कि काफी अच्छी चल रही है। उसने कहा, इतनी अच्छी चल रही है कि कई दफे तो वह बीमारों को कह देता है कि तुम बीमार ही नहीं हो। यह तो बड़ा ही डाक्टर कह सकता है जिसकी खूब चल रही हो। चल रही ऐसी हो कि अब उसे उपद्रव ज्यादा लेना ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो उसने कहा, इससे मैं सोचता हूं कि बिलकुल ठीक चल रही है। कई दफा आदमियों को कह देता है कि नहीं, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है।
दुकानें हैं; उनके अपने हित है। तुम्हारे ऊपर हजारों दुकानें चल रही हैं- पंडित की है, पुरोहित की है, धर्मगुरु की है। तुम्हारा पापी होना जरूरी है। तुमने बुरे कर्म किए हों, यह आवश्यक है; नहीं तो तुम्हारा बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने बालों का क्या होगा ? मसीहाओं का क्या होगा, जो आते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए?
अगर अष्टावक्र सही हैं तो सब मसीहा व्यर्थ हैं। फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई जरूरत नहीं; तुम छूटे ही हुए हो। तुम मुक्त ही हो ! अष्टावक्र की जैसे कोई भी दुकान नहीं है। जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहते। सीधी- सीधी बात कह देते हैं, दो टूक सत्य कह देते हैं।
‘तू निरपेक्ष (अपेक्षा-रहित), निर्विकार, स्वनिर्भर (चिदघन-रूप), शांति और मुक्ति है तू। अगाध बुद्धिरूप, क्षोभ-शून्य है तू। अतः चैतन्यमात्र में निष्ठा वाला हो।’
एक ही निष्ठा होनी चाहिए कि मैं साक्षी-रूप हूं, बस पर्याप्त है। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति धार्मिक है। और किसी निष्ठा की कोई जरूरत नहीं। न तो परमात्मा में निष्ठा की जरूरत है, न स्वर्ग-नरक में निष्ठा की जरूरत है, न कर्म के सिद्धांत में निष्ठा की जरूरत है। एक निष्ठा पर्याप्त है। और वह निष्ठा है कि मैं साक्षी, निर्विकार। और तुम जैसे ही निष्ठा करोगे, तुम पाओगे तुम निर्विकार होने लगे।
एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया। एक कक्षा को दो हिस्सों में बांट दिया। आधे लड़के एक तरफ, आधे दूसरी तरफ – अलग-अलग कमरों में। फिर पहले हिस्से को जाकर कहा कि यह गणित बहुत कठिन है; तुममें से कोई भी हल न कर पाएगा। एक गणित लिखा बोर्ड पर और कहा, यह इतना कठिन है कि तुम्हारी तो सामर्थ्य ही नहीं, तुमसे आगे की कक्षा के विद्यार्थी भी इसको हल नहीं कर सकते। लेकिन हम एक प्रयोग कर रहे हैं।
हम जानना चाहते हैं, क्या तुममें से कोई इसको हल करने के थोड़े-बहुत भी करीब आ सकता है? थोड़ी-बहुत विधि, दो-चार कदम भी ठीक उठा सकता है? यह असंभव है! उसने यह बार-बार दोहराया कि यह असंभव है। फिर भी तुम चेष्टा करो।
दूसरे कमरे में गया। उसी वर्ग के आधे लड़के। वही बोर्ड पर उसने गणित लिखा और कहा कि यह प्रश्न इतना सरल है कि यह असंभव है कि तुममें से कोई इसे हल न कर पाए। तुमसे नीची कक्षाओं के लड़कों ने हल कर लिया है। तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यह तुम्हारी कोई परीक्षा करनी है, तुम तो हल कर ही लोगे, यह इतना सरल है। सिर्फ हम यह जानना चाहते हैं कि क्या एकाध विद्यार्थी ऐसा भी है तुम्हारी कक्षा में जो इसमें भी भूल-चूक कर जाए।
सवाल वही, कक्षा वही। बड़े अंतर आए परिणाम में। पहले वर्ग में पंद्रह लड़कों में से केवल तीन लड़के हल कर पाए। दूसरे वर्ग में पंद्रह में से बारह ने हल किया, केवल तीन हल न कर पाए। इतना बड़ा अंतर। सवाल वही। उस सवाल के साथ जो भाव दिया गया, वह परिणामकारी हुआ।
अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुःसाध्य है। अष्टावक्र कहते हैं, बड़ा सरल है। जो दुःसाध्य कहते हैं, वे दुःसाध्य बना देते हैं। जो कहते हैं, बड़ा असंभव है, खड्ग की धार, वे तुम्हें घबड़ा देते हैं। जो कहते हैं, यह तो हिमालय पर चढ़ने जैसा है, इसमें तो विरले चढ़ पाते हैं- तुम छोड़ ही देते फिकर कि ‘विरले तो हम हैं नहीं, यह अपने बस की बात नहीं; तो चढ़ें विरले, हम इस झंझट में न पड़ेगे।
हम स्वागत करते हैं विरलों का, जाएं! मगर हम सीधे-सादे आदमी, हमें तो इसी घाटी में रहने दो!’
अष्टावक्र कहते हैं, यह बड़ा सरल है। यह इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जाग कर देखना पर्याप्त है।
यह मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है। यह मनुष्य की अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप है।
एक राजनेता सख्त बीमारी से उठा। तो डाक्टर ने सलाह दीः दो- तीन महीने तक आप कोई भी दिमागी काम न करें। राजनेता ने पूछा, ‘डाक्टर साहब! यदि थोड़ी राजनीति इत्यादि करूं तो कोई आपत्ति है?’ डाक्टर ने कहा, ‘नहीं, बिलकुल नहीं, राजनीति आप जितनी चाहें करें, बस दिमागी काम बिलकुल न करें।’
राजनीति में दिमागी काम है भी नहीं। राजनीति में तो हिंसा है, प्रतिभा नहीं; छीन-झपट है, संघर्ष है, शांति नहीं; चैन नहीं, बेचैनी है; महत्वाकांक्षा है, ईर्ष्या है, आक्रमण है; आत्मा नहीं।
धर्म अनाक्रमण है, अहिंसा है, प्रतियोगिता-मुक्ति है; संघर्ष नहीं, समर्पण है। किसी से छीनना नहीं है; अपना जो है, उसकी घोषणा करनी है। अपना ही इतना काफी है कि किसी से छीनना क्या है? छीनते तो वे ही हैं जिन्हें अपना पता नहीं।
टुकड़े-टुकड़े के लिए लड़ते हैं, और परमात्मा भीतर विराजमान है! टुकड़े-टुकड़े के लिए मरते हैं, और परम विस्तार भीतर मौजूद है। सागर मौजूद है, बूंदों के लिए तरसते हैं!
जिन्हें अपना पता नहीं है, वे ही राजनीति में होते हैं। और जब मैं राजनीति कहता हूं तो मेरा मतलब इतना ही नहीं कि वे लोग जो राजनीतिक पार्टियों में हैं। राजनीति से मेरा मतलब हैः वे सभी लोग जो किसी तरह के संघर्ष में हैं।
वह धन कोई अष्टावक्र मिले, कोई बुद्ध मिले तो कहने का कोई सार है। किससे कहना यहां !
चल पड़े दर्द पी कर तो चलते रहे. दर्द पी-पीकर लोग चलते रहते हैं। हार कर बैठ जाने से इनकार था।
और यह अहंकार की धारणा हो जाती है कि हारकर बैठने का मतलब तो गए, डूब गए, मर गए। चलते रहो, कुछ न कुछ करते रहो ! कुछ न कुछ पाने की चेष्टा में लगे रहो! नहीं तो खो जाओगे।
मिलता उन्हें है जो बैठ जाते हैं। मिलता उन्हें है जो रुक जाते हैं। परमात्मा भागने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, परम विश्रांति में मिलता है।
कभी थोड़ा बैठो ! कभी घड़ी भर खोजकर, सिर्फ बैठो, कुछ मत करो !
झेन फकीरों में एक प्रक्रिया हैः झाझेन। झाझेन का मतलब होता है: बस बैठो और कुछ मत करो। बड़ी गहरी ध्यान की प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहनी ठीक ही नहीं; क्योंकि प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं, बस बैठो, कुछ भी न करो।
जैसे अष्टावक्र जो कह रहे हैं, वही झेन कह रहा हैः बैठ जाओ! कुछ देर सिर्फ बैठो विश्राम में। कुछ देर सब ऊहापोह छोड़ो! कुछ देर सब महत्वाकांक्षा छोड़ो। मन की दौड़-धूप, आपाधापी छोड़ो! थोड़ी देर सिर्फ बैठे रहो, डूबे रहो अपने में!
धीरे-धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फैलना शुरू होगा। शुरू में शायद न दिखाई पड़े। ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में घर लौटते हो तो घर के भीतर अंधेरा मालूम होता है; आंखें धूप की आदी हो गई हैं। थोड़ी देर बैठते हो, आंखें राजी हो जाती हैं तो फिर प्रकाश मालूम होने लगता है। धीरे-धीरे कमरे में प्रकाश हो जाता है।
ऐसा ही भीतर है। बाहर-बाहर चले जन्मों तक, तो भीतर अंधेरा मालूम होता है। पहली दफा जाओगे तो कुछ भी न सूझेगा… अंधेरा ही अंधेरा! घबड़ाना मत ! बैठो ! थोड़ा आंख को राजी होने दो भीतर के लिए। ये आंख की पुतलियां धूप के लिए आदी हो गई हैं।
तुमने खयाल किया, धूप में जब तुम जाते हो तो आंख की पुतलियां छोटी हो जाती हैं। धूप के बाद एकदम आईने में देखना तो तुम्हें पुतली बहुत छोटी मालूम पड़ेगी, क्योंकि उतनी धूप को भीतर नहीं ले जाया जा सकता, वह जरूरत से ज्यादा है, तो पुतली सिकुड़ जाती है। वह आटोमैटिक है, स्वचालित सिकुड़न है।
फिर जब तुम अंधेरे में आते हो तो पुतली को फैलना पड़ता है, पुतली बड़ी हो जाती है। अंधेरे में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर आईने में देखना तो पाओगे पुतली बड़ी हो गई।
जो इस बाहर की आंख का ढंग है, वही भीतर की तीसरी आंख का भी ढंग है। बाहर देखने के लिए पुतली छोटी चाहिए। भीतर देखने के लिए पुतली बड़ी चाहिए। तो अभ्यास हो गया है पुराना। उस अभ्यास को मिटाने के लिए कुछ नया अभ्यास नहीं करना है। बस बैठ रहो !
लोग पूछते हैं, ‘बैठ कर क्या करें? चलो कुछ राम-नाम दे दो, कोई मंत्र दे दो; उसी को दोहराते रहेंगे। मगर कुछ दे दो कुछ करने को!’ लोग कहते हैं, आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए।
अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ सिर्फ बैठो ! बैठने का भी मतलब यह नहीं कि बैठो ही; खड़े भी रह सकते हो, लेट भी सकते हो। बैठने से मतलब इतना ही हैः कुछ न करो, थोड़ी देर चौबीस घंटे में अकर्ता हो जाओ! अकर्मण्य हो जाओ! खाली रह जाओ!
होने दो जो हो रहा है। संसार बह रहा है, बहने दो; चल रहा है, चलने दो। आवाज आती है आने दो। रेल निकले, हवाई जहाज चले, शोरगुल हो-होने दो, तुम बैठे रहो। एकाग्रता नहीं- तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे-धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे अष्टावक्र का अर्थ क्या है-अनुष्ठान-रहित होने का अर्थ क्या है?
‘साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल-नित्य जान इस यथार्थ (तत्व) उपदेश से पुनः संसार में उत्पत्ति नहीं होती।’
जिसको बुद्ध ने कहा है, अनागामिन- ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो फिर वापस नहीं आता। क्योंकि वापस तो हम अपनी आकांक्षा के कारण आते हैं, राजनीति के कारण आते हैं। वापस तो हम वासना के कारण आते हैं। जो यह जान कर मरता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं, उसका फिर कोई आगमन नहीं होता। वह इस व्यर्थ के चक्कर से छूट जाता है- आवागमन से।
‘साकार को मिथ्या जान !’
साकारमनृतं विद्धि निराकारं निश्चलम् विद्धि।
‘निराकार को निश्चल-नित्य जान।’
जो हमारे भीतर आकार है, वही भ्रांत है। जो हमारे भीतर निराकार है, वही सत्य है।
देखा कभी पानी में भंवर पड़ती है। भंवर क्या है? पानी में ही उठी एक लहर है, फिर शांत हो जाती है, तो भंवर कहां खो जाती है? भंवर थी ही नहीं; पानी में ही एक तरंग थी; पानी में ही एक रूप उठा था। ऐसे ही हम परमात्मा में उठी एक तरंग हैं। तरंग खो जाती, कुछ भी पीछे छूटता नहीं। राख भी नहीं छूटती। निशान भी नहीं छूटता। जैसे पानी पर तुम कुछ लिखो, लिखते ही मिट जाता है – ऐसे ही जीवन की सारी आकार की स्थितियां तरंगें मात्र हैं।
‘जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है।’
दर्पण के सामने तुम खड़े होते हो, प्रतिबिंब बनता है। बनता है कुछ दर्पण में? प्रतिबिंब बनता है, यानी कुछ भी नहीं बनता। तुम हट गए, प्रतिबिव हट जाता है। दर्पण जैसा था वैसा ही है। जैसे का तैसा। तुम्हारे सामने होने से दर्पण में प्रतिबिंब बना था, हट जाने से हट गया; लेकिन दर्पण में न तो कुछ बना और न कुछ हटा, दर्पण अपने स्वभाव में रहा।
यह सूत्र कहता है अष्टावक्र का, कि जैसे दर्पण के सामने खड़े हों, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है; लेकिन प्रतिबिंब वस्तुतः बनता है क्या? बना हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबिंब से धोखा मत खा जाना। बहुत लोग धोखा खाते हैं प्रतिबिंब से।
प्रतिबिंब के चारों तरफ दर्पण हैं- बाहर-भीतर; प्रतिबिंब में दर्पण ही दर्पण हैं, और कुछ भी नहीं है। ऐसा ही, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। परमात्मा भीतर, परमात्मा बाहर, परमात्मा ऊपर, परमात्मा नीचे, परमात्मा पश्चिम, परमात्मा पूरब, परमात्मा दक्षिण, परमात्मा उत्तर- सब तरफ वही एक है। उस विराट के सागर में उठी हम छोटी भंवरें, छोटी तरंगें हैं।
अपने को तरंग मान कर मत उलझ जाना। अपने को सागर ही मानना। बस इतनी ही मान्यता का भेद है- बंधन और मुक्ति में। जिसने अपने को तरंग समझा, वह बंध गया; जिसने अपने को सागर समझा, वह मुक्त हो गया।
जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है।
‘जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर.’
घड़ा रखा है। घड़े के भीतर भी वही आकाश है, घड़े के बाहर भी वही आकाश है। तुम घड़े को फोड़ दो तो आकाश नहीं फूटता। तुम घड़े को बना लो तो आकाश बिगड़ता नहीं। घड़ा तिरछा हो, गोल हो, कैसा ही आकार हो, इससे आकाश पर कोई आकार नहीं चढ़ता।
हम सब मिट्टी के भांडे हैं; मिट्टी के घड़े। ब्गहर भी वही है, भीतर भी वहीं है। इस मिट्टी की पतली सी दीवार को तुम बहुत ज्यादा मूल्य मत दे देना। यह मिट्टी की पतली सी दीवाल तुम्हें एक घड़ा बना रही है। इससे बहुत जकड़ मत जाना। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि यह मिट्टी की दीवाल ही मैं हूं, तो फिर तुम बार- बार घड़े बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हें वापिस खींच लाएगी।
कोई और तुम्हें संसार में नहीं लाता है; तुम्हारे घड़े होने की धारणा ही तुम्हें वापिस ले आती है। एक बार तुम जान लो कि तुम घड़े के भीतर का शून्य हो।
लाओत्सु कहते हैं : घड़े की दीवाल का क्या मूल्य है? असली मूल्य तो घड़े के भीतर के शून्य का होता है। पानी भरोगे तो शून्य में भरेगा, दीवाल में थोड़े ही! मकान बनाते हो तुम, तो तुम दीवाल को मकान कहते हो? तो गलती है। दीवाल के भीतर जो खाली जगह है, वही मकान है। रहते तो उसमें हो, दीवाल में थोड़े ही रहते हो! दीवाल तो केवल एक सीमा है।
असली में रहते तो हम आकाश में ही हैं। हैं तो हम सब दिगंबर ही। भीतर के आकाश में रहो कि बाहर के आकाश में, दीवाल के कारण कोई फर्क थोड़े ही पड़ता है? दीवाल तो आज है, कल गिर जाएगी? आकाश सदा है।
तो तुम भूल से घर को अगर दीवाल समझ लेते हो और घड़े को अगर मिट्टी की पर्त समझ लेते हो और अपने को अगर देह समझ लेते हो, तो बस यही बंधन है। जरा सी गलती, पढ़ने में जीवन के शास्त्र को-और सब गलत हो जाता है। बड़ी छोटी सी भूल है!
एक व्यक्ति अपने विचारों में डूबा बस में चढ़ गया और सीट पर बैठ कर सिगरेट पीने लगा।
‘साफ-साफ तो लिखा है कि बस में धूम्रपान वर्जित है, क्या आपने पढ़ा नहीं? क्या आपको पढ़ना नहीं आता’, कंडक्टर ने क्रोधपूर्वक उससे कहा।
‘पढ़ तो लिया, लेकिन लिखने को तो बस में बहुत कुछ लिखा है। मैं किस- किस की बात का पालन करूं?’ ‘यही देखो! यहां लिखा है, हमेशा हैंडलूम की साड़ियां पहनो!’
जरा सा ऐसी भूलों से सावधान होना जरूरी है। शरीर बहुत करीब है, इसलिए शरीर की भाषा पढ़ लेनी बहुत आसान है। और शरीर इतना करीब है कि उसकी छाया भीतर के दर्पण पर पड़ती है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन तुम शरीर में हो, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर के नहीं।
शरीर तुम्हारा साधन है; तुम साध्य हो। शरीर का उपयोग करो; मालकियत मत खो दो! शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के पार रहो- जल में कमलवत.