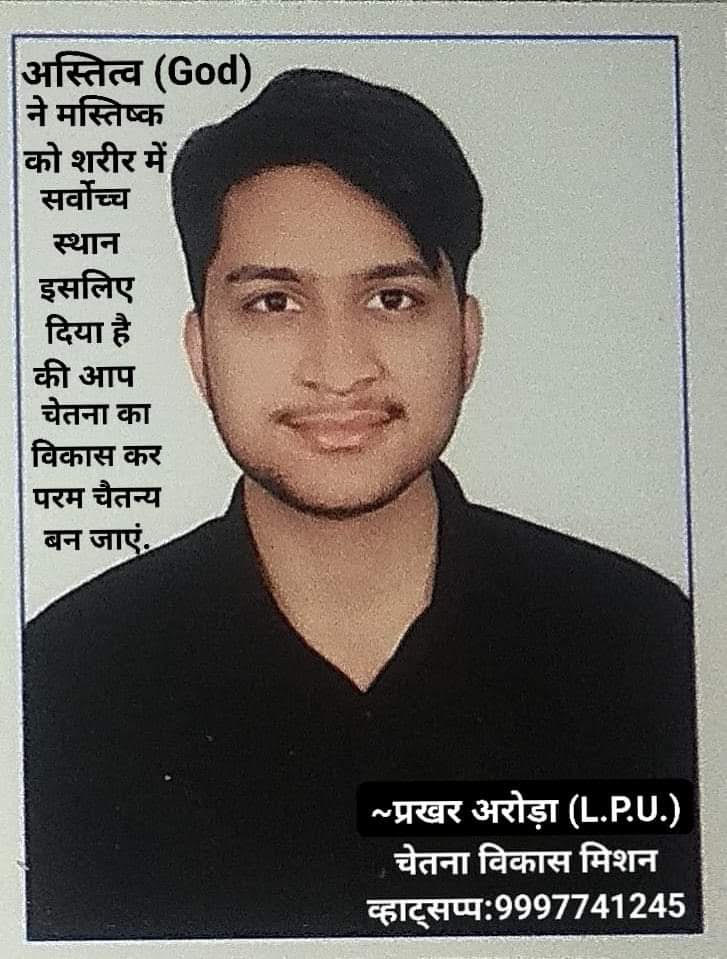प्रखर अरोड़ा
जब हम भारतीय दर्शन कहते हैं,तब हमारी दुविधा होती है कि इसे भारत में दर्शन या भारत की दर्शन परंपरा के रूप में लें या फिर भारतीय दर्शन इससे अलग की कोई चीज है, जैसे कि भारतीय संस्कृति। मेरे दृष्टिकोण से दर्शन अथवा फिलॉसफी एक विषय है और जैसा कि मैं सोचता रहा हूँ जैसे कोई भारतीय फिजिक्स या भारतीय केमेस्ट्री नहीं हो सकता ,वैसे ही भारतीय दर्शन भी नहीं हो सकता।
विज्ञान की तरह दर्शन की भी एक वैश्विक परम्परा है, जिसमें भारतीय मनीषियों का भी योगदान है। भारत या संसार का पूरबी हिस्सा माने गए मुल्कों में जीवन और जगत के बारे में सोचने के तरीके पश्चिम से तनिक भिन्न जरूर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक रहे हैं। पुराने जमाने में भारत में जिन दार्शनिक प्रश्नों से सिंधु सभ्यता के दौरान लोग टकरा रहे थे, बेबीलोनिया की सभ्यता के लोग भी टकरा रहे थे।
बुद्ध के ज़माने में जब हमारे इसी बिहार भूमि के एक हिस्से में मक्खलि गोसाल और महावीर जिन प्रश्नों से घिरे हुए थे, लगभग वैसे ही प्रश्न यूनानी दार्शनिकों को भी परेशां कर रहे थे। कहा जाता है, मध्यकाल में कुस्तुन्तुनिया के पतन के पश्चात् वहां के विद्वतजन जब यूरोपीय मुल्कों में गए तब वहाँ रेनेसां का दौर आरम्भ हुआ और हमारी पूर्वी दुनिया में कुछ सदियों केलिए अंधकारयुग आ गया। लेकिन समुद्री रास्तों की खोज के बाद पश्चिम के लोग जब भारत आए तब एक बार फिर वैश्विक तौर पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।
पश्चिम के विचारों ने भारतीय चेतना को अपनी परम्परा पर पुनर्विचार केलिए प्रेरित किया और कालान्तर में वेद, उपनिषदों और बुद्ध के विचारों से पश्चिम भी प्रगल्भ हुआ। इसलिए दर्शन को मैं क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक नजरिए से देखने का आग्रह रखता हूं।
आज हम जिसे आधुनिकता कहते हैं वह आखिर है क्या? रेनेसां और प्रबोधन के गर्भ से इस आधुनिकता का जन्म हुआ और यदि अतिसंक्षेप में कहें तो यह मध्ययुगीन तौर-तरीकों और नजरिये का निषेध है, अंत है। मध्ययुगीन खयालों और मूल्यों का नकार ही आधुनिकता का आधार बन जाता है। लेकिन क्या इस तरह की परिघटना केवल आधुनिक जमाने में ही हुई है।
मैं कहूंगा, नहीं। ये पहले भी होती रही हैं। पुराने जमाने में उपनिषदों की वैचारिकता को वेदान्त अथवा वेदों का अंत कहा गया। वैदिक ज्ञान के मुकाबले उपनिषदीय ज्ञान आधुनिकता है। और उपनिषदीय ज्ञान के मुकाबले बौद्ध और जैन विचार दर्शन कुछ अधिक नवीन, प्रांजल और अधिक आधुनिक हैं। इसलिए आधुनिकता कोई ठस या रूढ़ अवस्थिति नहीं है।
इसमें एक सातत्य है निरंतरता है। जब यह नैरंतर्य समाप्त हो जाता है, तब एक वैचारिक गतिहीनता की अवस्थिति आती है। यह जड़ता पुरातनता की प्रस्तावना करती है। और फिर परंपरा का भी समापन हो जाता है। परंपरा रूढ़ हो कर जड़ परिपाटी बनने लगती है। गतिहीनता अविवेक और अज्ञान पर जोर देती है और हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग परम्परा और परिपाटी के अन्तर को नहीं स्वीकार करना चाहते।
किसी परंपरा केलिए गतिशीलता आवश्यक होती है। इसके अभाव में हम किसी आधुनिकता की संकल्पना कर ही नहीं सकते। अर्थात् यह कि आधुनिकता और परम्परा का द्वंद्व निरन्तर चलता रहता है।
बिहार में पुराने ज़माने से दर्शन की एक जीवंत परंपरा रही है। मगध और मिथिला के ज्ञान-उर्वर इलाके विचारकों के आकर्षण केंद्र रहे। उपनिषद-काल में जनक ने वैदिक देवता इंद्र अथवा पुरंदर की जगह जब ब्रह्म की प्रस्तावना की थी तब वह वैचारिक क्रांति ही रही होगी। इंद्र ,जो कुछ अर्थों में लगभग लम्पट स्वभाव का था, की जगह अब ब्रह्म की प्रस्तावना थी।
सोमरस का पान करने वाले, रमणियों के साथ असीमित विलास करने वाले इंद्र का मुकाबला अब ऐसे ब्रह्म के साथ था,जो न खाता-पीता है,न सक्रिय रहता है। निर्गुण-निराकार की इस अवधारणा में कितनी आधुनिकता थी, आज हमारे विमर्श का विषय होना चाहिए। कपिल अपने कार्य-कारण सम्बन्ध की व्याख्या से दुनिया की द्वंद्वात्मकता को समझना चाहते हैं। बुद्ध कुछ और आगे आए। प्रतीयसमुत्पाद की अपनी प्रस्तावना में उन्होंने जगत को लगातार बनते और मिटते हुए देखा।
होने और विलोपित होने की सतत परंपरा को ही प्रतीत्यसमुत्पाद कहा गया है। एक का अंत दूसरे का जन्म है। इस के होने से उस की उत्पत्ति होती है। ‘ अस्मिन सति इदं भवति ‘। आज का विज्ञान इसकी आधुनिक व्याख्या के सिवा क्या है? पूरी दुनिया का मेटाबोलिज्म दरअसल प्रतीत्यसमुत्पाद की एक आधुनिक व्याख्या ही तो है।
लेकिन हमारी दार्शनिकता जगत की व्याख्या भर ही नहीं थी। क्या है और क्या होना चाहिए के बीच एक सम्यक सेतु की खोज हमारी दार्शनिक परंपरा का इष्ट रहा है। जैन दर्शन परंपरा में जिस स्यातवाद और अनेकांतवाद की विवेचना है उस पर कुछ समय ठहर कर सोचने का अनुरोध करना चाहूंगा।
सत्य एकमुखी नहीं, बहुमुखी हो सकता है। इस पृथ्वी का सत्य , इसका गुरुत्वाकर्षण ,गति के नियम और अन्य कायदे कोई जरूरी नहीं कि अन्य ग्रहों केलिए भी उतने ही सत्य हों। जो मेरा सत्य है, वह अन्य का सत्य भी हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे कोई जातक एक ही पहचान नहीं रखता। वह किसी का पिता हो सकता है,तो किसी का पुत्र और किसी का पति। इसलिए सत्य के अर्थ उसकी सापेक्षता पर निर्भर करता है।
जैन दर्शन के इस अनेकांतवाद में हम जिस बहुलतावादी दृष्टिकोण को पाते हैं ,वह इतना जनतांत्रिक है कि हमें आश्चर्य होता है कि उस ज़माने में महावीर ने इसकी कैसे संकल्पना की होगी। संभव है वैशाली में जो गणतंत्रीय राजव्यवस्था चल रही थी, उसका इस सोच पर प्रभाव हो। लेकिन यह अनेकांतवाद आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था केलिए अनुकूल और आधुनिक है। क्या हम बुद्धऔर महावीर के विचारों को पुरातन कह कर छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं!
यह ऐसा विषय है जिस पर बोलने और विमर्श करने केलिए तय समय से काम नहीं चलेगा। दर्शन की हमारी महान परंपरा में वैविध्य है। हमने सांख्य, योग ,न्याय , वैशेषिक , पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में अपनी दर्शन परंपरा को व्यवस्थित करने की कोशिश है। हम जिस प्रदेश में बैठे हैं इसी के एक तेजस्वी सपूत महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा ने अपने सातवें दर्शन परमार्थ -दर्शन की व्याख्या इसी शीर्षक से लिखे एक ग्रन्थ में की है।
मैं जब भी भारत की दर्शन परंपरा पर विचार करता हूँ तब मुझे महामहोपाध्याय का आदरपूर्वक स्मरण होता है। संस्कृत के विद्वान इस उद्भट विद्वान की हमारे यहाँ इतनी पूछ नहीं है,जिस के वह अधिकारी थे। जब हमें भारत की दर्शन परंपरा में आधुनिकता की तलाश करनी हो और हम उनका स्मरण नहीं करें यह हमारी कृतघ्नता या अज्ञानता होगी। महामहोपाध्याय ने 1905 ईस्वी में हिंदी जुबान में यूरोपीय दर्शन शीर्षक से एक किताब लिखी। अद्भुत किताब है।
पूरे पाश्चात्य दर्शन की उनकी अपनी व्याख्या है। यह किताब हिंदी में राहुलजी द्वारा लिखित ‘दर्शन-दिग्दर्शन ‘ से लगभग चार दशक और बर्ट्रेंड रसेल द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ़ वेस्टर्न फिलॉसोफी से भी इतने ही दशक पहले लिखी गई है।
परमार्थ दर्शन भी उसी के आसपास लिखी गई है। यानि बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में। उनकी मेधा पर आश्चर्य होता है। शर्मा जी कहते थे दार्शनिक दो तरह के होते हैं। एक श्रेणी संग्रहिता प्रवृत्ति के दार्शनिकों की होती है, दूसरी ऋषि प्रवृति के दार्शनिकों की। संग्रहिता प्रवृत्ति के लोग शास्त्रों का हवाला देते हैं और ऋषि प्रवृत्ति के लोग मौलिक बातें रखते हैं। शर्मा जी ऋषि प्रवृत्ति के थे।
परमार्थ दर्शन उनकी मौलिक कृति है, मीमांसा कृति नहीं। कुल मिला कर अपने दर्शन की उनकी व्याख्या यही है कि विभिन्न विधियों से संसार की व्याख्या का कोई अर्थ नहीं है। दर्शन का उद्देश्य होना चाहिए। कोई जातक स्वार्थ से सर्वात्म अथवा परमार्थ की ओर जब अभिगमन करता है, तो यह उसकी मुक्ति भी हो जाती है।
व्यक्तिगत मुक्ति का उनके यहां कोई स्थान नहीं बनता, वे सर्वात्मवाद अथवा सामाजिक मुक्ति की कामना और प्रस्तावना करते हैं। बोल्शेविक क्रान्ति के बहुत पहले लिखी गई इस कृति को कोई महत्व इसलिए नहीं मिला कि उनकी किताब संस्कृत में आई थी। कोई पृष्ठभूमि भी उन्हें उपलब्ध नहीं थी। जर्मन कम्युनिस्ट विचारक कार्ल मार्क्स ने अपने प्रसिद्ध लेख ‘ जर्मन आइडिओलॉजी ‘ में लिखा है कि अब तक के दार्शनिकों ने विभिन्न रूपों में इस दुनिया की व्याख्या की है,लेकिन प्रश्न यह है कि इसे बदला कैसे जाय।
सबको ज्ञात है, रामावतार शर्मा के जीवनकाल में मार्क्स का उपरोक्त लेख दुनिया के सामने नहीं आ सका था। उसका प्रथम बार प्रकाशन 1932 में हुआ। क्योंकि उस लेख को गैरजरूरी समझ कर स्वयं मार्क्स ने प्रकाशन के योग्य शायद नहीं समझा था। रूसी शोधार्थियों ने मार्क्स के घरेलु कचरे से उसे हासिल किया था। आज वह लेख मार्क्स के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला केंद्रीय लेख है। लेकिन आश्चर्य यह है कि रामावतार शर्मा जी ने अपनी हिंदुस्तानी दर्शन -परंपरा के रास्ते भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जहाँ मार्क्स पहुंचे थे।
यदि परमार्थ भाव नहीं है तब इस दर्शन -परंपरा का कोई अर्थ नहीं है। यही हमारे दर्शन परंपरा की आधुनिकता है और इस पर हमें थोड़ा गर्व भी है।
लेकिन आखिर में पूरी विनम्रता से आप सुधि जनों से प्रश्न करना चाहूंगा कि आज के पोस्ट ट्रुथ के जमाने में जब हम आधुनिकता क्या,उत्तराधुनिकता से भी आगे के दौर में हैं, इन विमर्शों की कोई जरूरत समाज को सचमुच है क्या? मेरा अन्तर्मन कहता है हमारा समाज आज भी इन प्रश्नों से घिरा है।
ऐसे समय में जब सत्य को अप्रासंगिक और प्रचार को आवश्यक करार दिया जा रहा हो, हमें अपनी दार्शनिक परम्परा को जीवन्त बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उसकी जड़ता समाप्त कर सकें। (चेतना विकास मिशन).