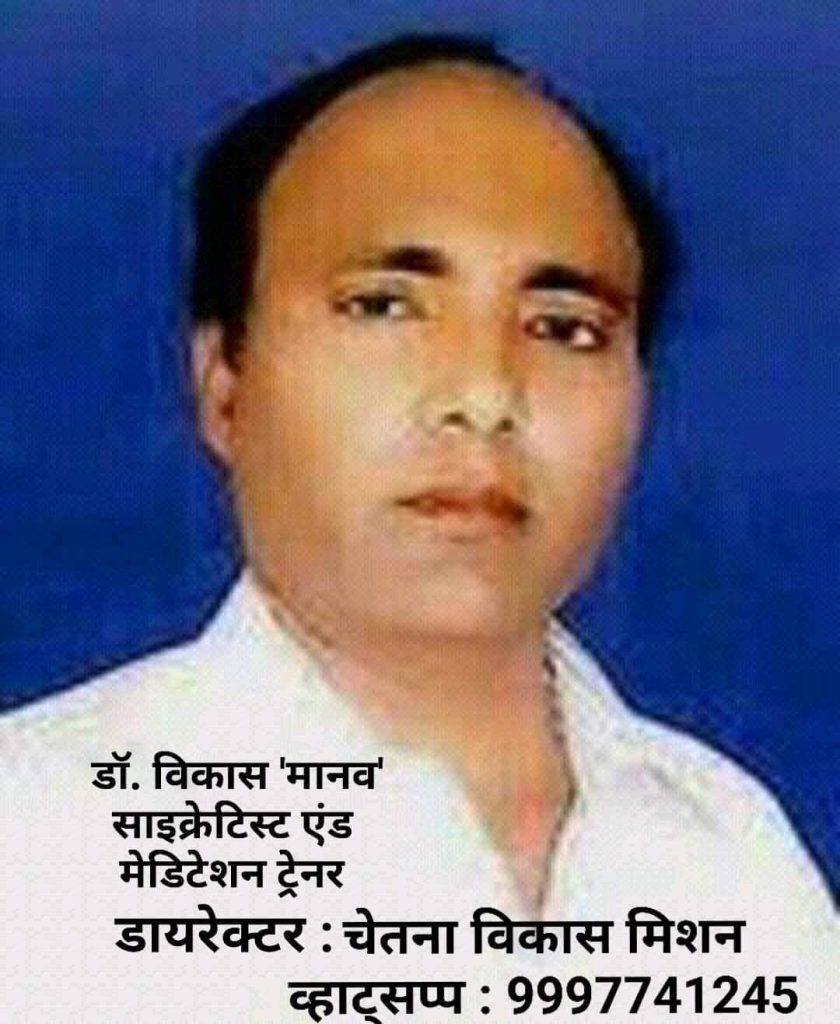डॉ. विकास मानव
_धर्म का जो अर्थ किया जा रहा है–क्या वह उचित है ? इसकी व्याख्या की जा रही है–क्या वह ग्राह्य है ? धर्म के अर्थ का अनर्थ कर इसके स्वरूप, भाव और उद्देश्य को समूल नष्ट करने का एक योजनाबद्ध दुश्चक्र रचा जा रहा है। सत्ता पाने की होड़ और सत्ता से खिसक जाने की आशंका–इन दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा है।_
मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अँधा और बहरा हो चुका है कि उसे निरीह मानवता का करुण क्रंदन न सुनाई दे रहा है और न दिखाई दे रहा है। धर्म के सम्बन्ध में जो विकृति दिखाई दे रही है, उसमें अन्य कारणों के आलावा “रिलीजन” शब्द का बहुत बड़ा हाथ है।
अंग्रेज जब भारत आया तो उसने “धर्म” शब्द सुना। उसके यहाँ धर्म शब्द जैसा कोई व्यापक अर्थ वाला शब्द नहीं था। इसलिए उसने धर्म का अनुवाद कर दिया–“रिलीजन”। रिलीजन में न तो धर्म का भाव ही है और न ही इस जैसी व्यापकता। धर्म एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक रिलीजन शामिल हो सकते हैं। रिलीजन को हमारे यहाँ मत, पंथ या उपासना-पद्दति कहा गया है।
अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक सम्प्रदाय हैं अनेक उपासना-पद्धत्तियाँ हैं, अनेक प्रार्थनाएं हैं–फिर भी धर्म एक है।
‘धर्म’ शब्द अति गूढ़ व महत्वपूर्ण है, तभी तो धर्म की स्थापना के लिए श्रीकृष्ण के रूप में स्वयं भगवान् ने इस भारत भूमि पर अवतार लिया और कहा-“धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।”
जहाँ धर्म है, वहीं विजय है ,इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं -” यतो धर्मस्ततो जयः।”
_तो आइये, हम धर्म को जानें, इसके वास्तविक अर्थ को समझें और इसके स्वरुप को पहचानें :_
“धर्म” शब्द “धृ”-धारण करना-इस धातु में “मन” प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है।”
धृयते पुण्यात्मभिरिति धरति लोकं वा” अर्थात्-पुण्यात्माओं के द्वारा जो धारण किया जाता है, वह धर्म है। अथवा–जो लोक को, विश्व को धारण करता है, वह धर्म है।
धर्म ही सबकी धारणा करता है। धर्म छूट जाय तो कोई वस्तु नहीं टिकेगी। इसलिए हमारे यहाँ धर्म के चार चरण बताये गए हैं। जिस प्रकार बैल के लिए आधार उसके चार पैर होते हैं, उसी प्रकार धर्म में चार चरणों पर सब कुछ टिका हुआ है। शरीर भोजन पर टिका है, तो भोजन करना शरीर-धर्म का पालन करना है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है। इसके बाद बुद्धि की बारी आती है।
बुद्धि से परे है ‘अहम्’। अहम् भी तुष्ट होना चाहिए। अंत में है–‘आत्मा’। इस प्रकार शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से युक्त जो मनुष्य है, इसकी धारणा कर सके, वही धर्म है।
धर्म किसी व्यक्ति पर लादने की वस्तु नहीं है। वह किसी संप्रदाय, समाज, मजहब विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। दरअसल, धर्म संसार में प्रचलित अनेक जीवन-शैलियों में से अपने विवेक द्वारा अपनाई गई और आचरण में लाई गई जीवन-शैली का नाम है। आज यदि संसार में अच्छाई में, भलाई में, मानवता में कोई उन्नति दिखाई पड़ती है तो उसके मूल में है धर्म।
यदि नास्तिकों में सदाचार और मनुष्यता के दर्शन होते हैं तो उसके मूल में है उनका धर्म के प्रति विश्वास। यदि ईश्वर के मानने वालों में क्रूरता और अमानवीयता की प्रबलता दिखाई पड़ती है तो उसका कारण है–धर्म के प्रति ढोंग।
धर्म पूजा-पाठ तथा अनुष्ठानों का विषय नहीं है, अपितु व्यवहार का विषय है, आचरण का विषय है जिसका असर समाज पर पड़ता है। मनुष्य के स्वार्थ ने, स्वार्थदृष्टि ने धर्म को बाँट दिया है। आज उसे खंडित धर्म दिखाई दे रहा है। सम्प्रदायों ने धर्म के टुकड़े कर दिए हैं। धर्म अब हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, आर्य समाजी धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म आदि अनेक रूपों में बंट गया है।
धर्म का अर्थ है–विषय भोग से निवृत्ति तथा शुभ में प्रवृत्ति। धर्म का अर्थ है–आत्मा से, परमात्मा से साक्षात्कार करने का साधन। धर्म सिद्धांत नहीं, आचरण है। यह आत्मा में प्रेम जगाता है, संसार के प्रति वैराग्य जगाता है और मनुष्य को तटस्थ तथा वीतरागी बना देता है।
स्वयम् के भाव में अर्थात्–“स्व”भाव में जीना धर्म है। “स्व”भाव से च्युत होना अधर्म है। अधर्म का अर्थ है-“स्व”(आत्मा) को त्याग कर संसार की अन्य वस्तुएं पाने का प्रयास। यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि “रथ” क्या है? आपका उत्तर होगा–धुरी, चक्र और पटलों का जोड़ रथ है।
इसी प्रकार जीवन में तप, संयम और अहिंसा का जोड़ धर्म है। धर्म जीवन के लिए जल है। जीने के लिए मात्र रोटी ही नहीं, तप, संयम और अहिंसा रुपी जल भी आवश्यक है।
*धृयते पुण्यात्मभिः इति धर्मः*
पुण्यात्माओं के द्वारा जिस श्रेष्ठ तत्व को धारण किया जाय, वही धर्म है। ईश्वर धर्म और अधर्म दोनों में है। जब तक ईश्वर को हम सर्वत्र नहीं देखेंगे, तब तक हम समस्त विश्व के एकत्व का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हरेक व्यक्ति में ईश्वर के दर्शन कीजिये–देखिये वे ही सब हाथों से काम कर रहे है, सब पैरों से चल रहे हैं, सब मुखों से भोजन कर रहे हैं, सब मनों से मनन कर रहे हैं।
वे स्वतः प्रमाण हैं। यही जानना धर्म है। समस्त जगत का अखंडत्व–यही धर्ममत है। “वसुधैव कुटुम्बकम्”–यही धर्म सिद्धांत है।
चैतन्य ही अनंतश्वरूप है, मानव भी अनंत है और अनंत ही अनंत की उपासना में समर्थ हो सकता है। धर्मप्राण उपनिषद् के वाक्य हमें इस पथ की ओर संकेत करते हैं और उस पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं–
*क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयोः वदन्ति।*
जो धर्म के गलियारे से होकर जाता है, उस्तरे की धार की तरह तेज है, दीर्घ है और कठिन है–इससे पार पाना कठिन है।
*”उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।”*
अर्थात उठो, जागो,जब तक लक्ष्य तक न पहुँचो, तब तक मत रुको।
व्यवहार में हम सब जगह दो शक्तियों की क्रिया- प्रतिक्रिया देखते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत काम करती प्रतीत होती हैं। ये दो शक्तियां बाह्य जगत में आकर्षण-विकर्षण और अंतर्जगत में राग-द्वेष, शुभ-अशुभ के रूप में प्रकाशित हैं। हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं और किसी से दूर रहना चाहते है।
इस आकर्षण-विकर्षण का कारण लोगों को अज्ञात है। जिस दिन इसका पता चल जायेगा उसी दिन दो शक्तियों की प्रतीति भी नष्ट हो जायेगी। तब हमें ज्ञात हो जायेगा कि शक्तियां दो नहीं एक है। दो की तो प्रतीति मात्र है। इस प्रतीति को ही नष्ट करने का नाम धर्म है।
हमारे चारों पुरुषार्थों का आधार धर्म ही है। धर्म जीवन में बहुत आवश्यक है। उपभोग से काम की प्राप्ति होती है। पर उपभोग भी धर्म के अंतर्गत आता है। धर्मानुसार उपभोग करने पर शांति मिलती है तथा काम की पूर्ति होती है। काम की पूर्ति भी धर्मानुसार ज़रूरी है।
काम-कामना-इच्छा मन का गुण है। मन चंचल है। मन कहीं-का-कहीं चला जाता है। इसलिए उसके लिए बुद्धि रुपी लगाम चाहिए। बुद्धि उसको खींच कर रखेगी। फिर आत्मा जो रथ (शरीर) पर बैठी है वह ठीक तरह से बैठी रह सकेगी। बुद्धि सारथी का कार्य करती है। आत्मा रथी है। रथ है–शरीर और इसमें जुते हुए हैं घोड़े जो हैं हमारी इन्द्रियां।
*”आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च।*
*बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।।”*
लगाम ढीली होने पर इन्द्रिय रुपी घोड़े गलत मार्ग पर चले जायेंगे। बुद्धि को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। पैर मंदिर के वजाय मदिरालय की ओर मुड़ सकते हैं। यदि बुद्धि धर्मानुसार न चली तो वह कहीं-की-कहीं ले जा सकती है।
मन का गुण है ‘काम’। उसकी तृप्ति बुद्धिपूर्वक हो, बुद्धि का आधार धर्म हो तो ही श्रेष्ठ कार्य हो सकेगा जो सुख देगा। इसीलिए कहा गया है कि अर्थ (धन)धर्म के लिए हो तो धर्म बढ़ता है। धर्म जितना बढ़ता है, उससे अर्थ और काम के सेवन की इच्छा उतनी ही कम होती जाती है। फिर धर्म ही मुक्ति का द्वार खोल देता है।
“जगत का अखंडत्व”-ही धर्ममत है। “वसुधैव कुटुम्बकम्”-यही धर्म सिद्धांत है।
“यह अनेकत्व में एकत्व का ज्ञान” करा देता है।
*धर्म के तीन स्कंध :*
1-विद्या, अध्ययन, ज्ञानार्जन,
2-यज्ञ जिसका अर्थ है–उत्तम क्रियाओं को करना तथा
3-तपश्चर्या अर्थात्– ईश्वरीय ज्ञान।
इसी प्रकार धर्म के तीन भाग हैं– पहला भाग है-दार्शनिक। इसमें धर्म के सारे विषय, मूल तत्व, उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के उपाय हैं। दूसरा भाग है–पौराणिक। यह स्थूल उदाहरणों द्वारा दार्शनिक भाग को स्पष्ट करता है। इसमें महापुरुषों और अलौकिक पुरुषों के जीवन के उपाख्यान हैं। तीसरा भाग है अनुष्ठान संबंधी।
यह धर्म का स्थूल भाग है। इसमें पूजा-पद्धति, आचार, अनुष्ठान, पुष्प, धूप, दीप, धूनी आदि विविध प्रकार की इन्द्रियग्राह्य वस्तुएं हैं। धर्म का यह स्थूल भाग ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार मनुष्य को अध्यात्म- लाभ के लिए स्थूल शरीर के द्वारा साधना करनी पड़ती है। ये पूजा, अनुष्ठान, आचार, पुष्प, धूप, दीप, धूनी आदि उसके स्थूल साधन हैं जो धर्म के ही अंग हैं।
यह देखा जा सकता है कि जितने प्रसिद्ध धर्म हैं, वास्तविकता यह है कि धर्म अनेक नहीं एक है। वह जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, देश, काल, पंथ आदि की दीवारों में जकड़ कर बाँट दिया गया है और वह अनेक रूपों में भाषित हो रहा है। हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी इसके नाम हो सकते हैं। नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, भाग अनेक हैं।
स्थूल रूप में अलग-अलग प्रतिभाषित होते हैं पर उन सब में मूलतत्व एक है–वह ( “तत्व” और वह “तत्वदर्शन”), उनके ये तीन विभाग हैं–दार्शनिक, पौराणिक और आनुष्ठानिक। कोई धर्म दार्शनिक भाग पर अधिक बल देता है तो कोई अन्य भागों पर। प्रत्येक धर्म वाले अपने मत की व्याख्या करके उसी को एकमात्र सत्य कहकर उसमें विश्वास करने के लिए कहते हैं। कोई-कोई तो दूसरों को अपने मत में लाने के लिए और उसीके अनुसार चलने के लिए हथियार तक उठा लेते हैं।
वे ऐसा दुष्टता से करते हैं–ऐसा नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है। मानव मस्तिष्क में सहज उत्पन्न धार्मिक कट्टरता नामक”व्याधि” की प्रेरणा से वे ऐसा करते हैं। यह धार्मिक कट्टरता, धर्मान्धता एक भयानक बीमारी है। मानव में जितनी दुष्टता उपजी है, वह उसी बीमारी ने जगाई है।
सभी धर्मों का अपना- अपना पुराण-साहित्य है। लेकिन सभी कहते हैं “केवल हमारे पुराणों की कथाएं कपोलकल्पित नहीं हैं। ईसाई मतानुसार ईश्वर “पंडुक” (एक प्रकार का कबूतर) का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनके लिए यह पौराणिक सत्य है, मात्र पौराणिक कहानी नहीं। हिन्दू लोग “गाय” को माता, देवी भगवती के आविर्भाव के रूप में मानते हैं।
ईसाई कहते हैं–यह सब कपोल-कल्पना है। इस प्रकार के विश्वास का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, यह केवल पौराणिक कहानी है, मात्र अन्धविश्वास है।
यहूदी समझते हैं कि यदि एक संदूक के दो पल्लों में दो देवदूतों की मूर्तियां स्थापित की जाएँ तो उस प्रतीक को मंदिर के पवित्रतम भीतरी भाग में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी सुन्दर स्त्री या पुरुष की मूर्ति हो तो वे कहते हैं कि यह एक वीभत्स प्रतिमा मात्र है। इसे तोड़ डालो।
यदि कोई कहे कि हमारे अवतारों ने औरों की अपेक्षा अधिक आश्चर्यजनक कार्य किये तो दूसरे लोग कहेंगे कि यह केवल अन्धविश्वास है। इसी प्रकार एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की पूजा-पद्धति व अनुष्ठानों को घोर अन्धविश्वास मानते हैं। ईसाईयों के लिए लिंगोपासना की मूर्ति वीभत्स है और हिंदुओं के लिए ईसाईयों का अनुष्ठान विशेष “सैक्रेमेंट” वीभत्स है।
हिन्दू कहते हैं कि किसी मनुष्य की हत्या करके उसके मांस को खाना, उसके खून को पीना पैशाचिक कृत्य है। लेकिन कुछ जंगली जातियां ऐसा करती हैं। उनका विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति साहसी होता है तो वे लोग उसकी हत्या करके उसके ह्रदय को खा जाते हैं।
कारण–वे समझते हैं कि ऐसा करके वे उस साहसी व्यक्ति के साहस और वीरता नामक गुण ग्रहण कर रहे हैं।
अपने-अपने पंथ, अपने अपने संप्रदाय के धर्म को श्रेष्ठ ठहराने की होड़ रहती है। किन्तु जहाँ अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को हेय समझने की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीँ ज़ोर जबरदस्ती का जन्म हुआ। संगठन शुरू हो गए। जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, वर्ग विशेष की दीवारों में मनुष्य-मनुष्य को बाँट कर संगठन शुरू हो गए। समता के विपरीत हो गए वे। असमता बढ़ने लगी।
लेकिन जो धर्म अपने ह्रदय में “वसुधैव कुटुम्बकम्” और “विश्व बंधुत्व” का उदात्त भाव अनुभव करते हैं, वे लंबी-चौड़ी बातें नहीं करते और न इस कारण मानव को मानव से काट कर जाति, वर्ण, संप्रदाय की रचना करते हैं। उनके मन में सचमुच सम्पूर्ण मानवता के प्रति बंधुत्व का भाव रहता है।
वे केवल बातें न बना कर काम कर दिखाते हैं। आदर्श के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिए विश्व एक परिवार है।
*क्या कथित धर्मों में कोई “सार्वभौमिक भाव” ?*
ऎसा भाव खोजने का कार्य अत्यंत कठिन है। हम सभी मानव हैं। हम लोगों में कुछ पुरुष हैं, कुछ स्त्रियां हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं लेकिन हैं तो सभी मानव। सभी मानव जाति के अंतर्गत आते हैं। यही सार्वभौमिक भाव खोजना है।
इसमें मनुष्यत्व का जो भाव है, वह सब में विद्यमान है। वह अमूर्त भाव उसी परम तत्व का है। सार्वजनीन धर्म के बारे में भी यही बात है। यह “ईश्वर रूप” से पृथ्वी केें सभी धर्मों में विद्यमान है–
*”मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव।”*
अर्थात् मैं इस जगत में मणियों के भीतर सूत्र की भांति विद्यमान हूँ। प्रत्येक मणि को एक धर्म विशेष, मत या संप्रदाय विशेष कहा जा सकता है। अलग- अलग मणियाँ एक-एक धर्म हैं और वह तत्व ही सूत्र रूप में उन सबमें विद्यमान है.
*विविधता ही जीवन का मूल :*
बहुत्व के बीच में एकत्व का होना सृष्टि का नियम है। हम लोग मनुष्य होते हुए आपस में अलग हैं लेकिन मनुष्य जाति के अंश के रूप में हम सब एक हैं। जब हम व्यक्ति विशेष होते हैं तो हम अलग-अलग होते हैं। पुरुष होने से हम स्त्री से अलग हैं पर मनुष्य होने के नाते स्त्री पुरुष एक हैं। मनुष्य होने के नाते हम जीव जंतुओं से अलग हैं।
किन्तु प्राणी होने के नाते स्त्री पुरुष जीव जंतु सभी समान हैं और “एक सत्ता” के नाते हमारा सबका विराट विश्व के साथ एकत्व है। भगवान ही वह विराट सत्ता है। वह ही इस जगत- प्रपंच के रूप में प्रकट है। उस ईश्वर से जुड़े हुए हम सब एक हैं। लेकिन हमारी चेष्टाएँ बाह्य रूप से अलग हैं और अलग रहेंगीं।
इसी प्रकार सार्वजनीन धर्म का यह अर्थ है कि किसी मत विशेष में संसार के सभी लोग विश्वास करें, उसके अनुसार चलें तो यह सर्वथा असंभव है। ऐसा समय कभी नहीं आएगा की सब लोगों का मुख एक जैसा हो जाय, . रंग एक जैसा हो जाय।
ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी एक ही पौराणिक तथ्य में विश्वास करने लगें। यह भी नहीं हो सकता कि सभी एक ही अनुष्ठान पद्धति को मान लें और उसे अपना लें। यदि कभी ऐसा हो भी जाय तो सृष्टि लुप्त हो जायेगी। कारण की “विविधता”ही जीवन का मूल है और वैचित्र्य ही उसकी विशेषता है।.
हम लोगों का आकार किसने बनाया?–विषमता ने। सम्पूर्ण साम्यभाव होने से सम्पूर्ण विनाश निश्चित होता है। प्रकृति के साम्यावस्था में प्रलय हो जाती है।
यदि हम सब लोग एक प्रकार से विचार करेंगे, तो विचारों में विविधता नहीं आएगी। विविधता न होने से सजीवता नहीं रहेगी। हम निर्जीव हो जायेंगे, निष्क्रिय हो जायेंगे। हमारे मन में कोई भाव नहीं उठेगा। इसलिए यह भिन्नता, यह विषमता ही हमारी उन्नति का प्राण है।
हमारे चिंतन की सृष्टा है। जिस तरह हमने स्वाभाविक रूप से एकत्व को स्वीकार किया है, उसी प्रकार यह भिन्नता विषमता भी स्वीकार करनी पड़ेगी।
जैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के वर्तन लेकर जल भर लें, कोई कटोरी लाये, कोई लोटा लाये, कोई घड़ा लाये, तो कोई बाल्टी लाये। जल भरने के बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्तन के जल ने स्वाभाविक रूप से अपने अपने वर्तन का आकर ग्रहण कर लिया है। परंतु वर्तन में वही एक ही जल है जो सबके पास है।
धर्म के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। हमारे मन भी उन वर्तनों के सामान हैं। हम सब ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तनों में जो जल भरा है ,ईश्वर उसी जल के समान है।
प्रत्येक वर्तन में भगवान् का दर्शन उस वर्तन के आकार के अनुसार होता है। फिरभी सब जगह एक ही तत्व है। वह घट-घट में विराजमान है।