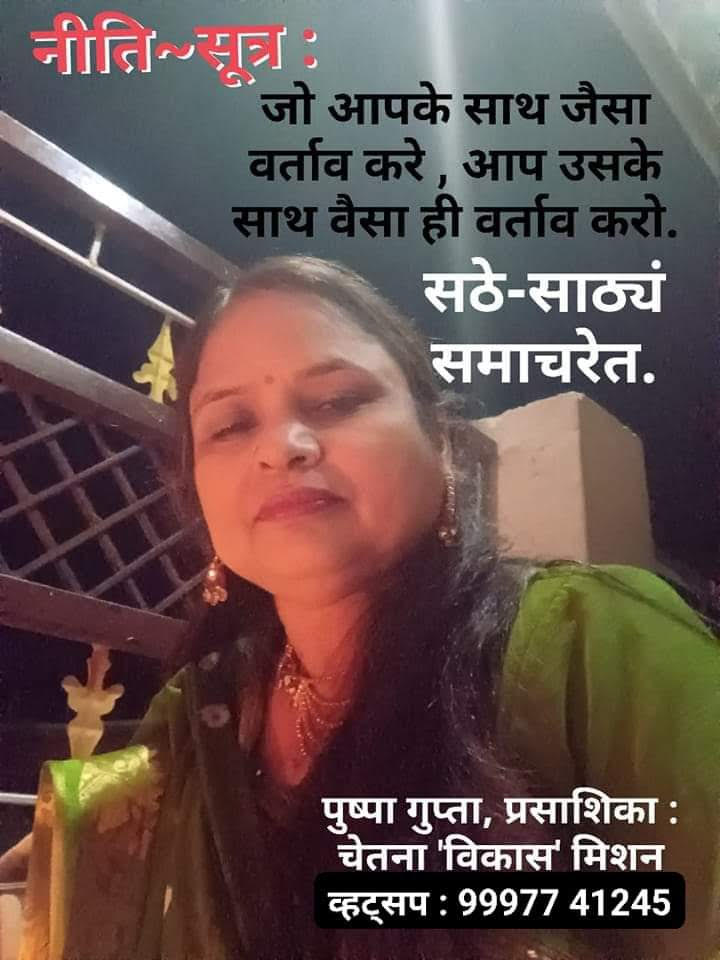पुष्पा गुप्ता
देवासुर संघर्ष आरंभिक अवस्था में वर्ग संघर्ष न था, वर्णसंघर्ष तो हो ही न सकता था। यह यथास्थित और परिवर्तन के बीच टकराव था।
परिवर्तन की सूझ और इस दिशा में पहल असुर या साध्यदेव युग में कुछ गिनती के लोगों में ही हो सकता था। उन्हीं के लिए देव और बरम शब्दों का प्रयोग होने लगा। संज्ञाएं प्रायः दूसरों के द्वारा दी जाती हैं।
इनके प्रचलित हो जाने पर, इसे वह व्यक्ति या समुदाय भी स्वीकार कर लेता है, जिसे यह नाम दिया जाता है। इसकी प्रकृति को समझने के लिए पुनः भाषा की ओर मुड़ें । यद्यपि यह शब्दावली भी उस काल से कई हजार साल बाद के साहित्य से ली गई है, परंतु इससे वस्तु-स्थिति का जितना विश्वसनीय चित्र उभरता है वह वाचिक परंपरा की शक्ति को प्रकट करता है।
देव असुरों को बलवान/ असाधारण पराक्रमी (वल, *बलीयान, असुर), घमंडी (मन्यमान), निकम्मा (अकर्मा), उत्पादन विरोधी (असुर) परिरक्षणवादी (रक्ष), अकिंचन (अनप्न/ अराध), द्रोही (द्रुह/ अभिद्रुह), द्वेषी(द्विष, द्वेषधत्त, ब्रह्मद्विष), खोटी नीयत वाला (अघशंस), हिंसक (जघ्नु, रिष, हंता, धूर्त), आतताई (तायु), लुटेरा (परिपंथी), दरिंदा (वृक), पापी (पाप,अघ), बिगड़ैल (दुःशेव), अभिशस्ति (कटुभाषी, हिंसक), मिथ्याभाषी/ मिथ्याचारी (अनृत), अधातुर/ रूखा सूखा कुछ भी खाने को तैयार/ नरभक्षी (अत्रि), मूढ़ (मूर, अचित), दमनकारी, सताने वाला (दास), लुटेरा (दस्यु ), बाधा डालने वाला (परिबाध), मायावी (मायिन्), जातुधान (यातु), चोर (मुषीवान्), घुमक्कड़ (निरामिण, अहि), अपराधी (अंह), निर्लज्ज (अहृयाण), कुटिल कुचाली (हुरश्चित) वैदिक देवताओं से भिन्न देवों को मानने वाले (अन्यदेव), निंदक (निद, देवनिद) इन्द्र विरोधी (अनीन्द्र), विष्णुद्रोही/यज्ञद्रोही (मखनाशन > हता मखं न भृगवः > का रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात), कच्चा मांस खाने वाला (क्रव्याद), घोरचक्षु, अनवायं, पिशुन (किमीदिन), निशाचर, अंधेरे में रहने/ बढ़ने वाले (कृष्णयोनि, तमोवृध), दुष्कर्मी (दुष्कृत) ।
इनमें से कोई भी शब्द उनकी दीनता, हीनता, पराभव का सूचक नहीं है। पिछड़ेपन, उपद्रवी प्रकृति, मनमानेपन और वैदिक समाज के मानकों पर आपराधिक प्रवृत्ति का द्योतक अवश्य है।
वैदिक समाज इनके ऐसे गुणों में भी दोष देखता था (दानव, दानु, दनुज) जिनका अपने और अपनों के संदर्भ में गौरव मानता था जैसे दानशीलता (सुदानु औशिज; आदित्या रुद्रा वसवो सुदानव) । उनसे देव समाज स्वयं डरा रहता था (सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । ऋ. 1.11.2) और कामना करता था कि उनसे सामना न हो (अप त्यं परिपंथिनं)।
वे अन्यदेव थे, किन्हीं दूसरे आराध्यों – रुद्र, वरुण, मातृ देवियों-, आदि शक्तियों में आस्था रखते थे। परंतु उनके प्रति भयमिश्रित आस्था कृषिकर्मी भी रखते थे और उन्होंने आगे चल कर उन्हें अपने देव समाज में सहयोगी बना कर मिला भी लिया था, परन्तु उन्नत अर्थतंत्र के आराध्यों से पिछड़ा और इसलिए सहयोगी और सेवक बना कर समायोजित किया था। रुद्र जो कृषि पूर्व के प्रभंजन या टारनेडो का मानवीकरण हैं, वह प्रचंड वृष्टि, तड़ित. और वायुवेग का मिश्रित मानवीकरण है, पर साथ ही जीवन दाता जल का भी मानवीकरण है।
यह मनुष्य, पशु, प्रकृति में भेद नहीं करता। विनाशकारी शक्ति है, पर साथ ही इससे वर्षा होती है इसलिए यह जीवन दाता (जलाषभेषज) भी है। इसकी सबसे सुथरी छवि पहले मंडल के 43वें सूक्त की कुछ ऋचाओं में मिलता है:
*गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषभेषजम्। तच्छंयोः सुम्नमीम।। यः शुक्र इव सूर्या हिरण्यमिव रोचते। श्रेष्ठो देवानां वसुः।। शं नो करत्यर्वते सुगं मेषाय मेष्ये। नृभ्यो नारिभ्यो गवे।।*
(1.43.4-6)
जिस तरह देव असुरों की निंदा करते थे उसी तरह असुर/ राक्षस देवों की निंदा करते थे, इसका हमें पता चलता है, पर निंदा के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया जाता था, या क्या आरोप लगाए जाते थे, इसका पता नहीं चल पाता। उनका सबसे बड़ा अभियोग था कि देव, बरम (ब्राह्मण) उन उपयोगी वनस्पतियों को आग लगा कर नष्ट करते है जिनके फल-फूल. बेर, कंद और साग से सबका भरण होता है।
इसलिए संभव है ‘आग लगाने वाला’ अर्थात् देव और बरम, भर्त्सना के रूप में असुरों ने प्रयोग करना आरंभ किया जो इनकी संज्ञा बन गई और ब्राह्मण स्वयं आग होने का दावा करने लगे :
*यो हि अग्निः स द्विजः विप्रैः मन्त्रदर्शिभिरुच्यते।*
(मनु 3.212).
आग के दूसरे गुण – प्रकाश, ज्ञान और प्रकाश पिंडों, ग्रहों, नक्षत्रों से साधर्म्य के आघार पर महिमा मंडन आसान था। असुर और उनके आराध्य देवों से शत्रुता नहीं रखते थे। वे यज्ञ में बाधा डालते थे, उसका ध्वंस करते है। रुद्र के गण दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस करते हैं, दक्ष को क्षति नहीं पहुंचाते।
कथा में भले दक्ष को कर्मकांडीय यज्ञ करते दिखाया गया हो, यह बुद्धिमानों द्वारा प्रजापालन का नया तरीका था। असुरों को मूर, अचित, मूरदेव कहते हैं तो दक्ष प्रजापति का आशय समझा जा सकता है। वह कृषि की ओर अग्रसर समुदाय के प्रतीक हैं, न कि व्यक्ति विशेष।
देव अपने लिए जिन विशेषणों का या अपने जिन गुणों पर गर्व करते हैं वह है श्रम, तप, व्रत, जागरूकता। जिन लोगों ने यज्ञ का कृषिकर्म त्याग कर कृषि की नकल को कृषि से भी श्रेयस्कर बताने वालों ने समूची उर्वरा भूमि (पृथिवी) को वेदी में समेट लिया और पुरानी व्यवस्था को बदल दिया (क्व ऋतं पूर्व्यं गतं) और करिश्माई यज्ञ (उत्पादन) करने करने लगे।
पुराने यज्ञ से तो केवल अनाज पैदा हो सकता था, ये अपने यज्ञ से संतान भी पैदा करा सकते थे, किसी का अनिष्ट भी कर सकते थे। इसी तरह इन्होंने श्रम, तप, व्रत का भी अर्थ बदल दिया। पहले किसान तपती धूप में तपता हुुआ, हाड़ बजाने वाली ठंढ सर्दी में ठिठुरता और बरसात में भीगता और जंगली जानवरों को भगाता हुआ श्रम और तप कर रहा था।
अपने अडिग संकल्प (व्रत) के कारण जान जोखिम में डाल कर खेती कर रहा था। यह समझाने पर भी समझ में न आएगा क्योंकि समझने का अर्थ है मनोगत रूप में ही सही, उन अनुभवों से गुजरना। इसमें हम थोड़ी सहायता ही कर सकते है।
जगह जगह से प्रताड़ित होते रहने के बाद देवों ने पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र को चुना था जहां से उन्हें कोई भगा न सका। कौसानी के रास्ते में हमें उन सीढ़ीदार खेतों के दर्शन निकट से हुए जिन्हें पहाड़ी जंगल झाड़ और काट-जला कर, पहाड़ को तराश सीढ़ी नुमा कियारे – केदार (धान के खेत)- बनाते हुए तलहटी से चोटी तक तैयार किया गया था जिन पर उन्होंने अपनी बस्ती बसाई थी।
उस चरण पर जब धातु का आविष्कार यदि इस असाधारण श्रम को याद करें तो उस महान साधना और सिद्धि का पृथु या पृथी (विस्तार करने वाले, समतल बनाने वाले), जो भी इस अभियान के प्रतीकपुरुष हैं, के इस विधान को समझा जा सकेगा कि जिस क्षेत्र को जिस व्यक्ति ने तैयार किया है उस पर उसका शाश्वत अधिकार है, जैसे शिकार पर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसके बाण से वह मारा गया हो :
*पृथोः अपि इमां पृथिवीं भार्या पूर्वविदो विदुः। स्थाणुच्छेदस्य केदारं आहुः शल्यवतो मृगम्।।*
(मनु 9.44).
इसी धारणा पर यह दावा आधारित है कि यह समस्त पृथ्वी ब्राह्मण की है, उसी की कृपा से सभी का भरण पोषण होता है। क्योंकि किसानी की ओर पहल करने वालों को बरम (ब्राह्मण) और देव कहा जाता था।
अपने को भूदेव आदि कहने के पीछे भी किसी तरह की धूर्तता नहीं है, नासमझी अवश्य है, क्योंकि इसका जाति से संबंध ही न था। इसका सीधा अर्थ था आग लगाने वाला, लुतरा/लुत्ती लगाने वाला जो अपशब्द था। आज भी चुगली करने और फूट डालने के लिए आग लगाने का मुहावरा काम आता है।
जिस कृषक का आंतरिक कार्यविभाजन तीन वर्णों में हुआ उसके लिए विश (स्थायी निवास करने वाले, समाज) – देवानां विशः, विशे जनाय, तां ई विशः न राजानं वृणाना , तस्मै विशः स्वमेवा नमन्ते यस्मिन् ब्रह्मा राजनि पूर्व एति ।। कृष्टी/ चर्षणी (किसान) परि कृष्टीनां रथ्यं रयीणां , यह रोचक है कि किसान का अर्थ भी श्रेष्ठ था (अयुजो असमो नृभिर् एकः कृष्टीरयास्यः), जैसे आर्य – अर/हलधर का अर्थ भी अर्य या पूज्य था , जन- जनिता (पैदा या उत्पादन करने वाला) यज्ञियासः पञ्च जना , कहा जाता था।
यह प्रयोग ऋग्वेद काल तक जारी रहा इसे हम पीछे के उदाहरणों से देख आए हैं। केवल इतना ध्यान रखना होगा कि ऋग्वेद में भाषा का कच्चा-पक्का प्रयोग किया जाता है, इसलिए त्रि, पंच, सप्त, दश, शत और सहस्र का प्रयोग एक ओर तो समग्र/ विश्व के आशय में होता है और दूसरी ओर इनके गणना मान के रूप में, इसलिए यज्ञियासः पञ्च जना का अर्थ हुआ कृषिकर्म में लगे हुए समस्त जन।
इसकी ओर सायण का ध्यान नहीं गया इसलिए वह इसकी व्याख्या वर्णवादी सीमा करने का प्रयास करते हैं।
पर हमारी समस्या यह है कि वे कौन थे जिन्होने कार्यविभाजन को जाति मे बदल दिया, खेत को वेदी में बदल दिया, उत्पादक श्रम, तप, व्रत को अनुत्पादक साधना, पंचाग्नि सेवन, निर्वस्त्र हो कर हिमानी पर्यावरण में ध्यानस्थ होने के माध्यम से नई सिद्धियों का अनुत्पादक पर दुष्कर और आत्मपीड़क विकल्प अपनाया पर किसानी के लिए तैयार न हुए। न हुए तो क्यों?
भौतिकवादी समाज अंतर्मुखी कैसे हुआ। हम उस युगांतर के विषय में उस जिज्ञासा को दुहराना चाहते हैं जिसे ऋग्वेद मे इस रूप में पेश किया गया था-
*यज्ञं पृच्छाम्यवमं स तद् दूतो विवोचति।*
*क्व ऋतं पूर्व्यं गतं कस्तद् बिभर्ति नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी।।*
(1.105.4)
मैं उस अवम् (आज की दृष्टि में हेय यज्ञ – उत्पादन कर्म – के विषय में, उसका विवेचन तो अग्निदेव ही कर सकते हैं, पर वह पुरानी व्यवस्था कहां चली गई,. इस नई व्यवस्था का आधार क्या है, धरती आकाश, कोई तो मुझे बताए!