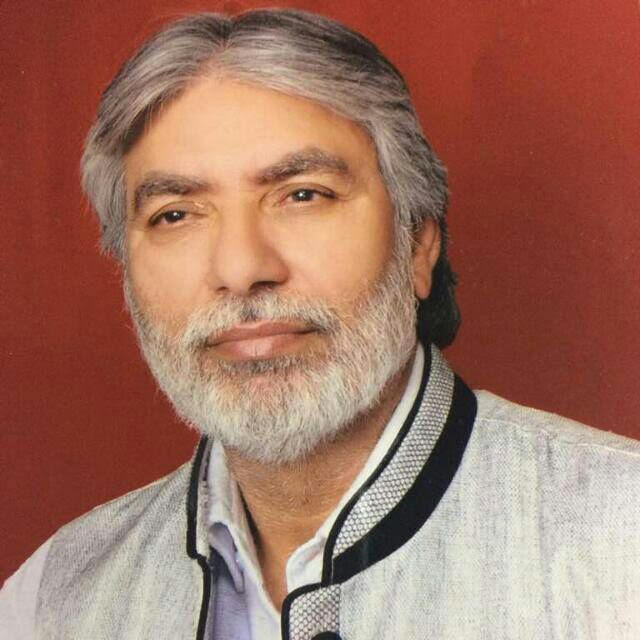रविंद्र सिंह पटवाल
आजादी मिलने के बाद से हम लोकतंत्र और संसदीय राजनीति के जरिये जिस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, उसमें 140 करोड़ भारतीयों की पहचान आज एक भारतीय नागरिक की करीब-करीब खत्म हो चुकी है।
असल में जो खुद को आज भारतीय नागरिक मानते हैं, और इस पर जोर देते हैं वे ही सबसे अलग-थलग पड़े हुए हैं, और उन्हें हर बार मुंह खोलने पर किसी न किसी अस्मिता की पहचान वाले वर्ग के कोप का भाजन बनना पड़ता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने देश और इसके निवासियों को एक ऐसे ओक्टोपसी जकड़न में फांस रखा है, जिसमें वे अपनी खुद की मौत के साथ इस राष्ट्र के भी विखंडित स्वरूप को जन्म दे रहे हैं।
लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे यह धीरे-धीरे एक विषबेल की तरह बढ़ते हुए आज एक आम भारतीय का गला घोंट रहा है, जो अपनी पहचान के साथ जुड़कर हंसते-हंसते खुद को कुर्बान होते देखते हुए भी खुश है? या कहें कि उसके पास अब इस मोहपाश से निकलने का कोई चारा नजर नहीं आता।
किसी मार्क्सवादी के लिए क्लासिकल अर्थों में सामंती या पूंजीवादी समाज वर्गीय आधार पर विभाजित होता है, और असल में यही जमीनी हकीकत भी है। लेकिन इसके साथ ही समाज, पूर्व के सामाजिक विभाजन, जातीय संरचना और पौराणिक गाथाओं से मानसिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उतना ही प्रभावित भी रहता है। और भारत जैसे देश में, जिसने पिछले 72 वर्षों में एक गणतांत्रिक स्वरूप ग्रहण किया, जिसमें संसदीय लोकतंत्र के लिए चुनावी मताधिकार के जरिये चुने हुए प्रतिनिधित्व द्वारा शासन की बागडोर संभालने का अनुभव देखा है, उसने आधुनिक लोकतंत्र और पुरातन स्वरूपों के उन सभी नकारात्मक स्वरूपों को इतनी गहराई से आम जनमानस में गूंथने का काम कर दिया है कि एक आम भारतीय के लिए अपनी पहचान आज एक भारतीय नागरिक के रूप में साफ़-साफ़ समझ पाने के लिए नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं।
नई-नई आजादी मिलने के दौरान हमारी संसद और विधानसभाओं के भीतर वे लोग अधिकाधिक प्रवेश पा सके, जो किसी न किसी स्वरुप में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के हिस्से थे। यह स्वाभाविक भी था कि हर दल और हर राजनेता के पास अपने-अपने स्वतंत्र भारत का सपना था। इसलिए आजादी हासिल होने के कुछ वर्षों तक तो ऐसा लग सकता है कि हमने लंबी-लंबी छलांगें लगाई हैं। इसमें भारत-पाक विभाजन की त्रासदी के बाद भी औपनिवेशिक शासन के द्वारा लुटे पिटे राष्ट्र को एक बार फिर से खड़ा करने का संकल्प दिखता था। राजे-रजवाड़ों, नवाबों का भारतीय राज्य में विलय, भूमि सुधार के जरिये देश के कई हिस्सों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, पाकिस्तान से आये हुए लाखों सिख और हिन्दू शरणार्थियों को बसाने की कवायद जैसी कई बातें हैं, जिसमें राज्य की ओर से सराहनीय प्रयास किये गये।
इसी प्रकार देश में शिक्षा नीति, विज्ञान, उद्योग, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए नियोजित विकास और पंच-वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। समाज के पिछड़े और दलित अनुसूचित वर्ग के उत्थान और सामाजिक आधार पर आरक्षण के जरिये उनके बीच से एक पहचान को मान्यता दी गई।
लेकिन इसके साथ ही नई-नई आजादी के उल्लास के धीमे पड़ते जाने के साथ साथ आंतरिक दृष्टि और उस दृष्टि में अपना और अपनों का विकास ने जोर पकड़ना शुरू किया। कई मामलों में भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में वे बातें रहने दी गईं, जो कभी अंग्रेज अपने शासन को बरकरार रखने के लिए गुलाम भारत के नागरिकों पर आजमाते थे। इसका उपयोग विशेष तौर पर उन आंदोलनों और उसके कार्यकर्ताओं पर किया गया जो शासन द्वारा प्रदत्त धीमी आजादी के बरक्श आज और अभी शोषण से मुक्ति चाहते थे।
उदाहरण के लिए तेभागा और तेलंगाना के किसान आंदोलन को देखा जा सकता है। या इसी तरह केरल में दुनिया के इतिहास में पहली बार चुनी गई किसी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बड़ी तेजी से भूमि सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में किये गए व्यापक सुधारों ने जहाँ एक तरफ नेहरु की कांग्रेस को सकते में डाल दिया, वहीं केरल के भीतर सामाजिक-आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के हाथों से जमीन और मजबूत शिक्षण संस्थान छिन जाने के भय ने नेहरु को राज्य सरकार को भंग करने के लिए प्रेरित किया।
कांग्रेस में भले ही नेहरु अधिकाधिक समाजवादी सोच के जाने जाते रहे हों, और प्रकट रूप में उनकी सरकार द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर औद्योगिक विकास और देश में शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास किये गये, वहीं पर इसके साथ ही साथ प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा सार्वजनिक रूप से धार्मिक मान्यताओं को पहचान दिलाने सहित यूपी में गोविन्द बल्लभ पन्त द्वारा जिलाधिकारी के जरिये बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति को विराजमान जैसे प्रयोग भी नेहरु के शासनकाल में ही हुए थे।
वामपंथी हिस्से के पहले से ही कांग्रेस से अलग होने और इसके साथ ही समाजवादी धारा के लगातार कांग्रेस से टूटकर विभिन्न प्रान्तों में विपक्षी दलों के रूप में अपनी पहचान बनाने के प्रयासों में पहचान की राजनीति को हवा देने का काम शुरूआती दो दशकों में खूब हुआ। दक्षिण में द्रमुक ने पिछड़ों और दलितों के बहुसंख्यक आकार को जिस प्रकार से चुनावी सफलता की गारंटी बना डाला उसने चुनावी जीत की बाध्यता ने कांग्रेस को भी अधिकाधिक ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समुदाय की पहचान से जोड़ दिया, जिसमें ब्राह्मण शासक वर्ग की भूमिका में विराजमान रहा।
समाज की पिछड़ी और दकियानूसी सोच को हवा देने के लिए सिर्फ इन्हीं मुख्य दलों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति तो अभी भी हिंदुत्व की पहचान के साथ एक अखंड हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना लिए आरएसएस का इसमें सबसे बड़ा हाथ था, जिसने इस पूरे काल में उस अवचेतन स्तर पर सोई हुई जातीय श्रेष्ठता, एक अलग धर्म के रूप में मुस्लिम धर्म की कट्टरता, जनसंख्या के विस्फोट, उनके हिंसक होने और हिन्दुओं के जन्मजात धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णुता की कनफुसिया प्रचार के जरिये एक नए बारूदी विस्फोट का आधार देने का काम किया, जो पहले से ही हमारे समाज में विद्यमान थी।
कांग्रेस को लगातार मुस्लिम परस्त साबित करने, वामपंथियों को विदेशी सोच और देश विरोधी बताने के इस सघन कुत्सित अभियान के केंद्र में लगातार हिन्दुओं की झूठी घटती संख्या और धर्मनिरपेक्षता के खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया, जिसने एक स्तर पर पहले से ही आम हिन्दुओं वो चाहे उच्च जाति के हों या पिछड़े वर्ग के, के मन में संदेह, घृणा की विषबेल लगातार पुष्पित पल्लवित होने दी, जिसके लिए बड़े मौके जयप्रकाश नारायण और बाद के दौर में इंदिरा की निरंकुशता ने और अंततः राजीव गांधी के नौसिखिये अवसरवादी राजनीतिक समझ ने प्रदान किये, जिसके बारे में आज देश में सभी को पता है।
आज देश की दो सबसे प्रमुख पार्टियाँ हाशिये पर खड़ी हैं। पहली कांग्रेस और दूसरी वामपंथी पार्टियाँ। एक जिसकी पहचान एक मध्यमार्गी पार्टी के तौर पर थी, जिसमें वाम और दक्षिण धड़े दोनों का ही प्रतिनिधित्व रहता था और दूसरा वाम दल, जो राजनीतिक आजादी के बाद देश में वास्तविक आर्थिक, सामाजिक और समतामूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य से आंदोलनरत था। लेकिन प्रारंभिक चुनावी सफलता के बाद केरल में सरकार के गिरा दिए जाने से उसके भीतर भी संसदीय संघर्ष और गैर संसदीय संघर्ष की लड़ाई में कौन प्रमुख है, को लेकर अवसरवादी और अतिवामपंथी दो धुरियां बन गईं, जिसने अंततोगत्वा भारतीय वामपंथ के पूरे आंदोलन को ही विभ्रम की स्थिति में डाल दिया।
इसके बरक्श आरएसएस ने देश में हिन्दुत्ववादी एजेंडे के साथ मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसके सामने चुनौती के रूप में कोई विचारधारात्मक लड़ाई नहीं बल्कि हिन्दू बनाम पिछड़ा, दलित अस्मिता की क्षेत्रीय पहचानें हैं, जिनके पास कोई राष्ट्रीय सरोकार की जगह क्षेत्रीय क्षत्रप बनने की लालसा और उसमें भी अगुआ तबके के पिछड़े और दलित जातियों का बोलबाला बना हुआ है, जो जब-तब हिंदुत्व की बोगी में सवार होने और उतरने के क्रम में शामिल रहता है।
89 के मंडल-कमंडल के दौर के बाद से भारतीय राजनीति की दशा-दिशा में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है। पिछले तीन दशकों से भारत में भारतीय नागरिकों के आधार पर विकास का कोई मॉडल काम नहीं कर रहा है, और उसका दबाव भी अब चुनावी राजनीति में खत्म हो गया है। इस दौर में जब देश अपनी जातीय पहचान को तलाशने में लगा हुआ था, एकाधिकारवादी पूंजी और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भारत में लूट के लिए नई जमीन तैयार करने के लिए नव उदारवादी आर्थिक स्वरुप के जिस मॉडल को नरसिंहराव की कांग्रेस सरकार ने पेश किया, उस पर भाजपा और कांग्रेस ने कुछ अंतराल के लिए जिस नए मध्य वर्ग और सेवा क्षेत्र के आधार को विकसित कर एक नखलिस्तान का दिवा-स्वप्न पेश किया था, वह 2010 के आते-आते अपने असली स्वरुप में सबके सामने आने लगा है।
आज जहाँ एक तरफ जमीनी स्तर पर सूचना क्रांति के जरिये इन्टरनेट के माध्यम से साइबर हमले के चलते एक भारतीय की पहचान हिन्दू, मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव, दलित की बना दी गई है, यह उसे जमकर तोड़ने और जो कुछ भी थोड़ा-बहुत नेहरू के मॉडल से मिलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां, सस्ता सुलभ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीज, खाद, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और अन्न मिला करता था, उसे देश के 90% सवर्ण, अवर्ण, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक से मरहूम कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए कोई आवाज नहीं गूंजती। जिस प्याज की महंगाई के कारण जनता पार्टी की सरकार गिर गई, उससे आज सैकड़ों गुना जुल्मों-सितम सहकर भी भारतीय समाज के मुंह से आह तक नहीं निकलती।
आज देश के सबसे बड़े भक्षक ही देश के रक्षक के रूप में प्रत्यारोपित कर दिए गए हैं। वे देश की अकूत संपत्तियों को बड़ी तेजी से देश के ही नागरिकों के द्वारा निवेश किये गए बैंकों में जमा अरबों-खरबों रुपये को ऋण या शेयर के जरिये बटोर रहे हैं, बन्दरबांट कर रहे हैं, घाटा दिखाकर कंपनियों को धड़ाधड़ बंद करते जा रहे हैं, विदेशों में सेफ हैवन में ठिकाने लगा रहे हैं और उसमें से ही 40 प्रतिशत को देश में विदेशी निवेश बताकर अपने लिए रेड कार्पेट वेलकम पा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि इस देश को वे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आने वाले तीन दशकों में बनाकर दिखाने वाले हैं।
राजनीतिक दल उनके लिए भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ा रिस्क टेकर बताते उनकी जीभ में ऐंठन भी नहीं होती, क्योंकि भारतीय नागरिक संसदीय चुनावी दलदल में एक नागरिक अधिकार संपन्न भारतीय की जगह बजबजाता हुआ कीड़ा बनकर रह गया है, जो सिर्फ अपनी जातीय भावनाओं से आहत होता है। उसे अपनी निजता की सुरक्षा, अपने संवैधानिक अधिकार, संसद, तमाम आधिकारिक तंत्र (सीबीआई, ईडी, सीएजी, लोकपाल), न्यायपालिका और प्रेस की स्वतंत्रता पर वाजिब और गंभीर सवाल खड़े करने के लिए किसी ने तैयार ही नहीं किया इस बीच में।
लेकिन इसी बीच में भारत के किसान आंदोलन ने, जो इस संकट को पिछले चार दशकों से झेल रहा था, ने बड़ी खूबसूरती से एक बड़ी ताकत के रूप में सामने ला खड़ा कर दिया है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। आज सत्ता ने उन्हें जिस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है, उससे वे अपनी पहचान के आगे जाट, सिख, हिन्दू, मुस्लिम की जगह पर किसान को प्राथमिकता देने के लिए विवश हुए हैं। इस ताकत ने ही उन्हें करीब एक साल से टिका रखा है, वरना इस निरंकुश सरकार ने हर आन्दोलन और पार्टी को उनकी ही कमियों के आधार पर बुरी तरह से मुंह की खाने के लिए विवश कर दिया था।
आज किसान खुद को 65% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखने की कोशिश कर रहा है। उसकी लड़ाई किसी छद्म हिंदुत्व से नहीं बल्कि विश्व के बड़े इजारदारे घरानों, विश्व बैंक, अमेरिका और उनके भारतीय दलालों से है जो आज पूरे भारत के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र के ढाँचे को चट करने के साथ-साथ भारतीय कृषि पर कब्जा कर खुदरा व्यापार को भी कब्जे में लेकर न सिर्फ करोड़ों ग्रामीण आबादी को घुटने-घुटने पर लाने का इरादा रखते हैं, बल्कि एक करोड़ खुदरा व्यापारियों को भी उनका हरकारा बनने के लिए अपने आप मजबूर कर देने का इरादा रखते हैं। आज किसान आन्दोलन न सिर्फ अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि वह शहरी निम्न एवं गरीब तबके की दो जून की रोटी की लड़ाई अपरोक्ष रूप से लड़ रहा है।
चुनावी गणित के पासे में बड़ी पूंजी ने जो बाजी पूरी तरह से भारतीय नागरिक के लिए उलट कर रख दी है, उसे विफल बनाने के लिए आज वर्गीय आधार पर किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष ने एक मजबूत आवाज दी है, इसमें यदि व्यापक तादाद में शहरी गरीब, मजदूर, महिला, अल्पसंख्यक और मध्य वर्ग शामिल होता है तो संभव है कि संसदीय राजनीति के इस 72 साल के पतन के बाद उम्मीद की एक नई किरण देश के नागरिकों के सामने आये, जहाँ जाति, समुदाय, लिंग, क्षेत्रीय अस्मिता को बरकरार रखते हुए भी भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान को सर्वोपरि रखकर समानता, बंधुत्व, और आजादी का अनुभव वे भी कर सकें और दूसरे को भी इसकी स्वतन्त्रता देने का खुलापन दिखा सकने में उन्हें संकोच न हो।
रविंद्र सिंह पटवाल स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं