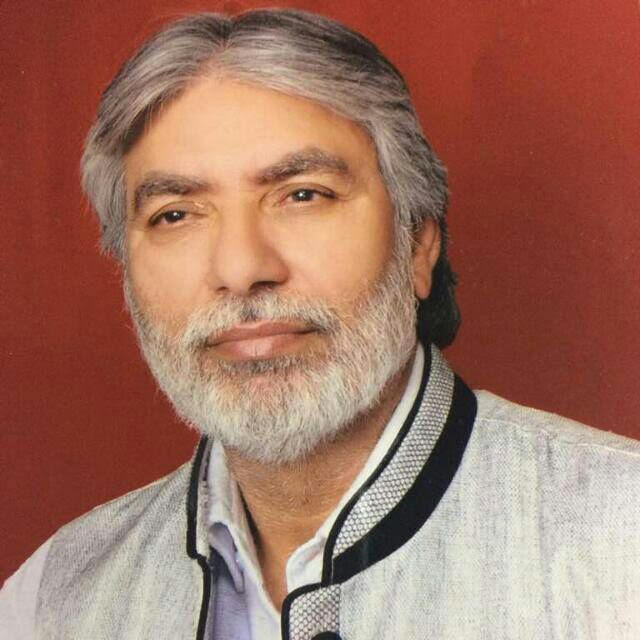राजेन्द्र शर्मा
यह कहने में शायद ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय राजनीति में बाबा युग आ पहुंचा है। एक दिन खबरों में गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर एक और अपेक्षाकृत लंबी रिहाई और उसके दौरान सार्वजनिक आयोजनों में हिस्सेदारी की चर्चा होती है, तो अगले दिन छत्तीसगढ़-मप्र में विशेष रूप से सक्रिय बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जैसे किसी तेजी से उभरते, नये बाबा के कारनामों की चर्चा होती है। उसके अगले दिन शासन द्वारा अनुमोदित, पोषित जग्गी वासुदेव जैसे किसी सद्गुरु के किसी भव्य सार्वजनिक आयोजन की चर्चा होती है, तो इसी बीच स्थानीय ख्याति के किंतु विवाद में लोकप्रियता खोजने वाले किसी बाबा के, किसी की ‘धर्म/जाति-द्रोही’ की जीभ काटकर लाने वालेे के लिए लाखों-करोड़ों रुपए के ईनाम के ऐलानों या अल्पसंख्यकों के कत्लेआम के आह्वानों, की खबरें आने लगती हैं।
बेशक, इन बाबाओं में भारी भिन्नताएं हैं। मोटे तौर पर कम से कम तीन-चार ढीली-ढाली श्रेणियां तो आसानी से बनाई ही सकती हैं। इनमें एक श्रेणी तो राम रहीम, आसाराम बापू, रामपाल, प्रज्ञा ठाकुर आदि से लेकर, पिछले ही महीने अपने मठ में बच्चियों के यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किए गए कर्नाटक के एक मठ के स्वामी तक, ऐसे साधु वेशधारियों की ही बनाई जा सकती है, जो आपराधिक मामलों के लिए सजा काट रहे हैं या मुकदमों का सामना कर रहे हैं। बेशक, यह श्रेणी खासी भीड़-भाड़ वाली है। फिर भी, इसकी याद दिलाने का मकसद कम से कम यह इशारा करना नहीं है कि साधु-वेशधारी सब ऐसे ही ठग या अपराधी ही होते हैं। हां! इस वेश के ऐसे दुरुपयोग की संभावनाओं के संबंध में और सबसे बढ़कर इसके परजीवियों की ओट बन सकने के संबंध में, हिंदीभाषी समाज बहुत पहले से सचेत रहा है। ‘नारि मुई, घर संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भये सन्यासी’ जैसी लोकोक्तियां, इसी सहज-सावधानी का तकाजा करती हैं।
कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे भगवावेशधारियों का कानून के सामने अभियुक्त बनना तथा उनका सजा तक पहुंचना भी, विरले ही कभी हो पाता है और हरेक मामले में इसके लिए उनकी जघन्यता के शिकार हुए लोगों के तथा पत्रकारों के, बहुत लंबे तथा कठिन संघर्ष और राजनीतिक-न्यायिक व्यवस्था के कई-कई संयोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
राम रहीम तथा आसाराम बापू इसके खास उदाहरण हैं। यानी जो मामले इस तरह उजागर होते हैं, वे तो सिर्फ पानी में तैरते हिमखंड की ऊपर से दिखाई देने वाली चोटी भर हैं। बेशक, यह सब नया हर्गिज नहीं है। लेकिन, इन भगवाधारी अपराधियों के लिए सत्ता के संरक्षण की दीदादिलेरी और इसलिए इनकी खुद को सभी नियम-कानूनों से ऊपर मानने की बढ़ती हेकड़ी जरूर नई है। और इससे भी ज्यादा नई है इस श्रेणी के संबंध में खासतौर पर गौर करने वाली एक और बात, और वह यह कि विभिन्न स्तरों पर, इन सभी धर्मगुरु पद के दावेदारों का, सत्ता के साथ जो परस्पर उपयोगिता का संबंध रहा है, उसमें देश के कानून के अंतर्गत उन्हें सजा मिलने या उनके अभियुक्त होने से, शायद ही कोई अंतर पड़ता है।
उल्टे सत्ताधारियों के सामने उनकी सौदेबाजी की ताकत कुछ कमजोर पड़ने से, अब उनका राजनीतिक उपयोग और ज्यादा खुलकर होने लगता है। राम-रहीम का हरियाणा-पंजाब में उपचुनावों तक में सत्ताधारियों द्वारा खुलेआम इस्तेमाल, इसी का साक्ष्य है। रामपाल जरूर अपने विशेष सामाजिक समर्थक आधार के चलते, इसका अपवाद हो सकता है।
एक और श्रेणी में हम यती नरसिम्हानंद, साध्वी शकुन पांडे, बजरंग मुनि, कालीचरण जैसे भगवावेशधारियों की विशाल और मौजूदा शासकों के आशीर्वाद व अनुमोदन से पिछले करीब एक दशक में जबर्दस्त तेजी से बढ़ी तथा ज्यादा से ज्यादा उग्र होती जाती फौज को रख सकते हैं। यह बढ़ती फौज, साधुओं के अखाड़ों तथा गद्दियों के परंपरागत फिर भी बढ़ते ताने-बाने के बीच, विहिप समेत आरएसएस नियंत्रित संगठनों व शासन के प्रभाव से धीरे-धीरे बढ़ती हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक गोलबंदी से भिन्न, एक दबाव समूह का काम कर रही है। यह दबाव समूह हिंदू धार्मिकता की पूरी संकल्पना को ही, सांप्रदायिक उग्रता और खासतौर पर मुस्लिम द्वेष की ओर धकेल रहा है। यह श्रेणी वर्तमान सत्ताधारी राजनीति का हाशिया ही बनाती है। हाशिया से आशय यह कि उसके द्वारा पोषित, संरक्षित होते हुए भी, जरा सी सुरक्षित दूरी से पोषित, संरक्षित है, जो इन भगवाधारियों को उग्रता की कुछ अधिक स्वायत्तता देता है और सत्ताधारियों को, उनके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी से इंकार करने की छूट।
जाहिर है कि एक तीसरी श्रेणी परंपरागत अखाड़ों व गद्दियों से जुड़े बाबाओं की ही है, जो अपनी धार्मिक आस्थाओं के हिंदुत्ववादी सांप्रदायीकरण से बहुत खुश चाहे न हों, पर अनेकानेक कारणों से, जिनमें सत्ता से नजदीकी से हासिल होने वाले अतिरिक्त प्रभाव से लेकर, हिंदू धार्मिक प्रतीकों के बढ़ते बोलबाले से हासिल होने वाला अतिरिक्त महत्व तक शामिल हैं, वे अपने धार्मिक विश्वासों के सांप्रदायीकरण के बुलडोजर का मुकाबला करने में असमर्थ हैं और प्राय: अनिच्छुक भी हैं। वास्तव में, उनके बीच से प्रतिरोध की ऐसी इच्छा के उदाहरण भी ज्यादा से ज्यादा दुर्लभ ही होते गए हैं।
बेशक, रामकृष्ण मिशन जैसे कुछेक सम्मानजनक अपवाद अब भी बचे हुए हैं। दूसरी ओर, आर्य समाज को जिस तरह से हिंदुत्ववादी सांप्रदायीकरण की मुहिम ने पूरी तरह से पचा लिया है, इस मुहिम के बोलबाले का आंखें खोलने वाला उदाहरण है। इस तरह आर्य समाज की सीमित सामाजिक सुधार की ही नहीं, हिंदू श्रेष्ठïता की अपनी दावेदारी की सीमाओं में ही सही, फिर भी धार्मिक सुधार की उसकी सीमित भूमिका के भी पूरी तरह से खत्म कर दिए जाने का, इससे मुखर साक्ष्य क्या होगा कि तथाकथित सनातनी हिंदू परंपरा की मूर्ति पूजा, जातिवादी भेदभाव तथा स्त्री-अधिकारहीनता के काफी उग्र विरोध के आधार पर, स्वामी दयानंद ने, अक्सर शास्त्रार्थ तक पहुंच जाने वाले शास्त्रार्थों के जरिए जिस आर्य समाज को खड़ा किया था, वह पिछली सदी के आखिर तक आते-आते, न सिर्फ विहिप आदि की ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ की मुहिम में बढ़-चढ़कर शामिल हो चुका था, बल्कि अब बाकायदा उसी ‘सनातन धर्म’ का झंडा फहराने वालों में शामिल है, जिसके खिलाफ स्वामी दयानंद ने कभी अपनी ‘पाखंड खंडिनी पताका’ गाड़ी थी।
चौथी और एक आखिरी श्रेणी हम रामदेव, श्री श्री, जग्गी वासुदेव, माता आनंदमयी जैसे उन अत्याधुनिक बाबाओं/ माताओं की बना सकते हैं, जिनका धर्म का कारोबार कारपोरेट तौर-तरीकों से चलता है। वास्तव में यह संयोग ही नहीं है कि इस श्रेणी का एक पांव बाकायदा कारोबार में है यानी मालों के उत्पादन तथा मुनाफा लेकर वितरण में। और जैसे आज देश की सत्ता, हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ताकतों और कारपोरेटों के गठजोड़ के हाथों में है, उसी प्रकार धर्म के ये कारोबारी, वर्तमान सत्ताधारी गठजोड़ का जरूरी हिस्सा हैं।
सत्ताधारी संघ परिवार के धार्मिक मोर्चे के भगवाधारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारकूनों से अलग, जो धर्म के नाम पर सीधे आम लोगों के बीच वर्तमान सत्ता के लिए समर्थन जुटाने का काम करते हैं, यह श्रेणी देश में और विदेश में भी, अपेक्षाकृत संपन्नतर तबके के बीच, उसके लिए अनुमोदन-समर्थन जुटाने का काम करती है। बेशक, रामदेव की जगह इस श्रेणी में भी जरा अलग है, जो कारपोरेट के रूप में आयुर्वेदिक उत्पादों से लेकर, खाद्य सामग्री तथा सौंदर्य प्रसाधनों तक के आम उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने कामयाब रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि बाबाओं का यह उभार, सिर्फ हिंदू धार्मिक परंपरा तक ही सीमित नहीं है। उस पैमाने पर न सही, पर विभिन्न रूपों में यही परिघटना अन्य धार्मिक परंपराओं के मामले में भी देखी जा सकती है। फिर भी सत्ता से जैसा अभिन्न गठजोड़, हिंदू धर्म के नाम लेवा कारपोरेट बाबाओं का है, वैसी स्थिति दूसरी धार्मिक परंपराओं के कारपोरेटनुमा धर्मगुरुओं को हासिल नहीं है।
यह भी याद रहे कि इन श्रेणियों के बीच कोई चीन की दीवार नहीं खिंची हुई है और इनमें काफी आवाजाही चलती रहती है। आदित्यनाथ का देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर जमा होना, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बेशक, उनसे पहले भी उन्हीं की पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक भगवाधारी मुख्यमंत्री का तजुर्बा कर के देखा था। लेकिन, वह तजुर्बा ज्यादा नहीं चला और महिला होने के नाते, भगवावेश के बावजूद उमा भारती की मुख्यमंत्री की पारी काफी कम समय में ही निपट गई। शायद, इसलिए भी कि वह मोदी-पूर्व काल की भाजपा थी, जो शासन का उस तरह खुलेआम हिंदुत्ववादी सांप्रदायीकरण करने में झिझकती थी, जैसा अब नया नार्मल बन चुका है। वैसे उनसे पहले भी देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर कई वर्ष तक एक केसरियाधारी रहा था, जो परंपरागत अर्थों में राजनीतिक नेता भी नहीं था। हमारा इशारा अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एन टी रामाराव की ओर है। पर आदित्यनाथ, उमा भारती आदि से उनकी समानता शायद, भगवा वेश की भारतीय परंपरा से जुड़ी, अतिरिक्त स्वीकार्यता के उपयोग तक ही सीमित है।
दूसरी ओर, आदित्यनाथ एक परंपरागत मठ की धार्मिक परंपरा से, जिसका हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक दिशा में राजनीतिकरण तो उनके गुरु, अवैद्यनाथ के समय में ही हो गया था, सीधे संघ परिवार द्वारा संचालित हिंदुत्ववादी राजनीतिक श्रेणी में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के पैमाने पर विधिवत बाबा राज, यहां से एक प्रकार से एक कदम ही दूर रह जाता है। बेशक, भारत में त्याग की और उसके चिन्ह के रूप में भगवावेश के सम्मान की परंपरा बहुत पुरानी है। ऋषियों-मुनियों के व्यापक सम्मान के अलावा, जिसमें हर प्रकार के राजाओं द्वारा आदर-सम्मान तथा दक्षिणा दिया जाना भी शामिल था, गौतम बुद्घ और एक हद तक अशोक भी, त्याग के लिए सम्मान के अनोखे उदाहरण हैं। लेकिन, वह परंपरा सत्ता से दूरी, उससे स्वतंत्रता, उसके त्याग के, सम्मान की परंपरा है। त्याग के प्रतीक सन्यास का सत्ता तक पहुंचने के लिए उपयोग करने की परंपरा, उस प्राचीन भारतीय परंपरा को सिर के बल खड़ा करना है।
राजनीति में बाबाओं के उभार की यह समूची परिघटना, भारत में इस समय सत्तारूढ़ हिंदुत्व-कारपोरेट-बाबा गठजोड़ का ही परिणाम है। और यह सत्तासीन गठजोड़ खुद, उस नवउदारवादी व्यवस्था का परिणाम है, जो मूलत: एक असमानता बढ़ाने वाली और इसलिए, समाज के विकास को कुंठित तथा बाधित करने वाली व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था को चलते रहने के लिए, बढ़ते पैमाने पर उसी प्रकार धार्मिक वैधता का सहारा चाहिए, जैसे कि मध्यकाल तक के शासकों को इस वैधता के सहारे की जरूरत होती थी। वास्तव में उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन व्यवस्थाओं तथा उनकी जरूरतों से जुड़े वर्तमान चेतना के विकास को देखते हुए तो, उन्हें कथित धार्मिक वैधता के सहारे की और ज्यादा तथा धार्मिक पहचान के आधार पर शत्रुओं को खोजने व उनके खिलाफ युद्घ की मुद्रा में रहने की हद तक, जरूरत होती है। दुनिया भर में इस समय नव-फासीवादी ताकतों का जिस तरह का उभार देखने को मिल रहा है, इसी का सबूत है। आखिरकार, लोगों से भूखे पेट भजन कराना भी आसान तो नहीं ही है।
*(लेखक साप्ताहिक पत्रिका ‘लोक लहर’ के संपादक हैं।)*