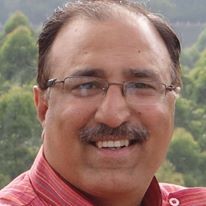जवरीमल्ल पारख
लगभग दो सौ साल के लंबे उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी हासिल हुई। लेकिन इस आज़ादी की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। लाखों-लाख लोग विस्थापित हुए, हजारों-हजार लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गये, औरतें अपमानित हुईं और बच्चे अनाथ हो गये। 1857 में अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों ने जो महाविद्रोह किया उसमें हिंदू और मुसलमान, सवर्ण और दलित, स्त्री और पुरुष सभी ने भाग लिया था। इस महाविद्रोह का चरित्र अखिल भारतीय और बहुवर्गीय था। मेरठ से जो सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए निकले थे उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को अपना शासक घोषित किया था।
लेकिन देश के बहुत से सामंती शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, नतीजा यह हुआ कि इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों की पराजय हुई। अंग्रेज यह जान चुके थे कि यदि हिंदू और मुसलमान एकबद्ध रहेंगे तो भारत पर वे लंबे समय तक शासन नहीं कर पायेंगे। इसी का नतीजा था कि उन्होंने ऐसे कई कदम उठाये जिससे भारत की हिंदू जनता के दिलों में यह बैठाया जा सके कि मुसलमान तुम्हारे भाई नहीं बल्कि शत्रु हैं जिन्होंने लगभग एक हजार साल तक तुम पर शासन किया है। तुम्हारे धर्मस्थलों को तोड़ा है, तुम्हारी औरतों को अपमानित किया है और जबर्दस्ती तुम्हारा धर्म परिवर्तन कराया गया है। मुसलमानों के दिमागों में भी यह बैठाया गया कि तुमने एक हजार साल तक शासन किया है। अगर देश आज़ाद होगा तो हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण तुम्हें गुलामों सा जीवन जीना पड़ेगा।
इतिहास की इस सांप्रदायिक व्याख्या को उन हिंदुओं और मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया जिनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था और जो यह मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और वे कभी एक साथ नहीं रह सकते। यहां इस तथ्य को रेखांकित करने की ज़रूरत है कि केवल मुस्लिम लीग ही नहीं हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन करते थे। जबकि कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, राष्ट्र को धर्म के आधार पर परिभाषित करने के सिद्धांत के विरुद्ध थी। हमारे आज़ादी के आंदोलन का यह आंतरिक संघर्ष था जिसका नतीजा देश के विभाजन में निकला और इसी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से प्रेरित नाथूराम गोडसे के हाथों आज़ादी के आंदोलन के सबसे महान नायक महात्मा गांधी मारे गये। नाथूराम गोडसे का संबंध हिंदू महासभा से भी था और आरएसएस से भी था।
आज़ादी के आंदोलन का दूसरा अंतर्विरोध वर्ण व्यवस्था और जातिवाद था। उन्नीसवीं सदी में समाज सुधार के जो आंदोलन चले उसने जातिवाद पर भी प्रहार किया। राजा राममोहन राय से लेकर विवेकानंद तक ने किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था की मुखालफत की लेकिन जातिवाद पर निर्णायक प्रहार उन समाज सुधारकों और चिंतकों ने किया जो समाज के दलित वर्ग से आये थे। ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर उनमें प्रमुख थे। इन समाजों से आये नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन के नेताओं के सामने यह उचित सवाल रखा कि अगर देश आज़ाद हुआ तो क्या दलितों के साथ वैसा ही अमानवीय व्यवहार होगा जैसा सदियों से होता आया है।
क्या उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। ये ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर आज़ादी के संघर्ष को देना ज़रूरी था। 1932 में अंबेडकर और गांधी के बीच जो समझौता हुआ उसने इस बात को रेखांकित कर दिया कि आज़ाद भारत में दलित समुदायों के साथ सदियों से चला आ रहा अमानुषिक भेदभाव समाप्त किया जाना ही जरूरी नहीं है बल्कि नागरिकता के उन सभी अधिकारों की संवैधानिक गारंटी देनी होगी जिनसे अब तक उन्हें वंचित रखा गया है। आज़ादी के आंदोलन ने इस बात का एहसास भी कराया कि अगर एक समतावादी समाज बनाया जाना है तो जो वर्ग और समुदाय पिछड़े रह गये हैं उनके लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। आरक्षण व्यवस्था उन्हीं में से एक प्रयत्न है।
भारत से अलग होकर जो पाकिस्तान बना उसने एक धार्मिक राज्य बनने का फैसला किया लेकिन भारत ने दूसरा मार्ग चुना। 1946 में जो संविधान सभा गठित की गयी उसमें बी आर अंबेडकर को भी शामिल किया गया और उन्हें उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया जिसका दायित्व संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अंबेडकर आधुनिक विचारों में यकीन करने वाले महान चिंतक थे। गांधी, नेहरू आदि की तरह वे भी धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और समानता में यकीन करते थे। वे भी चाहते थे कि देश के संविधान का आधार धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय हो। इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों पर संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और जिसे विस्तृत बहस के बाद संविधान सभा ने स्वीकार किया।
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत ने अपने को संप्रभु धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। यह भारतीय इतिहास में एक नये युग की शुरुआत थी। जिस संविधान के अंतर्गत भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, उसमें सर्वोच्च सत्ता स्वयं भारत की जनता थी जिसने अपने को यह संविधान प्रदान किया था। संविधान की नज़र में प्रत्येक भारतीय नागरिक चाहे उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी नस्ल, उसकी भाषा कुछ भी क्यों न हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष या वह हिंदुस्तान के किसी भी इलाके का रहने वाला क्यों न हो, सब बराबर थे और सबको समान अधिकार हासिल थे। स्वतंत्रता, समानता और पारस्परिक भाईचारे के सिद्धांत पर इस लोकतांत्रिक गणतंत्र की नींव रखी गयी थी, जिसकी सबसे बड़ी पहचान धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावादी संस्कृति थी।
लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि भारत का संविधान जिन मूल्यों पर टिका था, भारतीय समाज वैसा नहीं था। सामंती और औपनिवेशिक दौर की विकृतियां भारतीय समाज में बहुत गहरे रूप में धंसी हुई थीं। जीवन के हर क्षेत्र में विषमता व्याप्त थी। जाति, धर्म, भाषा, लिंग और क्षेत्र के आधार पर हर स्तर पर भेदभाव व्याप्त था। आर्थिक विषमता के कारण जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जीवन की बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित था। अशिक्षा, अंधविश्वास और असमानता के विरुद्ध हर स्तर पर संघर्ष करने की ज़रूरत थी। यह सिर्फ़ सरकारी आदेशों और नीतियों से ही संभव नहीं था। इसके लिए व्यापक जन अभियान की ज़रूरत थी। यह इसलिए भी ज़रूरी था कि इसी के द्वारा हम एक देश के रूप में अपने को एकजुट रख सकते थे और तरक्की भी कर सकते थे।
1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब राष्ट्र का नवनिर्माण सबसे बड़ा प्रश्न था। उस दौर में इस बात को गहराई से महसूस किया गया था कि शांति, सद्भाव, भाईचारा और पारस्परिक सहयोग द्वारा ही देश का निर्माण और प्रगति संभव है। लेकिन यह भी सच्चाई थी कि नवनिर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाएं और समस्याएं भी कम नहीं थी। दरअसल, आज़ादी के बाद के दो दशकों को हम तभी सही ढंग से समझ सकते हैं जब हम उसे गांधी-नेहरू-अंबेडकर-भगतसिंह विचारधारा के संदर्भ में समझने का प्रयास करें। संविधान निर्माण के संदर्भ में ही नहीं भारत के नवनिर्माण के संदर्भ में भी यह विचारधारा सबसे व्यापक और गहरे असर को दर्शाती है। इन राष्ट्रीय नेताओं के विचार बहुत से मामलों में एक-दूसरे से भिन्न थे, लेकिन वे अपने को लोकतांत्रिक विचारधारा के दायरे में ही बनाये रखते हैं, जिसमें उनका बल एक आधुनिक, उदार, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी समाज बनाने पर है। इस विचारधारा का मुख्य विरोध सांप्रदायिक तत्ववाद और ब्राह्मणवादी मनुवाद से भी था और आज भी है।
आज़ाद भारत में उन्नति और विकास के नये-नये रास्ते खुल रहे थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसा घटित हो रहा था, जो चिंतनीय था, जो भविष्य के प्रति आशंकाएं पैदा कर रहा था। इस दौर का शासक वर्ग चाहता था कि जनता अपनी दयनीय हालत से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग न चुनकर वर्ग सहयोग का मार्ग चुने। वह इस बात को समझे कि उसके पास वोट देने की जो शक्ति है उससे वह ऐसे शासकों को सत्ता पर बिठा सकती हैं जो उनके हितों के प्रति ईमानदार हो और उसकी प्रगति के लिए निष्ठापूर्वक काम करे। लेकिन उन सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो इस बात में यकीन करती थी कि पूंजीवाद से देश की प्रगति मुमकिन है, उन्होंने सत्ता में आने या बने रहने के लिए जाति और धर्म का खुलकर इस्तेमाल किया।
धीरे-धीरे उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जनता के वास्तविक हितों के लिए काम करने की बजाय जाति और धर्म के आधार पर उनके वोट हासिल कर सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। जवाहर लाल नेहरू जैसे नेता जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गहरी आस्था रखते थे और इस खतरे को जानते थे कि आरएसएस और भारतीय जनसंघ जैसे संगठन देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हैं क्योंकि वे बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन हासिल कर लोकतंत्र का खात्मा कर सकते हैं और फासीवादी सत्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन उनका यह विश्वास था कि जनता धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चलते हुए इन सांप्रदायिक संगठनों को कभी इतना ताकतवर नहीं बनने देगी कि वे सत्ता पर काबिज हो सकें। नेहरू यह नहीं देख सके कि स्वयं उनकी पार्टी में ऐसे तत्व काफी बड़ी तादाद में थे जिनकी सोच न केवल दक्षिणपंथी थी बल्कि सांप्रदायिक भी थी।
आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण की चुनौतियां और उसको लेकर उम्मीदों की अभिव्यक्ति नेहरू युग की समाप्ति के साथ-साथ कमजोर पड़ने लगी थी। पूंजीवादी विकास के जिस रास्ते पर देश चल रहा था, उससे भारतीय पूंजीपति वर्ग मजबूत होने लगा था। उसके लिए अब किसी तरह के आदर्शवाद की ज़रूरत नहीं थी। इस बात को धीरे-धीरे भुलाया जा रहा था कि यह आज़ादी कितने लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद हासिल हुई है।
यही नहीं देश को एकजुट रखने के लिए सांप्रदायिक और सवर्णपरस्त जातिवादी पूर्वाग्रहों के विरुद्ध व्यापक संघर्ष करने की ज़रूरत को भी अनदेखा कर दिया गया। संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की जो बात कही गयी वह कभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का अंग नहीं बन सकी। नतीजतन आरएसएस जैसा फासीवादी संगठन जिसे आज़ादी के बाद भी काम करने की छूट दे दी गयी थी, जनता के बीच सांप्रदायिक और जातिवादी ज़हर फैलाने के अपने अभियान को बिना किसी डर के चलाती रही और हिंदू जनता के बीच अपनी जड़ें मजबूत करती गयी। अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने इसको अनदेखा ही रहने दिया।
1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तो उनकी छवि तानाशाह की बन गयी। उस समय देश में जो कुछ भी हो रहा था, उसके लिए वे ही जिम्मेदार लगती थीं। इसलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना लोकतंत्र की रक्षा के लिए ज़रूरी लगता था। इसलिए जब आपातकाल हटाकर कांग्रेस ने चुनाव कराने का फैसला लिया और कांग्रेस को परास्त करने के लिए जब सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर एक पार्टी बनाने पर एकमत हुए तो उनका यह फैसला सही लगा। लेकिन उस समय इस बात की अनदेखी की गयी कि जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ भी शामिल हुई है जिसकी बुनियादी आस्था आरएसएस में है और आरएसएस न लोकतंत्र में यकीन करता है और न संघात्मक गणराज्य (फेडेरल रिपब्लिक) में।
दरअसल 1967-68 से ही कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनसंघ के साथ गठबंधन की शुरुआत कर दी थी। इस तरह एक फासीवादी-मनुवादी संगठन को लोकतांत्रिक वैधता प्रदान कर दी गयी। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में तो आ गयी लेकिन वह ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह सकी। भारतीय जनसंघ भी जनता पार्टी से अलग हो गयी और उसने एक नये नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने को पुनर्गठित कर लिया। लेकिन अल्प समय में सत्ता में रहने का लाभ यह हुआ कि प्रशासन में वह घुसपैठ करने में कामयाब हुई।
1980 में इन्दिरा गांधी की राजसत्ता में वापसी हो गयी लेकिन सांप्रदायिकता के विरुद्ध उसका संघर्ष पहले की अपेक्षा कमजोर पड़ चुका था। 1980 के बाद देश के कई भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए मुरादाबाद, नैली, भागलपुर में हुए दंगे दरअसल दंगे नहीं थे, मुसलमानों का बड़े पैमाने पर नरसंहार था। 1980 के बाद खालिस्तान की मांग करते हुए आतंकवाद की जो लहर उभरी और जिसके कारण पंजाब, दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में निरपराध लोगों पर हमले किये गये। सिख उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और उसे खाली कराने के लिए जो सैनिक कार्रवाई की गयी उस दौरान सैकड़ों निर्दोष लोग भी मारे गये।
इसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गयी। इसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों में पांच हजार लोग मारे गये। हालांकि इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी कामयाबी मिली। लेकिन यह कामयाबी हिंदू प्रतिक्रिया का नतीजा थी। आरएसएस ने इस बात को समझ लिया कि अगर हिंदू जनता को सांप्रदायिक आधार पर भड़काया जाए तो वे भी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। रामजन्म भूमि आंदोलन का मकसद आरएसएस का सत्ता हथियाना था।
कांग्रेस नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा शुरू से ही घोर दक्षिणपंथी ही नहीं था, बल्कि संघ परिवार के साथ सहानुभूति रखने वाला भी था। इसी हिस्से ने 1949 में बाबरी मस्जिद में राम की मूर्तियां रखवाने में भूमिका निभायी थी। इसी ने बाद में शिलान्यास भी करवाया था और बाद में इसी हिस्से ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को होने दिया था। कांग्रेस और भाजपा के बीच फर्क यही था कि कांग्रेस सत्ता में रहने के लिए सांप्रदायिकता के प्रति नरम रुख अपनाती थी, जबकि भाजपा इस देश की धर्मनिरपेक्षता और बहुसांस्कृतिकता की परंपरा को ध्वंस कर बहुसंख्यकवाद पर आधारित ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी।
बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि आंदोलन ने भारतीय राजनीति को निर्णायक रूप से बदल डाला। चुनावों में भाजपा का समर्थन लगातार बढ़ता गया। ज़रूरत इस बात की थी कि अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के विरुद्ध संघर्ष करतीं ताकि जनता के बीच उसके समर्थन को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इसके विपरीत बहुत सी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर अवसर मिलते ही भाजपा के साथ गठबंधन करने में नहीं हिचकिचाती थीं। 1998 में जब पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी तब उसको समर्थन देने वाली कई और पार्टियां भी थीं।
1999 में यह समर्थन और बढ़ा जिसके कारण भाजपा लगातार पांच साल तक केंद्र में सत्तासीन रही। आपातकाल के बाद से वामपंथी पार्टियों की नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से बाहर रखना। लेकिन वे यह नहीं देख पाये कि सत्ता से बाहर रहकर भी सत्ता से नजदीकियों का लाभ भाजपा को लगातार मिलता रहा। शायद इसका कारण यह था कि वे अब भी कांग्रेस और भाजपा का मूल्यांकन एक ही तरह से कर रहे थे। तानाशाही प्रवृत्ति की पार्टी (कांग्रेस) और फासीवाद पार्टी (भाजपा) के बीच के अंतर को वे तब तक नहीं समझ पाये जब तक कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं हो गया।
पिछले तीन दशकों में सांप्रदायिकता के उभार ने देश के माहौल को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभायी है। 6 दिसंबर, 1992 को संविधान को धता बताते हुए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने चार सौ साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मुंबई और दूसरे शहरों में हिंसक कार्रवाइयां हुईं। इन घटनाओं ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा की। जहां भी वे अल्पसंख्यक थे, उन्हें मुख्यधारा से अलगाने की प्रक्रिया तेज हो गयी।
इसकी प्रतिक्रिया भी हुई। इसी दौरान कश्मीर के हालात बिगड़ते चले गये। कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में आतंकवादी कार्रवाइयां बढ़ गयीं। 2002 में गोधरा की घटना और उसके बाद गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार ने हालात को और अधिक बिगाड़ा जिसका पूरा लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार ताकतवर होती गयी और नतीजतन 2014 से यह पार्टी एक बार फिर से केंद्र में सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने का अर्थ केवल एक सांप्रदायिक पार्टी का मजबूत होना ही नहीं है। वह एक ब्राह्मणवादी-मनुवादी पार्टी भी है जो संविधान प्रदत्त समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करती।
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह दौर आज़ादी के बाद का सबसे संकटपूर्ण और चुनौती भरा दौर है। धर्म के नाम पर जिस तरह एक पूरे वर्ग को देश के दुश्मन की तरह पेश किया जा रहा है और उन्हें संविधान में मिले नागरिक अधिकारों से वंचित कर उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक में तब्दील किया जा रहा है, वह इस राजसत्ता के फ़ासीवादी चरित्र का ही प्रमाण है। भारत का यह फ़ासीवाद अपने चरित्र में अतिदक्षिणपंथी भी है और ब्राह्मणवादी भी। मौजूदा राजसत्ता के विरुद्ध संघर्ष उन सब भारतीयों का कर्त्तव्य है जो भारतीय संविधान में यक़ीन करते हैं और जो भारत की बहुविध धार्मिक, जातीय, भाषायी और सांस्कृतिक परंपरा को बचाये रखना चाहते हैं क्योंकि असली भारत इसी परंपरा में निहित है जिसे हिंदुत्वपरस्त ताक़तें ख़त्म करना चाहती हैं।
मौजूदा राजसत्ता के चरित्र को समझने के लिए आरएसएस की विचारधारा को समझना जरूरी है। वे अपनी राजनीतिक विचारधारा को हिंदुत्व नाम देते हैं। यह विचारधारा उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर से ग्रहण की थी जिन्होंने 1923 में ‘हिंदुत्व’ नामक पुस्तक लिखी थी। आरएसएस ने अपने इन राजनीतिक उद्देश्यों को कभी छुपाया नहीं। इस संगठन के दूसरे सरसंघचालक एम एस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक ‘वी ऑर अवर नेशनहुड’ में जो विचार पेश किये उसके पीछे फासीवाद और नाज़ीवाद का प्रभाव भी था। इस पुस्तक में गोलवलकर यह प्रश्न उठाते हैं कि ‘अगर निर्विवाद रूप से हिंदुस्थान हिंदुओं की भूमि है और केवल हिंदुओं ही के फलने-फूलने के लिए है, तो उन सभी लोगों की नियति क्या होनी चाहिए जो इस धरती पर रह रहे हैं, परंतु हिंदू धर्म, नस्ल और संस्कृति से संबंध नहीं रखते’ (गोलवलकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा : एक आलोचनात्मक समीक्षा, शम्सुल इस्लाम, फारोस, नयी दिल्ली, पृ. 199)।
स्वयं द्वारा उठाये इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे लिखते हैं कि ‘वे सभी जो इस विचार की परिधि से बाहर हैं, राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं रख सकते। वे राष्ट्र का अंग केवल तभी बन सकते हैं जब अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें। राष्ट्र का धर्म, इसकी भाषा एवं संस्कृति अपना लें और खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें। जब तक वे अपने नस्ली, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अंतरों को बनाये रखते हैं, वे केवल विदेशी हो सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रति मित्रवत हो सकते हैं या शत्रुवत’ (वही, 199)। गोलवलकर की इन बातों का अर्थ यही है कि भारत केवल हिंदुओं का राष्ट्र है और बाकी सभी धार्मिक और नस्ली समुदाय विदेशी हैं। वे भारत में रह सकते हैं लेकिन जब वे ‘अपने विभेदों को पूरी तरह समाप्त कर दें’ और ‘खुद को पूरी तरह राष्ट्रीय नस्ल में समाहित कर दें’।
अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि ‘अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें राष्ट्र के रहमो-करम पर, सभी संहिताओं और परंपराओं से बंधकर केवल एक बाहरी की तरह रहना होगा, जिनको किसी अधिकार या सुविधा की तो छोड़िए, किसी विशेष संरक्षण का भी हक़ नहीं होगा’ (वही, पृ. 201-202)। अगर वे अपने को राष्ट्रीय नस्ल में समाहित नहीं करते हैं तो ‘जब तक राष्ट्रीय नस्ल उन्हें अनुमति दे वे यहां उसकी दया पर रहें और राष्ट्रीय नस्ल की इच्छा पर यह देश छोड़कर चले जाएं’। स्पष्ट है कि आरएसएस के अनुसार हिंदू राष्ट्र में गैर हिंदुओं विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को नागरिकता के वे अधिकार नहीं मिल सकते जो हिंदुओं को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होंगे। यानी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। यह संयोग नहीं है कि आरएसएस ने अपनी प्रेरणा फासीवाद और नाजीवाद से ग्रहण की है। इस पुस्तक में गोलवलकर ने अल्पसंख्यकों के प्रति जर्मनी और इटली ने जो रवैया अपनाया, उसकी न केवल प्रशंसा की बल्कि उसे अनुकरणीय भी माना।
(जवरीमल्ल पारख रिटायर्ड प्रोफेसर हैं।)