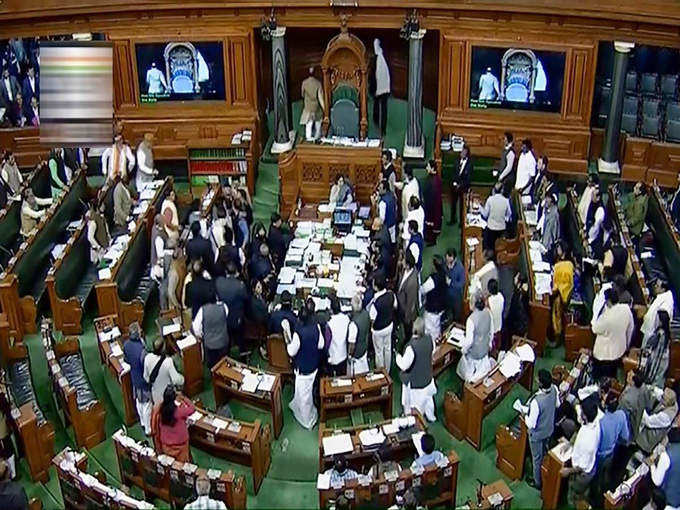उद्योग और रासायनिक उद्योगों के व्यापार समूह यूनियन कार्बाइड के पीछे लामबंद हुए। आपदा के बाद के वर्षों में भी यूनियन कार्बाइड के सीईओ को तत्कालीन अमेरिकन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसका नाम बदल दिया गया है। उस वक्त पूरे उद्योग की ताकत और सुरक्षा का बचाव करने की भावना काम कर रही थी। दूसरी ओर, अकादमिक इंजीनियरों और औद्योगिक इंजीनियरों ने यूनियन कार्बाइड के इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया कि किसी असंतुष्ट कामगार द्वारा भंडारण टैंक में पानी डाल दिए जाने से रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई और नतीजतन गैस का रिसाव हुआ। मुझे याद है कि मैंने एक अकादमिक सम्मेलन की रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें यूनियन कार्बाइड ने ये किस्सा बयां करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। इस त्रासदी के चलते कंपनी के कुछ कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं के बारे में बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। हालांकि आपको यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेने का वादा किया था। जमीन पर ये निश्चित रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। याद रखें कि यह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेजी का शुरुआती दौर भी था। जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि ये उद्योग कितने जोखिम भरे हैं, उन्होंने सुरक्षित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने की छवि बनाने के लिए अपने निवेश में बढ़ोतरी कर दी।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन के मानवविज्ञान विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष किम फॉर्चून ने 2001 में प्रकाशित अपनी किताब “एडवोकेसी आफ्टर भोपाल: एनवायरमेंट्लिज्म, डिजास्टर, न्यू ग्लोबल ऑर्डर्स” में आपदा के बाद के परिणामों के बारे में बताया है। यह पुस्तक 1984 में गैस रिसाव के वर्षों बाद 90 के दशक की शुरुआत में भोपाल में हुई घटनाओं का ब्योरा देती है। रोहिणी कृष्णमृूर्ति ने फॉर्चून से भारत में उनके अनुभवों और इस आपदा द्वारा भारत में पर्यावरणवाद को आकार दिए जाने के बारे में बातचीत की है

आपने भोपाल गैस त्रासदी के कुछ साल बाद 1990 और 1992 के बीच भारत में जमीनी स्तर पर कार्य किया। भोपाल में जनता का मूड क्या था?
शुरुआती तौर में मैं तमिलनाडु में शोध करने के मकसद से भारत गई थी और तब मेरी सोच थी कि भोपाल त्रासदी मेरे काम का मुख्य फोकस न होकर पृष्ठभूमि में रहेगी। लेकिन जब मैंने मामले के मूल निपटारे (सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1989 में भोपाल के सभी मुकदमों के अंतिम निपटारे का निर्देश दिया था, जो 47 करोड़ डॉलर की राशि के बराबर था) के तुरंत बाद भोपाल का दौरा किया तो वहां आक्रोश और डर का माहौल था। उस समय गैस पीड़ितों को अंतरिम राहत राशि तक नहीं मिल पा रही थी।
वो बहुत तात्कालिक और दुखद समय था। अपने शोध के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं अंग्रेजी भाषा में लेखन में मदद करके आंदोलन की सेवा कर सकती हूं, क्योंकि अदालत की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती थी। मैंने भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, महिला संगठन (भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन या भोपाल गैस प्रभावित कामकाजी महिला संघ) और आपदा के बारे में अपना खुद का ब्योरा लिखने वाले यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के एक बहुत ही मुखर कार्यकर्ता, दोनों के साथ काम किया। मैंने उनकी लेखनी का अंग्रेजी अनुवाद करने में मदद की। उन्होंने मुझे तकनीकी ब्योरे के साथ वास्तव में वहां घटित घटनाओं को समझने का गुर सिखाया। उस समय भोपाल में तमाम तरह के काम हो रहे थे। एक काम, पीड़ितों को अंतरिम राहत का भुगतान दिलाने पर चल रहा था, जो बेहद जरूरी था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मामले की सुनवाई के लिए अब भी कुछ प्रयास किए जा रहे थे।
भोपाल में जमीनी स्तर के आंदोलन ने भारत में पर्यावरणवाद को कैसे आकार दिया ?
उस समय भारत में जमीनी स्तर पर पर्यावरणवाद में तेजी आई थी, जिसने असल में पर्यावरणवाद के पुराने स्वरूप से मुकाबला किया, जो बाघों को बचाने जैसे संरक्षणवादी उपायों पर केंद्रित था। उस वक्त कृषि आंदोलन, महिला आंदोलन जैसे विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों ने सिर उठा लिया। देश भर में लोगों को एक साथ लाने वाली अनेक बैठकें हुईं और तब यह भावना थी कि इसका जमीनी स्तर से आना जरूरी है। नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत में जमीनी स्तर के संगठन प्रभावशाली रूप से मजबूत थे और उन संरचनात्मक समस्याओं को अच्छी तरह से समझते थे, जो न केवल भोपाल बल्कि देश भर में अन्य पर्यावरणीय नुकसान पैदा करती हैं। ऐसे कई उच्च शिक्षित लोग थे जो ग्रामीण इलाकों में या असंगठित समुदायों के साथ काम करने के लिए पहुंच गए थे। संगठनों में बहुत अधिक क्षमता और आपस में विचारों का बड़े पैमाने पर आदान-प्रदान हो रहा था। प्रौद्योगिकी सभी के लिए समृद्धि लाएगी, इस विचार पर अत्यधिक विश्वास करने के लिए भारतीय राज्यसत्ता की जबरदस्त आलोचना हो रही थी। अफसरशाही की भी गहरी आलोचना की गई, जो कुछ मायनों में थोड़ी विडंबनापूर्ण थी क्योंकि और अधिक लोकतंत्र से भोपाल त्रासदी को रोकने में मदद ही मिलती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से भोपाल आपदा के बारे में अपने शिक्षण में मैंने जिन चीजों पर जोर देने की कोशिश की है उनमें से एक यह है कि हमने इस प्रकार की आपदाओं को रोकने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण नहीं देखा है। भोपाल न केवल प्रौद्योगिकी के नाकाम वादे का एक बहुत नाटकीय प्रतीक बन गया, बल्कि इसे हरित क्रांति की विफलता के संकेत के रूप में भी देखा गया क्योंकि यह कीटनाशकों का निर्माण कर रहा था। और चूंकि भोपाल कांड पर सालाना श्रद्धांजलि समारोह होते थे, इसलिए इसमें देश भर से लोग आते थे। इस प्रकार भोपाल ऐसा स्थान बन गया जहां लोग साथ आकर कल्पना करने लगे कि आम जनमानस का पर्यावरणवाद कैसा होगा।
इसके अलावा पश्चिम के साथ क्या करना है…, आधुनिकता के साथ क्या करना है, इस पर भी काम चल रहा था। स्थानीय लोगों के लिए ये घटना बहुराष्ट्रीय निगम की गहरी विफलता थी जिसने वास्तव में उन उम्मीदों को धराशायी कर दिया कि विदेश से आई वस्तुएं अपने साथ तमाम अच्छी चीजें लेकर आती हैं और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कामगार उस कंपनी से बहुत निराश थे जिस पर उन्होंने भरोसा किया था।
क्या आपको लगता है कि नौकरशाही, त्रासदी रोक पाने के लिए आवश्यक जांच और संतुलन बिठा पाने में नाकाम रही और क्या यह आपदा के बाद भी असफल रही?
मुझे लगता है कि यूनियन कार्बाइड भोपाल परिसर जैसी सुविधाओं की निगरानी करना नौकरशाही का एक मजबूत कार्य होगा। लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। आज भी ये नहीं किया गया है। भारत में हमारे पास अब भी बहुत कम संख्या में ऐसे निरीक्षक हैं जो अत्यधिक जोखिम वाले औद्योगिक परिसरों का दौरा और जांच कर रहे हैं। वास्तव में अमेरिका में भी यह चिंताजनक है। उनसे कई चीजें छूट जाती हैं। हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां हमें बाद में एहसास हुआ कि उद्योग किसी दिए गए रसायन का अपने रिकॉर्ड से कहीं अधिक भंडारण कर रहा है। अग्निशमन विभाग को नहीं पता कि वे क्या भंडारित कर रहे हैं और इसलिए यह जोखिम पैदा करता है क्योंकि कंपनियों की कोई निगरानी नहीं है। आने वाले वर्षों में अमेरिका में इसके और भी बदतर होने की आशंका है।
आपदा के बाद और भोपाल की तरह जब एक बार चीजें तात्कालिकता की अवधि से आगे बढ़ जाती हैं तब नौकरशाही का ध्यान भटक जाता है। भोपाल में आप इसे त्रासदी स्थल की साफ-सफाई कर पाने में नाकामी के रूप में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मुआवजे के संदर्भ में योजना ने केवल व्यक्तिगत भुगतान प्रदान किया और जीवित समुदायों के लिए संरचनात्मक स्थितियों में वास्तव में कोई सुधार हो पाया।
भोपाल गैस त्रासदी से कैसे निपटा जाना चाहिए था?
सबसे बुनियादी बात यह है कि आपदा होनी ही नहीं चाहिए थी। हमें निरीक्षण की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी जो इसे रोक पाती। मुझे भोपाल त्रासदी को तकनीकी रूप से बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला है और मेरे लिए यह बहुत स्पष्ट है कि इसे रोका जा सकता था। इस दायरे में संयंत्र के मूल डिजाइन (जो कि अमेरिका में हुआ था) से लेकर भारत में श्रमिकों के प्रशिक्षण तक की बात शामिल है। आपदा की रात संयंत्र में अनेक सुरक्षा प्रणालियां काम ही नहीं कर रही थीं। ऐसी चेतावनी के साथ ऑडिट रिपोर्ट अमेरिका भेजी गई थीं कि हालात ठीक नहीं हैं। यूनियन कार्बाइड के एक बहुत ही मुखर कामगार ने मुझे बताया कि संयंत्र की संरचना को लेकर भी यूनियन कार्बाइड के इंजीनियरों ने तर्क दिया था कि उन्हें घनी आबादी वाले इलाके के बीचोंबीच इतने बड़े टैंक में ऐसे खतरनाक रसायन का भंडारण नहीं करना चाहिए। उनके पास छोटे पात्रों में भंडारण का विकल्प था। त्रासदी के बाद न्याय मिलना कठिन होता है। पीड़ितों को अंतरिम राहत भुगतान हासिल होने में आठ साल लग गए और प्राप्त हुई धनराशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। लोगों को लगातार यह चिंता सताती रही कि वे गैस पीड़ित के रूप में अपनी वस्तु-स्थिति साबित नहीं कर पाएंगे। उनमें से कई पक्की दीवारों वाले घरों में नहीं रहते थे। उन्हें यह साबित करना था कि गैस रिसाव की रात वे कहां रह रहे थे। लोग उस कागजी कार्यवाही की सत्यता को लेकर चिंतित थे। मुआवजा अदालतों के भोपाल आने पर पीड़ितों को न्यायाधीशों के सामने खड़े होकर मुआवजे के अपने अधिकार का बचाव करना पड़ा। इस व्यवस्था ने पीड़ितों पर सबूत और औचित्य का बहुत अधिक बोझ डाल दिया, जिन्हें निश्चित रूप से ऐसी हालातों का सामना नहीं करने देना चाहिए था।
जब मैं भोपाल में थी तब वे पीड़ितों की देखभाल के लिए अस्पताल का निर्माण शुरू ही कर रहे थे। शुरुआती दौर से ही ये धारणा बन गई थी कि वास्तव में वह अस्पताल आपदा से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की सेवा के लिए बनाया ही नहीं गया था। अस्पताल दूर था और इसका ज्यादा ध्यान संभ्रांत लोगों पर था। मैं सचमुच नहीं जानती कि उस अस्पताल ने कुछ दशकों में क्या किया है। मेरा मानना है कि आपदा से उबरने के लिए विद्यालयों समेत सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करने की आवश्यकता है जो अनजाने में औद्योगिक जोखिम की चपेट में न आए। मेरा मानना है कि वास्तविक तैयारी का मतलब सार्वजनिक शिक्षा की ठोस व्यवस्था है। भोपाल में न्याय का एक अन्य पहलू निश्चित रूप से उस परिसर की साफ-सफाई और फैक्ट्री स्थल पर बिखरे कचरे के नतीजतन होने वाला जल प्रदूषण रहा होगा।
क्या आपको लगता है कि अब तक घटित हो चुकी ज्यादातर औद्योगिक त्रासदियों को रोका जा सकता था?
मेरा मानना है कि पेट्रोकेमिकल्स स्वाभाविक रूप से खतरनाक हैं। ऐसे परिसरों के निकट रहने वाले निवासियों के साथ-साथ कामगारों के लिए भी पेट्रोकेमिकल्स के रोजमर्रा के जोखिम और धीमे खतरे रहते हैं। मुझे लगता है कि औद्योगिक सुविधाएं बेहतर ढंग से चलाई जा सकती हैं। उन कंपनियों की पहचान करना अहम है जो बेहतर काम करती हैं और अपनी साइटों पर जोखिम कम करने में पूरी तत्परता से सक्रिय हैं। इस कड़ी में हम बड़े टैंक भंडारण की बजाए छोटे टैंक भंडारण के उपयोग की मिसाल ले सकते हैं।
दक्षिणी कैलिफोर्निया में जहां मैं रहती हूं, उसके नजदीक दो रिफाइनरियां हैं जो अब भी शोधन प्रक्रिया में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग करती हैं। अगर ये रसायन बाहर निकल जाए तो यह विनाशकारी साबित होगा। दुनिया भर की अधिकांश रिफाइनरियां अब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग नहीं करती हैं। सरकारों को कंपनियों को जवाबदेह बनाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सबसे सुरक्षित विकल्पों का उपयोग करें।
भोपाल त्रासदी से हुए नुकसान को समझने में विज्ञान की कितनी भूमिका रही और तब से टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च कितना विकसित हुआ है?
उस समय और ऐतिहासिक रूप से पर्यावरण विज्ञान बहुत रूढ़िवादी रहा है क्योंकि वैज्ञानिक यह नहीं कह सकते कि एक्स के चलते वाई का परिणाम सामने आता है। नुकसान अधिक असमान रूप से होता है। भोपाल के बारे में दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि इस बात पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है कि आपदा ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। भोपाल में त्रासदी के तुरंत बाद के हालात पर सवाल नहीं उठाया जा सका। विपदा के तत्काल बाद नुकसान को समझने के लिए विज्ञान की आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि वो मंजर बेहद नाटकीय था। हालांकि, नुकसान की सीमा का आकलन करने में ये जरूर सामने आया और यही मुकदमेबाजी की असल वजह थी। गैस रिसाव से बचे लोगों और वकीलों ने तर्क दिया है कि भारतीय राज्यसत्ता ने नाटकीय रूप से नुकसान की सीमा को कम करके आंका है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान में अनुसंधान का अविश्वसनीय रूप से फलना-फूलना, 1990 के दशक के बाद घटित घटनाओं में से एक है। हम तब की तुलना में आज बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि तब हमें ये मालूम नहीं था कि उस समय के कई रसायन खतरनाक थे। यह बहुत ही गंभीर है कि गर्भावस्था के दौरान रासायनिक संपर्क बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकता है। वायु प्रदूषण सिर्फ आपके फेफड़ों को ही प्रभावित नहीं करता, यह अल्जाइमर रोग और मधुमेह से भी जुड़ता है। प्रदूषण लोगों पर क्या असर डालता है, इसकी समझ नाटकीय रूप से बढ़ी है।
हालांकि, मुझे लगता है कि विनियमन में उस विज्ञान का उपयोग करने की हमारी क्षमता बहुत अधिक सीमित है। इनमें से कुछ या बहुत कुछ राजनीतिक इच्छाशक्ति और नियामक प्रक्रिया पर उद्योग का असाधारण प्रभाव है। नियामक विज्ञान को विशेष प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाने की आवश्यकता है। उद्योग जगत, नियामक निर्णय लेने में अकादमिक अध्ययनों का बहुत अधिक उपयोग करने के खिलाफ दबाव प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। हमें शासन में विज्ञान को शामिल करने का एक बेहतर तरीका खोजना होगा। यहां तक कि सबसे अच्छी स्थितियों में भी, जहां आपके सामने कोई राजनीतिक विरोध ना हो, यह चुनौतीपूर्ण है। हमें विष विज्ञान (टॉक्सिकोलॉजी), महामारी विज्ञान और आणविक रसायन विज्ञान पर अध्ययन जारी रखने के लिए सिर्फ कोष उपलब्ध कराते रहना होगा। एक बार विज्ञान सामने आने पर हमें इसका उपयोग करने में सक्षम होना पड़ेगा। जाहिर है, ये रास्ता अभी खुला नहीं है।
आपकी किताब में वकीलों, पत्रकारों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा भोपाल गैस कांड को अलग-अलग तरीके से पढ़े जाने के बारे में भी बात की गई है। क्या आप इसे विस्तार से बता सकती हैं?
लोगों द्वारा समस्याओं की पहचान कर उन्हें चिन्हित किए जाने और उनके निपटारे के लिए क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर उनकी सोच के बीच भिन्नता है। उनमें से कुछ मतभेद निहित स्वार्थों के कारण हैं जो समस्या का अस्तित्व ही न होने का दिखावा करना चाहते हैं। हालांकि अन्य प्रकार के अंतर भी हैं। यदि आप चिकित्सा जगत के किसी पेशेवर से मुख्य समस्या और भावी प्राथमिकता क्रियाओं के बारे में पूछते हैं, तो उनके पास कानूनी पेशेवर या इंजीनियर या पास में रहने वाले सामुदायिक व्यक्ति की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण होगा। समस्या की समग्र समझ के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और ज्ञान स्वरूपों के साथ काम करने की कला सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अक्सर ये अविश्वास में तब्दील हो जाता है क्योंकि यहां एक भावना काम करती है जो मतभेद को हमारी समझ को बढ़ाने में मददगार मानने की बजाए एक समस्या मान लेती है। भोपाल त्रासदी के बाद जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वह यह है कि पर्यावरणीय खतरों और पर्यावरणीय नुकसान को समझने में सामुदायिक ज्ञान को बेशकीमती माना जाने लगा है।
यूनियन कार्बाइड ने आपदा की नैतिक जिम्मेदारी ली और उन्होंने संदेश दिया कि भारत में ताकतें एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने को लेकर ज्यादा उत्सुक थीं, जिससे पीड़ितों को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या ऐसे संदेशों ने उनके पक्ष में काम किया?
हां और न, दोनों। दरअसल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सवाल किससे करते हैं। निश्चित रूप से उद्योग और रासायनिक उद्योगों के व्यापार समूह यूनियन कार्बाइड के पीछे लामबंद हुए। आपदा के बाद के वर्षों में भी यूनियन कार्बाइड के सीईओ को तत्कालीन अमेरिकन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसका नाम बदल दिया गया है। उस वक्त पूरे उद्योग की ताकत और सुरक्षा का बचाव करने की भावना काम कर रही थी। दूसरी ओर, अकादमिक इंजीनियरों और औद्योगिक इंजीनियरों ने यूनियन कार्बाइड के इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया कि किसी असंतुष्ट कामगार द्वारा भंडारण टैंक में पानी डाल दिए जाने से रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई और नतीजतन गैस का रिसाव हुआ। मुझे याद है कि मैंने एक अकादमिक सम्मेलन की रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें यूनियन कार्बाइड ने ये किस्सा बयां करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। इस त्रासदी के चलते कंपनी के कुछ कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं के बारे में बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। हालांकि आपको यह भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेने का वादा किया था। जमीन पर ये निश्चित रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। याद रखें कि यह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तेजी का शुरुआती दौर भी था। जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि ये उद्योग कितने जोखिम भरे हैं, उन्होंने सुरक्षित और सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने की छवि बनाने के लिए अपने निवेश में बढ़ोतरी कर दी।