जवरीमल्ल पारिख
फ़िल्मों के संदर्भ में यह सवाल बार-बार उठता रहा है कि सिनेमा में कलाकार बड़ा होता है या कहानी। फ़िल्म के संदर्भ में जब हम कहानी की बात कर रहे होते हैं तब वह कहानी नहीं जो शब्दों में लिखी गयी है बल्कि वह कहानी जिसे हम फ़िल्म के पर्दे पर घटित होता हुआ देखते हैं।
दरअसल शब्दों में लिखी कहानी महज एक ‘आइडिया’ होती है जिसे पढ़कर या सुनकर फ़िल्मकार (निर्देशक और/या निर्माता) इस संभावना को तलाशता है कि क्या इस आइडिया को फ़िल्म में रूपांतरित किया जा सकता है।

यदि उसमें इसकी संभावना नज़र आती है तो वह पटकथा लेखक को उस आइडिया पर पटकथा लिखने का काम सौंपता है। यह मुमकिन है कि आइडिया उस पटकथाकार का ही हो, या यह भी संभव है कि आइडिया फ़िल्म निर्देशक या निर्माता का हो या किसी पूर्व प्रकाशित कहानी, उपन्यास, नाटक आदि से आइडिया लिया गया हो।
फिल्म में पटकथा की भूमिका
बहुत से फ़िल्म निर्देशक अच्छे पटकथा लेखक भी होते हैं। लेकिन जो भी हो, उस आइडिया के फ़िल्मांतरण के लिए पटकथा का लिखा जाना जरूरी है जो कहानी लेखन और फ़िल्म निर्देशन से स्वतंत्र काम है।
सिनेमा निर्माण का सबसे पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम पटकथा लेखन है।पटकथा लेखन कहानी या उपन्यास लिखने से बिल्कुल भिन्न तरह का काम है। आइडिया स्वयं उसका हो या किसी ओर का, इससे खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिनेमा जो एक दृश्य माध्यम है उसकी पटकथा दरअसल दृश्य कथा होती है।
पटकथाकार वह पहला व्यक्ति होता है जो कहानी के विचार को दृश्य के रूप में विकसित करता है। फ्रेम दर फ्रेम या शॉट दर शॉट भले ही न सोचे लेकिन सीन दर सीन तो उसे सोचना और विकसित करना होता है। उसकी कल्पना में कहानी दृश्य दर दृश्य आगे बढ़ती जाती है और वह उन दृश्यों को कागज पर उतारता जाता है।
जब वह किसी दृश्य के बारे में सोचता है तो केवल कलाकारों के बीच होने वाली बातचीत ही नहीं सोचता है बल्कि उन क्रियाओं के बारे में भी सोचता है जिन क्रियाओं को फ़िल्म में घटित होना होता है। उसे यह भी सोचना होता है कि ये क्रियाएं किन पात्रों के बीच घटित होनी है, कहां घटित होनी है, किन स्थितियों के बीच घटित होनी है। उस समय सुबह है, शाम है या रात। उस समय पात्रों की मन:स्थिति कैसी है और उसकी मन:स्थिति में क्या बदलाव हो रहे हैं।
वह अगर कोई बात कह रहा है तो गुस्से में कह रहा है, उदास होकर कह रहा है, या बेमन से कह रहा है। ठीक जब वह कुछ कह रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है। अगर ध्यान दें तो एक अच्छा पटकथा लेखक मौलिक रचनाकार से किसी भी अर्थ में कमतर नहीं होता।
वह फ़िल्म का एक विस्तृत प्रारूप कागजों पर बना लेता है। होता यह प्रारूप ही है क्योंकि निर्देशक अन्य कलाकारों, तकनीशियनों, निष्पादकों की मदद से उसे फ़िल्म के रूप में साकार करता है। इस पूरी प्रक्रिया में निर्देशक केंद्र में होता है। अंतिम निर्णय उसका होता है।
लेकिन एक अच्छा फ़िल्मकार अपने को दूसरों पर थोपता नहीं बल्कि अन्यों के साथ मिलकर टीम की तरह काम करता है। इस टीम में कलाकार भी शामिल है। लेकिन सदस्य के रूप में निर्णायक के रूप में नहीं।
यहां यह प्रश्न जरूर उठता है कि जब पटकथा लिखी जा रही होती है तब क्या पटकथा लेखक के मन में कोई कलाकार विशेष होता है। मेरे विचार में अच्छे पटकथा लेखक के मन में पात्र ही होते हैं, कलाकार नहीं होते।
अगर किसी वजह से कोई कलाकार उसके दिमाग में होता है या उसे बताया जाता है कि इसका नायक (या नायिका) अमुक स्टार होगा, तो पटकथा लेखन में उस कलाकार की अभिनय संबंधी विशिष्टताएं और सीमाएं पटकथा को जाने-अनजाने प्रभावित करने लगती है।
यह प्रवृत्ति उन फ़िल्मकारों में ज्यादा दिखायी देती है जो फ़िल्म की कामयाबी और नाकामयाबी को कलाकार पर निर्भर मानते हैं और उस कलाकार की लोकप्रियता को अपनी फ़िल्म में भुनाना चाहते हैं और वे पटकथा लेखक पर दबाव डालते हैं कि उस विशिष्ट कलाकार को ध्यान में रखकर पटकथा लिखे।
लेकिन इसका असर कहानी की मूल प्रकृति पर आमतौर पर नकारात्मक पड़ता है। हां, यह अवश्य है कि पटकथा पढ़ने के बाद पात्रों की चरित्रगत विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए निर्देशक ऐसे कलाकारों का चयन करता है जो पात्रों के सर्वाधिक अनुरूप हो।
कई कलाकार ऐसे होते हैं जो सब तरह के चरित्र का निर्वाह सक्षम ढंग से कर पाते हैं और कई कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी रेंज बहुत सीमित होती है और सबसे कमजोर कलाकार वे होते हैं जिनमें अभिनय क्षमता बहुत कम होती है और उन्हें किसी भी तरह का चरित्र दे दिया जाये वे आमतौर पर अपने व्यक्तित्व से बाहर नहीं निकल पाते। हां ये जरूर संभव है कि इसके बावजूद वे काफी लोकप्रिय हों। यह भी मुमकिन है कि उनका व्यवसाय उनसे बेहतर अभिनेताओं की तुलना में ज्यादा सफल हो।

नाटक की सफलता कलाकारों पर निर्भर
कलाकारों की भूमिका की दृष्टि से नाटक और सिनेमा में कुछ बुनियादी अंतर है। नाटक कलाकारों का माध्यम है।
निर्देशक कलाकार को निर्देशित नाटक के मंचन से पहले करता है लेकिन जब नाटक मंच पर खेला जा रहा होता है तब उसकी सफलता और उत्कृष्टता पूरी तरह कलाकारों पर निर्भर करती है जो अपनी प्रत्येक प्रस्तुति से कुछ सीखता है और उसमें सुधार करता है।
इसके विपरीत फ़िल्म निर्देशक का माध्यम है। कलाकार को निर्देशक के अनुसार ही काम करना होता है। फ़िल्म सदैव कलाकारों पर निर्भर हो यह जरूरी नहीं है।हिंदी में ही बहुत सी ऐसी फ़िल्में बनी हैं जिनमें कोई बड़ा कलाकार नहीं होता, इसके बावजूद फ़िल्म कामयाब भी हुई है और उत्कृष्ट भी।
मसलन बूट पालिश, अब दिल्ली दूर नहीं, दोस्ती, जैसी कई फ़िल्में हैं जिनमें लोकप्रिय कलाकारों के न होने के बावजूद फ़िल्में देखी भी गयी और सराही भी गयी।
कई फ़िल्मों में कलाकारों से अलग कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दर्शकों को ज्यादा आकृष्ट करती हैं। फ़िल्म देवदास (1955) में रेल के दृश्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
जुरासिक पार्क में अभिनेताओं से ज्यादा आकर्षण डायनासोर थे। हॉलीवुड में ऐसे प्रयोग बहुत हुए हैं जिनमें कोई काल्पनिक जानवर, एलियन या और कुछ को फ़िल्म के केंद्र में रखा गया होता है।
इसी तरह हिंदी सिनेमा में गीत और संगीत ने फ़िल्म से स्वतंत्र अपनी एक जगह लोगों के बीच बना ली है। बहुत सी फ़िल्में तो केवल इसलिए लोकप्रिय हुईं क्योंकि उनके गीतों के पीछे लोग दिवाने थे। जबकि उनकी कहानी बहुत साधारण थी।
यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अच्छी कहानी पर बनी फ़िल्म में बिल्कुल अनजाने और अपरिचित कलाकार रातों-रात कामयाब स्टार बन गये और अगर बाद की फ़िल्मों में उन्हें उत्कृष्ट कहानी वाली अच्छी फ़िल्में नहीं मिलती है तो लोग उन्हें भूल भी जाते हैं।
कई अभिनेता और अभिनेत्रियां बहुत कामयाब होती हैं। उन्हें लगातार फ़िल्में मिलती रहती हैं। उनकी फ़िल्में चलती भी हैं लेकिन अच्छे अभिनेता के तौर पर उनकी ख्याति नहीं बन पाती।
इसकी वजह या तो यह होती है कि वे औसत दर्जे के कलाकार होते हैं, या उनका फ़िल्मों का चयन बहुत साधारण होता है जो फ़िल्में कामयाब तो होती हैं लेकिन जिन्हें जल्दी ही भुला दिया जाता है।
कुछ बेहतरीन कलाकार हमेशा अच्छी और अलग सी कहानी की खोज में रहते हैं। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि ऐसी ऑफबीट फ़िल्म से बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता इसलिए वे बीच-बीच में पॉपुलर सिनेमा में भी काम करते हैं।
नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, पंकट कपूर जैसे कलाकार दोनों तरह की फ़िल्मों में काम करते रहे हैं और अपने अंदर के कलाकार का संतुष्ट रखने के लिए नाटकों में भी काम करते हैं।
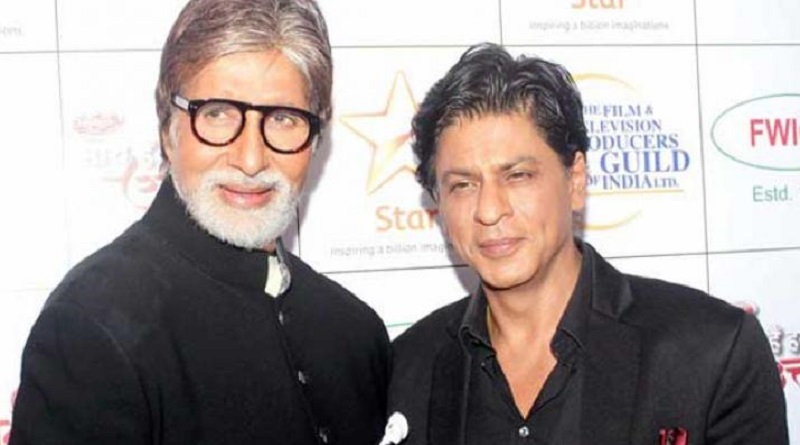
मीडिया बनती है अभिनेता को स्टार
अभिनेता को स्टार दर्शक और मीडिया बनाता है। मीडिया फ़िल्म की कामयाबी का श्रेय फ़िल्म के लेखक, निर्देशक और उसमें महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले कलाकारों को देने की बजाय केवल नायक (और कभी-कभार नायिका) को देते हैं। उन्हें सातवें आसमान पर चढ़ा देते हैं। वे अभिनेता जो मीडिया के इस प्रचार के झांसे में आ जाते हैं और मानने लगते हैं कि वे सचमुच स्टार बन गये हैं।
ऐसे स्टारों को यह गलतफहमी होने लगती है कि उनकी वजह से ही फ़िल्में चलती हैं और फिर वे निर्देशक को डिक्टेट करने लगते हैं, उन पर हावी होने लगते हैं। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि वे फ़िल्म से संबंधित सभी बातों को न केवल जानते हैं बल्कि निर्देशक को भी निर्देशित करने लगते हैं।
इस अहंकार के चलते वे फ़िल्म में या अपने चरित्र में ऐसे बदलाव के लिए आग्रह करते हैं जो फ़िल्म की कहानी के लिए बहुत अनुकूल नहीं होते। ऐसे बलशाली कलाकार आमतौर पर सीखना भी बंद कर देते हैं। चूंकि वे यह मानते हैं कि फ़िल्म की कामयाबी उन पर निर्भर करती है इसलिए वे हर फ़िल्म में अपनी खास (चलने, बोलने और पहनने की) शैली को दोहराने लगते हैं।
हिंदी (और कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं का) सिनेमा का संसार जिस तरह आगे बढ़ा है और उसमें कहानी की बजाय स्टारों को ज्यादा महत्त्व दिया जाने लगा है और दर्शकों की अभिरुचि भी उसी तरह की हो गयी है क्योंकि फ़िल्म में पर्दे पर तो कलाकार ही नज़र आता है और उसे ही वह फ़िल्म का आदि और अंत समझने लगता है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत अच्छी कहानी के लिए गुंजाइश बहुत कम रह गयी है।
ये भी पढ़ें-
- मट्टो की साइकिलः यह फिल्म हर मज़दूर को क्यों देखनी चाहिए?
- ‘गायब होता देश’ और ‘एक्सटरमिनेट आल द ब्रूटस’ : एक ज़रूरी उपन्यास और डाक्युमेंट्री

फिल्मों में नया फार्मूला
एक बड़ा कारण यह भी है कि फ़िल्म निर्माण में बहुत अधिक निवेश की जरूरत होती है इसलिए पैसा लगाने वाला कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। कहानी की संकल्पना भी कुछ ऐसे फार्मूलों पर टिकी होती है जिसको कहानी में शामिल करने से वे समझते हैं कि फ़िल्म अवश्य कामयाब होगी।
यहां 1994 की फ़िल्म ‘हम आपके हैं कौन’ का उदाहरण लिया जा सकता है जिसकी अपार सफलता ने ऐसी फ़िल्मों की लंबी लाइन लगा दी जिसमें हिंदू विवाह का भव्य आयोजन एक जरूरी फार्मूला बन गया था।
ऐसे कई फार्मूले फ़िल्मों में चलते रहते हैं। जब वे घिस-पिट जाते हैं तो कोई नया फार्मूला सामने आता है। फार्मूलों की खोज लोकप्रियता के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहानी के लिए सबसे जरूरी है उसका प्रासंगिक होना।
राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में बदलाव का असर फ़िल्मों पर भी पड़ता है। फार्मूले मुमकिन है कि लंबे समय तक बने रहें लेकिन कहानी में बदलाव का मुख्य कारण उसकी प्रासंगिकता है।
जब मुख्यधारा का सिनेमा प्रासंगिकता को ठीक से समझने में असफल रहता है और जनता की बदलती अभिरुचि का भी गलत आकलन करता है तो फ़िल्में पिटने लगती है।
पिछले एक दशक से मौजूदा दक्षिणपंथी-सांप्रदायिक राजनीति के प्रभाव में कई फ़िल्में बनी हैं और कई फ़िल्मकार मानने लगे हैं कि लोगों की सोच काफी बदल गयी है।
नतीजा यह है कि बहुत सी फ़िल्में ऐसी बन रही हैं जिनमें इस राजनीति का असर दिखायी दे रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस राजनीतिक प्रभाव में बन रही अधिकतर फ़िल्में नाकामयाब भी हो रही है क्योंकि ये फ़िल्में उनकी वास्तविक अभिरुचि से मेल नहीं खातीं।
आज जनता की वास्तविक अभिरुचि को मुख्यधारा की फ़िल्मों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। ओटीटी प्लेटफार्म ने जो विकल्प प्रस्तुत किये हैं उसने कहानी और कलाकार के समीकरण को भी प्रभावित किया है। ओटीटी में कामयाबी के लिए पहली जरूरत है, नयी तरह की कहानी जिसे नये ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। यहां घिसेपिटे फार्मूले से ज्यादा यथार्थवादी प्रस्तुति को अधिक पसंद किया जा रहा है।
दूसरी विशेषता यह है कि यहां स्टार नहीं बल्कि कलाकार की मांग है। नतीजा यह है कि वे कलाकार ओटीटी पर ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं जो अपने काम से पहचाने जाते हैं न कि नाम से। इसका असर मुख्यधारा पर भी अब दिखने लगा है।


























