*(परिसीमन पर विपक्षी दलों की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन का भाषण, अनुवाद : संजय पराते)*
यहाँ उपस्थित विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण और अन्य प्रतिनिधिगण, आप सभी को मेरा सलाम। सबसे पहले, हम सभी की ओर से, मैं तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम. के. स्टालिन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज हम सभी को यहाँ एकत्रित किया है।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्तावित परिसीमन हमारे सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। विभिन्न रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिना किसी परामर्श के परिसीमन प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। यह अचानक उठाया गया कदम किसी संवैधानिक सिद्धांत या किसी लोकतांत्रिक अनिवार्यता से प्रेरित नहीं है, बल्कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित है।
अगर जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उत्तरी राज्यों की सीटों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, जबकि संसद में दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय कमी आएगी। यह भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उत्तर में उनका प्रभाव अधिक है। अगर परिसीमन पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा, क्योंकि हम 1973 से अपनी जनसंख्या को कम कर रहे हैं, जब पिछला परिसीमन किया गया था, जिसमें लोकसभा में सीटों की संख्या पुनर्गठित की गई थी।
हमारे राज्यों को अब 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के ईमानदारी से क्रियान्वयन के लिए दंडित किया जाना तय है। जब कोई राज्य राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नीति को ईमानदारी से लागू करता है, तो उस राज्य पर इसी कारण से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। न केवल इस विचार को नकारा जा रहा है, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें दंडित भी किया जा रहा है। यही वर्तमान मुद्दे का सार है।
1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, देश के केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नहीं थी। इसे केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए एक नीति के रूप में घोषित किया था। बहरहाल, कई राज्य इसे प्रभावी रूप से लागू करने में विफल रहे। दूसरी ओर, हमारे राज्यों ने इसे सराहनीय रूप से लागू किया है। केंद्र सरकार ने इस उपलब्धि के लिए बार-बार हमारी प्रशंसा की है। फिर भी, वही केंद्र सरकार अब हमें लक्ष्य हासिल करने और उससे आगे जाने के लिए दंडित कर रही है। दृष्टिकोण ऐसा ही लगता है — अब आपकी आबादी कम है, इसलिए अब आप कम फंड और कम प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। यह निंदनीय है।
हमारे राज्य, जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए समर्पण के साथ लागू किया है, उन्हें पहले से ही एक और तरह से दंडित किया जा रहा है। यह दंड संवैधानिक रूप से हमें मिलने वाले करों में से हमारे हिस्से को कम करने के रूप में है। इसे सही ठहराने के लिए हमारी घटती जनसंख्या का हवाला दिया जा रहा है। 10वें वित्त आयोग के दौरान केरल का हिस्सा 3.875% था, जो अब 15वें वित्त आयोग में घटकर मात्र 1.925% रह गया है। जनसंख्या नियंत्रण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि होती है। बहरहाल, धन का वितरण करते समय, इस पर कोई विशेष विचार नहीं किया जाता है।
यदि हमारे संसदीय प्रतिनिधित्व को और कम कर दिया जाता है, जबकि राष्ट्र की संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी में गिरावट जारी है, तो हम एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना करेंगे, जिसमें फंड के हमारे सही हिस्से की मांग और इसके लिए हमारी राजनीतिक आवाज दोनों एक साथ कम हो जाएगी। इस मुद्दे की गंभीरता और उसके महत्व को मान्यता देते हुए ही हम यानी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब अब विरोध में एकजुट हो रहे हैं।
हमारे समन्वित प्रतिरोध की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन के निमंत्रण पर हम यहां एकत्रित हुए हैं। हम एक संयुक्त कार्रवाई समिति बना रहे हैं। केंद्र सरकार राजकोषीय नीतियों से लेकर भाषा नीति और सांस्कृतिक नीतियों तक के लिए कार्रवाई करती हैं, यहां तक कि प्रतिनिधित्व का निर्धारण भी। केंद्र सरकार की यह कारगुज़ारी भारत की संघीय प्रणाली और लोकतांत्रिक ढांचे को अस्थिर कर रही है। इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
भारतीय संविधान भारत को ‘राज्यों के संघ’ के रूप में पहचानता है, जो हमारे संघीय चरित्र को रेखांकित करता है। यह संघ और राज्यों के बीच संतुलन बनाता है। परिसीमन पर वर्तमान प्रयास इस संतुलन को बाधित करता है, जो कि जनसंख्या नियंत्रण जैसी राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में विफल रहने वाले राज्यों को असमान रूप से सशक्त बनाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लिंग समानता को प्राथमिकता देने वाले राज्यों को उनके प्रगतिशील विकल्पों के लिए दंडित करता है। यह एक विकृत प्रोत्साहन है, क्योंकि राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने के डर से मानव विकास में निवेश करने से हतोत्साहित करता है। केंद्र सरकार को यह जांचना चाहिए कि क्या यह रुख राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा या हमें पीछे की ओर ले जायेगा।
भारत की संघीय संरचना को छोटे समुदायों और क्षेत्रीय पहचानों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था। भारत की संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने केंद्रीय अधिकारिता (सेंट्रल एथॉरिटी) को संतुलित करने के लिए राज्यों के अधिकारों की वकालत करते हुए ‘बहुमत के अत्याचार’ के खिलाफ चेतावनी दी थी। 1988 में सरकारिया आयोग ने फिर से इसे यह कहते हुए मजबूत किया कि “संघवाद केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि संविधान की एक मौलिक विशेषता है।”
इस सिद्धांत को अनदेखा करने वाला परिसीमन औपनिवेशिक युग के केंद्रीकरण को पुनर्जीवित करने के जोखिम की अनदेखी करता है, जहां विविध आवाज़ों को बहुमत एजेंडा के नीचे दबा दिया गया था। इसकी अंतिम परिणति यह थी कि भारतीय लोग उपनिवेशवादियों के खिलाफ एकजुट हो गए और उन्हें देश से बाहर निकाल फेंका। आज के मामलों में जो शीर्ष पर हैं, उन्हें हमारे इतिहास पर ध्यान देना चाहिए और उससे सीखना चाहिए।
भारत की संघीय संरचना हमारे लोकतंत्र की एक आधारशिला है, जिसे संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रीय पहचानों के विशाल ग्रामीण मोज़ेक (पच्चीकारी) को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत को परिभाषित करने वाली विविधता केवल एक जनसांख्यिकीय आंकड़ा भर नहीं है; यह वह आधार है, जिस पर हमारी एकता की स्थापना की गई है। एक मजबूत संघीय प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि अपने अद्वितीय इतिहास, भाषा और सांस्कृतिक विरासत के साथ हर क्षेत्र की राष्ट्रीय संवाद में एक आवाज हो।
परिसीमन की वर्तमान प्रक्रिया हमारे समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं के संरक्षण के लिए एक गंभीर खतरा है। इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भाषाई कारकों को ध्यान में रखे बिना पूरी तरह से केवल जनसंख्या के आधार पर फिर से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, उन क्षेत्रों को हाशिए पर रखने की संभावना को बल देता है, जिन्होंने लंबे समय से अपनी अलग पहचान को संरक्षित किया है। यह हमारे राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो न केवल राष्ट्र की जनसांख्यिकीय रचना
में योगदान करते हैं, बल्कि इसके सांस्कृतिक परिदृश्य को भी समृद्ध करते हैं।
भारत की ताकत इसकी बहुलता में निहित है। हमारी सांस्कृतिक और भाषाई विविधताएं ऐसी संपत्ति हैं, जो हमारे राष्ट्र को मजबूत करती हैं, जिससे हम दृष्टिकोण और नवाचारों की एक विस्तृत श्रृंखला का दोहन करने में सक्षम होते हैं। केरल की ‘कुडुम्बश्री’ पहल, जिसने लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया, और तमिलनाडु की मध्यान्ह भोजन योजना, इन राज्यों के विशिष्ट नवाचार हैं, जो बाद में राष्ट्र के लिए खाका (उल्लेखनीय नमूना) बन गए। केंद्रीकरण की शक्ति ऐसे स्थानीयकृत समाधानों को रोक देगी, जो भारत की विविधता को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सांस्कृतिक संरक्षण और संघवाद परस्पर जुड़े हुए हैं, भारतीय अनुभव इसे रेखांकित करता है।
जब छोटे या कम आबादी वाले राज्य राजनीतिक ताकत खो देते हैं, तो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। बड़ी आबादी वाले राज्यों के प्रभुत्व वाली एक समरूप संसद क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को दरकिनार कर सकती है, जो उस बहुलतावाद को नष्ट कर देगी, जिसकी परिकल्पना आधुनिक भारत के संस्थापकों द्वारा की गई है। एक केंद्रीकृत प्रक्रिया, जो इन कारकों को नजरअंदाज करती है, न केवल क्षेत्रीय आवाज़ों को कमजोर करती है, बल्कि उस संतुलन के लिए भी खतरा पैदा कर देती है, जिसने भारत को एकजुट और विविध गणराज्य के रूप में पनपने की अनुमति दी है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ सार्थक संवाद में संलग्न होना चाहिए और हमारे विचारों को शामिल करना चाहिए, ताकि परिसीमन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले राज्यों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करने से राजनीतिक और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा और हमारे बहुलतावादी लोकतंत्र की विविधता कमज़ोर होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले पर केरल का रुख़ स्पष्ट है। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण, जो संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और राजनीतिक कारणों से कुछ राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करने का प्रयास करता है, केरल को अस्वीकार्य है। परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय केवल आम सहमति से ही लिया जाना चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद संसदीय सीटों का परिसीमन अनिवार्य किया गया है। इसी प्रावधान के तहत पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा की संख्या 489 से बढ़कर 543 हो गई। बहरहाल, संविधान के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया है। परिसीमन कराने या इसमें देरी करने के निर्णय केवल सत्ता में बैठे लोगों की क्षणिक राजनीतिक सुविधा के आधार पर लिए गए हैं।
1976 के 42वें संविधान संशोधन ने 2000 के बाद पहली जनगणना के बाद तक परिसीमन को रोक दिया था। इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के बावजूद, देश में जनसंख्या की असमानता बनी रहीं, जिसके कारण 84वें संविधान संशोधन ने 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद तक परिसीमन रोक को बढ़ा दिया। 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, और अगली जनगणना 2031 में होने वाली है। बहरहाल, केंद्र सरकार उससे पहले ही परिसीमन के लिए जोर दे रही है।
2011 की जनगणना में केरल की जनसंख्या वृद्धि मात्र 4.92% थी, जबकि 2001 से 2011 के बीच राष्ट्रीय औसत 17.7% था। इस अवधि के दौरान हमारे सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई है। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों का आखिरी बार पुनर्गठन 1973 में किया गया था। उस समय केरल की आबादी भारत की आबादी का 3.89% थी। हालांकि, अगले चार दशकों में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण, 2011 तक देश की आबादी में केरल की हिस्सेदारी घटकर मात्र 2.76% रह गई।
यदि परिसीमन की प्रक्रिया अभी की जाती है, तो केरल की घटती जनसंख्या के कारण संसदीय सीटों की संख्या में कमी आएगी। जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्यों को दंडित किया जाना अनुचित है। हम इस अन्याय का विरोध करने के लिए दृढ़ हैं। संघीय सिद्धांतों और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को बरकरार रखा जाना चाहिए।
जबकि मौजूदा परिसीमन प्रयास के पीछे राजनीतिक चालबाज़ी स्पष्ट है, यह ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भारतीय संघवाद और हमारी सांस्कृतिक और भाषाई विविधताओं के संरक्षण के लिए व्यापक निहितार्थों पर भी विचार करे। उन्हें कमज़ोर करने वाली कोई भी कार्रवाई न केवल हमारी राजनीतिक संस्थाओं को अस्थिर करेगी, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक समाज की नींव को भी कमज़ोर करेगी।
केंद्र सरकार का यह तर्क कि हमारे राज्यों को आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, को सच नहीं माना जा सकता। केंद्र यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि यह आनुपातिक वितरण संसदीय सीटों की मौजूदा ताकत के आधार पर होगा या जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर। इसलिए, केंद्र सरकार को हमारी आशंकाओं को दूर करना चाहिए। एकतरफा उपायों से बचना और लोकतंत्र और संघवाद के सार को संरक्षित करना केंद्र की जिम्मेदारी है।
हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परिसीमन की प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि संसद में हमारी वर्तमान आनुपातिक सीटों की हिस्सेदारी बनी रहे। यह वह आम सहमति है, जिस पर हम सभी को पहुंचना है। मुझे यकीन है कि हम ऐसा करने में सक्षम होंगे, और यह बैठक संयुक्त कार्रवाई समिति के गठन और कामकाज के लिए मजबूत आधार के रूप में काम करेगी, जो हमारी आम सहमति को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए पहलकदमी को आगे बढ़ाएगी।
मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि संघवाद संघ की ओर से कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह राज्यों का अधिकार है। हमारा सामूहिक प्रतिरोध सिर्फ़ सीटों के लिए नहीं है; यह एक विविधतापूर्ण और समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है।
*(अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)*


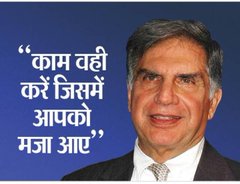























Add comment