जाहिद खान
1 अक्टूबर, 1919 यही वो तारीख है जब तरक़्क़ीपसंद शायर मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म हुआ था। तरक़्क़ीपसंद तहरीक के शुरुआती दौर का अध्ययन करें, तो यह बात सामने आती है कि तरक़्क़ीपसंद शायर और आलोचक ग़ज़ल विधा से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने अपने तईं ग़ज़ल की पुर-ज़ोर मुख़ालफ़त की, उसे जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया। यहां तक की शायर-ए-इंक़लाब जोश मलीहाबादी, तो ग़ज़ल को एक काव्य विधा की हैसियत से मुर्दा क़रार देते थे।
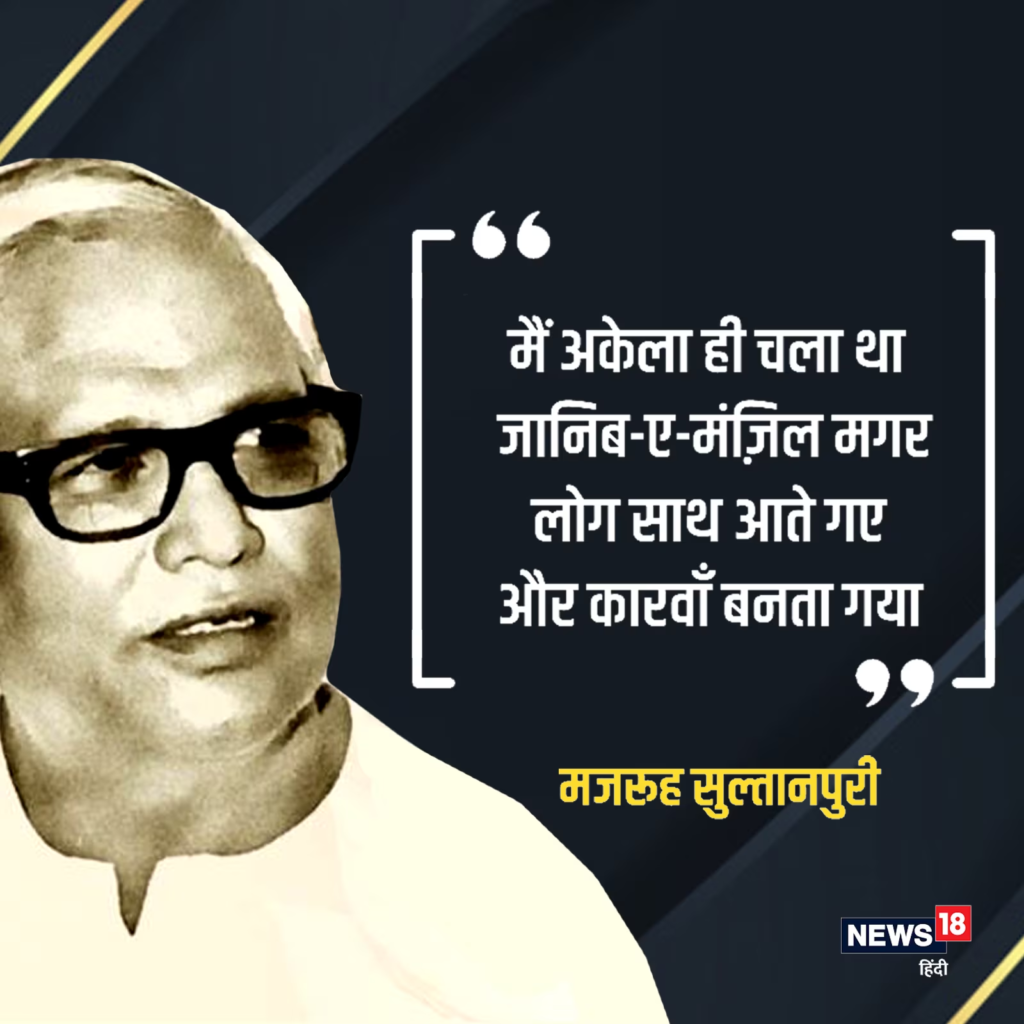
विरोध के पीछे अक्सर यह दलीलें होती थीं कि ग़ज़ल नए दौर की ज़रूरतों के लिहाज़ से नाकाफ़ी ज़रिया है। कम अल्फ़ाज़ों, बहरों-छंदों की सीमा का बंधन खुलकर कहने नहीं देता। लिहाज़ा उस दौर में उर्दू अदब में मंसूबाबंद तरीके़ से नज़्म आई। फ़ै़ज़ अहमद फै़ज़, अली सरदार जाफ़री, साहिर लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, वामिक़ जौनपुरी और मजाज़ वगैरह शायरों ने एक से बढ़कर एक नज़्में लिखीं।
मजरूह सुल्तानपुरी ने ना सिर्फ़ ग़ज़लें लिखीं, बल्कि वे उन शायरों में शामिल रहे, जिन्होंने ग़ज़ल की हमेशा तरफ़दारी की और इसे ही अपने जज़्बात के इज़हार का ज़रिया बनाया। ग़ज़ल के बारे में उनका नज़रिया था,‘‘मेरे लिए यही एक मोतबर ज़रिया है। ग़ज़ल की ख़ुसूसियत उसका ईजाज़-ओ-इख़्तिसार (संक्षिप्तता) और जमईयत (संपूर्णता) व गहराई है। इस ऐतिबार से ये सब से बेहतर सिन्फ़ (विधा) है।’’
मजरूह सुल्तानपुरी से पहले ग़ज़ल की यह ज़मीन मीर, सौदा, मोमिन, ग़ालिब, और दाग़ के साथ-साथ हसरत मोहानी, इक़बाल, जिगर, फ़िराक़ का घर-आंगन हुआ करती थी। अली सरदार जाफ़री के अल्फ़ाज़ में कहें, तो ‘‘मजरूह ग़ज़ल के इस आंगन में किसी सिमटी सकुचाई दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक निडर, बेबाक दूल्हे की तरह दाखिल हुए थे।’’ ग़ज़ल की जानिब मजरूह की ये बेबाक़ी और पक्षधरता आख़िर समय तक क़ायम रही। ग़ज़ल के विरोधियों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद ज़हीर ने अपनी क़िताब ‘रौशनाई’ में मजरूह सुल्तानपुरी की ग़ज़ल की जानिब इस जज़्बे और हिम्मत की दाद देते हुए लिखा है,‘‘मजरूह को बंबई में गोया दो मोर्चों पर जंग करनी पड़ती थी। एक तरफ़ वह अपने पहले के रिवायती ग़ज़ल गायकों और शाइरों से तरक़्क़ीपसंदी के उसूलों को सही मनवाने के लिए लड़ते, दूसरी तरफ तरक़्क़ीपसंद लेखकों की अक्सरियत से ग़ज़ल को स्वीकार कराने और उसकी अहमियत को तसलीम करवाने के लिए उन्हें असाधारण साहित्यिक वाद-विवाद करना पड़ता।’’
मजरूह सुल्तानपुरी की इस बात से हमेशा नाइत्तेफ़ाक़ी रही, कि मौजूदा ज़माने के मसाइल को शायराना रूप देने के लिए ग़ज़ल नामौज़ूअ है, बल्कि उनका तो इससे उलट यह साफ़ मानना था,‘‘कुछ ऐसी मंज़िलें हैं, जहां सिर्फ़ ग़ज़ल ही शायर का साथ दे सकती है।’’ कमोबेश यही बात क़ाज़ी अब्दुल ग़फ़्फ़ार, मजरूह की वाहिद शायरी की किताब ‘ग़ज़ल’ की प्रस्तावना में लिखते हुए कहते हैं, ‘‘मजरूह का शुमार उन तरक़्क़ीपसंद शायरों में होता है, जो कम कहते हैं और (शायद इसलिए) बहुत अच्छा कहते हैं।
ग़ज़ल के मैदान में उसने वह सब कुछ कहा है, जिसके लिए बाज़ तरक़्क़ीपसंद शायर सिर्फ़ नज़्म का ही पैराया ज़रूरी और ना—गुज़ीर (अनिवार्य) समझते हैं। सही तौर पर उसने ग़ज़ल के क़दीम शीशे (बोतल) में एक नई शराब भर दी है।’’ क़ाज़ी अब्दुल ग़फ़्फ़ार की यह बात सही भी है। उनकी एक नहीं, कई ऐसी ग़ज़लें हैं जिसमें मौज़ूअ से लेकर उनके कहने का अंदाज़ निराला है। मसलन
सर पर हवा-ए-ज़ुल्म चले सौ जतन के साथ
अपनी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ।
जला के मिशअल-ए-जाँ हम जुनूँ-सिफ़ात चले
जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले।
मजरूह, मुशायरों के कामयाब शायर थे। ख़ुशगुलू होने की वजह से जब वे तरन्नुम में अपनी ग़ज़ल पढ़ते, तो सामाईन झूम उठते थे। ग़ज़ल में उनके बग़ावती तेवर अवाम को आंदोलित कर देते। वे मर मिटने को तैयार हो जाते। ग़ज़ल के मुख़ालिफ़ अक्सर इस सिन्फ़ की यह कहकर, मुख़ालफ़त करते हैं कि ‘‘ग़ज़ल इसलिए हमारे काम की नहीं, क्योंकि ये अवामी आर्ट में शामिल नहीं।’’ मजरूह सुल्तानपुरी, ग़ज़ल के इन मुख़ालफ़ीनों को जवाब देते हुए कहते, ‘‘ये दुरुस्त नहीं है।’’ उनकी दलील होती कि ‘‘क्योंकि, ग़ज़ल को हमने उसके लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर हम उसे इस्तेमाल करते और नाकामयाब हो जाते, तब ये बात कही जा सकती थी।
ख़याल में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। हर वक़्त आदमी लेक्चर देने के या मंतिक़ी (तार्किक) बहस करने के मूड में नहीं होता। बाज़ जुजबी (कोई-कोई) चीजे़ं ऐसी होती हैं, जिन्हें बयान करने के लिए ग़ज़ल की ज़रूरत है। ग़ज़ल उन जज़्बात को दो मिसरों में बयान करती है। ये ठीक है कि इस दौर में नज़्म बहुत ज़रूरी है। मगर ग़ज़ल की ज़रूरत नहीं है, ये कहना भी बिल्कुल ग़लत है।’’
मजरूह सुल्तानपुरी ग़ज़ल की अहमियत और उसकी ज़रूरत पर यह कहकर बचाव करते, ‘‘ग़ज़ल फार्म के लिहाज़ से बहुत सेहत-मंद चीज़ है। इस ज़माने में सियासी चीजे़ं ज़रूरी तौर पर ग़ज़ल में कही जा सकती हैं। और इस तरह से कही जा सकती हैं कि दूसरों को मुतास्सिर किया जा सके। यही वजह है कि ग़ज़ल की अहमियत अपनी जगह पर है। और इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।’’
ग़ज़ल के विरोधी इस विधा पर यह इल्ज़ाम लगाते कि ‘‘ग़ज़ल, खु़र्दा अंदेशी है और खु़र्दागोई। यानी छोटा सोचना और छोटा-छोटा कहना।’’ ग़ज़ल के इन विरोधियों को मजरूह का कड़ा जवाब होता, ‘‘ये ऐतराज़ नज़्म पर भी हो सकता है। नज़्म में भी बसा-औक़ात (अक्सर) एक छोटे से ख़याल को बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। इश्क़-ओ-आशिक़ी के सिलसिले में माशूक़ के आने और जाने पर नज़्में भी मौजूद हैं।’’
अपनी बात को मनवाने के लिए उसके हक़ में उनकी दलील होती, ‘‘अच्छी ग़ज़ल में हमेशा एक मूड मिलता है। मसलन अगर हम ग़मगीन (उदास) हों तो हर चीज़ ग़मगीन नज़र आती है। दरख़्त, दीवार, ग़रज़ की हर चीज़ पर ग़मगीनी का असर होता है। ऐसी हालत में ग़ज़लें कही जाती हैं, तो उनमें एक मूड मिलता है।’’ मिसाल के तौर पर शायर मीर तक़ी मीर की एक मशहूर ग़ज़ल को देखिए,
हमारे आगे तिरा जब किसू ने नाम लिया
दिल-ए-सितम-ज़दा को हम ने थाम थाम लिया
मिरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में
तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया।
मीर तक़ी मीर की इस ग़ज़ल में ग़ुस्सा है। और ग़म और ग़ुस्से में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ग़ज़ल के बारे में मजरूह सुल्तानपुरी की कैफ़ियत थी, ‘‘अगर अहम रवायती और इस्तलाही (पारंपरिक) तारीफ़ से हटकर तकनीकी तौर पर देखें, तो हमें मालूम होगा कि ग़ज़ल दो मिसरों का नाम है। लेकिन एक ही शेर सुनकर न सुनने वाला ख़ु़श होता है और न कहने वाला। इसलिए तरतीब देकर ग़ज़ल कहा जाता है। हक़ीक़तन दो मिसरे ही ग़ज़ल होते हैं।’’
मजरूह दीगर शायरों से किस तरह से ज़ुदा और ख़ास थे, गर इसे जानना है, तो उनके समकालीन एक और बड़े शायर अली सरदार जाफ़री की इस बात पर ग़ौर फ़रमाएं, जिसमें मजरूह सुल्तानपुरी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने लिखा था,‘‘एक और ख़ुसूसियत जो मजरूह को आम ग़ज़ल-गो शायरों से मुम्ताज़ करती है, यह है कि उसने समाजी और सियासी मौज़ूआत को बड़ी कामयाबी के साथ ग़ज़ल के पैराया (शैली) में ढाल लिया है। आम तौर पर ग़ज़ल-गो शायर समाजी और सियासी मौज़ूआत के बयान में फीके-सीठे हो जाते हैं या उनका अन्दाजे़-बयां ऐसा हो जाता है कि नज़्म और ग़ज़ल का फ़र्क बाक़ी नहीं रहता। मजरूह के यहां यह बात नहीं है।’’
मिसाल के तौर पर उनकी एक नहीं, ऐसी कई ग़ज़लें हैं जिनमें उन्होंने समाजी और सियासी मौज़ूआत को कामयाबी के साथ उठाया है। इनमें उनके बग़ावती तेवर देखते ही बनते हैं। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में ये ग़ज़लें, नारों की तरह इस्तेमाल हुईं।
सितम को सर-निगूं, ज़ालिम को रुसवा हम भी देखेंगे
चल ऐ अज़्मे बग़ावत चल, तमाशा हम भी देखेंगे
अभी तो फ़िक्र कर इन दिल से नाज़ुक आबगीनों की
ब-फै़ज़-ए-अम्न फिर साग़र में दरिया हम भी देखेंगे
निग़ारे-चीं का घायल तोड़ता है दम सरे-मक़तल
बचा ले आके एजाज़-ए-मसीहा हम भी देखेंगे
ज़बीं पर ताज-ए-ज़र पहलू में ज़िंदॉं, बैंक छाती पर
उठेगा बेकफ़न कब ये जनाज़ा हम भी देखेंगे।