जाहिद खान
साहिर लुधियानवी का शुरुआती दौर, देश की आज़ादी के संघर्षों का दौर था। लेखक, कलाकार और संस्कृतिकर्मी अपनी रचनाओं एवं कला के ज़रिए आज़ादी की अलख़ जगाए हुए थे। गोया कि साहिर भी अपनी शायरी से यही काम कर रहे थे। उनकी एक नहीं कई ग़ज़लें हैं, जो अवाम को अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने की आवाज़ देती हैं। एक ग़ज़ल में वे कहते हैं,‘‘सरकश बने हैं गीत बग़ावत के गाये हैं/बरसों नए निजाम के नक्शे बनाये हैं।’’ तो दूसरी ग़ज़ल में वे कहते हैं,‘‘एहसास बढ़ रहा है हुक़ूक़-ए-हयात का/पैदाइशी हुक़ूक़-ए-सितमपर्वरी की खैर।’’ साहिर की इन रचनाओं में वर्ग चेतना स्पष्ट दिखलाई देती है। अपने हक़, हुक़ूक़ के लिए एक तड़प है, जो उनकी शायरी में मुख़र होकर नुमायां हुई है।
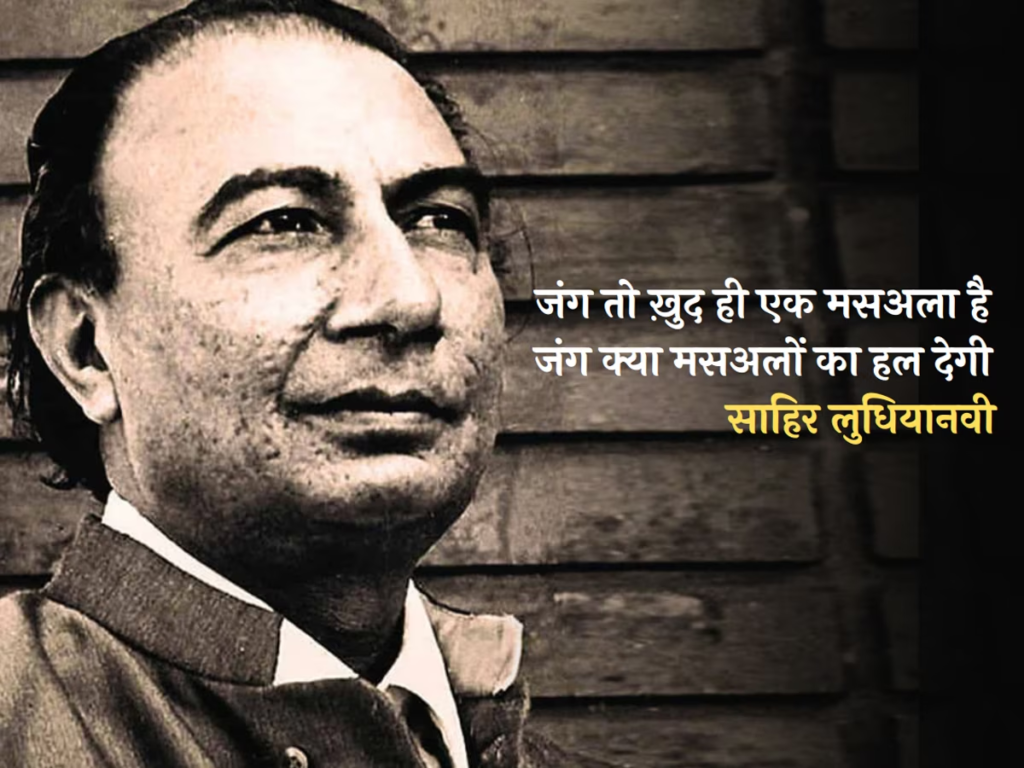
तरक़्क़ीपसंद तहरीक से जुड़े हुए तमाम रचनाकारों की तरह साहिर का भी मानना था कि मज़दूर और किसान ही देश में बदलाव की इबारत लिखेंगे। यही वजह है कि वे अपनी रचनाओं में इन्हीं का आह्वान करते हुए लिखते हैं,‘‘जश्न बपा है कुटियाओं में, ऊंचे एवा कांप रहे हैं/मज़दूरों के बिगड़े तेवर, देख के सुल्तां कांप रहे हैं/जागे हैं इफ़्लास के मारे, उट्ठे हैं बेबस दुखियारे/सीनों में तूफ़ां का तलातुम, आंखों में बिजली के शरारे।’’ अपनी इंक़लाबी ग़ज़लों और नज़्मों की वजह से साहिर लुधियानवी का नाम थोड़े से ही अरसे में उर्दू के अहम शायरों की फ़ेहरिस्त में शामिल हो गया। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजाज़, अली सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, मख़दूम की तरह वे भी घर-घर में मक़बूल हो गए। नौजवानों में साहिर की मक़बूलियत इस कदर थी कि कोई भी मुशायरा उनकी मौज़ूदगी के बिना अधूरा समझा जाता था। ‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें’ साहिर लुधियानवी की वह किताब है, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस किताब से उन्हें अवाम की मुहब्बत मिली, तो नक़्क़ादों से जी भरकर तारीफ़। इस शानदार मजमूए पर उन्हें कई अदबी ईनाम मिले। जिनमें ‘सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार’, ‘उर्दू अकादमी पुरस्कार’ और ‘महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार’ भी शामिल है। ‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें’ किताब में उनकी ज़्यादातर नज़्में संकलित हैं और ये सभी नज़्में एक से बढ़कर एक हैं। एक लिहाज़ से देखें, तो ‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें’ साहिर की प्रतिनिधि किताब है। शीर्षक नज़्म ‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें’ में साहिर के जज़्बात क्या खू़ब नुमायां हुए हैं, ‘‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें, कल के वास्ते/वरना यह रात, आज के संगीन दौर की/डस लेगी जानो-दिल को कुछ ऐसे, कि जान-ओ-दिल/ता उम्र फिर न कोई हंसी ख़्वाब बुन सके।’’ साहिर की इस नज़्म को ख़ूब मक़बूलियत मिली। ग़ुलाम मुल्क में नौजवानों को यह नज़्म अपनी सी लगी। एक ऐसा ख़्वाब जो उनका भी है। जैसे मुस्तक़बिल के लिए उन्हें एक नई मंज़िल मिल गई।
किताब ‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें’ में ही साहिर लुधियानवी की नज़्म ‘परछाइयां’ शामिल है। यह उनकी पहली तवील नज़्म है। ‘परछाइयां’ उनकी पसंदीदा नज़्मों में से एक थी। जब साहिर मुशायरे में ये नज़्म पढ़ते, तो हजारों का मज़मा इसे दम साधे सुनता रहता। तरक़्क़ीपसंद तहरीक के बानी सज्जाद ज़हीर भी साहिर की इस नज़्म पर फ़िदा थे। हमीद अख़्तर, जो साहिर के अजीज दोस्त थे, के नाम एक ख़त में उन्होंने लिखा था,‘‘तुम्हारे दोस्त ने ऐसी आला दर्जे की नज़्म लिखी है, जो मुद्दतों याद रहेगी।’’ ‘परछाईयां’, दुनियावी अमन की हिमायत में जंग के मौजू़अ पर लिखी गई, एक बेहतरीन नज़्म क़रार दी जाती है। सोवियत यूनियन और अमरीकी ब्लॉक के दरमियान जारी शीत युद्ध इस नज़्म का बैकग्राउंड है।
ये नज़्म सभी को इंसानियत और भाईचारे का सबक़ देती है। जंग पर सवाल उठाती है। साहिर के मुताबिक़ जंग से सिर्फ़ तबाही और बर्बादी के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। इस लंबी नज़्म की चंद लाइनों पर ख़ुद ही ग़ौर फ़रमाएं, ‘‘चलो कि चल के सियासी मुक़ामिरों से कहें/कि हम को जंग—ओ-जदल के चलन से नफ़रत है।/जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास न आए,/हमें हयात के उस पैरहन से नफ़रत है।” बग़ावत और वतनपरस्ती में डूबी हुई इस पूरी नज़्म में ऐसे कई उतार-चढ़ाव हैं, जो पाठकों को बेहद प्रभावित करते हैं। ‘परछाइयां’ के अलावा ‘खू़न फिर ख़ून है !’, ‘मेरे एहद के हसीनों’, ‘जवाहर लाल नेहरू’, ‘ऐ शरीफ़ इन्सानों’, ‘जश्न-ए- ग़ालिब’ ‘गांधी हो या ग़ालिब हो’, ‘लेनिन’ और ‘जु़ल्म के ख़िलाफ़’ जैसी शानदार नज़्में इसी किताब में शामिल हैं।
यह किताब वाक़ई साहिर का शाहकार है। साहिर लुधियानवी की शुरुआती नज़्में यदि देखें, तो दीगर इंक़लाबी शायरों की तरह उनकी नज़्मों में भी ब्रिटिश हुकू़मत के ख़िलाफ़ एक ग़ुस्सा, एक आग है। साहिर की एक नहीं, कई ऐसी नज़्में हैं, जो उस वक़्त वतन परस्त नौजवानों को आंदोलित करती थीं। नौजवान इन नज़्मों को गाते हुए, गिरफ़्तार हो जाते थे। मसलन ‘‘तुमने जिस खू़न को मक़्तल में दबाना चाहा/आज वह कूचा-ओ-बाज़ार में आ निकला है/कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर/खू़न चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से/सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से।’’ (नज़्म-‘ख़ून फिर ख़ून है !’)
लाखों लोगों की क़ुर्बानियों और लंबी जद्दोजहद के बाद, साल 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के मतवालों और तरक़्क़ीपसंद अदीबों ने जिस मुल्क का तसव्वुर किया था, आज़ादी के चंद दिनों बाद ही उनका वह ख़्वाब टूटा। सैद्धांतिक तौर पर भले ही देश लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया, पर व्यावहारिक तौर पर उसमें कई बुराइयां आ गईं। आर्थिक आज़ादी और समानता के सवाल, अनसुने रह गए। मज़हब के नाम पर मुल्क में हिंदू-मुस्लिम के बीच टकराव और लड़ाइयां होने लगीं। जा़हिर है कि ऐसे माहौल में तरक़्क़ीपसंद अदीब कहां ख़ामोश रह जाने वाले थे। सच्चा लेखक, संस्कृतिकर्मी चुप बैठ सकता भी नहीं। प्रतिकूल हालात में ही मालूम चलता है कि उसकी पक्षधरता कहां है ?
वे किसके साथ खड़े हैं? ज़ेहनी तौर पर साहिर लुधियानवी आर्थिक आज़ादी के तरफ़दार थे। जिसका स्पष्ट रूप उनके नज़दीक सोशलिज्म था। अपने एक इंटरव्यू में खु़द उन्होंने यह बात क़बूली थी। साहिर अपनी एक नज़्म में मुल्क के हुक्मरानों से ख़िताब करते हुए कहते हैं,‘‘आओ ! कि आज ग़ौर करें इस सवाल पर/देखे थे हमने जो, वह हंसी ख़्वाब क्या हुए/दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफ़्लास क्यों बढ़ा/खुशहाली-ए-अवाम के असबाब क्या हुए ?/……..जमहूरियत-नवाज़, बशर दोस्त, अमन ख़्वाह/ख़ुद को जो ख़ुद दिए थे वह अल्क़ाब क्या हुए/मज़हब का रोग आज भी क्यों ला-इलाज है/वह नुस्ख़ा-हाए-नादिर—ओ-नायाब क्या हुए।’’ (नज़्म-‘26 जनवरी’)
आज़ादी के बाद कहने को हमारे मुल्क में हर शोबे में तरक़्क़ी हुई। इंसान चांद और मंगल तक जा पहुंचा। लेकिन आज़ादी के संघर्ष में जो जीवन मूल्य हमने अपनाए थे और आज़ादी के बाद जिन संवैधानिक मूल्यों पर हमारी जम्हूरियत क़ायम है, आहिस्ता-आहिस्ता उन मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। गांधी के मुल्क में उनका ही फ़लसफ़ा आज हाशिए पर है। गांधी के नाम पर तमाम हुकूमतें ढोंग तो करती हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलने को तैयार नहीं। भारतीय संस्कृति के नाम पर जनता के ऊपर ज़बर्दस्ती इकहरी संस्कृति थोपी जा रही है। साहिर लुधियानवी इन कारगुज़ारियों के बरख़िलाफ़ थे।
उन्होंने अपनी नज़्मों में इसकी हमेशा मुख़ालफ़त की। नये निज़ाम में भी उनके बग़ावती तेवर नहीं बदले। गांधी शताब्दी और ग़ालिब शताब्दी के अंत पर उन्होंने बड़ी ही तल्ख़ी और ग़ुस्से से अपनी नज़्म ‘गांधी हो या ग़ालिब हो’ में लिखा, ‘‘गांधी हो या ग़ालिब हो/ख़त्म हुआ दोनों का जश्न/आओ, इन्हें अब कर दें दफ़्न/ख़त्म करो तहज़ीब की बात, बन्द करो कल्चर का शोर/सत्य, अहिंसा सब बकवास, हम भी क़ातिल तुम भी चोर।’’
आज भले ही साहिर लुधियानवी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी ग़ज़लें, नज़्में और नग़में मुल्क की फ़िज़ा में गूंज-गूंजकर इंसानियत और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे शानदार शायर, नग़मा निगार कभी मरते नहीं, बल्कि मरकर अमर हो जाते हैं। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़्मों और नग़मों में मुल्क और अवाम के लिए, जो समाजवादी ख़्वाब बुना था, अफ़सोस ! आज भी उस ख़्वाब की ताबीर नहीं हुई है। आज़ भी वह ख़्वाब हमें प्रेरित करता है और आगे भी करता रहेगा,‘‘आओ कि कोई ख़्वाब बुनें, कल के वास्ते’’
कभी ख़ुद पे कभी हालात पे रोना आया
बात निकली तो हर इक बात पे रोना आया
ग़म और ख़ुशी में फ़र्क़ न महसूस हो जहां
मैं दिल को उस मक़ाम पे लाता चला गया
अपनी तबाहियों का मुझे कोई ग़म नहीं
तुम ने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी
ले दे के अपने पास फ़क़त इक नज़र तो है
क्यूं देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम
अभी न छेड़ मोहब्बत के गीत ऐ मुतरिब
अभी हयात का माहौल ख़ुश-गवार नहीं
हम ग़म-ज़दा हैं लाएं कहां से ख़ुशी के गीत
देंगे वही जो पाएंगे इस ज़िंदगी से हम