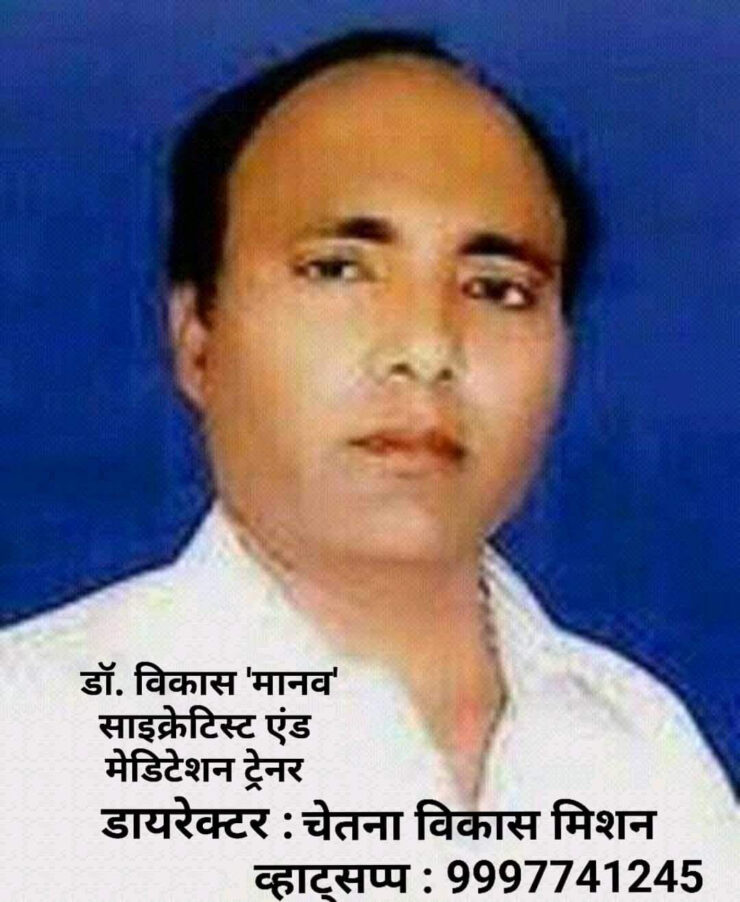डॉ. विकास मानव
चेतन मन की अवस्था को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मन की जिस अवस्था में हम दिन-रात काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, उठते-बैठते, चलते-फिरते, जागते हैं, वह है–चेतन मन की अवस्था। अर्ध चेतन मन की अवस्था में व्यक्ति चेतन अवस्था से ज्यादा सच्चा और ईमानदार हो जाता है, वह बेहोशी में कुछ बडबडाता है, नशे की स्थिति में कुछ बोलता है–जो अधिकतर सच्चाई के निकट का होता है।
ऐसी बेहोशी या नशे की दशा से मुक्त होने पर उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहता क्योंकि उसका बोलना और कुछ करना उसके sub-conscious state of mind के क्षेत्र का विषय होता है जो होश की स्थिति में गायब हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह नहीं है कि वह झूठ बोल रहा है, बल्कि यह है कि उसके मन का आयाम ही बदल गया है।
होश में आने पर उसके मन का आयाम चेतन हो जाता है। अवचेतन या अचेतन मन की अवस्था यदि और गहरी और बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ऐसी स्थिति में फिर उसके चेतन अवस्था में लौटने की संभावना नाममात्र की ही रह जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत गहराई के अन्तराल में सम्मोहन विधि द्वारा ले जाता है तो वह अपने जीवन के पीछे की अवस्था में चला जाता है, युवावस्था, किशोरावस्था, शैशवास्था यहाँतक कि जन्म के समय की भी अवस्था।
ज्यादा सावधानी के द्वारा तो वह पिछले जन्म में और कई जन्म पीछे चला जाता है। लेकिन अर्ध चेतन मन की अवस्था से ज्यादा कहीं गहरी अवस्था होती है अचेतन मन की अवस्था।मन की एक विशेषता या कहें कि कमी यह है कि वह किसी वस्तु को देखता है तो उसे तोड़कर देखता है। मन की इस प्रक्रिया में जीवन खण्ड-खण्ड हो जाता है।
हमारा मन जिस वस्तु को देखता है, चाहे वह बडी हो या छोटी हो, उसे दो हिस्सों में बांटकर ही देखता है। एक साथ एक वस्तु को कभी नहीं देख पाता। वह देखेगा तो एक हिस्सा छिपा रहेगा। आजतक किसी व्यक्ति के मन ने किसी भी वस्तु को सम्पूर्णता में नहीं देखा। इसलिए जहाँ भी मन होगा, अपूर्ण अनुभव ही होगा क्योंकि मन की एक सीमा होती है। सीमा से परे जाकर वह कोई कार्य नहीं कर सकता। उसका अनुभव अपूर्ण होगा, विचार अपूर्ण होगा, अपूर्ण ही दृष्टि होगी। इसलिए मन के द्वारा हम जो निर्माण करते हैं, वह निर्माण काल्पनिक हो जाता है।
हम लोग जो फेसबुक पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वहस करते हैं और दावा करते हैं हम सही हैं, तुम गलत हो। हम अ-मन की अवस्था में हैं, हम आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, हम सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत और लोक-लोकान्तरों में भ्रमण करते हैं। हमारी विधि सही है, उसमे अमुक विशेषता है। तुम्हारी विधि अपूर्ण है, उसमें अमुक कमी है, मैं तुम्हारी विधि से सहमत नहीं हूँ।
उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अरे ! इसमें कौन सी खास बात कह दी आपने ? जब शास्त्रों में एकता नहीं है, दर्शन में एकता नहीं है, तो व्यक्ति की बात में एकता कैसे हो सकती है ? साम्य कैसे हो सकता है ? अरे भाई ! विषमता ही तो सृष्टि की विशेषता है, असमानता ही तो विश्व की जान है। विभिन्नता ही, मतभिन्नता ही तो प्रकृति का अस्तित्व है। जहाँ भिन्नता समाप्त हुई, वहीँ प्रलय निश्चित है।
त्रिगुणात्मिका प्रकृति की साम्यावस्था में ही तो प्रलय होती है। हम सब जानते हैं–हमारे विचार एक से नहीं हो सकते, हमारे कार्य-आचरण एक से नहीं हो सकते, हमारे मन एक से नहीं हो सकते। यहाँ तक कि हमारे शरीरों की बनावट भी एक सी नहीं हो सकती। हमारे चेहरे एक से नहीं हो सकते, नाक, कान, नेत्र, हाथ, पैर सब अलग अलग होते हैं। तो दो व्यक्तियों के विचार, सिद्धान्त सोचने-विचारने के आयाम भी एक से कैसे हो सकते हैं? इसलिए मन से निर्मित संसार में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन हैं, वे एक तरह से व्यर्थ हैं, पूर्णता की ओर ले जाने वाले नहींहैं।
संसार में दो प्रकार के लेखन हुए हैं–पहला वह जो उन लोगों के वचन हैं जिन्होंने मन के अस्तित्व से अलग होकर आत्मा द्वारा पूर्ण को जाना है। दूसरा वह है जो उन लोगों के वचन हैं जिन्होंने मन को व्यवस्थित कर, शिक्षित कर, अध्ययन से, विचार से, चिंतन-मनन से, तर्क से, अनुभवों से मन को विकसित किया है और फिर जगत और माया को लिपिबद्ध किया। पहला लेखन ‘धर्म’ कहलाया और दूसरा लेखन ‘दर्शन’ या ‘शास्त्र’ कहलाया।
धर्म और दर्शन में यही अन्तर है और यही कारण है कि जितने भी शास्त्र हैं, वे सब अधूरे हैं। वे कितनी भी ऊँची बात कहें, लेकिन होगी वह ‘मन की ही बात’।
अरस्तू कितना ही कहे, प्लेटो कितना ही कहे, कांट और हीगल भी कितना ही कहें, वे सब उनके विचार हैं, निष्कर्ष हैं, अनुभव है, लेकिन अनुभूति नहीं। मन से जन्म लेता है-दर्शन और मन के ऊपर उठ जाने पर अर्थात्–अ-मन की अवस्था में जो उत्पन्न होता है, वह है धर्म। अ-मन की स्थिति में जो घटित होता है–वह है आत्मा की क्रिया और मन की उपस्थिति में जो घटित होता है–वह है–प्रतिक्रिया।
प्रतिक्रिया क्रिया को देखकर जानबूझ कर की जाती है, इसलिए उसमें दुर्भावना आ जाती है, उसके उद्देश्य और प्रयोजन कलुष से भर जाते है। भारत का सनातन धर्म मन से ऊपर उठकर अ-मन की अवस्था में उत्पन्न हुआ है। जबकि संसार के अन्य धर्म(उन्हें तो सही मायने धर्म ही नहीं कहा जा सकता) क्रिया की प्रतिक्रया स्वरुप उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वे सब लड़ाते हैं। सनातन धर्म जोड़ता है–मानव से मानव को, मानव से प्राणिमात्र को और मानव से जड़ वस्तु को भी। सनातन धर्म के अनुसार कण भी व्यर्थ नहीं है, कण-कण में ईश्वर है।
अन्य धर्म आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए शास्त्र नहीं, शस्त्र उठा लेते हैं। दर्शन में संघर्ष है, शास्त्रों में संघर्ष है, विचारों में संघर्ष है, क्रियाओं में संघर्ष है क्योंकि ये सब मन के धरातल से जन्मे हैं।
धर्म उसी व्यक्ति के द्वारा जन्म लेता है, जिसका मन खो गया है, जो पूर्णत्व को जानता है। लेकिन जो धर्म को समझने वाले लोग हैं, वे मन से समझते हैं। उनके पास इसके आलावा और कोई मार्ग नहीं है। यही कारण है कि मन से समझा जाने वाला धर्म सांप्रदायिक युद्ध का कारण बनता है। धर्म के स्वरुप और वास्तविक ध्यान के स्वरुप को जानने-समझने के लिए अ-मन की स्थिति को उपलव्ध होना अनिवार्य है।
*कारण शरीर :*
सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को सूक्ष्मलोक में भोग भोगते हुए यदि स्थूल शरीर उपलब्ध हो गया तो फिर वह स्थूल शरीर के माध्यम से शेष कर्मफलों को भोगता है जीवनकाल में। इसी को कहते हैं–‘नियति’ अथवा ‘प्रारब्ध’।गर्भ में स्थित स्थूल भ्रूण में सूक्ष्म शरीर का प्रवेश एक अपूर्व प्राकृतिक घटना है जो अपने आप में स्वचालित है।
जैसे जल अपने स्वभाव के अनुसार अपने- आप नीचे की ओर प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी अपने योग्य और अनुकूल स्थूल शरीर को हो जाता है उपलब्ध।
आत्मा को स्थूल शरीर की प्राप्ति तथा भौतिक जीवन जीने के लिए सूक्ष्म शरीर आवश्यक है। सूक्ष्म शरीर के अभाव में आत्मा न स्थूल शरीर को प्राप्त कर सकती है और न तो भौतिक जीवन जीने को हो सकता है उसे उपलब्ध।
यदि किसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाय तो आत्मा के लिए स्थूल शरीर प्राप्त करना पूर्णतया असम्भव है। सूक्ष्म शरीर का विसर्जन होने पर दो अपूर्व आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं:पहली आध्यात्मिक घटना यह कि आत्मा सदैव के लिए आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाती है। जन्म और मृत्यु उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। दोनों का अभाव हो जाता है।
सदैव के लिए स्थूल शरीर से मुक्त हो जाती है वह और सदैव के लिए स्थूल शरीर की यात्रा समाप्त हो जाती है और उपलब्ध हो जाती है सदैव के लिए कारण शरीर को।
कारण शरीर को ‘लिंग शरीर’ भी कहते हैं। कारण शरीर एक ऐसे केन्द्रबिन्दु पर है जिसके एक ओर है–सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और दूसरी ओर है– मनोमय शरीर और आत्म शरीर। कारण शरीर को उपलब्ध होने पर आत्मा का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह जाता है–न स्थूल शरीर से और न तो सूक्ष्म शरीर से।
सूक्ष्म शरीर ही जन्म, जीवन और मरण का कारण है। जब वह भी स्थूल शरीर की तरह नष्ट हो जाता है तो मनुष्य के लिए फिर मानव शरीर में जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं रहता।
दूसरी अपूर्व आध्यात्मिक घटना यह घटती है कि आत्मा और परमात्मा के बीच जो अन्तर था, जो सीमा थी और जो थी दूरी, वह सदैव के लिए हो जाती है समाप्त। कारण शरीरधारी आत्मा के लिए अधोमार्ग बन्द हो जाता है सदैव के लिए और उर्ध्वगामी मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
ब्रह्माण्ड के छः भाग ‘शिवक्षेत्र’ है। कारण शरीर की उर्ध्वगामी यात्रा शिवक्षेत्र की यात्रा है। उस यात्रा की सीमा पर पहुँच कर आत्मा कारण शरीर को त्याग कर मनोमय शरीर को धारण कर लेती है और उसके द्वारा यात्रा करती है फिर ‘विष्णु क्षेत्र’ की और जब विष्णु क्षेत्र की सीमा समाप्त हो जाती है तो उस अवस्था में आत्मा अपने निज शरीर अर्थात् आत्म शरीर द्वारा ‘ब्रह्म क्षेत्र’ की करती है यात्रा।
इस यात्रा के पूर्ण हो जाने पर आत्मा को जो शरीर उपलब्ध होता है, वह है–ब्रह्माण्डीय शरीर या ब्रह्म शरीर (cosmic body) है यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि सूक्ष्म शरीर तक आत्मा की अधोगामी यात्रा है और शरीर को जब सूक्ष्म शरीर के नष्ट होने के बाद उसे कारण शरीर उपलब्ध होता है तो उसकी उर्ध्वगामी यात्रा होती है शुरू।
यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो जितनी भी योग-तंत्र की साधनाएं हैं, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य है सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व का नाश। न सूक्ष्म शरीर रहेगा और न तो फिर फंसना पड़ेगा भवचक्र के मायाजाल में। न जन्म होगा और न तो होगी फिर मृत्यु ही। हमेशा के लिए छूट जायेगा स्थूल शरीर का बन्धन। समस्त साधनाओं की सबसे बड़ी और अन्तिम उपलब्धि है–सूक्ष्म शरीर का नाश। इसमें सन्देह नहीं कि शुरू से लेकर अबतक इस संसार में जितने भी सिद्ध, महात्मा, योगी और सन्त साधक हुए हैं, उन सभी का एकमात्र का उद्देश्य रहा है सूक्ष्म शरीर का विसर्जन और उनका जब यह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वे निकल पड़ते हैं उर्ध्वयात्रा पथ पर।
पितर लोक:नित्य और अनित्य पितर गण:कारण शरीर में तीन भाग प्राणतत्व और एक भाग मनस्तत्व रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की भौतिक वासना नहीं रहती। केवल रहता है ‘मैं’ का भाव अर्थात् ‘मैं’ का बोध और उस ‘मैं’ के भाव में पिछले कई जन्मों के रहते हैं आध्यात्मिक संस्कारों के मूलतत्व जिससे आत्मा को उर्ध्वलोक में जाने के लिए प्राप्त होती है गति भूमण्डल प्रथम वसुमंडल है।
पहले और दूसरे वसुमंडल की सीमा पर भूलोक जैसे प्राकृतिक वातावरण का एक सूक्ष्मलोक है जिसे पितर लोक कहते हैं। पितर लोक दो भागों में विभक्त है जिनको उर्ध्वभाग और अधोभाग कहते हैं। उर्ध्वभाग में नित्य पितरगण निवास करते हैं और अधोभाग में निवास करते हैं–अनित्य (नैमित्तिक) पितरगण।
ऊर्ध्व भाग में सदैव सूर्योदय रहता है लेकिन अधोभाग में सूर्योदय रहता है केवल पन्द्रह दिन। उन्हीं पन्द्रह दिनों को ‘पितृपक्ष’ की संज्ञा दी गयी है। पितृपक्ष के अतिरिक्त (350) दिनों में वहां रात्रि रहती है। सम्पूर्ण अधोभाग रात्रि के अन्धकार में सदैव लीन रहता है। नित्य पितरगण पितर लोक के मूल निवासी हैं। वे सदैव अपने लोक में बने रहते हैं, न तो ऊपर के लोकों में जाते हैं और न ही नीचे के लोकों में आते हैं। वे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं।
उनका कार्य है–अनित्य पितर लोक के निवासियों को उनके स्तर के अनुकूल व्यवस्था का अंग बनाना, व्यवस्था में उनसे सहयोग लेना और अनित्य पितर लोक के निवासियों को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करना और उन्हें अगले जन्म के लिए तैयार करने के लिए विशेष शिक्षण देना।(एक प्रकार से वह सुधार गृह जैसे स्थल का रूप है)। उनका शरीर अग्नितत्व प्रधान और शरीर का रंग तांबे जैसे होता और आकार-प्रकार मनुष्य जैसा ही होता है।
वे श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। सौम्य, शान्त, गम्भीर और आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका। उनके अधिपति को ही धर्मराज की संज्ञा दी गयी है। वह फ़न उठाये सर्प का रत्नजड़ित मुकुट धारण करते हैं। नित्य पितर गण वास्तव में समस्त मानव जाति के लिए कल्याण कारी भावना रखते हैं। पितर लोक के अधोभाग अनित्य (नैमित्तिक) पितरों के निवास स्थान हैं।
अनित्य पितरगण कौन हैं ? मृत्योपरान्त आत्मा कुछ समय के लिए वासना लोक अथवा प्रेतलोक में निवास करती है, भले ही वह आत्मा किसी भी कोटि की क्यों न हो। वासना क्षय होने के पश्चात् वह सीधे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है और तब तक वहां निवास करती है जब तक उसे पार्थिव जगत में अपने संस्कारों के अनुकूल गर्भ उपलब्ध नहीं हो जाता। गर्भ कब उपलब्ध होगा ?–यह निश्चित नहीं है। यदि दीर्घ काल तक वह जन्म न ले सकी तो वह पितर बन जाती है और पितर लोक के अधोभाग में निवास करने के लिए चली जाती है। उसे ‘पित्रात्मा’ कहते हैं।
यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि देवता से अधिक पितर मनुष्य के निकट हैं। देवता से अधिक सहायता भी करते हैं वे अपने परिवार की। परिवार के सदस्यों की रक्षा करना, रोग-शोक से उनको दूर रखना, वंश- परंपरा को बनाये रखना, शुभ और मांगलिक कार्यों में आने वाले विघ्न-बाधाओं का निवारण करना पित्रात्मा का कर्तव्य होता है।
अपने परिवार से वे केवल यही आशा रखतीं हैं कि परिवार के लोग उन्हें याद रखें, इस निमित्त ब्राह्मण भोजन, दान-पुण्य आदि कार्य उनकी पुण्य तिथि पर करें। परिवार वाले सभी ऐसा नहीं करते हैं तो पित्रात्मा अपने परिवार को तरह-तरह से कष्ट पहुंचाती है, दुःख देती है–इसी को ‘पितरबाधा’ या पित्र -दोष कहते हैं। जिस परिवार में पितरबाधा रहती है, वह परिवार किसी न किसी प्रकार का कष्ट, दुःख, क्लेश भोगता ही रहता है।.
सदस्यों में आपसी मतभेद, तनाव, कोई न कोई व्याधि बराबर बनी रहती है परिवार में। अपने पराये हो जाते हैं, मित्र भी शत्रु बन जाते है, पड़ोसियों से, व्यवहरियों से, रिश्तेदारों से सम्बन्ध ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब ग्रहों के प्रतिकूल होने से होता है। कुछ सीमा तक यह सत्य है, पर अधिकांश मामलों में यह सब पितर-दोष के कारण ही होता है। ऐसा करने में उन पितरों का एक ही प्रयोजन होता है कि उनके परिवार के सदस्य केवल उनकी पुण्यतिथि पर कुछ दान-पुण्य, ब्राह्मण-भोजन आदि कर दें। यह भी निर्विवाद सत्य है कि परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पितरों की पुण्यतिथि पर जो भाव पूर्ण और श्रद्धापूर्वक दान-दक्षिणा, भोजन, तर्पण आदि किया जाता है उसका सूक्ष्म अंश पितरों को अवश्य प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार की समृद्धि में सहयोग प्रदान करने लगते हैं।
वंशहीन परिवार की वंशवृद्धि में भी सहायता करने लगते हैं। आज समय तेजी से बदल रहा है। आज की पीढ़ी की सोच बदल गयी है, उनकी आस्था और उनके विश्वास बदल गए हैं। वे यह सब हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुडी हुई गूढ़ रहस्यमयी बातों में विश्वास नहीं रखते। न तो वे इसे जानते हैं और न ही वे इसे मानते हैं। वे न तो उसे जानना चाहते हैं और न तो मानना ही चाहते हैं।
इसी कारण आज समाज के अधिकांश युवावर्ग में हताशा, निराशा, क्लेश, संताप का वातावरण देखने को मिलता है। नयी पीढ़ी के युवा लोग अपने बुजुर्गों की इस बारे में बताई गयी बातों को समझना-जानना तो दूर, उन्हें सुनना भी पसन्द नहीं करते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं कि वे अपने को उनसे ज्यादा प्रगतिशील, समझदार, पढ़ा-लिखा और तथाकथित विज्ञानसम्मत मानते हैं। पर यह उनकी भूल है, यह उनकी छोटी सोच है।
हमारा हज़ारों वर्षों से आध्यात्मिक रूप से समुन्नत भारत और उसकी सांस्कृतिक विरासत आज पाश्चात्य शोध और अनुसन्धान का विषय बन चुका है, नित्य-प्रति कोई न कोई ऐसी खोज हो रही है जो हमारे ऋषियो, मुनियों, सन्तों, साधकों द्वारा जो अतीत में खोजा गया था, आज सब प्रमाणित होकर जगत के सामने आ रहा है जिससे भारत के प्रति अन्य देशों की सोच बदल रही है। इतना ही नहीं, विदेशों (अमेरिका, फ़्रांस, जर्मनी, कनाडा, रूस आदि देशों) में बहुत बड़े पैमाने पर अनुसन्धान हो रहे हैं, जिनके परिणाम से वे देश चमत्कृत हैं।
*सूक्ष्म ध्यान योग :*
लोग जब मनोमय शरीर के द्वारा कुण्डलिनी साधना करते हैं तब उस स्थिति में उनके लिए कुछ भी असम्भव नहीं रह जाता, कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती। वे हज़ारों मील की दूरी पर बैठे किसी भी व्यक्ति के मनोभावों और विचारों को तत्काल जान-समझ सकते हैं।
इतना ही नहीं, एक ही समय में अपने आपको कई स्थानों पर प्रकट भी कर सकते हैं। कुण्डलिनी शक्ति की यह विशेष सिद्धि है।
कुण्डलिनी-साधना क्रम में प्राण, मन और आत्मा की साधना है। जहां तक कुण्डलिनी- योग का प्रश्न है, वह ‘हठयोग’, ‘राजयोग’ और ‘ज्ञानयोग’ का समन्वय रूप है। हठयोग द्वारा प्राण की साधना, राजयोग द्वारा मन की साधना और ज्ञानयोग द्वारा आत्मा की साधना संम्पन्न होती है.
हठयोग का विषय प्राणायाम है। ‘हठ’ शब्द का ‘हकार’ श्वास का और ‘ठकार’ ‘प्रश्वास’ का बोधक है। श्वास का मतलब है –‘प्राण’ और प्रश्वास का मतलब है–‘अपान’। श्वास-प्रश्वास अर्थात्–प्राण और अपान वायु।
दूसरी ओर ‘हठ’ शब्द का प्रयोग ‘इड़ा’ और ‘पिंगला’ नाड़ी के लिए भी किया जाता है। ‘ह’ अथात् ‘इड़ा’ नाड़ी और ‘ठ’ अर्थात् ‘पिंगला’ नाड़ी। श्वास का प्रवाह इड़ा नाड़ी में और प्रश्वास का प्रवाह पिंगला नाड़ी में होने के कारण ही संभवतः ‘हठ’ शब्द का प्रयोग उन दोनों नाड़ियों के लिए किया गया है।
तीसरी महत्वपूर्ण नाड़ी ‘सुषुम्ना’ है। यह नाड़ी शून्य नाड़ी है। शून्य शब्द शक्तिवाचक है। अतः यह शक्तिवाहिनी नाड़ी है। इस नाड़ी में एकमात्र शक्ति का प्रवाह है। यहाँ शक्ति का मतलब ‘चेतना’ से समझना चाहिए। मानव शरीर में कुल 72 हज़ार नाड़ियां हैं। सुषुम्ना मार्ग से शक्ति प्रवाहित होकर चेतना के रूप में उन 72 हज़ार नाड़ियों के जाल में फैली रहती है। प्राणायाम के द्वारा प्राण की साधना हठयोग का मुख्य लक्ष्य है।
राजयोग का विषय है–ध्यान। ध्यान का सम्बन्ध मन से है। ध्यान के द्वारा मन पर अधिकार प्राप्त करना राजयोग का मुख्य लक्ष्य है। ध्यान का मतलब है वैज्ञानिक आधार पर मनुष्य के आतंरिक व्यक्तित्व का आमूल-चूल रूपान्तरण और बाह्य जगत से आन्तर जगत में प्रवेश। यही कारण है कि सभी साधना सम्प्रदायों में ध्यान को स्वीकार किया गया है। संसार में सभी धर्मों में विवाद है। केवल एक बात के सम्बन्ध में विवाद नहीं है और वह है–ध्यान।
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन आदि सभी के सिद्धांत बहुत भिन्न भिन्न हैं लेकिन ध्यान के सम्बन्ध में इस संसार में कोई मतभेद नहीं है। जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से होकर जाता है। परमात्मा तक यदि कभी कोई पहुंचा है तो एकमात्र ध्यान की सीढियां ही साथ देती हैं।
चाहे जीसस हों, चाहे मुहम्मद हों, चाहे महावीर हों और चाहे हों बुद्ध–सभी ध्यान की बात करते हैं।
सुषुम्ना नाड़ी के महत्त्व का पहला कारण यह है कि वह अधो लघुमस्तिष्क में स्थित ‘सहस्रार’ से कुण्डलिनी शक्तिकेंद्र ‘मूलाधार’ को जोड़ती है।
दूसरा कारण यह है कि कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत और चैतन्य होकर इसी नाड़ी मार्ग से ‘सहस्रार’ में प्रवेश करती है जहाँ उसका (शक्तितत्व का) संयोग ‘शिवतत्व’ से होता है जिसे तंत्र की भाषा में ‘सामरस्य महामिलन’ अथवा ‘सामरस्य भाव’ कहते हैं। तंत्र का यही ‘अद्वैत सिध्दिलाभ’ है।.
तीसरा कारण यह है कि इस नाड़ी द्वारा ‘षट्चक्र भेदन’ भी होता है जिसकी सहायता से साधक क्रमिक उन्नति करता है साधना के क्षेत्र में।
चौथा कारण यह है कि सुषुम्ना के भीतर एक और महत्वपूर्ण नाड़ी है जिसे ‘चित्रिणी’ नाड़ी कहते हैं। चित्रिणी नाड़ी ‘ज्ञानशक्ति-वाहिनी’ नाड़ी है। यह कुण्डलिनी से निकलकर लघु मस्तिष्क के केंद्र में उस नाड़ी से जुड़ती है, जो उस केंद्र से निकलकर आज्ञाचक्र में ‘गुह्यनी’ नाड़ी से मिलती है।
चित्रिणी’ नाड़ी ही एक ऐसी नाड़ी है जो ‘अचेतन’ मन को ‘चेतन’ मन से जोड़ती है। इसी नाड़ी-मार्ग से अचेतन मन की अविश्वसनीय शक्तियां अचेतन मन की सीमा लांघकर चेतन मन में कभी-कदा प्रकट हो जाती हैं जिसके चमत्कार देखकर लोग हतप्रभ रह जाते हैं। इसी को ‘सिद्धि’ कहा जाता है। इसके आलावा इसी नाड़ी के द्वारा मानव मस्तिष्क को वह ज्ञानशक्ति प्राप्त होती है जिसका आविर्भाव कुण्डलिनी में होता है और जो मस्तिष्क की रहस्यमयी कोशिकाओं में क्रमशः–मेधा, धी, विवेक, बुद्धि एवं संकल्प आदि शक्तियों को जन्म देती है।
हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी ब्रह्माण्ड के जिस भाग में है, उसे हमारे धर्मग्रंथों में ‘वैश्वानर’ जगत कहते हैं। वैश्वानर जगत तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग में अनेक लोक-लोकान्तर हैं। 5- हमारे चारों तरफ के वायुमण्डल में मानवी विचारों की अदृश्य तरंगों के आलावा उन लोक-लोकान्तरों में निवास करने वाले अज्ञात प्राणियों के विभिन्न प्रकार के विचारों की भी तरंगें बराबर तैरती रहती हैं।
वे अदृश्य तरंगें हमारे अधो लघुमस्तिष्क से लगातार सामूहिक रूप से टकराती रहती हैं जिन्हें हमारा चेतन मन हर क्षण, हर पल ग्रहण करता रहता है। वह जिस माध्यम से ग्रहण करता है, वह है–एकमात्र सुषम्ना नाड़ी। यह सुषम्ना के महत्व का पांचवां कारण है।
सबसे पहले वे अदृश्य तरंगे ब्रह्मरंध्र मार्ग से होकर अधोलघु मस्तिष्क स्थित ज्ञानतन्तु-समूह में प्रवेश करती हैं और वहां से सुषुम्ना मार्ग द्वारा अचेतन मन में प्रविष्ट होती हैं। इतना ही नहीं, वे तरंगे पुनः विचारों में परिवर्तित होकर चेतन मन के द्वारा प्रकट होना चाहती हैं। लेकिन अचेतन मन इसके लिए बाधक बन जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि अचेतन मन बाधा न डाले तो हम उन विचार तरंगों के लगातार आघात से कभी के समाप्त हो गए होते। अगर समाप्त नहीं भी होते तो पागल अवश्य ही हो जाते।
वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि वायुमण्डल में तैर रही विचार तरंगों के अस्तित्व को किसी भी अवस्था में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वैसे उन्हें नष्ट या निष्क्रिय करने के लिए रेडियो और टेलीविजन की तरंगें लगातार प्रयत्नशील रहती हैं।
योग के इस सिद्धांत को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि अचेतन मन भले ही अवरोधक हो लेकिन कभी कदा उसकी सीमा को तोड़कर अच्छे-बुरे बाह्य विचार चेतन मन में प्रकट हो ही जाते हैं। वे जितने ही प्रखर और भावना पूर्ण होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही प्रखर और आवेशमयी होती है।
कभी-कभी देश-काल व पात्र के अनुसार बाह्य विचार ऐसे रहस्यमय ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं जिन्हें हम ‘आन्तर्ज्ञान’ कहते हैं।
बिना इन्द्रिय की सहायता से जो ज्ञान प्राप्त हो, वह ‘आन्तर्ज्ञान’ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति ‘जीवभाव’ में जी रहा है। जीवभाव का मतलब है–व्यक्ति की आत्मा, मन, प्राण और शरीर का जोड़ है। आत्मा से जब मन का सम्बन्ध प्रथम बार सृष्टि क्रम में आने पर जुड़ता है तो उसीके साथ उसमें विचार, भाव, भावना, वासना, कल्पना के तत्व भी मन के माध्यम से आत्मा से जुड़ जाते हैं।
जो जन्म-जन्मान्तर तक उसी के साथ संस्कार बनकर यात्रा करते रहते हैं और अगले जन्म के कारक भी बनते हैं। मन आत्मा की चंचल अवस्था है, वह अस्थिर है और है गतिमान भी। मन ही आत्मा को भी अस्थिर और गतिमान किये हुए है। अब आत्मा जो भी कार्य करती है या करना चाहती है, उसके लिए उसे अपने मन पर निर्भर रहना पड़ता है। मन स्वयं सोच-विचार करता है, भाव और भावना का प्रवाह मन की सतह पर चलता रहता है। लेकिन जब वह कोई कर्म करता है तो वह अपनी स्थूल कर्मेन्द्रियों की सहायता लेता है।
हाथों-पैरों से, मुख से, नेत्रों से, कानों से वह अपने अनुभव प्राप्त कर कर्म संपन्न करता है। कर्म करता है मन और उसका ‘आरोपण’ होता है आत्मा में। अर्थात् मन के द्वारा किये गए अच्छे-बुरे कर्म के लिए आत्मा स्वयम् को उत्तरदायी मान लेती है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के मन को सोचने-समझने और कर्म करने के लिए अपने स्थूल उपकरण (इन्द्रियों) की सहायता लेनी पड़ती है। उसके अनुभव और ज्ञान में इन्द्रियों की भी अपनी व्याख्या जुडी हुई होती है।
इसलिए इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि इन्द्रियों की पहुँच की एक सीमा होती है, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान भी इसीलिए सीमित होता है। उस ज्ञान को पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन, जो ज्ञान बिना इन्द्रियों की सहायता से, बिना मन की सहायता से आत्मा को स्वयं होता है, वही ज्ञान ‘आन्तर्ज्ञान’ होता है। वह ज्ञान त्रिकाल सत्य होता है।
जहां तक प्रकृति का साम्राज्य है, वहां तक मानवी- प्रज्ञा कार्य करती है। प्रकृति और मानवी प्रज्ञा से जो परे है, वही सत्य है और उस सत्य की उपलब्धि आन्तर्ज्ञान से ही सम्भव है। आइंस्टीन का नाम किसने नहीं सुना ? उन्होंने एक बार कहा था कि जब हम जीवन और ब्रह्माण्ड के रहस्यों को जानने का प्रयत्न करते हैं तो मन भय और आशंकाओं से घिर जाता है। पर हमें कभी जिज्ञासाओं को कुंठित नहीं होने देना चाहिए।
मैं मानता हूँ कि सही वैज्ञानिक प्रगति केवल आन्तर्ज्ञान से ही सम्भव है। ज्ञान वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है। फिर भी ज्ञान हमारा वहीँ तक साथ देता है या दे सकता है–जहां तक वह जानता है और सिद्ध कर सकता है। पर एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ मस्तिष्क अचानक बोध के उच्चतर स्तर पर पहुँच जाता है। इस स्थिति को ‘सहजोप्लब्धि’ या आन्तर्ज्ञान–कुछ भी कहा जा सकता है। संसार के सभी महान् अविष्कार मानव प्रज्ञा के आगे की इस रहस्यमयी अनुभूति द्वारा ही सम्भव हुए हैं।
सत्य की खोज योगी भी करता है और वैज्ञानिक भी। मगर दोनों की खोज के मार्ग और साधन भिन्न-भिन्न हैं। जिस तरह की सत्य की खोज में वैज्ञानिक आजकल लगे हुए हैं, वह यथार्थ नहीं है जो हमें आँखों से दिखलायी देता है। यदि बोध- क्षमता के मार्गों को स्वच्छ और निर्मल रखा जाय तो हमें सब कुछ वैसा ही दिखलायी देगा जैसा कि वह वास्तव में है–अनन्त, असीम, अपार। जब तक ऐसा नहीं होता, सत्याभास्, यथार्थता, नित्य-अनित्य–सब एक जैसे प्रतीत होंगे।
हाँ, यहाँ मैं सुषुम्ना नाड़ी के महत्त्व का एक और कारण बतलाता हूँ। जो सूत्र ब्रह्माण्ड से मानव को जोड़ता है और जिस माध्यम से ब्रह्माण्ड में व्याप्त ‘समष्टिरूपा विराट चेतना’ या ‘परम चेतना’ का सम्बन्ध मानव स्थित ‘व्यष्टिरूपा परा चेतना’ से जुड़ता है–वह सूत्र और वह माध्यम एकमात्र ‘सुषुम्ना नाड़ी’ ही है।
कुण्डलिनी साधना के चार क्रम हैं :
प्रथम क्रम में कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है। वह चैतन्य होती है।
द्वितीय क्रम में कुण्डलिनी शक्ति का उत्थान होता है।
तृतीय क्रम में कुण्डलिनी शक्ति द्वारा क्रमशः षट्चक्र भेदन होता है.
चतुर्थ क्रम में उसका ब्रह्माण्ड स्थित ‘शिवशक्ति’ से सामरस्य महामिलन होता है।
इन चारों क्रमों में कुण्डलिनी-शक्ति का एकमात्र उपादान–सुषुम्ना नाड़ी ही है।अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अचेतन मन की असीम अलौकिक शक्ति अर्थात् ‘परामानसिक चेतना’ ही योगतंत्र की एकमात्र कुण्डलिनी शक्ति है। सर्पिणी की कुंडली के आकार के तन्तु में रहने के कारण ही उसे ‘कुण्डलिनी शक्ति’ की संज्ञा दी गयी है। इसीलिए आगमशास्त्र ( तंत्रशास्त्र )में कहा गया है– “कुंडले$प्यास्ति इति कुंडली”।