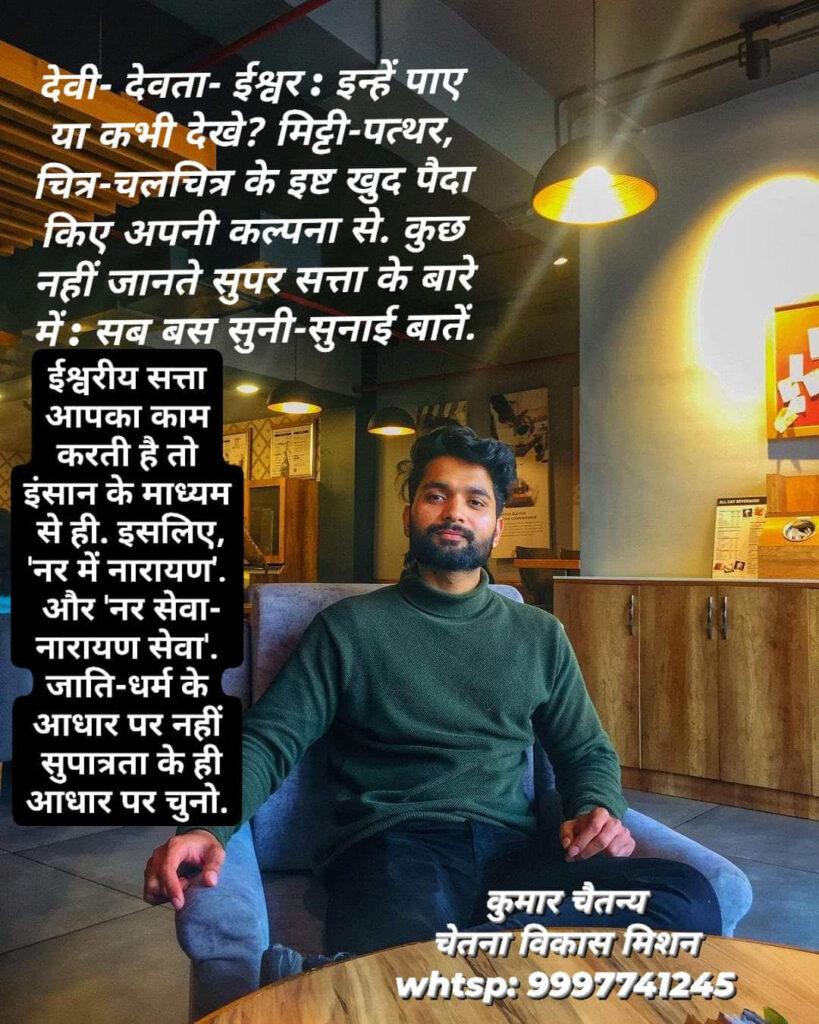(स्वयं प्रकाश की शब्द-संरचना)
~ कुमार चैतन्य
नीलकांत सफर कर रहे थे। चूंकि वह जनता थे, इसलिए थर्ड क्लास में सफर कर रहे थे और चूंकि वह थर्ड क्लास था, इसलिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे का आखिरी कम्पार्टमेंट था। बाकी ट्रेन या तो फस्र्ट थी या शयनयान या आरक्षिक या और कुछ। लगता था, साधारण थर्ड के इस कम्पार्टमेंट को भी पीछे ही पीछे मात्र दयावश या औपचारिकता निभाने के लिए जोड़ दिया गया है। जब ट्रेन कहीं रुकती तो प्लेटफार्म पर बीचोंबीच फस्र्ट के डिब्बे होते जहां चाय, पानी, पान-सिगरेट, फल-फ्रूट, पूछताछ, स्टेशन-मास्टर सब सामने ही होता। साधारण थर्ड अक्सर प्लेटफार्म से बहुत दूर जंगल में रुकता, जहां से हर स्टेशन पर बहुत सारे प्यासे अपने-अपने लोटे-गिलास लेकर वाटरहट की तरफ भागते जो अक्सर सूखी या खाली या बंद होती… तब आगे का कोई नल या प्याऊ बर्र का छत्ता बन जाता। दो-चार पानी पी पाते, चार-छह भर पाते कि सीटी बज जाती और लोग वापस दुम की तरफ भागते। यह सब इतना तय कि सहज व ‘शाश्वत’ सा था कि कोई इस बारे में नहीं सोचता। सोचता भी तो बस यही कि मुसाफिरी में तो यह सब चलता ही है।
नीलकांत उसी डिब्बे में थे। डिब्बे में भारी भीड़ थी। लोग भेड़-बकरियों की तरह भरे हुए थे। कुछ लोगों की नजर में हो सकता है, यह उचित ही हो, पर पूरा भरोसा है कि आप उन कुछ लोगों में से नहीं है। क्योंकि आपको भी ऐसी ही स्थितियों में सफर करना पड़ता है। तो… लोग एक-दूसरे पर लदे जा रहे थे। जितने बैठे थे, उनसे ज्यादा खड़े थे और कुछ लटके भी थे। ऊपर की सीटें सामान से भरी हुई थी और फर्श औरतों से। दोनों स्थान पर बीच-बीच में कुछ आदमी भी फंसे हुए थे। बच्चों को हर जगह पाया जा सकता था। वे पानी मांग रहे थे और गर्मी से बेजार हो रहे थे। उन्हें पानी पिलाया जा रहा था और पेशाब करवाया जा रहा था। वे रो रहे थे या सो रहे थे या छींक रहे थे। वे हैरान थे कि हलकान थे। डिब्बे की सीटों पर एक-दो-तीन बा$कायदा नंबर पड़े हुए थे और एक तरफ की दीवार पर लिखा हुआ था- ‘पैंतीस सवारियों के लिए।’ इसे पढक़र अंदाजा होता था कि रेलवे में काम करने वाले आदमी कितने मजाकिया हैं। मसलन ये लिखने वाले। अब पाखाने का आलम देखिये। इस डिब्बे के यात्री, थर्ड क्लास के मुसाफिर, खासकर नन्हें या किशोर मुसाफिर जनरल-नॉलेज के क्षेत्र में दिशा-मैदान या जंगल के परिचय से आगे नहीं बढ़ पाये थे और पाखाने में घुसते ही पता चलता था कि वे बेचारे काफी देर इसी दुविधा में पड़े रहे होंगे कि किधर मुंह करके बैठा जाए। तिस पर टोंटिये में पानी भी नहीं था। साबुन के स्थान पर किसी धर्मप्राण ने ढेर सारी मिट्टी जरूर भर रखी थी और आईना नहीं था तो क्या बुरा था? ऐसी स्थिति में अपना थोबड़ा देखकर खामखां आदमी का मूड ऑफ ही होता! इस संडास में तीन सज्जन बाहर को मुंह उचकाये इधर-उधर सहारा लिए खड़े थे। सोचना डर पैदा करता था कि क्या हो, यदि इस समय डिब्बे में किसी सज्जन या देवी को इस भव्य कक्ष की आपातकालीन जरूरत पड़ जाए जिस पर ‘प्रसाधन’ लिखा है।
इसी डिब्बे में नीलकांत सफर कर रहे थे। खड़े हुए। इसी संडास में।
खैर, बाद में उन्हें डिब्बे में धंसने में सफलता भी मिल गई। पर संडास की बदबू दिमाग से नहीं गई। और हालांकि इस संघर्ष में उनकी बूढ़ी अटैची का कमजोर हैण्डल टूट गया और नतीजतन उन्हें उस बूढ़ी अटैची को बच्चों की तरह छाती से चिपकाकर रखना पड़ा। पर घुस तो गए ही, पाखाने से तो अच्छे ही हैं।
यहां आकर नीलकांत ने देखा कि जहां बहुत सारे आदमियों को पांव सरकाने को भी जगह नहीं है और कई अब तक लटक रहे हैं या निरंतर इस ताक में टंगे हैं कि कब आदमियों की तरह आराम से पैर टिकाने या पुट्ठे टिकाने का मौका मिल जाए… वहीं कुछ आदमी लेटे हुए हैं। और बा$कायदा पूरी बर्थ घेरकर लेटे हुए हैं। इससे नीलकांत को उस झगड़े का भी सुराग मिल गया, जो न जाने कब से खड़ों और लेटों में चल रहा था। वे कह रहे थे। हमने भी किराया दिया है। जवाब मिल रहा था हम ठेठ वहां से आ रहा हैं, जहां से ये ट्रेन बनी है, ठेठ बम्बई से। वे कह रहे थे, आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है, चाहे बम्बई से आओ, चाहे लंदन से। जवाब मिल रहा था, अजी साहब एक बर्थ के लिए कुली को पांच रुपए दिए हैं। रात-भर का मामला है, आप तो घंटे-दो घंटे में उतर जाएंगे। इस पर हल्ला मचाने वाले जरा ढीले पड़ जाते, पर थोड़ी देर बाद वही सब शुरू हो जाता। नीलकांत को लगा, जो लेटे हुए हैं, वे कितने हृदयहीन हैं! माना कि आपने पांच रुपए दिए हैं औार आपको बहुत दूर जाना है, पर कम दूरी वाले क्या मुफ्त में स$फर कर रहे हैं। क्या उन्हें टिकने-भर का अधिकार नहीं? औरतें तक खड़ी हुई हैं और ये बेशरम पैर पसारे पड़े हुए हैं। यह कोई इंसानियत है? और उसे देखो… सींकिया पहलवान को! कैसे आंखें मींचे पड़ा है, जैसे गहरी नींद में हो। समझता है, हम धोखे में आ जाएंगे। बोलने वाले भी साले यों ही हैं। घंटेभर से कांय-कांय कर रहे हैं, यह नहीं होता कि हाथ पकडक़र उठाकर बैठा दें सालों को। देखते हैं, कोई क्या कर सकता है? चालीस आदमी खड़े कांय-कांय कर रहे हैं और चार बेशरमी से पड़े हुए हैं। धन्य हो! और जिन्हें जरा-सी भी टिकने की जगह मिल गई है, वे ऐसे चुप हैं, जैसे खड़े हुओं से कोई हमदर्दी नहीं, लेटे हुओं पर कोई गुस्सा नहीं! नीलकांत ने घड़ी देखी। ट्रेन चले हुए आधा घंटे से भी ज्यादा हो गया था। आमतौर पर इतनी देर में मुसा$िफरों के झगड़े खत्म हो जाते हैं और जान-पहचान, हंसी-खुशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर क्या बात है? आदमी क्यों इतना लड़ता है? किसे इस ट्रेन में अनन्त काल तक रहना है? नीलकांत ने सोचा।
तभी अचानक नीलकांत को महसूस हुआ कि गर्मी कुछ ज्यादा ही है। पंखे देखे। चल रहे थे। खिड़कियां बंद थी। नीलकांत को आश्चर्य हुआ कि इस तर$फ उनका ध्यान अब गया! यह भी कि अब तक किसी ने खिड़कियां खोली क्यों नहीं? उनके पास वाली खिडक़ी से सटकर एक लडक़ा खड़ा था। नीलकांत ने लडक़े से कहा, जरा खिडक़ी खोल दीजिए। ‘नहीं खुलती’ लडक़े ने बत्तीसी निकालते हुए जवाब दिया। नीलकांत को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लडक़े को अटैची पकड़ाते हुए कहा- हटिए, मैं खोलता हूं। हटाहटी में एक बच्चे का पैर कुचल गया। खैर, नीलकांत ने खूब जोर लगाया, लेकिन खिडक़ी टस से मस नहीं हुई। नीलकांत ने फिर जोर लगाया। जांच-परख की, फिर जोर लगाया, फिर दिमाग लगाया। फिर ताकत, फिर दिमाग, लेकिन खिडक़ी नहीं खुली। दूसरी भी नहीं खुली। तीसरी तक उन्हें किसी ने जाने नहीं दिया। बीसियों लोग पहले ही कोशिश कर चुके थे। सारी खिड़कियां जाम थीं। नीलकांत हताश हो गए। पसीने-पसीने हो गए। खीझ गये। डिब्बे के बहुत लोग उनकी इस हरकत को देख रहे थे और खिडक़ी पर विभिन्न टिप्पणियां कर रहे थे। एक गाय जैसे चेहरे वाले बाबा ‘नहीं खुलती तो छोड़ो, बददाश्त कर लो’ की अपील कर रहे थे। एक उग्र से व्यापारी सज्जन कह रहे थे कि साले सब रेलवाले चोर हैं (इसलिए खिडक़ी को छोड़ो, वह नहीं खुलेगी।) ऊपर की सीट पर आराम से बैठा एक दढिय़ल गरज रहा था- तोड़ दो। मैं कहता हूं, तोड़ दो नहीं खुलती तो। यानी लोग अपने-अपने दिमा$ग के हिसाब से नीलकांत को सुझाव दे रहे थे और जिनसे यह भी नहीं हो रहा था, वे सरकार को गालियां दे रहे थे, और बाकी सब इस सबको टाइम पास करने का नुस्खा समझकर चुपचाप सबका मजा ले रहे थे।
नीलकांत ने जेब से रूमाल निलाकलकर पसीना पोंछा तो वह लडक़ा जल्दी करने लगा- भाई साहब! अपनी अटैची सम्हालो। लगा, उलझ पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे किसी पर। चुपचाप अटैची सम्हाल ली।
आखिर गलती किसकी है? नीलकांत सोचने लगे। जब ट्रेन में इतनी जगह नहीं है तो क्यों इतने टिकट देते हैं! ज्यादा मुसािफर हैं तो ज्यादा गाडिय़ां क्यों नहीं चलाते? लोग लटक-लटक कर सफर कर रहे हैं, लोग सामान रखने की जगह पर भी बैठे हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, लोग पाखाने में भरे हुए हैं… और रेलवे फिर भी घाटे में जा रही है! क्यों? कौन दोषी है? क्या वह बुकिंग क्लर्क जिसने इतने ज्यादा टिकट काट दिए? या वह मिस्त्री, जिसने रेल रवाना होने से पहले खिडक़ी-दरवाजे नहीं जांचे? या वे सज्जन जो कुलियों को पांच-पांच रुपए देकर पूरी बर्थ पर कब्जा किए हुए हैं? या वे अमीर, जिनके लिए पांच-पांच फस्र्ट के डिब्बे बीच में लगाए गए हैं?
सोचने लगे। फिर उलझ गए। पर सोचने तो लगे, हालांकि नतीजे तक नहीं पहुंचे। पर उलझे तो। पर पता नहीं, क्यों इन चीजों पर सोचने लगे, हालांकि पढ़ते तो धर्मयुग, इलस्ट्रेट वीकली वगैरह ही हैं। वे लोग तो चाहते थे कि नीलकांत प्रदूषण के बारे में सोचें, जातियों के तुलनात्मक विवेचन पर सोचें, परामनोविज्ञान और आधुनिक प्रेतविद्या के बारे में सोचें, स्वीडन के मुक्त यौवन और अमरीका की स्वतंत्र पत्रकारिता के बारे में सोचें, सोचें कि शास्त्री जी मरे या उनकी हत्या हुई… पर वे तो अपनी दुर्दशा के लिए दोषी कौन हैं? इस पर सोचने लगे! गजब हो गया!! खैर, सेठजी चिंता न करें, नीलकांत इन तकलीफों के बारे में तभी तक सोचेंगे, जब तक उन्हें बैठने के लिए ठीक-ठाक जगह नहीं मिल जाती, या हद से हद जब तक वह सफर जारी है। गाड़ी से उतर जाने पर वह गाड़ी के बारे में सब भूल जाएंगे और फिर वही सोचने लगेंगे, जो सेठ लोग सोचवाना चाहते हैं। पर क्या पता? अगर कल कोई दूसरी तकलीफ आई- आएगी ही- और वे सोचने लगे कि उसका असली जिम्मेदार कौन है- तो…?
नीलकांत को प्यास लगी। स्टेशन अभी दूर था। सामने एक लुगाई अपने बच्चे को सुराही से पानी निकालकर पिला रही थी। नीलकांत की इच्छा हुई- पर लुगाई और सुराही और गिलास सब बेहद गंदे थे। नीलकांत हाइजिन के बारे में सोचने लगे और प्यासे रह गए। फिर रूमाल निकालकर गरदन पोंछी। पंखों की तरफ देखा। बराबर चल रहे थे, पर लगता था, एग्जास्ट फैन हैं, जो हवा देते नहीं, खींचते हैं। इधर-उधर नजर दौड़ाई कि कहीं टिकने की कोई संभावना नजर आ जाए। नहीं आई। हारकर फिर खिड़कियों के बारे में सोचने लगे।
नीलकांत की इच्छा हुई,वापस उसी संडास में चले जाएं। खड़े यहां भी हैं, वहां भी थे। वहां कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो थी, माना कि बदबू और गंदगी और सबसे ज्यादा अपने संडास में होने का अहसास- ऐसी ही कुछ परेशानियां थी, पर यहां क्या कम परेशानी है? और सुविधा क्या है? सिवा इस गरिमा के कि डिब्बे में है, संडास में नहीं? लिहाजा चलो वापस संडास में।
लेकिन वापस जाना असंभव था। बहुत कुछ बाहर था और कुछ भीतर भी था, जो रोक रहा था। झख मारकर भविष्य के बारे में सोचने लगे। संडास वाले का क्या भविष्य है? किसी को भी हाजत होते ही वहां से बाहर निकाल दिया जाना। और यहां? संभावना है कि कभी तो कोई स्टेशन आएगा, तो कुछ सवारियां उतरेंगी और उन्हें भी टिकाने की जगह मिलेगी ही। उस सुंदर भविष्य के लिए- जब वे दूसरों की बराबरी में बैठे होंगे- इस वर्तमान में कुछ कष्ट उठा लें तो क्या हर्ज है?खिड़कियां ही खुल जातीं तो तन-बदन थोड़े ठंडे होते। कइयों को उन पर टिकने की जगह भी मिल जाती। और खिडक़ी साली, उनके बारे में सोचते रहने से तो खुलने से रहीं। कोई औजार-वौजार होता तो…अब नीलकांत सोचने लगे कि कौन-सा औजार होता, जिससे खिडक़ी खोली जा सकती? और इससे भी पहले कौन-सी तरकीब होती, जिससे इन पसरे हुए सज्जनों को उठाकर बैठाने पर मजबूर किया जा सकता? एक तरीका तो यह कि लड़ लिया जाए। और अधिकांश लोग उनका ही साथ देंगे। और दूसरा यह कि स्टेशन आने पर गार्ड को बुलाकर लाया जाए कि इन महापुरुषों को… तभी गाड़ी रुक गई।
नीलकांत ने सोचा, चलो गार्ड को बुला लायें, पर वह मिलेगा? और मिला भी तो आने के लिए तैयार हो जाएगा? और आ भी गया तो इनको उठा सकेगा? अगर वह फस्र्ट के किसी मुसाफिर के साथ चाय पी रहा हो तो? और सा$फ मना न भी करे चलने के लिए… पर चले; चले तब तक गाड़ी ही चल पड़े तो? और नीलकांत नीचे ही रह जाए तो? और मान लो किसी तरह चढ़ भी जाएं और यह जगह भी फिर न मिले तो? और पहली बात तो यह कि अभी अटैची किस को सम्हलाकर जाएं? ताला इसमें है नहीं। और हालांकि इसमें ऐसा क्या है जो किसी के काम आ सके। फिर भी। और यह लडक़ा? हालांकि लेटे हुए लोग उठेंगे तो इसे भी बैठने की जगह मिल सकती है, लेकिन अभी इससे कहूं कि जरा मेरी जगह और अटैची देखना, मैं गार्ड को बुलाकर ला रहा हूं तो देखेगा? सवाल ही नहीं उठता। एक बात और है। क्या भरोसा कि इतना सब करने पर भी मुझे जगह मिल ही जाएगी?
उतरूं, न उतरूं की इसी दुविधा में नीलकांत पड़े रहे और ट्रेन ने सीटी मार दी। ट्रेन फिर खिसकने लगी और आगे बढऩे लगी। तभी प्लेटफार्म की तरफ से आठ-दस काले-कलूटे फटेहाल मजदूर दांत निकालते हुए दौड़ते हुए आए और एक-दूसरे को पुकारते-चीखते एक-एक करके सब उसी में चढ़ गए। पहले एक चढ़ा… उसने दूसरे का हाथ पकडक़र उसे भी चढ़ा लिया, उसने तीसरे को… इस तरह सब चढ़ गए। पीछे-पीछे दो धाकड़ लुगाइयां भी चढ़ा ली गई और भागते-भागते आखिरी आदमी, गेंती-फावड़े-तगारी वगैरह भी चढ़वा दिए और छलांग मारकर खुद भी चढ़ गया।इस नई भीड़ से दरवाजे और गलियारे में खड़े लडक़े और बाबू लोग बुरी तरह अंदर की तरफ धकेल दिए गए, एकदम कचरे की तरह। परस्पर धक्के को ठेठ अंत तक महसूस किया गया और डिब्बे में चिल्ल-पुकार मच गई। मजदूरों के तपे हुए चेहरों के बीच खिली बिजली जैसी नीग्रो हंसी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी भाषा में बुलंदी से बतियाते रहे और ट्रेन पकडऩे में सफल हो जाने की खुशी मिलकर मनाते रहे। उनके कपड़े कोयले के बुरादे से काले हो रहे थे और उस पर मैल और पसीने की मोटी तहें जमी हुई थीं। सफेयतपसंद आदमी यथासंभव उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे और एक साहब ने- जो दुर्भाग्य से उनके पास ही फंसे हुए थे- नाक पर रूमाल भी लगा लिया था। उनका बस चलता तो वे आंखे, नाक, सिर, पूरे शरीर पर रूमाल लगा लेते। पर इससे होता क्या? जो जहां थे सो रहते ही, गायब तो नहीं हो जाते, अलबत्ता उन साहब का दम जरूर घुट जाता।
फिर क्या हुआ कि बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, तिरछे होकर लोगों के बीच से जगह बनाते हुए नीलकांत के सामने से होते हुए डिब्बे के बीच तक आ गए यानी उन्होंने नीलकांत को पीछे छोड़ दिया। वे न लड़ रहे थे, न बक रहे थे, न घबरा रहे थे, न आपा खो रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि वे इस भीड़ और परेशानी के आदी हैं और कुछ नहीं समझ रहे। शायद हमेशा अप एण्ड डाउन करते हैं। लुगाइयां भी आ गईं। उन्होंने अपने कसे हुए जिस्मों पर कसी हुई कांचली पहन रखी थीं और उनके सिर के बालों की चोटी खूब ताकत से कसकर गूंथी हुई। पीठ लगभग नंगी थी, पसीने में तर। एक पीठ नीलकांत के एकदम सामने से, करीब-करीब उसे छूते हुए गुजरी। ऐसी स्वस्थ, पुष्ट, सबसे सुन्दर पीठ कि नीलकांत के मन में वाह-वाह सी होने लगी। बड़े भारी उनके घाघरे थे और जूतियां इतनी मरदानी और ऐसी भारी कि एक पड़ जाए तो थोबड़ा लहूलुहान हो जाए। वे हंस रही थीं और ठिठोली के मूड में थीं, पर किसी की क्या मजाल जो उन्हें छेडऩे की सोच भी सके। मर्दों ने अंदर पहुंचते ही खिड़कियों के सामने से लोगों को हटाकर उन्हें जांच, परखा, खोलने की कोशिश की और फिर उनमें से एक ने- जो थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा, बल्कि उनके मेट जैसा लग रहा था- अपनी भाषा में पीछे दरवाजे के पास खड़े आदमी को पुकारकर कुछ कहा। गेंती मांगी थी, क्योंकि वह लोगों के बीच से ही होती हुई आ गई। गेंती का सिरा एक खिडक़ी के सबसे निचले खांचे में एक खास कोण से फंसाकर उसने अपनी साथी से कहा- दबा। अब इस दूसरे आदमी ने गेंती के हत्थे पर एक खास जगह नपी-सधी ताकत लगाई और एक झटके में खिड़क़ी खुली गई। सब लोग अपढ़ मजदूरों के इस कारनामे को बड़े कौतुहल से देख रहे थे और जाहिर है कि वे खिडक़ी के खुल जाने से चकित और खुश हुए। वे भी, जिन्होंने बहुत कोशिश की थी और नाकामयाब रहे थे और सोच रहे थे, जब हम पढ़े-लिखों से नहीं खुली तो इन अपढ़ गंवारों से क्या खुलेगी? वे भी, जिन्हें मजदूरों की क्षमताओं पर पूरा-पूरा संदेह था और वे भी, जिन्हें डर था कि गेंती या ताकत के इस्तेमाल से खिड़कियां टूट जाएंगी। सिर्फ लेटे हुए लोग खिड़कियां खुल जाने से खुश नहीं थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि अब उनका लेटा होना बाहर से भी दिख जाएगा और सब साले मच्छरों की तरह इस डिब्बे पर टूट पड़ेंगे। लेकिन उसमें से दो को तो लुगाइयों ने ही पैर सिकोडऩे पर बाध्य कर दिया और खुद आराम से बैठकर पसीना सुखा रही थीं। उन्होंने अपनी भाषा में लेटे हुओं को डांटकर कुछ कहा था- वे जिसका अर्थ तो नहीं, आशय जरूर समझ गए थे और सोचकर सिकुड़ गए थे कि पैर नहीं हटाए तो पुट्ठे भी हटाने पड़ेंगे।
धीरे-धीरे उन बांकों ने सारी खिड़कियां खोल दीं और सारे पसरे पैर और फैले पुट्ठे हटाकर रख दिए, ठाठ से बैठ गए और फिर हंसने लगे। खड़े हुए फिर चकित थे और कई मजदूरों के साथ उनकी बराबरी में बैठने को लालायित। इस स्टेशन से मानो सारे डिब्बे का नक्शा ही बदलना शुरू हो गया था। खिड़कियां खुलते ही सारे डिब्बों में उजाला हो गया था और ताजी हवा के ठंडे झोंके सपाटे भर रहे थे। बाहर हरे-भरे लहराते खेत थे और पेड़ और नदियां और पहाड़- और उन सब पर बड़ी सुहानी शाम बिखर रही थी। थोड़ी देर में ये लोग कोई गीत शुरू कर देंगे। उदासियां दूर भाग जाएंगी। नीलकांत खुश थे, हालांकि खड़े थे। नीलकांत सफर कर रहे थे, पर खुश थे।