सतीश भारतीय
भारतीय कृषि व्यवस्था का एक व्यापक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। इन क्षेत्रों के किसान प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं। मगर, वर्तमान कृषि में कई चुनौतियाँ बरकरार हैं, जो कृषि की निरंतरता को भंग कर रही हैं। रासायनिक कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कृषि विविधता की कमी, पोषण की दृष्टि से असंतुलित आहार, पारिस्थितिकीय असंतुलन और सामूहिक कृषि सहभागिता की अनुपस्थिति जैसी समस्याएँ सतत कृषि के लिए गंभीर बाधाएँ बनी हुई हैं।
ग्रामीण भारत के किसान बड़े पैमाने पर बाहरी संसाधनों पर निर्भर हैं। ऐसे में उर्वरक, कीटनाशक, बीज और कृषि उपकरण बाजार से खरीदने पर किसानों की लागत बढ़ जाती है। साथ ही, प्राकृतिक संसाधनों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, पारंपरिक बीजों की जगह मिश्रित और अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देने के कारण स्थानीय पारिस्थितिकी असंतुलित हो रही है।
जलवायु परिवर्तन भी कृषि के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और असामान्य तापमान परिवर्तन के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अधिकतर किसान पारंपरिक फसलों और कृषि विविधता से दूर हो गए हैं, जिससे कृषि जोखिम बढ़ गया है।
इसके अतिरिक्त, एक बड़ी समस्या पोषण की कमी भी है। किसानों की खाद्य प्राथमिकताएँ सीमित हैं। वे मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा फसलों पर निर्भर होते हैं, जिससे उनके आहार में पोषण की कमी देखी जाती है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी और जल संसाधनों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है।
सामाजिक दृष्टिकोण से भी कृषि को मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्तमान में किसान व्यक्तिगत स्तर पर कृषि करते हैं और बाजार तक उनकी पहुँच सीमित होती है। इस कारण वे उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते और बिचौलियों के माध्यम से अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं।
कृषि की चुनौतियों पर सागर के ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखने वाली पार्वती आदिवासी बयान करती हैं, “हमारे पूर्वज बिना रासायनिक खाद के भी अच्छी फसल उगाते थे, लेकिन अब ज़मीन इतनी कमजोर हो गई है कि बिना बाहरी साधनों के कुछ नहीं उगता। जलवायु परिवर्तन और जल संकट ने खेती को संघर्षमय बना दिया है।”
वहीं, सागर के ग्रामीण इलाकों में खेती करने वाले कृषक राजाराम अहिरवार का मानना है, “पहले बारिश के समय और मात्रा का अंदाज़ा होता था, लेकिन अब मौसम बदल रहा है-कभी बाढ़, तो कभी सूखा। हमारी फसलें भगवान के भरोसे रह गई हैं। हमें टिकाऊ कृषि की ओर लौटना होगा। इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।”
आगे नारायण पटेल बताते हैं,“मैं बरखेड़ा गाँव का निवासी हूँ। दो एकड़ भूमि के साथ मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। इन सदस्यों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं बहुत चिंतित रहता था। लेकिन जब से मानव विकास संस्था की पहल से मुझे और गाँव के कई किसानों को कृषि कार्य में मजबूती मिली है, खरीफ सीजन में मेरी आजीविका में व्यक्तिगत रूप से ₹30,000 की वृद्धि हुई है। ऐसे ही अन्य किसानों को भी लाभ मिल रहा है।”
इसी तरह, अमरमऊ गाँव के किसान राहुल पटेल अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, “मैंने जब प्राकृतिक खेती अपनाई, तो मेरी लागत घटी और आमदनी बढ़ी। पहले हर सीजन में ₹6,500 तक रासायनिक इनपुट पर खर्च होता था, अब सिर्फ ₹1,200 में जैविक तरीके से खेती कर रहा हूँ। मिट्टी की सेहत सुधरी, फसल की गुणवत्ता बढ़ी, और बाजार में अच्छी कीमत भी मिली। मैं आज आत्मनिर्भर किसान हूँ।”
समाधान और सतत कृषि की ओर बदलाव
स्थायी कृषि के लिए सबसे अच्छा उपाय जैविक और पारिस्थितिकीय कृषि प्रणालियों को अपनाना है। किसानों को जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशकों और स्थानीय संसाधनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। खेतों में जैविक खाद जैसे जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य आदि का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होगा।
जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसानों को विविधतापूर्ण फसल प्रणाली अपनाने, जल-संरक्षण तकनीकों जैसे तालाब, खेत तलाई और ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने, और स्थानीय जलवायु के अनुसार कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
कृषि विविधता को बढ़ाने के लिए बहुफसलीय खेती, कृषि वानिकी, बागवानी और पशुपालन को जोड़ना ज़रूरी है। इससे किसानों को पूरे वर्ष आय प्राप्त होगी और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगा। पोषण की दृष्टि से किसानों को अपने आहार में विविधता लाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। घरों के आसपास पोषण उद्यान (किचन गार्डन) विकसित कर स्थानीय स्तर पर सब्जियाँ, फल और अनाज उगाने से पोषण में सुधार होगा।
बाजार में किसानों की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक संगठनों जैसे किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना ज़रूरी है। इससे किसान अपने उत्पादों को बेहतर मूल्य पर बेच सकेंगे और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होगी।
मानव विकास सेवा संघ (MVSS) द्वारा सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। संगठन द्वारा कृषि संसाधन केंद्र (BRC) और जैव-प्रयोगशाला (Bio Lab) स्थापित कर किसानों को जैविक कृषि की तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है। किसान फील्ड स्कूल और प्लांट डॉक्टर जैसी पहलें किसानों को वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान से जोड़ रही हैं।
इन सभी प्रयासों के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और सतत कृषि को प्रोत्साहित करना संभव है। सामूहिक प्रयासों और जागरूकता के माध्यम से ग्रामीण भारत में कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाया जा सकता है।


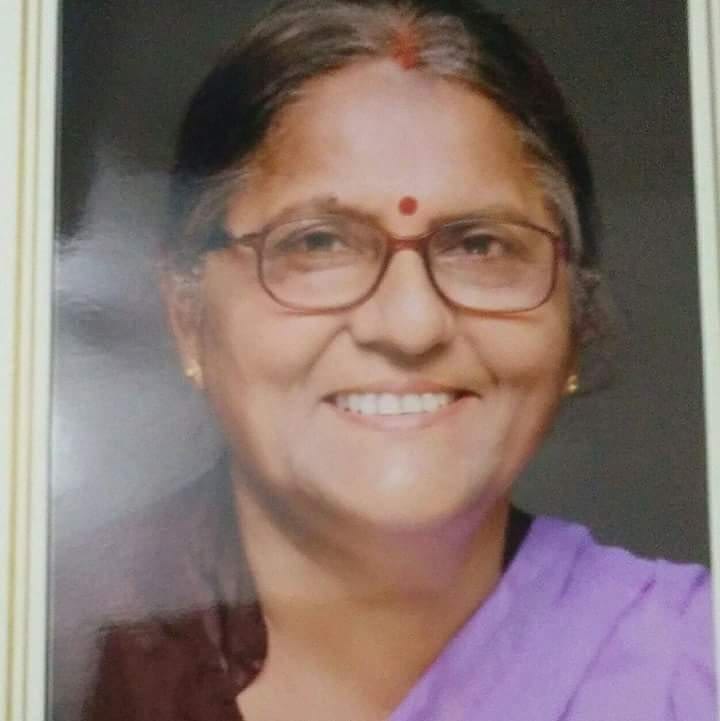






















Add comment