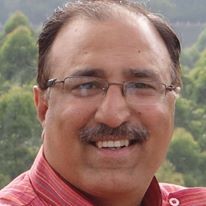सत्येंद्र रंजन
नरेंद्र मोदी के काल में चुनाव जीतने का हाल तक कारगर रहा भाजपाई एजेंडा अब संभवतःलाभ घटने के नियम का शिकार हो गया है।लाभ घटने के नियम हालांकि अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, मगर अक्सर राजनीति में भी इसके जरिए किसी पार्टी या नेता के फैलते या सिकुड़ते प्रभाव को समझने की कोशिश की जाती है। इस सिद्धांत के मुताबिक उत्पादन के बाकी इनपुट्स (घटकों) को समान रखते हुए सिर्फ किसी एक इनपुट को लगातार बढ़ाने पर आरंभ में उत्पादन बढ़ता है, लेकिन धीरे-धीरे वृद्धि दर घटने लगती है और एक सीमा के बाद वह शून्य हो जाती है। श्रम, जमीन (या अन्य प्राकृतिक संसाधन), पूंजी, और टेक्नोलॉजी उत्पादन के प्रमुख इनपुट हैं। प्रबंधन के स्वरूप को भी अब एक इनपुट समझा जाता है।
भाजपा के मामले में इस सिद्धांत की याद इसलिए आती है, क्योंकि 1989 के बाद से पार्टी ने हिंदुत्व पर खास जोर देते हुए, और उसे लगातार तीखा और कई मौकों पर उन्मादी बनाते हुए अपनी राजनीतिक पूंजी बढ़ाई। नरेंद्र मोदी इसके प्रबंधन में खासे धारदार साबित हुए। 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनकी ‘हिंदू हृदय सम्राट’ की जो छवि बनी (या बनाई गई), वह अभी पिछले साल तक चुनावी जीत सुनिश्चित करने का कमोबेश कारगर औजार बनी रही। इसके साथ आर्थिक उदारीकरण, “अच्छे दिन” जैसे वायदों और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रचार महत्त्वपूर्ण इनपुट बने रहे।
उपरोक्त आर्थिक सिद्धांत से आज की सूरत को समझने के कोशिश में यह कहा जा सकता है कि भाजपा ने बाकी इनपुट्स को विश्वसनीय बनाने की चिंता छोड़ कर सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को उत्तरोत्तर तीखा करने पर अधिक यकीन किया। मगर ऐसा लगता है कि जनता के बीच प्रभाव के लिहाज से यह रणनीति इस वर्ष जनवरी में अयोध्या में नव-निर्मित राम मंदिर के उद्घाटन के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी हिंदुत्व से आकर्षित जन समुदाय में उस रोज शायद इस एजेंडे की जीत का विश्वास हो गया। उसके बाद उनका ध्यान बाकी इनपुट्स पर गया, जिन पर वहां मोदी सरकार का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा की राजनीतिक पराजय इसी परिघटना का परिणाम रही।
भाजपा नेतृत्व में सामूहिक विचार-विमर्श तथा सच को सच की तरह स्वीकार करने की संस्कृति होती, तो पिछले चार जून को पार्टी जल्दबाजी में विजयघोष नहीं करती। ना ही उसके बाद वह लगातार यह संदेश देने की कोशिश करती कि कुछ भी नहीं बदला है। चूंकि पार्टी के अंदर आज निर्णय प्रक्रिया कुछ व्यक्तियों के बीच सिमटी हुई है, इसलिए उनके हितों के मुताबिक नए कार्यकाल में भाजपा ने निरंतरता का दिखावा करने की जिद कर ली। लेकिन यह दांव उलटा पड़ रहा है।
भाजपा नेतृत्व खुले दिमाग से चुनाव नतीजों का विश्लेषण करता, तो वह इस सवाल पर गौर करता कि अयोध्या में मंदिर बनने और चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर देने के बावजूद पार्टी ने अपना बहुमत क्यों गंवा दिया? हिंदुत्व एजेंडे का प्रमुख पहलू मुस्लिम विरोधी भावनाओं को हवा देना रहा है।
1990 के दशक से इस एजेंडे को उभारने के क्रम में मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद आदि को समानार्थी रूप में पेश कर उन्हें “हिंदू राष्ट्र” के शत्रु के रूप में पेश करने का भ्रामक कथानक प्रचारित किया गया है। 2024 के चुनाव अभियान में भाजपा ने इस रणनीति पर खासा जोर दिया। हिंदुत्व विमर्श में “हिंदू राष्ट्र” का एक अन्य शत्रु कम्युनिस्ट रहे हैं। पिछले आम चुनाव में नक्सलवाद और अर्बन नक्सलवाद का भय खड़ा करने में भी भाजपा नेताओं ने अपनी काफी ऊर्जा लगाई।
इसके बावजूद चुनाव परिणाम निराशाजनक रहा, तो पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए था कि यह फॉर्मूले के साथ अब Law of Diminishing Returns लागू होने लगा है। मगर गुजरे पौने तीन महीनों में भाजपा ने इस समझ का पूरा अभाव दिखाया है। नतीजतन, इस दौर में भी पार्टी ने हिंदुत्व की भावना उभारने वाले भावनात्मक मुद्दे लगातार उछाले हैं। उनमें से कुछ पर गौर कीजिएः
- कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानदारों को अपनी नाम-पट्टिका लगाने का आदेश जारी किया गया। मकसद, नाम से मजहब की पहचान करना और इसके जरिए मजहबी खाई को और चौड़ा करना था।
- केंद्र ने आनन-फानन नए वक्फ़ बोर्ड कानून का विधेयक संसद में पेश कर दिया। मकसद, इस संदेश को और पुष्ट करना है कि भाजपा सरकार मुसलमानों को “ठीक” कर रही है।
- प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से “सांप्रदायिक” पर्सनल लॉ को खत्म कर “सेक्युलर” निजी संहिता लागू करने का एलान किया। मकसद फिर से इस नैरेटिव को जिंदा करना है कि पहले की सरकारों ने मुसलमानों के साथ “विशेष” व्यवहार किया, जिसे मोदी सरकार अब सुधार रही है।
- अब जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के साथ कांग्रेस के चुनावी समझौते को लेकर भाजपा नेतृत्व ने धारा 370 से जुड़े “हिंदुत्ववादी” जज्बात को उभारते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। मकसद संदेश देना है कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ “संपूर्ण एकीकरण” किया, जबकि कांग्रेस और प्रकारांतर में पूरा विपक्ष चुनावी फायदे के लिए उस सफलता को पलटने की हद तक जाने को तैयार है।
भाजपा नेतृत्व के लिए यह गंभीर आत्म-मंथन का विषय है कि क्या इनमें कोई भी मुद्दा कारगर रहा? कुछ वर्ष पहले को याद करें। तब भाजपा अपने उछाले हर मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने के लिए अपने विपक्षियों को मजबूर कर देती थी। उनसे ऐसा माहौल बनता था, जिसमें समाज दो खेमों में बंट जाता था। इस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भाजपा का मकसद पूरा होता रहता था। लेकिन इस बार मीडिया में बहुप्रचारित होने के बावजूद ये तमाम प्रयास जनता के स्तर पर किसी तरह का भावावेश पैदा करने में विफल रहे हैं।
इस सिलसिले में 2022 को याद करें। तब प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 9 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ लगाने का आह्वान किया था। देखते-देखते ऐसे घर ढूंढने तब मुश्किल हो गए, जिन पर तब तिरंगा ना लगा हो। वही आह्वान इस महीने भी नरेंद्र मोदी ने किया। इस बार आम तजुर्बा यह रहा कि ढूंढने पर भी ऐसे घर शायद ही दिखें, जिन पर 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा लगा रहा हो। यह ऐसा संकेत है, जिससे भाजपा नेतृत्व चाहे तो महत्त्वपूर्ण सबक ग्रहण कर सकता है।
संभव है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी हो कि नरेंद्र मोदी का सितारा अस्त होने की ओर है। लेकिन उस पर ग्रहण लगने के संकेत स्पष्ट हैं। नीतिगत या शासन संबंधी मुद्दों पर यू-टर्न इस रुझान का सिर्फ एक संकेत है। इसका दूसरा संकेत पार्टी के अंदर मोदी-शाह के वर्चस्व का क्षरण है। पहला संकेत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार के बाद वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खींचतान से मिला। तमाम संकेत हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मनमाफिक फैसले नहीं थोप पाया।
यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में तमाम बातें महज मीडिया की अटकलें हैं। मगर जम्मू-कश्मीर में जो हुआ, वह कयास नहीं, बल्कि पुष्ट खबर है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 44 उम्मीदवारों की जारी पहली सूची जारी हुई, लेकिन कुछ ही देर में पार्टी नेतृत्व को उसे वापस लेना पड़ा। उसके बाद पार्टी ने उस रोज सिर्फ उन 16 सीटों के लिए पहली सूची जारी की, जहां पहले चरण में मतदान होना है।
लिस्ट वापसी इसलिए हुई, क्योंकि जिन नेताओं को टिकट दिए गए, उनको लेकर जम्मू इलाके के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। नाराज नेताओं ने मीडिया के सामने आकर शिकायत जताई कि पार्टी में जीवन खपा देने वाले नेताओं की उपेक्षा करते हुए कुछ समय पहले ही दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया है।
लेकिन दूसरे दलों से नेताओं को लाकर मोदी-शाह टिकट दें, तो यह उनके दौर में कोई नई बात नहीं है। चुनाव जीतने की कथित क्षमता रखने वाले बाहरी नेताओं से इस दौर में भाजपा अपने को भरती चली गई है। क्या गुजरे दस वर्षों में इसको लेकर भाजपा के अंदर से कभी वैसी आवाज उठी थी, जैसा जम्मू में हुआ है? और क्या कभी पार्टी में अंदरूनी मतभेद के कारण मोदी-शाह अपने निर्णय वापस लेने पर इस तरह मजबूर हुए थे?
ये तमाम घटनाएं इस बात की ही पुष्टि करती हैं कि चुनावी लोकतंत्र में नेताओं की हैसियत वोट खींच सकने की उनकी क्षमता से बनती है। (ये क्षमता कैसे निर्मित होती है, यह अलग चर्चा का विषय है।) 2024 के आम चुनाव ने स्पष्ट किया कि नरेंद्र मोदी की वोट खींचने की क्षमता अब उतार पर है। उसके बाद जिन मुद्दों को भाजपा ने उछाला, उन पर समर्थक समूहों की ठंडी प्रतिक्रिया से नैरेटिव कंट्रोल करने की मोदी-शाह की क्षमता के क्षीण होने के संकेत मिले हैं। उसका असर होता अब दिख रहा है।
तो क्या इन संकेतों के आधार पर यह समझ लेना उचित होगा कि मोदी-शाह जिस तरह की सियासत के वाहक हैं, उसका भी क्षय शुरू हो गया है?
यह एक गंभीर प्रश्न है। इस बारे में कोई राय बनाने के पहले राजनीति और भारत की वर्तमान राजनीतिक-अर्थनीति (political economy) के स्वरूप को ध्यान में रखना होगा।
भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी के रूप में भाजपा का उदय 1990 के बाद से शासक वर्ग की तरफ से अपनाई गई एक खास रणनीति का परिणाम रहा है। रणनीति यह है कि मेहनतकश जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवालों को सार्वजनिक चर्चा से बाहर रखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को जज्बाती मुद्दों में उलझाए रखा जाए। 1990 के बाद तीन परिघटनाएं हावी हुईं, जिन्हें हम मार्केट (नव-उदारवाद), मंदिर एवं मंडल के नाम से पहचान सकते हैं। नरेंद्र मोदी का दौर आते-आते भाजपा इन तीनों परिघटनाओं का प्रतिनिधित्व करती दिखने लगी। या इसे ऐसे कहा जाए कि ये तीनों परिघटनाएं भाजपा में समाहित हो गईं।
2024 के आम चुनाव की विशेषता यह है कि उपरोक्त परिघटनाओं के इर्द-गिर्द लोगों की गोलबंदी की इसमें सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं। मगर अभी इनके बरक्स किसी वैकल्पिक विमर्श के खड़ा होने का कोई संकेत नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वह 1990 के दशक में प्रचलित हुए विमर्श एवं शब्दावलियों की कैद बना हुआ है।
जबकि जब तक वैकल्पिक विमर्श या नीतियों की पैरोकार ताकतें राजनीतिक क्षितिज पर नहीं उभरती हैं, मोदी शैली की राजनीति के निश्चित क्षय की संभावना कमजोर बनी रहेगी। लोग अपनी नाराजगी बेशक आज सड़कों से लेकर मतदान केंद्रों के अंदर तक जाकर जताने लगे हैं, लेकिन वे इसके लिए भी तीन दशक पुराने विमर्श की पैरोकार किसी शक्ति को ही माध्यम बनाने को विवश हैं। आम मतदाताओं की ऐसी मजबूरी चुनावी लोकतंत्र वाले ज्यादातर देशों में आज देखने को मिल रही है।
इसलिए जो लोग मोदी शैली की राजनीति को अतीत की बात बनाना चाहते हैं, उनके सामने चुनौती वैसा विमर्श खड़ा करने की है, जिसके केंद्र में मेहनतकश आवाम के वास्तविक हित हों। विकास का वह विमर्श हो, जो आम जन को उनके un-freedoms (स्वतंत्रताओं से वंचित करने वाली परिस्थितियों) से मुक्त करने पर केंद्रित हो। जब तक ऐसा नहीं होता, लोगों को विकास के बाजारवादी तर्क और identity politics (अस्मिता आधारित राजनीति) से भटकाने की स्थितियां बनी रहेंगी। और तब तक मोदी शैली की राजनीति का विकल्प नहीं उभर सकेगा, भले मोदी खुद राजनीति के केंद्र में ना रह जाएं।