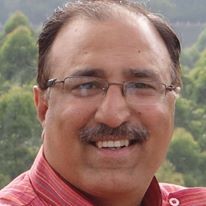पुष्पा गुप्ता
*गन्धः सुवर्णे फलमिक्षुदण्डे नाकारि पुष्पं खलु चन्दनस्य।*
*विद्वान् धनाढ्यश्च नृपश्चिरायुः धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभूत्॥*
~चाणक्यनीति (9:3).
[सोने में सुगंध नहीं होती। गन्ने में फल नहीं लगते। चंदन पर फूल नहीं आते। विद्वान (प्राय:) धनवान नहीं पाए जाते। और (न्यायी) राजा (प्राय:) दीर्घजीवी नहीं होते। लगता है, विधाता को कोई बुद्धिमान सलाहकार नहीं मिला।]
यानी मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी अपूर्ण है। पूर्णत्व मात्र एक प्रत्यय (idea) है जो मनुष्य की चेतना का उन्मेष है, उसकी चिर अभिलाषा। मानव चेतना के इसी उन्मेष ने पूर्ण ईश्वर की परिकल्पना की होगी। ईश्वर भक्त के मन में है, ज्ञानी की अवधारणा में है, कर्मयोगी के योग: कर्मसु कौशलम् में है।
जहां भी है, मनुष्य से स्वतंत्र नहीं है। चौरासी लाख योनियों में केवल मनुष्य ईश्वर का भार ढो रहा है। कंधे पर नहीं, चेतना में। उसकी चेतना से स्वतंत्र किसी भी धर्म के ईश्वर का कोई पता ठिकाना मिले तो जाकर उसका दर्श-पर्श कर आया जाए। उससे कुछ गुफ़्तगू भी। सनातन में बस नेति नेति के कंटीले तार की बाड़ भर नज़र आती है।
फ़िलहाल इस सुभाषित से मनुष्य की फ़ितरत का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। मनुष्य को प्राय: अपने प्रतिद्वंद्वी में कोई गुण, कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। उसी तरह अपने में कोई बुराई नज़र नहीं आती। बहुत चपेट में प्रतिद्वंद्वी के किसी गुण को नकारना असंभव हो गया तो उसे टालकर उसके दस अवगुण गिना देगा।
कोई योग्य हुआ तो तत्काल बोलेगा–होगा, लेकिन बहुत बेईमान है। कोई ईमानदार हुआ तो बोलेगा–होगा लेकिन बिलकुल निकम्मा है।
बहुत विद्वान हुआ को कह देगा, होगा लेकिन व्यवहार में बिकुल अनाड़ी है, बहुत व्यवहार-कुशल हुआ तो बोलेगा, होगा, लेकिन कुछ आता-जाता नहीं, एकदम पैदल है।
आजकल शैक्षणिक डिग्री को फ़र्ज़ी घोषित करने का नया फ़ैशन ईजाद हुआ है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों के बारे में निश्चित तौर पर कहना लगभग असंभव है कि कौन कहां तक पढ़ा है।
प्रतिद्वंद्वी से पूर्ण होने की अपेक्षा दरअसल अपनी अपूर्णता, अपने अवगुणों को ढकने का एक कवच है।
कहते हैं, राजतंत्र बहुत बुरा था। राजा आपस में भिड़ते रहते थे। लेकिन कई प्रसंग आते है जहां प्रतिद्वंद्वी की वीरता, बहादुरी या अन्य गुणों से अभिभूत, उसे हराने के बावजूद उसकी तारीफ़ की गई और मित्र बना लिया गया।
और जनतंत्र में?
प्रतिद्वंद्वी के किसी गुण की, किसी उपलब्धि की तारीफ़? भूल जाइए। मुझे तो आज तक नहीं सुनाई पड़ी। आपको पड़ी हो तो आप ख़ुशक़िस्मत हैं।
यह बीमारी इतनी व्यापक है कि मैदान में उतरे प्रतिद्वंद्वी ही नहीं, उनके समर्थक, उनके लग्गू भग्गू तक इसकी चपेट में हैं। संदेह हो तो फ़ेसबुक महाराज के साम्राज्य का एक चक्कर लगा आइए।
_पता नहीं, राजतंत्र से जनतंत्र की यात्रा उत्थान की है या पतन की।_
(चेतना विकास मिशन)