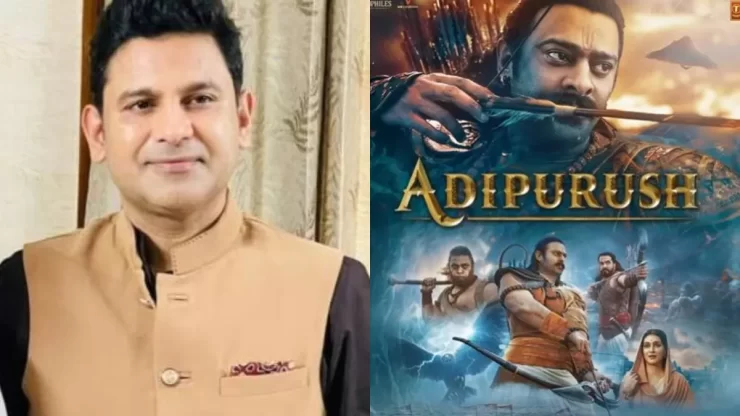दुष्यन्त

चलो, किसी बहाने हिंदी फिल्मों के संवादों पर विमर्श शुरू हुआ। ‘आदिपुरुष’ ने यह बहस छेड़ी है। बुद्धिजीवी भद्रजन हिंदी फिल्मों के विमर्श से अमूमन दूर रहते रहे हैं। हमारा मध्यमवर्गीय समाज भी दशकों तक सिनेमा को युवाओं के लिए बुराई की तरह देखता रहा है। बच्चों को टोका जाता रहा है- ‘फिल्में देखोगे तो बिगड़ जाओगे’। कोई संचार माध्यम केवल पवित्रता लिए हुए नहीं होता। हर संचार माध्यम नए दरवाजे खोलता है। हरेक के खतरे भी हैं और सकारात्मक पहलू भी।
सिनेमा को अगर जीवन सीखने के माध्यमों में से एक माना जाए तो यह किसी किताब से कम नहीं है। मेरी निजी राय है कि सिनेमा को कायदे से स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाए तो यह समाज को सुंदर बनाने की दिशा में कुछ सार्थक हो सकता है। सिनेमा संस्कृतियों के बीच पुल बनाता है, इंसानों के मध्य बेहतर जुड़ाव का रास्ता बनाता है, जीवन जीने के अलग-अलग तरीकों, नैतिकताओं से मिलवाते हुए व्यवहार में उदार बनाकर बेहतर मनुष्य बनाने का काम चुपके-चुपके करता है। हालांकि यह सभी कलाओं की बुनियाद मानी जाती है कि ये हमें उदार बनाती हैं। अगर कोई कलाकृति हमें उदार नहीं बनाती तो कला होने से ही संदिग्ध हो जाती है।
हिंदी सिनेमा की संवाद परंपरा भी बड़ी खास और अलहदा रही है। लंबे समय तक ऐसी भाषा में संवाद होते थे जो केवल हिंदी फिल्मों की अपनी यूनिवर्सल सी भाषा थी। पात्र कहां से है, कितना पढ़ा-लिखा है, इस बात का उस पात्र के संवादों से कोई रिश्ता नहीं दिखता था। सकारात्मक तरीके से देखें तो इसका सुख भी था, सहूलियत भी थी। बड़े वर्ग को बिना किसी बाधा के कहानी में इन्वॉल्व रखना संभव होता था। हालांकि जब कुछ दशक पहले स्थानीयता की प्रामाणिकता को तरजीह देने वाले फिल्मकारों ने भाषा की स्थानीयता को फिल्म के संवादों में शामिल किया, तो संवादों का एक अलग ही रंग खिलकर आया। इसके सुख भी थे, तो चुनौतियां भी भारी थीं। उदाहरण के तौर पर कहानी उदयपुर की हो, पर अगर पात्र राजस्थानी भाषा के नाम पर सवाई माधोपुर-करौली या गंगानगर या भरतपुर की भाषा उसी लहजे और शब्द में बोलेगा, तो चाहे राजस्थान से बाहर के लोग इसे नोटिस भी न करें, पर भाषा के लोकल टच के नाम पर जो मूर्खता प्रकट होगी वह राजस्थान के दर्शकों में सबसे पहले उस कंटेंट से झुंझलाहट पैदा करेगी।
कहानी और पात्रों की भाषा के संदर्भ में स्थानीयता की प्रामाणिकता के साथ एक बड़ी चुनौती काल विशेष में भाषा के निर्वहन की भी होती है। अगर पीरियड फिल्म है तो यह चुनौती अपने चरम पर पहुंच जाती है। वैसे चुनौती मानो तो होती है, वरना जो मन में आए, जो सहज भाव से आए वही पंथ है। हालांकि चुनौती का द्वंद्व मीडियम की व्यापकता के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ा बजट, बड़े ऑडिएंस को संबोधित करने की विवशताएं कंटेंट को पवित्रता के साथ कहां निभाने देती हैं भला! पर इसका सुंदर सैद्धांतिक पक्ष यह भी है कि हिंदी सिनेमा के संवादों में खिचड़ीपन या भाषाई विविधता उसे कबीर की सधुक्कड़ी भाषा परंपरा से जोड़ती है।
संवाद क्या है? जीवन में बोलने के व्यवहार का नाटकीय रूप या सृजनात्मक रूप। तो फिर सवाल उठता है कि इस बोलने के व्यवहार की हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है, ‘ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे, आपहूं शीतल होय।’ यही आदर्श भी है, पर यह कोई यूटोपियन आदर्श नहीं है कि जिसे संभव न बनाया जा सके। गांव में एक मौजिज व्यक्ति थे, उनके लिए मशहूर था कि गुस्से में भी उनका अपनी वाणी पर संयम अद्भुत था। घोर गुस्से में भी बस यही कहते, ‘मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी’। यह है भाषा को बरतने का हुनर और अभ्यास। कहने का भाव यह है कि आप क्या बोलते हैं, यह सीधे तौर पर आपके चयन और अभ्यास का विषय है। अच्छे सिनेमा में संवाद अगर जीवन के करीब हों तो उसे बेहतर माना जाता है। आदर्श और यथार्थ की संधि पर खड़े संवाद दूर तक, देर तक असर रखते हैं। इतना आदर्श भी न हो कि अव्यावहारिक लगे, इतना यथार्थ भी न हो कि आदर्श की ओर जाने के रास्ते ही बंद हो जाएं। सिनेमा के संवाद लेखक की भीषण दुविधा और काम की मुश्किलें देखिए कि उसे आदर्श, यथार्थ, सरोकार और मनोरंजन के चार पहलुओं के बीच में अपना काम करना होता है। गालियों या तालियों का प्रसाद इसी से तय होना होता है।
हम नाटकों, कहानियों, फिल्मों की बदलती भाषा को जीवन में बदलती भाषा के साथ जोड़कर देखें तो काफी चीजें सहज हो सकती हैं। यह जोड़कर देखना मुश्किल काम नहीं है, जरूरत है कि देखना चाहें। हिंदी पट्टी के मध्यमवर्गीय परिवारों में भाषा का व्यवहार पिछली तीन पीढ़ियों में जिस तेज गति से बदला है, शायद उससे पहले की 5-7 पीढ़ियों में न बदला हो। यहां यह भी मेरी राय है कि महादेश भारत के महा हिंदी प्रदेश में भी कई सदियों के बहुसंख्य भाषाई रूप एक साथ एक समय में मौजूद रहते हैं। हिंदी सिनेमा ने संवादों में एक खास हिंदी का ईजाद या विकास किया है, जो केवल हिंदी पट्टी ही नहीं, गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विस्तार करती है। हिंदी फिल्में गैर हिंदी क्षेत्रों के लोगों को हिंदी बोलना सिखाती रही हैं। यह योगदान अपने प्रभाव विस्तार के लिहाज से केंद्र-राज्य सरकारों के और गैरसरकारी हिंदी इदारों से बड़ा रहा है। शायद इसकी ठीक-ठीक तुलना हिंदी पट्टी में हिंदी अखबारों के योगदान से ही की जा सकती है, जिन्होंने अघोषित रूप से, परोक्ष रूप से हिंदी भाषा को न केवल बचाया है, उसे जनमानस में एक अच्छे स्तर पर समृद्ध किया है।
(लेखक हिंदी सिनेमा के गीतकार-स्क्रिप्ट राइटर हैं)