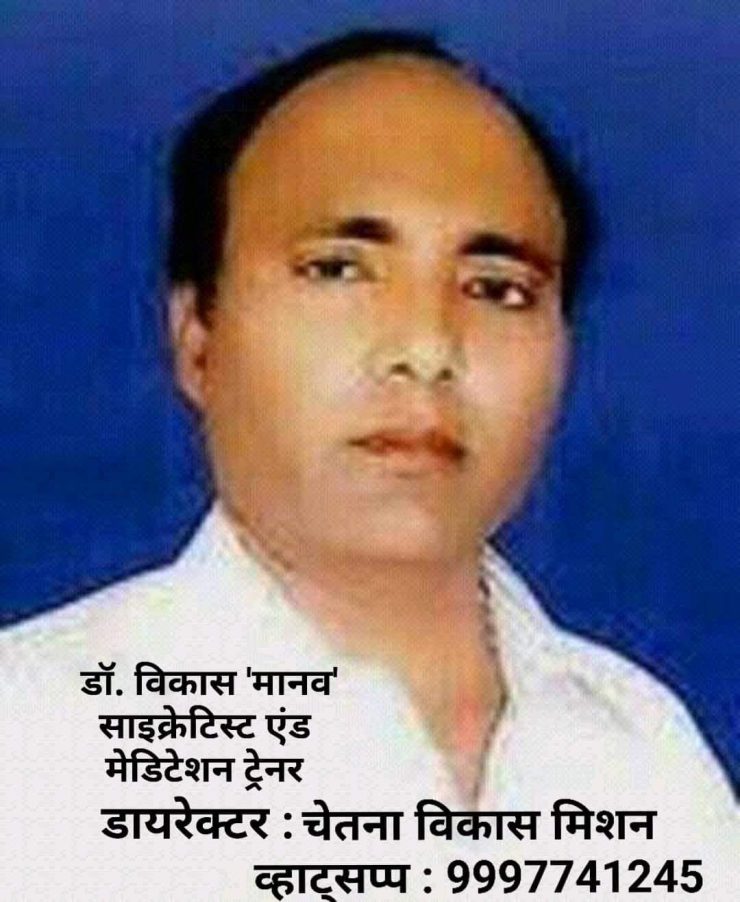डॉ. विकास मानव
एकं सद्विप्रा: बहधा वदन्ति।
— ऋग्वेद (1.164.46)
सत्य स्वरूप ईंश्वर एक है, विद्वज्जन उसे बहुत नामों से कहते हैं।
*मुख्यत: तीन बिन्दु :*
(i). ईश्वर एक है, सभी देवता उसकी शक्तियों के नाम हैं।
(ii). न तस्य प्रतिमा अस्ति।
-ईश्वर निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा / मूर्ति नहीं। मूर्ति पूजा जड़ता है।
(iii). ईश्वर का कोई शरीर नहीं, नस-नाड़ी नहीं । सर्वव्यापी ईश्वर मनुष्य या अन्य किसी प्राणी रूप में अवतार नहीं ले सकता। अवतारवाद की अवधारणा जड़तापूर्ण है।
*कुछ कतिपय उद्धृत :*
(i) तदेवाग्निस् तदादित्यस् तद्वायुस् तदु चन्द्रमा:।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ताsआप: स प्रजापति:।।
— यजुर्वेद 32.1
अर्थात् वह प्रजापति ब्रह्म है, वही शुक्र है, वही आप: है, वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है।
सभी का स्वामी होने से प्रजापति, सबसे महान् होने के कारण ब्रह्म, अग्नि के समान प्रकाश स्वरूप होने से अग्नि, शान्त स्वभाव होने से चन्द्रमा, दुष्टों को दण्ड देकर रुलाने वाला होने से, वह रुद्र कहलाता है। ये सभी नाम किसी चेतन देवी-देवता के नहीं, अपितु, ईश्वर के ही नाम हैं जो उसकी विविध शक्तियों को अभिव्यक्त करते हैं।
(ii) न तस्य प्रतिमाsअस्ति यस्य नाम महद्यशः।
— यजुर्वेद 32.3
जिसकी इतनी महिमा है , जिसने विशाल ब्रह्माण्ड की रचना की है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। उसका कोई शरीर नहीं, कोई आंख नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी वह संकल्प मात्र से, समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करता है।
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता
पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः।
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता
तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्।।
— श्वेताश्वतर-उपनिषद् 3.19
परमेश्वर के हाथ नहीं, परन्तु अपने शक्तिरूप हाथ से सब का सृजन और ग्रहण करता है ; पग नहीं, पर सर्व व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान् है ; उसके चक्षु नहीं , परन्तु सबको यथावत् देखता है ; श्रोत्र नहीं, फिर भी सब की बातें सुनता है ; वह समस्त विश्व को जानता है, परन्तु उसे जानने वाला कोई नहीं। उसको सनातन, सबसे श्रेष्ठ और सब प्रकार से पूर्ण होने से महान् पुरुष कहते हैं ।
(iii) स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम्
अस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्।
कविर्मनीषी परिभुः स्वयम्भूर्
याथातथ्यतोsर्थान् व्यदधाच्छाश्तीभ्यः समाभ्यः।।
–— यजुर्वेद 40.8
अर्थात् वह ब्रह्म सर्व व्यापक है, (शुक्र) सर्वशक्तिमान् है, (अकाय) काया रहित /शरीर रहित है, (अव्रणम्) उसमें कोई छिद्र / दोष नहीं, (अस्नाविरम्) नस-नाड़ी रहित है, (शुद्धं) शुद्ध, पवित्र है, (अपापविद्धम्) पापरहित है, वह कोई पाप नहीं करता, (कवि) सर्वज्ञ है, (मनीषी) सब जीवों की मनोवृत्तियों को जानने वाला है, (स्वयम्भूः) अनादि, शाश्वत है, उसका कोई माता-पिता नहीं (Self- Born / Causus Causa), उसने अपनी समस्त प्रजा के लिये वेद ज्ञान दिया है।
जब उसका शरीर नहीं , नस – नाड़ी नहीं, आंख नहीं, हाथ-पांव नहीं, वह जन्म कैसे ले सकता है ? यह ध्यान देने योग्य है कि ये सारे अवयव जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर में संनिहित होते हैं और ईश्वर का तो कोई शरीर ही नहीं ! इसके अतिरिक्त सर्व व्यापक ईंश्वर एक छोटे से शरीर में कैसे समाहित हो सकता है ?
(क) डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् अपने भगवद्गीता भाष्य में अवतारवाद के विषय में लिखते है :
ईश्वर कभी सामान्य रूप में जन्म (अवतार) नहीं लेता। अवतार केवल मानव की आध्यात्मिक एवं दैवी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। अवतार दिव्यशक्ति का मानव शरीर में सिकुड़ कर व्यक्त होना नहीं, बल्कि मानव- प्रकृति का ऊर्ध्वारोहण है जिसका दिव्य शक्ति से मिलन होता हैl
(ख ) ईश्वर को रावण या कंस के वध के लिये अवतार लेने की क्या आवश्यकता है ? सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् , अन्तर्यामी ईश्वर जो संकल्प मात्र से समस्त सृष्टि की रचना करता है, तो क्या वह उनकी जीवन लीला संकल्प मात्र से, हृदयाघात (Heart-attack) या मस्तिष्क सम्फोट (Brain-Haemarage) द्वारा समाप्त नहीं कर सकता ?
अतः ईश्वर को मानव शरीर धारण करने की ज़हमत उठाने की क्या आवश्यकता है !
(ग) हर देश, हर युग में राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति पैदा होते रहते हैं और होते रहेंगे। क्या बिन-लादेन व बगदादी रावण और कंस से कम राक्षस-प्रवृत्ति के थे ? अगर राष्ट्रपति बराक ओबामा, ओसामा बिन-लादिन की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बग़दादी की हत्या करवा सकते हैं, तो क्या कोई पराक्रमी महापुरुष, ईश्वर की प्रेरणा से रावण व कंस का वध नहीं कर सकता ? यदि हर राक्षस को मारने के लिये ईश्वर को अवतार लेना पड़े, तो ईश्वर सदा-सर्वदा के लिये अग्निशमन कार्य (Fire-fighting) में व्यस्त दिखाई देगा।
(घ) अवतारवाद पुराणों की अवधारणा है। वेद, उपनिषद्, षड्दर्शन में कहीं भी ईश्वर के अवतार के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। उनकी मान्यता है कि धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेता है। पुराणों में मत्स्य अवतार तथा कूर्मावतार का वर्णन है। मत्स्य अवतार या कूर्म अवतार से किन दुष्टों का संहार हुआ और कैसे धर्म की स्थापना हुई ?
कई विद्वानों का मत है कि पुराणों में वर्णित अवतार की परिकल्पना जीव की पृथ्वी पर उत्पत्ति (Evolution of life on Earth) को इंगित करती है। अतः पुराणों की अवतार की अवधारणा गहन अन्वेण, शोध एवं चिन्तन की अपेक्षा रखती है। इसे शाब्दिक अर्थ में (Literally) लेने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
संक्षेप में, ईश्वर अवतार की अवधारणा वेद – उपनिषद् – दर्शन-शास्त्र के अनुरूप नहीं है ; न ही यह तर्क संगत है ; न तो ईश्वर का अवतार लेना सम्भव है और न ही आवश्यक।
*ऋग्वेद (1.3.12) का ये मंत्र को सदा स्मरणीय :*
महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना।
धियो विश्वा वि राजति ।।
अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञान एक सागर है, जो दिव्य दृष्टि से, विश्व को प्रकाशित करता है।
अनेक- ईश्वरवाद ( Polytheism), सर्वेश्वरवाद ( Henotheism), देवी-देवतावाद तथा उनका मानवीकरण ( Pantheon of gods and their Personification), मूर्ति पूजा, (Idol Worship), ईश्वर-अवतारवाद (Incarnation of God) की भूलभुलैया (Labyrinth) में भटकने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ये सभी अवधारणाएं अवैदिक हैं।
*आधारभूत प्रश्न :*
क्या शक्ति ही ईश्वर का स्वरुप है ? ब्रह्माण्ड की हर वस्तु का आदि और अन्त है, उसमें हर कण का निर्माण और विनाश होता रहता है। यदि ब्रह्माण्ड ही ईश्वर है तो वह सर्वशक्तिमान, अविनाशी और अनन्त कैसे है ?
*हमारा उत्तर :*
शक्ति ईश्वर नहीं है, वह ‘ईश्वरतत्व’ का गुण है। यह गुण भी ‘ईश्वरतत्व’ में तब पैदा होता है जब वह स्थूल की ओर पहला कदम बढ़ाता है। जब वह स्थूल पदार्थ के निर्माण की दिशा में अग्रसर होता है तो वह प्रथम चरण में शक्ति के रूप में परिलक्षित होता है। अपनी मूल अवस्था में वह तत्व निर्गुण होता है क्योंकि गुण भी उसी तत्व के कारण पैदा होता है और उसी में समाहित हो जाता है।
जब तक शक्ति के प्रदर्शन के लिए स्थूल उपलब्ध नहीं होता तब तक वह शक्ति प्रभावहीन रहती है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि धन शक्ति का प्रभाव तभी दृष्टिगोचर होता है जब ऋण शक्ति हो। शक्ति दो विभवान्तरों के बीच ही क्रियाशील होती है। अकेले धन शक्ति ,ऋण शक्ति के अभाव में निष्क्रिय है।
‘ईश्वरतत्व’ सृष्टि निर्माण के हेतु स्वयं दो भागों में विभक्त हो जाता है। वह स्वयम ही विभवान्तर पैदा करता है और ऋण तथा धन शक्तियों में बदल कर निर्माण और विध्वंस के खेल रचता है। यह धन और ऋण (पुरुष और प्रकृति) धन शक्ति के ही दो रूप हैं।
क्योंकि जब हम ऋण शक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि दो शक्तियों में से एक की तीव्रता कम है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि ऋण शक्ति में शक्ति है ही नहीं। तर्कशास्त्र कहता है कि तुलनात्मक विश्लेषण के बिना ‘है’ और ‘नहीं’ की कल्पना नहीं की जा सकती। ‘शून्य’ नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जिसे हम शून्य कहते हैं वहां भी ‘कुछ’ होता है। इसीलिए शक्ति की नकारात्मक कल्पना असम्भव है।
‘ईश्वरतत्व’ स्वयं अपनी इच्छानुसार अपने को दो रूपों में विभक्त करता है। वह एक रूप में ‘जड़ता’ की ओर अग्रसर होता है और दूसरे रूप में ‘मुक्त’ रहता है। पहले रूप पर दूसरा रूप प्रतिक्रिया करता है और इस प्रकार वह अपने आपको परिलक्षित करता है। फिर पहला रूप जड़ता के कई स्तर तक बंट जाता है और असंख्य विभवान्तर वाली वस्तुओं का निर्माण करके एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करने लगता है। ब्रह्माण्ड में हो रही समस्त घटनाओं और क्रियाओं का यही कारण है।
वह एक ही तत्व कई रूपों में इसी प्रकार बदल गया है। यह ब्रह्माण्ड उस ‘मूलतत्व’ के लिए ऋण का काम करता है जिसका निर्माण भी उसी ‘मूलतत्व’ से हुआ है। इसलिए ब्रह्माण्ड को ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप कहा जा सकता है। वह ‘ईश्वरतत्व’ ही ब्रह्माण्ड के कण-कण में जड़ता की विभिन्न स्थितियों में विद्यमान है।
यह ब्रह्माण्ड ‘ईश्वरतत्व’ द्वारा निर्मित प्रकृति मात्र है। उसका निर्विकार स्वरुप अरबों गुना बड़ा है। उसका स्वरुप इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना भी दुष्कर है। यह ब्रह्माण्ड उसी ईश्वरतत्व के छोटे से हिस्से में व्याप्त है। यह उसी से निर्मित है और एक दिन उसी में समाहित हो जायेगा। क्योंकि जो जिससे बना है वह अपने मूल रूप में समाहित हो जाता है। ईश्वर का ‘सच्चिदानंदस्वरूप’ तर्क से परे है। उसे केवल ज्ञानी ही अपने ज्ञान चक्षुओं से देख सकता है।
*आध्यात्मिक जगत :*
आध्यात्मिक जगत क्या होता है ?
आध्यात्मिक जगत का मतलब होता है–आत्मसत्ता में प्रवेश। कोई भी साधना हो, चाहे वह योग की हो या हो तंत्र की–भौतिक जगत से शुरू होती है और पारलौकिक जगत का अतिक्रमण करती हुई आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट होती है।
मुख्य रूप से तीन ही जगत हैं–भौतिक जगत, पारलौकिक जगत और आध्यात्मिक जगत। इन्हीं तीनों में सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ है।
साधना-भूमि में सर्वप्रथम भौतिक जगत का अतिक्रमण होता है जिसके परिणामस्वरूप समस्त इन्द्रियों से मन का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है।
जैसा कि हम सब भली-भांति जानते हैं कि मनुष्य शरीर में पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच कर्मेन्द्रियाँ होती हैं। मन उनका अधिष्ठाता है। अर्थात् मन अपना कार्य इन्हीं इन्द्रियों की सहायता से कर पाता है।
स्थूल शरीर में यदि इन्द्रियां मन का साथ न दें तो मन व्यर्थ हो जाता है, उसकी व्यर्थता तब समझ में आती है जब स्थूल शरीर छूट जाता है। मन इस नयी परिस्थिति में व्याकुल हो जाता है। क्योंकि मन के भीतर हज़ारों साल के वही संस्कार विद्यमान हैं और मन उनका आदी रहता है।
मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका स्थूल शरीर जिसमें समस्त इन्द्रियां विद्यमान रहती है, छूट जाता है। अब उसे जीवित अवस्था की तरह भूख लगती है, प्यास लगती है और काम-वासना सताती है। इस विकट अवस्था में मृत व्यक्ति का मन व्याकुल होकर इधर-उधर भटकता है पर उसे कहीं कोई राहत नहीं मिलती, कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है क्योंकि मन की इन्द्रियां उसके पास उपस्थिति नहीं होती हैं।
उस व्याकुल, पागल की स्थिति मन वाला मृत व्यक्ति वासना के प्रबल वेग के फलस्वरूप ही प्रेत शरीर को उपलब्ध हो जाता है।
भौतिक जगत में जब व्यक्ति भौतिक शरीर से साधना करता है तो सर्वप्रथम भौतिक जगत का ही अतिक्रमण होता है। इसका फल यह होता है कि साधक के मन का सम्बन्ध इन्द्रियों से समाप्त हो जाता है। साधना का प्रथम लाभ या उद्देश्य है मन की मनमानी कम करना, मन को क्षीण करना। मन का उसकी इन्द्रियों से सम्बन्ध विच्छेद करना।
इसके बाद साधना में पारलौकिक जगत का अतिक्रमण होता है। इसके परिणामस्वरूप बुद्धि से मन का सम्बन्ध टूट जाता है। यहाँ यह समझने की बात है कि कोई व्यक्ति जब कोई भी कार्य करने को उद्यत होता है तो सर्वप्रथम उसे कार्य के सफल होने के लिए संकल्प लेना होता है।
बिना संकल्प किये कार्य शुरू करने पर असफलता ही हाथ लगती है। संकल्प में मनुष्य का बुद्धितत्व कार्य करता है। बुद्धि अच्छा क्या है, बुरा क्या है ? –इसका विवेक जगाती है। अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है और बुरा करने से रोकती है। उसको इस तरह समझा जा सकता है कि मनुष्य ने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन मन्दिर भगवान के दर्शन करने जायेगा तभी अपना दैनिक कार्य शुरू करेगा।
लेकिन जब वह घर से बाहर निकला तो रास्ते में मदिरा की दुकान मिल गयी और उसका मन भटकने लगा। फल यह हुआ कि वह निकला था मंदिर जाने के लिए और मन ने उसे मदिरालय पहुंचा दिया। यदि हमने संकल्प कर रखा है तो बुद्धि मन की लगाम कस कर रखेगी। हमारे मदिरालय की ओर उठने वाले कदम वह रोक देगी। तो जब पारलौकिक जगत का अतिक्रमण होता है तो बुद्धि से मन का सम्बन्ध भी टूट जाता है।
साधना के तीसरे चरण में साधक का प्रवेश आत्मजगत में होता है जिसकी उपलब्धि है–मन और आत्मा का सम्बन्ध भंग होना। साधक को अपनी आत्मा का बोध मन के साथ सम्बन्ध भंग होने पर ही होता है और यह आत्म-बोध जिस वातावरण में, जिस स्थिति में होता है, वह है–अध्यात्म।
मगर आद्यात्म जगत में प्रवेश के मार्ग में इन्द्रियां, मन और बुद्धि बाधक हैं। इन तीन बाधाओं का निवारण आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब हम तीनों के अस्तित्व का अलग-अलग बोध करें। साधारणतया हम तीनों का बोध एक साथ करते हैं। अलग-अलग बोध होना अति कठिन कार्य है। इसी कठिन कार्य को करने के उपाय को साधना कहते हैं, तपश्चर्या कहते हैं।
*आत्मबोध की उपलब्धि :*
बोध और अनुभूति में अन्तर है। बोध बाह्य विषय से और अनुभूति आन्तरिक विषय से सम्बंधित है। सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व का बोध होता है, आत्मतत्व का ज्ञान होता है, उसके बाद अनुभूति होती है।
*अनुभूति किसकी ?*
आत्मा की और उसके बाद आत्मखण्ड की। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे हमारे सामने आग है, उसे देखना केवल उसके अस्तित्व का बोध करना है और आग का स्पर्श करना उसकी अनुभूति है। इसी प्रकार आत्मा के अस्तित्व को जानना, समझना, देखना आदि उसका मात्र बोध है।
उसके आन्तरिक स्वरुप, गुणधर्म आदि से परिचित होना तथा आत्मस्वरूप को उपलव्ध होना तथा साथ ही साथ ‘आत्मखण्ड’ से भी परिचित होना आत्मानुभूति के विषय हैं।
*’आत्मखण्ड’ से तात्पर्य :*
कोई भी आत्मा पूर्णात्मा नहीं है। पूर्णात्मा केवल परमात्मा है। आत्मा नाम की वस्तु तो एक ही है लेकिन देश, काल व पात्र के अनुसार भिन्न-भिन्न विशेषण उसके साथ जुड़ जाने के कारण वह जीवात्मा, मनुष्यात्मा, प्रेतात्मा, देवात्मा आदि संज्ञा ग्रहण कर लेती है।
फिर भी आत्मा रहती है खण्डित ही। जीवों में नर जीव और मादा जीव, मनुष्यों में पुरुष और स्त्री, प्रेतों में भूत-पिशाच, प्रेत, और उनकी स्त्री सत्ता भूतिनी, पिशाचिनी, प्रेतिनी आदि। इसी प्रकार देवात्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए।
सृष्टि के प्राक्काल में जैसे मूल परमतत्व ने दो खण्डों में विभाजित होकर ‘शिवतत्व’ और ‘शक्तितत्व’ की संज्ञा धारण कर ली। उसी प्रकार उसी अखण्ड, अनन्त विराट सत्ता से निर्गत होने वाली आत्मा सबसे पहले ‘अहम्’ के रूप में निःसृत हुई और साथ ही उसकी विपरीत सत्ता जिसे ‘प्रकृति’ कहा जाता है, ‘इदम्’ के रूप में अवतरित हुई।
अहम् आत्मा है और इदम् है आत्मा की प्रकृति। पहला खण्ड है पुरुषतत्व प्रधान और दूसरा खण्ड है स्त्रीतत्व प्रधान। दोनों एक ही सत्ता के दो रूप और दो खण्ड हैं। यह अध्यात्मशास्त्र का अति गम्भीर विषय है। किसी शास्त्र, किसी दर्शन में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है। सब ओर भ्रान्ति ही भ्रान्ति ही। केवल वे ही लोग इस विषय का ज्ञान कर सके हैं जिन्होंने आत्मानुभति और आत्म साक्षात्कार कर लिया है।
उन्हीं के द्वारा अनुभूत होने के बाद ही यह गूढ़ और गहन विषय प्रकाश में आ सका है।
इसी प्रकार मन के बारे में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। मन क्या है ?–इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। योगी के लिए, तान्त्रिक के लिए, ज्योतिषी के लिए और वैद्य के लिए मन का अस्तित्व भिन्न- भिन्न है। कोई-कोई लोग मन को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं।(पदार्थ के तीन रूप होते हैं–ठोस, द्रव और गैस या ऊर्जा रूप। मन के भी इसी प्रकार के तीत रूप हैं।) लेकिन जहां तक ‘कुण्डलिनी योग’ का सम्बन्ध है, उसमें मन को आत्मा का ही एक भाग माना गया है।
वास्तव में आत्मा और मन एक ही वस्तु के दो रूप हैं। जो रूप स्थिर है, निष्क्रिय है–वह आत्मा है और जो रूप क्रियाशील है, चैतन्य है– वह है मन। उसकी जो क्रियाशीलता और चैतन्यता है, उसकी साक्षी आत्मा है। बस, आत्मा और मन में यही भेद है। मूल में दोनों एक ही सत्ता का प्रतिपादन करते हैं।
आत्मा की तरह मन के भी दो रूप हैं। पहला रूप आत्मा के पुरुषतत्व प्रधान ‘अहम्’ के साथ और दूसरा रूप उसके स्त्रीतत्व प्रधान ‘इदम्’ के साथ संयुक्त है। मन का अस्तित्व मात्र मनुष्य में है–इसीलिए वह मनुष्य है। मानवेतर प्राणियों में केवल प्राण का आभास है, मन के अस्तित्व का नहीं।
इसीलिए तो उन्हें ‘प्राणी’ कहा जाता है। प्राणी कहने से तात्पर्य प्राणतत्व मुख्य होने के कारण है।
अपने-अपने मन के साथ आत्मा के दोनों खण्ड ‘अहम्’ और ‘इदम्’ सृष्टि के उन्मेष काल में ही काल के प्रवाह में पड़कर एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों का वियोग कब, कैसे और किस अवस्था में हुआ–यह नहीं बतलाया जा सकता।
लेकिन इतना तो निश्चित है कि आत्मा की तरह मन के दोनों खण्ड भी एक दूसरे से मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं और फिर उसी वियोगजन्य व्याकुलता के फलस्वरूप पुनर्मिलन की आशा में ‘अहम्’ पुरुषशरीर में और ‘इदम्’ स्त्रीशरीर में बार-बार जन्म ग्रहण करता रहता है। यही क्रम आदिकाल से चला आ रहा है।
आत्मा और मन के अपने अपने-अपने दोनों खण्डों का मिलना आवश्यक है, तभी पूर्णात्मा होगी और तभी पूर्ण मन होगा। पूर्णात्मा होने का मतलब है–जन्म-मरण से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति और भवचक्र से मुक्ति। तान्त्रिक लोग इसी अवस्था को ‘सामरस्य भाव’ अथवा ‘अद्वैत स्थिति-लाभ’ कहते हैं।
योगियों का ‘परम निर्वाण’ भी यही है। लेकिन परम निर्वाण, परम मुक्ति या अद्वैत स्थित लाभ उसी स्थिति में सम्भव है जब आत्मा के साथ उसका मनस्तत्व आत्मा से छूट जाता है। आत्मा और मन की मिलकर जो द्वैत स्थिति है, वह हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।
यही है ‘कैवल्य’, यही है अदैतावस्था’ जहाँ आत्मा के साथ कोई दूसरा तत्व नहीं बचा है।