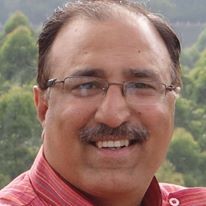पुष्पा गुप्ता
तिब्बत की तरफ से एक हमला कुमाऊं पर तेरहवीं सदी की शुरुआत में, यानी ‘राजुला-मालाशाही’ के निर्धारित कथा समय बारहवीं से पंद्रहवीं सदी के लगभग बीच में हुआ था।
हालांकि उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होने के बजाय पूरब से पश्चिम की तरफ थी। उस समय ‘सुई’ के नाम से प्रतिष्ठित मौजूदा लोहाघाट में मिला सन 1223 ईसवी का एक शिलालेख बताता है कि ‘परम सौगत (बौद्ध राजाओं का विरुद), परम भट्टारक महाराजाधिराज श्रीमान क्राचल्लदेव नरपति ने अपने शासन के सोलहवें वर्ष में कीर्तिपुर (कुमाऊं) के राजाओं को हराकर विजयराज्य का वरण किया और यहां अपना शासन स्थापित किया।’
शिलालेख लिखे जाने की जगह ‘श्रीसंपन्ननगर’ बताई गई है, जिसे अभी पश्चिमी नेपाल के दुल्लू कस्बे के तौर पर जाना जाता है। इससे ही पता चलता है कि तिब्बती मूल के खस बौद्ध राजा क्राचल्ल देव ने सन 1207 ई. में दुल्लू में ही अपने राजवंश की गद्दी संभाली होगी। कुमाऊं से सटा हुआ पश्चिमी तिब्बत का ङारी क्षेत्र बारहवीं से पंद्रहवीं सदी के बीच छोटे रजवाड़ों वाले इलाके से उठकर महान मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बना, फिर उसके बिखराव के क्रम में ल्हासा और गूगे-पुरंग की सत्ताओं के बीच झूलता रहा।
इस दौर की शुरुआत में खसों की एक शाखा ङारी में काफी ताकतवर थी और उसके राजकाज का दायरा पूरे पश्चिमी नेपाल में फैला हुआ था। फिर पश्चिमी तिब्बत पर ल्हासा का दबदबा मजबूत होने के क्रम में यह सत्ता नेपाल की तरफ खिसकती गई और इसकी तिब्बती पहचान विलुप्त होती गई।
ङारी (अंग्रेजी वर्तनी न्गारी) का उच्चारण नेपाल में ‘खारी’ किया जाता है और अभी ङारी क्षेत्र से आए लोगों की पहचान वहां खस-आर्यों के सिर्फ एक हिस्से से जुड़ी है, जिसे ‘खरियाल ब्राह्मण’ के रूप में जाना जाता है।
*चल्ल नहीं, खस-मल्ल :*
तिब्बत से आए इस बौद्ध राजवंश के शिलालेख बोधगया और लुंबिनी में भी मिलते हैं, हालांकि इसके नाम को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। नेपाल में इसे खस-मल्ल वंश के रूप में याद किया जाता है लेकिन हजारीप्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यास ‘चारु चंद्रलेख’ में इसी के राजा अशोक चल्ल पर बात करते हुए इसको ‘चल्ल वंश’ बताते हैं।
समस्या यह है कि इसके राजाओं के नाम में कोई उपनाम आना बहुत बाद में, आधी वंश परंपरा निकल जाने के बाद शुरू होता है।
नागराज, चाप, चापिच्ल, क्राशिचल्ल, क्राधिचल्ल, क्राचल्ल, अशोक चल्ल, जितारी मल्ल, आनंद मल्ल, रिपु मल्ल, संग्राम मल्ल, आदित्य मल्ल, कल्याण मल्ल, प्रताप मल्ल, पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल, सूर्य मल्ल, अभय मल्ल। 12वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक चली अट्ठारह राजाओं की इस दो सौ साल से भी लंबी स्थानीय वंश परंपरा का कोई जोड़ तुर्कों और पठानों के हमलों वाले उस दौर में समूचे दक्षिण एशिया में नहीं खोजा जा सकता था।
चाहें तो हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी की किताब में अशोक चल्ल ज्यादा सम्मान का अधिकारी था।
बोधगया में अशोक चल्ल ने सन 1255 से 1278 के बीच कई शिलालेख लगवाए, जिनमें अपना उल्लेख ‘खश राजाधिराज’ के रूप में किया। लुंबिनी और निगलिहवा में रिपु मल्ल ने अशोक स्तंभ पर ही अपनी इबारत खुदवा दी थी और दुल्लू में सन 1357 में राजा पृथ्वी मल्ल का लगवाया हुआ प्रस्तर स्तंभ उसके पुरखों की जानकारी देता है।
इस शिलालेख में ही बताया गया है कि सम्राट नागराज ने सेम्जा को अपनी राजधानी बनाया। सन 1356 ई. की तारीख वाले उसके एक स्वर्णपत्र में ‘बुद्ध, धर्म, संघ’ के साथ-साथ ‘ब्रह्मा, विष्णु, महेश, का भी उल्लेख है, जिससे उसके धार्मिक संचरण का पता चलता है। हालांकि संस्कृत के करीब की प्राचीन नेपाली भाषा में उसका मंगलाचरण पूरी तरह बौद्ध है- ‘ओम् मणि पद्मे हुम्। मंगलम् भवतु श्रीपृथ्वीमल्लदेवः लिखितम् इदम् पुण्यम् जगती सिद्यस्या।’
इस खस राजवंश का हिंदूकरण कत्यूरी वंश की तरह झटके में तो नहीं हुआ, न ही उसकी तरह इसने स्वयं को ‘परम श्रमण रिपु’ (श्रमणों का महाशत्रु) लिखना शुरू किया, लेकिन राजा रिपु मल्ल के समय से ही हिंदू संस्कार इसमें आने शुरू हुए और पृथ्वी मल्ल के बाद इसकी बौद्ध पहचान पूरी तरह विलुप्त हो गई।
समाज पर इसका असर अलग से नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन जाति विभाजन से इसे खोखला कर दिया और दो पीढ़ी बाद यह तितर-बितर हो गया।
*जातिबिहीन समाज का जातिगत बंटवारा :*
राजुला-मालूशाही की महागाथा और लोकदेवता कलबिष्ट के जागर को ज्यादा नजदीक से समझने के लिए बेरहमी से यथार्थ के पीछे पड़ना जरूरी है। ईसा की पहली सहस्राब्दी पूरी होने के आसपास- सौ-दो सौ साल उसके पीछे और तीन-चार सौ साल आगे, मोटे तौर पर पांच सौ वर्षों में पहाड़ों के अवैदिक खस समुदाय का वैदिक-सनातनी समुदाय में रूपांतरण संपन्न हुआ। इस बदलाव के समय खसों के कुछ राजा और जहां-तहां पूरा समुदाय भी बौद्ध धर्म को मानता था।
सभी खस बौद्ध थे, ऐसे दावे का अभी कोई आधार नहीं दिखता। कहीं-कहीं उनके पाशुपत/शैव, शाक्त या नाथपंथी होने का संकेत भी मिलता है। इनमें नाथपंथियों का शैव धर्म के रास्ते सनातन में प्रवेश सबसे बाद में हुआ, इस मान्यता के भी कुछ सूत्र नेपाल के मगर समुदाय में दिखाई पड़ते हैं। खसों के धर्मांतरण का काम ज्यादातर शंकराचार्य परंपरा के तहत हुआ, लेकिन कुछ भूमिका इसमें रामानंद और मध्वाचार्य से जुड़ी भक्ति आंदोलन की धाराओं की भी हो सकती है।
इसे विचार और दर्शन की नजर से देखने पर ज्यादा महीन नतीजे निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसका असली कमाल यह रहा कि लगभग कबीले जैसे ढांचे वाले जातिहीन खस समुदाय को एक जातिग्रस्त समाज में बदल दिया गया। इससे उसकी ताकत कमजोर हुई और सामूहिक स्वाभिमान रसातल में चला गया।
यह कोई अमूर्त निष्कर्ष नहीं, एक ठोस हकीकत है, जिसे जानने के लिए हमें बड़ी खस आबादी वाले तीन सटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल की मौजूदा सामाजिक श्रेणियों का एक जायजा लेना होगा, जिसके लिए थोड़े धुंधले, फिर भी काफी ठोस आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं।
*आबादी में रेडिकल चेंजिंग :*
सबसे पहले नेपाल, जहां खस-आर्य एक स्वीकृत सामाजिक श्रेणी है। नेपाली संसद के समानुपातिक प्रतिनिधित्व में इसके लिए सबसे ज्यादा, 30.2 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखी गई हैं। सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 29.3 प्रतिशत सीटें वहां मूलनिवासी समुदायों के लए, 15.3 प्रतिशत मधेसियों के लिए, 13.8 प्रतिशत दलितों के लिए, 6.6 प्रतिशत थारुओं के लिए और 4.4 प्रतिशत मुसलमानों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं।
मूलनिवासियों में 5 प्रतिशत नेवार और 6 प्रतिशत तामाङ भी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर हिस्सा बौद्धों का है।
नेपाल की आबादी में खुद को खस-आर्य के रूप में दर्ज कराने वाले लोगों में 16.6 प्रतिशत हिस्सा खस छेत्रियों का, 12.18 प्रतिशत पर्बते ब्राह्मणों का और 1.61 प्रतिशत खस ठकुरी लोगों का है। खुद को खस बताने वाली कुछ और जातियों की गिनती दलितों और मूलनिवासियों में कर ली गई है, हालांकि जनगणना में उनका प्रतिशत साफ बताया गया है। भारत में जाति-आधारित आखिरी जनगणना अब से कोई एक सदी पहले ही कराई जा सकी थी, लिहाजा इस बारे में कोई भी आंकड़ा बिल्कुल ठोस नहीं है। फिर भी चुनावों के दौरान इस तरह के आंकड़े उछलते रहते हैं लिहाजा एक मोटा अनुमान जरूर लगाया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश में 25 प्रतिशत आबादी दलितों की, 14 प्रतिशत पिछड़ी जातियों की, 5 प्रतिशत आदिवासियों की और 5 प्रतिशत सिख, मुस्लिम, बौद्ध यानी अन्य की बताई जाती है। बाकी 51 प्रतिशत जनसंख्या क्षत्रियों और ब्राह्मणों की कही जाती है, जिसमें 38 प्रतिशत क्षत्रिय और बाकी- शायद 13 प्रतिशत ब्राह्मण हैं। उत्तराखंड के सामाजिक श्रेणीकरण का मामला बहुत समस्याग्रस्त है और यह समस्या मुख्यतः ब्राह्मणों के 25 प्रतिशत होने के दावे से आती है।.
मैदानी इलाके का दखल इस राज्य में हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है लिहाजा कुछ समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं।
ब्यौरे में जाएं तो यहां 19 प्रतिशत दलित, 18 प्रतिशत पिछड़े, 13 प्रतिशत मुसलमान और 3 प्रतिशत आदिवासी हैं। बाकी 47 प्रतिशत आबादी क्षत्रियों-ब्राह्मणों की मान ली जाए तो इसमें इन दोनों का अलग-अलग हिस्सा तय करने की बात रह जाती है, जिसके 35 अनुपाते 12 होने का अनुमान है। नेपाल जैसे एक स्वतंत्र देश और भारत के दो राज्यों की जनसंख्या की तुलना अवास्तविक न लगे, इसलिए इन तीनों इकाइयों की कुल आबादी का जिक्र कर देना भी जरूरी है।
सन 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 77 लाख, उत्तराखंड की 1 करोड़ 11 लाख और नेपाल की 3 करोड़ 5 लाख होने का अनुमान है।
तीनों ही इलाकों में अनुपस्थित, यानी रोजी-रोटी के लिए मैदानी इलाकों में गई आबादी का प्रतिशत भी कमोबेश एक सा ही है। जाहिर है, ये आंकड़े समानता का तो नहीं लेकिन एक स्तर की समतुल्यता का संकेत जरूर देते हैं।
किसी भी जनसांख्यिकीय अध्ययन में नेपाल की तुलना भारत से करना अटपटा होगा, लेकिन इन दोनों राज्यों से उसकी तुलना उतनी अटपटी नहीं मानी जाएगी। इससे एक बात बिल्कुल साफ निकलती है कि इन तीनों पहाड़ी क्षेत्रों में क्षत्रियों और ब्राह्मणों की सम्मिलित हिस्सेदारी लगभग एक तिहाई से आधे तक की है, जो भारत के मैदानी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है।
*ऐसे बदला पहाड़ का चेहरा :*
बड़े भारतीय राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में समाज की जातीय हिस्सेदारी के आंकड़े बिल्कुल धुंधले हैं लेकिन चुनावी मौकों पर यहां ऊंची जातियों का मत प्रतिशत कुल वोटों का 18 से 20 प्रतिशत बताया जाता है। इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अलावा भूमिहार/त्यागी, कायस्थ और खत्री के अलावा वैश्य समुदाय का एक हिस्सा भी शामिल माना जाता है।
मोटा अनुमान है कि ब्राह्मण-क्षत्रिय आबादी यहां 12 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। दिल्ली जैसे शहराती इलाकों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में यह उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम ही निकलेगी।
यानी एक बात तो तय है कि खस दखल वाले पहाड़ी इलाकों में क्षत्रियों और ब्राह्मणों का प्रतिशत शेष भारत के दोगुने से भी ज्यादा और कहीं-कहीं चार गुना तक है। यह तभी संभव है, जब खसों को वैदिक दायरे में लाने के लिए उनके बहुसंख्य हिस्से को क्षत्रिय-ब्राह्मण बनने की सुविधा दी गई हो। ‘राजुला मालूशाही’ के किस्से और ‘कलबिष्ट’ के जागर में इस रूपांतरण का कोई संकेत नहीं मिलता, पर इन दोनों रचनाओं में सामुदायिक खस जीवन की झांकियां मिलती हैं।
खासकर ‘कलबिष्ट’ में कुछ नए मिजाज के विधि-निषेध समाज पर लागू हो जाने की छटपटाहट मिलती है, जो सिर्फ नौलखिए दीवान सकराम पांडे की दौलत, जमीनों पर उसके अधिकार और किसी का भी इस्तेमाल कर लेने की उसकी क्षमता के रूप में जाहिर नहीं होती। बांसुरी सुनने की इच्छुक एक विवाहित स्त्री के पास बैठना एक बांके नौजवान की निर्मम हत्या की वजह बन जाता है।
उसकी धरती, उसके पेड़-पंछी, उसके इशारे पर दौड़ पड़ने वाले सैकड़ों जानवर उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। निश्चित ही यह एक अलग किस्म का जीवन था, जो वहां जारी रह गया। किसी नई खुदमुख्तार राजुला का अकेले एडवेंचर पर निकलना फिर सैकड़ों साल तक संभव नहीं हो सका।