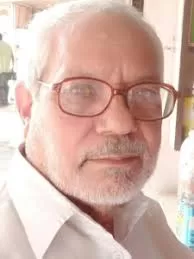
तेजपाल सिंह ‘तेज’
समकालीन परिस्थियों के दृष्टिगत पारवारिक अलगाव….
बचपन से ही सुनते आए है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। यह एक दार्शनिकता का प्रमाण भी कहा जा
सकता है और व्यैतिक सोच का मानवीय विचार बिंदु भी। आज के मेरे संस्मरण में वास्तविकता के दर्शन भी है औरअनुभवों का खुलासा भी। कोई माने न माने किंतु यह सच है कि वर्तमान समाज में शादी के कुछ की दिनों/महीनों/वर्षोंबाद पति-पत्नि के बीच परस्पर अलगाव का मसला/चलन बढ़ता ही जा रहा है। परिवार टूट भी रहे हैं। न जाने कितने हीतलाक के मामले लम्बे समय से न्यायालय के विचाराधीन हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में अलगाव तेज़ी से और रातों रातहो रहा है। बल्कि ये बहुत धीरे-धीरे हो रहा है और कई बार छोटी सी घटनाएं भी परिवार के टूटन का कारण बन जातीहैं। कहने को तो वो एक घटना होती है लेकिन उसके नतीजे दूरगामी होते हैं।
उम्र के फ़र्क़ के साथ-साथ मां और बच्चों के मूल्यों में अंतर आ जाता है। मिसाल के लिए अगर मां बहुत धार्मिक हैं और उन्होंने बच्चों को भी अपने ही संस्कार देने का प्रयास किया तो यह ज़रूरी नहीं कि बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को मानें।
आज के समय में अक्सर यहीं से टकराव की शुरूआत होती है। अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी देखा गया है कि आमतौर से अलग होने वाले माता-पिता और बच्चों के बीच अलग होने की वजह को लेकर कोई संवाद नहीं होता।
कहने में मुझे गुरेज नहीं इस प्रकार के मामले आजकल समूचे समाजों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसका मुख्य कारण
पति-पत्नी में धार्मिक और अंधविश्वासी विचारधारा में मेल न हो पाना है। इस प्रकार की असंगत सहमति पति-पत्नि केबीच अलगाव का कारण बन जाती है और ये पता ही नहीं चलता कि आख़िर वजह क्या है।
इसके अलावा भाई-बहनों के अलग मिज़ाज और माता-पिता का किसी एक बच्चे के प्रति गहरा लगाव भी
अलगाव की वजह बन जाते हैं। अलगाव के नतीजे हमेशा ही ख़राब हों ऐसा भी नहीं। बहुत से केस में इसके नतीजे बहुतसकारात्मक रहे हैं। मिसाल के लिए कई समाज में तलाक़ को बुरा माना जाता है। लेकिन एक तल्ख़ रिश्ते में रहने सेबेहतर है अलग हो जाना। हालांकि पति-पत्नी के बीच का अलगाव बच्चों के लिए मुश्किल बन जाताक़ है, बेशक पति-पत्नीसाथ-साथ ही रह रहे हों। ऐसे में पति-पत्नि के बीच स्लीप डाइवर्स के स्थिति जरूर बन जाती है। यह अक्सर जब होता है,
तब पति और पत्नि के बीच धार्मिक और सामाजिक सोच में गहरा अंतर हो। यहाँ मां-बाप का कोई मसला ही नहीं होता।ऐसा भी नहीं है कि परिवार में अलगाव स्थाई हो या पूरे परिवार से अलगाव हो। कई मर्तबा कुछ समय बाद लोगफिर से मिल जाते हैं। इस सबके बावजूद रिसर्चरों का कहना है कि जो लोग परिवार से अलग होने का फ़ैसला करते हैंअथवा स्लीप डाइवर्स जैसे रहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो ज़्यादा मज़बूत इरादों वाले और आत्मनिर्भर होते हैं। कई बारअलगाव होने के कारण साथ-साथ रहना एक सामाजिक मजबूरी भी होती है। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अलगाव केअक्सर नुक़सान ही होते हैं। ऐसे नुकसान को फायदा समझना न केवल नासमझी है, अपितु मानसिक उलझन का प्रमाणसिद्ध होता है। लगभग ऐसे ही हालात मेरे भी रहे हैं। मेरी ससुराल वालों ने तो मुझे देखने भर की जहमत नहीं उठाई थीऔर मेरे भाई ने मुझे बिना बताए ही सगुन ले लिया था। ऐसे में मैं मूकदर्शक बन कर रह गया। शेष आप सहज ही ऐसीशादी के भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं।
यथोक्त के आलोक में मेरे दिमाग में एक सवाल बार-बार उठता है कि मुझे अब भी समझ में नहीं आता कि लोगों
को शादी करना क्यों जरूरी होता है। अगर आप अपने जीवन में एक व्यक्ति चाहते हैं तो आपको शादी के बंधन में बंधनेकी क्या जरूरत है, यह सिर्फ पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती?’ तो क्या शादी करना एक गैरजरूरी गठजोड़ है? क्याआपको नहीं लगता कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और उनके लिए अकेले रहना ही काफी है। एक अच्छाइंसान जब तक रो सकता है, रोता है। लेकिन जिस दिन वो रोना बंद कर देता है, तो उसके साथ गलत करने वाले लोगरोने लगते हैं। दरअसल इंसान जिंदगी में उस दिन टूट जाता है, जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता अर्थात उसका साथदेने वाला कोई नहीं होता। यह भी सच कि जो इंसान किसी को छोड़ने की जल्दी में होता है, उसे जाने देना चाहिएक्योंकि तुम्हारे रोकने पर भी वो नहीं रुकेगा। वैचारिक वैमंस्य इसका खास कारण होता है। और उस समय जब आपअकेले हों, तो कभी भी ये सोचने से मत डरिए कि मैं अकेला हूँ। ये सोचना कि मैं अकेला हूँ, काफी है, है न? यह एकपरंपरागत मानसिकता का परिणाम होता है। अधिकतर लोग शादी की परंपरागत शर्तों को तोड़ने का साहस ही नहीं करपाते और न ही समकालीन सामाजिक/वैचारिक/धार्मिक /शैक्षणिक परस्थितियों के अनुकूल ही बदलते। समकालीनसरोकारों के दृष्टिगत और पारवारिक अलगाव की हालत से बचने के भाव से एक कहानी के जरिए अपने मन की बात कोपाठकों के सामने रखा था जिसमें मेरे अपने निजी अनुभव और सामाजिक अनुभवों को उल्लेख भर ही नहीं अपितु
समस्या के कारणों और उनकी निराकरण की बात भी की गई है। यथा -शादी का समकालीन समाज शास्त्र
शादी की कहानी कोई नई थोड़ी है। ना ही कोई नया रास्ता है। चाहे-अनचाहे सभी इस रास्ते से गुजरते हैं। कुछ
चाहकर और कुछ न चाहकर भी।…. कुछ कम उम्र में तो कुछ चढ़ी उम्र में। किंतु कमाल का सच ये है कि इस रास्ते में आईबाधाओं के किस्से चुटकलों के जरिए तो सुनने/पढ़ने को खूब मिलते हैं किंतु इस चुटकलों के सच को कोई भी पति अथवापत्नी व्यक्तिश: स्वीकार नहीं करता। क्यों…. ? लोक-लज्जा का डर, पुरूष को पुरुषत्व का डर, पत्नी को स्त्रीत्व का डर…. ।डर दोनों के दिमाग में ही बना रहता है…. इसलिए पति व पत्नी दोनों आपस में तो तमाम जिन्दगी झगड़ते रहते हैं किंतुइस सच को सार्वजनिक करने से हमेशा कतराते हैं। किंतु यह भावना कष्टकारी है। व्यापक तौर पर देखा जाए कि हमारेसमाज में किसी भी सच को कोई भी उजागर करना का मन नहीं बना पाता।
आधुनिक भारत में चाहे राजनीतिक दल वोटों के लिए, चाहे मन्दिरों के पुजारी सेविकाओं की चाहत में, चाहे
तथाकथिक सामाज सेवी संस्थाएं …. या फिर कोई भी भीड़ जुटाने के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा लगाते है तो
मुझे ये महिला सशक्तिकरण का नाटक मुझे तो बड़ा ही बचकाना लगता है….मुझे तो महिला के मुकाबले कोई और सशक्तनहीं लगता…. महिला अपनी पर उतर आए तो क्या नहीं कर सकती ?…. बेटा-बेटी के अलावा पति की क्या मज़ाल किउसके सामने कोई भी बोल पाए? यह बात अलग है कि ग्रामीण भारत की महिलाओं और पढ़ी-लिखी शहरी महिलाओं केपुरुष को बौना बनाए रखने के तरीके अलग-अलग होते हैं। हाँ। कुछ अपवाद होना तो स्वभाविक है….न सभी पुरुष एक सेहोते हैं और न सभी महिलाएं ही।
दोस्तों! एक समय था कि जब शादी के मामले में लड़के और लड़की की इसके अलावा कोई भूमिका नहीं होती थी
कि वो दोनों आँख और नाक ही नहीं अपितु साँस बन्द करके माँ-बाप अथवा दूसरे सगे-संबन्धियों की इच्छा के अनुसारशादी के लिए तैयार हो जाएं। इसके पीछे समाज का अशिक्षित होना भी माना जा सकता है। किंतु जैसे-जैसे समाज मेंशिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ तो नूतन समाज के विचार पुरातन विचारों से टकराने लगे, अब शादी के मामलेमें लड़के और लड़की की इच्छाएं भी पुरातन संस्कृति के आड़े आने लगी हैं। फलत: पिछले कुछ दशकों से यह देखने कोमिल रहा है कि शादी के परम्परागत पहलुओं के इतर शादी से पहले लड़के और लड़की को देखने का प्रचलन जोरों पर है।
पहले यह उपक्रम केवल शहरों-नगरों तक ही सीमित था किंतु आजकल तो यह उपक्रम दूरस्थ गाँवों तक पहुँच गया है।झुग्गी – झौंपड़ीयाँ तक भी इस प्रथा की ज़द में आ गई हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
यहाँ एक सवाल का उठना बड़ा ही जायज लगता है कि शादी के उद्देश्य से लड़के और लड़की की पंद्रह-बीस
मिनट की मुलाकात में लड़का लड़की और लड़की लड़के के विषय में क्या और कितना जान पाते होंगे, कहना कठिन है।सिवाय इसके कि एक दूसरा, एक दूसरे की चमड़ी भर को ही देख-भर ले। दोनों एक दूसरे की नकली हंसी को किसी नकिसी हिचकिचाहट के साथ दबे मन से स्वीकार कर लें। इस सबका कोई साक्षी तो होता नहीं है। अगर हो भी तो उनकाइस प्रक्रिया में कुछ भी कहने का कोई अधिकार यदि होता है तो वह केवल लड़के और लड़की को केवल शादी के लिएतैयार करना होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि दो अनजान चेहरों के बीच पहली
बैठक में बात शुरु करने में कुछ न कुछ तो हिचकिचाहट होती ही है। अमूनन देखा गया है कि शादी के बन्धन में बन्धने जारहे जोड़े को दूसरी मुलाकात का मौका प्राय: दिया ही नहीं जाता।
धार्मिक बाधाएं इस सबके सामने खड़ी कर दी जाती हैं। हमको इस धार्मिक उपक्रम ने इस हद तक कमजोर और
कायल बना दिया है कि हम सारा समय लड़के और लड़की की कुंडलियाँ मिलाने में गवां देते हैं। फिर ये कैसे मान लियाजाए कि शादी की पुरातन रीति आज की रीति से भिन्न है? हाँ! इतना अंतर अवश्य है कि पहले समय में लड़के और लड़कीका मिलान करने में दोनों ही पक्षों के माता-पिता की सीधी जवाबदारी होती थी और आजकज इस जवाबदारी का एकबड़ा हिस्सा लड़के और लड़की पर डाल दिया जाता है, नूतन संस्कृति और शिक्षा के प्रादुर्भाव के चलते माँ-बाप की येमजबूरी भी है। वह इसलिए कि आजकल के पढ़े-लिखे बच्चों के माता-पिता इसलिए असहाय हैं कि वो बच्चों की स्वीकृति केबिना ‘हाँ’ या ‘ना’ कहने की स्थिति में नहीं होते। दूसरे, बच्चों की शिक्षा का स्तर और कामयाबी के चलते माँ-बाप की मर्जीके कोई मायने नहीं रह गए हैं। और हों भी क्यों, लड़का और लड़की को कामयाब होने के बाद भी अपनी इच्छानुसार जीनेकी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए कि नहीं?
व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो यह कतई सच है कि प्रथम दृष्टि में, आजकल लड़के और लड़की को शादी से पूर्व
मिलने का मौका तो अवश्य दिया जाता है किंतु उसके बाद उन्हें फोन पर भी बातचीत करने का मौका न दिए जाने तककी कवायद होती है। यह बात अलग है कि आज के संचार के विविध माध्यमों और नई-नई तकनीकी संचार युक्तियों के युगमें लड़का–लड़की चोरी-छिपे फोन, वाटसेप, इंटरनेट या फिर फेसबुक के जरिए बराबर बात करते रहते हैं।….किसी कोकानों-कान खबर नहीं होती। किंतु फोन, वाटसेप, इंटरनेट या फिर फेसबुक के जरिए बात करने का वो अर्थ तो नहीं होसकता जो साक्षात बात करने में होता है। क्योंकि फोन, वाटसेप, इंटरनेट या फिर फेसबुक के जरिए बात करने में बाडी-लेंगुएज़ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता जबकि इसके उलट साक्षात मुलाकात में बाडी-लेंगुएज़ बहुत कुछ खुलासा करजाती है। किंतु हम बच्चों को शादी से पूर्व एक से ज्यादा बार मिलने का मौका ही नहीं देते। और न ही बच्चों के माता-पिताही दोबारा ऐसा कोई मौका लेने का प्रयास करते हैं। बस! घड़ी-भर का मिलना पूरे जीवन का बन्धन बना दिया जाता है।यह कहाँ तक उचित है?
सच तो ये है कि शादी जीवन का एक अकेला ऐसा सौदा है जो एक-दो दिन की मुलाकात में ही तय मान लिया
जाता है जबकि एक टी। वी। या फ्रिज जैसी दैनिक उपयोग की चीजें खरीदने की कवायद में सप्ताह, हफ्ता ही नहीं, यहाँतक की कई-कई महीने तक लग जाते हैं…. कौन सी कम्पनी का लें? इसकी क्या और कितने दिनों की गारंटी है?….
इसका लुक औरों के मुकाबले कैसा है?…. न जाने क्या-क्या….? न जाने कितने मित्रों से इसकी जानकारी हासिल कीजाती हैं…. । इतना ही नहीं, सब्जी तक दस दुकानों की खाक छानने के बाद भाव-मोल करने के बाद ही खरीदी जातीहैं।….किंतु लड़का-लड़की के बीच जीवन-भर का रिश्ता बनाने में जान-पहचान के बजाय बच्चों की शिक्षा के स्तर औरउनकी आमदनी के विषय में ही ज्यादा सोचा जाता है।…. और कुछ नहीं।
लगता है कि यही प्रक्रिया आजकल के रिश्तों में टूटन का खास कारण है।…. बच्चों की कमाई भी इसका एक
कारण हैं, एक दूसरा एक दूसरे की कमाई पर हक जताने की जिद में हमेशा उलझे रहता हैं….लड़का और लड़की के घरवाले भी इस कवायद में कम भूमिका नहीं निभाते…. लड़का और लड़के के घर वाले लड़की की कमाई को हर-हालहथियाने की कोशिश में लग रहते हैं, और लड़की अपनी कमाई को लड़के के नाम क्यूँ करदे, इसी उलझन में फंसी रहतीहै।…. पड़े भी क्यूँ न? जो लड़की अपने माँ-बाप के घर को छोड़कर लड़के के साथ उसके घर में रहने के लिए बाध्य होतीहै तो क्या वह अपनी कमाई से ससुराल वालों को पालने के लिए भी बाध्य है? यदि ऐसा होता है तो लड़की के लिए शादीके क्या माने रह जाते है?
हाँ! मान-सम्मान अता करने की बात अलग है। इस जद्दो-जहद के चलते लड़का और लड़की के बीच मतभेद हो
न हो, घर वाले दोनों के बीच में दीवार खड़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। केवल माँ-बाप ही लड़का और लड़की केबीच की दीवार नहीं बनते, अपितु अनेक बार लड़का और लड़की भी अपने बीच दीवार खड़ा करने में पीछे नहीं रहते।
इसी कश-म-कश के चलते, यह देखा गया है कि शादी हो जाने के बाद पति-पत्नि एक दूसरे को निभाने, या यूँ कहूँ किपति-पत्नि के सामने इस रिश्ते को ढोने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं रह जाता।
जहाँ तक कुंडलियों के मिलान का सवाल है, यह एक ढौंग प्राय: है इसे अन्धविश्वास की सज्ञ भी दी जा सकती है
जो सदियों से होता आ रहा है और पता नहीं भविष्य इस परिपाटी को कब तक ढोने को बाध्य होगा। यहाँ यह सवालउठता है कि क्या ये कुंडली-मिलान रिश्तों के अमरत्व की कोई गारंटी देता है। क्या कुंडली-मिलान वाले जोड़ों के बीच
कभी कोई दरार नहीं पड़ती? क्या उनका जीवन-भर मधुर साथ बना रहता है? क्या उनके जीवन में कोई प्राक्टतिक बाधानहीं आती? जैसी कि कुंडली मिलाते समय आशा की जाती है।…. । व्यापक रूप से ये भामक मानसिकता है, ऐसा करनेसे कभी भी किसी दम्पति को आशातित शांति शायद कभी नही और कतई नहीं मिलती। यह उपक्रम अपने को स्वय धोखादेने के बराबार है। मुझे लगता है कि इसके इतर यह अच्छा होगा कि लड़के और लड़की की जन्मकंडली के बदले उनकीचिकित्सीय कुंडलीयों का मिलान भी किया जाना चाहिए। मैं जामता हूँ कि मेरे इस प्रस्ताव को एक मानसिक रोगी कीविचारधारा समझ नकार ही दिया जाएगा किंतु मेरी इस बात के महत्व को खुशवंत सिंह की पुस्तक ‘दिल्ली’ में उद्धृतमहात्मा शेख सादी के इस बयान से जाना जा सकता है – “यदि औरत बिस्तर से बेमजा उठेगी तो बिना किसी वजह के हीमर्द से बार-बार झग़ड़ेगी।” किंतु ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी पुरुष अथवा औरत मानने वाली नहीं है। किंतु ऐसाहोता है। रिश्तों की खटास में यह भी एक और सबसे बड़ा कारण है। इस कारण के बाद आता है….दौलत का सवाल….
श्रंगारिक संसाधनों की उपलब्धता…. गहनों की अधिकाधिक रमक…. आदि…. आदि। पुरुषों के मामले में दहेज का
लालच…. और न जाने क्या-क्या। क्या लड़के और लड़्के के माता-पिता द्वाराइस ओर कुंडलियाँ मिलाते समय ध्यान दियाजाता है? अमूनन नहीं….पुरातन स्मय में कम से कम देहातो में कोई पिता लडक़ी के रिश्ते के लिए कोई लड़का तलाशकरने कहीं जाता था तो सुनने में आता था कि लड़की की दादा/दादी अपने बेटे ये नसिहत घर से बिदा करते थे कि देख,“लड़का बेशक गरीब घर का ही हो किंतु “पट्ठा” और बस पट्ठा हो। कभी किसी लल्लू के साथ बांध दे बेटी को…. सारी उम्रदुख झेलने के लिए। रोटी-रोजी का जुगाड़ तो बच्चे मेहनत – मजदूरी करके सब कर ही लेते हैं…. समझा कि नहीं ….अबजा और मेरी बातों को ध्यान में रखना।“ अब यह सुधी पाठकों पर निर्भर है कि दादी के इस कथन का कैसे और किस संदर्भमें अर्थ निकालते हैं।
और यदि ऐसा नहीं हो पाता यानी कि पति और पत्नी दोनों की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति चाहे किसी भी
कारण से नहीं हो पाती तो अक्सर ऐसा कारण उत्पन्न हो जाता है कि इन तमाम कारणों के चलते रिश्तों में खटास आजाने के कारण या तो विछोह हो जाता है, या फिर जीवन-भर दम्पति को एक दूसरे को हारे-मन ढोते रहने को बाध्यहोना पड़ता है। पति-पत्नि की एक-दूसरे से कमर भिड़ी रहती है। इसी कश-म-कश में जीवन तमाम हो जाता है। हाँ! येबात अलग है कि समाज का एक बड़ा वर्ग, खासकर इस व्यवस्था से पीड़ित पति/पत्नि सरेआम इस बात को स्वीकार करनेसे कतराता हैं। क्योंकि उनके सामने समाज में सिर उठाकर जीने का सवाल हमेशा बना रहता है। चेहरे पर चेहरा लगाएरहते हैं…. कोई और पहल करे तो वो भी करे। यह मौका कभी आता ही नहीं…. । क्योंकि जन-सामान्य उस सामाजिकभीरुता के कारण उस मुखौटे को उतारने का साहस कर ही नहीं पाते, जो भिरुता उन्हें विरासत में मिली है। इसी इंतजारमें अपने मन की बात को मन में दबाए रहते हैं।…. चिड़चिपन उनके सिर पर सवार हो जाता है किंतु इस सव अवस्थासे उबर ने के लिए कुछ भी कर नहीं पाते। हाँ! शहरी पढ़े-लिखे लड़के और लड़कियों की हालत ग्रामीन इलाके के लड़केऔर लड़कियों की हालत शहरी लड़के और लड़कियों की हालत से जुदा है। उसका मूल कारण शिक्षा के उतार – चढ़ाव काहै। मौटे तौर पर गाँव अभी भी भारत की पुरातन संस्क्ति और सभ्यता को ढोने से नहीं बच पाए है और शहरी आबादीपश्चिमी संस्कृति की गुलाम होती जा रही है…. । उनके लिए भारतीय सामाजिक, आर्थिक , धार्मिक, सांस्कृतिक और
राजनीतिक मूल्यों कोई अंर्थ नहीं रह गया है। आज का युवा पीढ़ी अपने जीवने को दायरों में बन्धकर नहीं, खुले आसमानमें जीना चाहती है जहाँ किसी प्रकार की परम्परातग्त बाध्यता न हो।
नवभारत टाइम्स – 06/ 02/ 2015 में छपे एक सर्वे के जरिए यह तथ्य सामने आया है कि ज्यादातर दम्पत्तियोंके बीच शादी वाला प्यार शादी होने के पहले दो सालों में ही फुर्र हो जाता है तो कुछ का तीन सालों बाद। और जिनकाबचा भी रहता है …. इनके सामने किसी न किसी प्रकार की सामाजिक मजबूरी ही होती है। ये पहले कभी होता होगाकि पति-पत्नी बुढ़ापे में एक दूसरे के मददगार बने रहते थे…. । आज समय इतना बदल गया है कि बुढ़ापा आने से पहलेही सारा खेल बिगड़ जाता है। पहला बच्चा पैदा होने के साथ ही पत्नी का प्रेम पति के प्रति इतना कम हो जाता है किपति उसके लिए उधार की चीज बन जाता है…. ऐसा उधार कि जिसे वो उतार तो नहीं सकती । बस! ढोने भर के लिएबाध्य होती है….पति की हालत भी कमोवेश यही होती है। यहाँ भी लोक-लाज ही ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए आड़ेआती है।…. इस विछोह के पीछे एक और जो कारण होता है…. वो है – लगभग 80/90 प्रतिशत पति अपनी पत्नी को हीअपनी जायज या नाजायज सम्पत्ति का मालिक बनाने का काम करते है।….कारण चाहे जो भी हों। और जब जैसे ही पत्नीको इस सच का पता चल जाता है, वैसे ही वो पति पर धीरे-धीरे सवार होती चली जाती है और पति की उपेक्षा करनाशुरू कर देती है। उसे अक्ल जब आती है, तब उसकी अपनी औलाद खासकर बेटा/बेटे अपना असली रूप दिखाने कीहालत में आ जाते हैं।…. यानी बेटों के सिर पर एक और चोटी उग आती है…. माने उनकी शादी हो जाती है। । अब घर मेंबहू का दखल भी शामिल हो जाता है।…. बेटियाँ तो अपने घर यानी ससुराल चले जाने के बाद भी अपने माँ-बाप के प्रतिकिसी न किसी प्रकार अपने अपनत्व का निर्वाह करती ही रहती हैं। बेटों के बारे में क्या कहा जाए…. । आप सब इसयर्थाथ से परिचित ही होंगें…. फिर भी पता नहीं…. । प्रत्येक दम्पत्ति के मन में बेटा पैदा करने की जिज्ञासा ज्यादा हीबनी रहती है….पता नहीं क्यों?
एक और सार्वभौम सत्य है कि 70 से 80 प्रतिशत औरतों के पति पत्नी के जीवित रहते ही मृत्यु को प्राप्त हो जातेहैं। फलत: पत्नियों को ऐसा पीड़ा भरा असहाय जीवन जीना पड़ता है जिसकी कल्पना करना भी दूभर होता है। एकउपेक्षित जीवन जीना….और वहशी आँखों की किरकिरी बने रहना विधवाओं की नियति हो जाती है। कुछ लोग कहसकते हैं कि विधवा की देखभाल के लिए क्या उसके बच्चे नहीं होते। इस सवाल का उत्तर वो जीवित विधुर और विधवाअपने गिरेबान में झाँककर खोजें कि मृत्यु के बाद उनके स्वयं के बच्चे उनका कितना ध्यान रखते हैं।
दान-दहेज की बात के इतर इस ओर कभी किसी का ध्यान शायद ही गया हो। लगता तो ये है कि इसके कारणों
को खोजने का प्रयत्न भी शायद नहीं किया गया जो अत्यंत ही शोचनीय विषय है। मुझे तो लगता है कि समाज में ये जोप्रथा है कि लड़का उम्र के लिहाज से लड़की से प्रत्येक हालत में कम से कम पाँच वर्ष बड़ा होना ही चाहिए, इस प्रकार कीसारी विपदाओं के लिए जिम्मेदार है। शायद आप भी इस मत से सहमत होंगे कि उम्र के इस अंतर को मिटाने की खासीआवश्यकता है। लड़का-लड़की की उम्र यदि बराबर भी है तो इसमें हानि क्या है? या फिर शादी के एवज पारस्परिकरिश्तों को क्यूँ न स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। विछोह तो आगे-पीछे होना तय है ही तो भला धुट-घुटकर जीवनयापन करने की बाध्यता शादी ही क्यों हो?
इस सबसे इतर, नवभारत टाइम्स दिनांक 23/05/2015 के माध्यम से अनीता मिश्रा कहती हैं कि शादी सिर्फ
आर्थिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने भारत का माध्यम नहीं है। लड़कियों को ऐसे जीवन साथी की तलाश रहतीहै जो उन्हें समझे। उनकी भावनात्मक जरूरतें भी उनके साथी के महत्तवपूर्ण हों। वो फिल्म ‘पीकू’ में एक संवाद काहवाला देती हैं….“ शादी बिना मकसद के नहीं होनी चाहिए। फिल्म की नायिका का पिता भी पारम्परिक पिताओं सेहटकर है। वह कहता है, ‘ मेरी बेटी इकनामिकली, इमोशनली और सेक्सुअली इंडिपेंडेंट है, उसे शादी करने की क्याजरूरत?’ मैं समझता हूँ कि यह तर्क अपने आप में इमोशनल जरूर है। फिर भी यह आम-जन का ध्यान तो आकर्षित करताही है।
अनीता जी आगे लिखती है कि यहाँ एक सवाल यह भी है कि विवाह संस्था को नकारने का कदम स्त्रियां ही क्यों
उठाना चाहती है। शायद इसके लिए हमारा पितृसत्तात्मक समाज दोषी है। वर्तमान ढांचे में विवाह के बाद स्त्री कीहैसियत एक शोषित और उपयोग की वस्तुस की हो जाती है। आत्मनिर्भर स्त्री के भी सारे निर्णय उसका पति या पेशंट केपरिवार वाले ही करते हैं। शादी होने के बाद (कुछ अपवादों को छोड़कर) उसका पति मालिक और निरंकुश शासक कीतरह ही व्यवहार करता है। ऐसे में स्त्री के लिए दफ्तर की जिन्दगी और घरेलू जिन्दगी में तालमेल बिठाना मुश्किल होजाता है। कहा जा सकता है कि ज्यादातर स्त्रियों को दफ्तर में काम करने के बाद भी घर में एक पारम्परिक स्त्री की तरहखुद को साबित करना होता है। किसी भी स्त्री को जब सफलता मिलती है तो यह भी जोड़ दिया जाता है कि उसने करियरके साथ सारे पारवारिक दायित्व कितनी खूबी से निभाए। जबकि पुरुषों की सफलता में सिर्फ उनकी उपलब्धियां गिनीजाती है। कामकाजी लड़कियों के लिए शादी के बाद इतनी सारी चीजों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है।नतीजतन विवाहेतर संबंधों में खटास आ जाती है…. यहाँ तक की तलाक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसीमिसालें देखकर आज कई लड़कियां शादी नहीं करने का निर्णय ले रही हैं। वे अपनी आजादी को पूरी तरह जीना चाहती हैंऔर अपने व्यक्तित्व और संपति की मालिक खुद होना चाहती हैं।
यहाँ यह सवाल उठना भी लाजिमी है कि शादी समाज की एक जरूरी व्यवस्था रही है किंतु आजादी चाहने
वाली लड़कियां शादी को एक बन्धन की तरह देखती हैं। फिर मानव समाज की दृष्टि से एक सामाजिक व्यवस्था के तौरपर विवाह का विकल्प क्या है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि बदलते परिवेश में स्त्री शादी का विकल्प खुद खोजे?जाहिर तौर पर अब तक पुरुषों की आर्थिक स्वनिर्भरता और सक्षमता ने केवल उन्हें ही निर्णय लेने का अधिकार दे रखाथा। अब अगर महिलाएं भी इसी हैसियत में पहुँचने के बाद अपनी जिन्दगी की दिशा तय करने वाला फैसला खुद लेनेलगी हैं तो इसमें गलत क्या है? फिर क्यों न आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम महिला को शादी करने, न करने का फैसलाखुद लेने दिया जाए?
उपर्युक्त के आलोक में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी के प्रश्न का हल एक लम्बी प्रक्रिया से होकर गुजरेगा।नन-फानन में कुछ भी नहीं होने वाला है। किंतु इस प्रकार की बहसों का जन्म लेना सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कोगति तो प्रदान करता ही है।
लेखक के बारे में –
वरिष्ठ कवि/लेखक/आलोचक तेजपाल सिंह तेज एक बैंकर रहे हैं। वे साहित्यिक क्षेत्र में एक प्रमुख लेखक, कवि
और ग़ज़लकार के रूप ख्याति लब्ध हैं। उनके जीवन में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिन्होंने उनको जीना सिखाया। उनकेजीवन में अनेक ऐसे यादगार पल थे, जिनको शब्द देने का उनका ये एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने एक दलित के रूप मेंसमाज में व्याप्त गैर-बराबरी और भेदभाव को भी महसूस किया और उसे अपने साहित्य में भी उकेरा है। वह अपनीप्रोफेशनल मान्यताओं और सामाजिक दायित्व के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। इस लेख में उन्होंने अपने जीवन के कुछ उनखट्टे-मीठे अनुभवों का उल्लेख किया है, जो अलग-अलग समय की अलग-अलग घटनाओं पर आधारित हैं। अब तक उनकीविविध विधाओं में लगभग तीन दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्यपुरस्कार (1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। अगस्त 2009 मेंभारतीय स्टेट बैंक से उपप्रबंधक पद से सेवा निवृत्त होकर आजकल स्वतंत्र लेखन में रत हैं।

























Add comment