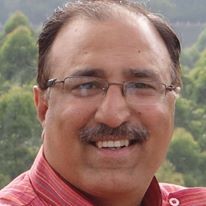[प्रस्तुत लेख, प्रो. जी. मोहन गोपाल के भाषण का लिप्यांतरित व आंशिक रूप से संपादित स्वरूप है। यह भाषण उन्होंने “न्यायिक नियुक्तियां व सुधार” विषय पर कैंपेन फॉर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) द्वारा 18 फरवरी, 2023 को आयोजित एक सेमिनार के प्रथम सत्र में दिया था। सत्र का विषय था– “न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप”। प्रो. जी. मोहन राव, नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु के पूर्व कुलपति और भारत के उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पूर्व निदेशक हैं।]
‘हस्तक्षेप’ से क्या आशय है? हस्तक्षेप से आशय है वह भूमिका निभाना, जो आपको नहीं निभानी चाहिए या वह काम करना, जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी ज़रुरत नहीं है। यह तो हुआ हस्तक्षेप का शाब्दिक अर्थ।
जब हम कहते हैं कि सरकार न्यायिक नियुक्तियों में ‘हस्तक्षेप’ कर रही है तो हमारा आशय होता है कि वह इस प्रक्रिया में ऐसी भूमिका निभा रही है जो उसे नहीं निभानी चाहिए, जो ठीक नहीं है। और जैसा कि श्री [आदित्य] सोंधी [वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट] ने कहा, यह कई तरीकों से होता है। यह केवल सरकार और कॉलेजियम के बीच औपचारिक संवाद से नहीं होता। यह कई अन्य परोक्ष और प्रत्यक्ष, व्यक्त और अव्यक्त तरीकों से होता है। जैसा कि श्री सोंधी ने कहा, हमें इस हस्तक्षेप को उसके व्यापक स्वरुप में देखना होगा। हमें बार की भूमिका और बार के राजनीतिकरण को भी समझना है, जिसके बारे में श्री सोंधी ने बात की। यह बहुत महत्वपूर्ण है और न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप के मुद्दे से गहराई से जुड़ा हुआ है।
इन सब बातों को तो हम सब स्वीकार करते हैं।
हमारे सामने अब सवाल यह है कि वर्तमान व्यवस्था में किस तरह के सुधार इस हस्तक्षेप से निपटने, इससे मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं? विशेषकर यह कि क्या कॉलेजियम प्रणाली में सुधार इस हस्तक्षेप को रोकने का सबसे बेहतर तरीका होगा? क्या इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? क्या कॉलेजियम का स्थान किसी आयोग को लेना चाहिए? क्या वर्तमान कॉलेजियम में कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में तनिक भी संदेह होगा कि मुख्य न्यायाधीश [जस्टिस यू.यू.] ललित सहित कोई भी न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप को सही ठहराएगा। जब मैं हस्तक्षेप की बात करता हूं तो मेरा अर्थ होता है कि ऐसा कुछ करना जो सरकार को नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा करना जो वांछनीय नहीं है। जब हम न्यायिक नियुक्तियों में हस्तक्षेप को रोकने की बात करते हैं तो हम कॉलेजियम या किसी वैकल्पिक संस्था की भूमिका पर भी बात करते हैं। जस्टिस ललित का कहना है कि कॉलेजियम से बेहतर कोई वैकल्पिक प्रणाली नहीं है और हमें इसे ही बनाये रखना होगा। कॉलेजियम के विकल्पों पर विचार करने के लिए अन्य सत्र निर्धारित है और मैं उसके कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल सरकार द्वारा व्यवस्था में हस्तक्षेप पर बात करना चाहूंगा और यही हमारे समक्ष असली मुद्दा है भी।
हस्तक्षेप हो रहा है, यह तो स्वीकृत बात है। जिस बात पर हमें विचार करना है वह यह है कि इस हस्तक्षेप के कारण और परिणाम क्या हैं। आखिर यह हस्तक्षेप होता क्यों है? हमारे पास बहुत सीमित समय उपलब्ध है और इसलिए मैं केवल कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा।
सबसे पहले कुछ तथ्यों की बात करता हूं। मैंने आंकड़े देखे और आंकड़े हमेशा हमें कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाईट के अनुसार, यूपीए और एनडीए के शासनकाल में – अर्थात मई 2004 से लेकर अब तक – सुप्रीम कोर्ट में 111 जजों की नियुक्ति की गई। इन 111 जजों में से 56 की नियुक्ति यूपीए के दस साल के कार्यकाल में हुई और एनडीए के शासनकाल के अब तक के 8 साल और 9 महीनों में 55 जजों की नियुक्ति हुई। दोनों आंकड़े लगभग बराबर हैं। लेकिन जब हम हस्तक्षेप के प्रभाव की बात करते हैं तो कुछ दिलचस्प तथ्य उभरकर सामने आते हैं। हम अब इन नियुक्तियों की विवेचना करेंगे जो कि निश्चित रूप से एक व्यक्तिनिष्ठ कवायद है।

हम देखना यह चाहते हैं कि क्या दस साल के यूपीए शासन और 8 साल व 9 महीने के एनडीए शासन में राजनीतिक रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त जजों की नियुक्ति की गई? हम उनके व्यक्तिगत विचारों और जज बनने के पूर्व के उनके जीवन को अपनी विवेचना का आधार नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया होगी। हम केवल उनके निर्णयों को देखेंगे क्योंकि वे हमें उनका आकलन करना का एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करते हैं। जब मैं अपने परिप्रेक्ष्य से इन्हें देखता हूं – और मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उतना समय हमारे पास नहीं है – तो मैं पाता हूं कि यूपीए के कार्यकाल में ऐसे 6 न्यायाधीश थे, जिन्हें हम मोटे तौर पर संविधानवादी न्यायाधीश कह सकते हैं – मतलब यह कि वे संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे। मैं उन्हें उदारवादी या प्रगतिशील नहीं कहूंगा – मैं उन्हें केवल संविधानवादी कहूंगा जो पूरी दृढ़ता से, पूरी गहराई से यह मानते थे कि केवल और केवल संविधान ही उनके निर्णयों की कसौटी होना चाहिए। मैं ऐसे केवल 6 न्यायाधीश ढूंढ पाया जिनके बारे में अपने दिल पर हाथ रखकर मैं यह कह सकता था कि अगर मेरे द्वारा दायर कोई प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत हो तो उस पर जो निर्णय वे सुनाएंगे – चाहे वह मेरे पक्ष में हो या मेरे खिलाफ – वह निस्संदेह केवल संविधान की उनकी समझ पर आधारित होगा और संविधान के अतिरिक्त किसी भी अन्य कानून से प्रभावित नहीं होगा। ऐसे जजों की संख्या एनडीए शासनकाल में नौ हो गई। क्यों? इसलिए नहीं कि एनडीए सरकार ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश बनाने में रूचि रखती थी, जिनकी संविधान में असंदिग्ध निष्ठा हो। वास्तविकता इसके ठीक उलट है। मुझे तो लगता है कि प्रयास यह था कि न्यायपालिका को ऐेसे लोगों से भर दिया जाए जो संविधान को उखाड़ फेंकें। लेकिन यह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि कॉलेजियम ने सरकार की कार्यवाहियों का प्रतिरोध किया। इस अवधि में, विशेषकर 2019 के पहले, सरकार ने ऐसे प्रयास किए थे, जैसे श्री सोंधी के मामले में और कई अन्य मामलों में हुआ। जस्टिस (अकील) कुरैशी के मामले में भी, जिनकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो व्यवस्था के शिकार हुए। उन्हें निश्चित रूप से अभी सुप्रीम कोर्ट में होना था. वे और ये सभी लोग व्यवस्था के शिकार हुए। जब कॉलेजियम ने देखा कि दूसरी ओर से दबाव बढ़ता जा रहा है तो उसने प्रतिरोध किया। कॉलेजियम के कुछ सदस्यों – एक संस्था के रूप में कॉलेजियम ने नहीं, क्योंकि वह तो एक नित परिवर्तित होने वाला समूह है – ने यह सुनिश्चित किया कि संविधानवादी जज पदोन्नत हों। इस प्रतिरोध से ऐसे जजों की संख्या में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी। कुल 55 या 56 जजों में से वे क्रमशः 6 और 9 ही थे। दूसरी तरफ हम यह देखें कि ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जो संविधान के बाहर जाकर सनातन धर्म, वेदों या प्राचीन भारतीय विधिक सिद्धांतों को अपने निर्णय का आधार बनाते हैं। वे धार्मिक हो सकते हैं, वेदों में उनकी गहरी आस्था हो सकती है, वे नियमित रूप से पूजा करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब वे जज के रूप में अदालत में बैठते हैं तब वे केवल संविधान को अपनी अलग-अलग व्याख्याओं का आधार बनाते हैं। सवाल यह है कि उनमें से कितने संविधान से ऊपर जाकर, उससे परे हटकर सोचेंगे और यह इसलिए नहीं कि वे सरकार के प्रभाव में हैं या सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद पाने के इच्छुक हैं – बल्कि इसलिए कि वे सचमुच वेदों आदि को संविधान से ऊपर मानते हैं। कम से कम निर्णयों के आधार पर तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ऐसे किसी भी जज की नियुक्ति यूपीए सरकार द्वारा की गई थी। एक या दो ऐसे हो सकते हैं जो संविधान के अलावा किसी अन्य चीज़ कुछ सीमा तक को विधि का स्त्रोत मानते हैं। लेकिन एनडीए के सत्ता में आने के बाद ऐसे नौ जज नियुक्त किए गए जिनमें से पांच अभी भी कार्यरत हैं – मैं उनके नाम नहीं लूंगा – जो अपने निर्णयों में यह स्पष्टतः इंगित कर चुके हैं कि उन्हें संविधान से बाहर जाना ही होगा, जैसा कि उदाहरण के लिए अयोध्या मामले में हुआ। कुछ जजों ने संविधान से बाहर जाकर अपना निर्णय सुनाया। तो इस प्रकार ऐसे जजों, जो परंपरावादी हैं या धर्म से प्रेरित हैं और जो धर्म, न कि संविधान को कानून का स्त्रोत मानते हैं, ऐसे जजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
मुझे लगता है कि यह सब सन् 2047, जब भारत अपनी स्वाधीनता की शताब्दी बनाएगा, तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की परियोजना की दो चरणों की रणनीति का पहला चरण है और यह लक्ष्य संविधान को उखाड़ फेंककर हासिल नहीं किया जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान की इस तरह से विवेचना और व्याख्या करेगा कि आपको लगेगा कि यह तो हिंदू राष्ट्र का ही संविधान है। पहले चरण में ऐेसे जज नियुक्त किए गए जो धार्मिक ग्रंथों को विधि का स्त्रोत मानते थे, लेकिन वे यह बात खुलकर नहीं कहते थे। दूसरा चरण, जो अब शुरू होने वाला है, उसमें ऐसे जज नियुक्त किए जाएंगे जो खुलकर यह स्वीकार करेंगे कि उनके निर्णय का स्त्रोत फलां-फलां धर्मग्रंथ है और वे संविधान की मनमानी व्याख्या करेंगे। इसकी शुरूआत हिजाब मामले से हो गई है, जिसमें दो जजों ने कहा कि संविधान में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द का प्रयोग किया गया है, ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द का नहीं। पंथनिरपेक्षता का संबंध पंथ से है, धर्म से नहीं। अर्थात, धर्म तो संविधान पर लागू होगा। बल्कि धर्म ही संवैधानिक विधि है। और धर्म से उनका आशय क्या है? धर्म से उनका आशय है– सनातन धर्म। जो वे कह रहे हैं, वह यह है कि सनातन धर्म ही हमारी संवैधानिक विधि है। यह पहली बार है कि इस लक्ष्मण रेखा को पार किया गया है। जज साहेबान जो कह रहे हैं, वह यह है कि कानून को लागू करते समय हमें धर्म पर विचार करना होगा। किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, जिसमें दिखाया गया है कि कर्नाटक के स्कूलों में होम करने की इजाजत है, लेकिन हिजाब पहनने की नहीं। कारण यह है कि हिजाब का संबंध पंथ से है और होम का धर्म से और धर्म पूरी पृथ्वी व पूरी मानवता की भलाई के लिए है, इसलिए स्कूलों में धर्म का पालन करने में कोई समस्या नहीं है। अब क्या कोई ऐसा पंथ है जो अपने आपको धर्म नहीं मानता?
अब हम नए दरवाजे खोल रहे हैं। हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं। हाल में एक हाईकोर्ट जज ने वैदिक स्त्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि ये स्त्रोत एक विशिष्ट कानून के प्रावधानों का आधार हैं। यह अगला कदम है। गलत साबित होने की आशंका को परे रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह चरण पूरा होते-होते, आज से 24 साल बाद, हम यह कह सकेंगे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और मजे की बात यह है कि इस हिंदू राष्ट्र के निर्माण का आधार होगा सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान संविधान की व्याख्या!
व्यक्तिगत तौर पर विधि के एक विद्यार्थी के रूप में मैं नहीं चाहूंगा कि कॉलेजियम में विधि मंत्री बैठकर यह सुनिश्चित करें कि यह एजेंडा पूरी तरह लागू हो। आज कॉलेजियम में, जैसा कि मैंने पहले बताया, संविधानवादी जजों की संख्या बढ़ी है। इनमें से कुछ कॉलेजियम के सदस्य हैं। कॉलेजियम इस बारे में भले ही कुछ बोल नहीं सकता हो, लेकिन वह उस खतरे, उस जोखिम से अनजान नहीं है, जो देश के सामने प्रस्तुत हैं। वह प्रतिरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे खतरा दिख रहा है।
दूसरी बात यह है कि हमारा संविधान और उसकी दृष्टि, हमारे देश का संचालन कर रहे कुलीन तंत्र की दृष्टि और उसके मूल्यों से एकदम अलग है। यह देश कुलीन तंत्र के हाथ में है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में सारी शक्तियां केवल चार समुदायों के हाथों में केंद्रित हैं। स्वतंत्रता के पहले, उनके खिलाफत में ब्रिटिश और मुस्लिम ताकतें थीं। लेकिन अब संविधान के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है, जो उनका मुकाबला कर सके, जिसकी शक्ति और प्रभाव उनके बराबर हो। पाकिस्तान सहित कई देशों का संविधान कुलीन तंत्र के हितों के रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए वहां कुलीन तंत्र और संविधान के बीच कोई टकराव नहीं है। पर भारत का संविधान अलग है। उसमें जानते-बूझते लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि जैसे मूल्यों का समावेश किया गया है और इसलिए वह सत्ताधारी हिंदू कुलीन तंत्र की विश्वदृष्टि को सीधे चुनौती देता है।
इस टकराव का पहला प्रकटीकरण भारत में न्यायिक स्वतंत्रता को रेखांकित करने के प्रयास के पहले चरण में हुआ। न्यायपालिका ने संविधान की मंशा के खिलाफ जाते हुए एक के बाद एक कई प्रगतिशील कानूनों को रद्द कर दिया। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 38(1) के अनुरूप थे, जो एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की बात करता था, केवल एक नई राजनैतिक या आर्थिक व्यवस्था की नहीं, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना करने की ओर प्रवृत्त हों। इस प्रक्रिया को बाधित करने पर जस्टिस कृष्णाअय्यर व मोहन कुमारमंगलम ने कड़ी प्रतिक्रिया की। हम भले ही कुमारमंगलम को संदर्भ से हटकर उद्धृत कर रहे हों, लेकिन वे जो कह रहे थे, वह यह था कि “संवैधानिक कार्यक्रम और दृष्टि को बाधित करना बंद करो”। और कृष्णाअय्यर सहित जस्टिस भगवती, जस्टिस चिनप्पा रेड्डी और जस्टिस डी.ए. देसाई, जिन्हें स्नेहवश ‘गैंग ऑफ़ फोर’ कहा जाता था – इन चारों ने संविधान और न्यायपालिका के दृष्टिकोण में तारतम्य बिठाने का काम किया। इसके बाद, 1991 में मंडल आया। मेरा मानना है कि यह संयोग नहीं है कि इसके ठीक अगले ही साल, 1992 में, कॉलेजियम सिस्टम स्थापित हो गया। यह एक तरह से मंडल की प्रतिक्रिया थी। कार्यपालिका और विधायिका में तेजी से प्रवेश कर रहे पुनरुथानशील ओबीसी से न्यायपालिका को बचाना ज़रूरी था। सरकार और कार्यपालिका का नियंत्रण यदि ऐसे सामाजिक समूह के हाथों में जा रहा था जो कुलीन तंत्र का हिस्सा नहीं था, तो उसे रोकना ज़रूरी था। तो इसलिए उस समय कॉलेजियम प्रणाली का विरोध राजनैतिक वर्ग की ओर से नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक नियुक्तियों पर श्रेष्ठ वर्ग का नियंत्रण बना रहे। अगर आप आज के सुप्रीम कोर्ट को देखें तो आप पाएंगे कि वह एक दुर्ग है, एक किला है, जिसमें सामाजिक दृष्टि से कोई विविधता नहीं है। हां, लैंगिक दृष्टि से स्थिति बेहतर है। मैंने भी सोशल मीडिया पर पांच सम्मानित और विद्वान विधिवेत्ताओं के चित्र को देखा, जो सुप्रीम कोर्ट की महिला जज भी हैं। इस चित्र के साथ यह टिप्पणी भी देखने को मिल थी– “वे कहते हैं कि ये पांच महिलाएं हैं, लेकिन मुझे तो उस चित्र में पांच ब्राह्मण दिख रहे थे।” तो इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट में विविधता का अभाव घोर चिंता का विषय है क्योंकि इसका नतीजा है प्रतिनिधित्व का अभाव। तो इस प्रकार, न्यायपालिका को एक दुर्ग, एक द्वीप बनाने की परियोजना सफल रही है और इसके कारण न्यायपालिका कमज़ोर पड़ रही है।
अब सरकार अगला कदम उठाने जा रही है। वह कह रही है, “देखिये, हम भी अब न्यायपालिका का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोहन कुमारमंगलम न्यायपालिका का उपयोग उसे संवैधानिक लक्ष्यों से जोड़ने में करना चाहते थे, उसी तरह हम न्यायपालिका का उपयोग संविधान को विसर्जित करने और भारत में धर्मराज्य स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं।” दरअसल, यह इरादा बार के मंतव्यों को प्रतिबिंबित करता है। कुलीन तंत्र न्यायपालिका नहीं, बल्कि बार को नियंत्रित करता है। आप किसी भी हाईकोर्ट को देखिये और आप पाएंगे कि दो या तीन समुदायों का बार और बेंच पर लगभग संपूर्ण वर्चस्व है। तो इसलिए, मेरा निष्कर्ष है कि इस सरकार, जिसका घोषित उद्देश्य लोकतंत्र के स्थान पर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, को न्यायिक नियुक्तियों में कोई भी भूमिका, कोई भी अधिकार देना खतरनाक होगा। वर्तमान स्थितियों में हमें कॉलेजियम को संरक्षित करना ही होगा। हम एक ऐसी सरकार, जो संविधान के मिशन में पलीता लगाने पर आमादा है, को न्यायिक नियुक्तियों में कोई भूमिका या शक्तियां नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकारें बहुत अलग थीं, लेकिन इस सरकार का एक सुस्पष्ट विचारधारात्मक एजेंडा है।
संविधान की रक्षा हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि कॉलेजियम इस बात को समझे कि उसका काम संविधान की दृष्टि और उसके मूल्यों की आक्रमण की रक्षा करना है। उसे बेंच में ऐसे लोगों को स्थान देना होगा जो संविधान को उसे कमज़ोर करने वाले हमलों से उसकी रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध हों। न्यायपालिका को मजबूती देने के लिए कॉलेजियम को उसे समावेशी बनाना होगा। धर्म, जाति, क्षेत्र, आर्थिक वर्ग – इन सभी दृष्टियों से न्यायपालिका में विविधता होनी चाहिए। न्यायपालिका एक सतरंगी इंद्रधनुष की तरह होना चाहिए, जिसे देखकर हर एक को लगे कि वह उसकी न्यायपालिका है और उसे उसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
अंत में मैं डॉ. आंबेडकर द्वारा 1930 में प्रथम गोलमेज़ सम्मलेन में प्रस्तुत ज्ञापन की चर्चा करना चाहूंगा। इस दस्तावेज में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेज के लिए आठ अत्यंत उपयोगी सुरक्षा उपायों की मांग की थी। उपाय क्रमांक चार था– विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। उपाय क्रमांक पांच था– कार्यपालिका व न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। उन्होंने आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था की नींव रखी थी। उनका प्रस्ताव था कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती का नियमन इस तरह से होना चाहिए, जिससे सभी समुदायों को पर्याप्त और उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, क्योंकि यह आवश्यक है। केवल अनुसूचित जातियां या डिप्रेस्ड क्लासेज ही नहीं, बल्कि सभी समुदायों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने गोलमेज़ सम्मलेन से कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेज केवल उत्तरदायी सरकार नहीं चाहते, बल्कि वे प्रतिनिधिक सरकार भी चाहते हैं। किसी अन्य ने प्रतिनिधिक सरकार की मांग नहीं की। प्रतिनिधिक सरकार की मांग को हमने भुला दिया और इसलिए आज देश पर कुलीन तंत्र की सरकार काबिज़ है। कॉलेजियम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान की रक्षा हो। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका में विविधता हो और वह प्रतिनिधिक बने। तभी न्यायपालिका न केवल संविधान बल्कि उसके मूल्यों की भी प्रहरी बन सकेगी। आज ऐसे कितने जज हैं जो खड़े होकर यह कह सकते हैं कि वे संविधान के संरक्षक हैं? शायद कई. आज ऐसे कितने जज हैं जो खड़े होकर यह कह सकते हैं कि वे लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के संरक्षक हैं? बहुत कम। तो हमें संविधान के कथ्य की रक्षा करना है, केवल उसके ढांचे की नहीं।
अनुवाद : अमरीश हरदेनिया,