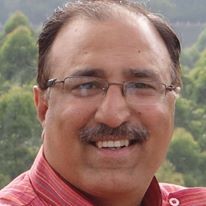प्रफुल्ल कोलख्यान
अभी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए होनेवाले चुनाव की गहमागहमी है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम ने सब को चौंका दिया है। चुनाव में राजनीतिक दलों की जीत-हार होती रहती है। कई बार परिणाम सारे अनुमान के विपरीत भी निकलते हैं। लेकिन इस बार ऐसा जरूर कुछ है कि परिणाम पर नजर रखनेवाले लोग परिणाम को संदेहास्पद मानने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं।
कांग्रेस कि शिकायत अपनी जगह बनी हुई है। इसके अलावा भी देश-विदेश में राजनीति और सुरक्षा के क्षेत्र में लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद नई तरह की हलचल शुरू हो जायेगी। इधर भारत की राजनीति में नीतिगत ही नहीं कुछ संरचनागत परिवर्तन भी आशंकित हैं। नागरिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सब पर सजग नजर बनाये रखे।
‘ऐसा होना चाहिए’ कहना शायद थोड़ा आसान होगा, लेकिन कहना जरूरी है कि ‘ऐसा है’। ऐसा है कहने पर उन लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिन्होंने ऐसी उत्पन्न की है या जो इस स्थिति को बनाये रखना चाहते हैं। यथा-स्थिति और यथा-गति बनाये रखनेवाले अपने मनमानेपन की ‘सुरक्षा परिधि’ से बाहर निकलकर किसी वैचारिक द्वंद्व में पड़ने का ‘अकारण’ जोखिम नहीं उठाना नहीं चाहते हैं।
ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं जो बताते हैं कि सभ्यता में सब से ज्यादा जोखिम तो ‘सुरक्षा परिधि’ में ही पलता है। ऐसी मनःस्थिति व्यक्ति की हो तो अधिक चिंता की बात नहीं होती है लेकिन इस मनःस्थिति के सार्वजनिक और सामाजिक बन जाने पर सभ्यता में दर्ज ‘बहु-जन-हिताय’ का मर्म पठनीय नहीं रह जाता है।
स्थाई बहुमत बनानेवाले या अपने को स्थाई बहुमत का हिस्सा होने के मनोभाव के कारण भी अधिकतर लोग ‘सुरक्षा परिधि’ में बने रहकर यथा-गति और यथा-रीति को स्वीकार लेते हैं वे यथास्थितिवाद की जड़ता में पड़े रहते हैं और परिवर्तन के हर प्रयास का अवरोधक बन जाते हैं। न तो सुविधाजनक लगनेवाली किसी स्थिति में कोई वास्तविक सुरक्षा रहती है और न हर परिवर्तन का परिणाम शुभ लेकर आता है।
यथा-स्थिति और परिवर्तन में एक तरह की रस्साकशी हमेशा चलती रहती है। परिवर्तन प्रकृति की बुनियादी प्रवृत्ति है और यथा-स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया का स्वाभाविक ठहराव। पानी और सभ्यता दोनों को उन में होनेवाले परिवर्तन की गति से पवित्रता और सार्थकता हासिल होती है। आजादी के आंदोलन के बाद भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में नई दिशा का संकेत अब साफ-साफ दिखता है।
वर्तमान की बेचैनी से निकलकर कुछ भिन्न, पीछे रह गये और आंतरिक शक्ति की तलाश जरूरी है। चुनाव में जीत-हार अपनी जगह लेकिन लोकतंत्र के चाल-चरित-चेहरा में हो रहे बदलाव से ‘मुंह चुराना’ बहुत महंगा पड़ सकता है। आजादी की प्राप्ति के बाद से ही कम-से-कम दो रास्तों का विकल्प ‘हम भारत के लोगों’ के सामने रहा है। एक अतीत की तरफ जाने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि भविष्य की तरफ जाने की कोशिश की जानी चाहिए।
उस समय भविष्य की तरफ बढ़ने के विकल्प को हमारे पुरखों ने अपनाया। आज फिर से उस समय न अपनाये दूसरे विकल्प को जिंदा कर दिया गया है। अभी की वास्तु-स्थिति यह है कि पहले अपनाये गये विकल्प की भविष्योन्मुखी दिशा पूरी तरह बदली नहीं है और अतीतोन्मुखी दिशा ठीक से पकड़ी नहीं जा सकी है। इन दोनों में घमासान जारी है। बेचैनी दोनों में भरपूर है।
दोनों ही स्थिति में बेचैनी से बाहर निकलने के लिए यथास्थिति को तोड़ना ही होगा। यहां वर्तमान के आंगन में अतीत और अन-अतीत के द्वंद्व से उत्पन्न कोलाहल और कलह परेशान करता है और यथा-स्थिति को लगभग अकाट्य बना देता है। ऐसी ही स्थिति में सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता और राजनीतिक साहस की जरूरत होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अतीत में भारत की बहुत बड़ी जन-संख्या को उत्पीड़ित करनेवाले सामाजिक अन्याय की सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना व्यवस्था का हिस्सा रही है।
आज की संवैधानिक प्रगति के बाद ऐसी किसी संरचना या ढांचा की तरफ देखना भी गुनाह है, जिस में सामाजिक अन्याय के किसी भी रूप और तत्व की थोड़ी-सी भी आशंका हो। ऐसे में अतीत की तरफ थोड़ी-बहुत ताक-झांक तो की जा सकती है लेकिन उस तरफ एक भी कदम बढ़ाना काफी खतरनाक हो सकता है। इतना खतरनाक की उधर की ओर एक कदम बढ़ाते ही वर्चस्वशालियों का आकर्षक अतीत कम-से-कम सौ कदम अपनी ओर खींच ले सकता है।
लोक-परलोक की काल्पनिक यात्रा कराते हुए लोकतंत्र के भंवर में डाल दे सकती है। अतीत में संस्कृति के बुझे हुए तारों का सांस्कृतिक ब्लैक-होल इतना शक्तिशाली है कि उस का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है। न्यायपूर्ण सामाजिक संरचना और राजनीतिक ढांचा के लिए संघर्षशील कई साथियों को उस ब्लैक-होल में समाते हुए हम ने देखा है। नमा! नाम क्या लेना!
रही भविष्य की तरफ बढ़ने की बात तो उस में भी अवमूल्यित हो चुके पुराने मूल्यों, खंडित मर्यादाओं, समाज-विरोधी सामाजिक रीति-रिवाजों और प्रचलन से बाहर हो चुकी प्रथाओं की जकड़न से भी छुटकारा मुश्किल ही होता है। कहते हैं कि मानव शरीर के कई प्रयोजनहीन अंदरूनी अंग आज भी मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं।
जाहिर है कि कुछ लोगों के मन में पुराने मूल्यों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के प्रति इतना तीव्र आग्रह और आकर्षण रहता है कि वे किसी भी तरह से उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोग यदि शक्तिशाली होते हैं तो उन के आस-पास के बाकी लोगों के लिए समाज-आर्थिक कारणों के चलते उस से छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। ऐसे लोगों की भविष्योन्मुखी गति की दृष्टि अतीतोन्मुखी ही बनी रहती है। ऐसे लोग प्रगतिशील दिखते और होते हुए भी किसी गंभीर वैचारिक द्वंद्व में ‘इधर’ रहते हुए भी ‘उधर’ ही होते हैं।
यह एक स्थिति होती है जिस में यथास्थितिवाद टूटता हुआ दिखता तो है, मगर टूट नहीं रहा होता है। जाति-वर्ण की व्यवस्था के अंतर्गत ‘हम’ और ‘अन्य’ के रूप में निरंतर चिह्नित करनेवाला भेद-भावमूलक मानसिक अलगाव खतरनाक ढंग से सक्रिय रहता है। समझ में आने लायक बात है कि जाति-व्यवस्था से क्यों और कैसे आज भी छुटकारा संभव नहीं हो पा रहा है! कुछ भी, कुछ भी कहना मुश्किल है। कुल मिलाकर यह कि समझना उतना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल कहना है। ऐसा इसलिए कि कुछ सवालों के जवाब अपने अंदर से निकलने पर ही आत्म-स्वीकृत होते हैं। दूसरों के दिये जवाब को मानने में दिक्कत होती है।
लोगों के एकत्रीकरण, एकी-करण और आत्मसातीकरण में फर्क होता है। एकत्रीकरण में लोगों को एक जगह या एक मुद्दा पर जमा किया जाता है। यह कुछ घंटों या दिनों के लिए होता है। विभिन्न ‘हित समूहों’ में समन्वय और समायोजन की प्रक्रिया से उन्हें ‘एक हित समूह’ में लाना एकी-करण है। वहीं विभिन्न सामाजिक-समूह की भिन्नताओं का ऐतिहासिक प्रक्रिया में समाप्त होकर उनकी पहचान के सारे चिह्न का एक में स्व-चालित विलयन आत्मसातीकरण (Assimilations) है। राजनीति का काम लोगों के एकत्रीकरण से चलता है।
संस्कृति का लक्ष्य लोगों के एकी-करण स प्रभावित और परिभाषित होता है। इतिहास की सकारात्मक दिशा और प्रक्रिया का लक्ष्य आत्मसातीकरण (Assimilations) के लिए पहचान के चिह्नों के स्व-चालित विलयन सामाजिक क्रांति के लिए जरूरी होता है। मार्क्सवाद का ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक वैज्ञानिक भौतिकवाद इस बात के तत्व और महत्व को न सिर्फ समझता है बल्कि उसे बरतना भी चाहता है। मुश्किल यह है कि मार्क्सवाद ढीले हाथ से संभलता नहीं है और हाथ के सधे रहने का माहौल हमेशा साथ नहीं देता है, ऐसे में कोई करे भी तो क्या करे; ‘गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त’
भारत में भिन्न-भिन्न ‘हित समूह’ अलग-अलग समय पर जत्थों में आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना किसी संघर्ष के ये सारे जत्थे दूध-मिस्री की तरह घुल-मिल जाते रहे हों। दूध-मिस्री होने में सदियां लगी हैं। हां, नये जत्थे के आगमन पर उस का मुकाबला करते हुए पहले आये जत्थों के दूध-मिस्री होने की प्रक्रिया तेज हो जाती रही होगी। आर्य, शक, हूण आदि सभी एक दूसरे को आत्मसात करते हुए पहचान के एक वृत्त में आ गये। लेकिन इस में काफी वक्त लगा। आज इन में से किसी की भी उस अर्थ में कोई भिन्न पहचान नहीं है।
अंतिम जत्थे के रूप में इस्लाम आया। इस्लाम के माननेवालों का वैसा आत्मसातीकरण (Assimilations) नहीं हो सका, तो उस के कई कारण थे। पहला तो यही कि इस्लाम के माननेवाले अपनी पहचान की पुरानी भौगोलिक और धार्मिक स्मृतियों को जीते रहे। उन के मन में श्रेष्ठ होने का भाव पहले आये जत्थों से कहीं अधिक था। अपने श्रेष्ठ होने का भाव जिस किसी में होता है, उस में सामनेवाले के हीन होने का भाव बहुत तगड़ा होता है।
इस्लाम के बाद आनेवाले ब्रिटिश अपने से पहले आये ‘जत्था’ के रूप में नहीं आये, व्यापारी के रूप में आये। पहली नजर में, ब्रिटिश लोग न तो आक्रामक के रूप में आये न सामाजिक जुड़ाव बनाने के लिए आये, वे व्यापार और मुनाफा के लिए आये। अंग्रेजों के आने पर शासक के मन में शुरू-शुरू में वैसा खौफ नहीं था। जब खौफ सताने लगा और सत्ता के हाथ से चले जाने का एहसास हुआ तब तक सामाजिक स्तर पर सहमिलानी गंगा-जमुनी संस्कृति की शुरुआत हो चुकी थी।
समाज में जारी सहमिलान की ठीक-ठीक खबर न नये पुराने शासक को थी, न नये शासक को थी। शासक को तो इस का आभास तब हुआ जब 1857 के नेतृत्व का जिम्मा का उन से आग्रह और अपील की गई। इस आग्रह और अपील में एक अबूझ पहेली थी कि हिंदू-मुसलमान के बीच एकता का यह सूत्र कब बना और अब प्रकट हुआ।
ब्रिटिश हुकूमत के हितैषियों ने 1857 के गुजर जाने के बाद इस पर काफी सोच-विचार किया और हिंदू-मुसलमान की एकता के सूत्र को तोड़ने और उलझाने की परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के आगमन के पहले के भारत को स्वर्णिम अतीत और ब्रिटिश आगमन के बाद के भारत को स्वर्णिम भविष्य की सूचना के रूप में वर्णित किया जने लगा।
चालाक ब्रिटिश हुकूमत को यह समझते देर नहीं लगी कि हिंदू-मुसलमान एकता के सूत्र गैर-सवर्ण हिंदुओं और धर्मांतरित मुसलमानों के मिलने से बनी है। कहना जरूरी है कि गैर-सवर्ण गरीब हिंदू और धर्मांतरित गरीब मुसलमानों में निज-श्रेष्ठता का भाव उतना जोरदार नहीं था, जितना तीखा भिन्न-भिन्न तरह के अपने उत्पीड़न का दर्द था। विभिन्न प्रकार के अन्याय और गरीबी के दर्द ने उन्हें एक कर दिया था। हालांकि उन के हाथ में सिर्फ उन का जीवन-अनुभव था, नेतृत्व नहीं था।
कहने का आशय यहां इतना ही है कि ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदू-मुसलमान एकता को तोड़ने, उलझाने और उस में अविश्वास का जहरीला धुआं भरने की पूरी कोशिश की। अपनी इस कोशिश में ब्रिटिश हुकूमत ने ‘श्रेष्ठ भारतीय हितैषियों’ का भी बेहिचक, लेकिन सावधान, इस्तेमाल किया। इन ‘श्रेष्ठ भारतीय हितैषियों’ में संपन्न हिंदू और मुसलमान दोनों थे। अंग्रेज काफी सावधान थे। उन की सावधानी की जड़ में ‘मंगल पांडे फेनोमिना’ काम कर रहा था, यह तो स्पष्ट ही है।
बाद में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ जाने से ब्रिटिश हुकूमत को आंदोलन के उत्ताप से बचाव का थोड़ा-बहुत आश्वासन तो जरूर मिल गया। महात्मा गांधी एक मात्र ऐसे नेता थे जिन से ‘डील’ करने का ब्रिटिश हुकूमत को लंबा अनुभव था। गांधी उन्हें ठीक से जानते थे और वे भी गांधी को ठीक से जानते थे।
दस साल की पूर्ण बहुमतवाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के शासन की प्रवृत्तियों को देखते हुए, आज की राजनीतिक परिस्थिति में भारत के लोग अपनी जड़ों को बेचैनी से टटोलने लगे हैं। यह भी सच है कि भारत देश तो बहुत पुराना है लेकिन भारत राष्ट्र तो आजादी के आंदोलन से बना है। जाहिर है कि भारत राष्ट्र को समझने के लिए आजादी के आंदोलन को समझना जरूरी है।
भारत की आजादी के आंदोलन के बारे में यह सोचना प्रासंगिक हो उठा है कि आजादी के आंदोलन के दौरान हम अपनी पुरानी के साथ एकत्र हो कर संघर्ष कर रहे थे या फिर अपनी पुरानी पहचान को भारतीय की पहचान में समाहित कर आजादी के आंदोलन में संघर्षशील थे। यह स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत की आजादी का आंदोलन में ‘हम भारत के लोगों’ का आंदोलन था, भारतीयों का नहीं।
संविधान को आत्मार्पित भी ‘हम भारत के लोगों’ ने किया था, हम ‘भारतीयों’ ने नहीं। अपनी समस्त पुरानी पहचान को विलोपित नहीं तो कम-से-कम स्थगित करते हुए ‘भारतीय’ होना था। भारत के संविधान के शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के दो प्रसंग का उल्लेख से इस बात को थोड़ा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। बाबासाहेब ने कहा था कि “हमें पहले भारतीय और अंततः भी भारतीय होना चाहिए।” ‘चाहिए’ यह भारतीय होने की आकांक्षा को व्यक्त करता है, स्थिति को नहीं।
इस आकांक्षा को पूरा करना हमारा दायित्व था और है; हम दायित्व कितना पूरा कर पाये यह एक अन्य सवाल है और उत्तर अलग से अपेक्षित है। बाबासाहेब ने यह भी कहा कि “मेरी निष्ठा अपने लोगों के प्रति भी है और इस देश के प्रति भी।” बाबासाहेब की प्रतिबद्धता बिल्कुल साफ-साफ समझी जा सकती है। बाबासाहेब की स्वतंत्रता की अवधारणा बिल्कुल साफ और सकारात्मक थी, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी बहुजन का शोषण करनेवाले के खिलाफ जारी रहेगा। आजादी के आंदोलन में ‘हम भारत के लोगों’ में ‘अपने लोग’ की ‘पहचान’ अलग भी रखते थे।
अब यह कहा जा सकता है कि आजादी के आंदोलन का संघर्ष ‘हम भारत के लोगों’ का संघर्ष था। इस संघर्ष ‘हम भारत के लोगों’ में मोटे तौर पर एक बात में सहमति थी कि भारत पर अंग्रेजों का शासन समाप्त होना चाहिए। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं चाहते थे। जो लोग आजादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से शरीक थे वे भी और जो नहीं थे वे भी अपनी-अपनी पहचान को पूरी ताकत के साथ पकड़े हुए थे।
अपनी-अपनी पहचान से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए संघर्ष की तैयारी में थे। ध्यान देने की बात यह है कि ‘हम भारत के लोगों’ की पहचान के आधार इतने विविध और बहुमुखी थे, इन में भौगोलिक क्षेत्र, धर्म, भाषा, समुदाय आदि शामिल थे कि भिन्न आधारवाले लोगों के लिए किसी की पहचान की संवेदनशीलता को समझना और महसूस करना भी बहुत मुश्किल था। ‘हम भारत के लोगों’ की पहचान की जटिलता का इशारा इतने से हो गया है, ऐसा माना जा सकता है।
आजादी की प्राप्ति के बाद विभिन्न पहचान के लोगों की अपनी-अपनी जागरूकता और चालाकियों के ‘हिसाब’ से सक्रियता भी बढ़ी। वर्चस्वशाली समुदाय अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए नये सिरे से तत्पर हो गया। लेकिन विभाजन से घायल देश की चुनौती का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऊपर से महात्मा गांधी की हत्या के चलते देश और देश के विभिन्न समुदायों की मानसिकता का अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है।
आजादी की प्राप्ति के समय भारत राष्ट्र में शामिल कर लिये गये देशी रियासतों और जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में उत्पन्न जटिलताएं अपनी जगह थी। दुनिया भर के ‘बुद्धिजीवियों’ के बीच चल रही चर्चा में यह ‘चिंता’ थी कि देखा जाये भारत और उस की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितने दिन टिकती है! दो-दो विश्व युद्ध से बाहर निकली दुनिया में ऐसी चर्चाओं का अपना महत्व था, जिस से विदेश नीति सीधे-सीधे प्रभावित हो रही थी।
दुनिया ‘शीत युद्ध’ के भंवर में फंसी थी। फिर भी भारत गुट-निरपेक्ष रहने की अधिकतम कोशिश करता हुआ आत्म-निर्णय की शक्ति अर्जित करते हुए आत्म-निर्भर हो रहा था। भारत बिल्कुल सीमित और तत्कालीन अर्थ में बेढब समाजवाद की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस बीच सोवियत संघ का विघटन हो गा। यह समकालीन दुनिया की बहुत बड़ी घटना साबित हुई। दूसरी तरफ उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) का दौर शुरू हो गया।
दुनिया एक-ध्रुवीयता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कुल मिलाकर यह कि नई विश्व व्यवस्था बन रही थी। पहचान की राजनीति कहीं भीतरी सतहों में सक्रिय थी। ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति नये सिरे से शुरू हो गई। असल में हिंदुत्व की राजनीति में भी पहचान का तत्व जरूर रहा है। हिंदुत्व में पहचान का तत्व पुराना नहीं बल्कि बिल्कुल भिन्न था, हां इस के औजार जरूर पुराने, बहुत पुराने थे। इतना कहा जा सकता है कि हिंदुत्व की राजनीति ‘हिंदुओं की जाति विभाजित पुरानी पहचान’ के ऊपर ‘हिंदुओं’ की ऐसी नई पहचान बना रही थी जिस में जाति की पीड़ा को कम करने के आश्वासन या उपाय के बिना राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू-एकत्रीकरण की ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की प्रक्रिया शुरू हुई।
हिंदू-एकत्रीकरण की इस ‘सोशल इंजीनियरिंग’ से कांग्रेस और मंडल दोनों की सत्ता-राजनीति ध्वस्त हो गई। वैश्विक परिस्थिति और घरेलू राजनीति दोनों ही वाम-पंथी राजनीति के बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। वाम-पंथी नेतृत्व अपनी समस्याओं से जूझ रहा था। जाहिर है कि विचारधारा का भ्रामक वातावरण आवरण और आच्छादन तैयार कर हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू को हिंदुत्व की राजनीतिक पहचान से जोड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई।
कहना न होगा कि हिंदुत्व की राजनीति को अर्थ-पूर्ण सफलता मिली। माहौल ऐसा बना कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक दूसरे का पर्याय बनाने और मानने-मनवाये की प्रक्रिया में सर्वस्तरीय मनोवैज्ञानिक गति-मति जुड़ने लगी। इस के साथ ही उच्च-कुल-शील की भी भूमिका में नये किस्म की तेजी दिखने लगी।
हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू-पहचान के सारे द्वंद्व को आच्छादित कर लिया। 2024 में राम मंदिर के बन जाने और दस साल के शासन के बाद हिंदू-पहचान के आच्छादन में स्वाभाविक फाट आ गई। ‘न्याय योद्धा’ राहुल गांधी की यात्राएं और विपक्ष की एकजुटता से गठित इंडिया अलायंस ने इस फाट को और अधिक चौड़ा कर दिया। नतीजा ‘चार सौ के पार’ की घोषणा के साथ चुनाव में उतरी मगरूर भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई।
महत्वपूर्ण यह है कि इस में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका सामने आई। अयोध्या यानी फैजाबाद में अद्भुत हुआ। वहां हिंदुत्व की राजनीति और भिन्न सामाजिक पहचान सीधे एक दूसरे के आमने-सामने थी और हिंदुत्व की राजनीति को लोगों ने पराजित कर दिया।
इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हरा दिया। इस अर्थ में भी यह बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में रेखांकित की जा सकती है। तो फिर, ऐसे में जातिवार जनगणना का महत्व बहुत अधिक हो जाता है।
लोकतंत्र की सार्थक शक्ति संवाद और संतुलन से निकलती है। मुश्किल तब होती है जब ‘शक्ति’ संवाद को संचालित करने लगती है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुसंख्यक का दबाव बना रहता है। इस बहुसंख्यक का गठन पहचान के विभिन्न आधारों पर बनता है। कहना न होगा कि लोकतंत्र में मतदाता संख्या का अपना महत्व होता है। जीवन के बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुमत से तय नहीं किया जा सकता है।
बहुसंख्यक यदि बहुमत की जगह दखल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निदेशित करने लगे तो इस से लोकतंत्र की गुणवत्ता क्षतिग्रस्त होती है। भारत के संदर्भ में एक और कठिनाई है। मत बनाने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया में यदि जन-हित का विवेक स्थगित या शक्ति के किसी स्वरूप से विपथित हो जाये तो इस से भी मत निर्माण का परिप्रेक्ष्य बिगड़ जाता है।
जातिवार जनगणना से सामाजिक अन्याय और आर्थिक विषमताओं को दूर या कम करने में मदद मिल सकती है। यह इस का सकारात्मक पक्ष है। लेकिन यदि इस से पहचान की राजनीति और सामाजिक संघात को बढ़ावा मिलने लगे तो यह कठिन स्थिति होगी।
ऐसे में सार्वजनिक जीवन में पहचान के सामाजिक आधार को घर परिवार में सीमित कर बाहर में संवैधानिक पहचान या अपने भारतीय पहचान को लेकर दृढ़तापूर्वक खड़ा होना होगा। यह ‘दोहरी या दोमुंही’ पहचान का नहीं ‘बहुस्तरीय पहचान’ में सार्थक और सकारात्मक संतुलन का प्रसंग है। राजनीति की यथा-गति और पहचान में संतुलन के सवाल का जवाब तो हासिल करना ही होगा। क्या यह संतुलन संभव है। हां, ऐसा बिल्कुल संभव है, संभव है भारत-विवेक!