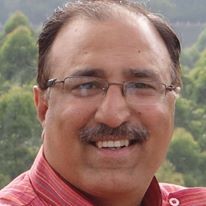(मेरे साधनाकालीन जीवन पर आधारित घटनाक्रम)
~ डॉ. विकास मानव
पूर्व कथन : _आप हवा नहीं देखते तो क्या वह नहीं है? स्वास मत लें, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी. अगर आप सत्य नहीं देख पाते तो यह आपका अंधापन है. अगर आप अपेक्षित को अर्जित नहीं कर पाते तो यह आपकी काहिलताजनित विकलांगता है._
मेरा स्पस्ट और चुनौतीपूर्ण उद्घोष है : *"बिल से बाहर निकलें, समय दें : सब देखें, सब अर्जित करें."*
आप अदृश्य को और उसकी शक्तियों को अविश्वसनीय मान बैठे हैं, क्योंकि इनके नाम पर तथाकथित/पथभ्रष्ट तांत्रिकों, कथित गुरुओं की लूट और भोगवृत्ति रही है। इन दुष्टों द्वारा अज्ञानी, निर्दोष लोगों को सैकड़ों वर्षों से आज तक छला जाता रहा है। परिणामतः प्राच्य विद्या से लोगों का विश्वास समाप्तप्राय हो गया है।
_*तंत्र ‘सत्कर्म’- ‘योग’ और ‘ध्यान ‘ की ही तरह डायनामिक रिजल्ट देने वाली प्राच्य विद्या है. इस के प्रणेता शिव हैं और प्रथम साधिका उनकी पत्नी शिवा. जो इंसान योग, ध्यान, तंत्र के नाम पऱ किसी से किसी भी रूप में कुछ भी लेता हो : वह अयोग्य और भ्रष्ट है. यही परख की कसौटी है.*_
तंत्र के नियम और सिद्धान्त अपनी जगह अटल, अकाट्य और सत्य हैं। इन पर कोई विश्वास करे, न करे लेकिन इनके यथार्थ पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जिनको साक्ष्य या निःशुल्क समाधान चाहिए वे व्हाट्सप्प 9997741245 पर संपर्क कर सकते हैं.सूक्ष्मलोक, प्रेतलोक, अदृश्य शक्तियां, मायावी शक्तियां आदि सभी होती हैं. प्रेतयोनि और देवयोनि को निगेटिव और पॉजिटिव एनर्ज़ी के रूप में विज्ञान स्वीकार कर चुका है.
योगेश्वरानंद ने कहना शुरू किया : मैंने तुमसे सात तत्व और उनसे सम्बन्धित सात शरीरों की चर्चा की थी।
जी हाँ ! मुझे स्मरण है : मैंने सिर हिलाकर उत्तर दिया।
विषय अति गम्भीर है। समझ लो मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान और अध्यात्मविज्ञान का स्वास्थ्य है यह विषय। सम्पूर्ण विश्वब्रह्माण्ड सात तत्वों के आधार पर मुख्य रूप से सात भागों में विभक्त है। सातों भागों के ऊपर *सप्तर्षि मण्डल* है और सप्तर्षि मण्डल के ऊपर *ध्रुव मण्डल* है। ध्रुव मण्डल ब्रह्माण्डीय चेतना का मूल स्रोत है। ध्रुव मण्डल के ऊपर *परम शून्य* है जो परब्रह्म परमात्मा का पर्याय है। परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक परमतत्व है। उसी का लघु संस्करण 'आत्मा' है।
_आत्मा का भी एक लघु संस्करण है और वह है--'मन'। इस विश्वब्रह्माण्ड में मन केवल मनुष्य में है और इसीलिए वह 'मनुष्य' या 'मानव' कहलाता है।_ब्रह्माण्ड के सातों भागों को सात लोक कहते हैं। प्रत्येक भाग एक लोक है और उस लोक का एक लोकांतर भी है। सप्तलोक के अधिष्ठाता सप्तर्षि हैं। सप्तर्षि और सप्तलोक ध्रुव-मण्डल के अधीन है।
यह हुई इस विषय की पृष्ठभूमि.
योगेश्वरानंद थोड़ा रुककर आगे बोले : आत्मा की स्वशक्ति को ‘चेतना’ कहते हैं। सातों लोकों में चेतना के भिन्न-भिन्न रूप हैं किन्तु प्रत्येक अवस्था में आत्मा का रूप एक ही रहता है। उसमें परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसमें आरोहण और अवरोहण अवश्य होता है।
आत्मा का आरोहण और अवरोहण
आत्मा एक ऐसा तत्व है जो विकाररहित, शाश्वत और नित्य है। उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। सभी अवस्थाओं में उसका एक ही स्वरूप रहता है। परमात्मा से नैसर्गिक रूप से प्रेरित होकर आत्मा दो प्रकार की यात्रा करती है। पहली यात्रा को अवरोहण यात्रा कहते हैं। यह आत्मा की अपने मूलबिन्दु से अधोगमन यात्रा है यानी ऊपर से नीचे की ओर यात्रा।
इस यात्रा-काल में आत्मा, ‘आत्मबुद्धि शरीर’ को धारण करती है। इसी शरीर को ‘ब्रह्माण्ड काया’ या ‘ब्रह्मशरीर’ भी कहते हैं। इस शरीर की आत्मा में बुद्धि का जागरण होता है जिसके अनुसार आत्मा अपने आपको जानती-समझती है।
पुनः वह क्रमशः नीचे को उतर कर आत्मशरीर, मनःशरीर, सूक्ष्म शरीर या प्राण शरीर, वासना शरीर या भाव शरीर (प्रेत शरीर), छाया शरीर और अन्त में स्थूल शरीर ग्रहण करती है। आत्मा की विशेषता यह है कि शुरू से वह जिस शरीर को छोड़ती है, उसके तत्व को लेकर अगले शरीर को ग्रहण करती है।
दूसरे शरीर में पहले शरीर का तत्व बीजरूप में विद्यमान रहता है जिसे ‘कोष’ की संज्ञा दी गयी है। अवरोहण यात्रा का अन्तिम पड़ाव स्थूल शरीर और स्थूल जगत है।
इस शरीर में पिछले सभी शरीरों के तत्व बीजरूप अथवा कोषरूप में विद्यमान रहते हैं जो आत्मा के आरोहण यात्रा में सहयोगी सिद्ध होते हैं।
त्रिपुटी :
सात तत्वों में प्रथम तीन तत्व आत्मतत्व, बुद्धितत्व और मनस्तत्व को त्रिपुटी कहते हैं। इन तीनों तत्वों के मिश्रण से मनुष्य के अविनाशी अंश का निर्माण हुआ है जो कभी नष्ट नहीं होता। प्रथम तीन तत्वों से सम्बंधित लोकों को दिव्यलोक कहते हैं। मनुष्य का अविनाशी अंश सदैव दिव्य लोकों में बना रहता है।
विशुद्धात्मा जब त्रिपुटी को स्वीकार करती है तो उसे दिव्यात्मा कहते हैं। किन्तु दिव्यात्मा जब ‘चतुष्क’ में प्रवेश करती है तो उसे अहं का बोध होता है और इसी अहं के बोध के फलस्वरूप उसमें जीवभाव आ जाता है। जीवभाव के उत्पन्न होने पर आत्मा को तीसरी संज्ञा प्राप्त होती है और वह संज्ञा है- जीवात्मा।
जीवात्मा को उपलब्ध होते ही आत्मा माया-जाल में फंस जाती है और भूल जाती है अपने निज स्वरूप को.
चतुष्क :
स्थूल तत्व यानी भू-तत्व, छाया तत्व, वासना तत्व और प्राण तत्व–ये चार तत्व ‘चतुष्क’ हैं। इस चतुष्क को उपलब्ध होने पर जीवात्मा मनुष्य बनने के लिए अग्रसर होती है। किन्तु इसके लिए उसे ‘मन’ की आवश्यकता पड़ती है और जब इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो वह मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठती है और जब जीवात्मा को मनुष्य शरीर उपलब्ध हो जाता है तो उसे ‘मनुष्यात्मा’ कहते हैं।
विशुद्धात्मा, दिव्यात्मा, जीवात्मा और मनुष्यात्मा–ये चार रूप हैं आत्मा के।
आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य शरीर को उपलब्ध होते ही माया के आवरण के कारण अपनी पिछली यात्रा को भूल जाती है वह। यात्रा पर निकलने से पूर्व उसका स्वरूप क्या था ? कहाँ से यात्रा शुरू की थी और अन्त में कहां पहुँची है ?–यह भी भूल जाती है वह माया के कारण। ऐसी स्थिति में शरीर को ही सब कुछ समझने लगती है वह और उसकी यह समझ और यह धारणा जीवन-मरण का कारण बन जाती है जिस कारण उसी धारणा के फलस्वरूप बार-बार जन्म लेती है और बार-बार मरती है।
फिर जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती उसे। आवागमन बराबर बना रहता है जब तक उसमें अहं भाव बना रहता है। यह अहं भाव ही जीवात्मा को माया से मुक्त नहीं होने देता। हर काल में, हर स्थिति में अहं का अस्तित्व बना रहता है। अहं की अभिव्यक्ति “मैं” के द्वारा होती है और यह “मैं” कभी नहीं मरता।
शरीर छूटने के बाद भी “मैं” का अस्तित्व रहता–इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए।
आत्मा की यात्रा का उद्देश्य :
आत्मा की अवरोहण और आरोहण यात्रा का उद्देश्य क्या है ?
मेरा प्रश्न सुनकर योगेशरानंद बोले–परमात्मा का ही एक महत्वपूर्ण अंश है आत्मा जिसे मैंने परमात्मा का लघु संस्करण कहा है। परमात्मा से आत्मा का वियोग किस कारण, किस प्रयोजन हेतु और कब हुआ ?–इन प्रश्नों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए और न तो हुए हैं अभी तक इनके समाधान, लेकिन एक बात अवश्य है और वह यह कि आत्मा सदैव व्याकुल रहती है परमात्मा में लीन होने के लिए।
जिस क्षण वह परमात्मा से अलग हुई, उसी क्षण से वह व्याकुल रहने लगी उस परम सत्ता में विलीन होने के लिए। आत्मा की यही व्यग्रता, आकुलता और आतुरता उसे नैसर्गिक रूप से अवरोहण और आरोहण यात्रा के लिए प्रेरित करती है फिर वह अपनी अन्तहीन यात्रा पर निकल पड़ती है जिसका अन्त होता है–मनुष्य शरीर की उपलब्धि में।
मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन सम्भव है और उस मिलन का आधार है–आध्यात्मिक साधना।
जब तक आध्यात्मिक साधना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक बराबर आत्मा जीवन-मरण के चक्र में घूमती रहती है।
इसी को माया कहते हैं। यह चक्र कब तक चलेगा–बतलाया नहीं जा सकता। जन्म-मरण की अनवरत यात्रा का नाम ही जीवन है जिसे ‘बहिरजीवन’ कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और जीवन है जिसे ‘अंतर्जीवन’ कहते हैं। मरण से पुनर्जन्म की यात्रा अंतर्जीवन है।
इस अंतर्जीवन में कौन-कौन-सी घटनाएं घटती हैं ? जीवात्मा किन-किन स्थियों से होकर गुजरती है ?–यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता।
परमात्मा और प्रकृति का यह गूढ और अबूझ रहस्य है। मरणोत्तर जीवन का यह रहस्य अभी तक अनावृत नहीं हो पाया है।
थोड़ा ठहर कर योगेश्वरानंद आगे कहने लगे–मानव शरीर को उपलब्ध होने पर जीवात्मा माया के कारण अपने-आपको, अपने स्वरूप को भूल जाती है, रोज मृत्यु की घटना घटती है फिर भी मनुष्य ऐसे जीता है कि जैसे उसे कभी नहीं मरना है। यह समझ में नहीं आता है उसके कि वह भी मर सकता है।
एक-न-एक दिन यह मरणधर्मा शरीर उससे भी छूट जाएगा, शरीर छूटते ही यह संसार भी छूट जाएगा। मनुष्य रोज-रोज लोगों को मरते देखता है लेकिन वह स्वयं भी कभी मरेगा–इसका ख्याल उसे क्यों नहीं आता है ?
इसका कारण है कि मर्त्य देह में जो बैठा है, वह मर्त्य नहीं है। मृत्यु की परिधि है पर केंद्र में मृत्यु नहीं है। वह जो देख रहा है, सुन रहा है, जान-समझ रहा है, वह देह, प्राण और मन का द्रष्टा है।
वह जानता है कि मैं द्रष्टा हूँ और देह, प्राण और मन से पृथक हूँ। मैं मर्त्य का द्रष्टा हूँ, मर्त्य नहीं हूँ। वह जान रहा है कि मेरी मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो मात्र देह-परिवर्तन है। मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। मृत्युओं को पार करके मैं अमरतत्त्व रूप में शेष रहता हूँ।
अमर का मतलब है जो कभी भी किसी भी स्थिति में मृत नहीं होता। लेकिन यह अमूल्य बोध उसे अचेतन मन में ही होता है, चेतन मन में नहीं। उस बोध को अचेतन से चेतन मन में लाना ही मुक्त हो जाना है। मृत्यु प्रत्यक्ष दिखती है।
अमर का बोध परोक्ष है। उसे जो भी प्रत्यक्ष बना लेता है, वह जान जाता है कि उसका न जन्म है और न तो है उसकी मृत्यु ही है। वह जीवन जो जन्म और मृत्यु के अतीत हो, उसे जान लेना और उसे प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है।
मनुष्य और भय :
मनुष्य हर अवस्था में भयभीत है–उठते-बैठते, सोते-जागते भय बना हुआ है। प्रत्येक विचार में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक व्यवहार में भय है। प्रेम में-घृणा में, पुण्य में-पाप में–सब में भय है। लगता है–मनुष्य की पूरी चेतना ही भय से निर्मित है।
मनुष्य का विश्वास, उसकी धारणाएं, उसका धर्म और ईश्वर भय के अतिरिक्त क्या है ? आखिर यह भय है क्या ?
भय के रूप अनेक हैं पर ‘भय’ एक ही है। जो यह मृत्यु है, वह मूल भय है। मिट जाने की आशंका ही समस्त भय के मूल में है। भय अर्थात मिट जाने की आशंका। इस आशंका से बचने का पूरे जीवन का प्रयास चलता है। सारे प्रयास इस मूल असुरक्षा से बचने के लिए हैं, पर पूरे जीवन की दौड़ भी होना सुनिश्चित नहीं हो पाता। दौड़ हो जाती है खत्म पर असुरक्षा वैसी-की-वैसी ही बनी रहती है।
जीवन हो जाता है पूरा और मृत्यु टल नहीं पाती है। इसके विपरीत जो जीवन दिखता था, वह पूरा होकर मृत्यु में परिणत हो जाता है। तब ज्ञात होता है कि जीवन मानो था ही नहीं, केवल मृत्यु ही विकसित हो रही थी। जन्म और मृत्यु जैसे एक ही जीवन के दो छोर थे।
यह मृत्यु का भय है क्यों ? मृत्यु तो अज्ञात है, अपरिचित है। उसका भय कैसे होगा ? जो चीज अज्ञात है, उससे सम्बन्ध भी क्या हो सकता है ?
वस्तुतः जिसे हम मृत्यु का भय कहते हैं, वह मृत्यु का न होकर जिसे हम जीवन मानते हैं, उसके खो जाने का भय है। जीवन ज्ञात है, मगर मृत्यु अज्ञात है। उसी ज्ञात के खो जाने का भय है। जो ज्ञात है, उससे हमारा तादात्म्य है।
वही हमारा होना (being) बन गया है, वही हमारा अस्तित्व बन गया है। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा सम्बन्ध, हमारा विचार, हमारा संस्कार, हमारी सम्पत्ति–यही सब मिलकर हमारे “मैं” के प्राण बन गए हैं। यही सारे मिलकर हमारा “मैं” हो गया है। मृत्यु इसी “मै” को छीनने आती है, लेकिन यह अच्छी बात है कि मृत्यु भी हमारे उस “मैं” को छीन नहीं पाती। मृत्यु की स्थिति में भी उसी ‘मैं” का बोध बराबर होता रहता है।
हम इस भय से बचने के लिए इन सब को जीवन में एकत्र करते रहते हैं। हम यह सुरक्षा पाने के लिए प्रयास करते हैं मगर होता है इसके विपरीत। इसे खो देने की आशंका जो अज्ञानता है और जो निर्मूल है, वह झूठा भय बन जाती है।
मनुष्य साधारणतया जो भी करता है, वह सब जिसके लिए किया जाता है, उसके विपरीत चला जाता है। अज्ञान में आनन्द के लिए सब कदम दुःख में ले जाते हैं। अभय के लिए चला गया मार्ग भय की ओर ले जाता है।
जो “स्व” की प्राप्ति मालूम होती है, वह “स्व” होता नहीं। बस यही सब तो माया है। यदि हम इस सत्य के प्रति जागृत हो जाएं, यदि हम यह जान सकें कि जिसे हमने “मैं” जाना है, वह मैं (आत्मा) नहीं है, वह मात्र केवल “अहं” ही ह और जब तक इस “अहं” का बोध शेष है, तब तक “मैं”( आत्मा ) की अनुभूति से हम दूर हैं।
भय का विसर्जन आवश्यक है। यह कैसे सम्भव है ?
-मैंने प्रश्न किया।
योगेश्वरानंद बोले : मृत्यु से जो परे है, वही खोता है–इस सत्य को जानने के लिए कोई क्रिया, कोई उपाय नहीं करना है। केवल उन-उन तथ्यों को जानना-समझना है और उन-उन तथ्यों के प्रति जागना है जिन्हें हम समझते हैं कि “मैं”(आत्मा) हूँ जिससे हमारा तादात्म्य है। यही जागरण “स्व” और “पर” को अलग कर देता है।
क्योंकि “स्व” और “पर” का तादाम्य ही भय है और उनका पृथक-पृथक बोध भयमुक्ति है, अभय है। हमारे दार्शनिकों ने इसी भय को ‘माया’ (अज्ञानता) की संज्ञा दी है।
अध्यात्म- साधना :
अध्यात्म-साधना से आपका क्या तात्पर्य है ?
मेरे इस प्रश्न के उत्तर में योगेश्वरानंद ने कहा- आत्मा और उससे सम्बन्धित जो परमज्ञान है, उसी का नाम ‘अध्यात्म है। ज्ञान जब तक क्रिया रूप में परिणत नहीं होता, तब तक वह व्यर्थ है–“ज्ञानं भारः क्रियाम् बिना।” अर्थात क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है।
और वह क्रिया क्या है ?
वह क्रिया है एकमात्र ‘योग’। योग के साधन से आत्मा का परमात्मा से पुनः संयोग होता है। पुनः योग होता है दोनों का। आत्मा का अस्तित्व विलीन हो जाता है परमात्मा के अस्तित्व में। इसी का नाम “मोक्ष” है, इसी का नाम परममुक्ति है और इसी का नाम है–“निर्वाण”। इसके बाद आत्मा फिर कभी परमात्मा से अलग नहीं होती।
आत्मा कई बार जन्म लेती है, बार-बार शरीर धारण करती है, इसलिए कि उसे परममोक्ष उपलब्ध हो। इसी परममोक्ष के लिए ही आत्मा जन्म और मृत्यु के कष्ट को भोगती है।
*मोक्ष की धारणा :*
योग के विषय में बतलाने से पूर्व मैं मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है ?--इस पर विचार करूँगा. योगेश्वरानंद बोले : समस्त प्राणियों में केवल मात्र मनुष्य ही विचारशील प्राणी है। मनुष्य ही आदर्श नियमों का निर्माण करता है और केवल मनुष्य ही वर्तमान के आधार पर अतीत तथा अनागत अर्थात भूत और भविष्य को एक श्रृंखला में जोड़ने का प्रयास करता है।
_आदर्श नियमों द्वारा सामूहिक सामाजिक जीवन का नियमन मानव की ही विशेषता है और इसी विशेषता का परिणाम है कि प्रत्येक काल और स्थान में मानव ने जीवन-दर्शन का प्रतिपादन किया है। मानव ने जहां एक ओर जिस जीवन-दर्शन को विकसित किया, वहीं दूसरी ओर सभी अपने सम्बन्धित पक्षों के साथ वह हिन्दुत्व के रूप में आविर्भूत हुआ।_हिंदुत्व :
वेदों के प्रणेताओं, उपनिषदों के मनीषियों, धर्मशास्त्रों के रचयिताओं, स्मृतिकारों और समय-समय पर आविर्भूत होने वाले समाज-सुधारकों ने जिस वैयक्तिक और सामाजिक जीवन-दर्शन को प्रतिपादित किया, उसी को हिंदुत्व की संज्ञा मिली।
हिंदुत्व वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के प्रति एक दृष्टिकोंण है। हिंदुओं ने सामाजिक संगठन से सम्बंधित समस्याओं पर काफी गम्भीरता से ध्यान दिया है और मानव जीवन के संगठन को जहां तक सम्भव हो सका, उत्तमतम बनाने का प्रयास किया है।
इसी प्रयास से हिन्दुत्व की आधारभूत धारणाएं और नियमित हिन्दू सामाजिक संगठन की प्रणाली की रूपरेखाएँ भी विकसित हुई हैं।
हिन्दू जीवन-यापन में मानवीय जीवन की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं के समन्वय का प्रयास किया गया है।
समन्वय के आधार :
समन्वय के दो आधार हैं–एक इहलौकिक जीवन की आवश्यकताएं और दूसरा–इस जीवन और संसार से परे जीवन की आवश्यकताएं तथा उद्देश्य। इस संसार में केवल एक मात्र हिन्दू के लिए यह संसार एक रंगमंच के अलावा और कुछ नहीं है और मानव जीवन एक साधन मात्र है, रंग-मंच पर एक किरदार मात्र है, वह साधन, वह किरदार जिससे जीवन-स्वातंत्र्य अर्थात मोक्ष की उपलब्धि होती है।
शरीरी आवश्यकताओं की पूर्ति तो जैविक गुण है और आवश्यकता भी। मानवीयता नितान्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से आगे उठा हुआ एक कदम है क्योंकि शरीर नश्वर है, अमर है तो केवल आत्मा। आत्मा को निरन्तर प्रबुद्ध करते हुये जीवन-स्वातंत्र्य की प्राप्ति का प्रयास ही मानवीयता है।
इस दृष्टिकोण की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि मानव जीवन केवल शरीरी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है। मानवीयता तो निहित है–शास्त्र प्रणीत धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने में। मानवीयता ही मांग है–मोक्ष और उसकी प्राप्ति धर्म से होती है। अतः समस्त मानव जीवन धर्म से बंधा हुआ है।
मोक्ष जीवन और संसार से विमुख होने पर प्राप्त नहीं होता। वह प्राप्त होता है जीवन को उसकी स्वाभाविक अभिरुचियों के साथ अपनाने में.
पुरुषार्थ :
पुरुषार्थ धर्म के साथ-साथ जीवन अर्थ और काम से भी बन्धा हुआ है। धर्म, अर्थ और काम का समन्वय साधन है, साध्य तो एकमात्र मोक्ष है। कर्म के माध्यम से धर्म, अर्थ और काम को साधन के रूप में अपनाने से मोक्ष रूपी परमलक्ष्य की उपलब्धि सम्भव है। इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं।
पुरुषार्थ आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य केवल पुरुष बने रहना ही नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य है–मानवी स्तर से उठकर मानवीयता की ओर अग्रसर होना जिसका तात्पर्य है–पुरुष से पुरुषोत्तम और नर से नरोत्तम होना।
*मानव शरीर और कर्म :*
सृष्टि के विशाल क्षेत्र के अन्तर्गत न जाने कितने लोक-लोकांतर हैं--यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, किन्तु यह निश्चित है कि सर्वश्रेष्ठ लोक एकमात्र 'भू-लोक' है और भू-लोक का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। इसलिये कि मानव योनि कर्मयोनि है और भोगयोनि भी।
_मनुष्य को छोड़कर इस विश्वब्रह्माण्ड में सभी योनियाँ भोग-योनियाँ हैं। कर्म करने की क्षमता और कर्मफल को भोगने की शक्ति केवल मनुष्य में है। ईश्वर के बाद कोई है तो वह है मनुष्य। मनुष्य ईश्वर के अत्यन्त निकट है--इतना निकट कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।_
यदि वास्तविकता समझी जाय तो देवता मनुष्य से नीचे है। देवयोनि पूर्णतया भोगयोनि है। देवता भोग से ऊबे हुए हैं। मानव शरीर को उपलब्ध होने के लिए वे सदैव लालायित रहते हैं, इसलिए कि भोग से अधिक 'कर्म' का महत्व है। कर्म केवल मनुष्य कर सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं।
_बेटे विकास ! सचमुच मानव शरीर अत्यन्त दुर्लभ, अत्यन्त मूल्यवान और अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ. योगेश्वरानन्द ने कहा :_
मृत्यु के समय जब मेरा शरीर मुझसे अलग होता है तो यही समझता हूँ कि कोई अपना था जिसने मेरा साथ हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दिया है। दारुण कष्ट होता है अपनी मृत काया को देखकर बन्धु !...अच्छा आज यहीं तक, कल आऊंगा तो आगे चर्चा होगी--इतना कहकर स्वामी योगेश्वरानन्द उठे और चल दिये।
*कर्म का आधार :*
मैं प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करता था। आगे के विषयों को जानने की इच्छा थी। लेकिन धीरे-धीरे एक मास का समय व्यतीत हो गया। कुछ शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए महाशय। रहा न गया, उनके निवास पर पहुंच गया। कमरे का दरवाजा भीतर से बन्द था। खटखटाया दरवाजा लेकिन नहीं खुला। सोचा--,सो रहे होंगे।
_खिड़की थोड़ी-सी खुली थी। झांक कर देखा--भीतर थोड़ा अंधेरा था। देखा--पद्मासन की मुद्रा में ध्यानस्थ थे महाशय। विघ्न डालना उचित नहीं समझा मैंने, वापस लौट आया।_
लेकिन उस समय घोर आश्चर्य हुआ जब एक परिचित व्यक्ति ने बतलाया कि स्वामीजी अभी-अभी आये थे और अपना थैला रखकर चले गए। बोले--थोड़ी देर में आता हूँ।
_सकपका कर देखा--पहचान गया--स्वामी जी का ही थैला था। हे भगवान ! यह कैसे सम्भव है ? स्वामीजी यहां कब और कैसे आये ? कुछ समय पहले तो उनको समाधि की अवस्था में देखा था मैंने बन्द कमरे में अपनी ही आंखों से। निश्चय ही यह कोई सिद्ध पुरुष हैं--इसमें सन्देह नहीं।_
अभी खड़ा-खड़ा यही सब सोच रहा था कि सामने से सीढियां चढ़कर आते हुए दिखलायी दिए महाशय। मुझे देखकर सहज भाव से मुस्कराए।
आप कब चले आये स्वामीजी ?--मेरे प्रश्न में कौतूहल और जिज्ञासा का मिला-जुला भाव था। आधा घण्टा से अधिक हो गया--स्वामीजी बोले--देखा, तुम्हारी कोठी बन्द है। ताला लगा है तो नीचे घाट की ओर चला गया मैं।
_हे भगवान ! यह कैसे सम्भव है ? आधा घण्टा पहले तो मैंने स्वामीजी को बन्द कमरे में समाधिस्थ देखा था। निश्चय ही यह कोई योग का अद्भुत चमत्कार है--इसमें सन्देह नहीं। मैं मौन रहा, बोला कुछ नहीं। लेकिन उस दिन से स्वामीजी के प्रति एक गहन आध्यात्मिक भाव ने जन्म ले लिया मेरे भीतर।_
आगे कुछ सुनने की इच्छा है ?--स्वामीजी ने कमरे में बैठते हुए हँसकर पूछा।
क्यों नहीं ? उसी की तो एक महीने से प्रतीक्षा कर रहा था।
स्वामीजी बोले--मानव जीवन कर्म प्रधान है और उस कर्म का आधार है--मन, वाक और देह। कर्म से ही मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार की गतियाँ बनती हैं। कर्म के परिणाम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कुकर्मी व्यक्ति जन्म और मृत्यु अर्थात आवागमन के चक्र में फंसा रहता है और सुकर्मी को उससे मुक्ति मिल जाती है।
_जीवन-मरण तथा आवागमन से छुटकारा पाना मानव जीवन का लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति उन धर्म-कर्मों से होती है जो वेद विहित हैं और जिनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद विहित कर्म एक ओर निवृत्ति की ओर ले जाता है और दूसरी ओर प्रवृत्ति की ओर।_
जीवन का उच्चतम ध्येय निवृत्ति है, न कि प्रवृत्ति। निवृत्ति आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। आत्मज्ञान से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो मनुष्य को इस संसार से उठाकर अभ्युदय और निःश्रेयस की ओर ले जाता है जिसमें *आत्मवत सर्वभूतेषु* की भावना रहती है।
_जीवन की उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जो रागात्मक वृत्ति (रजो वृत्ति) को नियन्त्रित रखता है।_
पुरुषार्थ क्या है ?मेरे इस प्रश्न के उत्तर में योगेश्वरानन्द बोले–पुरुषार्थ दरअसल जीवन-दर्शन का एक सिद्धान्त है। जीवन-दर्शन के एक सिद्धान्त के रूप में पुरुषार्थ से तात्पर्य है–धर्म के माध्यम से अर्थ और काम की साधना और अन्त में मोक्ष की उपलब्धि।
मानव जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है–मोक्ष जिसका एकमात्र साधन है–धर्म। इसलिए ‘धर्म’ मोक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन केवल धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है क्योंकि मोक्ष मानव जीवन की एक सतत विकास-प्रक्रिया है अर्थात अभ्युदय का चर्मोत्कर्ष है।
मोक्ष का सम्बन्ध पारलौकिक जीवन से है जो इहलौकिक जीवन का उन्नयन है। इहलौकिक जीवन का स्वाभाविक विकास अर्थ और काम से होता है–वह अर्थ और काम जो धर्म पर आधारित हो। अर्थ और काम का सम्बन्ध सांसारिक जीवन से है। धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है अतः धर्म का स्तर अर्थ और काम की अपेक्षा उच्चतर है।
पुरुषार्थ एक साधना है जिसमें धर्म के आधार पर अर्थ तथा काम की अर्थात इहलौकिक जीवन की साधना करते हुए पारलौकिक जीवन के साधने का उपक्रम है। पुरुषार्थ अभ्युदय और निःश्रेयस की साधना का माध्यम है।
इतना कहकर अखिलेश्वरानंद चुप हो गए। सायंकाल का समय हो गया था। अब तक उनके दो शिष्य आ गए थे। यौगिक क्रियाओं के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई।
भोजनोपरांत मैंने प्रश्न किया–तीसरा पुरुषार्थ ‘काम’ क्या है ?
तीसरा पुरुषार्थ काम (संभोग) :
सनातन धर्म के विचार-दर्शन में शरीर और मन की आवश्यकताओं की महत्ता को बराबर स्वीकार किया गया है जिसका प्रमाण यह है कि ‘काम’ को जीवन का एक आदर्श मान लिया गया है।
‘काम’ भी एक पुरुषार्थ के रूप में सनातन धर्म के विचार में व्याप्त मान्यता को व्यक्त करता है और काम-ऐषणाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति आवश्यक है क्योंकि उनका प्रादुर्भाव प्राकृतिक है और उनका दमन मानसिक तथा समामाजिक अव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करता है।
धर्म और अर्थ के साथ जीवन में काम के आदर्श का सामंजस्य स्वीकार करने का तात्पर्य यही है कि जीवन-दर्शन के इहलौकिक और पारलौकिक पक्षों का उचित समन्वय हो सके।
कामुकता और नारी :
सनातन धर्म के विचार-दर्शन में नर-नारी के नैसर्गिक आकर्षण को ‘काम’ का स्वरूप माना गया है। वह नैसर्गिक आकर्षण ही प्रेम है जिसकी अभिव्यक्ति तीन प्रकार से होती है।
नर-नारी के प्रेम की एक अभिव्यक्ति है ‘दाम्पत्य जीवन’ जो गृहस्थ आश्रम का आधार है। इस संदर्भ में रोमानी प्रेम एक सतत अभिलाषा नहीं है, बल्कि दाम्पत्य जीवन का पूर्व रूप है।
शकुन्तला-दुष्यन्त, मालती-माधव, नल-दमयन्ती और शिव-शक्ति की कथाएँ इसका उदाहरण हैं। इसका दूसरा राज है एक सतत आध्यात्मिक अभिलाषा जिसकी अभिव्यक्ति कृष्ण की लीलाओं, विद्यापति चण्डीदास के गीतों में हुई है।
इस प्रसंग में नर-नारी को आदि पुरुष और आदि प्रकृति का रहस्यात्मक स्वरूप समझा गया है। नर-नारी का संसर्ग शरीर तथा आत्मा के संसर्ग का खेल है।
‘काम’ इसी रहस्य की आवश्यक अभिव्यक्ति है जिसकी वृहत व्याख्या काम-शास्त्र और तन्त्र-ग्रंथों में की गई है। ‘काम’ को समाज में अधिकांशतया घृणा की दृष्टि से देखा गया है जो काम के प्रति गलत दृष्टिकोंण का परिणाम है।
अगर ऐसा न होता तो ‘काम’ को देव का स्थान न दिया गया होता। खजुराहो के मन्दिरों की दीवारों पर बने कामाभिव्यक्ति और मैथुनात्मक मूर्ति-चित्र इसी रहस्य की कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं। साहित्य में इसी रहस्य को श्रृंगारिकता की शैली में व्यक्त किया है।
यही शैली आगे चलकर नायिका-भेद तथा नख-शिख-वर्णन की साहित्यिक परम्परा में प्रस्फुटित हुई। गोपी और त्रिपुर सुन्दरी इसी रहस्यमयी अभिव्यक्ति से उत्पन्न धारणाएं हैं।
श्रृंगारिक अभिव्यक्ति का एक आधार आध्यात्मिक है और दूसरा इहलौकिक श्रृंगारिक प्रेमाभिव्यक्ति की प्रतीक है–गणिका ( नगरवधू या वेश्या).
नारी के दो रूप :
नारी के दो रूप हैं–एक पूज्या रूप और दूसरा है–भोग्या रूप। पूज्या रूप में नारी ‘माता’ है। भोग्या रूप दाम्पत्य सम्बन्ध में पत्नी का है और और तीसरा रूप है– गणिका का।
गणिका नर-नारी के नैसर्गिक आकर्षण की तीसरी अभिव्यक्ति है जिसके अभाव में समाज कें आदर्श स्वरूप में पतन होना आवश्यक है। समाज में पतन को रोकने के लिए प्राचीन काल से गणिका के अस्तित्व को न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि उसे उसके काम के लिए आदर का स्थान दिया गया।
गोपी और त्रिपुर सुन्दरी आदि यदि अध्यात्मोन्मुख प्रेमिका के धारणात्मक रूप हैं तो गणिका इहलौकिक रोमानी प्रेम की अभिव्यक्ति की प्रतीक है।
गणिका (वेश्या) की धारणा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुई है। आम्रपाली, नगरवधू, विषकन्या, देवदासी आदि इसके मुख्य रूप हैं। गणिका का इतिहास काफी लम्बा है जिसका प्रारम्भ वैदिक काल से होता है। गणिका को समाज का एक आवश्यक अंग माना जाता था और आज भी समाज में उसे महत्व दिया गया है।
भारतीय संस्कृति में व्याप्त नारी के प्रति दुविधापूर्ण विचारों को समझा जा सकता है। नारी एक ओर माता है, पत्नी है जो पुरुष की पूरक धर्मपत्नी और अर्धांगिनी है, वहीं दूसरी ओर वह गणिका भी है। प्रेमिका के रूप में एक ओर नारी प्रतीक है सतत रहस्यात्मक अभिलाषा की, पुरुष के प्रति सतत आकर्षित प्रकृति की या चैतन्य को आकृष्ट करने वाली माया-शक्ति की ओर, दूसरी ओर गणिका अथवा इहलौकिक प्रेमिका की–वह प्रेमिका जो पुरुष के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उद्दीपन का सम्बल है।
पत्नी के रूप में नारी केवल त्याग और तपस्या की मूर्ति है। पतिव्रता का आदर्श भी यही है कि मन, वचन और कर्म से पत्नी अपने को पति में लीन कर दे। पत्नी और प्रेमिका अपने-अपने स्थान पर अलग हैं और यही कारण है कि नारी पत्नी है ,एक ओर पूज्या है और दूसरी ओर प्रमदा भी है, इसीलिए नारी विश्वब्रह्माण्ड की सबसे रहस्यमयी प्राणी है जिसके स्वरूप की थाह देवता भी प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं।
स्वामी योगेश्वरानंद ने कहा–तंत्र-साधना-मार्ग एक प्रकार से नारी की उसी रहस्यमयी परिधि को मापने का प्रयास है।
ध्यान-तंत्र-शास्त्र नारी पर ही निर्भर है क्योंकि इसका का मूलाधार एकमात्र नारी ही है।
मोक्ष आपकी दृष्टि में क्या है?
मेरे इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी योगेश्वरानंद बोले :
मोक्ष के कई अर्थ हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय की धारणा में मोक्ष आवागमन से सदैव के लिए मुक्ति है। वास्तव में मोक्ष की धारणा रहस्यात्मक और आध्यात्मिक है। मोक्ष की धारणा का सम्बन्ध इस आधारभूत प्रश्न से है कि जीवन का वस्तुतः उद्देश्य क्या है और जीवात्मा का संसार और उस रहस्यत्मिका शक्ति से क्या सम्बन्ध है जिसके लिए ‘नेति’ शब्द का प्रयोग किया गया है।
सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके सामने जीवन के अंततोगत्वा उद्देश्य का यह प्रश्न सदैव विद्यमान रहता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने से भारतीय संस्कृति में उस रहस्यात्मक विचार का उदय हुआ है जिसका स्रोत वेदों में वर्णित ‘ऋत’ की धारणा है।
एक सनातनी व्यक्ति के लिए मानव से परे कोई और सत्ता है। मानव अनादि नहीं है, अनादि तो है–वह सत्ता जिससे स्वयं मानव उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल मानव ही बने रहना नहीं, क्योंकि मानव जीवन क्षणभंगुर है।
मानव शरीर, जन्म, विकास, वार्धक्य (वृद्धावस्था) तथा मृत्यु का शिकार है। मानव जीवन का स्वाभाविक उद्देश्य है उस अनादि सत्ता में मिल जाना क्योंकि जो अनादि है, वह अनन्त और असीम भी है। मनुष्यत्व से देवत्व की ओर अग्रसर होना भी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
‘मोक्ष’ इसी उद्देश्य की पूर्ति का एकमात्र और अन्तिम पड़ाव है। मोक्ष मनुष्य के जीवन के संसार में आवागमन से पूर्ण विश्राम है।
अखिलेश्वरानंद बोले–लगभग 5-6 दिन रहे योगेश्वरानंद वहां। इस अवधि में इस विषय पर आगे विस्तृत चर्चा हुई जिसे मैं फिर कभी सुनाऊंगा। इस समय रात अधिक हो गयी है।
इतना कहकर अखिलेश्वरानंद उठे और सीढियां उतर कर अस्सीघाट की ओर चले गये। मैं उन्हें जाते हुए देखता रहा। कैसा व्यक्ति है यह रहस्यमय सन्यासी ?
(लेखक मनोचिकित्सक, ध्यान प्रशिक्षक और चेतना विकास मिशन के निदेशक हैं)