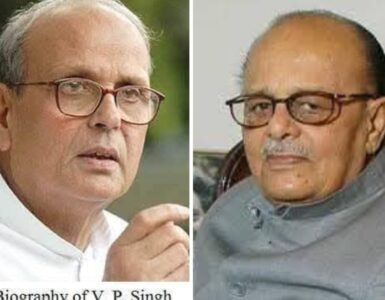दुनिया के दूरदर्शी देश अचानक आने वाले उस दिन के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। जिस तेजी से दुनिया में स्वर्ण की मांग बढ़ी है, जिस गति से विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक इसका भंडारण कर रहे हैं, यह उसी तैयारी का हिस्सा है। चीन लगातार अमेरिकी डॉलर में अपने निवेश और अपने मुद्रा भंडार में मौजूद डॉलर की मात्रा को इसीलिए घटा रहा है। वह डॉलर बेच कर लगातार सोना खरीद रहा है। यह रुझान अनेक देशों में है।वैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल के महीनों में सोने की काफी खरीदारी की है। मगर भारत में आसन्न संकट को लेकर आम तौर पर जागरूकता का अभाव है। यहां यह धारणा बनी हुई है कि पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था पुख्ता है और उससे अधिक से अधिक जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिणाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था से अधिक जुड़ती चली जा रही है। आज भी यह परिघटना सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जबकि ये वक्त सतर्क हो जाने का है। वरना, जिस रोज पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था ढही, भारत में भी लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे।
सत्येंद्र रंजन
पूंजीवाद के उदय के लगभग तुरंत बाद से ब्रिटिश पत्रिका द इकॉनमिस्ट उदारवाद (Liberalism) का मुखपत्र रही है। इसके विचार और पूंजीवाद के विकासक्रम में हमेशा एक तालमेल रहा है। जब उभर रहा बुर्जुआ वर्ग (आज के अर्थ में पूंजीपति) सामंती शिकंजे से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था, तब उनके हितों की वकालत करते हुए 1843 में इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी।
तब से ही इस पत्रिका को वैश्विक पूंजी के मुखपत्र के रूप में देखा गया है। अर्थव्यवस्था में Liberalism का अर्थ राजतंत्रीय शिकंजे से कारोबारी वर्ग को मुक्ति की मुहिम से संबंधित है। बुर्जुआ वर्ग ने उसी मुहिम के तहत सामाजिक-सांस्कृतिक उदारता की भी वकालत की। इसलिए अर्थव्यवस्था और समाज एवं संस्कृति में उदारता लाने की कोशिशें एक ही घटनाक्रम का हिस्सा रही हैं। इस तरह उदारवाद एक समग्र सोच के रूप में विकसित हुआ। कुल मिलाकर आज जब हम उदारवाद कहते हैं, तो उसका व्यवहारिक अर्थ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त व्यक्तिवादी संस्कृति से होता है।
द इकॉनमिस्ट इसी उदारवाद की पैरोकार रही है। पूंजी के बदले स्वरूप से साथ उसकी पैरोकारी का संदर्भ और मुद्दे भी बदलते रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब ये पत्रिका शांति की वकालत कर रही थी, तो बहुत से प्रगतिशील- यहां तक कि वामपंथी भी- उससे भ्रमित हुए थे। तब उन्हें आगाह करते हुए मई 1915 में व्लादीमीर इल्यिच लेनिन ने लिखा था-
‘द इकॉनमिस्ट ब्रिटिश करोड़पतियों का मुखपत्र है। यह युद्ध के मामले में एक बहुत ही स्पष्ट राय व्यक्त कर रही है। सबसे पुराने (पूंजीवादी) और धनी देश की उन्नत पूंजी के प्रतिनिधि युद्ध पर आंसू बहा रहे हैं और लगातार शांति की जरूरत बता रहे हैं। लेकिन द इकॉनमिस्ट सिर्फ इसलिए शांति की वकालत कर रही है, क्योंकि वह क्रांति की संभावना से भयभीत है।’ (Lenin: Bourgeois Philanthropists and Revolutionary Social-Democracy (marxists.org))
जाहिर है, उस दौर में ये पत्रिका सबसे धनी ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों के मुताबिक पत्रकारिता करती थी। जैसे-जैसे ब्रिटिश पूंजी वैश्विक पूंजी का रूप लेती गई, पत्रिका की राय भी उसी के अनुरूप विकसित हुई। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में निजी स्वतंत्रता और उदार उसूलों की पुरजोर वकालत करने वाली ये पत्रिका साथ-साथ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी हितों की पैरोकार बनी रही है। उन्हीं हितों के अनुरूप विश्व दृष्टि या सोच को फैलाने में इसने आधुनिक इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। (Liberalism Is as Bad as the Economist Makes It Sound (jacobin.com))
लाजिमी है कि वर्तमान में द इकॉनमिस्ट नव-उदारवाद और वॉशिंगटन कनसेंस से संबंधित नीतियों के समर्थन की एक सशक्त आवाज है। लेकिन अब ये आवाज कांपती मालूम पड़ रही है। अब इस पत्रिका ने उस रुझान को स्वीकार करते हुए एक पूरा अंक निकाला है, जिसे नजरअंदाज करने या जिसकी अहमियत कम करके बताने में हाल के वर्षों में उसकी पूरी ताकत लगी रही थी।
हालिया दशकों में अमेरिका से संचालित भूमंडलीकरण का महिमामंडन इस पत्रिका की प्राथमिकता रही है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आई एक-ध्रुवीय दुनिया अंतिम विकल्प है और सारी दुनिया को इसके अनुरूप ढल जाना चाहिए- यह इस पत्रिका का नजरिया रहा है। जब कभी या जहां कहीं से इस व्यवस्था को चुनौती मिली, उसे बदनाम करना, उसे गुमराह कोशिश बताना, या उसके महत्त्व को कम करके बताना- द इकॉनमिस्ट का प्रयास रहा है।
लेकिन अपने ताजा अंक (The new economic order | May 11th 2024 | The Economist) में पत्रिका ने स्वीकार किया है कि यह व्यवस्था अब अतीत की बात होने जा रही है। दुनिया में एक नई आर्थिक व्यवस्था का उदय हो रहा है। इन स्थितियों में दुनिया दो भागों में बंटी नजर आ सकती है। इस परिघटना के केंद्र में चीन है, जिसके उदय ने पश्चिम के अनेक सदियों से चले आ रहे वर्चस्व के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है।
पत्रिका ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया हैः लिबरल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धीरे-धीरे बिखर रही है- संभव है कि इसका अचानक अंत हो जाए। (The liberal international order is slowly coming apart (economist.com)).
इसमें कहा गया है- “पुरानी व्यवस्था में बिखराव हर जगह नजर आ रहा है।” अपने नजरिए के मुताबिक पत्रिका ने इस परिघटना को एक आसन्न आपदा के रूप में पेश किया है। कहा है कि इस क्रम में दुनिया में अराजकता और हिंसा का दौर आ सकता है। इस संभावना से पत्रिका इतनी भयाक्रांत है कि उसने टिप्पणी की है- चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, व्लादीमीर पुतिन, और अन्य सनकी लोगों की सोच जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम बनाने की हो, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वे लोग उदार व्यवस्था को सिर्फ हवाई आदर्श ही नहीं मानते, बल्कि इसे अमेरिकी सत्ता का मूर्त रूप भी मानते हैं- ऐसी सत्ता, जो अब अपेक्षाकृत क्षय की अवस्था में है।
सार यह है कि नव-उदारवादी व्यवस्था ढह रही है, इस हकीकत से आंख चुराने की स्थिति में अब वैश्विक पूंजी के पैरोकार नहीं हैं। इसलिए वे भयाक्रांत हैं- उस नई व्यवस्था के उदय की संभावना से, जिसके संचालन की डोर “सनकी” नेतृत्व वाले देशों के हाथ में हो सकती है। पत्रिका ने कहा है- अमेरिका में मजबूत आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए ऐसा महसूस हो सकता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था अपना अस्तित्व बचा लेगी- लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाएगा।
ये स्थिति क्यों आई, इसका विश्लेषण पेश करने के लिए पत्रिका ने एक लंबी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट छपी है और फिर छह शीर्षकों के साथ विशेष कवरेज किया है। विशेष रिपोर्ट ‘विश्व व्यवस्था दरक रही है- भूमंडलीकरण के अंत के बाद लोग इसकी कमी महसूस करेंगे’ शीर्षक से छपी है। इसमें भूमंडलीकरण की पृष्ठभूमि, तीन दशक तक के इसके अनुभव, और अब इस परिघटना के पलटने का जायजा लिया गया है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्यों पलटी? द इकॉनमिस्ट के मुताबिक इसके प्रमुख कारण हैः
- विश्व व्यापार संगठन का निष्क्रिय हो जाना, जिसके लिए अमेरिका प्रमुख रूप से जिम्मेदार है
- अपने रणनीतिक हितों की प्राप्ति के लिए प्रतिबंधों का सहारा लेना (इसकी जिम्मेदारी तो पूरी तरह अमेरिका पर ही है)
- घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक नीति लागू करना और उसके तहत बड़ी रकम सब्सिडी के तौर पर देना।
पश्चिमी देशों का आरोप है कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बावजूद चीन ने अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप नहीं बदला। उसने अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख भूमिका बनाए रखी। जिसका परिणाम उसके अभूतपूर्व उदय के रूप में हुआ। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पश्चिमी देश उत्पादन और व्यापार में उसका मुकाबला करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं।
- इस बीच चीन दुनिया में एक प्रमुख कर्जदाता देश बन कर उभरा है। इससे विभिन्न देशों की नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पकड़ ढीली पड़ गई है। चूंकि ग्लोबल साउथ के देशों को अब एक विकल्प मिल गया है, इसलिए उन्हें पश्चिमी पूंजी के हितों के मुताबिक चलने के लिए मजबूर करना पहले जैसा आसान नहीं रह गया है। नतीजा है, दुनिया का दो खेमों में बंटना।
- इस बीच अमेरिका की अंदरूनी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। आज अमेरिका सरकार पर कर्ज का बोझ रिकॉर्ड सीमा (35 ट्रिलियन डॉलर) तक पहुंच चुका है। उधर देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी कर्ज के बोझ से दबती चली जा रही है। इन सबसे अमेरिकी राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ा है। नतीजतन, वहां की व्यवस्था पहले जैसी कुशल नहीं रह गई है। इसका प्रभाव विश्व व्यवस्था पर भी पड़ा है।
इन परिघटनाओं से जो सूरत उभरी है, उसका विवरण द इकॉनमिस्ट ने अपने विस्तृत कवरेज में दिया है। ये रिपोर्ताज छह शीर्षकों के तहत छपी है, और ये शीर्षक कवरेज का सार बता देते हैं-
- वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के खंड-खंड हो जाने का खतरा है
- संकटों ने कैसे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को नया रूप दे दिया है
- दुनिया में पूंजी के आने-जाने की दर गिर रही है
- राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों का विस्तार हो रहा है
- डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने के संघर्ष आगे बढ़ा है
- वित्तीय व्यवस्था पर क्या होगा महाशक्तियों के बीच युद्ध का असर?
ये सारी प्रक्रियाएं वैसे तो 2007-08 की वैश्विक मंदी के बाद ही उभरने लगी थीं, लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध और रूस पर अनगिनत प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से इनमें खासी तेजी आ गई। अब उनका असर इतना फैल चुका है कि द इकॉनमिस्ट जैसी पत्रिका को भी इस सच को स्वीकार करना पड़ा है। लेकिन बात सिर्फ इस पत्रिका तक सीमित नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बढ़ते संकट पर हाल ही में वैश्विक पूंजी के एक अन्य मुखपत्र- ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने संपादकीय लिखा। (The long shadows of America’s growing debt (ft.com)). इसमें कर्ज लेकर अपना खर्च चलाने की अमेरिका में बढ़ती जा रही प्रवृति पर गंभीर चेतावनी दी गई है।
संपादकीय में कहा गया है- ….अपनी वैश्विक हैसियत के कारण अमेरिकी राजनेताओं में एक खतरनाक लापरवाही घर कर जाने की आशंका है। राजनीतिक एवं आर्थिक अनिश्चय के बीच कर्ज को नियंत्रित रखने के लिए टैक्स बढ़ाने और खर्च घटाने संबंधी कठिन निर्णयों को टाला जा रहा है। इस कारण अर्थव्यवस्था जोखिम भरे रास्ते पर चली गई है।
जोखिम वही है, जो इकॉनमिस्ट ने कहा है- अमेरिका केंद्रित वित्तीय व्यवस्था अचानक ढह सकती है। दरअसल, पत्रिका ने दिवंगत अमेरिकी साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एक कथन को अपना उप-शीर्षक बनाया है। हेमिंग्वे ने गरीबी के संदर्भ में कहा था कि गरीबी व्यक्ति धीरे-धीरे ग्रसती है, लेकिन एक मुकाम आने के बाद वह अचानक उस व्यक्ति को खा जाती है। तो कुछ वैसा ही कुछ वर्तमान वित्तीय व्यवस्था के साथ हो सकता है। धीरे-धीरे इसकी जड़ें कमजोर होती गई हैं- अब किसी दिन यह अचानक ढह सकती है।
दरअसल, दुनिया के दूरदर्शी देश अचानक आने वाले उस दिन के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। जिस तेजी से दुनिया में स्वर्ण की मांग बढ़ी है, जिस गति से विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक इसका भंडारण कर रहे हैं, यह उसी तैयारी का हिस्सा है। चीन लगातार अमेरिकी डॉलर में अपने निवेश और अपने मुद्रा भंडार में मौजूद डॉलर की मात्रा को इसीलिए घटा रहा है। वह डॉलर बेच कर लगातार सोना खरीद रहा है। यह रुझान अनेक देशों में है।
वैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल के महीनों में सोने की काफी खरीदारी की है। मगर भारत में आसन्न संकट को लेकर आम तौर पर जागरूकता का अभाव है। यहां यह धारणा बनी हुई है कि पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था पुख्ता है और उससे अधिक से अधिक जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परिणाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था से अधिक जुड़ती चली जा रही है। आज भी यह परिघटना सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जबकि ये वक्त सतर्क हो जाने का है। वरना, जिस रोज पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था ढही, भारत में भी लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे।