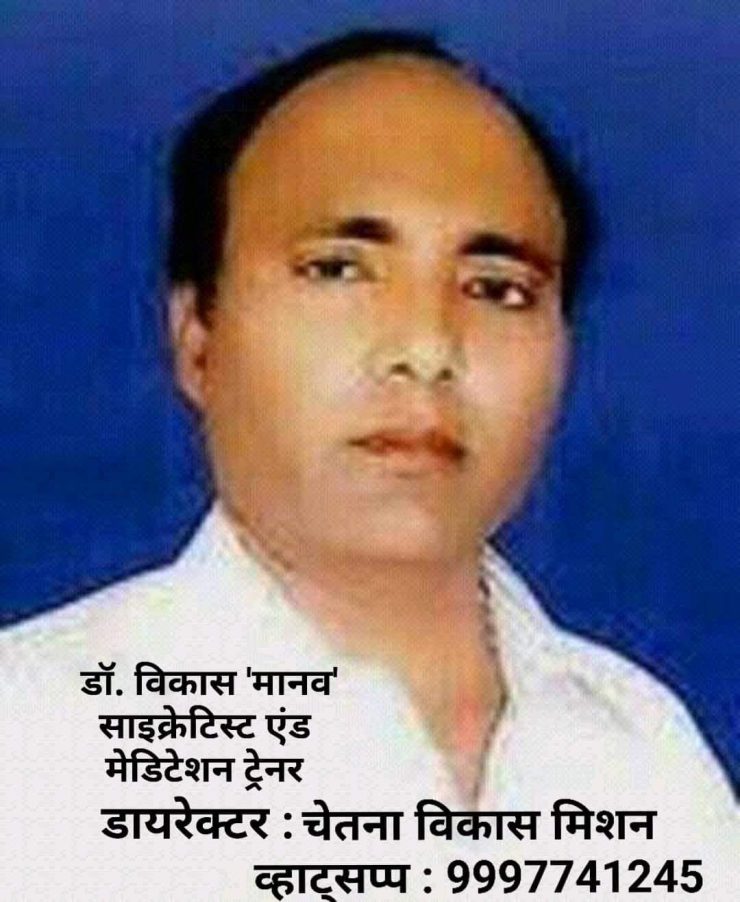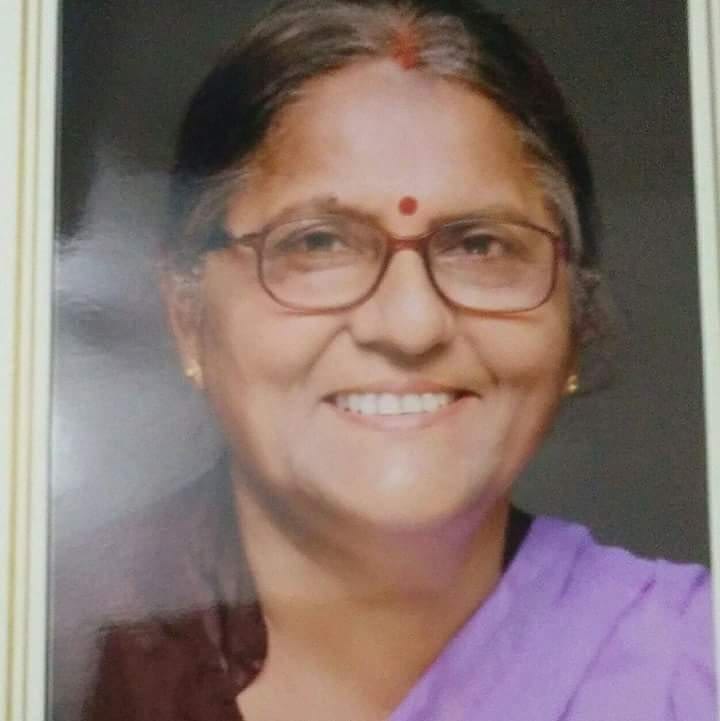डॉ. विकास मानव
_भारतीय अध्यात्म के मुख्य विषय हैं–योग और तन्त्र। इस विश्वब्रह्माण्ड में दो सत्ताएं हैं–आत्मपरक सत्ता और वस्तुपरक सत्ता। पहली सत्ता आन्तरिक है और दूसरी सत्ता है–बाह्य।_
आत्मपरक सत्ता का सम्बन्ध अन्तर्जगत से है जिसका विषय है #आत्मा। इसी प्रकार वस्तुपरक सत्ता का सम्बन्ध है बाह्यजगत से यानी भौतिक सत्ता से जिसका विषय है मन।
आत्मा और मन। दो सत्ताओं की तरह इस विश्वब्रह्माण्ड में एक मूलतत्व भी है जिसे आध्यात्मिक भाषा में #परमतत्व कहते हैं। उस परमतत्व के दो रूप हैं–आत्मा और मन। लेकिन दोनों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। आत्मा स्थिर है।
स्थिरता, द्रष्टाभाव और साक्षीभाव आत्मा का स्वभाव है और मन अस्थिर है। अस्थिरता, चंचलता मन का स्वभाव है।
योग-तन्त्र के अनुसार अनुभूति आत्मा में होती है। भाव आत्मा में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार विचार, इच्छा, कामना, अभिलाषा आदि मन में उत्पन्न होती है। इनका अनुभव मन में होता है। इन सभी का नाता-रिश्ता बाह्य जगत यानी भौतिक जगत से है।
*अनुभूति और अनुभव में अन्तर :*
साधारण जन अनुभूति और अनुभव में अन्तर नहीं जानता-समझता। वह अनुभूति की जगह अनुभव कह जाता है और अनुभव की जगह अनुभूति। जो इन्द्रियों और मन के माध्यम से हम जानते-समझते हैं, वह अनुभव है। साधारण मनुष्य फूल देखता है।
फूल सुन्दर और सुगन्धित है। फूल को देखकर मनुष्य को जो एहसास हुआ वह अनुभव है। इस अनुभव में मनुष्य को चक्षु इन्द्रिय और कर्ण इन्द्रिय की सहायता लेनी पड़ती है और फूल की सुंदरता और सुगन्ध की भावना वह मन में स्मृति रूप में संजो लेता है।
अनुभूति में ऐसा नहीं होता। अनुभूति में मनुष्य न तो इन्द्रियों की सहायता लेता है और मन की ही। मनुष्य जब इन्द्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इन्द्रीयों और मन का अतिक्रमण कर जाता है। वह मन के परे चला जाता है। अब मनुष्य द्रष्टाभाव से अपनी आत्मा के माध्यम से (बिना इन्द्रियों और बिना मन की सहायता से) जगत को देखता है तो उस समय मनुष्य को जो दिखायी देता है, वह जगत का चिन्मय रूप होता है।
चिन्मय रूप संसार का शुद्ध, निर्मल और अपरिवर्तनीय रूप होता है। जैसे आज गंगा बहुत प्रदूषित दृष्टिगोचर होती है, लेकिन यही गंगा चिन्मय रूप में अपने स्वच्छ, निर्मल रूप में आत्मा के माध्यम से दिखाई देगी आत्मा की इसी अवस्था को साक्षीभाव या द्रष्टाभाव कहते हैं। लेकिन बड़े कष्ट की बात है कि आज के तथाकथित युवा साधक बात- बात में “साक्षीभाव से’ या “द्रष्टाभाव से” कहते देर नहीं लगाते।
उन्हें साक्षीभाव का या तो तात्पर्य नहीं मालूम या अपने अहंकार से वे मुक्त होना नहीं चाहते। क्योंकि जिस व्यक्ति में साक्षीभाव प्रकट हो जाता है, वह कभी ऐसा प्रकट नहीं कर सकता।
अन्तर्जगत में आत्मा में हुई अनुभूति को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। क्योंकि अनुभूति स्वयं प्रमाण है, जैसे–स्वप्न में हम राजा बन गए। क्या हम जागने पर दिखा सकते हैं ? राजा बनने का साक्ष्य दे सकते हैं ? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वप्न में दिखी वस्तु प्रमाण नहीं है।
बहिर्जगत में घटी किसी घटना का हम प्रमाण दे सकते हैं, जैसे हमारी जेब में रुपया है जिसे हम दिखा सकते हैं। यही आत्मपरक सत्ता और वस्तुपरक सत्ता में अन्तर है।
तान्त्रिक साधना के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार की साधना अन्तरसाधना है और दूसरे प्रकार की साधना बहिर्साधना है। अंतर्साधना पूर्णरूप से योगपरक है जबकि बहिर्साधना योग पर आधारित बाह्य क्रियाओं पर आधारित है।
तन्त्र में इसी को आन्तर्याग और बहिर्याग कहते हैं। अन्तर्याग का सम्बन्ध आत्मपरक सत्ता से है, जबकि बहिर्याग का सम्बन्ध वस्तुपरक सत्ता से है। यह सत्य है कि बहिर्याग की समस्त साधनाएं संम्पन्न होने पर ही आन्तर्याग की साधना-भूमि में प्रवेश सम्भव है, अन्यथा नहीं। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो बहिर्याग का साधना-मार्ग अत्यंत कठिन है, अति गहन है और अति भावप्रधान है।
वस्तुपरक सत्ता से सम्बन्ध होने के कारण उसकी साधना-भूमि में उन भौतिक वस्तुओं, पदार्थों और क्रिया-कलापों का आश्रय लिया जाता है जो साधक के मन, प्राण और चित्त को चंचल व अस्थिर करने वाली होती हैं और सिद्ध होती हैं आत्मा में आकर्षण और मोह उत्पन्न करने वालीं। परिणामस्वरूप साधक को पथभ्रष्ट और साधनाच्युत होने का बराबर भय बना रहता है।
जरा-सी भी भूल-चूक आसमान से जमीन पर गिरा देती है एक क्षण में साधक को। जरा-सी भी असावधानी साधक को न इधर की रहने देती है, न उधर की। साधक न संसार का रह जाता है, न समाज का और न तो रह जाता है परिवार का ही। साक्षात नर्क बन जाता है वह अपने लिए। यही कारण है कि बहिरभूमि साधना-मार्ग में इष्ट और गुरु का होना अति आवश्यक है।
इष्ट रक्षा करता है और गुरु करता है मार्गदर्शन। यह कहना अनुचित न होगा कि इष्ट और गुरु दोनों अपने-अपने स्थान पर अपना महत्व रखते हैं।
अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों के उदय होने पर इष्ट की उपलब्धि होती है और इसी प्रकार अनेक जन्मों के शुभ संस्कारो के उदय होने पर सद्गुरु का दर्शन-लाभ होता है। साधक में योग्यता होनी चाहिए तभी तन्त्र-साधना-मार्ग पर व्यक्ति चल सकता है, अन्यथा नहीं।
यदि योग्यता नहीं है तो तांत्रिक साधना-मार्ग में न तो रुचि उत्पन्न हो सकती है और न ही आत्मा में जिज्ञासा का ही उदय हो सकता है।