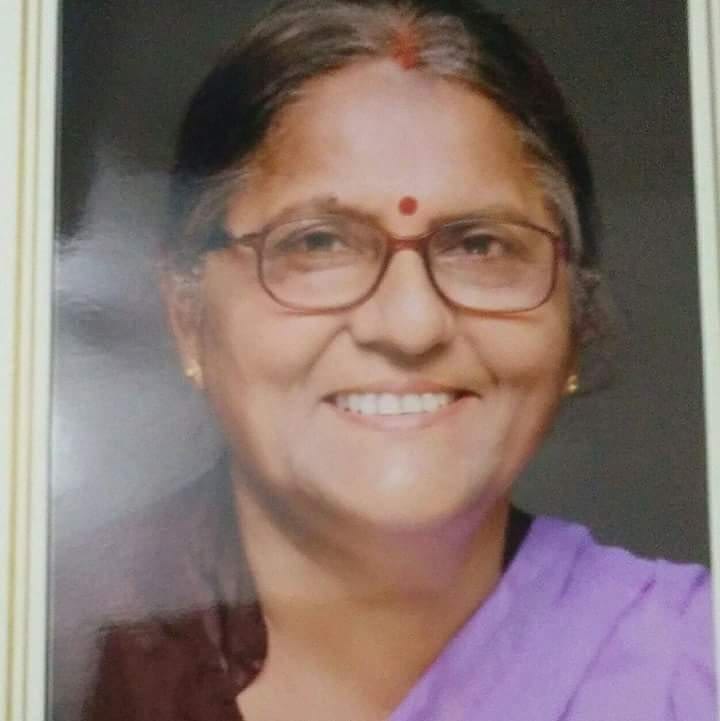डॉ. विकास मानव
मनुष्य ऐसी शक्ति के आधीन है जो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड में समान रूप से व्याप्त होते हुए एक है। उसी को भारतीय अध्यात्म कहता है-आदिशक्ति।
वास्तव में वही एकमात्र ऐसा साध्य कि है जिसकी खोज में मनुष्य हर जन्म में भटकता है और उसे प्राप्त करने के लिए उसकी आत्मा बार-बार जन्म लेती है।
कहने की आवश्यकता नहीं, तंत्र-मन्त्र-यंत्र उसी शक्ति को उद्भूत कर मानव कल्याण के लिए प्रकाशित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि तंत्र-मन्त्र- यंत्र वह माध्यम हैं जिसके द्वारा वह जगन्नियंत्रणकारिणी शक्ति भौतिक जगत में अपने आपको प्रकट करती है और प्रकट होकर मनुष्य की अभिलाषाओं को करती है पूर्ण और करती है उसका कल्याण।
यह सब तभी संभव है जब तंत्र-मन्त्र-यंत्र से सम्बन्धित पद्धति के अनुसार तांत्रिक अनुष्ठान और प्रयोग किये जाएँ।
वैदिक पद्धति, पौराणिक पद्धति और तांत्रिक पद्धति — ये तीन पद्धतियाँ हैं जिनमें तांत्रिक पद्धति अपने आपमें रहस्यमय है।
सभी पद्धतिओं में मन्त्रों का आविर्भाव होता है। तांत्रिक पद्धति में भी। मगर यह कार्य सभी के लिए सम्भव नहीं।
जिनके पास अपौरुषेय ज्ञान और ऊर्जा है, वे ही मन्त्रों की रचना कर और सिद्धि सकने में समर्थ हैं. इस के अधिकारी वे लोग हैं जो परम समाधि को उपलब्ध हैं।
मन्त्रों के आधार पर यंत्रों का निर्माण होता है। मन्त्र द्वारा यंत्र सिद्ध होने पर ही उसमें देवता के स्वरुप का आविर्भाव होता है और उसमें प्रकट होती है शक्ति।
प्रत्येक देवता के तीन रूप होते हैं–विग्रह रूप, मन्त्र रूप और यंत्र रूप। तीनों शक्तिपीठ हैं और तीनों रूपों की सिद्धि संभव है। प्रत्येक देवता का अपना एक मन्त्र और एक यंत्र होता है। किसी भी देवी-देवता की उपासना-साधना तभी सफल होती है जब उसके विधिवत् पूजन के साथ-साथ उसके यंत्र को धारण कर उस मन्त्र का निर्धारित संख्या तक जप किया जाय।
देवता तीन प्रकार के होते हैं–सात्विक, राजस और तामस। सात्विक देवता की उपासना उत्तरमुख, राजस देवता की साधना पूर्वमुख और तामस देवता की साधना पश्चिममुख बैठ कर करनी चाहिए। प्रत्येक देवी और देवता का अपना एक विशेष बीजाक्षर होता है जिसका अपना एक महत्व है।
मन्त्र के प्रारम्भ में बीजाक्षर को संयुक्त कर मन्त्र का जप करने से तत्काल लाभ होता है। जो व्यक्ति तंत्रोपासना के उपर्युक्त तथ्यों से भलीभांति परिचित हैं, वही तंत्रसाधना में प्रगति कर सकते हैं। तंत्रसाधकों के सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि प्रकट रूप में उच्चकोटि के तंत्रसाधकों की संख्या नगण्य है।
जो सच्चे अर्थों में तंत्रसाधक हैं, वे शीघ्र अपने आपको प्रकट नहीं करते। वे सदैव गुप्त रहने की चेष्टा करते हैं। वे ऐसा जीवन बिताते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि साधारण लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते कि वे तंत्रसाधक हैं।
हम जैसे लोग ऐसा न करें तो इस संसार और समाज में उनका रहना कठिन हो जाये, जीने न दें उनको लोग। उनकी साधना-उपासना में विघ्न उपस्थित हो, वह अलग।
उच्चकोटि के तंत्रसाधकों का साधना-मार्ग पूर्णरूप से योगपरक होता है। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है–महानिर्वाण। वे पूर्ण निरपेक्ष होते हैं। उनका जीवन अनासक्त और त्यागमय होता है।
वे जंगल में रहें, गुफा में रहें या रहें महल में और डूबे रहें आकंठ सुख और ऐश्वर्य के सागर में, लेकिन रहेंगे सब जगह निर्लिप्त होकर जैसे कीचड़ में कमल। वे बिखरेंगे तो दूसरों के लिए, वे दुःख-कष्ट उठाएंगे तो दूसरों के सुख के लिए, वे त्याग भी करेंगे तो दूसरों के लिए। वे हसेंगे या रोयेंगे तो दूसरों के लिए ही।
उनका अपने लिए कुछ भी नहीं होगा। उनके लिए मात्र केवल होगा–‘आत्मवत् सर्वभूतेषु।’
जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि देवता तीन प्रकार के होते हैं–सात्विक, राजस और तामस। राजस देवताओं को उपदेवता और तामस देवताओं को अपदेवता कहते हैं। सात्विक देवताओं का शरीर आकाश तत्व से बना हुआ होता है। आकाश सभी पञ्च तत्वों में प्रधान तत्व है, उसमें सभी तत्व एक एक कर विलीन हो जाते हैं।
विभिन्न प्रकार की साधना-उपासना आदि के द्वारा जब हम किसी सात्विक देवता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो वह सात्विक देवता हमारे आकाशीय शरीर के प्रति आकर्षित होकर उसके माध्यम से हमारी भावना के अनुरूप हमारी कामना को पूर्ण करता है।
साधना पथ में भ्रम और भ्रान्ति भी बहुत होती रहती है। साधना काल में विघ्न-बाधाएं भी बहुत आती रहती हैं। प्रायः निकृष्ट आत्माएं साधना में अड़चन भी डालने का प्रयास करती हैं। कभी-कभी दुष्ट आत्माएं वेश बदल कर उस देवी या देवता का स्वरुप धारण कर भ्रमित करने की चेष्टा करती हैं। पर सच्चे साधकों को वे भ्रमित नहीं कर पाती हैं।
उसका कारण यही है कि यदि वह सात्विक देवता है तो वह साधक के आकाशीय शरीर के प्रति आकर्षित होता है जिसका पता तत्काल साधक को चल जाता है क्योंकि उसके आकाशीय शरीर में एक शक्ति का एक विशेष संचार-सा होने लगता है।
यदि सात्विक देवता के स्थान पर राजस देवता या तामस देवता संपर्क स्थापित करता है तो साधक का आकाशीय शरीर के आलावा अन्य शरीर सक्रिय होते हैं जिनका पता भी साधक को तत्काल चल जाता है। हमारा आकाशीय शरीर जितना शुद्ध और निर्मल रहेगा, उस सात्विक देवता की कृपा उतनी ही अधिक उपलब्ध होगी।
दूसरी श्रेणी के देवता को राजस देवता कहते हैं। वे उपदेवता होते हैं। उनके शरीर का निर्माण वायु तत्व से हुआ रहता है। वायु तत्व को सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम प्राण कहते हैं। यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि उपदेवता इसी श्रेणी में आते हैं। वे रजोगुणी स्वभाव के होते हैं।
राजसी साधना उपासना से आकर्षित होकर उपदेवता हमारे प्राणमय शरीर से संपर्क स्थापित कर उसके माध्यम से हमारी कामना पूर्ण करते हैं। हमारी राजसी साधना-उपासना जितनी अनुकूल होगी, उतनी ही उनकी हमें कृपा उपलब्ध होगी। उपदेवताओं में प्राणशक्ति की प्रचुरता रहती है।
अपनी उसी शक्ति का आश्रय लेकर कभी- कभी वे भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं और साधक के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। सात्विक देवता ‘भाव’ के भूखे होते हैं। उनका एकमात्र भोजन भाव है। इसी तरह उपदेवता (यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि) का भोजन है– प्रेम, सौंदर्य, कला और भावना। आत्माकर्षिणी विद्या के द्वारा इन दोनों प्रकार के देवताओं को आकर्षित कर अपने मनोनुकूल किया जा सकता है।
जिस प्रकार हम अभौतिक स्तर की आत्माओं से संपर्क करने के इच्छुक रहते हैं और उनसे सहयोग चाहते हैं, उसी प्रकार सभी श्रेणी की आत्माएं भी हमसे संपर्क बनाने की इच्छुक रहती हैं और वे चाहती हैं कि मनुष्य उनका सहयोग करे, भौतिक स्तर की आवश्यकता की पूर्ति करे। देवता शब्द का अर्थ है–सदैव देने वाला। भले ही देवता किसी भी कोटि का क्यों न हो, वह सदैव देता है, लेता नहीं।
इस ब्रह्माण्ड की सीमा के अंतर्गत जितने भी जगत हैं, उनमें स्थूल जगत का महत्व सबसे अधिक है। उसी प्रकार सबसे अधिक महत्व है स्थूल जगत में निवास करने वाले मनुष्य का। क्योंकि बुद्धि, विवेक, विचार, ज्ञान, प्रज्ञा और मन–ये सब अपने अपने विकसित रूप में उसमें एक साथ उपस्थित हैं। इसलिए जितनी मानवेतर आत्माएं हैं, वे अपनी किसी भी कामना, भावना को साकार रूप देने के लिए मनुष्य के माध्यम से स्थूल जगत का ही आश्रय लेती हैं।
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि परब्रह्म परमेश्वर को भी अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए कई बार मनुष्य शरीर ग्रहण करना पड़ा और लेना पड़ा स्थूल जगत का आश्रय जिनकी लीला और चरित्र से प्लावित है हमारा धर्म और हमारी संस्कृति।
सात्विक आत्माएं जब मंत्राविष्ट होकर हमारे संपर्क में आती हैं, तो वे प्रसन्न होती हैं। उन्हें मनुष्य का सान्निध्य सुखद प्रतीत होता है। लेकिन सात्विक आत्माएं तभी हमारे संपर्क में आती हैं जब हम स्वयं शरीर से, मन से और आत्मा से सात्विक होंगे।
जिस स्तर के देवता से हमें संपर्क करना होता है तो हमें स्वयं को उसी स्तर का बनाना पड़ता है। तभी वे हमसे सम्बन्ध बनाएंगी। सात्विक आत्माएं धर्म और संस्कृति के उत्थान में, अध्यात्म के उत्थान में हमारे लिए सहयोगी सिद्ध होती हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे विचारों पर अपना प्रभाव डाल कर मठ, आश्रम, धर्मशाला, पाठशाला के निर्माण के लिए प्रेरित भी करती हैं। सहयोग करती है देवस्थापना के पवित्र कार्य में।
देवत्माओं के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और वह भी लोक कल्याण के कार्य में रत रहता है।
राजसी देवात्माएँ उपदेवता कहलाती हैं। यक्ष, गन्धर्व और किन्नर– ये तीन वर्ग उपदेताओं के हैं। 16 प्रकार के यक्ष- यक्षिणियां हैं। वे स्वयं सुन्दर होते हैं और सौंदर्य के प्रेमी भी होते हैं। मनुष्य के प्रति इनका विशेष आकर्षण होता है। सुन्दर और आकर्षक स्त्री के प्रति यक्षों की रूचि सर्वाधिक होती है। जहाँ सुन्दर, कमनीय, लावण्यमयी स्त्री को देखते हैं, तुरन्त मोहित हो जाते हैं वे उस पर और विभिन्न प्रकार से वे उसकी सहायता करते हैं अदृश्य रूप से।
यक्ष लोग अत्यधिक कामुक और रतिप्रिय होते हैं। वे कामक्रीड़ा और रतिक्रिया के समस्त गूढ़ रहस्यों से परिचित होते हैं। जो कलाकार काम और रति की विभिन्न मुद्राओं का आश्रय लेकर श्रंगारिक मूर्ति या चित्र का निर्माण करते हैं, उनको बराबर अगोचर सहयोग मिलता है यक्षों का।
जो लोग आत्माकर्षिणी विद्या की सिद्धि को उपलब्ध हैं, उनको तो इस दिशा में भरपूर सहयोग मिलता है यक्षों का। कभी-कभी तो सुन्दर मानव के रूप में भी प्रकट होकर मनुष्यों की सहायता करते हैं।
ऐसी ही यक्षिणियां भी होती हैं। वे भी जहाँ सुन्दर, आकर्षक, युवा व्यक्ति को देखती हैं, तुरंत मोहित हो जाती हैं वे। वे भी कामुक और रतिप्रिया होती हैं। उनकी ऑंखें मोरनी जैसी होती हैं। वे पुरुषों से संपर्क स्थापित करने के लिए सदैव लालायित रहती हैं। जिसने आत्माकर्षिणी विद्या के द्वारा किसी यक्षिणी को सिद्ध कर लिया है, उसकी प्रत्येक कामना को वे पूर्ण करती हैं।
साधक को इसका मूल्य चुकाना पड़ता है उसकी काम-पिपासा को शान्त करके। कभी-कभी यक्षिणियां भी सशरीर प्रकट हो जाती हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर लेती हैं। वास्तव में यक्षिणियां अति रहस्यमयी होती हैं। जो उनके चंगुल और मायाजाल में एक बार फंस गया, उसका फिर शीघ्र मुक्त होना संभव नहीं। इस विश्व ब्रह्माण्ड में जितने भी प्रकार के प्राणी होते हैं, वे सभी प्राण तथा उसके विभिन्न आयामों द्वारा संचालित होते हैं।
जहांतक आत्माओं का सम्बन्ध है, वे स्वयं की नैसर्गिक ऊर्जा द्वारा होती हैं संचालित और उसीके आधार पर इच्छानुसार रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी ही आत्माओं को विशुद्ध आत्मा कहते हैं।
यक्षों में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनमें प्राणशक्ति और आत्मशक्ति–दोनों का सामंजस्य है। वे जितने देवताओं के निकट हैं, कहीं उससे अधिक निकट हैं वे मनुष्यों के लिए। यजन करने वाली जाति को यक्ष कहते हैं। हमें यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि ब्रह्मा ने सबसे पहले पंचतत्वों में जल की उत्पत्ति की और उसके पश्चात् अन्य प्रणियों का निर्माण किया। जल का अर्थ है–जीवन देने वाला।
इसीलिए इसकी सबसे पहले उत्पत्ति की गयी प्राक्कल में। जिन-जिन प्राणियों का निर्माण हुआ था–वे सब मिलकर ब्रह्माजी के पास गए और कहने लगे कि हम सब भूख-प्यास से व्याकुल हैं। ब्रह्मा ने कहा–जल की रक्षा करो। एकमात्र जल ही जीवन है। कालान्तर में जल तत्व द्वारा ही अन्य पदार्थों का निर्माण होगा, इसलिए उसकी रक्षा करो।
यह सुनकर उन समस्त प्राणियों में से अधिकाँश बोल उठे–वयं रक्षामः (हम रक्षा करेंगे) और उनमें से कुछ बोल उठे–वयं यक्षामः (हम यजन करेंगे अर्थात् यज्ञ करेंगे)। ‘वयं रक्षामः’ बोलने वाले रक्ष संस्कृति के कारण आगे चल कर राक्षस या दानव कहलाये और ‘वयं यक्षामः’ कहने वाले यक्ष संस्कृति (यज्ञ-याग) के फलस्वरूप कहलाये–यक्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से एक समय दो ही जातियां थीं।
एक थी–यक्ष और दूसरी थी राक्षस। यक्ष ही आगे चलकर आर्यावर्त में मनु की सन्तान होने के फलस्वरूप मानव कहलाये। इस तरह पृथ्वी पर दानव और मानव दो प्रकार के शरीरधारी प्राणी बने सर्व प्रथम। मानव में प्रकृति प्रदत्त मन की प्रधानता है-इसीलिए उसे मनुष्य कहा गया। जबकि दानव में है बुद्धि चातुर्य की प्रधानता। अग्नि पुराण के अनुसार यक्षों की उत्पत्ति प्रचेता अर्थात् वरुण से हुई। इसलिए जलतत्व का प्रतीक वरुण है।
जलतत्व व्यापक काम की स्थिति है और यही कारण है कि यक्ष- यक्षिणियां अत्यधिक कामातुर और कामाचारी होते हैं। मनुष्य से सौ गुना अधिक कामाचारी होते हैं–यक्ष-यक्षिणियां।