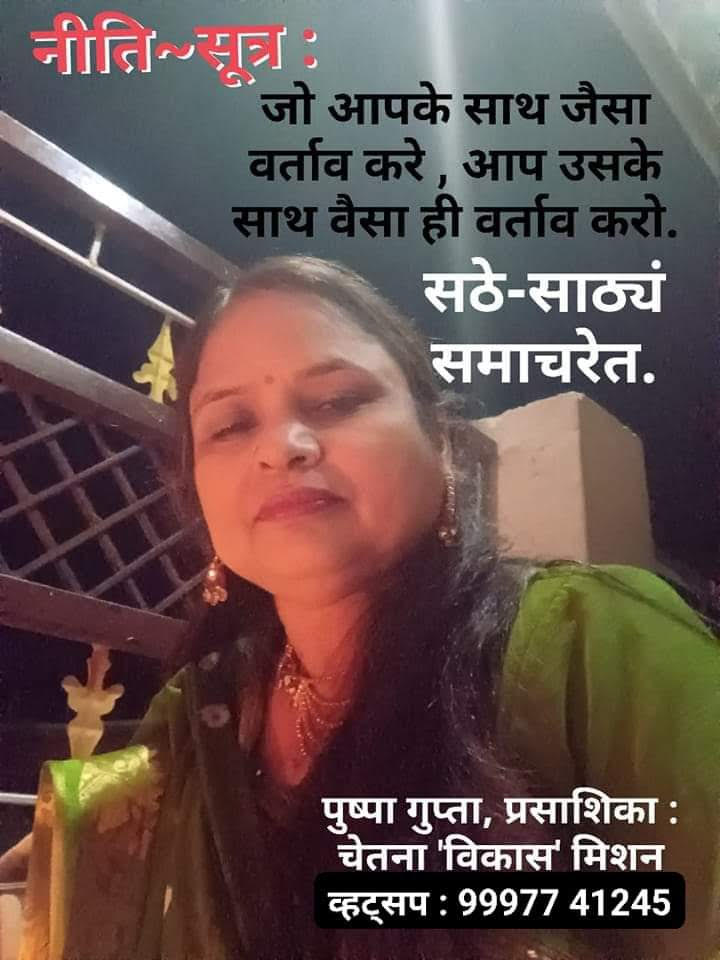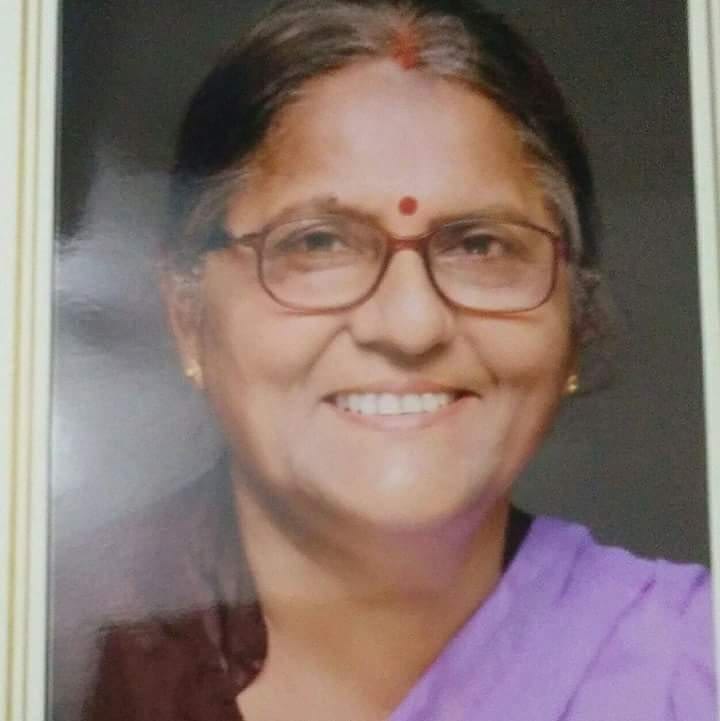पुष्पा गुप्ता
अथर्ववेद में शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है- व्यक्ति की बुद्धि की तीक्ष्ण करना उसे उत्तम शिक्षा के द्वारा उन्नत करना, उसके जीवन को प्रकाशित करना तथा प्रबुद्ध करना, उसे प्रगति की ओर ले जाते हुए सभी प्रकार के सौभाग्य से युक्त करना।
बृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभगाय|
संशितं चित् संतरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः।।
(अथर्व० ७.१६.१)
जीवन को सुखी और शान्ति से युक्त बनाना तथा उसे मधुरता प्रदान करना, यह शिक्षा का ही कार्य है।
शिवाः नः शंतमा भव समृडीका सरस्वति।
मा ते युयोम संदृशः।
(अथर्व० ७.६८.३)
शिक्षा मनुष्य को शान्ति देने के साथ ही मन को पवित्र करने वाली है। सद्विविचारों को पुष्ट करती है और जीवन में शक्ति प्रदान करती है।
यस्ते स्तनः शशयुर्यो मयोभूर्यः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः।
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवेऽकः।।
(अथर्व० ७.१०.१)
शिक्षा के द्वारा ही मानव में तेजस्विता आती है। अतएव शिक्षा के साथ संयम पर विशेष बल दिया गया है।
सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम्।
(अथर्व० ६.४१.२)
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते।
(अथर्व० ११.५.१९८)
यही कारण है कि कि महर्षि यास्क ने निरुक्त में आचार्य या शिक्षक का लक्षण देते हुए आचार एवं संयम की शिक्षा देने वाले को आचार्य कहा है-
आचार्य कस्मात् ? आचार्य आचारं ग्राहयति। आचिनोत्यर्थान्। आचिनोति बुद्धिम् इति वा।
(निरुक्त १.४)
महाभारत वनपर्व में बुद्धि के सात गुण बताए गए हैं-
शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ।
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः।
(२.१९)
अर्थात शब्द और अर्थ के गुणों को सुनने की इच्छा, सुनना, उसे ग्रहण करना, उसे विचारपूर्वक धारण करना, उसके सम्बन्ध में विचार करना, उसके अर्थ को ठीक-ठीक समझ लेना और वास्तविक ज्ञान को आत्मसात् कर लेना ही बुद्धि का गुण है। बुद्धि के इसी गुण से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानार्जन की इस प्रक्रिया में बुद्धि की वृत्तियों को उत्प्रेरित करने और जीवन्त बनाए रखने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है, वह साधन है आचार्य, शिक्षक या अध्यापक अध्यापक एक व्यापक शब्द है। जब हम इसे साधन के रूप में लेते हैं तो इसमें बालक के शिक्षक और शिक्षालय दोनों ही समाहित होते हैं। बालक का साध्य है शिक्षा साध्य और साधन का बड़ा ही पवित्र सम्बन्ध है। इस सन्दर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा भी है।
साधन में ही सब कुछ समाया हुआ है। जैसा साधन, वैसा साध्य साध्य और साधन में अन्तर नहीं है।
जगत्कर्ता ने हमें साधन पर यत् किंचित् अधिकार भी दिया है, पर साध्य पर नहीं। साधन जितना शुद्ध होगा, उतना ही साध्य शुद्ध होगा। इस विधान का एक भी अपवाद नहीं है।
इस दृष्टि से विचार करने पर बालक को शिक्षित करने में अध्यापक और शिक्षालय का उत्तरदायित्व बहुत गम्भीर हो जाता है।
एक मौलिक और जटिल प्रश्न है कि अध्यापक और शिक्षालय किसलिए हैं, शिक्षण क्या है? आज के सन्दर्भ में इसका महत्त्व और अधिक विचारणीय है। आचार्य विनोवा भावे ने कहा है कि ‘आज के इस अनुशासनपर्व में आचायों के अनुशासन एवं मार्गदर्शन में यदि प्रजा चलती है, तो प्रजा को सुख होगा।
समसामयिक सन्दर्भ में राष्ट्र के नवनिर्माण की भूमिका में अध्यापक के ऊपर एक महत्त्वपूर्ण दायित्व का भार है। यह भार थोपा नहीं गया है, अपितु सहज उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वाह इस देश का आचार्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं- वसिष्ठ, विश्वामित्र, मनु, कपिल, कणाद, वाल्मीकि, व्यास और चाणक्य, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अध्यापक के ऊपर उस युवापीढ़ी के निर्माण का भार होता है, जो आगे चलकर देश और समाज का निर्माण करता है। ऐसी दशा में विशेष विचारणीय है कि कैसी शिक्षा देना अपेक्षित है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जिसमें मुख्य वस्तु मन है मनु, मनुष्य और मानव शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत की मन् धातु से है, जिसका अर्थ है- मनन करना इस मन के शिक्षण और संवर्धन को हम शिक्षा कहते हैं।
मन ही इस जीवन प्रक्रिया का प्रमुख संचालक है। अतएव कहा गया है कि-
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।
मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है मन की इस कार्य प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन करते हुए उपनिषद् में कहा गया है-
यन्मनसा ध्यायति यद वाचा वदति यद् वाचा वदति, तत्कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते।
अर्थात् मनुष्य मन से जैसा विचार करता है, उसी प्रकार की बातें मुँह से कहता है। जैसी बातें मुँह से कहता है, उसी प्रकार के कार्य करता है और जिस प्रकार के कार्य करता है, उसी प्रकार का वह व्यक्ति हो जाता है। इसलिए मन की पवित्रता और शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य अध्यापक ही कर सकता है। वही आचार, विचार और शिष्टाचार की शिक्षा के द्वारा इस पवित्रता की ओर अभिरुचि जागृत कर सकता है। अतएव यजुर्वेद के ३४वें अध्याय के प्रारम्भ में ‘तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु’ की प्रार्थना की गई है।
मन को असाधारण शक्ति-सम्पन्न दिव्य ज्योति और ज्योतियों की ज्योति कहते हुए उसकी पवित्रता की प्रार्थना की गई है-
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।।
(यजु०३४.१)
मन में शुभ संकल्पों के आधान का उत्तरदायित्व आचार्य, शिक्षक और अध्यापक पर है।
इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद् के शीक्षाध्याय में शिक्षा का जो रूप प्रस्तुत किया गया है. वह विशेष माननीय है-
आचार्यः पूर्वरूपम्। अन्तेवासी उत्तररूपम्। विद्या सन्धिः। प्रवचनं संधानम्।
(तैत्ति० १.३.३)
आचार्य पूर्वरूप है, विद्यार्थी उत्तररूप है, विद्या दोनों को जोड़ती है और प्रवचन या उपदेश उसको जोड़ने का साधन है।
आचार्य या शिक्षक पूर्वरूप है, उसका जैसा आचरण कार्य व्यवहार होगा, वही विद्यार्थियों पर प्रतिफलित होता है, वह उत्तररूप है। जैसा गुरु वैसा शिष्य शिष्य गुरु का प्रतिविम्व है। गुरु के आदशों, कार्यों और व्यवहारों पर चलने वाला पथिक है। जैसा उसका मार्गप्रदर्शन किया जाएगा, वैसा ही उसका जीवन होगा। इस दृष्टि से विचार करने पर शिक्षक या अध्यापक के ऊपर महान् उत्तरदायित्व आ पड़ता है।
समाज के निर्माण में उसका अनुपम योगदान है। शिक्षक वह संस्था है, जिसका जाल छोटे से छोटे ग्राम से लेकर बड़े से नगर तक फैला हुआ है। उसमें चेतना और जागरूकता है। जीवन और राष्ट्र की गतिविधि को पहचानने की क्षमता है। भारतवर्ष हो नहीं, विश्व के विभिन्न विकासशील देशों में अध्यापकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया है। आज हमारी तात्कालिक आवश्यकता है कि अध्यापक अपने गुरुतर भार को स्वयंसेवी दृष्टि से अपनाते हुए राष्ट्र की उन्नति में अग्रसर होकर छात्रवृन्द का सफल मार्ग-प्रदर्शन करें।
युवावर्ग योग्य चरित्रवान् व्यक्तियों से अपने कर्तव्य की दीक्षा चाहते हैं. अपने आदर्शों और लक्ष्यों का यथार्थ प्रतिपादन] चाहता है. राष्ट्र की उन्नति और प्रगति में योगदान करना चाहता है, अत: अध्यापक का दायित्व हो जाता है कि वह छात्रों में अनुशासन को गरिमा को उदबुद्ध करते हुए उनमें संयम और अनुशासन का भाव जागृत करें। अथर्ववेद में इसीलिए कहा गया है-
वाचस्पतिनिं यच्छतु।
(अथर्व १.१.३)
शिक्षक स्वयं अनुशासन में रहता हुआ छात्रवृन्द को अनुशासन की शिक्षा दें।
श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार-
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् तदेवेतरो जनः।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।
( गीता ३.२१)
श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही अन्य व्यक्ति भी आचरण करते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति की मान्यता होती है, वही जनसाधारण की मान्यता होती है। अतः वर्तमान सन्दर्भ में राष्ट्रहितकारी आदर्श प्रस्तुत करना और तद्नुसार युवा पीढ़ी को सम्बोधित करना प्रत्येक अध्यापक का दायित्व है।
इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं में असामाजिक एवं अनैतिक तत्त्वों को प्रश्रय न दिया जाए। जनतन्त्र की रक्षा और उसके लिए बलिदान होने की भावना युवावर्ग में जागृत करनी होगी।
सम्प्रति समस्त देश के बहुमुखी विकास के लिए और सभी वर्ग के लोगों की समृद्धि को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने जिन नए आर्थिक कार्यक्रमों के परिपालन का आदेश दिया है, उन्हें सक्रिय रूप से सफल बनाने में युवावर्ग असाधारण सहयोग दे सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।