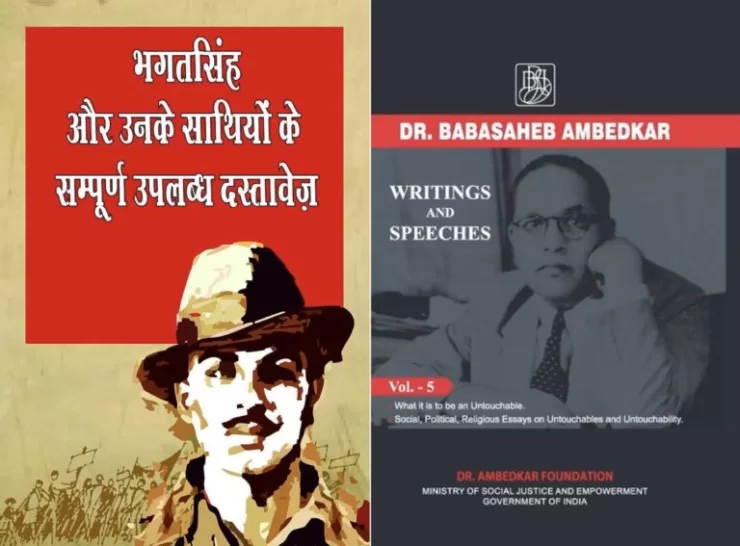कोई भी गरीब दंगों में इसलिए भाग नहीं लेता कि वह भूखा है, और रोटी की चाह में कुछ भी कर सकता है।यह गरीबों पर एक ऐसा आरोप है, जो आसानी से लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है।
कंवल भारती
भगत सिंह का ‘सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज’ शीर्षक लेख जून, 1928 के ‘किरती’ में छपा था। इस लेख के परिचय में संपादकीय टिप्पणी में लिखा गया है– “1919 के जलियांवाला बाग़ हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति तेज़ कर दी। इसके असर से 1924 में कोहाट [पाकिस्तान में एक शहर] में भयानक हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना में सांप्रदायिक दंगों पर लंबी बहस चली। इन्हें समाप्त करने की ज़रूरत तो सबने महसूस की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू-मुस्लिम नेताओं में सुलहनामा लिखाकर दंगों को रोकने के यत्न किए। इस समस्या के निश्चित हल के लिए क्रांतिकारी आंदोलन के विचारों को प्रस्तुत करते हुए भगत सिंह ने यह लेख लिखा।”[1]
भगत सिंह के इस लेख पर हम बाद में आएंगे। पहले यह समझ लें कि सांप्रदायिक समस्या क्या है? अक्सर इसे हिंदू-मुस्लिम फसाद या फिर धार्मिक कट्टरवाद के रूप में देखा और समझा जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग इसे दो राष्ट्र के सिद्धांत में समझने की कोशिश करते हैं। असल में सांप्रदायिक समस्या की जड़ में हिंदू-मुसलमान नहीं हैं। यह हिंदू-सिख की समस्या भी है, हिंदू-ईसाई की समस्या भी है और हिंदू-दलित की समस्या भी है। सांप्रदायिक समस्या को दो राष्ट्रों के सिद्धांत के नज़रिए से भी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ भाषा और क्षेत्र आदि की भी बहुत-सी राष्ट्रीयताएं जुड़ी हुई हैं। ताज़ा उदाहरण, मणिपुर में जारी दंगा है, जो हिंदू-मुस्लिम के बीच का दंगा नहीं है।
फिर सांप्रदायिक समस्या क्या है? इसे परिभाषित करना मुश्किल नहीं है। सबसे कम शब्दों में यदि कहना हो, तो यह सांप्रदायिक बहुमत की तानाशाही का नाम है। मतलब यह कि अगर कोई संप्रदाय बहुमत के आधार पर (राजनीतिक नहीं, सामाजिक बहुमत के आधार पर), अल्पसंख्यकों पर शासन करना अपना दैवीय अधिकार समझता है, तो उसका नाम सांप्रदायिकता है।
सांप्रदायिक समस्या क्यों और कैसे पैदा हुई? अक्सर भारत के ब्राह्मण इतिहासकार, चाहे वे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी, इसका दोष अंग्रेज़ों पर डालते हैं कि उनकी ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति ने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। यह आरोप सही नहीं है। कभी भी दो विशेषाधिकार-संपन्न वर्गों या संप्रदायों में फूट नहीं पड़ती। फूट वहां पड़ती है, जहां एक वर्ग या संप्रदाय विशेषाधिकार-संपन्न होता है, और दूसरे वर्ग या संप्रदाय के पास बहुत कम अधिकार होते हैं, या बिलकुल नहीं होते। फूट हमेशा धनी और निर्धन, शोषक और शोषित एवं संपन्न और विपन्न के बीच पड़ती है। यह फूट यानी असंतोष ही सांप्रदायिक दंगों का कारण बनता है। अंग्रेज़ों ने न तो वंचित वर्गों और संप्रदायों का निर्माण किया था, और न समाज का विभाजन किया था। ये सब भारत में पहले से अस्तित्व में थे।
यहां मैं डॉ. आंबेडकर के संदर्भ से भारतीय समाज के विभाजन का वह चित्र प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो उन्होंने 1919 में साउथबरो मताधिकार समिति के समक्ष अपने लिखित ज्ञापन में दिया था। उन्होंने कहा था कि सामान्यत: सांप्रदायिक आधार पर लोगों के दिमाग में जो समाज-विभाजन रहता है, वह इस रूप में रहता है– (1) हिंदू, (2) मुसलमान, (3) ईसाई, (4) पारसी, और (5) यहूदी। इनमें हिंदुओं को छोड़कर शेष संप्रदायों में परस्पर सामाजिक व्यवहार की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन हिंदुओं के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे हिंदू से पहले किसी जाति के सदस्य होते हैं; और प्रत्येक जाति के बीच सामाजिक व्यवहार की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। सामाजिक संपर्क और व्यवहार की दृष्टि से हिंदुओं के दो समूह हैं– सछूत और अछूत। अछूत पूरी तरह हिंदुओं में बहिष्कृत समुदाय या वर्ग है। इस प्रकार भारतीय समाज का वास्तविक विभाजन इस प्रकार है– (1) सछूत हिंदू, (2) अछूत हिंदू, (3) मुसलमान, (4) ईसाई, (5) पारसी, और (6) यहूदी।[2] इस विभाजन को आज भी नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता। साउथबरो मताधिकार समिति के एक सदस्य डब्लू. एम. हेली ने इसे स्वीकार करते हुए लिखा था कि “अछूत वे लोग हैं, जो नागरिक अधिकारों से वंचित रखे गए हैं। इसी की वजह से अछूत लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं किया जाता।”[3]

अब थोड़ी चर्चा इस संबंध में भी कि सांप्रदायिक विद्वेष इस सामाजिक विभाजन में कैसे पैदा हुआ? अब अछूतों को मैं इस चर्चा से दूर रखता हूं, और इसे केवल हिंदू-मुस्लिम संप्रदायों तक ही केंद्रित करता हूं। ब्रिटिश संसद द्वारा 1892 में इंडियन कौंसिल्स एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट में सरकार ने ‘सर्वसम्मत प्रतिनिधित्व’ के सिद्धांत को स्वीकार किया था। यह प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का सिद्धांत था। इस एक्ट के अंतर्गत निर्मित विधान-सभाओं में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रवेश दिया गया था। इसके बाद राजनीति में उनकी मांगें बढ़ती गईं। इसका कारण यह था कि मुसलमान अपने नागरिक हितों की सरकार से सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि हिंदुओं का जोर बहुसंख्यक वर्ग के शासन पर था। वे न सर्वसम्मति के शासन से सहमत थे, और न अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार थे। डॉ. आंबेडकर ने लिखा है कि बहुसंख्यक वर्ग के शासन के बारे में हिंदू नेता किसी भी परिसीमन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदू, बहुसंख्यक वर्ग के शासन के सिद्धांत को इतना पवित्र मानते थे कि उसका उल्लंघन पसंद नहीं करते थे।[4] हिंदू इसे आज तक स्वीकार करते और मानते चले आ रहे हैं, जबकि यह निरंकुशतावादी सिद्धांत है। आंबेडकर के अनुसार, यह राजनीतिक बहुमत नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक बहुमत है। राजनीतिक बहुमत बदलता रहता है, वह स्थायी नहीं होता, लेकिन सांप्रदायिक बहुमत स्थायी होता है और स्थायी बनाकर रखा जाता है।[5] लेकिन हिंदुओं का यह स्थायी बहुमत भी भ्रामक बहुमत है, क्योंकि इस बहुमत में वे अछूतों, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और आदिम जनजातियों को भी शामिल करके चलते हैं, जिनके हितों का वे सदैव विरोध करते हैं। इन समुदायों को अगर निकाल दिया जाए, तो उनके राजनीतिक बहुमत को अल्पमत में आते देर नहीं लगेगी।
बहुमत के शासन का यह निरंकुशतावादी सिद्धांत ही भारत में सांप्रदायिक फसाद की असली जड़ है। यह सिद्धांत हिंदुओं, और खासकर ब्राह्मणों के शासन को स्थापित करता है। कोहाट में हुए जिन दंगों का जिक्र भगत सिंह के लेख के परिचय में किया गया है, वे 1924 में ब्रिटिश भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के कोहाट शहर में 9 से 11 सितंबर के बीच हुए थे। रिकार्ड के अनुसार जून, 1924 में सरदार माकन सिंह का बेटा एक मुस्लिम लड़की को लेकर भाग गया था। इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। इसे हिंदुओं ने जबरन धर्मांतरण के रूप में प्रचारित किया। दंगे की आग आर्य समाज के आक्रामक उन्मादी प्रचार से भड़की थी। उस क्षेत्र में हिंदू और सिख आर्थिक रूप से प्रभावशाली थे। तत्कालीन प्रांतीय आयुक्त एच. डीन ने धार्मिक शत्रुता बढ़ाने के लिए आर्य समाज को जिम्मेदार ठहराया था। यह स्थिति तब थी, जब कोहाट में हिंदुओं और सिखों की संख्या 8 हज़ार थी और मुस्लिम अपनी आबादी में 19 हज़ार की संख्या में थे। इसका एक कारण यह भी था कि उन्नीसवीं सदी के अंत के साथ, कोहाट में धार्मिक-राजनीतिक चेतना की लहरें बढ़ गई थीं, और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के होने के कारण, उपमहाद्वीप के मुसलमानों ने राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए धर्म-आधारित मार्ग तलाश लिए थे।[6] कोहाट का मामला सीधे-सीधे दो अलग-अलग समुदाय के युवक और युवती के बीच प्रेम से संबंधित था। लेकिन हिंदुओं को इसे लव-जिहाद का मामला बनाकर तमाम मासूमों का खून बहाकर ही चैन आया। इस बहुमत के शासन को मनुष्यों के खून की परवाह न पहले थी, और न अब है। बस वह अल्पसंख्यकों पर हिंदुत्व का प्रभुत्व बनाए रखने की परवाह करता है, भले ही इसके लिए कितना ही इंसानी खून बहाना पड़े।
भगत सिंह के लेख में यह तो बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक बंटवारे की जो राजनीति की, उसके असर से 1924 में कोहाट में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वह दंगा हिंदू नेताओं द्वारा एक प्रेम कहानी को धार्मिक रंग देकर करवाया गया था। उसमें सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति की कोई भूमिका नहीं थी। भगत सिंह ने अपने लेख में हिंदुओं के बहुमत के शासन के तथाकथित पवित्र सिद्धांत की भी कोई आलोचना नहीं की है, जो भारत में हिंदू-मुस्लिम-फसाद और नफ़रत का सबसे प्रमुख कारण है।
1924 के कोहाट-दंगों के बाद, 1925 में लाला हरदयाल[7] ने हिंदुओं के लिए ‘राजनीतिक वसीयतनामा’ जारी किया था, जिसने भारत में हिंदू राज की नींव डाली थी। भगत सिंह के लेख में इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि लेख 1928 में लिखा गया था। लाला हरदयाल का राजनीतिक वसीयतनामा इस तरह था–
“मैं घोषणा करता हूं कि हिंदू जाति, हिंदुस्तान और पंजाब का भविष्य इन चार स्तंभों पर टिका है : (1) हिंदू संगठन, (2) हिंदू राज, (3) मुसलमानों की शुद्धि, और (4) अफ़ग़ानिस्तान तथा सीमांत क्षेत्रों की शुद्धि और उन पर विजय। जब तक हिंदू जाति ये चारों बातें पूरी नहीं कर लेगी, तब तक हमारी भावी संतानों की सुरक्षा पर हमेशा खतरा बना रहेगा और हिंदू जाति की सुरक्षा असंभव हो जाएगी। जैसे नेपाल में हिंदू धर्म है, उसी तरह अफ़ग़ानिस्तान और हमारे सीमांत क्षेत्रों में हिंदू धर्म स्थापित होना चाहिए, अन्यथा, स्वराज पाना व्यर्थ होगा।”[8]
इस राजनीतिक वसीयतनामे में अफ़ग़ानिस्तान और सीमांत क्षेत्रों की शुद्धि और उन पर विजय का मतलब है– वहां से मुसलमानों को साफ़ करना। क्या इस राजनीतिक वसीयतनामे में सांप्रदायिक दंगों का बीज नहीं बोया गया था? अगर हिंदुओं ने बहुमत के (हिंदू) शासन के पागलपन के सिद्धांत को न अपनाया होता, और सह-अस्तित्व में विश्वास किया होता, तो क्या भारत का विभाजन होता, क्या अफ़ग़ानिस्तान और सीमांती इलाक़े हमसे अलग होते, और क्या सांप्रदायिक दंगों का प्रश्न उठता? अगर हिंदू अपने इस पागलपन को आज भी महसूस नहीं करते, तो इसका एक ही अर्थ है कि वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। लेकिन, हिंदू-मुस्लिमों में बंटवारे के विरोध को पागलपन नहीं मानते, बल्कि बहुसंख्यकवाद के तहत उसे अपना अधिकार समझते हैं। दरअसल हुआ यह था कि साउथबरो मताधिकार समिति के समय वयस्क मताधिकार का नियम नहीं था। इसके विपरीत शिक्षा और संपत्ति के आधार पर लोगों को मतदान का अधिकार था। इस दृष्टि से दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियां मताधिकार के क्षेत्र से बाहर हो गईं थीं, क्योंकि उनके पास शिक्षा और संपत्ति, दोनों नहीं थे। शिक्षा और संपत्ति के लिहाज से अपर कास्ट के हिंदुओं और मुसलमानों से ही मतदाता बनते थे। शिक्षा और संपत्ति अपर कास्ट के हिंदुओं के पास थी, इसलिए मतदाता भी अपर कास्ट के हिंदुओं में अधिक थे, उनमें भी ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा थे। फिर भी, हिंदू अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए बहुसंख्यक होने का खेल खेलते थे, जो वे नहीं थे, और मुसलमानों को कम-से-कम सीटें देना चाहते थे। असल लड़ाई यही थी।
अब हम भगत सिंह के लेख में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि सांप्रदायिक दंगे रोकने का उनके पास कौन सा इलाज था? उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के दो कारण गिनाए हैं– धर्म और अर्थ। धर्म के बारे में वह लिखते हैं– “बस किसी एक व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफ़ी था और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। जब स्थिति यह हो तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है।”[9] हालांकि यह मुहावरा है, पर फिर भी, नास्तिक भगत सिंह के लिए हिंदुस्तान के भविष्य को ईश्वर पर छोड़ना अजीब लगता है।
भगत सिंह धर्म पर आगे और भी प्रहार करते हैं–
“इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा ग़र्क कर दिया है। और अभी पता नहीं कि ये धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे? इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है। और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई विरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है, जो अपना दिमाग़ ठंडा रखता है, बाकी सबके सब धर्म के ये अपने नामलेवा धर्म के रोब को क़ायम रखने के लिए डंडे-लाठियां, तलवारें-छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़कर मर जाते हैं। बाक़ी बचे, कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। इतना रक्तपात होने पर इन धर्मजनों पर अंग्रेज़ी सरकार का डंडा बरसता है और फिर इनके दिमाग़ का कीड़ा ठिकाने पर आ जाता है।”[10]
यहां भगत सिंह ने धार्मिक कट्टरवाद का प्रश्न उठाया है और धर्म के नाम पर एक-दूसरे का खून बहाने वालों को सही फटकार लगाई है। आगे उन्होंने दंगों को भड़काने में आग में घी डालने के लिए धार्मिक नेताओं और अखबारों की भूमिका की भी निंदा की है। उन्मादी पत्रकारिता पर उनकी आलोचना आज भी प्रासंगिक है–
“अख़बारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था; लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई-झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या?”[11]
सौ साल पहले की पत्रकारिता पर भगत सिंह के ये विचार आज की पत्रकारिता के लिए भी शत-प्रतिशत सही हैं। आज उसमें टीवी-पत्रकारिता भी शामिल हो गई है, और दोनों मिलकर धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इसके मूल में भी बहुमत के शासन का ही सिद्धांत है, जो भारत को हिंदुओं की भूमि मानकर चलता है, और गैर-हिंदुओं के प्रति सह-अस्तित्व का भाव नहीं रखता।
भगत सिंह ने ठीक ही धर्म को नकारा है। पर भारत जैसे धार्मिक देश में, जहां लोग विज्ञान से ज्यादा मुल्ला-पंडितों पर विश्वास करते हैं; और यहां के लोग क़र्ज़ लेकर भी धार्मिक यात्राएं करते हैं, और जिस देश का वैज्ञानिक भी धार्मिक कर्मकांड में आस्था रखता हो, वहां धर्म को नकारना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में धर्म समस्या का कारण तो है, बल्कि उसे नकारना समस्या का निदान नहीं है। फिर समस्या का निदान क्या है? निदान लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग और संप्रदाय को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित न रखा जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए और उन्हें यह महसूस न कराया जाए कि वे दोयम दर्ज़े के नागरिक हैं। आंबेडकर गलत नहीं कहते हैं कि धर्म भी भारत में सत्ता-प्राप्ति का एक साधन है। और अगर लोकतंत्र में भी धर्म के प्रभुत्व को मान्यता दी जाती है, तो कभी भी न स्वतंत्रता क़ायम रह सकती है, और न समानता का सिद्धांत लागू हो सकता है।[12] आज यही हो रहा है। धर्म के नाम पर बहुसंख्यकवाद सत्ता प्राप्त करने के बाद लोकतंत्र का पालन नहीं करता, बल्कि सभी गैर-द्विजों और सभी गैर-हिंदुओं के वैधानिक अधिकारों के हनन को अपने शासन की कार्य-योजना बनाता है। फिर जब गैर-द्विजों और गैर-हिंदुओं में असंतोष उभरता है, और वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, तो उसे कुचलने के लिए पुलिस-बल का प्रयोग किया जाता है, और पूरी योजना के साथ दंगा करा दिया जाता है। मणिपुर इसका भी उदाहरण है।
भगत सिंह धर्म को राजनीति से अलग करने पर जोर देते हुए कहते हैं–
“1914-15 के शहीदों ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। वे समझते थे कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसमें दूसरे का कोई दख़ल नहीं। न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए, क्योंकि यह सरबत [सबकी भलाई चाहनेवाले जन-समूहों] को मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता। …इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं, जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज़ है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठा हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहें अलग-अलग ही रहें।”[13]
भगत सिंह का यह विचार सांप्रदायिक विवाद के निदान में आज भी महत्वपूर्ण है। काश ऐसा हो सकता कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाता। लेकिन हुआ क्या? संविधान-निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तो स्वीकार किया, पर स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने, धर्मनिरपेक्षता के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, 101 ब्राह्मणों के पैर पखारकर, चरणामृत पीकर हिंदू पहचान ही भारत की क़ायम की। उस पर कांग्रेस ने सभी राज्यों के पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ब्राह्मण को बैठाकर (यहां तक कि अपवाद स्वरूप भी कोई गैर-ब्राह्मण नहीं) लोकतंत्र में ब्राह्मण-राज को प्रवेश करा दिया। पाकिस्तान को धर्म के आधार पर मुस्लिम राज्य बताकर भारत को हिंदू राज बनाने के लिए कांग्रेस के ब्राह्मण-तंत्र ने 1947 से ही काम करना शुरू कर दिया था। उसने हिंदी पट्टी के प्रत्येक जिले में रामलीला कमेटियां बनवाईं, आकाशवाणी पर प्रात: रामचरितमानस का नियमित पाठ कराया, और ‘कीर्तन’ नाम का एक नया लटका (धर्म-प्रदर्शन) शुरू किया, जो सत्तर के दशक तक इतना व्यापक हो गया था कि हिंदुओं में, घर-घर में कीर्तन होने लगा था। जबकि सच यह है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण बंटवारे की राजनीति के कारण हुआ था। मुसलमानों ने समझ लिया था कि हिंदुओं की बहुसंख्यकवाद की राजनीति में मुसलमान कभी भी भारत में न प्रधानमंत्री बन सकते हैं और न मुख्यमंत्री। इसलिए पाकिस्तान का निर्माण ही उनके हित में था। और यह भगत सिंह ने अपने एक अन्य लेख में स्वयं स्वीकारा भी है कि “कांग्रेस के मंच से आयतें और मंत्र पढ़े जाने लगे थे। उन दिनों धर्म में पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी थी।”[14]
एक और लेख में भगत सिंह लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर कोई भी नेता समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों का नहीं था, यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस भी नहीं, जो वेदों की ओर लौटने का आह्वान करते थे।[15]
भगत सिंह की दृष्टि में सांप्रदायिक दंगों का दूसरा कारण आर्थिक है। इसे उन्होंने इस तरह समझाया है–
“यदि इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ खोजें तो हमें इसका कारण आर्थिक ही जान पड़ता है। असहयोग के दिनों में नेताओं और पत्रकारों ने ढेरों क़ुर्बानियां दीं। उनकी आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। असहयोग आंदोलन के धीमा पड़ने पर नेताओं पर अविश्वास सा हो गया, जिससे आजकल के बहुत से सांप्रदायिक नेताओं के धंधे चौपट हो गए। कार्ल मार्क्स के तीन बड़े सिद्धांतों में से यह एक मुख्य सिद्धांत है। इसी कारण से तबलीग, तनकीम, शुद्धि आदि संगठन शुरू हुए और इसी कारण से आज हमारी ऐसी दुर्दशा हुई, जो अवर्णनीय है।”[16]
भगत सिंह का यह आर्थिक कारण समझ से परे है। अछूतों के लिए मुसलमानों के तबलीग और हिंदुओं के शुद्धि आंदोलन राजनीतिक थे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका कि वे अपनी-अपनी संख्या बढ़ाने के उपक्रम थे। उन्हें दंगे होने के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अछूतों के मुसलमान या ईसाई बनने पर सरकारी रोक न होने के कारण वे धर्मांतरण अवैध नहीं थे। भगत सिंह आगे आर्थिक कारण पर और भी ज़ोर देकर कहते हैं–
“बस, सभी दंगों का इलाज़ यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है, क्योंकि भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी ख़राब है कि एक व्यक्ति दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवा सकता है। भूख और दुःख से आतुर होकर मनुष्य सभी सिद्धांत ताक पर रख देता है। सच है, मरता क्या न करता।”[17]
यह तर्क कि भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह गरीबों पर एक ऐसा आरोप है, जो आसानी से लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। कोई भी गरीब दंगों में इसलिए भाग नहीं लेता कि वह भूखा है, और रोटी की चाह में कुछ भी कर सकता है। कोई गरीब किसी दंगे में तभी भूमिका निभाता है, जब उसमें किसी धर्म-समुदाय के खिलाफ नफ़रत की विचारधारा भरी जाती है। वह गरीबी की वजह से नहीं, नफ़रत की विचारधारा की वजह से दंगे में भाग लेता है। लेकिन यह सच है कि गरीबों में नफ़रत की विचारधारा जल्दी भर जाती है, क्योंकि अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे होने के कारण उनमें चेतना नहीं होती है।
लेकिन भगत सिंह का ज़ोर भी समाज-सुधार पर नहीं, आर्थिक सुधार पर ही था। उन्होंने आगे लिखा–
“लेकिन वर्तमान स्थिति में आर्थिक सुधार होना कठिन है, क्योंकि सरकार विदेशी है और यह लोगों की स्थिति को सुधरने नहीं देती। इसीलिए लोगों को हाथ धोकर इसके पीछे पड़ जाना चाहिए और जब तक सरकार बदल न जाए, चैन की सांस न लेना चाहिए।”[18]
यह किस तरह का विचार था भगत सिंह का? अगर 1928 में ही, जब भगत सिंह ने यह लेख लिखा था, सरकार बदल जाती, तो क्या आर्थिक सुधार हो जाते? सारे गरीबों को रोज़गार मिल जाता और सभी भूमिहीनों को भूमि मिल जाती? और ये सब कौन करता? अंग्रेज़ सरकार चली जाती तो किसकी सरकार बनती? क्या मजदूरों की सरकार बनती या उन हिंदू-मुस्लिम राष्ट्रीय नेताओं की, जो सिर्फ स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे, और स्वराज के निर्माण की कोई योग्यता नहीं रखते थे? जो हिंदू अछूतों को अपने कुंए की जगत पर नहीं चढ़ने देते थे, क्या वे उन्हें शिक्षा और रोज़गार देते? आंबेडकर ने कहा था कि अगर स्वतंत्रता का मतलब उस प्रभुत्व के विनाश से है, जो कोई व्यक्ति दूसरे पर क़ायम करता है, तो निश्चित रूप से आर्थिक सुधार ही एक मात्र सुधार है, जो होना चाहिए।[19] लेकिन क्या स्वराजवादियों की दृष्टि में स्वतंत्रता का यही अर्थ था? नहीं। वे स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि स्वराज यानी स्वयं का राज क़ायम करने के लिए लड़ रहे थे, और उनका उद्देश्य था अंग्रेजों के जाने के बाद देश के संसाधनों पर स्वयं कब्जा करना। आंबेडकर ने समाजवादियों की आर्थिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा था कि यह ज़रूरी नहीं है कि संपत्ति की बराबरी ही वास्तविक सुधार है और इसे किसी भी अन्य सुधार से पहले किया जाना चाहिए। उन्होंने समाजवादियों से पूछा कि क्या वे सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बगैर आर्थिक सुधार कर सकते हैं? भारत के समाजवादियों ने लगता है, इस प्रश्न पर कभी विचार ही नहीं किया।[20]
भगत सिंह का यह कहना कि आर्थिक सुधारों के लिए लोगों को अंग्रेज़ी सरकार बदलने की जरूरत थी, कई सवाल खड़े करता है। मसलन, उन्होंने इस सवाल पर विचार नहीं किया कि लोग ऐसी किसी भी क्रांति में तब तक भाग नहीं ले सकते, जब तक कि उनको यह यक़ीन न हो जाए कि क्रांति के बाद उनके साथ धोखा और भेदभाव नहीं होगा; या यह कि सरकार बदलने के बाद जो स्वराज-सरकार आती, वह आर्थिक सुधारों को भी लागू करती, इसकी क्या गारंटी थी? अक्सर वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत को पवित्र सिद्धांत समझने वाले मार्क्सवादी विचारक इस सवाल पर विचार करते ही नहीं। इसलिए इस पर भगत सिंह ने भी विचार नहीं किया। उन्होंने आगे लिखा–
“लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग-चेतना की ज़रूरत है। ग़रीब मेहनतकश और किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी ग़रीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता और देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताक़त अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों में तुम्हारा कुछ नुक़सान नहीं होगा, इससे किसी दिन तुम्हारी ज़ंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।”[21]
ग़रीबों और मजदूरों के लिए मार्क्सवादियों का यह विचार वाक़ई सुंदर है। पर सिर्फ सुंदर है, हकीक़त नहीं है। यह विचार इस धारणा पर आधारित है कि केवल दो ही वर्ग हैं– गरीब और अमीर, या मालिक और मजदूर। यह धारणा ही गलत है। आंबेडकर के शब्दों में यह उतना ही गलत है, जितना यह मानना कि मनुष्य का सरोकार केवल आर्थिक समृद्धि या उसके केवल प्रबुद्ध होने या केवल तार्किक होने से है, जो सभी वर्गों में मौजूद है।[22] भगत सिंह के समय में भी जाति मजदूर-एकता में बाधक थी, और आज भी है। क्या जाति को समाप्त किए बिना मज़दूर एकता हो सकती है? क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा वर्ग, अमीर और ग़रीब के अलावा, जातीय भेदभाव को नहीं मानता? क्या भगत सिंह नहीं जानते थे कि जातिप्रथा ने मज़दूर और सर्वहारा के एक वर्ग को दबाकर रखा था? क्या मज़दूरों के एक वर्ग को दबाकर मज़दूर-एकता क़ायम की जा सकती है? यदि नहीं, तो पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति कैसे संभव है? आंबेडकर का स्पष्ट कहना था कि मज़दूरों को एक श्रेणी में संगठित करने के लिए उनमें मौजूद ब्राह्मणवाद को पहले नष्ट करना होगा।[23]
लेकिन भगत सिंह अपने मत की पुष्टि रूस का उदाहरण देकर करते हैं। यथा–
“जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं, उन्हें मालूम है कि ज़ार के समय वहां भी ऐसी ही स्थितियां थीं, वहां भी कितने ही समुदाय थे, जो परस्पर जूत-पतांग करते रहते थे। लेकिन जिस दिन से वहां श्रमिक शासन हुआ है, वहां नक्शा ही बदल गया है। अब वहां कभी दंगे नहीं हुए। अब वहां सभी को इंसान समझा जाता है, ‘धर्मजन’ नहीं। ज़ार के समय लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही ख़राब थी, इसलिए सब दंगे-फसाद होते थे। लेकिन अब रूसियों की आर्थिक दशा सुधर गई है और उनमें वर्ग-चेतना आ गई है, इसलिए अब वहां किसी दंगे की ख़बर नहीं आई।”[24]
अकेले भगत सिंह ही नहीं, सभी मार्क्सवादी रूस की क्रांति के गुण गाते हैं, और भारत में उसे लागू करने का सपना देखते हैं, जो कभी संभव ही नहीं है। एक क्लासिक मार्क्सवादी की तरह भगत सिंह भी भारतीय संदर्भ से या तो कटे हुए थे, या उसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि रूस में वर्णव्यवस्था नहीं थी, वहां के लोग अपनी ग़रीबी को ईश्वर या भाग्य का लेखा या पूर्वजन्म का फल नहीं मानते थे। लेकिन भारत के ग़रीब और मज़दूर वर्ग के दिमाग़ों में ब्राह्मणों द्वारा भाग्य और पूर्वजन्म का कर्म-फल भरा हुआ है। वे इसी के लकीर के फ़क़ीर बने रहें, इसलिए उन्हें अनपढ़ बनाकर रखा गया। यही नहीं, उनमें जाति के आधार पर ऊंच-नीच के सोपान भी खड़े किए गए। क्या ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए इस सामाजिक ढांचे में सर्वहारा समाज में वर्ग-चेतना आ सकती है? जिन आर्थिक सुधारों से समाज में समानता आती हो, क्या ब्राह्मण शासक वर्ग ऐसे सुधारों को पसंद करेगा? ब्राह्मणवाद से लड़े बिना सिर्फ आर्थिक क्रांति का सपना देखा जा सकता है, जैसे भगत सिंह ने देखा, और जैसे आज के बहुत से मार्क्सवादी देख रहे हैं। और सपना कभी हकीक़त नहीं बनता। जब तक ब्राह्मणवाद के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी जाएगी, इस देश में न सामाजिक सुधार हो सकता है और न आर्थिक सुधार।
संदर्भ ग्रंथ :
[1] सत्यम, भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज़, राहुल फाउंडेशन, लखनऊ, संस्करण 2014, पृष्ठ 257; डा. जगमोहन सिंह एवं डा. चमन लाल, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज़, राजकमल पेपरबैक्स, नई दिल्ली, संस्करण 1991, पृष्ठ 217
[2] डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 1, 1989, देखिए, एविडेंस बिफोर दि साउथबरो कमेटी, पृष्ठ 249-250
[3] वही, पृष्ठ 275
[4] वही, देखिए, कम्युनल डेडलॉक एंड ए वे टू सोल्व इट, पृष्ठ 376-377
[5] वही, पृष्ठ 377
[6] पैट्रिक मैकगिन, कम्युनिलज्म एंड दि नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस : दि कोहाट रायट्स, 9-10 सितंबर 1924, साउथ एशिया रिसर्च, वाल्यूम 6, पृष्ठ 139-158
[7] यह लाला हरदयाल अगर वही थे, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो दुर्भाग्यपूर्ण है।
[8] डा. बाबासाहेब आंबेडकर : राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 8, पृष्ठ 129
[9] सत्यम, उपरोक्त, पृष्ठ 257
[10] वही, पृष्ठ 257-258
[11] वही, पृष्ठ 258
[12] डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 1, देखिए, एनिहिलेशन ऑफ़ कास्ट, पृष्ठ 45
[13] सत्यम, उपरोक्त, पृष्ठ 260
[14] वही, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, पृष्ठ 249
[15] वही, नौजवान भारत सभा और राष्ट्रीय नेतृत्व का मूल्यांकन, पृष्ठ 321-322
[16] वही, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज़, पृष्ठ 258-259
[17] वही, पृष्ठ 259
[18] वही, पृष्ठ 259
[19] डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 1, पृष्ठ 45
[20] वही, पृष्ठ 46
[21] सत्यम, उपरोक्त, पृष्ठ 259
[22] डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 17, पार्ट 3, पृष्ठ 179
[23] वही।
[24] सत्यम, उपरोक्त, पृष्ठ 259