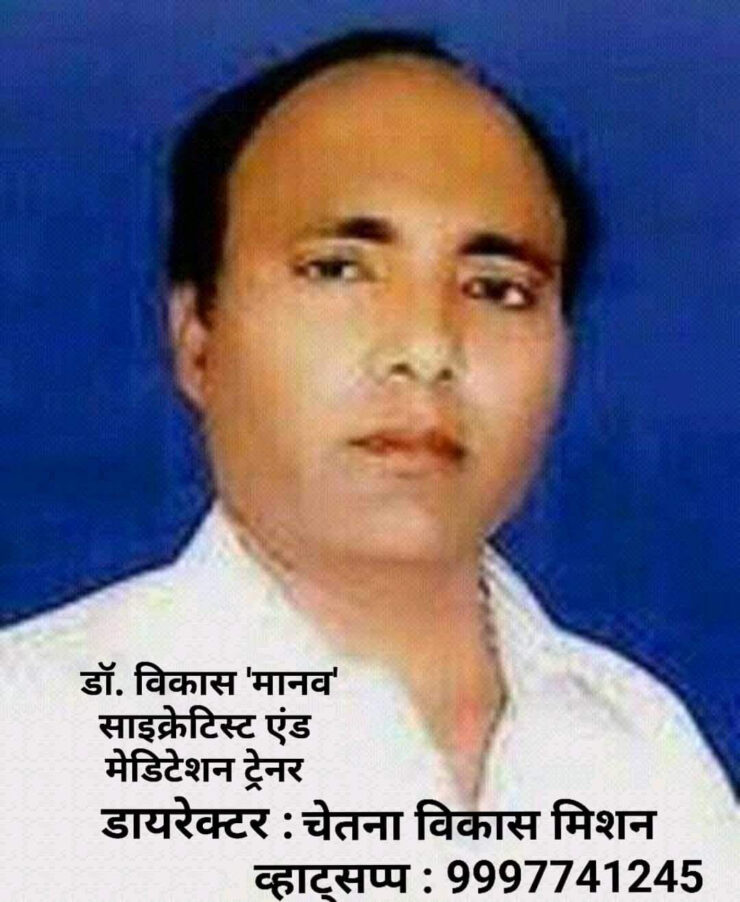डॉ. विकास मानव
वैदिक ग्रन्थों में परमात्मा और जीवात्मा को प्रायः ’आत्मा’ शब्द से ही कहा जाता है। दर्शन शास्त्रों, उपनिषदों, आदि, में यही प्रथा पाई जाती है। इससे अनेक बार संशय हो जाता है कि यहां परमात्मा विषय है अथवा जीवात्मा अथवा दोनों।
इन दोनों के गुण भी कुछ-कुछ मिलते हैं। इसलिए यह सन्देह और भी प्रगाढ़ हो जाता है। तब हम अपने ज्ञानानुसार पहला या दूसरा अर्थ कर देते हैं। फिर हम पाते हैं कि कई बार एक श्लोक/वचन एक की चर्चा कर रहा है, परन्तु अगला दूसरे की, और फिर तीसरा पहले की।
इस प्रकार प्रसंग थोड़ा अटपटा हो जाता है। इस लेख में मैंने ऐसा एक शब्द दर्शाया है जो कि दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होता है, परन्तु हम उसे एक ही अर्थ में लेने का आग्रह करते हैं।
प्रायः जहां भी ’ब्रह्म’ शब्द आता है, विशेषकर उपनिषदों में, हम बिना सोचे उसका एक ही अर्थ कर देते हैं – परमात्मा।
यह जीवात्मापरक भी हो सकता है, यह सोच हमारे मानसपटल पर आती ही नहीं। प्रायः सभी उपनिषद् के व्याख्याकारों ने भी इसी प्रकार अर्थ किए हैं। परन्तु इसमें कई बार कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सन्दर्भ में वह अर्थ सम्यक् नहीं बैठता। फिर भी, दूसरा अर्थ सोचने में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण, हम कठिनाई को किसी प्रकार अनदेखी करके आगे बढ़ जाते हैं।
विरले ही व्याख्याकार हैं जिन्होंने ’ब्रह्म’ का अर्थ जीवात्मा किया हो। उनमें से एक हैं विद्यामार्तण्ड डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, जिन्होंने ११ उपनिषदों का भाष्य किया है। आगे हम कुछ ऐसे स्थल देखते हैं जहां ब्रह्म के अर्थ जीवात्मा करने पर सारी गांठें खुल जाती हैं।
जबकि इस विषय में सन्देह मुझे अनेक बार हुआ, परन्तु बृहदारण्यकोपनिषत् में इसे स्पष्टतर रूप से कहा गया है। पहले हम उसी के कुछ उदाहरण देखते हैं।
इनमें प्रथम देखिए :
स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्यदेतदिदम्मयोऽदोमय इति। यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति। पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते॥
~बृहदारण्य उपनिषत् (४।४।५ )
अर्थात् निश्चय ही, वह यह आत्मा ब्रह्म है, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथिवीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय, सर्वमय, इस लोक से सम्बद्ध और उस लोक से सम्बद्ध है।
जैसा करता है, जैसा आचरण करता है, वैसा ही हो जाता है – जो भला करता है, तो भला हो जाता है, जो पाप करता है, तो पापी हो जाता है ; पुण्य कर्मों से उसका पुण्य होता है, पाप से पाप होता है।
इसलिए कहा गया है कि पुरुष काममय है। जैसी उसकी कामना होती है, वैसी उसकी कर्म की चेष्टा, संकल्प होता है; जैसा संकल्प होता है, वैसा कर्म करता है; जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है।
यह वर्णन स्पष्टतः जीवात्मा के विषय में है। इसलिए कोई भी व्याख्याकार यहां पर ’परमात्मा’ अर्थ नहीं कर सका। तथापि आरम्भ में ही उसको ’ब्रह्म’ कहा गया है। ब्रह्म को जीवात्मा न मानने के कारण, अधिकतर व्याख्याकारों ने यहां अर्थ किया है ’ब्रह्मवेत्ता’, परमात्मा को जानने वाला।
परन्तु आगे के वर्णन में तो सामान्य जीवात्मा की बात हुई है, जो पाप भी करती है और पुण्य भी, जबकि ब्रह्म को जानने वाला तो जीवन्मुक्त आत्मा होती है, मोक्ष की भागी होती है। यहां पर सत्यव्रत जी ने ब्रह्म का अर्थ किया है – बड़ा, सर्वश्रेष्ठ – और फिर क्योंकि ये विशेषण पुनः जीवन्मुक्त के लिए ही होते हैं.
तथापि मुख्य व्याख्या में उन्होंने जीवात्मा को ’आत्म-ब्रह्म’ के नाम से पुकारा है। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि “प्रकृति की तुलना में, जीवात्मा परमात्मा से अधिक निकट होता है.”
तदेष श्लोको भवति। तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य। प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्। तस्माल्लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामायमानोऽथाकामायमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति॥
~बृहदारण्यकोपनिषत् (४।४।६)
अर्थात् – उपर्युक्त विषय में किसी अन्य ऋषि का प्रमाण है – जहां भी उसका सूक्ष्म मन आसक्त होता है, उस में ही वह (आत्मा) कर्म के साथ लग जाता है। उस कर्म का अन्त (फल) पाता हुआ, वह जो कुछ इस लोक में करता है, वह उस कर्म को भोगने के लिए पुनः उस लोक से आता है (लौटता है)। यह है कामना करने वाले की गति।
अब कामना न करने वाले की गति कहते हैं। जो बिना कामना के होता है, निष्काम होता है, जिसके सभी काम पूर्ण हो गए होते हैं, जो आत्मा को प्राप्त करने की कामना करता है, उसके प्राण निकलते नहीं हैं (वह जीवन्मुक्त हो जाता है)। वह ब्रह्म होकर, ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है।
यहां यदि हम “ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति” में ’ब्रह्म’ को दोनों स्थानों पर परमात्म-अर्थक मानेंगे, तो शांकर अद्वैतवाद में फंस जायेंगे. इसलिए पहले ब्रह्म को जीवात्मा और दूसरे को परमात्मा मानना ही अर्थ-संगत है। ऐसा न मान सकने पर, अधिकतर भाष्यकारों ने पहले ’ब्रह्म’ का अर्थ पुनः ’ब्रह्मवेत्ता’ अथवा ’ब्रह्म में लीन’ किया है।
परन्तु उपनिषत्कार ’ब्रह्मवित्त’ शब्द से परिचित थे। सो, यहां ’ब्रह्म हो गया’ कहने से कुछ विशेष अर्थ तो नहीं हैं? कुछ और उद्धरण देखकर, इसपर चर्चा करेंगे।
“तदेष श्लोको भवति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति। तद्यथाहिनिर्ल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदँ शरीरँ शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव॥
~बृहदारण्यकोपनिषत् (४।४।६)
अर्थात् – यहां एक और प्रमाण है – जब हमारे मन में स्थित सभी काम छूट जाते हैं, तब मर्त्य (मनुष्य) अमृत हो जाता है। यहां (इस शरीर में ही) ब्रह्म को पा लेता है। जिस प्रकार सांप की निर्जीव केंचुली दीमक की बांबी पर फेंकी हुई पड़ी होती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा होता है (जीवन्मुक्त आत्मा का) और यह (जीवन्मुक्त आत्मा) अशरीरी हो जाता है, अमृत, प्राण और ब्रह्म ही हो जाता है, तेज-स्वरूप ही हो जाता है।
इसी प्रकार अन्य प्रकरण भी इसी उपनिषद् में पाए जाते हैं, जहां ब्रह्म के परमात्मा को छोड़कर अन्य भी अर्थ हैं। इनमें से कुछ मैं नीचे दे रहा हूं :
वाग्वै सम्राट परमं ब्रह्॥
~बृहदारण्यकोपनिषत् (४।१।२)
याज्ञवल्क्य जनक से कहते हैं :
निश्चय ही सम्राट ! वाणी परम ब्रह्म है। इसी विभाग में आगे की कण्डिकाओं में याज्ञवल्क्य उपर्युक्त प्रकार से क्रमशः प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और हृदय को भी ब्रह्म कहते हैं। सभी स्थानों में ब्रह्म का अर्थ ’महान्’ वा ’अतिश्रेष्ठ’ है, परमात्मा नहीं।
एवं हैवंविदँ सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातीदमागच्छतीति॥
~बृहदारण्यकोपनिषत् (४।३।३७)
इसी प्रकार, निश्चय से, इस प्रकार से (ब्रह्म को) जानने वाले को सब प्राणी कहते हैं, “यह ब्रह्म आ रहा है, यह जा रहा है।”
“स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेद॥”
~बृहदारण्यकोपनिषत् (४।४।२५ )
वह महान् अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत, अभय और ब्रह्म है। ब्रह्म अभय है। निश्चय ही जो ऐसे जानता है, वह भी ब्रह्म हो जाता है। यहां ब्रह्म-पद जीवात्मापरक है।
अन्य भी उदाहरण इस और अन्य उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। यहां मैंने कुछ अति स्पष्ट उद्धरण दे दिए हैं। अब इनपर चर्चा करते हैं।
’ब्रह्म’ शब्द ’बृहि वृद्धौ’ धातु से “बृंहतेर्नोऽच्च (उणादि० ४।१४६)” से मनिन् प्रत्यय लगाकर सिद्ध होता है, जिसकी व्याख्या में महर्षि दयानन्द लिखते हैं – बृंहति वर्धते तत् ब्रह्म ईश्वरो वेदस्तत्त्वं तपो वा – अर्थात् जो बड़ा हो, बढ़ता हो, इसलिए ईश्वर, वेद, तत्त्व और तप के इसके अर्थ होते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि जितने अर्थ शास्त्रों में दिए हैं, उससे अधिक भी अर्थ शब्दों के पाए जाते हैं। ब्रह्म भी ऐसा एक शब्द है।
उपर्युक्त बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में जो वाक् आदि को ब्रह्म उपाधि दी गई है, वह स्पष्टतया उनके महत्त्व के कारण है। तब यही अर्थ जीवात्मा के लिए लेने में क्या संकोच है ?
वस्तुतः, प्रकृति की तुलना में जीवात्मा इतना महान् है, कि यदि हम प्राकृतिक प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और हृदय को ब्रह्म कह सकते हैं, तो जीवात्मा तो कहीं अधिक बड़ा, महान् व शक्तिशाली है। इसी कारण से जीवात्मा का ब्रह्म अभिधेय उपयुक्त है। परन्तु प्रकृति के योग में वह प्रकृति की शक्तियों से बन्ध जाता है; उसके स्वयं क सामर्थ्य सीमित अथवा ढक जाते हैं।
इसको समझने के लिए एक केंचुए को देखिए – उसकी न तो आंखें हैं, न नाक, न कान। तो इस शरीर में आत्मा की कई शक्तियां आच्छादित हो गई हैं।
इसी प्रकार मनुष्य शरीर में भी, जो कि अन्य जातियों के शरीरों से कहीं अधिक सामर्थ्यवान् है, आत्मा की अनेकों शक्तियां दबी हुई हैं। जब वह इस प्राकृतिक बन्धन से छुटकारा पाता है, तब वह ’ब्रह्म’ हो जाता है, अपनी पूर्ण महानता को प्राप्त करता है। इस स्थिति में वह परमात्मा को देखने में भी समर्थ हो जाता है। उपनिषद् का वाक्य – ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति – ब्रह्म हो कर ब्रह्म को पा लेता है – इसी बात को पुनः पुनः हमें समझाने का प्रयत्न कर रहा है!
इसमें संशय न करते हुए, प्रकरणानुसार जीवात्मा का ग्रहण करके सही अर्थ करने चाहिए। अर्थ कैसे विकृत हो जाते हैं, उसके लिए निम्न उदाहरण है। बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में जीवात्मा वर्णित है। परन्तु चौदहवीं कण्डिका से ब्रह्म का ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रसंग में यह वचन आता है :
“स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसम्भेदाय॥”
~बृहदारण्यकोपनिषत् (४।४।२२)
अर्थात् – निश्चय ही, वह यह महान् व अजन्मा आत्मा जो कि विज्ञानमय, प्राणों में विराजमान है, जो हृदय (बुद्धि) के अन्दर के आकाश में स्थित है, जो सबको वश में करने वाला है, सबका ईश्वर है, सबका अधिपति है, वह साधु (अच्छे = पुण्यात्मक) कर्म से बड़ा नहीं होता, और असाधु (नीच = पापात्मक) कर्म से छोटा नहीं होता ; वह सर्वेश्वर है, भूतों का अधिपति है, भूतों का पालन करने वाला है, यह लोकों को छिन्न-भिन्न न होने देने के लिए सेतु और विशेष धारण करने वाला है।
यहां सभी विशेषण परमात्मा पर ही घटते हैं, परन्तु एक बात अटपटी लगती है – वह अच्छे कर्म से बड़ा नहीं होता और बुरे से छोटा नहीं होता – परमात्मा क्या कभी बुरा कर्म कर सकता है कि याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा. नहीं, यह प्रकरण जीवात्मा के विषय में ही यहां पर भी प्रवर्तित हो रहा है। तब फिर हम अन्य विशेषणों को कैसे समझें ? सो, जीवात्मा के प्रसंग में अर्थ इस प्रकार है – वह यह महान् अजन्मा आत्मा शरीर के प्राणों में विज्ञान (चैतन्य, consciousness) उत्पन्न करता है। वह मस्तिष्क के अन्दर एक छोटे प्रदेश में आश्रय लेता है। वह सम्पूर्ण शरीर को वश में रखता है, उसके ऊपर ईषण करता है, उसका अधिपति है (भूतों से केवल शरीरस्थ भूत उद्दिष्ट हैं, ब्रह्माण्ड-भर के नहीं)।
वह अच्छे कर्म या बुरे कर्म से प्रभावित नहीं होता (सुख-दुःख केवल शरीर तक सीमित होते हैं, आत्मा को नहीं छूते)। शरीर में स्थित सभी भूतों – प्राकृतिक तत्त्वों – का ईश्वर, अधिपति, पालने हारा है। वह शरीर में स्थित भौतिक लोकों = अवयव, जैसे फेफड़े, आमाशय, को छिन्न-भिन्न नहीं होने के लिए, सेतु का काम करता है और विशेष रूप से शरीर को धारण करता है (इसीलिए तो मृत्यु होने पर, जीवात्मा के शरीर त्याग देने पर, शरीर सड़ने लगता है)।
इस प्रकार अनेकों विशेषणों के हमको प्रसंगानुसार अर्थ करने पड़े, जो विशेषण प्रथमदृष्टया परमात्मा के लगते हैं। यही मेरे उपर्युक्त कथन का अर्थ था कि परमात्मा और जीवात्मा में ’आत्मा’ शब्द ही नहीं, अपितु अनेकों समानताएं हैं। जहां परमात्मा सम्पूर्ण विश्व को धारण करता है, वहीं जीवात्मा अपने शरीर को धारण करता है। जहां परमात्मा ब्रह्माण्ड में परिणाम लाता है, वहीं जीव अपने आसपास के भूतों को अपने अनुसार बदलने में समर्थ होता है।
जीव को इतना छोटा भी नहीं समझना चाहिए, जैसे कि वह स्वयं कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता। परमात्मा ने उसमें अनेकों सामर्थ्य स्थापित किए हैं, जिनका प्रयोग करना जीवन को सफल करना है, और निष्कर्मण्यता में बिता देना, जीवन को व्यर्थ बिताना है।
प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ते, समझते हुए, हमें बहुत चिन्तन करके अर्थ करना चाहिए। इतनी सदियां हमारे और उनके बीच में हैं कि बहुत अर्थ बदल गए हैं।
ब्रह्म शब्द ही नहीं, आत्मा, भूत, योग, आदि, कितने ही शब्द हैं, जो बहुत विस्तृत अर्थ वाले हुआ करते थे, परन्तु आज बहुत संकीर्ण हो गए हैं। यदि हमें पुरातन ग्रन्थों से सही ज्ञान प्राप्त करना है, केवल अपने जाने हुए को आरोपित नहीं करना है, तो हमें फूंक-फूक कर ही अर्थ करना पड़ेगा।