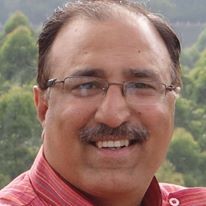ईश मिश्रा
आज के हालात में जब दुनिया भर में राष्ट्रोनमादी, दक्षिणपंथी ताकतों की मुखरता आक्रामक है; भारत पर सांप्रदायिक फासीवाद के बादल मंडरा ही नहीं रहे हैं, किस्तों में बरस भी रहे हैं; प्रतिरोध की ताकतें खंडित-विखंडित हैं; जनपक्षीय ताकतें सैद्धांतिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही हैं; दलित-आदिवासियों के हिमायतियों को अर्बन नक्सल बताकर हास्यास्पद आरोप लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति (वर्ण)-वर्ग के अंतःसंबंधों पर व्यापक विमर्श जरूरी है। मैंने इस बात को कई जगह रेखांकित किया है कि शासक जातियां ही आर्थिक तथा बौद्धिक संसाधनों पर नियंत्रण के चलते शासक वर्ग भी रहे हैं। वर्ग समाजों में जिस वर्ग का आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है, सांसकृतिक-बौद्धिक संसाधनों पर भी उसी का नियंत्रण होता है। शासक वर्ग के विचार ही युग चेतना का निर्माण करते हैं। इस लेख का मकसद, डॉ. अंबेडकर की कालजयी कृति जाति का विनाश के संदर्भ में क्रांति के लिए जाति का विनाश और जाति विनाश के लिए क्रांति की अवधारणा यानि, जय भीम-लाल सलाम नारे के निहितार्थ पर जारी विमर्श को आगे बढ़ाना है।
“भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मसला है, जिससे किसी भी सामाजवादी को निपटना ही पड़ेगा। जब तक वह ऐसा नहीं करता, वह क्रांति के अपने लक्ष्य को उपलब्ध नहीं कर सकता और खुशकिस्मती से यदि वह क्रांति करने में सफल हो जाता है, उसके लिए उसे सामाजिक व्यवस्था से मोर्चा लेना ही होगा। यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिस पर मेरे विचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी अगर क्रांति के पहले ध्यान नहीं देता, तो क्रांति के बाद उसे ऐसा करना ही होगा। यह इस बात को दूसरी तरह से कहना है कि आप किसी ओर भी मुंह कीजिए, जाति एक ऐसा राक्षस है, जो आपका रास्ता रोकेगा ही नहीं बल्कि काटेगा भी। जब तक आप इस राक्षस का वध नहीं करते, आप न तो राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और न ही आर्थिक सुधार”।
‘जाति का विनाश: प्रसिद्ध भाषण, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर को देने नहीं दिया गया’, के लंबे उद्धरण से लेख शुरू करने का मकसद सामाजिक चेतना के जनवादीकरण (वर्गचेतना के प्रसार) में अपेक्षित ब्राह्मणवादी अवरोध को नहीं, मार्क्सवादी और अंबेडकरवादी तत्ववादियों को संबोधित करना है, जो अंबेडकर के विचारों और मार्क्सवाद में अंतर्निहित असाध्य अंतरविरोधों का अन्वेषण करते हैं। अंबेडकर का मकसद जातिवाद का विनाश था, प्रतिस्पर्धी जातिवाद नहीं। मार्क्सवाद को वैचारिक श्रोत मानने वाली भारत की कम्युनिस्ट पार्टी/पार्टियों ने मार्क्सवाद को समाज की खास परिस्थियों को समझने के विज्ञान और वर्ग-संगर्ष की क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में अपनाने की बजाय, नजीर के रूप में अपना लिया। अंबेडकरवाद को अपना वैचारिक श्रोत मानने वाले कई अस्मितावादी समूह जवाबी जातिवाद को अपनी राजनीति का आधार मानते हैं तथा सामाजिक चेतना के जनवादीकरण के रास्ते में वर्णाश्रमी जातिवाद (ब्राह्मणवाद) के पूरक जातिवाद (नवब्राह्मणवाद) के रूप में सहयोगी गतिरोधक बन गए हैं।
असमानता की समस्या का समाधान जवाबी असमानता नहीं बल्कि समानता है, उसी तरह जातिवाद का समाधान जवाबी जातिवाद नहीं है, जाति-व्यवस्था का विनाश है। ब्राह्मणवाद का मूलमंत्र है: कर्म और विचार से स्वअर्जित, विवेक सम्मत अस्मिता की प्रवृत्तियों के बजाय जन्म की जीववैज्ञानिक अस्मिता की रूढ़िगत प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन। ऐसा करने वाले जन्मना अब्राह्मण ब्राह्मणवाद को पराजित करने के बजाय उसे मजबूत करते हैं तथा वस्तुतः नवब्राह्मणवादी हैं। मेरे विचार से जाति का विनाश भारतीय समाज की एक वैज्ञानिक समीक्षा है तथा मार्क्सवाद समाज की व्याख्या का एक गतिशील विज्ञान।
समाजवाद पर केंद्रित इसके खंड 3 और 4 (पृ. 51-60) में भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन की आलोचना के सार तथा मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांतों यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद की मूलभूत अवधारणाओं में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। एंगेल्स ने 1891 में कुछ तत्ववादी मार्क्सवादियों को लक्षित कर लिखा था कि मार्क्सवादी वह नहीं जो मार्क्स या उनके कामों का उद्धरण देता फिरे बल्कि खास परिस्थियों में वैसी प्रतिक्रिया दे जैसा मार्क्स देते। मार्क्स और एंगेल्स ने उत्पादन पद्धति के आधार पर ऐतिहासिक कालखंडों की विवेचना में बार-बार भौतिक विकास के चरणों की विषमता और तरीकों की विविधता रेखांकित किया है।
3 खंडों में मार्क्स की कालजयी रचना पूंजी यूरोप में विकसित हो रहे पूंजीवाद के राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा है, जहां नवजागरण तथा प्रबोधन (एनलाइटेनमेंट), क्रमशः सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्रांतियों ने सामाजिक विभाजन के जन्मगत आधार को समाप्त कर प्रमुखतः आर्थिक आधार में बदल दिया था। तभी तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा कि पूंजीवाद ने समाज को दो विरोधी, पूंजीपति और सर्वहारा खेमों में बांटकर वर्गीय अंतर्विरोध को सरल बना दिया। बारूद के अन्वेषण ने युद्ध-संबंधी मामलों में कुलीन वर्ग (नोबिलिटी) का एकाधिकार खत्म कर दिया तथा छापाखाना (प्रिंटिंग प्रेस) ने ग्रंथों पर पुजारी वर्ग का, लेकिन प्रतिष्ठा ने नए मानदंड स्थापित कर दिया, आर्थिक मानदंड।
नवजागरण इतिहास के नायकों की एक नई प्रजाति के उदय का भी गवाह रहा है, वित्तीय नायक। नवजागरण काल में पैदी का यह नायक अगले डेढ़ सौ सालों में परिधि से चलकर केंद्र में स्थापित हो गया। समाज विभाजन तथा वर्गीय अंतर्विरोध का मुख्य आधार आर्थिक बन गया। भारत में कबीर के साथ शुरू हुआ नवजागरण ऐतिहासिक कारणों से अपनी तार्किक परिणति को नहीं प्राप्त कर सका। औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने भारत में पूंजीवाद के स्वतंत्र, स्वाभाविक विकास और संभावित प्रबोधन सी बौद्धिक-सामाजिक क्रांति की संभावनाओं को समाप्त कर दिया।
मार्क्स को उम्मीद थी कि औपनिवेशिक शासन भारत में पूंजीवादी विकास के लिए, वर्णाश्रमी, एसियाटिक उत्पादन प्रणाली को समाप्त करेगा, जो अपनिवेशवाद का एक अनचाहा सकारात्मक उपपरिणाम होता, लेकिन मार्क्स ज्योतिषी तो थे नहीं, न ही भविष्यवाणियों से इतिहास के गतिविज्ञान के नियम निर्धारित होते हैं। औपनिवेशिक शासकों ने यहां पूंजीवाद की स्थापना के लिए एसियाटिक मोड को समाप्त करने के बजाय इंगलैंड में पूंजीवीद को और विकसित करने तथा औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार के लिए उसकी विसंगतियों का इस्तेमाल औपनिवेशिक लूट में किया। इसलिए भारत में पिरामिडाकार, वर्णाश्रमी जाति व्यवस्था के रूप जन्मगत सामाजिक विभाजन किसी सामाजिक क्रांति के अभाव में न सिर्फ कायम है, बल्कि चुनावी राजनीति में और जटिल हो गया है। 1885 में राजनीतिक आंदोलन के मंच के रूप में कांग्रेस की स्थापना के साथ उसके पूरक के रूप में सामाजिक आंदोलन के मंच के रूप में नेशनल सोशल कांफ्रेंस की भी स्थापना हुई।
“एक समय यह माना जाता था कि सामाजिक कार्यकुशलता के बिना सक्रियता के अन्य सभी क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। कुरीतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्यकुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस तथ्य की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ही ‘नेशनल कांग्रेस’ के जन्म के साथ ही ‘सोशल कांफ्रेस’ (समाज सुधार सम्मेलन) की नींव रखी गयी। …….कुछ समय तक कांग्रेस और कांफ्रेस एक ही साझा कर्म के दो डैनों की तरह काम करते रहे और उनका वार्षिक अधिवेशन एक ही पंडाल में होता रहा”। यह दौर राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुधार के पारस्परिक सहयोग और उनकी अनुपूरक भूमिका का दौर था, लेकिन यह पारस्परिक सहयोग जल्द ही पारस्परिक विरोध में बदल गया।
“जिस उदारता से कांग्रेस, सोशल कांफ्रेंस को अपने पंडाल का इस्तेमाल करने देती थी, वह स्वर्गीय तिलक के नेतृत्व में होने वाले प्रयासों के फलस्वरूप वापस ले ली गयी। पारस्परिक शत्रुता की भावना इतनी तीव्र हो गयी कि जब सोशल कांफ्रेंस ने अपना अलग पंडाल लगाना चाहा तो विरोधियों ने उसे जलाने की धमकी दी। इस तरह थोड़े ही समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी विजयी हुई और सोशल कांफ्रेंस गायब होते-होते विस्मृति का शिकार हो गयी”। वैसे भी सोशल कांफ्रेंस हिंदुओं में व्याप्त कुरीतियों को लेकर थी जाति तोड़ने के लिए नहीं। ऐतिहासिक साक्ष्यों से अंबेडकर बहुत तार्किक ढंग से राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार, यानी जातिवाद के अंत की अनिवार्यता साबित करते हैं।
कहने का मतलब यह कि यूरोप में प्रबोधन काल में बुर्जुआ (पूंजीवादी) जनतांत्रिक क्रांति सी कोई परिघटना यहां उन्नीसवीं सदी के अंत तक शुरू ही नहीं हुई। नेतृत्व में सवर्ण वर्चस्व के चलते राष्ट्रीय आंदोलन की समाज सुधार में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि तिलक जैसे कई दक्षिणपंथी नेता तो इसके प्रखर, मुखर विरोधी थे। मार्क्स ने विकास के चरण की महत्ता को रेखांकित किया है, यद्यपि क्रांतिकारी परिस्थितियों के चलते रूस में बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रांति अल्पजीवी रही। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखें तो अपूर्ण बुर्जुआ सामाजिक क्रांति की जिम्मेदारी भी कम्युनिस्ट आंदोलन की थी। रूसी क्रांति के प्रभाव में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के समय के विश्व-पंजीवाद के विकास के स्तर और औपनिवेशिक परिस्थियों के संदर्भ में, समाजवादी आंदोलन से पहले जाकर अतीत की जिम्मेदारी नहीं पूरी की जा सकती। अतीत से विरासत में मिली तत्कालीन परिस्थियों के तहत दोनों के संगम की जरूरत थी; मार्क्सवाद के सिद्धांतों को उस समय के वस्तुनिष्ठ यथार्थ में अनूदित करने की जरूरत थी।
कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा समाजवादी आंदोलन और जाति विरोधी आंदोलन में द्वंद्वात्म एकता स्थापित करना होना चाहिए था। अंबेडकर ने सही कहा है कि ऊंच-नीच जातियों में बंटे सर्वहारा की एकता और एकजुटता मुश्किल है। जातिविरोधी और समाजवादी आंदोलनों की एकजुटता तथा आंदोलनों में सामूहिक भागीदारी, सामाजिक चेतना के जनवादीकरण यानी मजदूरों में जातिवादी मिथ्या चेतना से मुक्ति और वर्ग चेतना के संचार का पथ प्रशस्त करती। मार्क्स ने दर्शन की गरीबी में लिखा है कि सर्वहारा अपनी मुक्ति की लड़ाई खुद लड़ेगा, लेकिन वर्ग चेतना से लैस, साझे वर्ग हित के आधार पर संगठित होकर ही इसके लिए समर्थ होगा, और सर्वहारा अपने को राजनीतिक पार्टी के रूप में ही समगठित कर सकता है।
भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन ने मार्क्सवाद को समाज को समझने और बदलने के उपादान के रूप में न अपनाकर मॉडल के रूप में अपनाया। मार्क्स ने यूरोप में 1848-51 की क्रांति-प्रतिक्रांतियों की हलचल के बाद एटींथ ब्रुमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में लिखा, “मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाता है, लेकिन जैसा चाहे वैसा नहीं, न ही अपनी चुनी हुई परिस्थितियों में, बल्कि अतीत की विरासत के रूप में मिली मौजूदा परिस्थितियों में। पूर्वजों के पीढ़ियों की लाशों के बोझ के रूप में, परंपराएं जिंदा कौमों के दिमाग पर दुःस्वप्न की तरह सवार रहती हैं।” इसलिए समाजवादी आंदोलन के लिए इस दुःस्प्न के भार को उतार फेंकने की जरूरत है।
जातिवाद हमारी पुरातन पड़ चुकी परंपराओं का प्रमुख अवयव है। घोषणा-पत्र में मार्क्स और एंगेल्स लिखते हैं, “हम पाते हैं कि पहले के युगों में लगभग हर जगह बहुत जटिल सामाजिक व्यवस्था थी, मध्ययुग में सामंती जमींदार; जागीरदार; गिल्ड मास्टर; नौकर-चाकर; कारीगर; सर्फ (किसान); और इनमें भी मातहती की तमाम श्रेणियां”। भारत में जाति-आधारित मातहती की तमाम श्रेणियों वाली पूर्व-आधुनिक जटिल जाति व्यवस्था के विनाश की दिशा में अंबेडकर के पहले, कोई संगठित प्रयास नहीं हुआ। जातिवाद विघटित होने के बजाय प्रतिक्रियावादी रूप में सुगठित हो गया।
कम्युनिस्ट आंदोलन के नेताओं को लगा कि समाजवाद में जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने-आप कुछ नहीं होता। वैसे ऐसा होता तो वैसा होता, किस्म का विमर्श निरर्थक होता है। वैसे भी जब आप इतिहास रच रहे होते हैं तब अलग बात होती है और जब पढ़ रहे होते हैं तब अलग, लेकिन बौद्धिक अनुमानों में क्या जाता है। यदि कम्युनिस्ट आंदोलन का एजेंडा सामाजिक और समाजवादी क्रांति का संतुलित युग्म होता तो शायद अंबेडकर भी उससे जुड़कर नेतृत्व प्रदान करते और सर्वहारा आंदोलन का स्वरूप अलग होता। जयभीम-लाल सलाम नारे को जेएनयू आंदोलन तक इंतजार न करना होता। शासक जातियां ही शासक वर्ग भी रही हैं।
1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सम्मेलन में डॉ. अंबेडकर ने कम्युनिस्ट नेताओं को आमंत्रित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि भारत में राजनीतिक रूप से कम्युनिस्ट उनके ज्यादा करीब थे। 1991 में छपी विमल मून की किताब बाबा साहब अंबेडकर में बीबीसी के हवाले से बताया गया है कि 1956 एक संदेश में उन्होंने कहा था, “आगामी पीढ़ी को बुद्ध और कार्ल मार्क्स-इनमें से किसी एक का चुनाव करना है।”
जाति का विनाश में डॉ. अंबेडकर समाजवादी आंदोलन की समीक्षा में लिखते हैं, “भारत के समाजवादी, यूरोप के अपने साथियों का अनुकरण करते हुए भारत के तथ्यों पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या लागू करना चाह रहे हैं। वे प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसकी गतिविधियां और आकाक्षाएं आर्थिक तथ्यों से बंधी हैं…। वे शिक्षा देते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार एक विराट भ्रम है और किसी अन्य सुधार के पहले जरूरी है कि संपत्ति की बराबरी लाकर आर्थिक सुधार लाया जाए”। मार्क्स की एक प्रमुख स्थापना है, अर्थ ही मूल है। लेकिन वे मूल की हिफाजत में सांस्कृतिक, बौद्धिक आदि संरचनाओं की महत्ता को कमतर नहीं आंकते। ग्राम्सी ने अपने वर्चस्व के सिद्धांत में इसकी विधिवत व्याख्या की है।
जर्मन विचारधारा में मार्क्स और एंगेल्स लिखते हैं, “शासक वर्ग का विचार ही शासक विचार भी है। जिस वर्ग का आर्थिक संसाधनों पर अधिकार होता है, बौद्धिक संसाधनों पर भी उसी का अधिकार होता है। पूंजीवाद सिर्फ माल का ही उत्पादन नहीं करता, विचारों का भी उत्पादन करता है”। जिसे वे युग का विचार कहते हैं, जो सामाजिक चेतना के चरित्र और स्वरूप के निर्धारण में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बौद्ध क्रांति के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति के बाद, शिक्षा पर एकाधिकार के चलते ब्राह्मणवादी युग चेतना या विचारधारा का वर्चस्व सदियों बना रहा। विचारधारा, मिथ्या चेतना होती है जो शासक और शोषित को एक सा प्रभावित करती हैं। अंग्रेजी शिक्षा नीति के अनचाहे सकारात्मक उपपरिणाम के रूप में शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता के चलते उभरी दलित चेतना तथा दलित प्रज्ञा एवं दलित दावेदारी के अभियान इस वैचारिक वर्चस्व के सामने सशक्त चुनौती बन गए हैं।
भारत के कम्युनिस्टों ने जातिवाद को एजेंडे पर नहीं रखा जो अंबेडकर ने किया। इस मुद्दे पर बहस की गुंजाइश यहां नहीं है, वह एक अलग चर्चा का विषय है। 1934 में “मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित आचार्य नरेंद्रदेव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें अवैध कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। ईएमएस नंबूदरीपाद इसके सह सचिव थे। किसान-मजदूरों की दृष्टिकोण से 1934-42 का दौर एक तरह से स्वर्णिम दौर था. जिसमें सीएसपी के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा और ट्रेड यूनियन एक सशक्त ताकत बन गए। सीएसपी के युद्ध विरोधी प्लेटफॉर्म को झटका देते हुए सोवियत संघ पर नाजी हमले से सीएसपी के कम्युनिस्ट सदस्य युद्ध के समर्थक हो गए। इसकी समीक्षा की गुंजाइश यहां नहीं है।
आजादी के बाद सीपीआई और सोशलिस्ट पार्टियां नेहरू सरकार के साथ सहयोग और विरोध पर बहस करते रहे। कई कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कांग्रेस में चले गए। विचारों के प्रसार के लिए चुनाव में शिरकत करने की नीति ने सीपीआई को चुनावी पार्टी में तब्दील कर दिया। 1960 के दशक के शुरू में कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट और धीरे-धीरे हाशिए पर चले जाने की कहानी इतिहास बन चुकी है। लगभग डेढ़ सौ साल पहले मार्क्स ने हेगेल को उल्टा खड़ा कर दिया था, भारत के कम्युनिस्टों ने मार्क्सवाद को उलट दिया।
रोहित की शहादत के विरुद्ध जेएनयू आंदोलन में उमड़े युवा-उमंगों के सैलाब की कोख से एक बहुप्रतीक्षित, इंकिलाबी नारा निकला– जयभीम-लालसलाम। यह सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय के अलग-अलग चल रहे आंदोलनों के संगम की स्वफूर्त, प्रतीकात्मक एकता की अभिव्यक्ति है। जेयनयू के वामपंथी छात्रों के एक समूह ने भगत सिंह अंबेडकर स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (बासो) की स्थापना प्रतीक को कार्य रूप देने की पहल के रूप में देखी जा सकती है।
‘क्रांति के बिना जाति का विनाश नहीं; जाति के विनाश के बिना क्रांति नहीं’। इस प्रतीकात्मक एकता को सैद्धांतिक तथा राजनीतिक रूप देने की जरूरत है, लेकिन इस एकता के विरुद्ध वामपंथी और अंबेडकरवादी दोनों तरह के तत्ववादियों ने शंखनाद कर दिया है। सोशल मीडिया में दोनों तबके जय भीम और लाल सलाम में असाध्य अंतर्विरोधों का भजन गाने में मस्त हैं। अंबेडकर और मार्क्स की विचारधाराओं में असाध्य या शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध की बात अपने आप में एक विडंबनापूर्ण अंतविर्रोध है, क्योंकि दोनों की ही विचारधाराओं का मकसद शोषण-दमन तथा हर तरह के भेदभाव से मुक्त, समतामूलक समाज की स्थापना है। पंजाब में दलितों का भूमि आंदोलन अंबेडकर के विचारों और मार्क्सवाद के सिद्धातों के समन्वय या जय भीम-लाल सलाम के प्रतीकात्मक नारे के व्यवहार की जीती जागती मिसाल है।
छात्रों की पहल पर शुरू हुए इस आंदोलन ने प्रतिष्ठा के अधिकार को जमीन के अधिकार से जोड़कर संघर्ष किया तथा कई गांवों में सफलता मिली। जिन जमीनों पर उन्होंने अपने अधिकार हासिल किए, उन पर साझा खेती की मिसाल कायम की। कहने का मतलब यह है कि अब सामाजिक अन्याय और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध अलग-अलग संघर्षों का वक्त नहीं है। परिवर्तनकामी अंबेडकरवादी और समाजवादी ताकतों की एकता और समेकित संघर्ष, वक्त का तकाजा है। डॉ. अंबेडकर का भी यही संदेश है कि मुक्ति का रास्ता बुद्ध और मार्क्स की शिक्षाओं में निहित है। अंबेडकर ने सही लिखा है कि जातिवाद ने श्रम विभाजन को श्रमिक विभाजन में तब्दील कर दिया। ऊंची-नीची जातियों में बंटे सर्वहारा की एकजुटता मुश्किल है। इसीलिए ‘जाति के विनाश बिना क्रांति नहीं और क्रांति के बिना जाति विनाश नहीं’।
ईश मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त अध्यापक हैं