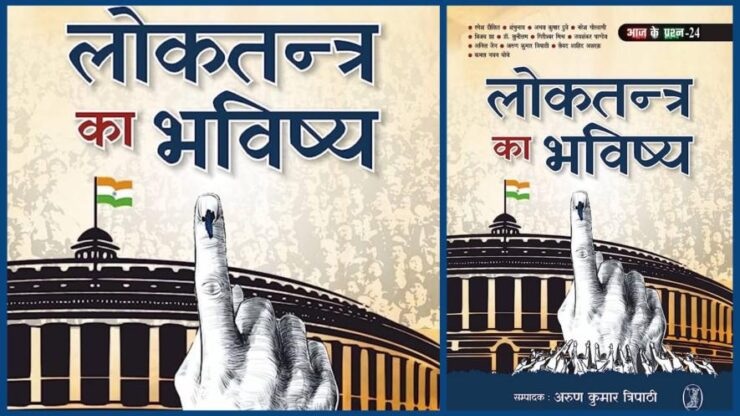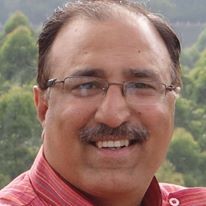(वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरुण कुमार त्रिपाठी के संपादकत्व में ‘आज के प्रश्न’ श्रृंखला के तहत ‘लोकतंत्र: अतीत, वर्तमान और भविष्य’ शीर्षक से एक किताब प्रकाशित हुई है। किताब में तकरीबन 12 लेखकों के लेख शामिल किए गए हैं। अरुण त्रिपाठी का कहना है कि इसकी अगली कड़ी में एक और किताब का प्रकाशन पाइपलाइन में है और बहुत जल्द ही वह पाठकों के सामने होगी। त्रिपाठी ने किताब की शुरुआत में एक भूमिका लिखी है। तकरीबन 17000 शब्दों में लिखी गयी इस भूमिका के शुरुआती हिस्से को यहां दिया जा रहा है। पेश है भूमिका-संपादक)
भारतीय लोकतंत्र पर सबसे गंभीर चर्चाएं आपातकाल के बाद हुई थीं। तब विद्वानों ने अंतिम निष्कर्ष के तौर पर यह मान लिया था कि भारतीय जनमानस इतना परिपक्व हो चुका है कि अब कोई भी तानाशाह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तमाम तरह के संकटों के बावजूद नब्बे के दशक को भारतीय लोकतंत्र का स्वर्ण युग कहा गया। क्योंकि केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर ही नहीं चला बल्कि पिछड़ी और दलित जातियों को सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने और सरकार के एजेंडा को प्रभावित करने का पर्याप्त अवसर मिला। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसका निर्णय पटना, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और हैदराबाद से होने लगा। राष्ट्रीय दलों का महत्व कम हुआ और क्षेत्रीय दलों की शक्ति बढ़ी। हर क्षेत्रीय नेता अपने प्रधानमंत्री बनने का सपना पालने लगा।
इसी स्थिति के कारण बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने यहां तक कह दिया कि हमें केंद्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। संचार माध्यमों की आर्थिक और तकनीकी ताकत पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई। राबिन जैफ्री जैसे मीडिया शोधकर्ताओं ने यहां तक लिखा कि आम आदमी के भीतर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। क्योंकि उसे डर है कि उसका गैरकानूनी व्यवहार अखबार में छप जाएगा। बल्कि पुलिस के भीतर मीडिया का खौफ बैठ गया है और इस नाते आम आदमी निर्भीकता से जीवन जी सकता है। इसी नब्बे के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जजों के दूसरे प्रसिद्ध मुकदमे(1993) के तहत कॉलेजियम प्रणाली का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की बजाय न्यायपालिका के अधिकार बढ़ा दिए। हालांकि इसी दौरान पूंजीवाद ने उदारीकरण और वैश्वीकरण के रूप में अपना नया रूप धारण किया और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा, बनवारी लाल शर्मा और डा ब्रह्मदेव शर्मा जैसे बहुत सारे लोकतांत्रिक चिंतकों और राजनेताओं ने उसे एक बड़े खतरे के रूप में देखते हुए आगाह किया।
पूंजीवाद का यह रूप अपना प्रभाव तो बढ़ा रहा था लेकिन बीच-बीच में उसे अलग-अलग झटके लग रहे थे। जैसे कि 2004 में वामपंथ के शक्तिशाली होने और केंद्र में यूपीए सरकार के साथ साझा न्यूनतम कार्यक्रम लागू होने और देश में तमाम तरह के आंदोलनों के तेज होने के साथ आर्थिक सुधार वह रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था जिसकी पूंजीवाद को अपेक्षा थी। संभवतः यूपीए सरकार को वामपंथी दलों के समर्थन का ही प्रभाव था कि सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के निजीकरण की गति धीमी रही। इसी के साथ गठबंधन सरकारों और बढ़ते भ्रष्टाचारों और उनके उजागर होने के साथ पूंजीवाद को अपनी साख और स्थिरता को लेकर आशंका भी हो रही थी। टूजी घोटाला, कोयला घोटाला, कामनवेल्थ घोटाला और ऐसे तमाम घोटाले व्यवस्था के भीतर स्थित नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक(सीएजी) जैसी संस्था ही उजागर कर रही थी। इस बीच सूचना के अधिकार के लागू हो जाने से व्यवस्था के भीतर से बहुत सारे रहस्य उजागर हो रहे थे। उससे उसी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थीं जिसने पारदर्शिता के लिए उसे लागू किया था।
वित्तमंत्री के तौर पर उदारीकरण का आरंभ करने वाले और प्रधानमंत्री के तौर पर उसे रफ्तार देने वाले डॉ. मनमोहन सिंह परेशान थे कि कैसे उदारीकरण को चलाएं और गवर्नेंस डिफिसिट यानी प्रशासनिक घाटे को भी दूर किया जाए और साथ ही लोकतंत्र के भी कायम रखा जाए। वे कहने भी लगे थे कि पुराने प्रशासनिक ढांचे के तहत उदारीकरण को साफ सुथरे तरीके से नहीं चलाया जा सकता। उसके लिए प्रशासनिक सुधार बहुत जरूरी है। लेकिन गठबंधन धर्म उन्हें बहुत सारे कदम उठाने से रोक रहा था। कड़ी कार्रवाई करने पर सरकार गिरने का खतरा था और न करने पर साख गिरने का। उधर उदारीकरण से प्रेरित भ्रष्टाचार ने सरकार को पंगु बना दिया था। पूंजीपति लगातार शिकायत कर रहे थे कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें चल ही नहीं रहीं।
अधिकारी निर्णय लेने से डर रहे हैं। पता नहीं कौन चपेटे में आ जाए। इस बीच भारत बनाम भ्रष्टाचार नामक संस्था का उदय होता है और कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार के भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त न्यायमूर्ति हेगड़े की ओर से दिए गए जांच के आदेश के बाद जो आंदोलन खड़ा होता है वह कर्नाटक को झटका देकर दिल्ली की केंद्र सरकार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। फिर अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी का उदय भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देने और पारदर्शी बनाने की एक अलग कहानी है। अन्ना आंदोलन की एक धारा उदारीकरण के विरोध और उस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से की जाने वाली लड़ाई से भी जुड़ी थी। फिर जनलोकपाल की मांग और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ ही कानून बनाने का फैसला मंत्रिमंडल से बाहर जनता की ओर से होने वाले आंदोलनों में लिए जाने का सवाल भी आया।
लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण की चासनी में डूबी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था को पवित्र करने का यह आंदोलन अंततोगत्वा एक ओर सिर्फ बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करने वाली आप जैसे विचारधारा विहीन दल के उदय में समाप्त हुआ तो दूसरी ओर हिंदुत्व और वैश्विक पूंजीवाद के मजबूत और अधिनायकवादी गठजोड़ के रूप में प्रकट हुआ। जनलोकपाल और केंद्रीय संस्थाओं की स्वायत्तता की जो अवधारणा प्रकट हो रही थी वह धीरे धीरे लोकलुभावनवाद और फिर निरंकुशतावाद और अधिनायकवाद की शिकार हो गई।
अपनी साख को बचाने और स्थिरता पाने के लिए कॉरपोरेट पूंजीवाद ने हिंदुत्व से हाथ मिला लिया। क्योंकि यूपीए का `धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र’ और वाममोर्चा का अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोध आपस में टकरा कर एक दूसरे से अलग हो गया था और उदारीकरण को अपना काम तेजी से करने के लिए किसी नए गठजोड़ की आवश्यकता थी जो उसे हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद से बढ़िया कौन दे सकता था। इस तरह अंतरराष्ट्रीय पूंजी को समर्थन देने वाली नीतियों के संतुलन के लिए बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद का ऐसा आख्यान रचा गया कि राजनीतिक अनिश्चितता लगभग समाप्त हो गई। प्रशासनिक कोताही की जगह पर प्रशासनिक आधिक्य का वातावरण बन गया। तकरीबन ढाई दशक बाद 2014 में देश में गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हुआ और बहुसंख्यकवादी पार्टी भाजपा को बहुमत मिलने के साथ भारतीय लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक सीमित किया जाने लगा।
निश्चित तौर पर कॉरपोरेट पूंजीवाद के योग से उभरी शक्ति ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। इसीलिए यह दावा खोखला नहीं है कि भारत बनाम भ्रष्टाचार के अन्ना आंदोलन के पीछे वे शक्तियां थीं। उनका लक्ष्य था किसी तीसरी और गुमनाम शक्ति को खड़ा करके कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे गठबंधन को बदनाम किया जा सके और फिर अच्छे दिन, साफ सुथरी सरकार और सबका साथ सबका विकास के नए नारे के साथ देश में ऐसी सरकार बनाई जा सके जो आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज कर सके बल्कि हिंदू राष्ट्र के गठन का मार्ग भी प्रशस्त कर सके। हिंदुत्व और लोगों को आर्थिक फायदा देने के इस कांबो पैकेज में एक ओर राम मंदिर बनाने, अनुच्छेद 370 खत्म करने और कॉमन सिविल कोड लाने का वादा था तो दूसरी ओर विदेश से काला धन लाकर हर नागरिक के खाते में 14-15 लाख डालने का लोकलुभावन वचन(जो कि बाद में चुनावी जुमला ही साबित हुआ)।
कहा तो यह भी गया कि सरकार वह अच्छी होती है जो न्यूनतम नियंत्रण करती है लेकिन निर्णय उल्टी दिशा में जाने लगे। वास्तव में यह सब नए किस्म के नागरिकों के सृजन का प्रयास था और नए राज्य के निर्माण का प्रयास था। जिस बाजार ने अपने विस्तार के लिए राज्य की शक्तियों को क्षीण किया था उसी ने अब अपने सुदृढ़ीकरण के लिए उसे ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। हिंदुत्व तो चाहता ही था कि मजबूत सरकार मिले ताकि जो आंतरिक शत्रु हैं(कम्युनिस्ट, मुस्लिम और ईसाई) उनसे निपटा जा सके। जो लक्ष्य अयोध्या आंदोलन से नहीं हासिल नहीं हो सका वह अन्ना आंदोलन ने पूरा कर दिया। भ्रष्टाचार और राज्य और उसे चलाने वालों की सुरक्षा के सवाल को विरोधियों के दमन का हथियार बना लिया गया। राज्य की सारी शक्तियां एक पार्टी, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर एक प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति और उसके दफ्तर यानी पीएमओ में केंद्रित होने लगीं।
भ्रष्टाचार मिटाने के लिए संस्थागत निर्णय लिए जाने की बजाय व्यक्तिगत निर्णय लिए जाने लगे। अचानक की गई नोटबंदी एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश और अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। उसकी जानकारी न तो रिजर्व बैंक को दी गई थी और न ही मंत्रिमंडल को। जनता को तो आगाह करने का सवाल ही नहीं था। दुखद बात यह है कि उस निर्णय का एलान किए जाते समय कहा गया था कि इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, कालाधन खत्म हो जाएगा और नकदी का चलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार घट गई, विपक्ष पस्त हो गया और सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई।
भले ही नारा `सबका साथ सबका विकास’ और `अच्छे दिनों’ का दिया गया लेकिन जो लोग वास्तव में वैसा चाहते थे वे सरकार के निशाने पर आ गए। केंद्र में गठबंधन का दिखावा जरूर किया गया लेकिन उसी के साथ यह संदेश दे दिया गया कि गठबंधन सिर्फ वही पार्टी कर सकेगी जो हिंदू हितों की बात करेगी। जो वास्तव में सबका साथ सबका विकास का काम करेगी उसका गठबंधन या तो होने नहीं दिया जाएगा या फिर चलने नहीं दिया जाएगा। इस बीच न्यायपालिका और मीडिया जैसी लोकतंत्र की महत्त्वपूर्ण संस्थाएं भारी दबाव में आती गईं। न्यायपालिका में नियुक्तियों के बारे में कॉलेजियम की संस्तुतियों पर सरकार की ओर से होने वाली देरी पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आंसू बहाने को बाध्य हुए।
उन्होंने कहा कि अगर हमें पर्याप्त संख्या में जज नहीं मिलेंगे तो न्यायपालिका अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकेगी। उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आजकल देश के विधि मंत्री और न्यायपालिका के बीच कॉलेजियम प्रणाली को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने कोलिजियम की ओर से भेजे गए 21 नामों में से 19 नाम लौटा दिए हैं और सिर्फ दो नामों को मंजूरी दी। सरकार की ओर से विधि मंत्री लगातार यह कह रहे हैं कि कॉलेजियम प्रणाली तो संविधान सम्मत नहीं है क्योंकि इसके लिए संविधान में कोई स्थान नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज इसे जजों द्वारा बनाए जाने वाले कानून के तर्क के आधार पर सही बता रहे हैं।
अब तो इस बहस में देश के उपराष्ट्रपति भी कूद पड़े हैं और उनका कहना है कि राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। वही आयोग जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि अभी भी इस देश में वे शक्तियां मौजूद हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया था और उन शक्तियों का मुकाबला न तो मीडिया कर सकेगा न ही एनजीओ। बल्कि उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत एक स्वायत्त न्यायपालिका ज्यादा सक्षम रूप से कर सकेगी। इस बहस में लोकसभा अध्यक्ष भी उतर आए हैं और उन्होंने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति का साथ दिया है।
अब बहस इस तर्ज पर चल निकली है कि न्यायपालिका बड़ी या संसद। 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए केशवानंद भारती के फैसले में प्रतिपादित संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत भी विवादित करार कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सिद्धांत संविधान में नहीं दिया गया था। यह सब न्यापालिका के सोच की उपज है। जबकि वह सिद्धांत कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है लेकिन उसके बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ सकती है।
भारतीय लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरों के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर चर्चा तब उठी जब एनडीटीवी नाम के चैनल को मौजूदा सरकार के सबसे चहेते और दुनिया के दूसरे नंबर के पूंजीपति गौतम अडानी ने खरीद लिया और अपनी निर्भीकता के लिए व सरकार की वाहवाही करने वाले मीडिया के लिए गोदी मीडिया जैसा पद ईजाद करने वाले चर्चित पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा देते हुए भारत में पत्रकारिता के भविष्य की आशंकाओं पर यूट्यूब पर एक भावुक संदेश जारी किया। रवीश कुमार ने कहा था, “ जो युवा पत्रकार बनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वे दलाल बनने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। जो आज पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं उन सबको झेलना पड़ेगा। कुछ लोग थक गए हैं और कुछ प्रोफेशन को छोड़ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि नौकरी बचाने के लिए पत्रकारिता में कोई आकर्षण बचा नहीं है।’’
हाल में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो को डिजिटल मीडिया की खबरों को सेंसर करने का अधिकार दे दिए जाने से पत्रकारों में बहुत बेचैनी है। सरकार की इस पहल की एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया समेत तमाम पत्रकारीय संस्थाओं ने निंदा की है। इसे आपातकाल के दौरान लगाई गई पाबंदियों जैसा ही बताया है। उसके बाद बीबीसी की ओर से `इंडियाः द मोदी क्विश्चन’ शीर्षक से बनाई गई डॉक्यूमेंटरी के भारत में प्रदर्शन पर रोक के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों और युवाओं के बीच जिस प्रकार का प्रतिरोध देखा गया उससे सेंसर की एक और बानगी उपस्थित हुई।
एक ओर केरल में वाममोर्चा के संगठन डीवाईएफआई ने जब उस डॉक्यूमेंटरी का पूरे राज्य में प्रदर्शन किया तो भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठनों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया। हैदराबाद में भी युवाओं ने विश्विविद्यालय में फिल्म का प्रदर्शन किया तो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब प्रदर्शन होने लगा तो बिजली काट दी गई और झाड़ियों से पथराव किया गया। जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जब प्रदर्शन का प्रयास किया गया तो पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया।
यह स्थिति वैश्विक मूल्यांकनों में भी साफ दिख रही है। फ्रांस की संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर ने अपने सर्वे में यह बताया है कि भारत की पत्रकारिता ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के पैमाने पर अब 150 वे नंबर पर आ गई है। पहले यह 142 वें पायदान पर थी। लेकिन हमारी सरकार किसी भी आलोचना को सुनने को तैयार नहीं है और वह हर प्रकार की चेतावनी और आशंका को खारिज करती है। फिलहाल सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बने भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज से जब भारत के लोकतंत्र के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि `किसी भी देश को भारत को लोकतंत्र के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भारत में लोकतंत्र 2500 साल पुराना है। यहां शाक्यों और लिच्छिवियों का गणतंत्र रहा है। इस दौरान भारत में लोकतंत्र के सारे स्तंभ मजबूत हैं। हमारे यहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ यानी प्रेस सारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।
सोशल मीडिया बहुत जीवंत है। इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।’ दरअसल रुचिरा कंबोज वही कह रही थीं जो कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से आयोजित लोकतंत्र सम्मेलन में बोल कर आए थे। उन्होंने कहा था, “ लोकतांत्रिक भावना हमारे सभ्यतागत लोकाचार का अविभाज्य हिस्सा है। भारत में 2500 साल पहले लिच्छिवियों के शासन में चुने हुए लोगों का नगर गणतंत्र था। वही भावना 10 वीं सदी के उत्तररामेरूर में थी। इससे प्राचीन भारत समृद्ध था। सदियों तक चला औपनिवेशिक
शासन उस भावना को दबा नहीं पाया। फिर जब भारत आजाद हुआ तो 75 साल से राष्ट्रनिर्माण की असाधारण कथा चल रही है। ’’
दरअसल लोकतंत्र और गणतंत्र का फर्क कम लोग समझते हैं और सरकार में बैठे लोग इसी घालमेल में लोगों को रखना चाहते हैं। वे यह साबित करना चाहते हैं कि चुनाव हुआ और सरकार चुन ली गई तो समझ लो कि लोकतंत्र कायम है। जबकि यह तो गणतंत्र है। लोकतंत्र इससे कहीं आगे की चीज है। इस अंतर को संविधान निर्माता डा भीमराव आंबेडकर ने बार बार स्पष्ट करने की कोशिश की लेकिन आंबेडकर का नाम लेने वाले न तो इस अंतर को स्पष्ट करते हैं और न ही किसी को साफ तौर पर रखने देते हैं।
जो लोग लिच्छिवियों और शाक्यों के गणतंत्र का हवाला देते हैं वे यह नहीं बताते कि गणतंत्र और लोकतंत्र में फर्क होता है। वही फर्क जो यूनान के प्राचीन गणतंत्र और आज के यूरोपीय और अमेरिकी गणतंत्र में है। सिर्फ शासन करने वालों को चुन लेने का अधिकार मिल जाने से लोकतंत्र कायम नहीं हो जाता। इस बारे में डॉ. आंबेडकर बताते हैं, “ लोकतंत्र का अर्थ एक राजनीतिक मशीन से लिया जाता है। माना जाता है कि जहां यह मशीन है वहां लोकतंत्र है। यह भी समझा जाता है कि जहां गणतंत्र है होगा वहां लोकतंत्र होगा। जहां संसद है और वयस्क लोग नियमित तौर पर होने वाले चुनाव में उसे चुनते हैं संसद कानून बनाती है वहां लोकतंत्र है। यानी यह एक तरह का राजनीतिक उपकरण है और जहां वह उपकरण है वहां लोकतंत्र होगा ही। क्या भारत में लोकतंत्र है या लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है?’’ (डा आंबेडकर, 20 मई 1956)।
वे अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं,“ एक तो लोकतंत्र का मतलब गणतंत्र से नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां संसदीय सरकार है उसका मतलब लोकतंत्र नहीं है। इसी कारण भ्रम पैदा होता है। लोकतंत्र इन दोनों से एकदम अलग चीज है। लोकतंत्र की जड़ें सरकार के स्वरूप में नहीं होतीं बल्कि उससे अलग होती हैं। लोकतंत्र प्राथमिक रूप से मिली जुली जीवन पद्धति है। लोकतंत्र की जड़ें सामाजिक संबंधों में होती हैं। जो लोग समाज बनाते हैं उनके साझा जीवन में होती हैं। समाज क्या है?
समाज वास्तव में एक समुदाय है जिसका कोई मकसद है, कल्याण करने की कोई इच्छा है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निष्ठा है, पारस्परिक सहानुभूति और सहयोग की भावना है। क्या यह चीजें भारतीय समाज में हैं? नहीं हैं। भारतीय समाज में व्यक्ति नहीं है। यहां ढेर सारी जातियों का संकलन है जो एक दूसरे से साझेदारी नहीं करतीं और उनमें सहानुभूति का कोई सूत्र नहीं है। जाति व्यवस्था के कारण यहां समाज के आदर्श नहीं है इसलिए लोकतंत्र नहीं है। हर चीज जाति व्यवस्था के आधार पर संगठित है।…जाति के कारण भारतीय लोग एक दूसरे से न तो शादी कर सकते हैं और न ही एक साथ भोजन कर सकते हैं।’’
डॉ. आंबेडकर की बातों को अगर जाति के साथ संप्रदाय के अर्थ में भी लागू किया जाए तो आज भारतीय समाज ज्यादा ही विभाजित है। यह जानते हुए कि इस देश में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह का अनुपात आबादी के 1 से 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ सामाजिक गोलबंदी और बहिष्कार से लेकर कानूनी अवरोध खड़े कर दिए गए हैं। आनर किलिंग से लेकर लव जेहाद के विरुद्ध कानून बनाने तक व्यक्ति के अधिकारों और सामुदायिक पारस्परिकता को खत्म करने के ही उपाय किए हैं। यह सब हमारे समाज को महज गणतंत्र बनाकर छोड़ देते हैं लोकतंत्र नहीं बनने देते।
लोकतंत्र क्या है और उसकी क्या अनिवार्य शर्तें हैं इस बारे में डा आंबेडकर का विमर्श बहुत प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है इस बारे में कोई आम राय नहीं है। मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण रखे जाते हैं लोकतंत्र के बारे में। एक दृष्टिकोण कहता है कि यह एक किस्म की सरकार की प्रणाली है। यानी लोकतंत्र वह प्रणाली है जहां जनता सरकार चुनती है। मतलब जहां प्रतिनिधित्व वाली सरकार है वहां लोकतंत्र है। उस जगह पर लोकतंत्र कायम मान लिया जाता है जहां पर वयस्क मताधिकार हों और समय समय पर चुनाव हों। जबकि दूसरा दृष्टिकोण यह कहता है कि लोकतंत्र सरकार की प्रणाली से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। वह समाज का एक संगठन है। लोकतांत्रिक रूप से गठित समाज की दो अनिवार्य शर्तें हैं।
- समाज में वर्गीय आधार पर जड़ता का अभाव
- व्यक्ति और समूह सदैव तालमेल करने को तैयार रहते हैं और हितों की पारस्परिकता को मान्यता देते हैं।
- डा आंबेडकर कहते हैं कि अगर दूसरी शर्त का पालन नहीं होता तो समाज अलोकतांत्रिक हो जाता है। वे कहते हैं कि जो लोग यह मानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव होता है वे तीन गलतियां करते हैं।
पहली गलती यह कि सरकार नामक संस्था समाज से भिन्न और कटी हुई होती है। जबकि वास्तव में वैसा नहीं है। सरकार उन तमाम संस्थाओं में से एक है जिसे समाज तैयार करता है ताकि वह कुछ दायित्वों का निर्वाह कर सके।
दूसरी गलती यह है कि वे यह समझ नहीं पाते कि सरकार को समाज के अन्तिम उद्देश्य और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब जिस समाज में सरकार खड़ी है वह समाज लोकतांत्रिक हो। अगर समाज लोकतांत्रिक नहीं है तो सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। अगर समाज वर्गों में बंटा है तो सरकार शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने में लगी रहती है।
तीसरी गलती यह है कि वे लोग नहीं समझते कि सरकार चाहे जैसी हो वह अफसरों यानी सिविल सर्वेंट्स पर निर्भर करती है। वे लोग कैसे हैं यह उस सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है जिसमें वे तैयार होते हैं।
इसलिए लोकतांत्रिक सरकार के लिए लोकतांत्रिक समाज होना अनिवार्य है। लोकतंत्र एक राजनीतिक मशीन से बड़ी चीज है। यह एक सामाजिक व्यवस्था से कुछ ज्यादा है। यह एक मानसिक रवैया है यह एक जीवन दर्शन है।
फिर वे इस बात पर आते हैं कि संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के तीन मूल्यों में से सबसे प्रमुख मूल्य कौन सा है? उनका कहना है कि कुछ लोग लोकतंत्र को समता और स्वतंत्रता से जोड़ते हैं। निश्चित तौर पर वे लोकतंत्र के सबसे गहरे सरोकार हैं। लेकिन उससे भी महत्त्वपूर्ण सवाल यह है कि समता और स्वतंत्रता किस चीज पर टिके रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह राज्य का कानून है जिस पर वे टिके रहते हैं। लेकिन यह सही नहीं है। समता और स्वतंत्रता को जो चीज टिकाती है वह है सहमनापन यानी fellowfeeling. इसका अर्थ है मित्रता का भाव। बुद्ध ने इसके लिए मैत्री शब्द दिया था। मैत्री का महत्त्व समझाते हुए डॉ आंबेडकर लिखते हैं कि मैत्री के बिना समता स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी और स्वतंत्रता समता को नष्ट कर देगी। लोकतंत्र में अगर समता स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करती और स्वतंत्रता समता को नष्ट नहीं करती तो उसकी वजह मैत्री है। इसलिए बंधुत्व ही लोकतंत्र का मूल आधार है।
यहां यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र गणतंत्र से कितना अलग है। लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप अलग अलग देशों में अलग अलग रहा है और किसी एक देश का लोकतंत्र हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। इसलिए यह कह पाना कठिन है कि लोकतंत्र क्या है और यह भी दावा करना मुश्किल है कि किसी देश में पूरी तरह से लोकतंत्र आ गया है। यह निरंतर विकासमान व्यवस्था है। लेकिन एक बात निश्चित है कि धुर वामपंथ और धुर दक्षिणपंथ लोकतंत्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं।
दोनों उसे विकास और जनता के नाम पर किसी पार्टी या चंद शासकों में केंद्रित कर देते हैं। और इस प्रकार वे लोकतंत्र के मध्यमार्ग को नष्ट कर देते हैं। कहीं रोटी बनाम स्वाधीनता की बहस है तो कहीं विकास लोकतंत्र का द्वंद्व छिड़ा है। लोकतंत्र का विमर्श शुरू करने पर यूनान और एथेंस की बात आती है। लेकिन एथेंस के लोग जिस लोकतंत्र की बात करते थे वह आज के लोकतंत्र से अलग रहा है। वहां 50 प्रतिशत लोग दास रहे हैं। उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था और न ही सरकार के गठन और संचालन में उनकी कोई भूमिका थी। 1688 की क्रांति से पहले इंग्लैंड का लोकतंत्र वैसा नहीं था जैसे बाद में हुआ। 1688 से 1832 के बीच वह कुछ और था और उसके बाद कुछ और हो गया। लोकतंत्र का स्वरूप तो बदलता ही रहा है उसका उद्देश्य भी बदलता रहा है।
पहले इंग्लैंड में लोकतंत्र का मकसद बादशाह की शक्तियों को कम करना था क्योंकि बादशाह कहता था कि मेरा कानून चलेगा जबकि संसद कहती थी उसका कानून चलेगा। आज के लोकतंत्र का मकसद लोककल्याण हो गया है। डा आंबेडकर इंग्लिश कांस्टीट्यूशन पर चर्चित पुस्तक लिखने वाले वाल्टर वेगहैट का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है बहस से चलने वाली सरकार। उसी संदर्भ में अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी उल्लेखनीय है जिसके तहत लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता का शासन होता है।
यहां लोकतंत्र की डॉ आंबेडकर की परिभाषा गौर करने लायक है। वे कहते हैं,“ लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप और पद्धति है जहां पर बिना खून खराबे के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाता है।’’ फिर वे इस बात पर भी आते हैं कि लोकतंत्र को कैसे कामयाब किया जाए।