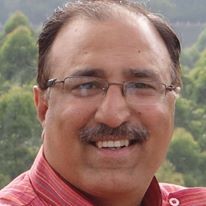(समाजवादी चिंतक डॉक्टर प्रेम सिंह ने यह लेख 27 दिसंबर 2018 को लिखा था जो दिल्ली की दीवारों पर लिखी वर्तमान की इबारत को पढ़ने की कोशिश है, कमोबेश यही हालत देश के हर शहर के हैं जहां पर दीवारें त्योहारों, जन्मदिन की बधाइयां और कॉर्पोरेट मुद्दों को लेकर रंगी हुई है । लेकिन युवाओं के ,किसानों के, मजदूरों के सवाल इन पोस्टरों से गायब है । डॉ प्रेम सिंह जी ने यह लेख सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के अध्यक्ष रहते हुए लिखा था, उक्त लेख को अग्नि आलोक में फिर से प्रकाशित किया जा रहा है ।-संपादक)
डॉक्टर प्रेम सिंह

यह टिप्पणी कोई पत्रकार साथी लिखता तो अधिक सार्थक होती और ज्यादा लोगों तक पहुंचती. दरअसल मैं इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई साथी इस विषय की तरफ ध्यान देगा और लिखेगा. लेकिन दिल्ली महानगर के चहरे-मोहरे, जिसकी अनंत छवियां और सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, पर गौर करने वाले पत्रकार अब नहीं रहे. अगर हैं तो अखबारों में वैसे लेखन के लिए जगह नहीं रह गई है. एक समय ‘जनसत्ता’ में पत्रकार सुशील कुमार सिंह ने दिल्ली पर कई दिलचस्प टिप्पणियां लिखी थीं. ‘जनसत्ता’ के ही मनोज मिश्र की दिल्ली संबंधी राजनीतिक रिपोर्टिंग में दिल्ली शहर का अक्स भी उभर कर आता था. दिल्ली विश्वविद्यालय के डीएवी कॉलेज (संध्या) में शिक्षक रहे समाजवादी साथी द्विजेन्द्र कालिया ने अस्सी के दशक में लघु पत्रिका ‘नया संघर्ष’ में पुरानी दिल्ली के कुछ प्रसंगों और अनाम लोगों पर रोचक टिप्पणियां लिखी थीं. प्रोफेसर निर्मला जैन ने दिल्ली के आधी सदी से ज्यादा (1940 से 2000) के सफ़र का लेखा-जोखा ‘हंस’ में धारावाहिक लिखा था, जो ‘दिल्ली शहर दर शहर’ पुस्तक के रूप में प्रकाशित है. कहने की जरूरत नहीं कि, अगर हम समझ सकें तो, किसी शहर का बाह्य स्वरुप उसके अंदर चलने वाली गहरी सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है.
दिल्ली महानगर पोस्टर-होर्डिंग और दीवार-लेखन के जरिये किये जाने वाले विज्ञापनों से पटा रहता है. सरकारों, राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों, उपभोक्ता उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के नित नए विज्ञापनों की झड़ी दिल्ली में लगी रहती है. देखते-देखते पिछले करीब तीन दशको में देश की राजधानी दिल्ली एक विशाल विज्ञापन में तब्दील हो गयी है. और इस रूप में यह दिल्ली पूरे देश में फ़ैल चुकी है. अब गांव-कस्बे भी दिल्ली से बाहर नहीं हैं. पूरा देश विज्ञापनबाज़ी का अखाड़ा बन चुका है. इन विज्ञापनों पर अकूत कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक और स्याही खर्च की जाती है. विज्ञापन उद्योग के अर्थशास्त्र पर कुछ चर्चा होती है, लेकिन इस परिघटना के राजनीति शास्त्र पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है.
मेरी आदत है कि दिल्ली में सफ़र करते या पैदल चलते वक्त मैं चौतरफा लगे पोस्टरों-होर्डिंगों और दीवार-लेखन पर नज़र डालते हुए चलता हूं. एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरी कोशिश इस परिघटना के राजनीतिक निहितार्थ समझने की रहती है. तरह-तरह के पोस्टरों-होर्डिंगों और दीवार-लेखन के अध्ययन से दिल्ली के दिल की बात जानी जा सकती है. सभी तरह के विज्ञापनों की तफसील में न जाकर यह टिप्पणी केवल धार्मिक त्योहारों पर ‘सभी भाई-बहनों’/’देशवासियों’ को बधाई देने वाले पोस्टरों-होर्डिंगों के बारे में है. वह भी इस साल के शारदीय नवरातों से लेकर छठ पर्व तक चलने वाले फेस्टिवल सीजन को आधार बना कर.
दिल्ली में त्योहारों पर बधाई के पोस्टर-होर्डिंग भाजपा और कांग्रेस की ओर से लगाए जाते रहे हैं. कहीं-कहीं बसपा के इक्का-दुक्का पोस्टर-होर्डिंग दिख जाते थे, जो आम आदमी पार्टी की जीत के बाद से लगभग बंद हो गए. दिल्ली में इस बार के शारदीय नवरातों से लेकर छठ पर्व तक चलने वाले फेस्टिवल सीज़न में एक ख़ास बदलाव देखने को मिला. राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं की ओर से बधाई देने वाले पोस्टरों/होर्डिंगों की जंग में कांग्रेस और उसके नेता शामिल नहीं थे. इस बार बधाई देने वाले पोस्टरों/होर्डिंगों की जंग भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीमित थी. कांग्रेस का यह सोचा-समझा फैसला था या महज़ संयोग, नहीं पता. कांग्रेस मौजूदा कारपोरेट राजनीति की जनक है और आगे भी उसकी प्रमुख खिलाड़ी रहेगी. लेकिन सांगठनिक रूप से देश की सबसे बड़ी पार्टी का अगर यह सोचा-समझा फैसला था, तो इसे एक सकारात्मक पहल माना जा सकता है. कम से कम इस रूप में कि वह कारपोरेट राजनीति के वल्गर डिस्प्ले को बुरा समझती है.
आम आदमी पार्टी ने धार्मिक त्योहारों पर बधाई की जंग में एक नया आयाम जोड़ा है. अभी तक भागवत कथा, रामकथा, रामलीला अथवा अन्य पुराण कथाओं आदि के आयोजन के विज्ञापन पार्टियां और नेता नहीं करते रहे हैं. मुझे देख कर हैरानी हुई कि आम आदमी पार्टी ने करीब 10-15 दिन पहले पूर्वी दिल्ली में ‘श्रीमद्भागवत कथाज्ञान यज्ञ’ के पोस्टर और होर्डिंग लगाए, जिनमें कथावाचक के साथ उसकी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की उम्मीदवार की तस्वीर छपी है. (इस उम्मीदवार के नाम के मतदाताओं पर संभावित धार्मिक प्रभाव को लेकर पिछले दिनों पार्टी ने जो स्वांग रचा, उसकी चर्चा मीडिया में हो चुकी है.) पिछले दो-तीन दशकों में धार्मिक कथावाचन के आयोजन हिंदू समाज में तेज़ी से फैले हैं. राजनीतिक पार्टियों में इस क्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई तेज हो सकती है. शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी है.
पार्टी का राजनीतिक दफ्तर खोलने पर हवन करने का प्रचलन शायद भाजपा में ही रहा हो. आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के दफ्तर का उद्घाटन हवन करके किया. हो सकता है दिल्ली की अन्य लोकसभा सीटों के दफ्तर खोलने पर भी हवन किया गया हो. केजरीवाल के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर किया गया हवन सभी को याद होगा! दिल्ली में पहले सरकार और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मानसरोवर यात्रियों को बधाई देने का विज्ञापन ज्यादा देखने को नहीं मिलता था. आम आदमी पार्टी ने मानसरोवर यात्रियों की बधाई के विशाल होर्डिंग महीनों तक स्थायी रूप से कुछ स्थानों पर लगाए रखे. राजनिवास मार्ग पर गुजराती समाज की बिल्डिंग के आगे रखे गए दो विशाल होर्डिंग मैंने यूनिवर्सिटी जाते वक्त महीनों तक देखे.
फेस्टिवल सीज़न की निरंतरता में आम आदमी पार्टी की ओर से ‘ईद मुबारक’ के छोटे पोस्टर उर्दू में केवल मुस्लिम इलाकों में चिपकाए गए. गोया ईद की मुबारक बात से बाकी धर्मावलम्बियों का लेना-देना न रहता हो. सिख समुदाय के धार्मिक उत्सवों को लेकर आम आदमी पार्टी के रवैये के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता. कुल मिला कर इस पार्टी के नेता देशवासियों को नागरिक के रूप में नहीं, केवल उनकी धार्मिक पहचान के साथ जोड़ कर देखते हैं. ऐसा वे डंके की चोट पर करते हैं.
राजनीतिक पार्टियों के धार्मिक त्योहारों पर बधाई के विज्ञापनों की बाढ़ का देश में बढ़ती साम्प्रदायिकता के साथ क्या रिश्ता है, इस सवाल पर मैं चर्चा नहीं करूंगा. इसलिए कि आरएसएस/भाजपा के फासीवाद से लड़ने वाले केजरीवाल के सेकुलर समर्थकों को यह हमेशा की तरह नागवार गुजरेगा. अलबत्ता इस परिघटना पर लोकतंत्र के सन्दर्भ में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं. मैं 21 दिसंबर को साथी एनडी पंचोली के साथ कार से दिल्ली से जालंधर जा रहा था. वहां अगले दिन जस्टिस राजेंद्र सच्चर के जयंती दिवस पर सोशलिस्ट पार्टी की ओर से संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को बचाने के उपायों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था. उसी सिलसिले में विज्ञापनों की परिघटना का हमारे लोकतंत्र के साथ क्या रिश्ता है, इस पर संक्षेप में उनके साथ चर्चा हुई. मैंने कहा कि विज्ञापन, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, एक नागरिक के रूप में व्यक्ति की अपने विवेक से चुनाव करने की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं. उनका मकसद लोगों को गुमराह करना होता है. जनता के धन की भारी बर्बादी से विज्ञापनों का तूमार लोकतान्त्रिक चेतना और प्रक्रिया को गहराई से कारपोरेट राजनीति के पक्ष में बदल रहा है. त्योहारों पर दी जाने वाली बधाइयों का धार्मिक आस्था से सम्बन्ध नहीं होता. छोटे नेता अथवा नेता बनने के अभिलाषी बधाई के पोस्टरों-होर्डिंगों पर बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीर जनता और पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते हैं, ताकि राजनीति में जगह बना सकें. राजनीति में जो काम संघर्ष के माध्यम से होना चाहिए, वह काम वे विज्ञापन के माध्यम से करते हैं. भारत में मीडिया, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें पूरी तरह से शामिल हो गया है. लिहाज़ा, नए नेता संघर्ष के रास्ते नहीं, विज्ञापन के रास्ते आते हैं. ऐसे में कारपोरेट राजनीति को बदल कर संवैधानिक राजनीति की स्थापना का काम असंभव नहीं तो दुर्गम अवश्य है. (इसी तरह सरकारों, पार्टियों, सामाजिक संगठनों, व्यावसायिक कंपनियों आदि के विज्ञापनों का विश्लेषण करें तो सभी के तार कारपोरेट राजनीति से जुड़े नज़र आएंगे.)
जिस तरह से देश का राजनीतिक और बौद्धिक नेतृत्व कारपोरेट राजनीति का हमसफ़र हुआ है, उसके चलते आगे लम्बे समय तक यह राजनीति भारत की भाग्य-विधाता बनी रहनी है. दिल्ली की धमन भट्टी में ढलने वाला यह कारपोरेट राजनीति का लोकतंत्र ही आगे फलने-फूलने वाला है. इस लोकतंत्र में तीन बहनों (मानसी 8 साल, शिखा 4 साल, पारो 2 साल) की बीमारी और भूख से मौत हो जाती है, लेकिन बुद्धिजीवी/पत्रकार/कलाकार/एक्टिविस्ट ऊंची आवाज़ में चिल्लाते रहते हैं – ‘दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा की नदियां बह रही हैं!’ इस लोकतंत्र के भीतरी कोनों से मजबूत नेता और/अथवा फौजी तानाशाह के लिए निरंतर पुकार उठती रहती है, लेकिन एनजीओ वाले लगातार ढोल पीटते रहते हैं – ‘आज़ादी के बाद लोगों ने पहली बार अपने हकों के लिए बोलना सीखा है!’ वे शहीदाना अंदाज़ में कहते हैं – ‘हमारा प्राथमिक सरोकार तो देश की जनता है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं!’
नवउदारवाद के पिछले तीन दशक के अनुभव ने साफ़ कर दिया है कि कारपोरेट राजनीति साम्प्रदायिक राजनीति से अविभाज्य है. लेकिन देश का सेकुलर खेमा यह मानने को कतई तैयार नहीं है. वह कारपोरेट राजनीति को चलाये रख कर धर्मनिरपेक्षता को बचाने का ढोंग करता है. फासीवाद के बरक्स लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाले यह सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि इस तरह से न धर्मनिरपेक्षता को बचाया जा सकता है, न लोकतंत्र को. जो बचाया जा सकता है, वह वर्ग-स्वार्थ है, और अंतत: वही बच रहता है! कारपोरेट राजनीति के विज्ञापन में तब्दील हुई दिल्ली के चेहरे पर यही इबारत लिखी होती है. कारपोरेट के क्रीत-दास इस इबारत का गलत पाठ जनता को बताते हैं.
(समाजवादी चिंतक डॉक्टर प्रेम सिंह ने यह लेख 27 दिसंबर 2018 को लिखा था जो दिल्ली की दीवारों पर लिखी वर्तमान की इबारत को पढ़ने की कोशिश है, कमोबेश यही हालत देश के हर शहर के हैं जहां पर दीवारें त्योहारों, जन्मदिन की बधाइयां और कॉर्पोरेट मुद्दों को लेकर रंगी हुई है । लेकिन युवाओं के ,किसानों के, मजदूरों के सवाल इन पोस्टरों से गायब है । डॉ प्रेम सिंह जी ने यह लेख सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के अध्यक्ष रहते हुए लिखा था, उक्त लेख को अग्नि आलोक में फिर से प्रकाशित किया जा रहा है ।-संपादक)