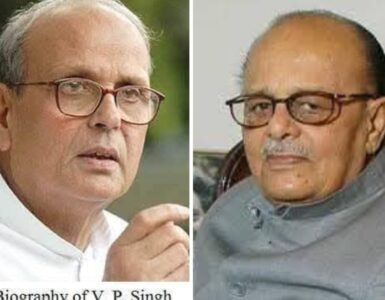प्रफुल्ल कोलख्यान
नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो चुके हैं। उनके लिए वे सारे खतरे खत्म हो चुके होंगे जिन खतरों की बातें वे परसों तक करते रहे थे। क्या गजब की बात है कि ‘खतरों’ से खेलते-खेलते उनका खुद खतरा बन जाना! एक भ्रम टूटकर इस तरह इतिहास के कूड़ेदान में जा गिरा। इतिहास सिर्फ कूड़ेदान नहीं होता, वह बनती-बिगड़ती सभ्यता के अनुभवों का खजाना भी होता है।
इतिहास के खजाना से एक अनुभव यह है कि लोगों की प्रेरणा के सूत्र सत्ता के लिए सिद्धांत बदलने वालों की कारगुजारियों से नहीं, सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़नेवालों के पराक्रम से निकलते हैं। नीतीश कुमार के लगातार नौ बार मुख्यमंत्री बनने से प्रेरणा का कोई सकारात्मक सूत्र नहीं निकलता है। प्रेरणा का सकारात्मक सूत्र निकलता है, दो अधूरे कार्यकालों के मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पराक्रम से! सावधान करता है उन लोगों से जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को कभी चैन से सत्ता पर रहने नहीं दिया!
भले ही नालंदा का नाम लेते समय नीतीश कुमार को सिर्फ अपने मतदाताओं का चेहरा दिखता हो, दुनिया को, सत्ता की परिधि से बार निकलकर साधना के शिखर पर पहुंचने वाले महात्मा बुद्ध का चेहरा दिखता है। हमें इतिहास में आने-जाने की सुविधा तो जरूर हासिल है, वहां घर बसा लेने के अपने खतरे हैं। इतिहास के प्रांगण में आना-जाना जारी रखते हुए, अपने समय की समस्याओं के हल तो वर्तमान में ही ढूंढने पड़ते हैं।
एक बात यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि यह लोकलुभावन और लोक भड़काऊ राजनीति (Demagoguery) का दौर है जो वर्तमान की कठोर जमीन पर पांव टिकने ही नहीं देता है; खींचकर, या तो सुदूर भूत या सुदूर भविष्य के सुनहरे विभ्रम में ले जाकर भरमाती रहती है। इसलिए, अब इस घटना को इतिहास के कूड़ेदान के हवाले करते हुए वर्तमान की कठोर जमीन पर बने रहने की जरूरत है।
आगे यह कि अब विपक्षी गठबंधन का क्या होगा? नहीं यह, वह सवाल नहीं है, जिसका जवाब खोजा जाना है। असली सवाल तो यह है कि लोकतंत्र का क्या होगा! संविधान का क्या होगा! भारत के संसदीय लोकतंत्र के अंतःकरण में हो रहे विस्फोटों का क्या होगा! अर्थनीति में सांठ-गांठ (क्रोनी कैपटलिज्म) का क्या होगा! भय-भूख-भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याओं का क्या होगा? बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के उपचार का क्या होगा! सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की विसंगतियों को दूर करने के इरादों का क्या होगा! लोकतांत्रिक बहुमत की ताकत को नृशंस बहुसंख्यकवाद की पिशाच-लीला में बदलने से रोकने के इरादों का क्या होगा?
नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो जाने से इतनी चिंता क्यों, इतने सवाल क्यों? क्या इन सवालों का जवाब ढूंढ़ने की कोशिश विपक्षी गठबंधन सिर्फ नीतीश कुमार के सहारे कर रहा था? ऐसा, बिल्कुल नहीं है। हां, इतना जरूर है कि इन सवालों के जवाब ढूंढने में उनके साथ होने और सहारे का भी योगदान हो सकता था। उनके योगदान से मतलब उनके मतदाताओं के योगदान से है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके मतदाताओं में इन सब सवालों पर सोचने की लियाकत बची हुई है। लियाकत ही नहीं अपनी लोकतांत्रिक ताकत का एहसास भी होगा ही।
एक बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि वह दौर बहुत खतरनाक होता है जिसमें काल्पनिक सवालों के अंबार तले वास्तविक सवाल दबा दिये जाते हैं। मूल सवाल तो विचारधारा का है। राहुल गांधी बार-बार विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं। विचारधारा के सवाल को समझना होगा। इसमें एक बात तो यह समझनी होगी कि वैचारिक उठाईगिरी से इन समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता है।
दूसरी बात यह है कि यह एक विचारधारा से किसी दूसरी विचारधारा के बीच का संघर्ष नहीं है। इस संघर्ष में एक तरफ भावधारा है तो दूसरी तरफ विचारधारा है। यदि ऐसा है तो सवाल यह है कि क्या विचारधारा किसी भी सूरत में भावधारा से मुकाबला कर सकती है या नहीं? इस पर जरूर सोचना होगा, एक बार नहीं हजार बार सोचना चाहिए।
फिलहाल, लगता है कि विचारधारा किसी भी तरह से भावधारा से नहीं निपट सकती है, वास्तविक कभी भी काल्पनिक से नहीं लड़ सकता है। वास्तविक का काल्पनिक से लड़ना वैसा ही ढोंग होगा जैसा ढोंग ओझा-गुनी भूत झाड़ने के नाम पर करते हैं। अकादमिक स्तर पर विचारधारा के सामने भावधारा टिक नहीं सकती है लेकिन लोकतंत्र के लिए अनिवार्य चुनावी संदर्भों में बाजी पलट जाती है; भावधारा के सामने विचारधारा का टिकना मुश्किल होता है।
एक बात को ध्यान में सदा रखना चाहिए कि मनुष्य न तो पूरी तरह विचार-शून्य हो सकता है और न ही भाव-शून्य! भावधारा जन-जीवन में जन्म-जात रूप से विन्यस्त रहती है! एक कामचलाऊ उदाहरण, जैसे किसी को भूख स्वतः लगती है, न लगे तो बीमारी, जिसके इलाज की जरूरत होती है। भूख मिटाने के लिए उपाय करना पड़ता है। भूख को अर्जित नहीं करना पड़ता है, भूख मिटाने के लिए अर्जन या उपार्जन करना पड़ता है। अर्जन या उपार्जन के लिए संसाधन चाहिए होता है, अनुकूल पारिस्थितिकी चाहिए होती है।
एक अन्य समस्या यह है कि विचारधारा को अर्जित करना पड़ता है। विचारधारा के अर्जन के लिए भी संसाधन और पारिस्थितिक नियंत्रण और संतुलन चाहिए होता है। विचारधारा के अर्जन में शिक्षण-प्रशिक्षण और तर्क-वितर्क की अपनी भूमिका होती है। यहां हमारी नजर शिक्षा व्यवस्था की तरफ, विश्वविद्यालयों की तरफ सहज ही चली जाती है। कहना न होगा कि कोई भी जनविरोधी राजनीतिक व्यवस्था, जैसे फासीवाद, पहला मौका मिलते ही शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस करने में जुट जाती है। यहां तहस-नहस का मतलब समाप्त करना नहीं, बल्कि, उसे बुद्धि विरोधी काम में लगाने का इंतजाम कर देना है। जनविरोधी व्यवस्था बुद्धिजीवी वर्ग की दुर्दशा करने के लिए अपने लंपटों को भिड़ा देती है। नजर उठाते ही अपने देश के माहौल में कुछ-न-कुछ तो जरूर दिख जायेगा।
बड़े-बड़े ज्ञानी-महात्मा अपने मंत्रों को सौ बार, हजार बार दुहराने में संकोच नहीं करते हैं! एक बार हम भी दुहरा लेते हैं – मनुष्य पूरी तरह से न तो भाव-शून्य हो सकता है, न विचार-शून्य। विचार और विचारधारा पर भी एक बात कहनी जरूरी है – विचार व्यक्तिगत तथा सामाजिक और तात्कालिक होता है, जब कि विचारधारा सार्वजनिक तथा सांगठनिक और ऐतिहासिक होती है – विचारधारा की रणनीतियां भले ही गोपनीय और तात्कालिक होती हों।
मुद्दे की बात यह है कि मनुष्य, जाहिर है इस प्रसंग में मतदाताओं, के मन में भाव और विचार के बीच की साझी जमीन पर भावधारा और विचारधारा का संगम क्षेत्र होता है। संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय राजनीतिक दलों को विचारधारा और भावधारा के इस संगम में लोकतांत्रिक स्नान करते रहना चाहिए। भारत के अस्तित्व की अनिवार्य विविधता और चेतना का मध्यमार्गी स्वभाव की आत्मा का सूत्र ‘मज्झिमनिकाय’ के पिटक में है।
विचारधारा में अधिकाधिक ऊभ-चुभ करने के कारण भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां चुनावी समर में डूबती चली गई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। परिणामतः 22 जुलाई 2008 को, यूपीए को लोकसभा में अपने पहले विश्वास मत का सामना करना पड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़े सोमनाथ चटर्जी उस समय लोक सभा के अध्यक्ष थे। यूपीए ने विपक्ष के 256 वोटों के मुकाबले 275 वोटों के साथ विश्वास मत जीता, (10 सदस्य वोट से अनुपस्थित रहे) और 19 वोटों से जीत दर्ज की। इस घटना के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़े सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया।
महत्त्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बीच राजनीतिक संबंध विच्छिन्न हो गया, कटुता भी आ गई। इसके बाद 2011 में पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा का चुनाव हुआ। इसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (SUCI) के बीच चुनावी समझौता हुआ। इस चुनाव से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 184 उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के 42 उम्मीदवार और सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (SUCI) के 1 उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। ममता बनर्जी के नेतृत्व में कुल 227 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आये। 295 सदस्यों की विधानसभा में अकेले दम बहुमत और सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। ममता बनर्जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वाम मोर्चा तथा कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हालत पश्चिम बंगाल में आज तक संभल नहीं पाई।
कहना यह है कि विचारधारा और भावधारा के संगम से बाहर ‘शुद्ध विचारधारा’ की तरफ बढ़ने से पश्चिम बंगाल राज्य में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राजनीतिक स्थिति ऐसी बन गई कि 34 साल के शासन के इतिहास के अलावा इस समय हाथ में कुछ भी नहीं है, आज किसको याद है कि दल का अनुशासन मानकर ज्योति बसु जैसे नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सके और अनुशासन न मानकर सोमनाथ चटर्जी दल के बाहर कर दिये गये।
संसदीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में भावधारा और विचारधारा के संगम स्थल को तलाशने की जरूरत है – यही वह अमृत कलश है, जिसकी तलाश संसदीय लोकतंत्र के चुनावों में दलों और गठबंधनों को होती है। एक बात यह भी कि संसदीय लोकतंत्र वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझान के लोगों को बहुत मुफीद नहीं लगता है। फिर भी वे संसदीय लोकतंत्र में भागीदार बनते हैं तो दोनों दो दिशाओं से चलकर इसी संगम स्थल पर आमने-सामने होते हैं।
यह संगम स्थल कांग्रेस पार्टी का मूल स्थान है। इस मूल स्थान से अधिक वाम होने के प्रयास का खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और अधिक दक्षिण होने के प्रयास का नतीजा राजीव गांधी और पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सामने आया।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में डॉ. मनमोहन सिंह के सामने दोनों खतरे थे। खुले बाजार का संबंध निश्चित ही दक्षिणपंथी विचार से होता है। डॉ. मनमोहन सिंह खुले बाजार के न सिर्फ प्रशंसक थे बल्कि, उसके समर्थक और कारीगर भी थे। असंतुलन के खतरे को दूर करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) का गठन हुआ। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश सदस्य सचिव थे, देश के कई प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी इसके सदस्य थे। अरुणा रॉय कई वर्षों से सूचना के अधिकार अभियान का नेतृत्व कर रही थीं; ज्यां द्रेज रोजगार गारंटी योजना पर काम कर रहे थे।
यूपीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में आरटीआई और रोजगार गारंटी योजना लागू करने का वादा किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम दिया गया, शायद प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह इसे लागू करने के प्रति उदासीन थे लेकिन सोनिया गांधी की दिलचस्पी मनरेगा में थी और यह लागू हुआ। सूचना के अधिकार (आरटीआई) का कानून भी लागू हुआ। लगता है, प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह की कुछेक उदासीनताओं को भांपकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम में श्रीमती सोनिया गांधी के हस्तक्षेप की बात उठाती रही होगी।
ध्यान देने की बात यह है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की संतुलनकारी भूमिका के कारण ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार दो बार लगातार चुनकर आई। उसके बाद भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपों पर, जिस में अदालतों में कोई दम नहीं पाया गया, विभिन्न आंदोलनों और भारतीय जनता पार्टी के अति उत्साही समर्थकों, आक्रामक प्रचार, दस साल के सत्ता विरोधी रुझान आदि के कारण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) 2014 में चुनाव हार गई। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतना हारना एक आम बात है और कई दृष्टिकोणों से अच्छा भी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने, जो अच्छे दिन लाने के वादा के साथ सत्ता में आई थी, न तो इसे आम रहने दिया और न अच्छा ही रहने दिया।
यह सब ध्यान में लाने की जरूरत इसलिए है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनावों का जीतना भी, हारना भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सक्रिय रखने के लिए आम भी रहे और अच्छा भी रहे! विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार के रहते भी भारतीय जनता पार्टी या उसके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सत्ता से बाहर करना संभव नहीं माना जा रहा था। हां, इंडिया गठबंधन (I.N.D.I.A – इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इनक्लुसिव अलायंस) का सारा चुनावी संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर बहुमत पाने से रोकने का है। ऐसे में चुनाव नतीजों के बाद भी विपक्षी गठबंधन के एक या दो घटक दलों का समर्थन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सरकार बनाने के लिए जरूरी होने पर मिलता ही।
हमारे अधिकतर दलों के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। कुछ के ऊपर तो गंभीर आरोप हैं। प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र को बिना किसी भेद-भाव के ‘पवित्र’ करने की उम्मीद बहुतों को थी। वे खुद ऐसे सामाजिक संवर्ग और आर्थिक वर्ग से आते हैं कि बहुतों को उम्मीद थी कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान करेंगे। ऐसे लोग निराश हुए हैं। इतने बड़े बहुमत और समय मिलने के बाद वे किसी और ही ‘खेल’ में लग गये। यह ‘खेल’ बंद हो, इसलिए विपक्षी गठबंधन को अधिक मजबूती के साथ चुनाव में उतरना चाहिए।
चुनाव के मैदान में विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाये या उस संगम स्थल की तलाश की जाये, जहां विचारधारा और भावधारा दोनों की साझी जमीन पर प्रवाहित रहती है! भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी को विचारधारा और भावधारा दोनों की साझी जमीन दिख सकती है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस हमेशा, कई बार गलत कारणों से भी, ‘अविश्वास और आरोपों’ के दायरे में रही है। न जाने क्यों! जब तक पता चले, तब तक पढ़िये भीष्म साहनी के उपन्यास ‘तमस’ का एक प्रसंग, साभार –
“मीटिंग शुरू हुई।
फिर अंतिम आइटम सामने आया : सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाना।
यह मीटिंग नहीं हो सकेगी – एक साथी बोला।
कांग्रेस के दफ्तर पर ताला चढ़ा है। लीग वालों से बात करो तो पाकिस्तान के नारे लगाने लगते हैं। वे हर बात पर कहते हैं, पहले कांग्रेस वाले कबूल करें कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, फिर हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और इस वक्त तो अपने-अपने मुहल्लों से कोई बाहर नहीं आ रहा। मीटिंग किसके साथ करोगे।”