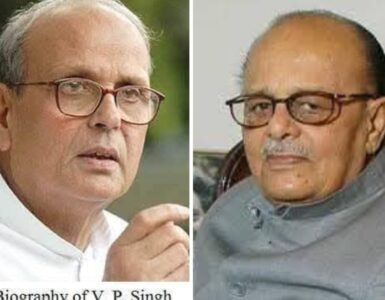विद्या भूषण रावत
पिछले दिनों दो बड़ी घटनाओं के चलते फिर एक पुरानी बहस खड़ी हो गई, जो रह-रह कर मुखर होती रहती है। यह बहस मीडिया से संबंधित है और हम सभी जानते हैं कि आमजनों में नॅरेटिव बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। यह कहा जाना भी अतिशयोक्ति नहीं कि जिसकी मीडिया होगी उसका नॅरेटिव चलेगा।

एक सीधा सा मतलब यह भी कि आज के दौर में सत्ता घटनाओं की तथ्यपरक रिपोर्टिंग से नहीं आती, बल्कि नॅरेटिव के हिसाब से और सुविधानुसार परोसी गयी खबरों से आती है। नई दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क (एनडीटीवी) पर अडाणी समूह के कब्जे के बाद उसके एक प्रमुख चेहरा रहे रवीश कुमार ने भी त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद से ही सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई गोया भारत में मीडिया ही खत्म हो गई।
अब दूसरी तस्वीर यह कि रवीश कुमार का नायकत्व बरकरार रहा है और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसके सब्स्क्राइबरों की संख्या संक्षिप्त अवधि में ही तीस लाख से ऊपर जा पहुंची है। इसके पहले आरएसएस समर्थकों ने उनका मज़ाक उड़ाया और कहा कि वे बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी तरफ बेचारे ‘उदारवादी’ उनकी ‘नौकरी’ जाने से दुखी और उनके लिए पैसा जुटाने तक को तैयार दिखे।

जाहिर तौर पर भारत में ऐसे फिजूल की बहसों में समय जाया करने में लोगों को विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन जो मीडिया की समझ रखते हैं, वे इतना तो जानते हैं कि एनडीटीवी जैसा संस्थान बिना बड़े पूंजीपति के चल नहीं सकता। इस हकीकत को भी समझा जाना चाहिए कि जब भारत मे इलेक्ट्रानिक मीडिया पत्रकारिता की शुरुआत हो रही थी, तब वह दौर था जब भारत में सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से दूर होना शुरू कर रही थीं और ‘वैश्वीकरण’ या ‘निजीकरण’ जैसे शब्द लोगों के शब्दकोश में आने लगे थे। हालांकि ‘निवेश’ जैसा शब्द तब भी बाहर ही था। 1982 में एशियन गेम्स के समय भारत में रंगीन टीवी ने घरों में प्रवेश किया और 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर मे सिख विरोधी दंगों में ‘खून का बदला खून से लेंगे’ जैसे नारे जो लगातार दूरदर्शन पर दिखाए जाते रहे। दंगों में इनका योगदान भी कम नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ दिनों तक दूरदर्शन पर लगातार उनकी हत्या और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों ने दूरदर्शन के जरिए देश भर मे एक सिख विरोधी राष्ट्रवाद पैदा किया, जिसका भरपूर लाभ कांग्रेस को आम चुनावों मे हुआ और राजीव गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीते।

वर्ष 1985 के बाद से भारत सरकार ने दूरदर्शन को थोड़ी आजादी दी और उसमें मनोरंजन के नए-नए कार्यक्रम जोड़े गए। धारावाहिकों की शृंखला मसलन, ‘हमलोग’, ‘बुनियाद’, ‘ये जो है जिंदगी’ आदि का प्रसारण लोगों को टीवी की दुनिया से जोड़ने में कामयाब रहा। फिर संस्कृति और धर्म के नाम पर रामानंद सागर द्वारा निर्देशित ‘रामायण’ धारावाहिक की शुरुआत हुई, जिसने अपार लोकप्रियता हासिल की। इस एक धारावाहिक ने दूरदर्शन को घर-घर पहुंचा दिया और फिर तो सरकार को भी इसमें ‘अवसर’ नजर आयी और लगे हाथ बी. आर. चोपड़ा को ‘महाभारत’ बनाने की जिम्मेवारी सौंप दी गई। इसने भी सफलता के नए आयाम पैदा कर दिए।
इधर सांस्कृतिक रंग लोगों पर चढ़ाया जा रहा था तो दूसरी और खबरों के नाम पर ‘जनवाणी’ जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। आम चुनावों का लाइव विश्लेषण प्रणय रॉय और विनोद दुआ के जरिए शुरू हुआ, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। नेताओं को टीवी पर आकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए लोगों को अच्छा लगता था। यही वह दौर था जब राजीव गांधी प्रेस को नियंत्रित भी करना चाहते थे।
इसी दौर मे प्रणय रॉय ने एनडीटीवी की स्थापना कर ली थी और दूरदर्शन में उनका एक शो ‘द न्यूज टूनाइट’ और ‘वर्ल्ड दिस वीक’ का प्रसारण शुरू हुआ। ये कार्यक्रम भी बेहद लोकप्रिय हुए। जबकि यह खबरों को निजी हाथों में देने की शुरुआत थी।
हालांकि उस दौर में यह पता नहीं था कि ‘खबरों का निजीकरण’ बाद में इतना खतरनाक हो जाएगा कि न्यूज चैनल खबरों का कारोबार शुरू कर देंगे।
फिर आया 1990 का दशक। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करने और पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा क्या हुई कि वे सबसे घृणित नेता बना दिए गए। प्रभुत्ववादी ताकतों ने आरक्षण की काट का मंत्र ढूंढ लिया था और वह था निजीकरण का मंत्र। इसके लिए मीडिया एक ऐसा हथियार था, जो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकता था। चूंकि सरकारी टीवी ‘दूरदर्शन’ के जरिए कई काम नहीं हो सकते थे, इसलिए ‘निजी खिलाड़ियों’ को आगे किया गया। प्रणय रॉय इसी नई आर्थिक नीतियों की उपज रहे हैं। इसके पहले वह दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में अध्यापन करते थे और धीरे-धीरे मीडिया से उनका जुड़ाव बढ़ा।
नब्बे के दशक के आखिर में एनडीटीवी को दूरदर्शन पर अंग्रेजी में न्यूज प्रोग्राम मिला। हिंदी में यह जिम्मेदारी ‘आज तक’ के पास थी। और फिर धीरे-धीरे अपने संपर्कों के जरिए एनडीटीवी इलेक्ट्रानिक मीडिया का बादशाह बन गया। चैनल ने अपने ‘सेक्यूलर’ चरित्र को बनाए रखा। हालांकि यह एक भद्रलोक का चैनल ही था, जिसमें आने के लिए सरकार के मंत्री तक उतावले रहते थे।
एनडीटीवी में एक दौर में वे ही लोग थे, जो किसी नेता या आला अधिकारी से जुड़े हुए थे। जब तक इलेक्ट्रानिक मीडिया में अधिक कंपनियां नहीं थीं। एक तरह से एनडीटीवी का एकाधिकार ही था, लेकिन धीरे-धीरे प्रिन्ट मीडिया के बड़े बादशाह और अंबानी जैसे कारोबारी भी इसमें कूद गए।
वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद एनडीटीवी के हालात थोड़े बुरे हो गए। वह सरकार के निशाने पर था।। लेकिन इसके पहले से ही बुनियादी आर्थिक सवालों को लेकर एनडीटीवी की नीति अस्पष्ट और ढुलमुल रही।
दरअसल, आर्थिक तौर पर एनडीटीवी के रवैये में मोदी सरकार से कोई मतभेद नहीं था। एनडीटीवी भी अन्य चैनलों की तरह मुक्त बाजार का हामी था और केवल अंतर इतना था कि एनडीटीवी के लोग थोड़ा संभल कर बोलने की कोशिश करते और दूसरे यही काम चिल्ला-चिल्ला कर करते।
फिलहाल यह सोच लेना कि एनडीटीवी भारत के दलित-पिछड़ों के सवालों को ईमानदारी से उठाएगा या किसी ‘नायक’ ने उसे बेहद समझदारी से उठाया है, तो मतलब साफ है कि इस देश के दलित-बहुजन जरूरत से ज्यादा भोले हैं।
जोतीराव फुले हों या पेरियार अथवा डॉ. आंबेडकर, सभी ने अपने पत्र-पत्रिकाएं निकालींलीं और लोगों से सीधे संवाद किया। फिर आजादी के बाद से ही आंबेडकरवादियों ने विभिन्न पत्र-पत्रिकाएं निकालीं, क्योंकि तथाकथित मुख्य धारा के अखबारों में उनके लिए जगह नहीं थी।
यहां तक कि 1970-80 के दशक में भी ‘भीम पत्रिका’ से लेकर, ‘दलित वॉयस’ जैसी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और इनका फोकस खबरों से अधिक आंबेडकरवाद को मजबूत करने में था। 1990 में भी मंडल कमीशन के समय आंबेडकरवादी पत्र-पत्रिकाएं आरक्षण के सवाल पर सक्रिय थे, लेकिन तकनीकी युग की शुरुआत सदी के शुरुआत में हुई जब इंटरनेट की क्रांति हुई और लोगों ने ब्लॉग लिखने शुरू किये। उस दौर में जो सबसे प्रभावशाली पत्रिका आई, वह थी– ‘राउंड टेबल इंडिया’, जो आंबेडकरवादी विचाराधारा का मुखपत्र बन गई। मुझ जैसे लोग भी जो ‘दलित वॉयस’ और ‘भीम पत्रिका’ पढ़कर आंबेडकरवादी आंदोलन की समझ बना सके थे, उनके लिए मनुवादी मीडिया से कोई संवाद संभव नहीं था। दलित-बहुजन पत्रिकाएं मनुवादियों से संवाद नहीं कर रही थीं, अपितु अपने-अपने समाज में आंबेडकरवादी एजेंडा चला रही थीं। एक हिसाब से यह भी बेहद महत्वपूर्ण था।
आज देश भर में आंबेडकरवाद की धूम मचाने का दावा करनेवाले बड़े विशेषज्ञ, चाहे वे विश्वविद्यालयों में बैठे विद्वान हों या पत्रकार हों, असलियत यही है कि आज जो स्थिति है उसके पीछे भगवान दास, लाहोरी राम बाली, वी. टी. राजशेखर, राजा ढाले, जे. वी. पवार, विजय सुरवाड़े, के. जमनादास, एन. जी. उइके जैसे लोगों के संघर्षों और लेखनी है।
1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का सत्ता में आना एक बड़े बदलाव की आहट थी और उत्तर भारत में हिंदी के अखबारों ने इस बदलाव का रूख मोड़ने के लिए अनेक खेल खेले। राममंदिर आंदोलन में अखबार खुलकर कूदे तो दूसरों ने आंबेडकरवाद के नाम पर नए लोगों को अपने यहां मंच प्रदान किया। आज के नामी आंबेडकरवादियों की लेखन की शुरुआत हिंदी दैनिक ‘राष्ट्रीय सहारा’ के ‘हस्तक्षेप’ कॉलम से शुरू हुई थी, लेकिन उस दौर मे भी पुराने प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने ब्राह्मणवादी मीडिया के साथ किसी भी प्रकार का संवाद करने से इनकार कर दिया।
कांशीराम जैसे लोगों ने कभी भी अपने आपको ब्राह्मणवादी पूंजीवादी मीडिया के अनुसार नहीं ढाला। उनका फोकस अपने समाज और उसमें हो रहे बदलाव पर था।
उत्तर भारत में दलित-पिछड़ों में बदलाव को बढ़ाने में और नए लेखकों को अवसर देने मे द्विभाषी पत्रिका ‘फारवर्ड प्रेस’ के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसी प्रकार इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ‘हम दलित’ भी देश के विभिन्न हिस्सों मे विशेषकर हिंदी पट्टी में वंचित समाज के मध्य बड़ी मजबूती से जा रही थी। अब इसका नाम ‘हाशिए की आवाज’ कर दिया गया है।
2014 के बाद भारत में सोशल मीडिया का बहुत जोर रहा। हिंदुत्ववादी शक्तियों ने तो इसे पहले ही समझ लिया था और इसके जरिए देश को एक ‘नया इतिहास’ बताया जा रहा था। ब्लॉगिंग का युग जा चुका था और फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का युग आ गया। जब मीडिया में भी काम करना बंद हो गया तो कई पत्रकारों ने यूट्यूब चैनल बना लिये। आज हजारों ऐसे यूट्यूब चैनल हैं। अधिकांश अपने जातिगत, धर्मगत पृष्भूमियों से संबद्ध हैं।
इसीलिए जो लोग रवीश कुमार के एनडीटीवी छोड़ने से यह महसूस कर रहे थे कि अब भारत मे लोकतंत्र खतरे में है, उनसे पूछा जाय कि क्या एनडीटीवी इसलिए खराब हो गया, क्योंकि उसे अडाणी ने खरीद लिया? क्या जब अंबानी ने दस वर्ष पूर्व इसमें निवेश किया था तो उन्होंने कोई शर्ते नहीं रख होंगी?
मूल सवाल यह है कि हिंदी चैनलों में दलित-पिछड़ों की कितनी भागीदारी है? अगर एनडीटीवी में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नए युवाओं को मौका दिया जाता तो निश्चित तौर पर उनकी असली उपलब्धि होती।
दुखद बात यह है जैसे मनुवादी मीडिया अपनी पहुंच बनाने के लिए तमाम तरह की तिकड़में करती हैं, वैसे ही दलित-बहुजनों के वैकल्पिक मीडिया में भी किया जा रहा है। पहुंच बढ़ाने के लिए हर खबर को मसाला लगाकर छाप देना ही मुख्य धर्म हो गया है। अब चर्चा समाज में एक सकारात्मक सोच के साथ बदलाव की नहीं, अपितु ब्राह्मण बनाम गैर-ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा आदि की बाइनरी में ही धारणाओं को रखा जा रहा है। संवाद अब समुदाय से नहीं है, अपितु ब्राह्मणों और सवर्णों से है। जाहिर तौर पर रोज रोज किसी अखबार की खबर पढ़कर उसे सोशल मीडिया पर चिपका देने मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि किसी खबर या घटना पर लगातार फॉलोअप करने से होगा।
(विद्याभूषण रावत सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और डाक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं। उनकी कृतियों में ‘दलित, लैंड एंड डिग्निटी’, ‘प्रेस एंड प्रेजुडिस’, ‘अम्बेडकर, अयोध्या और दलित आंदोलन’, ‘इम्पैक्ट आॅफ स्पेशल इकोनोमिक जोन्स इन इंडिया’ और ‘तर्क के यौद्धा’ शामिल हैं। उनकी फिल्में, ‘द साईलेंस आॅफ सुनामी’, ‘द पाॅलिटिक्स आॅफ राम टेम्पल’, ‘अयोध्या : विरासत की जंग’, ‘बदलाव की ओर : स्ट्रगल आॅफ वाल्मीकीज़ आॅफ उत्तर प्रदेश’ व ‘लिविंग आॅन द ऐजिज़’, समकालीन सामाजिक-राजनैतिक सरोकारों पर केंद्रित हैं और उनकी सूक्ष्म पड़ताल करती हैं।)