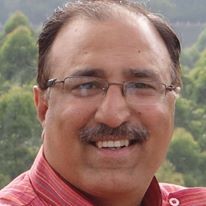सत्येंद्र रंजन
डॉ. मनमोहन सिंह ने 15 साल तक (पांच वर्ष वित्त मंत्री और दस साल प्रधानमंत्री के रूप में) प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रशासन (अथवा प्रबंधन) संभाला। उसके अलावा 18 अन्य वर्षों में भी परोक्ष रूप से उनका साया आर्थिक प्रबंधन पर रहा है।
मतलब यह कि पिछले 33 साल वो नीतियां अनवरत आगे बढ़ी हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में डॉ. सिंह का मूल्यांकन उनकी इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
कोई व्यक्ति, जिस आर्थिक (या अन्य) व्यवस्था का प्रतीक हो, अगर वह इतने लंबे समय तक एकरेखीय दिशा में चलती रहे और उसके बाद भी उसके सामने कोई ठोस या व्यावहारिक चुनौती उभरती ना दिखे, तो इतिहास में उसके स्थान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हर व्यक्ति का मूल्यांकन उसके समय के मद्देनजर होता है। मगर इस सिलसिले में ज्यादा महत्त्वपूर्ण पहलू उस व्यक्ति के योगदान का परिणाम होता है।
इसलिए डॉ. सिंह जिस समय भारत के आर्थिक प्रबंधन के केंद्र में आए, उसे समझना अहम है। अपनी उस भूमिका में उन्होंने जो किया, वह महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अहम यह देखना होगा कि उनके योगदान के अल्पकालिक एवं दूरगामी नतीजे क्या हुए।
मनमोहन सिंह के निकट रहे लोग उनकी कई निजी खूबियों का जिक्र करते हैं। अपनी मारुति 800 कार से उनके लगाव की कथा अक्सर सुनाई जाती है, जिसमें संदेश यह होता है कि वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वे अपने को आम मध्यवर्गीय भारतीयों का हिस्सा मानते रहे।
उनके अहंकार मुक्त स्वभाव की चर्चा भी की जाती है, और इस बात की भी, कि व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। ये सब अच्छे गुण हैं, जिनका किसी व्यक्ति में होना बेशक उसे सर्व-प्रिय बनाता है।
मगर व्यक्ति की ऐतिहासिक भूमिका का विश्लेषण करते समय ये खूबियां खास मायने नहीं रखतीं। तब अर्थ सिर्फ उसका योगदान और उस योगदान के प्रभाव या परिणाम रखते हैं। इस दौरान महत्त्व सिर्फ तथ्यों का होता है।
मनमोहन सिंह के योगदान पर विचार करते समय सबसे पहले तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि असल में वे एक टेक्नोक्रेट थे, जिन्हें समय के तकाजे ने राजनीति में संभवतः सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका में ला दिया। तो खास सवाल हैः वो समय क्या था और उसके तकाजे क्या थे?
हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का पूरा श्रेय मनमोहन सिंह को दिया जाता है, मगर यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि उनके वित्त मंत्री बनने से तकरीबन छह साल पहले से बननी शुरू हो गई थी।
राजीव गांधी के दौर में पेश बजटों में इस ओर जाने की झलक देखी जा सकती है। वीपी सिंह और चंद्रशेखर के समय तो इस अर्थव्यवस्था के “खुलेपन” की खुली वकालत देखने को मिलने लगी थी।
वीपी सिंह सरकार के वित्त मंत्री मधु दंडवते ने अपने बजट को स्वीकार्य बनाने के लिए यह जुमला प्रचलित किया था कि ‘बर्लिन की दीवार गिर चुकी है।’ संदर्भ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (पूर्वी जर्मनी) के ढहने, बर्लिन को बांटने वाली दीवार को तोड़े जाने और पश्चिमी जर्मनी के साथ उसके एकीकरण का था।
कुल मिला कर प्रतीकात्मक रूप में समाजवाद के सोवियत मॉडल की हिल रही जड़ों को संदर्भ बनाया गया। पीवी नरसिंह राव सरकार के सत्ता में आने और मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने तक यह संदर्भ अत्यधिक स्पष्ट हो चुका था।
भारत की अर्थव्यवस्था गहराई से सोवियत संघ से जुड़ी हुई थी। वहां 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुए बदलावों का खराब असर भारत पर पड़ा। जिस भुगतान संतुलन के संकट का जिक्र किया जाता है और जिससे उबारने का श्रेय डॉ. सिंह को दिया जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में इस युगांतकारी घटनाक्रम का बड़ा रोल था।
वैसे भी तजुर्बा यह है कि हर आर्थिक व्यवस्था में 30 से 40 साल में नवीकरण या फिर उसमें नए प्रयोग और आविष्कार का तकाजा पैदा होता है। नेहरूवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा तकाजा 1970 के दशक के मध्य से जाहिर होने लगा था। इसे पूरा ना करने का परिणाम वह संकट था, 1990 तक देश जिसमें आकर फंस गया। वहां से एक नई शुरुआत की जरूरत थी।
सवाल सिर्फ यह था कि ये शुरुआत कैसी हो? पुरानी आर्थिक नीतियों ने जो नया अभिजात्य या शासक वर्ग पैदा किया था, क्या सिर्फ उसके हितों और सपनों के आगे समर्पण कर दिया जाए या फौरी तौर पर कुछ समझौतावादी कदम उठाते हुए भी ‘समाजवादी ढंग के विकास’ लक्ष्यों के अनुरूप प्रयोग किए जाएं?
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, जिस समय अमेरिका ‘इतिहास के अंत’ और एकध्रुवीयता की स्थापना का एलान कर रहा था, उस समय ‘समाजवादी’ लक्ष्यों के अनुरूप प्रयोग की दिशा में जाना एक अतिमानवी चुनौती थी- खासकर उस देश में, जहां के शासक हलकों में वैचारिक रूप से इन लक्ष्यों की जड़ें हमेशा सतही ही रही थीं।
आर्थिक क्षेत्र में ‘इतिहास के अंत’ को स्थायित्व देने के लिए एकध्रुवीयता की प्रतिनिधि संस्थाओं- विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने फॉर्मूले ढांचागत समायोजन (structural adjustment) के रूप में ग्लोबल साउथ पर थोपने शुरू किए थे।
इस क्रम में ये संस्थाएं किसी तरह की वित्तीय मदद देने के पहले शासन की कमान ‘विश्वसनीय चेहरे’ के हाथ में चाहती थीं। उस मांग को पूरा करने के लिए नरसिंह राव ने टेक्नोक्रेट मनमोहन सिंह के हाथ में आर्थिक कमान दे दी।
अब चुनौती यह थी कि इस नए बने दबाव में हथियार डाल दिए जाएं या एक कदम पीछे हट कर उचित समय पर दो कदम आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जाए।
यहां ये उल्लेख जरूरी है कि वित्त मंत्री बनने से ठीक पहले मनमोहन सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ से बनाए गए साउथ कमीशन के महासचिव थे।
इस आयोग के अध्यक्ष तंजानिया के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और पूर्व राष्ट्रपति जुलियस न्येरेरे थे। आयोग 1987 में बना। 1990 में उसने अपनी रिपोर्ट दी।
इस रिपोर्ट का शीर्षक था- दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की चुनौतियां। आयोग ने उपनिवेशवादी शिकंजे को तोड़ कर आजाद हुए विकासशील देशों पर नव-उपनिवेशवाद के कायम हुए शिकंजे के प्रभावों का अध्ययन किया।
इसने विकासशील देशों में आत्म-निर्भरता और जन-केंद्रित विकास के बारे में अपने सुझाव दिए। इस कार्य के लिए ग्लोबल साउथ के देशों में आपसी सहयोग पर उसने जोर दिया।
इस प्रक्रिया से निकल कर आए मनमोहन सिंह से यह अपेक्षा रखने का तार्किक आधार था कि वे आईएमएफ की मंशाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे। उनसे अपेक्षा थी कि क्षणिक समझौता करते हुए भी वे भारत की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा एवं जन-केंद्रित विकास की जरूरतों के मुताबिक नीतियों का आविष्कार करेंगे।
डॉ. सिंह के मूल्यांकन के क्रम में यह बेरहम तथ्य हमारे सामने है कि इसका प्रयास करने के बजाय उन्होंने जो नीतियां अपनाईं वे साउथ कमीशन की रिपोर्ट की भावना के विपरीत थीं।
इस आलोचना में दम है कि अपनाई गई नीतियों के जरिए भारत ने आईएमएफ के नव-उदारवादी एजेंडे के आगे समर्पण कर दिया। भारतीय बाजार को बहुराष्ट्रीय पूंजी के लिए बिना शर्त खोल दिया गया, जबकि पड़ोस में चीन ने तकनीक एवं ज्ञान के ट्रांसफर की शर्तों के साथ अपना बाजार उसी दौर में खोला।
नतीजा यह है कि चीन आज तकनीक एवं आत्म-निर्भर उत्पादन के क्षेत्रों में महाशक्ति बन गया है, जबकि भारत अमेरिकी हाई टेक कंपनियों का बेलगाम बाजार बना हुआ है।
आईएमएफ का एजेंडा दरअसल, वॉशिंगटन सहमति (Washington Consensus) नाम से चर्चित नीतियों का ही व्यावहारिक रूप था, जिसका मकसद विश्व अर्थव्यवस्था को अमेरिकी हितों के अनुरूप ढालना था।
भारतीय जन मानस में इसे स्वीकार्य बनाने के लिए डॉ. सिंह ने फ्रेंच साहित्यकार और चिंतक विक्टर ह्यूगो की एक मशहूर उक्ति का हवाला जुलाई 1991 में दिए अपने बजट भाषण में दिया। उक्ति हैः An idea whose time has come cannot be stopped. यानी जिस विचार का समय आ गया हो, उसे रोका नहीं जा सकता।
डॉ. सिंह का तात्पर्य था कि उदारीकरण- निजीकरण- भूमंडलीकरण की नव-उदारवादी परियोजना का समय आ गया है, जिसे कोई नहीं रोक सकता।
इस तरह उन्होंने देश में लाचारी का वातावरण बनाने में योगदान किया। उन्होंने जो संदेश दिया, वह दरअसल उसके एक दशक पहले ब्रिटेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के दिए संदेश का दूसरे रूप में दोहराव था। थैचर ने इन नीतियों को स्वीकार्य बनाने के लिए ही कहा था- There is no alternative यानी कोई और विकल्प नहीं है।
गौरतलब है कि नव-उदारवादी परियोजना के आर्थिक चेहरे अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन कहे जाते हैं, वैसे ही इसके सियासी चेहरे रॉनल्ड रेगन (अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति) और थैचर हैं। इसीलिए इन नीतियों को रेगन-थैचर नीति भी कहा जाता है। भारत में मनमोहन सिंह वो चेहरा बने।
इस दिशा को चुनने के बाद जो हुआ, वह ज्ञात इतिहास है। जब किसी एक दिशा में आप चल देते हैं, तो उससे जहां पहुंचा जा सकता है, वहीं पहुंच सकते हैं।
आर्थिक नीतियों में वॉशिंगटन सहमति पर राजी होने के बाद विदेश नीति में ऐसा नहीं होता, यह संभव नहीं था। तो उस दिशा में बदलाव का चरम बिंदु भी डॉ. सिंह की सदारत में ही संपन्न हुआ, जब 2008 में भारत ने अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया।
इन तमाम नीतियों का क्या परिणाम हुआ है, उस बारे में नजरिया इससे तय होता है कि समाज के किस वर्ग से आप आते हैं। नए दौर में निवेशक और “वेल्थ क्रियेटर” नए देवता बन गए। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का उन्होंने खूब फायदा उठाया है।
पूंजीपतियों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार या द्वि-अधिकार (duopoly) कायम कर लिए हैं। जो लोग 1990 के दशक तक मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग का हिस्सा बन चुके थे, उन्हें भी इन नीतियों से लाभ हुआ।
आरंभिक दिनों में बाजार के हुए विस्तार से उनके लिए नए अवसर बने। चूंकि सामाजिक नेरैटिव पर इन्हीं वर्गों का नियंत्रण होता है, तो उनके बीच मनमोहन सिंह की देवता जैसी छवि बनना स्वाभाविक ही है।
इन नीतियों को स्वीकार्य बनाने के लिए आईएमएफ-वर्ल्ड बैंक ने गरीबी की परिभाषा बदल कर उसे मापने के लिए न्यूनतम कसौटियां तय कीं। उसी आधार पर तथ्यों के विरुद्ध यह दावा किया जाता है कि नव-उदारवादी व्यवस्था में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया।
लेकिन ये दावे सिरे से विवादास्पद हैं। हकीकत है कि इस दौर में विषमता बढ़ी है, जबकि तमाम सेवाओं के निजीकरण ने आम शख्स के लिए अवसरों को संकुचित किया है।
और यह केवल भारत की कहानी नहीं है। इन नीतियों ने जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतों की आर्थिक जड़ें खोखली कर दी हैं, तो फिर भारत जैसे विकासशील देश में जो हुआ, वह कोई हैरत की बात नहीं है। इस परिघटना को समझने के क्रम में असल सवाल यह है कि हम आर्थिक विकास से समझते क्या हैं?
हमारी निगाहें इन नीतियों को हर हाल में कामयाब दिखाने के लिए गढ़े गए पैमानों से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो बेशक हम इस दौर का उत्सव मना सकते हैं।
मगर हमारी सोच के दायरे में देश के सभी लोग हैं, वो बहुसंख्यक आबादी भी, जो अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दी गई है और आज की नीतियों में जिसकी कोई चिंता नहीं की जाती, तो फिर इस दौर का उत्सव मनाने का शायद ही कोई तर्क बचता है।
डॉ. मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत विशेषताएं और प्रधानमंत्री के रूप में उनके अनेक योगदान याद रखे जाएंगे। उनमें पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों पर उनकी दूरदृष्टि और संयम से भरी नीतियां भी थीं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उनकी सरकार ने जो प्राथमिकताएं अपनाईं, उनका स्वाभाविक परिणाम चीन के साथ संबंधों में पेच पड़ना था।
फिर भी ये कहा जाएगा कि उग्र राष्ट्रवाद या जज्बाती सियासत को हवा देने से डॉ. सिंह बचे और थोक भाव से जन कल्याण को नहीं ठुकराया। उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद देश में जो हुआ, उसकी रोशनी में उनका दौर एक बड़ी बात लगती है।
फिर यह अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति इतिहास का अंतिम निर्णायक नहीं होता। सिंह ने जो नीतियां अपनाईं उसके लिए उस समय तक बन चुकी राजनीतिक-अर्थव्यवस्था और कांग्रेस पार्टी की नई प्राथमिकताएं भी कम बड़ा कारण नहीं थीं।
कांग्रेस का परिवर्तन गौरतलब है। 1950 के दशक में कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे के विकास (socialistic pattern of development) की वाहक पार्टी बनने का कार्यक्रम अपनाया था।
उस नेहरूवादी दौर को पीछे छोड़ कर नव-उदारवादी युग में वह खुद को शासन की कुदरती पार्टी (natural party of governance) के रूप में देखने लगी।
यानी वह शासक वर्गों की हित रक्षक पार्टी होने का दावा करने लगी। स्वाभाविक है कि तीन W यानी Wealth creation, Work और Welfare कांग्रेस के घोषित लक्ष्य बन गए। जिन्हें अर्थव्यवस्था की समझ है, उन्हें मालूम है कि यह नव-उदारवादी दौर का राजनीतिक कार्यक्रम है।
अब यह विडंबना ही है कि जल्द ही शासक वर्गों ने कांग्रेस को ठुकरा कर अपने हित रक्षक के रूप में सांप्रदायिक एजेंडे की वाहक भाजपा को अपना प्रमुख सियासी औजार बना लिया।
बहरहाल, जो नाकामियां या दुष्परिणाम हैं, उनके लिए डॉ. सिंह को अकेले दोषी ठहराना उनके साथ न्याय करना नहीं होगा।
मनमोहन सिंह कोई सियासतदां नहीं थे। वे एक टेक्नोक्रेट थे। यह कांग्रेस का निर्णय था कि अब किस दिशा में जाना है।
उस दिशा की तरफ ले जाने के लिए उसे डॉ. सिंह सबसे योग्य संचालक नजर आए। इस भूमिका को डॉ. सिंह ने बखूबी निभाया। इतनी खूबी की साथ कि उनकी देखरेख में शुरू हुईं नीतियां आज पूरी आम सहमति के साथ भारत की शासन-नीति बनी हुई हैं।
तो साफ है कि डॉ. सिंह जिन नीतियों का चेहरा हैं, उनका प्रभाव उनके अपने निजी व्यक्तित्व से भी कहीं अधिक विराट रूप में हमारे सामने मौजूद है। उसकी प्रति विचारधारा कहीं है भी, तो उसका वजूद हाशिये पर ही है।
(