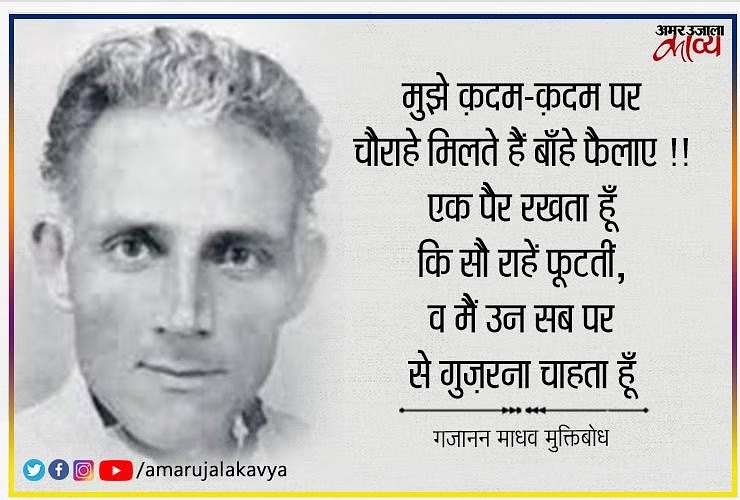मनीष आजाद
मुक्तिबोध की बेचैनी अन्य महत्वपूर्ण कवियों की तरह सिर्फ़ यह नहीं है कि दुनिया ऐसी क्यों है, बल्कि यह भी है कि मैं ऐसा क्यों हूं.
इसलिए उनकी तमाम रचनाएं इन्हीं दो दुनिया की आपसी जद्दोजहद से उपजी हैं. इसलिए मुक्तिबोध की रचनाएं बेहद ईमानदार रचनाएं हैं. अपने बारे में उनकी स्वीकारोक्ति देखिये –
‘हाय-हाय औऱ न जान ले
कि नग्न और विद्रूप
असत्य शक्ति का प्रतिरूप
प्राकृत औरांग…उटांग यह
मुझमें छिपा हुआ है.’ (दिमागी गुहान्धकार का ओरांग उटांग)
पूंजीवादी समाज के बारे में उनकी दृष्टि बहुत साफ है –
‘तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ
तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ.
तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध
तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र’ (पूंजीवादी समाज के प्रति)
लेकिन असल सवाल तो यह है कि पूंजीवादी समाज बदलेगा कैसे ? इसे कौन बदलेगा, इस जद्दोजहद में एक सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति की भूमिका क्या है ?
मुक्तिबोध की बेचैनी का उत्स यहीं से आता है इसलिए उनकी बेचैनी बेहद रचनात्मक बेचैनी है. दरअसल मुक्तिबोध उस पीढ़ी से आते हैं, जिसने भारत की ‘आज़ादी’ में अपना स्वप्न निवेश किया था. यह स्वप्न था –
‘मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में
सभी मानव
सुखी, सुन्दर व शोषण-मुक्त
कब होंगे ?’ (चकमक की चिनगारियां)
लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया इस स्वप्न पर जाला पड़ने लगा. यह समय ‘मोहभंग’ का नहीं बल्कि ‘स्वप्नभंग’ का था और यहीं से मुक्तिबोध की बेचैनी भी बढ़ने लगी.
बेचैनी उस स्वप्न को बचाने की, उस स्वप्न को जीवन देने की.
मुक्तिबोध एक समर्पित मार्क्सवादी थे इसलिए कहीं न कहीं वे अपने उस ‘स्वप्न’ को उस वक़्त की सीपीआई (CPI) से जोड़ कर देखने को मजबूर थे लेकिन अभी वह यह नहीं देख पा रहे थे कि सीपीआई ने इस ‘स्वप्न’ को यानी ‘क्रांति के प्रोजेक्ट’ को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.
इस संदर्भ में मुक्तिबोध की सीपीआई के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी ‘श्रीपाद अमृत डांगे’ को लिखी चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मुक्तिबोध ने तत्कालीन सीपीआई की रणनीति पर बहुत से तीखे सवाल उठाए हैं. वे लिखते हैं –
‘प्रतिक्रिवादी हमलों ने आज जो सफलता अर्जित की है, वो सिर्फ प्रेस की आर्थिक ताकत के कारण नहीं है, न ही यह सिर्फ कम्युनिस्ट विरोधी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ उनके वैचारिक रिश्तों के कारण है और न ही यह सिर्फ मध्य वर्ग में जड़ जमा चुके अवसरवादी रुझानों के कारण है. बल्कि यह प्रगतिशील आन्दोलन की भीतरी कमजोरियों और विशेषकर इसके नेतृत्व के पुराने पड़ चुके दृष्टिकोण के कारण भी है.’
हालांकि इस पत्र से यह भी पता चलता है कि मुक्तिबोध सीपीआई की वैचारिक सीमाओं को अभी ठीक से पूरी तरह पहचान नहीं पा रहे थे. दरअसल उस वक़्त यह मुश्किल भी था.
सीपीआई के यथास्थितिवादी/संशोधनवादी राजनीति से पूरी तरह मुक्त न हो पाने का ही परिणाम था कि हिंदी के कुछ अन्य प्रगतिशील रचनाकारों की तरह ही मुक्तिबोध के यहां भी जाति का दंश या उसके चित्र प्रायः नहीं मिलते. इस संदर्भ में मुझे फैज़ याद आते हैं, जिनकी रचनाओं में आश्चर्यजनक रूप से विभाजन का दंश या उसकी त्रासदी बहुत कम मिलती है. शायद इसका कारण उनकी यह सोच होगी कि मजदूर या गरीब आदमी सांप्रदायिक या अपने ही जैसे दूसरे गरीब मजदूर के खून का प्यासा कैसे हो सकता है !
इस तर्ज पर मुक्तिबोध को भी लगता होगा कि उनका सर्वहारा जातिवादी कैसे हो सकता है. यह वैचारिक सीमा या विचलन का स्रोत निश्चित रूप से उस वक्त की सीपीआई ही थी.
मुक्तिबोध द्वारा डांगे को लिखे उपरोक्त पत्र को बांग्ला सिनेमा के मशहूर हस्ताक्षर ‘ऋत्विक घटक’ द्वारा सीपीआई को 1954 में लिखे उनके पेपर ‘ON THE CULTURAL ‘FRONT’ के साथ देखने पर हम इन बेहद ईमानदार मार्क्सवादी रचनाकारों की तत्कालीन सीपीआई के साथ तनावपूर्ण रिश्ते और तत्पश्चात उनकी रचनात्मक बेचैनी को अच्छी तरह समझ सकते हैं.
बहरहाल मुक्तिबोध की रचनाएं अपनी बेचैनी में उस वक़्त के ‘वैचारिक किले’ में सेंध लगा रही थी, बाहर निकलने के गुप्त रास्ते बना रही थी, जिनके बारे में शायद मुक्तिबोध भी उतने सचेत नहीं थे, उनके राजनीतिक लेखों से तो यही लगता है.
60 का दशक भारत में हर लिहाज से बहुत मुश्किल दशक था. जैसे जैसे स्वप्न पर जाले बढ़ रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा घना हो रहा था. मुक्तिबोध की रचनाएं इसी दौर में परवान चढ़ी. यही वक़्त था जब उनकी किताब ‘भारतीय इतिहास : सभ्यता और संस्कृति’ पर प्रतिबंध भी लग चुका था. शायद इसीलिए मुक्तिबोध को ‘अंधेरे का कवि’ भी कहा जाता है.
महत्वपूर्ण है कि मुक्तिबोध ने साहित्य की तुलना ‘मशाल’ से न करके ‘लालटेन’ से की है. एक लालटेन अंधेरा तो भगाता ही है, लेकिन रोशनी के वृत के चारों तरफ अंधेरे को इकट्ठा भी कर लेता है, ताकि आप इस अंधेरे का अध्ययन कर सकें, इसकी प्रकृति पहचान सकें. यानी लालटेन की मद्धिम रोशनी में अंधेरे की सघन पड़ताल.
‘अंधेरे में’ इसी लालटेन की मद्धिम रोशनी में तो मुक्तिबोध ने हत्यारे ‘डोमा जी उस्ताद’ के साथ कवियों-कलाकारों-पत्रकारों…..का जुलूस देखा था –
‘चेहरे वे मेरे जाने-बूझे से लगते,
उनके चित्र समाचारपत्रों में छपे थे,
उनके लेख देखे थे,
यहां तक कि कविताएं पढ़ी थीं
भई वाह !
उनमें कई प्रकाण्ड आलोचक, विचारक जगमगाते कवि-गण
मन्त्री भी, उद्योगपति और विद्वान
यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात
डोमाजी उस्ताद
बनता है बलवन
हाय, हाय !!
यहां ये दीखते हैं भूत-पिशाच-काय.
भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब
साफ़ उभर आया है,
छिपे हुए उद्देश्य
यहां निखर आये हैं,
यह शोभायात्रा है किसी मृत-दल की.’
क्या इस मानीखेज दृश्य को मशाल से देखना सम्भव होता ?
डॉ. प्रभाकर माचवे ‘अंधेरे में’ कविता पर बहुत सटीक टिप्पणी करते हुए इसे ‘कविता में गुएरनिका’ (Guernica in verse) की संज्ञा देते हैं. लेकिन हम जानते हैं कि ‘पाब्लो पिकासो’ ने अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग ‘गुएरनिका’ (Guernica) किसी निराशा में नहीं बनायी थी बल्कि फासीवाद के अंधेरे-बर्बर चहरे को सामने लाने के लिए बनाई थी. अपने मुक्तिबोध भी इसी परंपरा से आते हैं.
इसलिए एक कवि से शब्द उधार लेकर कहें तो मुक्तिबोध की रचनाओं का अंधेरा कब्र का अंधेरा नहीं है, जहां ‘निर्मम शांति’ होती है. मुक्तिबोध की रचनाओं का अंधेरा गर्भ का अंधेरा है, जहां तीव्र बेचैनी है. जीवन की असीमित हलचल है. अंधेरे से रोशनी में आने की चरम छटपटाहट है.
ठीक इसी कारण मुक्तिबोध उस अंधेरे में भी अंधेरे से निकलने के ‘गुप्त मार्ग’ को पहचान पा रहे थे –
‘गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूं,
इतने में चुपचाप कोई एक
दे जाता पर्चा,
कोई गुप्त शक्ति
हृदय में करने-सी लगती है चर्चा !!
मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं उसको !
आश्चर्य !
उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व
दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव
पीड़ाएं जगमगा रही हैं.
यह सब क्या है !!’ (अंधेरे में)
भले ही मुक्तिबोध भविष्य की पगडंडी को साफ़-साफ़ न देख पा रहे हो, लेकिन भविष्य में उनका विश्वास बहुत अटूट था. ऐसा नहीं होता तो वे यह ऐलान क्यों करते –
‘हमारी हार का बदला चुकाने आएगा,
संकल्पधर्मी चेतना का रक्तप्लावित स्वर.’
मुक्तिबोध का यह ‘काव्य सत्य’ उनकी मृत्यु के 3 साल बाद 1967 में ‘जीवन सत्य’ में परिणत हो गया, जब सीपीआई-सीपीएम के वैचारिक घटाटोप को नेस्तनाबूद करते हुए भारत के क्षितिज पर ‘बसन्त का बज्रनाद‘ हुआ, यानी नक्सलबाड़ी आंदोलन पैदा हुआ. जाला लग चुके विलंबित स्वप्न को झाड़ा-पोछा गया. उसे साफ़ किया गया. उसमें विविध रंग भरे गए और उसे फिर से गांव-गांव जंगल-जंगल रोपा जाने लगा. लेकिन अफ़सोस कि यह शानदार दृश्य देखने के लिए मुक्तिबोध जीवित न थे.
अगर मुक्तिबोध इस वक़्त जीवित होते तो वे अपनी चर्चित कविता में ज़रूर संशोधन करते और कहते – ‘मुझे पुकारती हुई पुकार मुझे मिल गयी.’