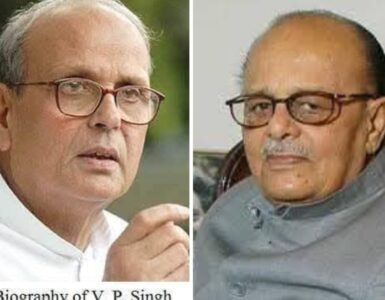रिंकू यादव
मुलायम सिंह यादव संघर्षो़ से उपजे-उभरे जमीनी नेता थे। उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। उन्होंने सामाजिक-राजनीतिक जीवन में सवर्णों के मजबूत प्रभुत्व से जूझते-लड़ते हुए हाशिए की पृष्ठभूमि से उत्पीड़ित समाज की आवाज बनकर 1990 के दशक में नायक के बतौर स्थापित हुए, मसीहाई छवि हासिल की।
मुलायम सिंह यादव ने राममनोहर लोहिया की अगुआई वाले समाजवादी धारा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वे 1967 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (संसोपा) के टिकट पर विधायक बने थे।
दरअसल,1990 के दशक के उथल-पुथल में बहुजन समाज से आने वाले जिन नेताओं ने राजनीतिक मंच पर नायक-मसीहा की छवि ग्रहण की, उन्होंने अपनी भूमिका निभा ली है और अब वे अंतिम विदाई ले रहे हैं। इसे कोई टाल भी नहीं सकता। यह प्रकृति का अटल सत्य है। मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान अब नहीं हैं। लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे नाम मौजूद हैं। इस पीढ़ी ने 1974 के आंदोलन के दौर में नये नेतृत्व के बतौर राजनीतिक मंच पर मजबूती से दस्तक दिया था।
लेकिन, किस भूमिका के कारण मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भी समाज के एक हिस्से के लिए वे घृणा के पात्र हैं? भले ही तमाम रंग की राजनीतिक धाराएं उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं, लेकिन सवर्ण-सांप्रदायिक तत्वों की घृणा आज भी अभिव्यक्त हो रही है।
दरअसल, 1990 का दशक हिंदी पट्टी, खासतौर पर बिहार-यूपी की समाज व राजनीति के लिए एक मोड़ है, जहां से एक नई सामाजिक-राजनीतिक परिघटना सामने आती है, जिसे मंडल परिघटना या उभार के बतौर चिन्हित किया जाता है।लेकिन, यह उभार केवल पिछड़ों तक सीमित नहीं था। पिछड़ों के साथ दलितों-आदिवासियों के राजनीतिक उभार का भी दौर था। इस उभार ने पूरे बहुजन समाज को एकजुट किया। सवर्ण वर्चस्व विरोधी चेतना के आधार पर नये सामाजिक-राजनीतिक समीकरण बना और बहुजन एकजुटता का रास्ता खोला। इसके केंद्र में था मंडल कमीशन की एक अनुशंसा का लागू किया जाना। यह अनुशंसा थी सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण। इसने तत्कालीन राजनीति की दशा-दिशा को बदलकर रख दिया। तब सामाजिक न्याय का प्रश्न राजनीति में महत्वपूर्ण हो गया। उत्पीड़ित समाज के लिए सम्मान-स्वाभिमान के साथ सत्ता का प्रश्न जुड़ गया तथा राजनीति की भाषा और व्याकरण तक बदल गया। इतना ही नहीं, तब विमर्श भी बदल गए और हाशिए पर रहनेवाले पिछड़े, दलितों और आदिवासियों की पहचान महत्वपूर्ण हो गई। इनके मोहल्ले-टोले भी राजनीति की परिधि से केंद्र की ओर आते हैं। वोट डालने में भी मुश्किलें झेलने वाला समाज वोट देने तक सीमित नहीं रहता। राजनीति में बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी की ओर बढ़ता है। इस बदलाव के भीतर से पिछड़ों-दलितों-आदिवासियों के बीच से बड़े पैमाने पर नीचे से ऊपर तक राजनीतिक नेतृत्व उभर कर आता ही है। यह द्विज नेतृत्व के मातहत स्थापित पुरानी राजनीतिक धारा के पिछड़े, दलित व आदिवासी नेतृत्व नहीं होता। ये पुराने दौर के दलित, आदिवासी व पिछड़े नेतृत्व की स्थिति में नहीं होते हैं। इन लोगों की निर्णायक राजनीतिक हैसियत व भूमिका होती है।
मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, शरद यादव, शिबू सोरेन और नीतीश कुमार जैसे नाम इस उभार व बदलाव के प्रतिनिधि व प्रतीक के बतौर सामने आते हैं। ये पिछड़े, दलितों व आदिवासियों की नेताओं के पहचान के साथ इन पहचानों की राजनीतिक दावेदारी के प्रतीक के बतौर सामने आते हैं। दलित, आदिवासी व पिछड़ों की स्वतंत्र राजनीतिक धारा सामने आती है। इन पहचानों के साथ राजनीतिक पार्टियां बनती हैं। इस परिघटना में सवर्णों का राजनीतिक एकाधिकार टूटता है। उत्पीड़ित जाति-समूहों के लिए राजनीति में आगे का रास्ता खुलता है।

यह नयी सामाजिक-राजनीतिक परिघटना थी, जिसे फिर चाहे वह दक्षिणपंथी सवर्ण हों या वामपंथी सवर्ण, सबने जातिवादी राजनीति/अस्मितावादी राजनीति के उभार के बतौर चिन्हित किया।
इस महत्वपूर्ण बदलाव को सवर्ण बुद्धिजीविता ने अपराधी-गुंडों-माफियाओं और भ्रष्टाचार व परिवारवाद के साथ जोड़ दिया। मानो राजनीति में अपराधी-गुंडों-माफियाओं का आगमन और भ्रष्टाचार व परिवारवाद जैसी विकृतियां इन पार्टियों व राजनेताओं के साथ ही उपजा हो! और गोया ब्राह्मणवादी सवर्ण घृणा राजनीतिक शुचिता-नैतिकता के आवरण में अभिव्यक्त हुआ! राजनीति में ऐसे तत्व और ऐसी प्रवृत्तियां पहले से मौजूद थीं।
खैर 1990 के दशक की सामाजिक-राजनीतिक परिघटना ने पुरानी राजनीतिक धाराओं को हाशिए पर डाल दिया। बिहार-यूपी में कांग्रेस आज तक नहीं खड़ा हो पायी है तो वामपंथ की भी जमीन खिसक गयी। वामपंथियों में भाकपा-माले ही कमोबेश अपने जनाधार को बचाकर रख पायी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले दलित-आदिवासी-पिछड़े नीचे ही रह जाते थे, वे हरेक धारा में ऊपर आने और दिखने लगे। वे केवल झंडा ढ़ोने वाले नहीं रहे। वे झोला टांगने तक भी सीमित नहीं रहे। विधानसभाओं से लेकर संसद में तादाद बढ़ने लगी। समाज में तब्दीलियां आईं। जहां वे नहीं दिखते थे, वहां पहुंचने लगे। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास, साहस व स्वाभिमान पैदा हुआ। वे दबने के बजाय तनने लगे। हालांकि जागरण के बुनियाद पर ही सत्ता तक की यह यात्रा हुई थी। जरूर ही इस सामाजिक-राजनीतिक परिघटना की पृष्ठभूमि में लंबे समय में वस्तुगत परिस्थितियां बनी हुई थीं। यह सब एकदम अचानक से नहीं हुआ था।
आज किसी राजनीतिक धारा-पार्टी की हैसियत नहीं रही कि वह आरक्षण का सीधे-सीधे विरोध कर सके। यहां तक कि हिंदुत्व और पूंजीवादी मुखौटे नरेंद्र मोदी को भी अतिपिछड़ा/पिछड़ा की पहचान का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हें मजबूर होकर राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पद पर दलित के बाद आदिवासी को बैठाना पड़ रहा है। असल में मंडल परिघटना से तय हो गया कि अब उत्पीड़ित जाति-समूह को सीधे सवर्ण नेतृत्व कबूल नहीं हो सकता। उन्हें अपना नेता चाहिए। अपने समाज की भागीदारी चाहिए।
मंडल उभार के जवाब में ब्राह्मणवादी-सवर्ण शक्तियों की ओर से आरएसएस के द्वारा संचालित प्रतिक्रियावादी मुहिम का केंद्र उत्तर प्रदेश ही बना। आगे मोर्चे पर मुलायम सिंह को ही होना था। मुलायम सिंह यादव 1989 में मुख्यमंत्री बने थे। यूपी ही बसपा के उभार का भी केंद्र था। खासतौर पर यूपी में सवर्णों के राजनीतिक वर्चस्व को दो छोर से चुनौती मिली थी। पिछड़ों के छोर से अगुआई मुलायम सिंह यादव ने की तो दलितों के छोर से कांशीराम-मायावती ने की। जबकि आरएसएस द्वारा संचालित मुहिम के केंद्र में राम और मंदिर होता है। ‘मंदिर वहीं बनाएंगे’ के नारे के साथ हिंदू पहचान को उभारने की आक्रामक मुहिम शुरु होती है। यूपी सरकार कारसेवकों से सख्ती से निपटती है। मुलायम सिंह यादव राजनीतिक साहस का परिचय देते हैं। इसके बाद इन ब्राह्मणवादियों के लिए मुलायम सिंह यादव ‘मुल्ला’ व ‘मौलवी’ मुलायम बन गए। मुलायम सिंह यादव सत्ता से बाहर होते हैं। शूद्र नेताओं की अगुआई में भाजपा सत्ता तक पहुंचती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है। लेकिन जब मंडल और बहुजन धारा एक साथ आती है तो नारा गूंजता है– ‘मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गये जय श्री राम!’ मुलायम सिंह यादव फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन यह एकता आगे बढ़ नहीं पाती है। दरहकीकत, मंडल-बहुजन उभार के अंतरविरोध भी थे, सीमाएं थीं। इस अंतर्विरोध की जड़ें भी ब्राह्मणवादी वर्ण-जाति व्यवस्था में ही थीं। बहुजन एकजुटता आगे नहीं बढ़ पाई।
मुलायम सिंह यादव जैसे नेता ही 60-70 के दशक से लेकर 90 के उभार तक संसदीय राजनीति में उत्पीड़ितों के पक्ष से साहस के साथ मैदान में होते हैं। वे राजनीतिक साहस दिखाते हैं और इस कारण सवर्ण प्रभुत्व और हिंदुत्व के शुरु हुए जवाबी हमले के खिलाफ सीधे मोर्चे पर होते हैं। यह उनका राजनीतिक साहस ही था कि फूलन देवी को संसद जाने का रास्ता बनाया। बहुजन छोर से महिला प्रतिरोध की नायिका के बतौर स्थापित होने का उनका मार्ग प्रशस्त किया।
बहरहाल, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं की ऐतिहासिक भूमिका मंडल उभार के साथ ऊंचाई तक पहुंचती है। ऐसे राजनेताओं का नायकत्व मंडल उभार के ऊंचाई तक पहुंचने के दौर तक के ऐतिहासिक सकारात्मक भूमिका व योगदान पर ही खड़ा होता है। बेशक, राजनीति में उत्पीड़ित जाति-समूहों के लिए आगे का रास्ता खोलने में उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका जरूर निभाई। भले भाजपा से उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन वे समाज की आगे की गति को नहीं पकड़ पाए। हमें यह समझना होगा कि वे उत्पीड़ितों के अन्य हिस्सों की उभरती राजनीतिक आकांक्षाओं को संबोधित करने के साथ सामाजिक न्याय के एजेंडा को पुनर्परिभाषित नहीं कर पाए। यही इन धाराओं और राजनेताओं की सीमा है। उनका पूरा प्रयास ब्राह्मणवादी वर्ण-जाति व्यवस्था के भीतर जातियों के बीच सामाजिक-राजनीतिक संबंध व शक्ति संतुलन को बदलने तक सीमित था। नायकों की चमक फीका पड़ने लगी। मसीहाई छवि दरकने लगी। ‘जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है!’ की गूंज को भी कमजोर पड़ना ही था।
मंडल उभार के नेता सबके नेता नहीं हो पाए। उनके अगुआई में खड़ी पार्टियां आज भी सबकी पार्टी नहीं हो पा रही हैं। .जबकि ये पार्टियां विशुद्ध रूप से केवल बहुजनों की पार्टियां कभी भी नहीं थीं। बसपा की शुरुआत बहुजनों की पार्टी के बतौर जरूर हुई थी लेकिन मायावती सर्वजन का नारा देकर भी सवर्णों की नेता नहीं हो सकीं। बिहार में राजद आज ‘ए टू जेड’ का नारा देकर भी सवर्णों का वोट हासिल नहीं कर पाता है। अखिलेश यादव परशुराम मंदिर बनाने की बात करते हुए भी सबका वोट नहीं ले पाते हैं। आज भी सबके नेता होने का विशेषाधिकार सवर्णों के पास ही है। शेष तो जाति या उत्पीड़ित समूह के नेता के बतौर ही सवर्ण इंटेलिजेंसिया द्वारा पेश किये जाते हैं। सचमुच में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान उत्पीड़ित जातियों-समूहों के ही नेता हैं, नायक हैं, और रहेंगे।