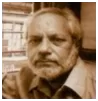
-तेजपाल सिंह ‘तेज’
गांधी जी और डॉ.भीमराव अंबेडकर के विचारों में कई अंतर थे। हालांकि, दोनों ही सुधारक थे और जाति प्रथा के ख़िलाफ़ थे। अंबेडकर बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों में अंतर थे। गांधी जी गीता में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे, जबकि अंबेडकर जी के मुताबिक, वर्णाश्रम व्यवस्था ही छुआछूत को जन्म देती है। गांधी जी दलितों के लिए ‘हरिजन’ शब्द का इस्तेमाल करते थे, जबकि अंबेडकर जी को यह पसंद नहीं था। गांधी जी लोगों का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत की समाप्ति को सामाजिक स्वीकृति दिलाना चाहते थे, जबकि अंबेडकर जी के मुताबिक, ऐसा संभव नहीं। अंबेडकर जी बौद्ध धर्म की करुणा और मानवता के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि में अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। गांधी और अम्बेडकर के विचारों में इतना अंतर था कि गांधी जी गीता में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक और छुआछूत के विरोधी थे जबकि डॉ.अम्बेडकर का मानना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था ही छुआछूत को जन्म देती है।
दलितों और पिछड़ों की ये गलतफहमी है कि वो पीला या भगवा कुर्ता पाजामा पहनने से हिन्दू हो जाएंगे सिर्फ वोट देने कुछ दिन के लिए हिंदू हो बाकी, तुम दलित पिछड़ा, ही रहोगे जैसे इस व्यक्ति को बराबर में बैठने पर फ़जीहत करके पीछे भगा दिया जाता है ठीक इसी प्रकार योगी जी ने स्टूल पर केशव प्रसाद मौर्य जी को बैठा दिया था। दलितों पिछड़ों को इतिहास उठा कर देखना चाहिए तो उसमें नजर आएगा कि भाजपा को वोट देने का मतलाब अपना शोषण करवाना है। ऐसे में गांधीवादी बौद्ध और अंबेडकरवादी बौद्ध का सवाल उठता है कि गांधीवादी बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट में क्या अंतर है? भिक्षु संघरक्षिता ( । M No। 6202517152) इस नए विषय पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि इस विषय का इतिहास से बहुत कुछ लेना-देना है।
गांधीवादी बौद्ध और अंबेडकरवादी बौद्ध में अंतर : हो सकता है कि पाठकों ने अब तक ऐसे शब्द नहीं सुने हों। पहला प्रश्न है, ‘ गांधीवादी बौद्ध कौन हैं? और अंबेडकरवादी बौद्ध कौन हैं? उनका एक दूसरे से क्या संबंध है? डॉ.बीआर अंबेडकर के बारे में तो सबने सुना ही होगा। इसलिए गांधीवादी बौद्ध और अंबेडकरवादी बौद्ध में अंतर समझने में किसी को भी कोई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। गांधी और अंबेडकर, ये दो नाम इतिहास के पन्नों में ऐसे दर्ज हैं कि आज की राजनीति में भी हमें ये नाम लगातार सुनने को मिलते हैं।
गांधीवादी बौद्ध और अंबेडकरवादी बौद्ध में अंतर को समझने के लिए हमें इतिहास को खंगालना होगा। यह बात उस समय की है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले डॉ.बीआर अंबेडकर को गांधीवादी लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए मनाने के लिए प्रयास किया । तब बाबा साहब ने कहा था, ‘ आप जो आंदोलन कर रहे हैं, उससे आपको आजादी मिलेगी, लेकिन मैं इस आजादी पर विश्वास नहीं करता। मैं राजनीतिक आजादी के जरिए देश के लोगों की आज़ादी में विश्वास नहीं करता। मैं देश के लोगों की आज़ादी में विश्वास करता हूँ। मेरे लिए लोगों की आज़ादी देश की आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश या समाज जैसी अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती। समाज लोगों से बनता है और एक राष्ट्र लोगों से बनता है। इसलिए मैं इस देश की राजनीतिक आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं बनूंगा क्योंकि मैं देश के लोगों की आज़ादी में विश्वास करता हूं। और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं।
डा। अम्बेडरकर आगे कहते हैं कि मैं देश में रहने वाले लोगों को आज़ाद करना चाहता हूँ। लेकिन जिस आज़ादी के लिए आप लड़ रहे हैं, उससे लोग आज़ाद नहीं होंगे। देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन देश में रहने वाले लोग गुलाम ही रहेंगे। क्योंकि अगर देश की आज़ादी होगी तो इससे देश का विकास तो होगा, लेकिन देश के लोगों का विकास नहीं होगा। अगर देश को आज़ादी मिल जाए, लेकिन लोगों को आज़ादी न मिले तो लोगों का विकास नहीं होगा बल्कि केवल देश का विकास होगा। देश का विकास होगा। यह देश बहुत आधुनिक बन सकता है, या बहुत अमीर बन सकता है, लेकिन देश की संपत्ति जीडीपी से देखी जा सकती है, कि देश बहुत अमीर है। लेकिन 90% संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में होगी।
यथोक्त के आलोक यहां यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि देश की आर्थिक अवस्था में यह सब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। लगता है कि देश को राजनीतिक सरकार नहीं अपितु देश की अडानी , अम्बानी जैसे धनिक लोग ही देश को चला रहे है क्योंकि देश की राजनीति को ऐसे धनिक लोग पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। यह अवस्था हम आए रोज अपने देश में देख रहे हैं। हैरत तो ये है कि सरकार भी इन जैसे लोगों के लिए ही काम कर रही है। सरकार खुद स्वीकार कर रही कि देश की 140 करोड़ आबादी में से 84 करोड़ आबादी आज भी सरकारी राशन के बल पर जिंदा है।
भिक्षु संघरक्षिता आगे कहते है कि देश की आर्थिक स्थिति हम सबके सामने है। देश की सिर्फ 5% संपत्ति आम लोगों के हाथ में है, तो इससे देश का विकास कहां से और कैसे हुआ? उदाहरणार्थ अगर 1000 लोगों की जीडीपी 10,000 रुपए है, और जनसंख्या केवल 10 लोगो की है। तो जब हम इसको प्रति व्यक्ति आय में विभाजित करेंगे, तो हर व्यक्ति के हिस्से में 1000 आएगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है क्योंकि सम्पत्ति का बराबर बटवारा नहीं है। वास्त्विक हालत ये है कि 10000 जीडीपी का अधिकतम भाग केवल चंद लोगों के पास है और आम लोग दो जून रोटी के लिए आज भी मोहताज है। लेकिन जब हम देश के स्तर पर इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो हम इसे 10 लोगों की जनसंख्या में बराबर बांट देंगे तो हर व्यक्ति के पास 1,000 होंगे। लोगों की नजर में और सरकारी आंकड़ों में यह ही दिखेगा कि हर व्यक्ति के पास 1,000 रुपये हैं। लेकिन वास्तव में, व्यावहारिक रूप से, क्या वे लोग 1,000 रुपये के मालिक हैं? नहीं। वह 10,000 सिर्फ़ 2 लोगों के हाथ में है। उसी तरह, अगर देश अमीर हो जाता है, अगर देश विकसित हो जाता है, तो वह विकास भी कुछ धनिक लोगों का ही होगा। भारत में 1 फ़ीसदी आबादी के पास देश की 40 फ़ीसदी दौलत है। साल 2022-23 में, देश के सबसे अमीर 1 फ़ीसदी लोगों की आय में हिस्सेदारी 22।6 फ़ीसदी और दौलत में हिस्सेदारी 40।1 फ़ीसदी थी। यह आंकड़ा ऐतिहासिक रूप से ऊंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट को थॉमस पिकेटी (पेरिस स्कूल ऑफ़ इकनॉमिक्स), लुकास चांसल (हार्वर्ड कैनेडी स्कूल), और नितिन कुमार भारती (न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी) ने तैयार किया है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक : 20 मार्च 2024 — Inequality in India: भारत की 1 फीसदी आबादी के पास देश की 40 फीसदी दौलत इकट्ठी हो गई है। साल 2000 के बाद से देश में अमीरों की दौलत लगातार बढ़ती ही जा रही है। (ABP News) भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की टोटल वेल्थ का 40% से ज्यादा हिस्सा है। इस बात की जानकारी ऑक्सफैम (Oxfam) ने हाल ही में जारी अपनी एक रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’ में दी है। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि देश की आधी यानी 50% आबादी के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% है। भारत में और बढ़ी अमीरी-गरीबी की खाई, वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई? क्या वाकई भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो गई है या फिर वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब की रिपोर्ट भारत को लेकर किसी तरह का पक्षपात कर रही है
12 अप्रैल , 2024: एम।जी। अरुण : अमीर-गरीब के बीच की खाई भारत में कभी छिपी नहीं रही है। पेरिस स्थित शोध संगठन वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब की ओर से हाल में जारी एक शोधपत्र में इसकी बस फिर से पुष्टि की गई है। अगर कुछ हुआ है तो यह कि खाई और चौड़ी हो गई है। देश के शीर्ष एक फीसद तबके की आमदनी और संपत्ति में हिस्सेदारी अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। शोधपत्र के निष्कर्षों में कहा गया है कि साल 2023 तक सबसे अमीर एक फीसद भारतीयों के पास देश की आय का 22।6 फीसद और संपत्ति का 40 फीसद हिस्सा था।
‘इनकम ऐंड वेल्थ इनइक्वेलिटी इन इंडिया, 1922-2023: द राइज ऑफ बिल्यनेर राज’ शीर्षक वाले शोधपत्र के अनुसार आजादी के बाद से 1980 के दशक की शुरुआत तक गैर-बराबरी में कमी आई थी लेकिन इसके बाद इसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई और 2000 के दशक की शुरुआत में यह बहुत तेज गति से बढ़ी। देश के शीर्ष एक फीसद लोगों ने 2022-23 में औसतन 53 लाख रुपए कमाए, जो औसत भारतीय की आय से 23 गुना अधिक है जिसने 2।3 लाख रुपए की आय सृजित की। देश के निचले पायदान के 50 फीसद और बीच के 40 फीसद लोगों की औसत आय क्रमश: 71, 000 रु। (राष्ट्रीय औसत का 0।3 फीसद) और 1,65,000 रु। (राष्ट्रीय औसत का 0।7 फीसद) रही। सबसे अमीर 9,223 लोगों (9।2 करोड़ वयस्क भारतीयों में से) ने औसतन 48 करोड़ रुपए कमाए (औसत भारतीय आय से 2,069 गुना)।
21वीं सदी की शुरुआत के वित्त वर्ष 2002 में शीर्ष 10 फीसद के पास संपत्ति का 57।1 फीसद हिस्सा था जबकि शीर्ष 10 फीसद के पास आय का हिस्सा 42।1 फीसद था। यह 15 फीसद अंक का अंतर है। अगले 20 वर्ष में शीर्ष 10 फीसद की आय का हिस्सा ज्यादा तेजी से बढ़ा और अंतर में काफी कमी आई। वित्त वर्ष 2022 तक अंतर आधा घटकर 7।3 फीसद रह गया।
दूसरी ओर, इस अवधि के दौरान शीर्ष 1 फीसद की आय और संपत्ति की तुलना करें तो रुझान एकदम विपरीत हैं। 2002 में, शीर्ष एक फीसद की संपत्ति का हिस्सा 25।4 फीसद था जबकि आय के लिए यह हिस्सा 16।7 फीसद था यानी दोनों का अंतर 8।7 फीसद था। 20 साल बाद 2022 तक यह अंतर बढ़कर 13।4 फीसद अंक हो गया।
नितिन कुमार भारती, लुकास चांसल, थॉमस पिकेट्टी और अनमोल सोमांची के लिखे शोधपत्र में कहा गया है, “ये विपरीत रुझान संकेत देते हैं कि वितरण के एकदम ऊपरी स्तर पर आय की तुलना में संपत्ति का केंद्रीकरण ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है।” नई जानकारी ने सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराया है जिनका कई अर्थशास्त्री इशारा करते आए हैं, भारतीयों के बीच बढ़ती संपत्ति असमानता, जिसे महामारी ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। नए निष्कर्षों ने के अनुसार अमीर तेजी से बढ़ रहे और गरीबों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा महंगे सामान का उपभोग कर रहे हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद निजी उद्यम में वृद्धि और पूंजी बाजार की वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिमटना बढ़ाया है। शोधपत्र इस बात से सहमत है कि 90 के दशक के आखिर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पारिश्रमिक वृद्धि ने इसमें आंशिक भूमिका निभाई होगी। वह कहता है कि यह मानने की वाजिब वजहें हैं कि बाद के वर्षों में पूंजी आमदनी ने यह भूमिका निभाई। शोधपत्र कहता है कि अंतिम छोर के 50 फीसद और बीच के 40 फीसद लोगों के हिस्से के सिकुड़े रहने का एक प्रमुख कारण गुणवत्ता आधारित शिक्षा का अभाव रहा है।
उदारीकरण के बाद से सेवा की अगुआई में हुई आर्थिक वृद्धि के भी ‘असमानताकारी’ असर हुए। एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में कार्यबल का 45।5 फीसद कृषि में लगा था, वहीं निर्माण से 12।5 फीसद और मैन्युफैक्चरिंग से महज 11।6 फीसद जुड़ा था और शेष (30।5 फीसद) सेवा क्षेत्र से जुड़े थे। शोधपत्र कहता है, “अपने ज्यादा कार्य बल को कृषि से हटाकर अधिक उत्पादक और बेहतर भुगतान वाले रोजगार में लगाने में भारत की अक्षमता बड़ी चुनौती बनी हुई है।”
वे एक मीडिया लेख में कहते हैं कि मौजूदा अनुमानों को रुझानों के आम संकेतक के रूप में देखा जाना चाहिए न कि सटीक स्थिति के रूप में। जिस बात पर विशेषज्ञ सहमत हैं, वह यह कि आय और संपत्ति पर बेहतर निष्कर्ष निकालने के लिए अच्छे डेटा की जरूरत है, जिससे इस मसले से निबटने के लिए कारगर समाधान तैयार करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट की कुछ खास बातें निम्नानुसार हैं-
- सिर्फ एक फीसद भारतीयों के पास देश की आय का 22।6 फीसद और संपत्ति का 40 फीसद हिस्सा है। शीर्ष एक फीसद भारतीयों के पास आय का हिस्सा दुनिया में सबसे अधिक है।
- आजादी के बाद से 80 के दशक के शुरुआती वर्षों में गैर बराबरी में गिरावट आई, उसके बाद यह बढ़ने लगी और 2000 के दशक के शुरू में बहुत तेजी से बढ़ी।
- शीर्ष एक फीसद ने वित्त वर्ष 2023 में औसतन 53 लाख रुपए की सालाना आमदनी अर्जित की जो औसत भारतीय की आय का 23 गुना है जिनकी आय 2।3 लाख रुपए थी।
- सबसे अमीर 9,223 लोगों (9।2 करोड़ वयस्क भारतीयों में से) की औसतन आमदनी 48 करोड़ रुपए थी (औसत भारतीय से 2,069 गुना)।
- उदारीकरण के बाद निजी उद्यम में वृद्धि और पूंजी बाजारों में बढ़ोतरी से ऊपर के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का इजाफा हुआ।
- निचले पायदान के 50 फीसद और बीच के 40 फीसद का हिस्सा सिकुड़ा ही रहा। इसका मुख्य कारण गुणवत्ता आधारित ऐसी व्यापक शिक्षा की कमी रही जो सिर्फ अभिजात्य के लिए ही नहीं बल्कि जन केंद्रित भी हो।
- अपने अधिक कार्यबल को कृषि से निकाल कर अधिक उत्पादक और बेहतर भुगतान वाले रोजगारों की तरफ ले जाने में भारत की अक्षमता।
- जब शुद्ध संपत्ति के पहलू से देखें तो भारतीय आयकर प्रणाली प्रतिगामी लगती है, आय और संपत्ति दोनों को शामिल करने के लिए कर संहिता के पुनर्गठन की जरूरत।
- अमीरों पर अधिक टैक्स: 2023 में 167 सबसे अमीर परिवारों की शुद्ध संपत्ति पर दो फीसद का सुपर टैक्स लगाने से राष्ट्रीय आय के राजस्व का 0।5 फीसद प्राप्त होता।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में व्यापक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है जिससे कि औसत भारतीय को वैश्वीकरण की मौजूदा लहरों का फायदा पहुंचे।
यथोक्त के आलोक में, अगर देश के लोगों का विकास करना है तो देश के लोगों को आज़ादी लानी होगी। अगर हम देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी की बात करेंगे तो हम देश में रहने वाले लोगों के विकास की भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम देश की राजनीतिक आज़ादी की बात करेंगे तो हम सिर्फ़ देश के विकास की बात करेंगे, लोगों के विकास की नहीं। तो, ये जो देश की राजनीतिक आज़ादी का सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत था? गांधी जी का। और ये जो देश के लोगों की सामाजिक आज़ादी का सिद्धांत है, वो किसका था? ये सिद्धांत डॉक्टर बी।आर। अंबेडकर का था। जो देश की सामाजिक आज़ादी को देश के विकास से जोड़ता है। यानि धनिक वर्ग का विकास ही देश का विकास है, यह गांधी जी की सोच थी। जबकि देश के समस्त लोगों का विकास, देश में रहने वाले लोगों का विकास ही देश का विकास है, यह डॉ.बी।आर। अंबेडकर का सिद्धांत था। तो मैंने ये बातें आपको इसलिए बताईं हैं ताकि आप समझ सकें कि मैं आपके मन में इन बातों के आधार पर क्या कहने जा रहा हूँ। वो ये है कि आज जो बौद्ध धर्म दिख रहा है, वो गांधीवादी बौद्ध धर्म है। कैसे? क्योंकि यहाँ भी देश के लोगों का विकास नहीं हो रहा है, बौद्ध लोगों और बौद्ध धर्म का विकास नहीं हो रहा है।
यहाँ बौद्धों के लिए क्या हो रहा है? बौद्ध धर्म में लोगों का विकास लोगों का विकास और बौद्ध धर्म का विकास दोनों अलग-अलग बातें हैं। बौद्ध धर्म का विकास बौद्धों का विकास और बौद्ध धर्म में रहने वाले लोगों का विकास, देश के विकास और देश में रहने वाले लोगों के विकास में वही अंतर है। देश की आजादी और देश में रहने वाले लोगों की आजादी में फर्क है। देश की आज़ादी में सिर्फ़ कुछ ही लोग आज़ाद थे और आज भीं कूच लोग ही आजाद हैं। आजादी से पूर्व सिर्फ़ 10-15% लोग ही आज़ाद थे। बाकी 85-90% लोग आज़ाद नहीं थे। उन्हें वो सारी सुविधाएँ नहीं मिलीं जो मिलनी चाहिए थीं। अगर आज भारत को अमीर कहा जा रहा है, तो सिर्फ 5% लोगों के पास ही संपत्ति का सबसे बड़ा भाग है और 95-95% लोगों के पास आज भी बहुत कम संपत्ति है। अर्थात आज भी आम लोग विकसित नहीं हुए हैं। क्योंकि इस देश में आधे से ज़्यादा, यानी 50% से ज़्यादा गरीब लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अत: इस अवस्था के बल पर देश को विकसित देश नहीं कहा जा सकता है।
यद्यपि बौद्ध धर्म में रहने वाले लोगों का विकास नहीं हुआ है, तथापि कुछ स्तर तक बौद्ध धम्म का विकास हुआ है। किंतु यह भी सच है कि देश में बौद्ध धर्म के नाम पर अनेक संगठन और पूरे भारत में अनेक बौद्ध विहार बने हैं। अकेले बोधगया में 100 से ज़्यादा बौद्ध मठ/विहार हैं। बहुत से लोग भिक्षु तो बन गए हैं, लेकिन क्या उन्होंने बौद्ध धर्म का विकास किया है? केवल और केवल बौद्ध धम्म के पंचरंगी झंडे घरों पर लगाए जा रहे हैं। लगभग 50,000 बिहार बनाए जा रहे हैं बिहारों में बौद्ध प्रतिमाएँ रखी जा रही हैं। चारों तरफ नमो बुद्धाय का नारा लगाया जा रहा है। लेकिन क्या भिक्षुओंयलोगों ने बौद्ध धर्म का विकास किया? अगर नहीं, तो मैं किस तरह के विकास की बात हो रही है? क्या केवल बौद्ध धर्म के लोगों के विकास की। बौद्ध धर्म के लोगों के विकास को मैंने लोगों की चेतना का विकास नाम दिया है। लोगों की चेतना के विकास को ही विकास माना जा सकता है। लेकिन लोगों की चेतना का विकास कैसे होगा? इसका जवाब खुद गौतम बुद्ध ने दिया था कि लोगों की चेतना को विकसित करने के लिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाने का रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति शील, समाधि और प्रज्ञा में स्थित है, और इन तीन रत्नों, सील, समाधि और प्रज्ञा में स्थित है, उसके सभी विकार समाप्त हो जाएंगे और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। वह जीवन के सत्य को जान जाएगा। उसके सभी विकार समाप्त हो जाएंगे, चाहे वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष हो। वह इन सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। और वह एक शुद्ध चेतना होगा। और वह शुद्ध चेतना एक अच्छे मानव समाज का निर्माण करेगी।
जब लोग वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने लगेंगे तो एक ऐसा समाज तैयार होगा जहाँ समानता समाज की नींव होगी। एक ऐसा समाज तैयार होगा जहाँ समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा आधारित होगा। मानव चेतना का विकास ही व्यक्ति का विकास होगा। और 2500 साल पहले बुद्ध ने जो संघ बनाया था, और जिस मार्ग पर वे चले थे, और जो रास्ता उन्होंने बनाया था, कि मैंने ये मार्ग पाया है, जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलेगा, उस व्यक्ति की चेतना का विकास वैज्ञानिक युग की ओर ले जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये शीर्ष विश्वविद्यालय रहे हैं जहाँ वैज्ञानिक युग की शुरुआत हुई थी। इन चेतनाओं के विकास के कारण बाद में ऐसी बहुत सी चीजों का आविष्कार हुआ। लेकिन आज भी लोगों की चेतनाएँ विकसित नहीं हुई हैं। लोगों की चेतना का विकास नहीं हो रहा है। फिर अभी बौद्ध धम्म का विकास इस स्तर पर ही हो रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़, बुद्ध बिहार बनाये जा रहे हैं। संगठन बनाये जा रहे हैं। भिक्षु बनाये जा रहे हैं।लेकिन जो भिक्षु बन रहे हैं, वो भी शील समाधि और प्रज्ञा पर काम नहीं कर रहे हैं। वो अपना सारा समय विरासत, ज़मीन, मूर्तियों के लिए लड़ने, उन्हें बचाने की लड़ाई में लगा रहे हैं। वो अपना समय इसी में बर्बाद कर रहे हैं। राज्य के लिए लड़ाई, संपत्ति के लिए लड़ाई, का कोई फायदा नहीं है। और जो पीछे की चीज है, जो अतीत की है, उसमें ऊर्जा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ऊर्जा लगानी है, तो अपनी चेतना के विकास में लगाइए। तभी लोगों की चेतना विकसित होगी, लोगों की बौद्धिकता विकसित होगी, लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे।
भिक्षु संघरक्षिता जी यह भी कहते है, ’अगर आप संन्यासियों के सफेद कपड़ों से चारों तरफ रंग कर दें, अगर आप सारे भिक्षापात्र भर दें, अगर पूरी दुनिया संन्यासियों और भिक्षापात्रों से भर जाए, अगर दुनिया भर में एक रंगा हुआ झंडा लगा दिया जाए, तो क्या इससे लोगों का विकास होगा? क्या लोग दुखों से मुक्त होंगे? बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति अपने दुखों और सुखों का कारण स्वयं होता है। अगर वो दुखी है तो वो खुद ही अपने दुखों और सुखों का कारण है। उसकी आशाएँ, अपेक्षाएँ, इच्छाएँ, उसकी वासना, उसका क्रोध, उसका लोभ, उसकी वासना, उसका लालच, ये सब उसके विकास को रोकते हैं। यही उसके दुखों का कारण है। इसलिए मैं बार-बार इन तीन बातों पर ध्यान दे रहा हूँ, सील, समाधि और प्रज्ञा। जिसमें सील, समाधि और प्रज्ञा होगी, इन तीन बातों में जो प्रतिष्ठा होगी, मन और चेतना का विकास होगा, और वैज्ञानिक युग की शुरुआत होगी। और जब लोगों में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा, तभी राष्ट्र में परिवर्तन होगा, तभी विश्व में परिवर्तन होगा।
सारांशत: यथोक्त के आलोक में यह कहा जा सकता है कि कुछ लोगों द्वारा नमो बुद्धाय कहने से, पंचरंगा झंडा लगाने से, या चीवर पहनने से लोगों की चेतना में कोई विकास नहीं होगा, लोगों का बौद्धिक विकास नहीं होगा, लोग दुखों से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए लोग, कपड़े की संख्या बढ़ाकर, पंचाल के झंडे की संख्या बढ़ाकर, पूजा करने वालों की संख्या बढ़ाकर, बौद्धों की संख्या बढ़ाकर, बौद्धों का विकास समझ रहे हैं। जो लोग इस विकास को समझ रहे हैं, मैं उन्हें गांधीवादी बौद्ध कह रहा हूँ।
और जो लोग बौद्ध धर्म के विकास को समझ रहे हैं, और जो लोग आत्म, समाधि और प्रज्ञा में स्थित होकर त्रिरत्नों का पालन कर रहे हैं, वे लोगों को दुख से मुक्त होने में मदद करते हैं, या वे स्वयं दुख से मुक्त होते हैं, और लोगों को दुख से मुक्त होने में मदद करते हैं। जो लोग लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करते हैं, अपनी चेतना का विकास करते हैं, लोगों का बौद्धिक विकास करते हैं, और लोगों को उनकी चेतना और बौद्धिक विकास को विकसित करने में मदद करते हैं, वे लोगों को उनके दुखों से छुटकारा पाने में मदद करते हैं और लोगों को उनके दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बताकर उन्हें उनके दुखों से छुटकारा पाने में भी मदद करते हैं। ऐसे लोग अंबेडकरवादी बौद्ध हैं।
यूं भी कह सकते है कि गांधीवादी बौद्ध और अंबेडकरवादी बौद्ध में मुख्य अंतर यह है कि गांधीवादी बौद्ध धर्म को अधिक आध्यात्मिक और अहिंसक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष के रूप में देखते हैं। गांधीवादी बौद्ध धर्म में अहिंसा, सत्य और आत्म-संयम पर जोर दिया जाता है, जबकि अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म में सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा पर जोर दिया जाता है। अंबेडकरवादी बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ना और उन्हें शिक्षा और सामाजिक न्याय प्रदान करना है। इस प्रकार, दोनों धाराओं में बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण और उद्देश्य में अंतर है।0000
(संदर्भ-https://youtu।be/k1oMAO0AvUs?si=0w78mnomHF6GGiS4) तेजपाल सिंह तेज (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार की तीन दर्जन किताबें प्रकाशित हैं- दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है, गुजरा हूँ जिधर से आदि ( गजल संग्रह), बेताल दृष्टि, पुश्तैनी पीड़ा आदि (कविता संग्रह), रुन-झुन, खेल-खेल में आदि ( बालगीत), कहाँ गई वो दिल्ली वाली ( शब्द चित्र), दस निबन्ध संग्रह (प्रतिक्रियात्मक) और अन्य। तेजपाल सिंह साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता के साहित्य संपादक, चर्चित पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक, आजीवक विजन के प्रधान संपादक तथा अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक के संपादक रहे हैं। हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार ( 1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से सम्मानित किए जा चुके हैं। स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर आप इन दिनों स्वतंत्र लेखन में रत हैं। 0000


























Add comment