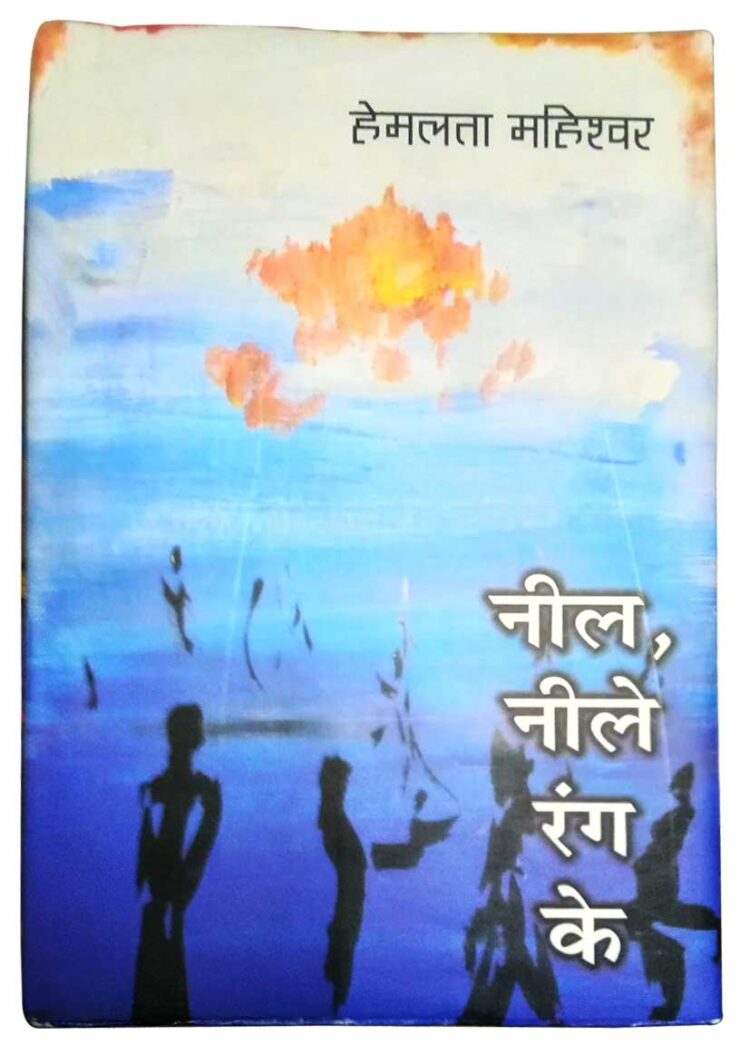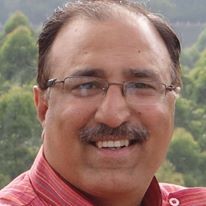कंवल भारती
हेमलता महिश्वर का पहला कविता संग्रह 2015 में आया था, नाम था ‘नील, नीले रंग के।’ अगर नाम में नील शब्द न होता, तो नीले रंग से वही अर्थ निकलता, जो हरे और भगवा रंग से क्रमश: इस्लाम और हिंदुत्व का अर्थ निकलता है। लेकिन यहां नील शब्द यातनाओं के दंश के अर्थ में आया है। एक कहावत है कि किसी को पीट-पीट कर नीला कर देना। शरीर पर पिटाई के पड़ने वाले इसी नीले निशान को लोकभाषा में नील कहते हैं। शरीर के नील कुछ समय बाद मिट जाते हैं। लेकिन वे दिल-दिमाग और मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कवियित्री हेमलता महिश्वर जिन नीलों की बात कर रही हैं, वे सवर्णों के अत्याचारों के नील हैं, जो हजारों साल से दलितों के दिल-दिमाग और मन पर अमिट बने हुए हैं। ‘नील, नीले रंग के’ नाम से कवियित्री ने पांच कविताएं लिखी हैं। पहली कविता इस प्रकार है–
नील नीले रंग के पड़ जाते थे
तन पर, मन पर
मार, बेगार और अपमान के।
याद है न, गर्दन में लटकती हांडी
और कमर में बंधी झाड़ू की रस्सी से
छलछला उठते रक्त-बिंदु।
यूं तो नहीं है आज गले में हांडी
कमर में झाड़ू
फटे बांस का टुकड़ा हाथों में
फिर भी जाते क्यों नहीं नीले निशान।[1]
यह कविता उस पेशवा-काल के इतिहास की याद दिलाती है, जिसमें दलितों को सार्वजनिक मार्गों पर गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाकर चलना पड़ता था। सचमुच जुल्म के निशान मिटते नहीं हैं। और ऐसे जुल्म के, जो समाज के सबसे कमजोर लोगों पर बिना किसी कारण के, सिर्फ उन्हें गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से यातनाओं के रूप में ढाए गए थे। असल में अत्याचारी लोग दलितों के मालिक नहीं थे, बस उनके हाथ में सत्ता की ताकत थी। डॉ. आंबेडकर[2] ने लिखा है कि जिस गांव या इलाकों में ये अभागे लोग रहते थे, वे उनके लिए ‘घेट्टो’ थे।[3]
साहिर लुधियानवी की एक बहुत ही मशहूर नज़्म है– “ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है/ खून फिर खून है टपकेगा तो जम जायेगा।” यह नज़्म किसी और पर फिट हो या न हो, पर दलितों पर जरूर फिट होती है। दलितों पर होने वाले ज़ुल्म को जाने कितनी सदियां बीत गईं, पर ज़ुल्म का अंत नहीं हुआ। वह आज भी जारी है। इसलिए ज़ुल्म के नील सूखते हैं, तो फिर हरे हो जाते हैं। ‘नील, नीले रंग के’ शृंखला की दूसरी कविता इसी भाव को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। यथा–
नील, नीले रंग के रोज फिर हो जाते हैं हरे।
आंदोलन नामांतरण का
विलास घोगरे की आत्महत्या
गोहाना, खैरलांजी और मिर्चपुर
या फिर चाहे
गैर दलित बस्ती की कुतिया[4]
ठग जाती हमको
गणतंत्र की यह कैसी दुनिया?
ज़ुल्म की ये घटनाएं स्वतंत्र भारत के गणराज्य में हुई हैं! इससे बड़ा विद्रूप और क्या हो सकता है? ज़ुल्म की आग में जलते बहुजन कहां तलाशें शांति? कवियित्री पूछती है–
गोहाना के जलते घर-द्वार
खैरलांजी का भौतमांगे परिवार
मिर्चपुर का वृद्ध
घोड़ी पर बैठा दलित जवान
दलित बस्ती का कुत्ता
न भौंक सकता गैर-दलित पर
रोटी भी न खा सकती इनकी बस्ती की कुतिया
जाने कब से, जाने कितने नील
तन-मन पर लिए
अंगारों पर लोटते मूक हम
अमन शांति को तलाशते बहुजन।[5]
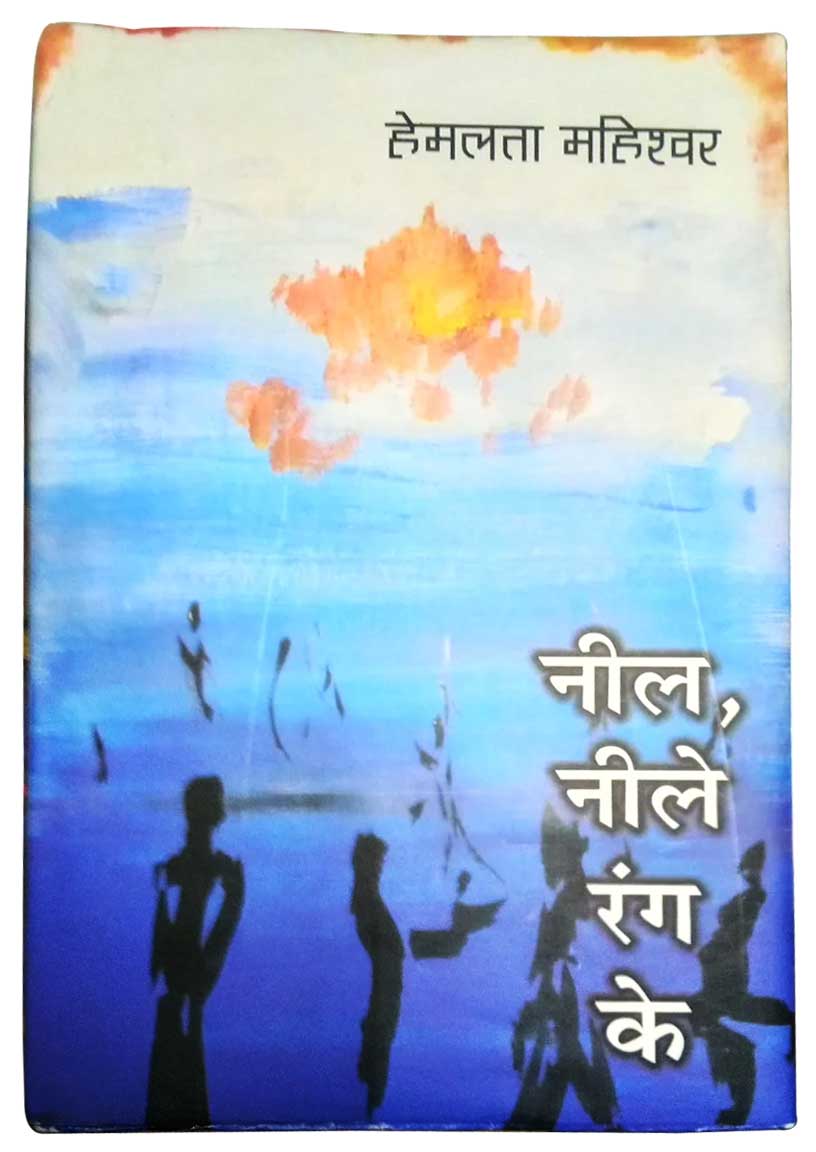
इसी कविता के अंत में कवियित्री नीले रंग को बाबासाहेब की धम्म-क्रांति से जोड़ देती हैं। यथा–
धम्म-दीक्षा ने याद दिलाया
नीले रंग का मतलब
नहीं ज़ख्मों के निशान
या उससे उपजी उदासी
उठी उंगली
बाबासाहेब की है बताती।
नीलों की गहराई का
नील गगन में हुआ विस्तार
सम्यक मार्ग पर चलते नील
अशोक चक्र में जा उभरे
स्वतंत्र गणतंत्र भारत की
तस्वीर लगी है पनपने।[6]
दलित कविता की यह बड़ी समस्या है कि वह भावुकता में अपने मूल से उखड़ जाती है। यह कविता भी अपने मूल से उखड़ गई। खैरलांजी में जिस भौतमांगे परिवार का नरसंहार हुआ था, वह बाबासाहेब के बौद्ध धम्म में ही दीक्षित था। क्या अशोक चक्र और गणतंत्र का नीला रंग उनकी हत्याओं को रोक सका?
‘नील, नीले रंग के’ की शृंखला की तीसरी कविता में आसमान और समंदर के रूपकों का अच्छा प्रयोग हुआ है। यथा–
तन-मन पर बनी नीलों की सघन चित्रकारी
धोने चले थे, फ़ेनिल था न पानी।
अतल समंदर भी न कर सका
नीलों को स्वीकार
नील समंदर के पानी में उभरे
समंदर का पानी नीला हो गया।
सोचा सुखा दूं कड़ी धूप में
धूप में रंग उड़ जो जाते हैं,
नील आसमान को नीला कर गए।[7]
इस कविता में शिल्प के साथ भाव भी सुंदर है। इसमें वेदना ने समष्टि की संवेदना का रूप लेने की कोशिश की है। आसमान के नीले रंग और समंदर के नीले पानी में दलितों की वेदनाओं के नील देखना कवि की अद्भुत कल्पनाशीलता है। लेकिन इसमें ‘चित्रकारी’ शब्द अखरता है, क्योंकि चित्रकारी से सुंदर का अर्थ ग्रहण किया जाता है, असुंदर का नहीं। नील असुंदर-बोधक है, सौंदर्य-बोधक नहीं।
इस शृंखला की चौथी कविता सबसे छोटी, सिर्फ चार पंक्तियों की रचना है, जिसमें नीले रंग के नील पीपल से गले मिलकर मनुष्यत्व की ओर बढ़ते हैं। यथा–
नील
नीले रंग के
पीपल से मिल गले
मनुष्यत्व की ओर बढ़ रहे थे।[8]
अगर पीपल बोधिवृक्ष के रूप में इस कविता में आया है, तो पीड़ित लोग बोधि के साथ ठीक ही मनुष्यत्व की ओर बढ़ रहे थे। पर यहां ‘थे’ क्यों? ‘हैं’ क्यों नहीं?
इस शृंखला की अंतिम कविता इस प्रकार है–
नील, नीले रंग के काले होकर
अमावस्या के आसमान में जा बिखरे
याद रखो कि काली घनी रात में
जबकि नहीं होता चांद
सितारे खूब चमकते हैं
बाबासाहेब का प्रकाश
हमारे भीतर दमक रहा है।[9]
यातनाओं के नील काले पड़कर अमावस की रात में बिखर गए हैं, अर्थात बाबासाहेब के ज्ञान के प्रकाश ने भीतर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अंधेरों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वेदना ने अपनी राह पा ली है।
एक विषय को एक ही शीर्षक के अंतर्गत कई कविताओं में रचने की एक परंपरा दलित कविता में भी इधर आ गई है। ‘नील, नीले रंग के’ बाद ‘बुद्ध’ और ‘उपस्थित/अनुपस्थित’ नाम से भी कवियित्री ने पांच-पांच कविताओं के रूप में पंचशील का प्रणयन किया है। ‘बुद्ध’ शृंखला में छोटी-छोटी पांच कविताएं हैं। पहली कविता एक ही पंक्ति की है, जो इस तरह है– “बुद्ध नहीं रहा फेर में शुद्ध के।”[10]
इस कविता के दो अर्थ हैं, एक यह कि बुद्ध ने शुद्धि-आंदोलन नहीं चलाया; और दूसरा यह कि बुद्ध शुद्ध-अशुद्ध या सही-गलत के फेर में नहीं पड़े। लेकिन ये दोनों ही अर्थ बौद्ध-धम्म के अनुरूप नहीं हैं। शांति भिक्षु शास्त्री ने, जो विश्वभारती शांति निकेतन में बौद्धदर्शन के आचार्य थे, लिखा है कि बुद्ध ने मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और मुक्ति के लिए तीन शुद्धियों का प्रतिपादन किया। इनमें पहली शील-विशुद्धि, दूसरी चित्त-विशुद्धि, और तीसरी दृष्टि-विशुद्धि है।[11] बुद्ध अगर शुद्धि पर जोर नहीं दे रहे थे, तो फिर लोग उनसे प्रभावित भी कैसे हो रहे थे?
‘बुद्ध’ शृंखला की दूसरी कविता इस तरह है–
अनित्य
हां, सब कुछ छीजना है
क्या सृजन में, क्या विघटन में
अणु क्या परमाणु भी
और फिर मुस्कुराता है बुद्ध
पोखरन में।[12]
इस कविता की ज़मीन 1998 में पोखरन में अटलबिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया परमाणु-विस्फोट है। निस्संदेह, हिंसा के घातक हथियार के आविष्कार से बुद्ध नहीं मुस्कुरा सकते थे। जिस बुद्ध की शरण ने हत्यारे अशोक को अहिंसक बना दिया हो, उस बुद्ध का परमाणु-विस्फोट पर मुस्कुराने का अर्थ था, उन्हें हिंसक बनाना। लेकिन यह ध्वनि इस कविता से नहीं निकलती। ध्वनि निकलती है, जगत के क्षण-क्षण नष्ट होने की, उसके अनित्य होने की। अनित्य का पोखरन-विस्फोट से संबंध स्पष्ट नहीं होता।
लेकिन शृंखला की तीसरी कविता में कवियित्री का बुद्ध युद्धरत नजर आता है–
बुद्ध कर रहा था
कर रहा है
अनवरत युद्ध।[13]
अवश्य ही यह बुद्ध का सामरिक युद्ध नहीं हो सकता। पर यह युद्ध किसके विरुद्ध और किससे चल रहा है? इसका भाव कविता में अमूर्त है। कविता में इतनी अमूर्तता कविता के लिए असुंदर होती है।
चौथी कविता में यह अमूर्तन और भी अधिक हो गया है। यथा–
बुद्ध हंस रहा था
कि रो रहा था
आंसू अपनी आंखों में लिए
अपनी मूर्ति के पास खड़ा था।[14]
जब कुछ मालूम ही न हो सके कि कोई क्या कर रहा है, हंस रहा है या रो रहा है, तो उस मन:स्थिति को ‘बेखुदी’ कहते हैं। इसे ‘बेहोशी’ भी कह सकते हैं। इस बेहोशी में जो दिखाई देता है, वह अंदर की परिकल्पना ही मूर्त रूप में उपस्थित होती है। लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं होता। उर्दू शायरी में बेखुदी की ऐसी अभिव्यक्तियां बहुत प्रकट हुई हैं। मिसाल के तौर पर मीर के ये शेर देखिए–
बेखुदी न मीर के जाओ
तुमने देखा है और आलम में।
बेखुदी ले गई कहां हमको
देर से इंतज़ार है अपना।[15]
मीर बेखुदी के आलम में इस क़दर खो गए थे कि अपने आपमें लौटने का ही इंतज़ार करते रह गए। कुछ यही आलम कवियित्री हेमलता महिश्वर का लगता है। उनकी यह स्थिति भूतकाल की है, क्योंकि बुद्ध मूर्ति के सामने खड़ा था, यह भूतकाल में ही संभव हो सकता था, वर्तमान में नहीं।
बुद्ध-शृंखला की अंतिम और पांचवी कविता इस प्रकार है–
बुद्ध का विस्तार
बुद्ध को ज़मीन से जोड़ रहा था
दायरा बुद्ध को छोड़ रहा था।[16]
ज़ाहिर है कि किसी भी चीज का विस्तार उसकी सीमाओं के बाहर ही होता है। सीमा ही उसकी अपनी ज़मीन होती है। यह ज़मीन क्षेत्र की भी होती है और विचार की भी। लेकिन यह कौन-सी ज़मीन है, जिससे जुड़कर बुद्ध अपना दायरा छोड़ रहे थे – क्षेत्र का भी और विचार का भी? विस्तार के साथ दायरा बढ़ता है, छूटता नहीं है। हालांकि यह भी बेखुदी की एक स्थिति लगती है, जिसे कबीर ने ‘हद-बेहद’ और ‘अनहद’ के रूप में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। यथा–
हद में पीव न पाइए, बेहद में भरपूर।
हद बेहद की गम लखै, तासौं पीव हजूर।।[17]
लेकिन कबीर की स्थिति हद-बेहद दोनों को छोड़कर ‘अनहद’ के मार्ग पर चलने की है। यथा—
हद बंधा बेहद रमैं, पल-पल देखे नूर।
मनवा तहां ले राखिया, जहां बाजै अनहद टूर।।
हद में रहैं सो मानवी, बेहद रहै सो साधु।
हद बेहद दोनों तजैं, तिनका मता अगाध।।[18]
लेकिन, यदि बुद्ध का दायरा छोड़ना अनहद की स्थिति में जाना है, तो बुद्ध का विस्तार उन्हें किस ज़मीन से जोड़ रहा था? यह प्रश्न बुद्ध को न हद में रहने देता है, न बेहद में और न अनहद में।
कविता की एक और शृंखला ‘उपस्थित/अनुपस्थित’ को लेते हैं। पहली कविता में कामवाली बाई या घर की साफ़-सफाई में दिन-रात खटने वाली घरेलू महिलाओं का दर्द है। यथा—
चिपकी रह जाती है
झाड़न में जितनी धूल
उतना-सा भी न रख पाईं वे
बचाकर अपना मन
मनोमन कई टन झाड़कर
घर की धूल।[19]
ईरान की शायरा शाहरुख हैदर की एक मशहूर नज़्म है, जिसमें वह कहती हैं—
मैं एक औरत हूं
अपनी तमाम पाबंदी के बाद भी औरत हूं।
क्या मेरी पैदाइश में कोई गलती थी?
या वह जगह गलत थी, जहां मैं बड़ी हुई?[20]
सच यह है कि यह दर्द सिर्फ ईरानी औरत का ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर औरत का है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्त्री अपना मन बचाकर नहीं रखती हैं। वह रखती हैं, पर वह मन शायद ही कभी पूरा होता है। कभी पति, कभी बच्चों, कभी सास-ससुर की सेवा और कभी अन्य जिम्मेदारियां उस मन को दबा देती हैं, हमेशा के लिए। दूसरी कविता में इसकी सटीक अभिव्यक्ति है—
फटर-फटर फटकती झाड़न
बस चमकाती रहीं
घर का मन
झाड़न की तरह
गंदले होते रहे उनके मन।[21]
तीसरी कविता में भी इसी दर्द की अभिव्यक्ति हुई है। और चौथी कविता में इसी दर्द को पालते हुए वे दुनिया से अनुपस्थित हो जाती हैं। यथा—
घर में
अपनी उपस्थिति का
एहसास दिलाते
वे दुनिया से अनुपस्थित हो गईं।[22]
‘उपस्थित/अनुपस्थित’ कविता की शृंखला कायदे से चौथी कविता में ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन ‘पंचशील’ का चक्र पूरा करने के लिए कवियित्री ने पांचवी कविता भी लिखी, जिसमें भावाभिव्यंजना पहली कविता वाली ही है। यथा—
फिर रगड़कर, ब्रश मारकर
निचोड़ दिया कटकटाकर
सुखाकर कड़ी धूप में
फिर तैयार कर लिया है स्त्री ने झाड़न
दुबारा इस्तेमाल के लिए
अपना मन भी
यूं ही धो-पोंछकर
फिर-फिर रखती है स्त्री
दुबारा धूल चढ़ाने के लिए।[23]
इस कविता में स्त्री-वेदना है, स्त्री-चेतना नहीं है। जब स्त्री-चेतना नहीं है, तो मुक्ति का विमर्श भी नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक वह झाड़न को फिर-फिर इस्तेमाल करने के लिए धोती रहेगी, सुखाती रहेगी। कारण, वह उससे निकलने का रास्ता नहीं जानती।
यह रास्ता कवियित्री की पहली कविता ‘पहेली’ में भी नहीं है। उसमें “आगे तीतर पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर” की तरह कवियित्री सिर्फ पहेली बुझाती रह जाती है कि “आगे आदिवासी, पीछे आदिवासी, नक्सली आदिवासी, माओ आदिवासी, मरता आदिवासी, और मरने से किसको बचाता आदिवासी, बोलो, अब तक कितने बचे आदिवासी?”[24] लेकिन जो बचे आदिवासी, वे किस करवट बैठे? क्या उनका कोई संघर्ष नहीं है? क्या वे बिना संघर्ष और लड़ाई के ही मरते हैं? क्या वे नियति के आगे समर्पित आदिवासी हैं? काश, कवियित्री ने इस ज़मीन पर खड़े होकर आदिवासी-चिंतन किया होता।
संग्रह की दूसरी कविता ‘अल्फ्रेड नोबुल’ है। यह वही अल्फ्रेड नोबुल हैं, जिनके नाम पर स्वीडन में नोबुल पुरस्कार दिया जाता है। इस कविता में अल्फ्रेड को विध्वंस का जनक कहा गया है। यथा–
अल्फ्रेड नोबुल
डायनामाइट बनते-बनाते
संभवत: क्या तुम मौत की तरफ बढ़ रहे थे?
या मौत से तुम संभवत: रत्ती भर बच रहे थे?
क्या देखा था आंखों ने तुम्हारी टाइम मशीन बनकर
कि शांति को कैसे लगाया जाता है पलीता?
अल्फ्रेड नोबुल तुम जनक विध्वंस के
निर्माण के पुरस्कर्ता कैसे बन गए?[25]
निस्संदेह अल्फ्रेड नोबुल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लेकिन उसका उद्देश्य पत्थरों की चट्टानों को तोड़ने के कठिन कार्य को आसान करने के लिए था, ताकि मार्ग और सुरंगें बनाने में सुविधा हो सके। लेकिन जब विश्वयुद्ध में उसके आविष्कार का प्रयोग मानव-विनाश में किया गया, तो उसे अपनी उस गलती का अहसास हुआ, जो उससे पहले उसके ज़हन में नहीं आई थी। उसके प्रायश्चित में उसने अपनी सारी संपदा और संपत्ति बेचकर उस धन का उपयोग उसने छह विभिन्न क्षेत्रों में नोबुल पुरस्कार देने का निश्चय करने में किया। क्या उसके इस त्याग का कोई मूल्य नहीं है? कोई भी कलाकार इस मानवीय चेतना की उपेक्षा कैसे कर सकता है?
हेमलता महिश्वर मिथकों में विश्वास नहीं करतीं, ऐसा उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था।[26] लेकिन उनके इस संग्रह में स्वर्ग के मिथक पर ‘स्वर्ग और स्त्री’ कविता को देखकर मैं हैरान रह गया। जिन मिथकों पर महात्मा जोतीराव फुले और बाबासाहेब आंबेडकर ने गंभीर और सर्वश्रेष्ठ शोधकार्य किया हो, क्योंकि मिथकों में ही मूलनिवासियों का इतिहास निहित है, जैसाकि कहा भी गया है कि मिथक इतिहास का धुंआ है,[27] उनके प्रति किसी लेखक की उदासीनता समझ से परे है। बहरहाल, मिथक पर उनकी यह कविता स्वागत-योग्य और गौरतलब है। इस कविता के केंद्र में स्त्री और स्वर्ग है। ‘स्वर्ग’ अपने आप में एक मिथक है, जिसकी उपस्थिति लगभग सभी धर्मों में है, यहां तक कि बौद्धधर्म में भी। इसका संबंध यथार्थ दुनिया से नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से है, जिसे परलोक कहते हैं। उसी परलोक में स्वर्ग और नर्क हैं। स्वर्ग के अपने ठाठ हैं और नर्क के अपने दुख हैं। हेमलता कहतीं हैं, स्वर्ग का संबंध सद्कर्मों से है। जो सद्कर्म करता है, वह स्वर्ग में जाता है, जहां आनंद ही आनंद है, और अप्सराओं से भरा इंद्र का दरबार है। यथा–
सद्कर्म करता आदमी पा जाता है स्वर्ग
और निर्मल आनंद
फिर आनंद ही ओढ़ता-बिछाता है
न केवल इतना कुछ और भी तो है ना
कामधेनु, कल्पवृक्ष
दरबार इंद्र का
कि अप्सराएं भी तो।[28]
ये अप्सराएं सद्कर्मी आदमी की भी सेवा करती हैं। आगे विमर्श इसमें यह है कि कवियित्री पूछती है, क्या सद्कर्मी देवियों की सेवा करने वाले ‘अप्सर’ भी स्वर्ग में हैं? यथा–
इंद्र के दरबार में बहुत सारी हैं
देवियां भी देवताओं की तरह
पर क्या कोई है अप्सर भी
अप्सराओं की तरह
चांपने को चरण देवियों के?[29]
आगे कवियित्री भाग्य में विश्वास करते हुए कहती है– “पुरुष का भाग्य/ सद्कर्म ही करवाता है/ पुरुष से।” फिर पूछती है–
तो क्या त्रिया का चरित्र
कुकर्म के अतिरिक्त
सद्कर्म करवाता होगा क्या स्त्री से?[30]
इसमें कवियित्री ने त्रिया-चरित्र को कुकर्मी मान लिया है, जिसका न कोई वैज्ञानिक आधार है और न समाजशास्त्रीय। बजाए मिथक का तार्किक पाठ करने के, उन्होंने कुपाठ कर दिया। इस कविता का अंत तो और भी अकाव्यात्मक हो गया है। यथा–
कि रखो स्वर्ग अपना अपने पास
तुम्हें मुबारक
डालती हूं मैं उस पर गारत
कि मुझको तो भाता है स्वतंत्र भारत।[31]
अब इसे कैसे समझा जाए कि स्वतंत्र भारत के नाम से वह क्या बिंब निर्मित करना चाहती हैं, और स्वर्ग से उसका क्या संबंध है?
‘परिवर्तन’ कविता में भी कवियित्री ने मिथक का प्रयोग किया है। हालांकि यह कविता प्राचीन हिंदू इतिहास के दो पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है, इसलिए इसे हम मिथक से अलग नहीं कर सकते। इस कविता में इस परिवर्तन की ओर संकेत किया गया है कि हिंदू इतिहास में गार्गी है, जिसे याज्ञवल्क्य ने भरी सभा में सिर काटने की धमकी देकर चुप करा दिया था, जबकि बौद्ध इतिहास में चुप न रहने वाली थेरी स्त्रियों का उदात्त इतिहास है। यथा–
गार्गी चुप हो जाओ वरना
टुकड़े तुम्हारे सिर के
नीचे गिर पड़ेंगे
याज्ञवल्क्य ने भरी सभा में
निडरतापूर्वक कहा था।
लोकतंत्र में अमर्त्य सेन के
आर्गुमेंटेरियन इंडियन[32] धमकाते नहीं
हमारे हर तर्क सुनने के पहले
नकारने को अब
एक जुमला उछाल देते हैं
‘आप नहीं जानती हैं।’
हम औरतें अब तुम्हें दिलाती हैं याद
भूल जाते हो तुम बार-बार
इस देश में है थेरियों का उदात्त इतिहास।[33]
इसमें अमर्त्य सेन के ‘आर्गुमेंटेरियन इंडियन’ का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। इसके बिना भी आधुनिक युग की पुरुषों के बराबरी के स्तर पर सक्रिय स्त्रियों का बिंब उभर रहा था। लेकिन गृह-त्यागकर भिक्षुणी बनी थेरियों के उदात्त इतिहास के बावजूद उनका यह कथन गलत नहीं है–
हम औरतों ने धीरे-धीरे
ह से हवाई जहाज चलाना
मुक्केबाजी करना
और तो और अंतरिक्ष में जाना
सीख लिया है।
अपने विकास में
तुम्हारे सहयोग से नहीं इनकार
पर यह भी तो करो स्वीकार
आधी दुनिया में याज्ञवल्क्य
तुमसे कुछ ज्यादा हैं।[34]
यदि याज्ञवल्क्यों की संख्या ज्यादा हैं, तो सवाल यह जरूर उठेगा कि क्या याज्ञवल्क्य हिंदू समाज में हैं, या भारतीय समाज में? यदि भारतीय समाज में हैं, तो कवियित्री याज्ञवल्क्य का सच हिंदू दृष्टि से स्वीकार कर रही है, और ऐसा करते हुए वह थेरियों का उदाहरण प्रतिपक्ष के रूप में दे रही है। फिर भी इस कविता की विशेषता यह है कि यह याज्ञवल्क्य को वर्तमान में स्त्री-विकास में अवरोधक के रूप में देखती है, और याज्ञवल्क्यों के विरुद्ध स्त्री-संघर्ष के बिंब को उभारती है।
एक कविता ‘बुधिया की दौड़’ है, जिसमें बुधिया दौड़ रहा है, पर वह जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा है, बल्कि एक अदद चिल्ड पानी की बोतल पाने के लिए मैराथन दौड़ रहा है। संवेदना की जिस ज़मीन पर इस कविता को रचा गया है, वह गरीबों का मार्मिक यथार्थ है। यथा—
बाबा को ले जाना था किराए का ठेला
चिल्ड सील्डपैक पानी पहुंचाना था
नहीं दी बोतल बाबा ने
देना पड़ता ना हर्जाना
एक बोतल यानी बीस रुपए
और पंद्रह रुपए यानी एक थाली झुनका भात
बताया था बाबा ने
जो दौड़ेगा, उसे मिलेगा बहुत कुछ
और पानी।
मैराथन नहीं,
बुधिया को दौड़ा रहा था पानी।[35]
इसी के साथ जुड़ी कविता ‘पकना/पकाना’ है, जिसे कविता कहना ही कविता का अपमान करना है। यह पाक-कला का कोई पाठ लगता है कि दाल कैसे पकाई जाती है, कम पकाओ तो कच्ची रह जाती है और अधिक पकाओ तो लप्सी बन जाती है। तेज आंच पर पहली सीटी और दूसरी सीटी मद्धम में नहीं, धीमी आंच पर। पर कविता इसमें कहीं नहीं है। इसी तरह की अकविता ‘विद्रोह’ में है, जिसमें यही स्पष्ट नहीं है कि कौन विद्रोह कर रहा है, और किसलिए? यथा—
मनोरमा, प्रियंका, दामिनी, गुड़िया
तलाश में इनकी दूर से दूर तक
ओढ़े चादर एक दर्द की
सोनी सोढ़ी, शीतल साठे, इरोम शर्मीला
चल पड़े हैं साथ
कि उग आई है भीतर सुनहरी चांदनी
रक्ताभ धूप, अग्नि तेज
और उत्ताल रहा उष्ण तूफ़ान।[36]
इस कविता में कुछ सामाजिक एक्टिविस्ट्स के नाम जरूर आए हैं, पर वे किस विद्रोह को रेखांकित कर रहे हैं, यह कविता कुछ नहीं बताती। इस कविता के दो तरह के पाठक हो सकते हैं, एक वे, जो इन नामों को जानते हैं, और दूसरे वे, जो इन नामों को नहीं जानते हैं। किन्तु दोनों ही पाठकों के लिए यह कविता निरर्थक है। ‘सोना हिरणी’ और ‘स्मृतियां’ भी इसी श्रेणी की अर्थहीन कविताएं हैं, जिनका न सिर नजर आता है और न पैर। बिंब हैं, पर वे किसी अर्थ का आभास नहीं कराते। इसी क्रम में ‘सवाल’ और ‘शीतल साठे के लिए’ दो कविताएं हैं। ‘सवाल’ में यह सवाल है कि ऐसा क्या है शिक्षा में कि ‘पहले सावित्री को विभूषित किया/ मल-विष्ठा से/ और आज सलामी दी मलाला को/ बंदूक की गोलियों से।’[37] लेकिन कवियित्री की यह किस तरह की समझ है कि वह हत्या के प्रयास को ‘सलामी’ की संज्ञा दे रही है? सलामी सम्मान के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। क्या तालिबानी आतंकियों ने मलाला को गोली मारकर सम्मान दिया था? ‘शीतल साठे के लिए’ कविता के केंद्र में भी यही सवाल है कि वह फुले-आंबेडकर के विचार को गाते-गाते शीतल क्यों हो गई? यथा—
शीतल
जिनकी दग्धता से उद्विग्न होकर
किनकी जलन से तप्त होकर
अशीतल हो गई
तुम्हारी शीतलता?[38]
लेकिन यह कविता यह सवाल नहीं उठाती कि किस फासीवादी सत्ता ने शीतल साठे जैसी लोकतांत्रिक प्रतिभाओं की सक्रियता को रोका? सवाल शीतल साठे जैसी कलाकारों के शीतल होने का नहीं है, बल्कि सत्ता के उस दमन का है, जो हिंदू राष्ट्रवाद के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को कुचल रहा है। उसके विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर इस कविता में क्यों नहीं है?
व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश, प्रतिरोध और एक मानववादी सुंदर समाज का स्वप्न यही तो दलित साहित्य के प्रतिमान हैं। अगर किसी दलित कविता में इसी का अभाव होगा, तो हम उसे किस आधार पर दलित चेतना की कविता कहेंगे? उदाहरण के लिए, ‘सावधान’ कविता में कवियित्री ने स्वयं की मुक्ति के कुछ चित्र प्रस्तुत किए हैं। यथा—
तोड़ दी थी उसी दिन अपनी दिमागी गुलामी
दहन की थी जब मनुस्मृति।
जाना था अर्थ बंधुता का जब
दीक्षा लेते हुए भरी सभा में
खचाखच निकाल फेंकी थीं मैंने
अपने हाथों से चूड़ी
और गले से मंगलसूत्र।
मैं तुम्हारी और तुम मेरे लिए
हमराह हो गए।[39]
दिमागी गुलामी केवल मनुस्मृति के दहन और बुद्ध-धम्म में दीक्षा लेने मात्र से दूर होने वाली वस्तु नहीं है। अगर बुद्धि किसी भी धर्म की लग्गू-भग्गू बनी रहती है, तो वह भी एक तरह की दिमागी गुलामी है। लेकिन अजीब विरोधाभास है कि कवियित्री की चिंता यह नहीं है, बल्कि अभारतीयों द्वारा संविधान पर नियंत्रण करना है। यथा—
सावधान
संशोधन की ले आड़
अभारतीय
संविधान पर तान रहे हैं
अपना वितान।[40]
अब यह सवाल उठना यहां लाजमी है कि ये अभारतीय कौन हैं? संविधान में संशोधन करने वाले अगर अभारतीय हैं, तो भारतीय कौन हैं? कवियित्री ने यहां परोक्ष रूप से मूलनिवासी और विदेशी का मुद्दा उठाया है, और यह मुद्दा पूरी तरह से डॉ. आंबेडकर की विचारधारा के विपरीत है, क्योंकि बाबासाहेब ने आर्यों को विदेशी मूल का नहीं माना है।[41] दूसरी बात यह गौरतलब है कि कविता के केंद्र में बाबासाहेब का मंदिर आंदोलन, पानी-सत्याग्रह, मनुस्मृति-दहन और धम्म-दीक्षा है, जिसने व्यक्तिगत रूप से कवियित्री को दिमागी गुलामी से मुक्त किया है। ऐसी स्थिति में अभारतीय और संविधान का मुद्दा कविता से मेल नहीं खाता।
एक कविता है ‘मैं कौन?’ यह कविता बलात्कार की शिकार स्त्री की मनोदशा का चित्रण करती है, जिसमें वह कहती है कि बलात्कार के समय बस उसका शरीर था, न वह स्वयं थी, न उसकी आवाज थी और न उसके आंसू थे। यह स्त्री-चेतना की अजीब अभिव्यक्ति है। इस कविता पर गौर करना जरूरी है। लेकिन पहले इस कविता की एक झलक देखिए—
मैं कब थी वहां
होती तो क्या सुनी न जाती मेरी चीखें?
कब थी वहां
होती तो क्या न दिखते मेरे आंसू?
मैं कब थी वहां
होती तो क्या न सन जाती देह उनकी
मेरे टपकते रक्त-बिंदुओं से
जो छलछला उठे थे सिर्फ योनि से नहीं,
ओठों से, गालों से भी दंतक्षत, नखक्षत
घायल क्षतविक्षत मैं?
मैं न थी, न हूं, बस देह थी
और हैं मेरे आंसू।[42]
हैरान कर देने वाली इस भावाभिव्यक्ति में क्या आक्रोश, प्रतिरोध या मुक्ति का कोई भाव दृष्टिगत होता है? क्या भौतिक रूप से यह संभव है कि कोई स्त्री बलात्कार के समय सिर्फ एक निर्जीव देह में बदल जाती हो, और उसकी स्वाभाविक चेतना लुप्त हो जाती हो? यह कविता न तो नारीवादी दृष्टि से, और न ही दलित-चेतना की दृष्टि से विचार के लिए कोई प्रभाव छोड़ पाती है।
कुछ और कविताएं हैं, जैसे– ‘हुकूमत’, ‘हिम्मत’, ‘डाक टिकट’, ‘बदलाव’, ‘असहजता’, ‘संवाद-सूत्र’, ‘विडंबना’, ‘छलना’, और ‘फंदे’। ये सारी कविताएं किसी गहरी अनुभूति से नहीं उपजी हैं, बल्कि किसी विचार की गहमागहमी ने इनकी ज़मीन तैयार की है। ‘हुकूमत’ का आधार एक अखबारी रिपोर्ट है, जिसमे बताया गया है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक हृदयाघात होता है। इसका संश्लेषण वह पुरुषों के विरोध में इस प्रकार करती हैं–
यदि बात न हो तुम्हारे मन की
तो घर से बाहर का रास्ता बताते हो
मेरी हंसी में बाधा पैदा करते
मेरी खुशियों में सेंध लगाते
दुखी तो होते हो तुम भी
तुम रोना तो नहीं भूले थे
रोने पर पाया था काबू
विकट अट्टहास लगाते
आंसू का देकर दान
मुस्कान तुम थे भूले
मुझको दखल मानते तुम
दुनिया से बेदखल हो गए।[43]
इस कविता का शीर्षक उन्होंने ‘हुकूमत’ इसी आधार पर रखा है कि घर में पुरुष की हुकूमत चलती है, स्त्री की नहीं। अर्थात पुरुष शोषक है और स्त्री शोषित। इसलिए कवियित्री का निष्कर्ष है कि स्त्री-दमन ही पुरुषों में हृदयाघात से अधिक मृत्यु-दर का कारण है।
‘हिम्मत’ कविता उन्होंने अनामिका की कविता ‘बेजगह’ को पढ़कर उसकी प्रतिक्रिया में लिखी है। अनामिका ने लिखा, “लड़कियां हवा, धूप, मिट्टी होती हैं/ उनका कोई घर नहीं होता।” हेमलता लिखती हैं– “क्या हवा, धूप, मिट्टी बांध लोगे? सुनूं तो जरा/ कब तक बांध लोगे?”[44] इस कविता में हेमलता ने अनामिका की बात का समर्थन किया है, और एक गंभीर व्यथा को हवा, धूप, मिट्टी में उड़ा दिया।
‘डाक टिकट’ में लिफाफे और डाक टिकट के माध्यम से एक बिंब रचने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रतीक स्पष्ट नहीं हैं। लिफाफे के साथ डाक टिकट का संवाद कुछ इस तरह है—
मैं तो नन्हीं-सी नाजुक पतली-सी टिकट हूं न!
तुम तो बहुत बड़े, बहुत-बहुत बड़े, मोटे और चिकने
मजबूत कागज के लिफाफे हो।
बच्चे भी तुमसे अलग करते फेंकते तुम्हें
सहेज लेते मुझको।
क्या बस इसलिए डरते हो?
तभी तो विदीर्ण कर देते मुझको।[45]
कोई भी बिंब तभी सार्थक होता है, जब वह कोई विचार भी स्पष्ट करता हो। इस कविता में टिकट किस विचार का प्रतीक है? विवाह का, स्त्री का, या किसी और चीज का? और आज के दौर में जब कूरियर-सेवा ने लिफाफे पर डाक टिकट की अनिवार्यता ही खत्म कर दी है, तो आने वाले समय में आने वाले लोग इस कविता का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे?
साहित्य में अनुभूतियों का विशेष योगदान होता है। अगर अनुभूति न हो, तो न कविता लिखी जा सकती है और न कहानी। दलितों पर लिखे गए सवर्ण-लेखन का मूल्यांकन हम अनुभूति के आधार पर ही करते हैं। अनुभूति के अभाव में ही सवर्ण-साहित्य में चित्रित दलित-जीवन यथार्थ से दूर दिखाई देता है। संयोग से हेमलता की ‘बदलाव’ कविता इसी श्रेणी में आती है। इसमें मैला कमाने वाली एक मेहतरानी की कथा है। कविता का आरंभ इस तरह होता है—
क्या खाते हो/ क्या पीते हो
जो ऐसा बदबूदार हगते हो।
आती हूं रोज तुम्हारा पाखाना साफ़ करती हूं
इस सड़ांध को धो जाती हूँ।[46]
यह अभिव्यक्ति पर-काया-प्रवेश की है। यह लेखिका की स्वयं की अनुभूति नहीं है। इसलिए इसे हम प्रामाणिक अनुभूति नहीं कह सकते। आगे कवियित्री ने मेहतरानी के मुंह से जो कहलवाया है, वह और भी निराशाजनक है। यथा—
मैं चाहती हूं तुम्हारे सामने खड़े होकर
तुम्हारे मन का संडास साफ करना
जो मनुस्मृति खाकर दिमाग में पचाकर
तुम मुंह से हगते हो
अपने घर को ही नहीं,
सारी दुनिया को संडास बनाए फिरते हो।[47]
अगर अनुभूति नहीं होती है, तो सहानुभूति से काम लिया जाता है, जैसे प्रेमचंद ने दलितों के प्रति सहानुभूति से लिखा। लेकिन ऊपर की अभिव्यक्ति सहानुभूति से भी रहित नजर आती है। सवाल यह है कि मेहतरानी कह किससे रही है, जबकि कवियित्री स्वयं भी दलित जाति से है। तब क्या मनुस्मृति खाकर दलित भी मुंह से हग रहा है, और सारी दुनिया को संडास बना रहा है? आगे यह मेहतरानी मन का संडास साफ़ करना चाहती है, वह भी झाडू और खोंपचे से। यथा—
अब मैं केवल तुम्हारे घर के द्वार में ही नहीं
तुम्हारे आंगन में ही नहीं
पिछवाड़े में भी
साफ-सुथरा भविष्य सजाना चाहती हूं
करारी-सी झाड़ू लेकर, खोंपचे से तुम्हारा
बजबजाता दिमाग निकालकर
दूसरा दिमाग रख देना चाहती हूं।[48]
गजब की कल्पना है, साफ-सुथरे भविष्य में भी झाडू-पंजा हाथ से नहीं छूटता।
इसी तरह ‘गलतफहमी’ कविता है। इस पर बात करने से पहले इसे देख लिया जाए। कविता की शुरुआत इस तरह होती है—
मत पालो गलतफहमी अपने भीतर
कि यह सूखी ठठरी लकड़ी या लड़की
जलाने पर बर्र से जल जाएगी
त्वचा उसकी गीली-गीली है
जलती है तो बिना लपट के भी
गर्म फुफकारें छोड़ती है।
सुनो तो जलाने के जतन में
तुम्हें भी तो बारंबार लगातार
साथ होना होता है उसके
सिली-सिली लकड़ी-सी लड़की
लड़की-सी लकड़ी जलती तो खुद है
पर उसकी जलन तुम्हारी ही नहीं
बाकी सबकी आंखों में भी
पानी भरती है।[49]
इसमें जिस गलतफहमी का जिक्र है, क्या वह यह है कि लड़की सूखी लकड़ी की तरह बर्र से जल जाती है, या यह है कि जलने से पहले वह गर्म फुफकारें छोड़ती है, या यह है कि लड़की-सी लकड़ी खुद ही जलती है? मेरी नजर में अगर कोई गलतफहमी है तो वह कवियित्री की खुद की गलतफहमी है, जो हाड़-मांस की जिंदा लड़की की तुलना एक निर्जीव वस्तु लकड़ी से कर रही है। लकड़ी को तो जलने पर जलन नहीं होती, वह फुफकारें नहीं छोड़ती और न चीखती-चिल्लाती है, पर लड़की जब जलती है, या जलाई जाती है, तो उसका संपूर्ण अस्तित्व जलता है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह किस संवेदना की कविता है? इसका अर्थ क्या है? इसकी रचना-प्रक्रिया क्या है? इसमें संदेह नहीं कि लड़की को लकड़ी की तरह जलाना यातना का प्रश्न है, पर यह कविता में कहां खुल रहा है?
‘असहजता’ कविता में कवियित्री ने यह रेखांकित किया है कि जिस तरह बुद्ध ने अपनी शिक्षा से दुःख का निराकरण किया, उसी प्रकार पुरुष ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्त्री को शिक्षित नहीं किया? यथा—
समाज के पुरुष हो न,
लेकर शिक्षा
तुमने एक अक्षर मुझे न बख्शा
तुम शिक्षित और मैं उपेक्षित
तुम्हारी नौकरी, मेरी बेकदरी
घर-बाहर तुम्हारा मान
भीतर मेरा अपमान।
क्या जानते हो तुम्हारे ज्ञान-संसार में
मेरी असफलता में तुम्हारा ही तो हाथ है।[50]
जाहिर है कि इस कविता में कवियित्री का इशारा दलित पुरुषों की ओर है, क्योंकि सवर्ण समुदाय में, किसी समय स्त्री-शिक्षा प्रतिबंधित होने के बावजूद, आज शिक्षा में स्त्री-पुरुष में भेदभाव नहीं है। किन्तु दलित वर्ग सदियों से शिक्षा से वंचित वर्ग रहा है। उसे शिक्षा की सुविधा सिर्फ लोकतंत्र में मिली, पर अभी भी उसे सवर्ण वर्गों के समान स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में दलित पुरुषों पर अपनी स्त्रियों को अशिक्षित रखने का आरोप लगाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता।
‘संवाद-सूत्र’ कविता में कवियित्री कहती है—
नालंदा, सोमनाथ या कि बाबरी मस्जिद
या फिर बुत बामियान के,
इनके विध्वंसकों में संवादहीनता होती जो
न मिलती विरासत में टूटी बिखरी सभ्यता।
न होता ध्वंस इमारतों का
संवेदनाओं का
और न ही बंधती गिरहें दिलों में।[51]
इस कविता में ‘संवादहीनता’ का क्या मतलब है? और वह किस तरह टूटी-बिखरी सभ्यता की विरासत के लिए जिम्मेदार है? विध्वंसकों के बीच परस्पर संवाद हो भी कैसे सकता था, जबकि उनके कालखंड अलग-अलग हैं? नालंदा के विध्वंस में ब्राह्मणों का हाथ है, सोमनाथ के विध्वंस में मुस्लिम हमलावर का, बाबरी मस्जिद के विध्वंस में भाजपा और आरएसएस के आक्रामक हिंदुत्व का, तो बामियान की बुद्ध प्रतिमा के विध्वंस में अफगान के तालिबानी उन्माद का हाथ है। धार्मिक उन्माद अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु ही नहीं होता, बल्कि वह उनकी कला-संस्कृति का भी विरोधी होता है। लेकिन कवियित्री अजीब बात कह रही है कि इन विध्वंसकों के बीच संवादहीनता होती, तो कला-संस्कृति की क्षति नहीं होती। इसका मतलब है कि वह यह मानती हैं कि विध्वंसकों के बीच संवाद था। लेकिन इस संवाद का कोई तथ्यात्मक आधार है?
ओमप्रकाश वाल्मीकि की एक चर्चित कविता का सारांश है कि तालाब, खेत, बैल, हल ठाकुर के, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, फिर अपना क्या?[52] इस तर्ज पर दर्जनों दलित कवियों ने लिखा और इस भाव का विस्तार किया। हेमलता महिश्वर की कविता ‘छलना’ भी इसी ज़मीन की रचना है। यथा—
मजदूर मैं/ भूखा-प्यासा मैं
ठंड में ठिठुरता, वर्षा में भीगता
चिलचिलाती धूप में
अपने पसीने से धरती सींचता
मेहनत मेरी, ताकत मेरी, अधीन तुम्हारी।
मेरे निर्माण पर, मेरे कौशल पर राज तुम्हारा।
उत्पादन मेरा, फिर भी दीन मैं, हीन मैं।[53]
लेकिन हेमलता ने वाल्मीकि की कविता का विस्तार अपनी कविता में इस अंत के साथ किया है—
अब तो मैं हूं जागा बन्धु
सबको मैं जगाऊंगा
मैं मरूंगा न सोचो तुम
अनेकानेक शंबूक ही शंबूक
पैदा करता जाऊंगा।[54]
जिस ज़मीन पर यह कविता लिखी गई, वह ज़मीन ही अंत में खत्म हो गई। शंबूक होने का मतलब कोई क्रांति नहीं है, मारा जाना है। इसलिए भाव की ज़मीन पर यह कविता कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है।
संग्रह की अंतिम कविता ‘फंदे’ है। इसमें कवियित्री ने सलाई पर स्वेटर बुनने वाले फंदों के रूपक का प्रयोग करते हुए पुरुष द्वारा स्त्री के विरुद्ध बुने गए फंदों की ऐंठन का बिंब रचा है। यथा—
दो फंदे नीचे, दो फंदे ऊपर
एक उल्टा तो चार सीधे
एक उतारो तीन बुन लो।
जाने कितने स्वेटर बनाए और उधेड़े
उधेड़ा तो सुलझाया भी।
पर ऐंठन तुम्हारे बुने फंदों की
न सुलझा पाई मैं।
जाने कितने ही वाष्पकण
सीने से उठकर
आंखों में धुआं भरते रहे।[55]
इस कविता में पुरुष के फंदों में फंसी स्त्री की वेदना का चित्रण हुआ है। यह कोई भी सामान्य स्त्री हो सकती है, जो सलाई पर ऊन के फंदों को सुलझा लेती है, लेकिन पुरुष के छल-प्रपंच के फंदों में उलझी रहती है। क्या यह स्त्री-चेतना की कविता है? अगर हां, तो इसमें वह स्त्री-चेतना कहां है?
समग्र रूप से मैं हेमलता महिश्वर की कविताओं को पढ़ते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनका स्वयं का जीवन संघर्षों से रहित है, जिसके कारण उन्हें दलितों के दुःख और दलित-चेतना का ज्ञान नहीं हो सका है। उनमें बौद्धधर्म की भावुकता है, लेकिन डॉ. आंबेडकर की वैचारिकी वह नहीं पकड़ सकी हैं।
संदर्भ :
[1] हेमलता महिश्वर, नील, नीले रंग के (कविता-संग्रह), 2015, शिल्पायन, शाहदरा, दिल्ली, पृ. 40-41
[2] डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वाल्यूम 5, देखिए, पहली किताब : अनटचेबल्स आर दि चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया’स घेट्टो।
[3] यहूदियों के लिए बनाए गए यातना शिविर।
[4] वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश के मुरैना में एक घटना घटित हुई थी। सवर्ण परिवार का कुत्ता एक दलित परिवार के घर में चला गया था। घर की मालकिन ने उसे खाने को रोटी दे दी। इस बात को लेकर सवर्ण परिवार ने दलित परिवार के साथ मारपीट की थी तथा पंचायत के द्वारा आर्थिक दंड लगाया गया था।
[5] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 42-43
[6] वही, पृ. 43-44
[7] वही, पृ. 45-46
[8] वही, पृ. 47
[9] वही, पृ. 48
[10] वही, पृ. 26
[11] शांति भिक्षु शास्त्री, ऊहापोह, 1955, बुद्ध विहार, रिसालदार पार्क, लखनऊ, पृ. 14-16
[12] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 27
[13] वही, पृ. 28
[14] वही, पृ. 29
[15] रामनाथ ‘सुमन’, मीर : जीवन, समीक्षा, व्याख्या और काव्य, प्रथम संस्करण 1959, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृ. 134-135
[16] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 30
[17] डा. युगेश्वर, कबीर समग्र, भाग एक, 1995, पृ. 499
[18] वही, पृ. 499-500
[19] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 34
[20] फेसबुक, फिरोज सैफी की वाल से, 4 अप्रैल 2023
[21] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 35
[22] वही, पृ. 37
[23] वही, पृ. 38
[24] वही, पृ. 19-23
[25] वही, पृ.24-25
[26] 2012 में मैंने उदभ्रांत शर्मा के महाकाव्य ‘त्रेता’ की एक आलोचनात्मक समीक्षा ‘त्रेता-विमर्श और दलित-चिंतन’ नाम से की थी, जिसे मैंने हेमलता महिश्वर को समर्पित किया था। दिल्ली में उसका विमोचन हुआ, जिसमें हेमलता जी को भी आमंत्रित किया गया था। मैं उस कार्यक्रम में नहीं जा सका था, पर हेमलता जी उपस्थित हुई थीं। कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करते हुए मुझे उदभ्रांत जी ने बताया कि हेमलता जी ने उस किताब पर यह कहकर बोलने से इनकार कर दिया कि वह मिथकों में विश्वास नहीं करतीं।
[27] वेंडी डोनिगर, दि हिंदूज : एन आल्टरनेटिव हिस्ट्री, 2009, पेंगुईन, पृ. 24
[28] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 31
[29] वही, पृ. 32
[30] वही, पृ. 32-33
[31] वही, पृ. 33
[32] अमर्त्य सेन की चर्चित पुस्तक ‘दि आर्गुमेंटेटिव इंडियन’ से निर्मित शब्द।
[33] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 69-71
[34] वही, पृ. 70
[35] वही, पृ. 50
[36] वही, पृ. 56
[37] वही, पृ. 60
[38] वही, पृ. 62
[39] वही, पृ. 64
[40] वही, पृ. 65-66
[41] देखिए, डा. आंबेडकर की चर्चित पुस्तक ‘शूद्र कौन?’
[42] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 72-73
[43] वही, पृ. 75-76
[44] वही, पृ. 77
[45] वही, पृ. 78
[46] वही, पृ. 80
[47] वही, पृ. 81
[48] वही।
[49] वही, पृ. 82-83
[50] वही, पृ. 84-85
[51] वही, पृ. 86
[52] यह कविता ‘ठाकुर का कुआं’ नाम से ओमप्रकाश वाल्मीकि के पहले कविता-संग्रह ‘सदियों का संताप’ (1989) में संकलित है। देखिए पृ. 3
[53] हेमलता महिश्वर, वही, पृ. 91-93
[54] वही, पृ. 93
[55] वही, पृ. 94-95