दिलचस्प है जहां कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन था, वहां मार्क्स के चिंतन में सर्जनात्मक योगदान न के बराबर हुआ. अगर हुआ भी तो उनके द्वारा जो शासक कम्युनिस्ट पार्टियों से प्रताड़ित किए गए थे. ऐसे निजामों ने अपने हर निर्णय के औचित्य साधन के लिए मार्क्स की सेवा ली, लेकिन हर उस व्यक्ति को संशोधनवादी भी ठहराया जो अपने ढंग से मार्क्स को पढ़ रहा था या उसकी व्याख्या कर रहा था.विडंबना यह है कि मार्क्सीय चिंतन में अधिक साहसी प्रयोग गैर साम्यवादी यूरोप में किए गए और प्रायः ऐसा जिन्होंने किया, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टियों ने निकाल बाहर किया. स्वतंत्र मार्क्सीय चिंतन और सत्ता के बीच यह उल्टा रिश्ता मार्क्स पर नहीं, इन पार्टियों पर प्रतिकूल टिप्पणी है.

अपूर्वानंद
मार्क्स पर उनके दो सदी बाद भी बहस-मुबाहसा होता रहता है. एक समय था जब मार्क्स, बौद्धिकता और जवानी का रिश्ता सहज माना जाता था. मार्क्सवादी होने का एक और अर्थ था परिवर्तनकामी होना, बल्कि परिवर्तनकारी होना. अब परिवर्तन का जिम्मा सरकार ने ही ले लिया है. भारत की सरकार ने अपनी एक संस्था का नाम ही दे दिया है: नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ इंडिया.
नौजवान मार्क्स के करीब आते थे बदलाव की प्रेरणा के साथ. यह कहना अधिक उचित है कि बदलाव की तड़प ही उन्हें मार्क्स के करीब ले जाती थी, यह नहीं कि मार्क्स से होकर वे बदलाव की राह पर आते थे. लेकिन यह बदलाव कोई रोज़ घटित होने वाली चीज़ नहीं थी. हर तीसरे रोज़ जो परिवर्तन रथ निकला करते हैं, उनपर सवार होकर उसे न आना था.
मार्क्सीय होने का मतलब भौतिकतावादी होना है. लेकिन मार्क्स का परिवर्तन व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों ही रूपों में मात्र जीवन की भौतिक परिस्थितियों में नहीं, बल्कि जीवन के प्रति नज़रिए में तब्दीली की महत्वाकांक्षा से प्रेरित है. इस रूप में यह आध्यात्मिक मिशन मालूम पड़ता है.
बदलाव या परिवर्तन मार्क्सीय चिंतन का उद्देश्य है या उसकी धुरी है. ‘दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की व्याख्या की है जब कि सवाल उसे बदलने का है’ यह मार्क्सीय उक्ति मार्क्स को दूसरे विचारकों से बिलकुल अलग ही स्तर पर स्थापित कर देती है.
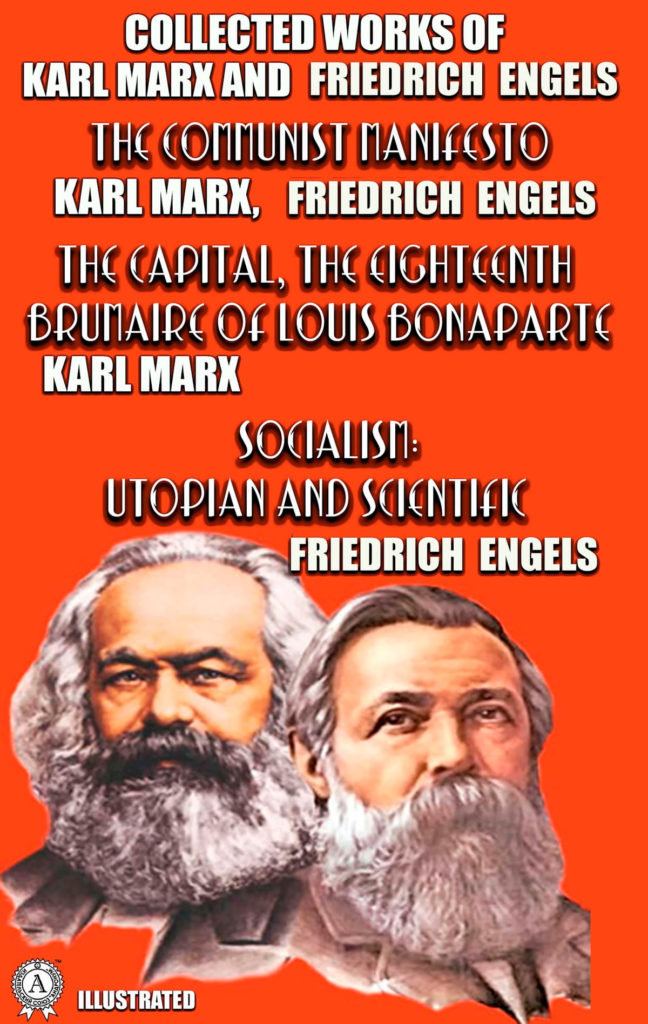
टेरी इगलटन की एक बात इस संदर्भ में बड़ी दिलचस्प है. उन्होंने मार्क्सवादी होने की मुश्किल की ओर इशारा किया है. वे कहते हैं कि मार्क्सवादी होने का अर्थ ही है कुछ करना. यह कुछ-कुछ बढ़ई होने की तरह है. बढ़ई होने का मतलब है कुछ बनाना, सिर्फ किसी शिल्प की कल्पना करना नहीं. इसलिए दार्शनिक और विचारक अवश्य ही और भी बड़े हुए हैं और उनकी मेधा किसी से कम नहीं, लेकिन ‘विचार करने का अर्थ ही यथास्थिति को बदल देना है’, यह जितना मार्क्स के साथ जुड़ा है, उतना शायद किसी और के साथ नहीं. ‘मैं सोचता हूं, इसलिए हूं’ की जगह ‘मैं करता हूं, इसीलिए हूं’, मार्क्स के कहे बिना ही उनके चिंतन का सार है.
जब क्रिया की बात हो रही हो तो हम भारतीय भी एक दावा गांधी की शक्ल में पेश कर सकते हैं. जैसे मार्क्सवादी होने का मतलब ही है क्रियाशील होना, वैसे ही आप सिर्फ चिंतक होकर गांधीवादी नहीं हो सकते. गांधी एक जगह मार्क्स से एक कदम आगे जान पड़ते हैं: उन्होंने अपने राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम से पहले उसे जायज ठहराने के लिए किसी मुकम्मल दार्शनिक ढांचे को खड़ा करने की जरूरत नहीं समझी. गांधी के दर्शन की बात दूसरों ने की, गांधी ने अपने कर्म के जरिए ही उसे विकसित किया.
प्रायः मार्क्सवादी गांधी को मार्क्स से इसीलिए कमतर आंकते रहे हैं क्योंकि वे उनके उपक्रम को बौद्धिक कम, भावनात्मक अधिक मानते हैं. ऐसा लगता है कि गांधी कुछ-कुछ अन्तःप्रेरणा से काम कर रहे थे और इसीलिए कई लोगों को उनके आंदोलन में तार्किकता खोजने में कठिनाई मालूम पड़ती है. जान पड़ता है, मानो गांधी को खुदाई इलहाम होता था जो उन्हें उनके अगले कदम की ओर ले जाता था. नेहरू जैसे वैज्ञानिक चेतना संपन्न बौद्धिक को भी वे एक जादूगर की तरह दिखलाई देते थे. उनके फैसलों से सहमत न होते हुए भी उनके साथ चलना जैसे किसी दैवी आदेश से हो रहा हो.
गांधी और मार्क्स में तुलना करके एक को दूसरे से श्रेष्ठ ठहराने का यहां इरादा नहीं और उससे अधिक गैर-मार्क्सवादी कार्य कुछ हो नहीं सकता. लेकिन एक अंतर ज़रूर है: मार्क्स अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए कोई क्रियाशील अभियान जीवन पर्यंत चलाने वाले न थे, गांधी ने खुद एक बड़ा संगठन खड़ा किया और कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया.
एक दूसरे अर्थ में मार्क्स और गांधी एक जैसे जान पड़ते हैं. दोनों ने असंभव आदर्श की कल्पना की. गांधी का अहिंसक समाज और मार्क्स का वर्ग-विहीन समाज दोनों ही नामुमकिन ख्याल हैं. लेकिन वे इतने ज़रूरी जान पड़ते हैं कि उनकी तामीर में ज़रा भी देर नहीं की जा सकती या नहीं की जानी चाहिए. दूसरा, एक के बिना दूसरा समाज बन नहीं सकता.
मार्क्स की ताकत इससे जाहिर होती है कि ज़िंदगी पुस्तकालयों में बिता देने वाले व्यक्ति ने दुनिया भर में शायद सबसे बड़ी तादाद में लोगों को घरों से निकलकर अपनी दुनिया को बदल डालने के अभियान में डाल दिया. इससे भी बावजूद एक पूरी शताब्दी की असफलता के, वह अभी भी संभावनापूर्ण लगता है.
मार्क्स की सफलता देखी गई थी समाजवादी क्रांतियों में: सोवियत संघ, साम्यवादी चीन, पूर्वी यूरोप में समाजवादी सरकारों के गठन में. लेकिन सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टियों ने मार्क्सीय स्वप्न को एक गैर मामूली यातना में बदल दिया, सत्ता के यथार्थ ने उसके रूमान को झुलसा दिया.
यह भी दिलचस्प है जहां कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन था, वहां मार्क्स के चिंतन में सर्जनात्मक योगदान न के बराबर हुआ. अगर हुआ भी तो उनके द्वारा जो शासक कम्युनिस्ट पार्टियों से प्रताड़ित किए गए थे. ऐसे निजामों ने अपने हर निर्णय के औचित्य साधन के लिए मार्क्स की सेवा ली, लेकिन हर उस व्यक्ति को संशोधनवादी भी ठहराया जो अपने ढंग से मार्क्स को पढ़ रहा था या उसकी व्याख्या कर रहा था.
विडंबना यह है कि मार्क्सीय चिंतन में अधिक साहसी प्रयोग गैर साम्यवादी यूरोप में किए गए और प्रायः ऐसा जिन्होंने किया, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टियों ने निकाल बाहर किया. स्वतंत्र मार्क्सीय चिंतन और सत्ता के बीच यह उल्टा रिश्ता मार्क्स पर नहीं, इन पार्टियों पर प्रतिकूल टिप्पणी है.
उदारवादी अर्थव्यवस्था की उछाह का झाग जब अमरीकी बैंकों के ढह जाने से बैठ गया, मार्क्स की तरफ पूंजीवादी दुनिया का ध्यान गया. मार्क्सीय साहित्य की बिक्री कई गुना बढ़ गई. अकादमिक विश्व में भी मार्क्सीय सिद्धांत व्यवस्था के प्रति दिलचस्पी बढ़ती हुई देखी गई. एक वक्त जिस देश ने कम्युनिस्ट को अमरीकीद्रोही का पर्यायवाची बना दिया था उसके विश्वविद्यालयों में मार्क्स बौद्धिक उत्तेजना के चिरंतन स्रोत बन गये हैं.
लेकिन क्या यही मार्क्स की सफलता है?
























